Question : "औरंगजेब अत्यधिक बदनाम बादशाह है।" इस प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
(1994)
Answer : मुगल बादशाहों में शायद सबसे ज्यादा बदनाम बादशाह औरंगजेब ही है। यदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों ने औरंगजेब के शासन काल की समीक्षा करते हुए जाटों, सतनामियों, सिखों, मराठों एवं राजपूतों में औरंगजेब के शासन के विरुद्ध विद्रोह करने को औरंगजेब की मुस्लिम कट्टरवादी विचारों के साथ जोड़ते हुए औरंगजेब को एक धर्मांध राजा कहा है। लेकिन इस विचार को सतीश चन्द्र, अतहर अली आदि इतिहासकारों ने मानने से इंकार करते हुए औरंगजेब की नीतियों के पीछे उसे अपने समय की परिस्थितियों को कारण माना है।
औरंगजेब की नीति या चरित्र पर किसी भी तरह का विचार आरोपित करने से पहले हमें दोनों तरह के विचारों के तर्कों को जानना उचित होगा। जब से दिल्ली में औरंगजेब के नाम का ‘खुत्बा’ पढ़ा गया, तभी से उसका धार्मिक झुकाव प्रकट होने लगा था। उसके पूर्वजों से कहीं अधिक उसे अपनी गद्दीनशीनी की न्याय संगतता सिद्ध करनी पड़ी, क्योंकि तब उसका पिता जीवित था। तब ऐसा करना शायद इसलिए भी आवश्यक था कि दारा शिकोह गद्दी के दावेदार के रूप में जीवित था। इसलिए धार्मिक-राजनीतिक अनन्यता के पुनरानुकूलन के माध्यम से इस्लामी अस्मिता को संरक्षित रखने के लिए उद्धत कट्टरपंथी वर्ग को शांत करने हेतु औरंगजेब को कुछ उपाय करने पड़े। इनमें से कुछ हैं- सिक्कों पर ‘कलिमा’ के प्रयोग की पाबंदी, सौर इलाही कैलेंडर के उपयोग पर रोक, राजपूत राजाओं की ‘टीका’ और तुलादान समारोहों की समाप्ति, यद्यपि बहुत से राजाओं के जन्मोत्सवों पर इन्हें मनाने की छूट थी। झरोखा-दर्शन पर पाबंदी, भांग-चरस और अन्य नशीले पेय-पदार्थों की बिक्री पर रोक, वेश्यागामिता और व्यभिचार पर पाबंदी, सती होना न चाहने वाली हिंदू विधवाओं को जलाए जाने की मनाही, कम उम्र के बच्चों के बंध्याकरण पर प्रतिबंध, सार्वजनिक संगीत समारोहों एवं ‘नवरोज’ मनाने पर पाबंदी आदि लगाई गयी थी। ये सब बातें उलेमा के सामाजिक दबाव और इस्लामी रीति-रिवाजों में सुधार लाने की वजह से लागू की गयी, न कि किसी प्रकार के उत्पीड़न के विचार से।
जाटों, सतनामियों, सिखों और मराठों के विद्रोहों का कारण इरफान हबीब और अन्य इतिहासकारों ने औरंगजेब की उत्पीड़नकारी नीतियों को नहीं, तत्कालीन कृषि संबंध संकटों को माना है, क्योंकि तब दोहरा भू-राजस्व जमा होता था, करों की दरें बड़ी-चढ़ी थीं और स्थानीय शासकों-अधिपतियों द्वारा जनता पर जुल्म ढाया जाता था। उनके अनुसार हो सकता है कि विद्रोह के सरगनों ने किसानों को इकट्ठा करने और उनकी मदद पाने के लिये ये नारे देकर उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया हो। काशी (वाराणसी) के विश्वनाथ और गोपीनाथ मंदिरों को अथवा मथुरा के वीरसिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशवराय के मंदिर को नष्ट करने का कारण यह हो सकता है कि उस समय मंदिर विद्रोहियों के अड्डे के रूप में कार्य करते थे।
औरंगजेब पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि उसने शाही नौकरयां देने में भेदभाव बरता था और अनेक प्रकार के कर या चुंगियां लगाई थीं। सन् 1665 में वस्तुओं का बिक्री कर मुसलमानां परकी दर से और हिंदुओं पर 5% की दर से तय किया गया। सन् 1667 में मुसलमानों पर से यह कर पूरी तरह से हटा लिया गया। 1671 में एक आदेश में हिंदुओं की वित्त विभाग में नौकरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन् 1675 तक आते-आते राजपूत मनसबदारों की संख्या में भारी कमी आ गयी। किन्तु अतहर अली ने यह सिद्ध किया है कि अकबर के जमाने में हिन्दू मनसबदारों की संख्या 22.5% थी, जबकि औरंगजेब के जमाने में यह संख्या बढ़कर 33.1% हो गयी। हो सकता है कि मराठों को खुश करने के लिए औरंगजेब को उन्हें मनसबदारियां देनी पड़ी हों, पर चूंकि जागीरदारी संकट की वजह से ऐसा करना संभव नहीं होता, इसलिए
युद्धप्रिय मराठों के वास्ते स्थान खाली करने के लिए राजपूतों की मनसबदारियां छीननी पड़ी हों। इस प्रकार, इस मत के अनुसार, राजपूतों का उत्पीड़न हुआ माना जाता है। उल्टे, ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जब तत्कालीन राजनीति को ध्यान में रखते हुए औरंगजेब ने अनेक राजपूतों को क्षमा कर दिया था, जैसे राजसिंह और जसवंत सिंह (जो उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से लड़े थे) को। अतहर अली यदुनाथ सरकार के आरोप कि औरंगजेब जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खत्म करना चाहता या आश्रित राज्य बनाना चाहता था, का भी खंडन करते हैं।
अतहर अली ने इस काल के सांख्यिकिय की अध्ययन के पश्चात् यदुनाथ सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘औरंगजेब की राजपूत विरोधी’ दृष्टिकोण का खंडन किया है। उसके अनुसार, औरंगजेब ने राजपूत विरोधी नीति कभी भी नहीं अपनाई। उसके शासन के प्रथम बीस वर्षों (1659-1679) में राजपूतों के प्रति शत्रुता के चिह्न कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते।
इसके विपरीत राजपूतों को औरंगजेब के शासन के प्रथम दो वर्षों में विशिष्ट रूप से सम्मान आदि प्राप्त हुए तथा वे शाही अनुकम्पा के पात्र बने। अतहर अली के अनुसार, इस काल में पदों में बढ़ोत्तरी होने के कारण उनकी संख्या का औसत 19% हो गया। शाहजहां के पूरे शासन काल में किसी भी राजपूत सरदार को 7000/7000 का मनसब प्राप्त नहीं था, किन्तु औरंगजेब के काल में जयसिंह और जसवन्त सिंह में से प्रत्येक को यह मनसब प्राप्त हुआ। औरंगजेब के काल के प्रथम बीस वर्षों में 1000 व उससे अधिक के राजपूत मनसबदारों की संख्या 14% थी जबकि शाहजहां के काल में इस स्तर के मनसबदारों की संख्या कुल 16% ही थीं।
सतीश चन्द्र के अनुसार, अपने शासन के बीस वर्षों के बाद जजिया कर लगाने के पीछे उसकी उत्पीड़नकारी नीति नहीं, बल्कि विस्तारवादी गतिविधियों के कारण रिक्त हुए खजाने को पूरा करने की आवश्यकता थी। सतीश चन्द्र उचित ही कहते हैं कि औरंगजेब को उसके उत्पीड़नकारी, कट्टरवादी नीतियों के लिए बदनाम करने की अपेक्षा उसके काल की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को गंभीरता से समझना चाहिए। औरंगजेब जो भी कर रहा था उसके पीछे उसका उद्देश्य मात्र इतना था कि सुदूर दक्षिण तक फैले मुगल साम्राज्य को किसी तरह एक रखा जा सके और अनगिनत विरोधियों के विरुद्ध उसके कुछ साथी और सहयोगी बन सकें। वह औरंगजेब ही था, जिसने किसानों की भलाई न कर सकने का दुःख व्यक्त किया था, जो राज्य के खजाने को सिर्फ जरूरत के अनुसार ही खर्च करता था और जिसका जीवन एक ‘जिन्दा पीर’ की तरह का था।
Question : सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान व्यापार के ढांचे का विवेचन कीजिये। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में तत्कालीन बस्तियों के स्वरूप को कहां तक प्रभावित किया?
(1994)
Answer : सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान व्यापार का ढांचा बहुत विकसित अवस्था में थे। सभ्यता की छोटी से छोटी बस्तियों में भी बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं के औजार पाये गये हैं, जो अमीर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विस्तृत विनिमय या व्यापार तंत्र की ओर संकेत करते हैं। सिन्धु सभ्यता के लोग राजस्थान की खेतड़ी खानों से तांबा, बलूचिस्तान और उत्तरी-पश्चिमी सीमांत से तांबा, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र और कश्मीर से सोना, अफगानिस्तान और ईरान से चांदी, कश्मीर या राजस्थान से सीसा, पूर्वी अफगानिस्तान में बदक्शां से वैदूर्यमणि, मध्य एशिया से फिरोजा और जेड, सौराष्ट्र या पश्चिमी भारत से गोमेद, श्वेतवर्ण स्फटिक और लाजवर्द पत्थर, गुजरात के समुद्री तट से समुद्री सीपियां, जम्मू में मांदा से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे।
सिन्धु सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर यह सब चीजें बंजारे व्यापारियों द्वारा और चरवाहों द्वारा पहुंचती थीं। इस बात की भी सम्भावना है कि शायद सिन्धु सभ्यता के प्रशासकों ने बहुत से क्षेत्रों में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत उपनिवेश भी स्थापित किया हो। विनिमय व्यवस्था का ठीक से ज्ञान नहीं होने के कारण व्यापारी वर्गों द्वारा मौसमी प्रवास आदि के बारे में भी सोचा जा सकता है।
हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने आपसी व्यापार और विनिमय को नियंत्रित करने के प्रयास किये। दूर-दूर फैली हुई हड़प्पाकालीन बस्तियों में भी नाप और तौल की व्यवस्थाओं में समरूपता है। तौल निम्न मूल्यांकों में द्विचर प्रणाली के अनुसार हैः 1, 2, 4, 8 से 64 तक फिर 150 तक और फिर 16 से गुणा होने वाले दशमलव 320, 640, 1600 और 3200 आदि तक। ये चकमकी पत्थर, चूना पत्थर, सेलखड़ी आदि से बनते हैं और साधारणतया घनाकार होते हैं। लम्बाई 37-6 सेंटीमीटर की एक फीट की इकाई पर आधारित थी और एक हाथ की इकाई लगभग 51-8 से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। नाप और तौल की समरूप व्यवस्था केन्द्रीय प्रशासन द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोगों में आपसी तथा अन्य लोगों के साथ विनिमय को व्यवस्थित करने के प्रयास की ओर इशारा करती है।
हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में काफी संख्या में मुहरें और मुद्रांकण पायी गयी हैं। ये मुहरें और मुद्रांकण दूरस्थ स्थानों को भेजे जाने वाले उत्पादों के उच्च स्तर और स्वामित्व की ओर संकेत करते हैं। इनका प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों में होता था। ऐसा लगता है दूरस्थ स्थान के साथ व्यापार विनिमय में इनका प्रयोग होता था।
पश्चिम एशिया के मेसोपोटामिया के साथ सिन्धु सभ्यता का विकसित व्यापार सम्बन्ध था। इसका प्रमाण मेसोपोटामिया के सूसा, उर, निप्पुर, किश एवं फारस की खाड़ी में फैलका, बहरीन एवं तेल असमार से सिन्धु सभ्यता के मुहरों से मिलती-जुलती लगभग दो दर्जन मुहरें, विशेषकर चौकोर सिंधु मुहरें मिली हैं। लोथल से मेसोपोटामिया की बेलनाकार छोटी मुहरें पाई गयी हैं। वैसे व्यापार की वस्तुओं का कम मिलने से प्रत्यक्ष व्यापार का प्रमाण कम मिलता है, पर शायद फारस की खाड़ी के रास्ते व्यापार होता था। मेसोपोटामिया में कुछ प्राचीन लेख पाये गये हैं, जिनसे उसके हड़प्पाकालीन सभ्यता के साथ व्यापार सम्बन्धों का पता चलता है। मेसोपोटामिया में स्थित अक्काड़ के प्रसिद्ध सम्राट सारगॉन (2350 ई.पू.) का यह दावा था कि दिलमुन, माकन (मकरान तट) और मेलुहा (सिन्धु सभ्यता के बंदरगाह या क्षेत्र) के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। मेसोपोटामिया के आरम्भिक साहित्य में मेलुहा के व्यापार समुदाय का जिक्र है, जो मेसोपोटामिया में रहता था। मेसोपोटामिया के एक अन्य लिखित दस्तावेज में मेलुहा की भाषा के सरकारी दुभाषिए का जिक्र है।
इन सब उदाहरणों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों और मेसोपोटामिया के लोगों के बीच संबंध अप्रत्यक्ष नहीं थे। उर शहर के व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ अन्य दस्तावेज भी पाये गये हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उर के व्यापारी मेलुहा से तांबा, गोमेद, हाथी दांत, सीपी, वैदूर्यमणि, मोती और आबनूस आयात करते थे। हड़प्पा में मेसोपोटामिया की वस्तुओं का न पाया जाना इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि परम्परागत रूप से मेसोपोटामिया के लोग कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल और चमड़े के उत्पाद बाहर भेजते थे। चूंकि ये सभी वस्तुएं जल्दी नष्ट हो जाती हैं, इस कारण इनके अवशेष नहीं मिले हैं। शायद चांदी भी निर्यात की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में चांदी के स्रोत नहीं थे। लेकिन वहां के लोग इसका काफी मात्र में प्रयोग करते थे। सम्भवतः यह मेसोपोटामिया से आयात किया जाता होगा।
सिन्धु सभ्यता के बड़े शहरों की अवस्थिति के कारणों का विश्लेषण करते समय विद्वानों ने इन शहरों के स्वरूपों को खाद्य उत्पादन के लिए उनकी समर्थता और व्यापार मार्गों व खनिज स्रोतों की निकटता से प्रभावित माना है। उदाहरणस्वरूप हड़प्पा शहर ऐसी जगह स्थित था, जो दक्षिण की ओर स्थित कृषि बस्तियों और उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित खानाबदोश चरवाहा बस्तियों को एक-दूसरे से विभाजित करती थी। इस प्रकार हड़प्पा के लोग दोनों समुदायों के संसाधनों का उपयोग कर सकते थे। यह एक बड़े शहर के रूप में इसलिए विकसित हो सका, क्योंकि एक व्यापारिक बस्ती के रूप में इसकी अवस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा की अवस्थिति इतनी उत्तम थी कि वह अपने चारों ओर 300 कि.मी. के क्षेत्र के भीतर हिन्दुकूश और पश्चिमोत्तर सीमान्त से फीरोजा तथा वैदूर्यमणि प्राप्त कर सकता था, नमक क्षेत्र से खनिज नमक, राजस्थान से टिन और तांबा, कश्मीर से सोने तथा एमिथिस्ट और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों से लकड़ी प्राप्त कर सकता था।
मोहनजोदड़ो का विकसित शहर के रूप में उभरना उसके समुद्र से अधिक निकट होने के कारण संभव हुआ, जिसके कारण यहां के वासियों का फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया पहुंचना आसान था। फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया वे क्षेत्र थे, जो सम्भवतः चांदी के मुख्य आपूर्तिकर्त्ता थे। इसलिए मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर बन गया था। इसी प्रकार लोथल निवासी दक्षिणी राजस्थान और दक्कन से संसाधन प्राप्त करते थे। सम्भवतः वे हड़प्पावासियों को कर्नाटक से सोना प्राप्त करने में मदद करते थे। कर्नाटक में सोने की खानों के पास समकालीन नवपाषाणयुगीन बस्तियां थीं। लोथल एक बंदरगाह नगर होने के कारण काफी विकसित नगर बन सका था। मकरान समुद्र तट पर सुतकागेनडोर हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार चौकी था। बलूचिस्तान, समुद्र तट के पास स्थित बालाकोट और सिंध में चन्हूदड़ो सीपीशिल्प और चूडि़यों के लिए प्रसिद्ध थे। लोथल और चन्हूदड़ो में लाल पत्थर और गोमेद के मनके बनाए जाते थे। चन्हूदड़ो में वैदूर्यमणि के कुछ अधबने मनके इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा निवासी दूर-दराज के स्थानों में बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे और उन पर काम करके उन्हें बेचते थे। पत्थरों के औजार बनाने के लिए सुक्कुर प्रसिद्ध था। इस तरह हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर व्यापार ढांचों से बंधे हुए थे और अपनी-अपनी भूमिका निभाते थे।
Question : मुगल सम्राट एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी।
(1994)
Answer : इंग्लैण्ड के सम्राट जेम्स (प्रथम) के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिन्स 1608 ई. में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, किन्तु वह सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका था। जहांगीर ने उसे ‘खान’ की उपाधि एवं 500 ‘जात-सवार’ की उपाधि दी थी। सन् 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिटलटन सूरत के समीप स्वालली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल रहा। सर थॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया। यहां उसने 1618 में अपने पक्ष में दो फरमान-एक बादशाह द्वारा तथा दूसरा शहजादा खुर्रम द्वारा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इन फरमानों से अंग्रेजों को व्यापार करने तथा आन्तरिक व्यापारिक करों से छूट मिल गयी। शाहजहां के काल में मुगल सेना ने अंग्रेजों के कारखानों पर आक्रमण किया था। बाद में अंग्रेजों ने भी बालासोर में स्थित मुगल नौ-बेडे़ पर आक्रमण किया था। लेकिन अंततः इनका संबंध अंग्रेजोंद्वारा माफी मांगने के बाद सुधरा। अंग्रेजों को हमेशा शक की नजर से देखने वाले औरंगजेब ने मुगल बेड़ों और हज यात्रियों पर आक्रमण करने के कारण बम्बई की अंग्रेज बस्तियों को घेरने का आदेश दे दिया था। बाद में बम्बई के अंग्रेज प्रमुख जॉन चाइल्ड द्वारा माफी मांगने पर ही उसका यह क्रोध शांत हुआ था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को बड़ी व्यापारिक सुविधायें दी थीं। बक्सर युद्ध में विजयी होने के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनीमुगल शासक शाह शुजा से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी प्राप्त करने में सफल रही थी। अंग्रेजों ने 1802 ई. में दिल्ली में प्रवेश किया और मुगल शासकों को अपने परनिर्भर बना लिया। अंततः 1857 के विद्रोह के बाद कम्पनी ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून (बर्मा) निर्वासित कर दिया और दिल्ली के किले पर पूर्ण अधिकार कर लिया।
Question : महाराष्ट्र धर्म का अर्थ एवं विशेषताएं
(1994)
Answer : 16वीं-17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में संत तुकाराम तथा गुरु रामदास समर्थ आदि द्वारा फ्महाराष्ट्र धर्म" का प्रचार हुआ, जिसके सिद्धान्त भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। इस धर्म के प्रणेताओं- ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और चक्राधर से लेकर एकनाथ, तुकाराम और रामदास तक, महाराष्ट्र के सभी संतों और दार्शनिकों ने भक्ति के सिद्धान्त एवं इस बात पर बल दिया कि सभी मनुष्य परमपिता ईश्वर की संतान हैं और इस कारण समान हैं। उनके जाति प्रथा का विरोध करने के कारण मराठा और कुन्बी जैसी निम्न जाति के लोग उनके अनुयायी बन गये। ये संत स्थानीय मराठी भाषा में ही उपदेश देते थे, जिससे इस भाषा को इच्छित गौरव प्राप्त हुआ और इसे एक साहित्य भी मिला। एक विशिष्ट मराठा पहचान उभर कर सामने आई, जिसने यहां के लोगों को एकता एवं लक्ष्य की भावना से प्रेरित किया। इस प्रकार महाराष्ट्र धर्म के प्रभावस्वरूप परंपरागत हिन्दू समाज की संरचना के अंतर्गत ही व्यक्ति वर्ग तथा समुदायों को उपरि-गतिशीलता (न्चचमत डवइपसपजल) के अवसर प्राप्त हुए। इस प्रकार तत्कालीन, सामाजिक व्यवस्था किसी की भी उन्नति में बाधक नहीं थी। अपनी योग्यता के बल पर व्यक्ति समाज में ऊंची से ऊंची पदस्थिति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता था। जैसाकि स्वयं सिंधिया के दृष्टांत से अनुमान लगाया जा सकता है, उसका जन्म एक दलित कुल में हुआ था, किंतु अपनी योग्यता के बल पर उसको समाज में सर्वोच्च पदस्थिति व प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इस तरह महाराष्ट्र धर्म ने मराठों को एकताबद्ध हो एक शक्ति बन कर उभरने में मदद किया।
Question : अभिलेखों तथा यूरोपीय यात्रियों के वृत्तान्तों से विजयनगर की प्रशासनिक संरचना के पूर्वांगों एवं दाय पर क्या प्रकाश पड़ता है?
(1994)
Answer : विजयनगर से सम्बन्धित अभिलेख अधिकांशतः मन्दिर से प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रमुख हैं- बेगापेल्लसी ताम्र पात्र अभिलेख (हरिहर-प्रथम का), भितरागुन्ता दान अभिलेख (संगम-प्रथम का), चन्नाराय पत्तिना अभिलेख (देव राय-द्वितीय)। यूरोपीय यात्रियों में से निकोली कॉन्टी (वेनेटियन का) ने देवराय प्रथम के काल का, पुर्तगाली डोमिन्गो पायस ने कृष्णदेव राय के समय का, पुर्तगाली नुनिज एवं बारबोसा ने भी कृष्णदेव राय के समय के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की उपयोगी जानकारी दी है।उपरोक्त वर्णित अभिलेखों एवं विदेशी यात्रियों के लेखों एवं विवरणों से विजयनगर की प्रशासनिक संरचना के बारे में सरलता से जाना-समझा जा सकता है।
उपरोक्त साक्ष्यों से पता चलता है कि विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रीय थी। राजा को ‘राजा’ कहा जाता था, जो ‘पूर्ण राजतन्त्र’ का उपभोग करता था। नागरिक, सैनिक एवं अन्य कार्यों में राजा ही सर्वोच्च शक्ति होता था और उसकी उत्पत्ति दैवीय सिद्धान्त पर आधारित थी। लेकिन राजा पर कुछ नियन्त्रण विधि एवं संस्थाओं का भी था। वैसे तो उत्तराधिकारी का वंशानुक्रम सिद्धान्त स्वीकार्य था। लेकिन सत्ता के लिए युद्ध भी होते थे। राजा के सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसका प्रधान महाप्रधानी कहलाता था। महाशान्तिग्रह विदेशी मामलों को, महानायकाचार्य अमर से नायकों या नायकारों पर नियंत्रण रखता था। भांडारिका खजाने की देखभाल करता था। धर्मशाला अधिकारी धार्मिक दानों एवं राजाओं की धार्मिक नीति को देखता था। मंत्रिगण कई बार वंशानुगत और कई बार चुने गये होते थे।
नुनिज एवं अब्दुल रज्जाक ने केन्द्रीय सचिवालय का उल्लेख किया है। इस सचिवालय में रायसिन (सचिव), कार्णिका (हिसाब कर्त्ता), मुद्राकर्त्ता (खजाने का इंचार्ज) आदि होते थे। साम्राज्य राज्यों या मंडलम (प्रांतों) में विभाजित था। कुछ का कहना है कि विजयनगर राज्य में 200 प्रांत थे, लेकिन के.ए.एन. शास्त्री इसे नहीं मानते। उनके अनुसार 6 प्रांत थे। प्रांतों का प्रमुख महामण्डलेश्वर होता था, जो अधिकांशतः राज परिवार का व्यक्ति होता था। प्रांतीय सरकार को एक हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी, उनका अपना दरबार, अधिकारी एवं सेना होती थी और उन्हें सिक्का जारी करने का अधिकार था। लेकिन महामण्डलेश्वर के एक जगह से दूसरी जगह भेजने एवं पदच्युत करने का अधिकार राजा को था।
विजयनगर के प्रांतीय प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता नायकर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार राजा भूमि का स्वामी समझा जाता था, जो अपने निर्भर लोगों को इसे दे सकता था। यह भूमि अनुदान (अमरम या क्षेत्र) एक निश्चित राजस्व के साथ सैनिक प्रमुखों को दिया जाता था। इन प्रमुखों को पोलियगार या नायक कहा जाता था। उन्हें एक निश्चित सेना रखनी होती थी और कुछ रकम केन्द्रीय सरकार को देनी होती थी। उन्हें अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखनी होती थी।
विजयनगर राजाओं ने पहले से चले आ रहे स्थानीय स्वशासन को बनाए रखा था। प्रत्येक गांव में एक सभा होती थी, जिसके सदस्य गांव के प्रमुख लोग होते थे। सभा को नई भूमि या सम्पत्ति लेने का अधिकार था। साथ ही उन्हें गांव की भूमि बेचने का भी अधिकार था। सभा को नए कर लगाने या पुराने कर हटाने एवं न्यायिक अधिकार भी था। नाडु व्यवसायिक श्रेणियों की सभा था, जिसके सदस्यों को नट्वारा कहा जाता था। इसे भी सभा की तरह अधिकार था।
ग्रामीण संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आयगर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक गांव एक पृथव्फ़ इकाई होता था और इसका कार्य 12 कार्यकारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें सामूहिक रूप से आयगार कहा जाता था, इन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। इनका पद वंशानुगत था और इन्हें अपना पद बेचने एवं गिरवी रखने का अधिकार था। इन्हें कर मुक्त भूमि ‘मान्यम’ वेतनस्वरूप दिया जाता था। सभी भूमि बिक्री कार्णिक नामक आयगार की जानकारी में ही बेचे जा सकते थे, जो इनका हिसाब रखता था। इन आयगारों में नाई, बढ़ई, धातुकर्मी आदि शामिल होते थे।
विजयनगर का राजस्व प्रशासन विस्तृत था, जिनके बारे में समकालीन अभिलेखों से जानकारी मिलती है। भूमि कर (शिस्त) आय का प्रमुख स्रोत था और इसके लिए एक विभाग था, जिसका नाम ‘अथवाने’ था। लगान उपज एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर लगाया जाता था। भूम कर सेतक होता था। भूमि कर के अलावा सम्पत्ति कर, विक्रय कर, व्यवसाय कर, सैनिक योगदान, विवाह पर कर आदि भी लगाये जाते थे। कर नकद या वस्तु में लिया जाता था। कर वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त किये जाते थे, कर वसूली के लिए कभी-कभी ठेका (Contract) भी दिया जाता था। ‘वरम’ एक व्यवस्था था, जिसमें भूमि मालिक एवं खेतिहर के बीच उपज का बंटवारा किया जाता था। विजयनगर राज्य की कुल आय 12,000,000 पराडो था। इसमें से सिर्फ आधा ही केन्द्रीय सरकार को मिलता था।
न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। नुनिज के अनुसार वहां ब्राह्मणों के कानून लागू थे। विजयनगर साम्राज्य में पुलिस तथा गुप्तचर व्यवस्था के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो काफी विकसित अवस्था में थे। साम्राज्य के सैनिक विभाग को ‘कंदाचार’ कहा जाता था, जिसका प्रमुख सर्व सेना पदाधिकारी होता था। सेना में हाथी, घोड़े़, ऊंट एवं पैदल सेना थी। अब्दुर्रज्जाक के अनुसार सैनिकों को प्रतिमाह वेतन मिलता था। नुनिज बताता है कि ऐसे 200 नायक थे जो अपने अमरम में हाथियों, घोड़ों एवं सेना को रखते थे।
अंत में, अभिलेखों एवं विदेशी यात्रियों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था काफी विकसित अवस्था में थी। लेकिन इतिहासकारों का मत है कि प्रशासन में नायकों के बढ़ते महत्व ही अंत में विजयनगर साम्राज्य के अंत का कारण बने।
Question : इतिहासकार के रूप में जियाउद्दीन बरनी।
(1994)
Answer : सल्तनत युग का सबसे प्रमुख इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी था। उसकी कृति तारीख-ए-फिरोजशाही उस युग की इतिहास कृतियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। बरनी ने इस ग्रंथ को 74 वर्ष की उम्र में 1357 ई- में पूर्ण किया। इस पुस्तक का शीर्षक फिरोजशाह तुगलक पर रखा गया है। बरनी ने इस पुस्तक का लेखन जब प्रारंभ किया तब उसकी याददाशत कमजोर हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप इसमें कई कालानुक्रमिक त्रुटियां रह गईं। इसके अलावा उसके व्यक्तिगत, वैचारिक, सामाजिक और सम्प्रदायी पूर्वाग्रहों का प्रभाव ऐतिहासिक घटनाओं की उसकी व्याख्याओं पर पड़ा। इन सब के बावजूद उस युग के इतिहास लेखन में बरनी का योगदान बेजोड़ रहा। इतिहास लेखन की लीक से हटते हुए उसने इतिहास को शासकों, दरबारों और युद्धों तक सीमित नहीं रखा। उसने प्रशासकीय विषयों और आर्थिक घटनाओं का वर्णन और विश्लेषण किया। उसने उस युग के विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य संघर्षों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें संदेह नहीं कि बरनी की रचनाओं का उपयोग करते समय काफी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि पर्याप्त तथ्य (जैसे तिथि और युद्धों का विवरण) देने में उसकी दिलचस्पी नहीं है। उसका इतिहास स्पष्टतः आत्मपरक (Subjective) है। यदि हम मध्यकाल के बौद्धिक इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो बरनी की कृतियों से हमें अनिवार्यतः मदद मिलेगी। बरनी की एक अन्य पुस्तक ‘फतवा-ए-जहांदारी’ राजनैतिक सिद्धांतों से सम्बन्धित है।
Question : जहांगीर एवं अकबर कालीन कथात्मक चित्र
(1994)
Answer : अकबर एवं जहांगीर का कलाओं के प्रति अत्यधिक रुझान था। मुगल चित्रकला का अन्य शैलियों से भिन्न एक अलग स्कूल के रूप में स्थान प्राप्त करना अकबर की इसी रुचि का परिणाम था। हालांकि ईरान में छवि चित्रण बनाने की परम्परा थी, परन्तु ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण का आयाम बिल्कुल नया था। घटना ऐतिहासिक हो या चित्रकार की शुद्ध कल्पना, शिकार या युद्ध के दृश्यों का अंकन करते समय चित्रकार एक बने- बनाये सूत्र का प्रयोग करता था, जैसा कि 1580 के आसपास चित्रंकित किये गये तैमूरनामा में किसी घटना का चित्रण करते हुए भी चित्रकार घटना से असंबद्ध दिखाई देता है। इसमें कलाकारों ने अपने मन में पूर्व स्थापित परिकल्पना के अनुसार किलों का आकार, नदी पार करने, दर्शकों अथवा युद्ध संबंधी दृश्यों का चित्रण किया है। अकबरनामा में भी कलाकारों ने इन दृश्यों की नकल की है या उन्हें अपने अनुसार ढाल लिया है। अकबर के काल के कुछ कथात्मक चित्र थे- हमजानामा (1562-1580 ई.), अनवर-ए-सुहेली (1570 ई.), तुतीनामा (1570-1580 ई.), तारीख-ए-खानदान ए तैमूरिया (1570-1600 ई.), तारीख-ए-अलफी (1570-1600 ई.) एवं रज्मनामा (1582 ई.)। वैसे तो जहांगीर शिकार के दृश्यों, पक्षियों और फूलों की चित्रकारी पंसद करता था पर उसने छवि चित्रण की परम्परा भी जारी रखी। जहांगीर के समय के कुछ कथात्मक चित्र राजकुंअर की पांडुलिपि और दीवाने हाफिज में मिलते हैं। इन चित्रों में एक प्रकार की सादगी और अनगढ़ सौंदर्य दिखाई देता है, जो अकबरी चित्रणशाला के परिष्कृत और सुंसस्कृत चित्रों में बिरले ही दिखाई पड़ता है।
Question : क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लगभग 750 एवं 1200 ई. के बीच दक्षिण भारतीय मंदिरों के स्थापत्य का रूप विधान एवं वर्ण्य विषय विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि की उपज थी?
(1994)
Answer : प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहना उचित ही होगा कि लगभग 750 एवं 1200 ई. के बीच दक्षिण भारतीय मंदिरों के स्थापत्य का रूप विधान एवं वर्ण्य विषय विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि की उपज थी। 750 से 1200 ई. के बीच दक्षिण भारतीय आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति तीन प्रमुख विशेषतायें लिए हुए थी। प्रथम, आठवीं सदी ई. के बाद से कृषि विस्तार और व्यवस्था में मंदिरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गयी थी। दक्षिण भारत में मंदिरों को दान अर्थात्् ‘देवदान’ में भूमि दिया जाने लगा, जो 8वीं से 13वीं सदी ई. में बड़ी मात्र में हुई। यद्यपि मंदिर-बस्तियों में भी ब्राह्मण लाभ प्राप्तकर्ताओं की ही संख्या अधिक थी और इन्हें ‘अग्रहार’ कहते थे। इस प्रकार आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में मंदिर दूसरे नम्बर की भू-स्वामी संस्था के रूप में उभरा। मंदिर अक्सर कृषि बस्ती के केंद्र बिंदु का काम करता था और विभिन्न पशुपालक, कृषक तथा आदिवासी समूहों को समन्वित करने के माध्यम की भूमिका निभाता था।
मंदिर भूमियों के किराए और तनख्वाह के जरिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों का एकीकरण हुआ। मंदिर की भूमि किराएदारों को किराए पर दी जाती थी। उस किराएदार को प्राथमिकता मिलती थी, जो उत्पादन में से अधिक भाग (मेलावरम) मंदिर को देते थे। इस काल में मंदिर एक शक्तिशाली आर्थिक संस्था, सामाजिक कार्य करने वाली संस्था एवं समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति निर्धारित करने वाली संस्था बन कर उभरी थी। दक्षिण भारतीय राजाओं एवं धनियों ने अपनी प्रस्थिति मजबूत बनाने के लिए खुलकर मंदिरों को दान दिया और मंदिरों का निर्माण किया था। पल्लवों के एक सौ सत्रह लेखों में से तिरपन में मंदिरों को भूमि तथा ग्रामदान का उल्लेख है। ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताब्दी के पचहत्तर अभिलेखों में से (जिन्हें चोलकालीन माना जाता है) उनचास अभिलेखों में मंदिरों को दान देने की चर्चा है। तिरुपति, तंजावुर, चिदंबरम आदि मंदिरों को इस प्रकार अभूतपूर्व संपदा प्राप्त होती गयी।
इस काल की दूसरी विशेषता थी- छोटे-छोटे राज्यों का उदय। सभी दक्षिण भारतीय राज्य आपस में बराबर युद्धरत रहते थे और एक-दूसरे से महान बनने-दिखाने का प्रयत्न करते रहते थे। इसी के परिणामस्वरूप सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में स्थित मंदिरों का एक शैली अर्थात् द्रविड़ शैली में होने के बावजूद अपनी-अपनी एक अलग एवं खास विशेषता है। राष्ट्रकूटों ने पर्वत काट कर उन्हें मंदिरों का स्वरूप दिया, तो पल्लवों ने पत्थर को तराश कर पाण्डयों ने मंदिरों के साथ तालाबों को जोड़ दिया, तो चोलों ने विशाल मंदिरों एवं विशाल गोपुरमों का निर्माण किया।
इस काल की तीसरी प्रमुख विशेषता थी- दक्षिण भारतीय राज्यों के महान राजाओं द्वारा अपने नाम पर मंदिरों का निर्माण करना, जो उनकी महानता का प्रतीक एवं यशोगान का प्रतिरूप होता था। राजराजा-प्रथम चोल द्वारा तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करना या राजेन्द्र प्रथम चोल द्वारा उत्तर भारत पर अपनी विजय को यादगार बना देने के लिए कांचीपुरम में गंगयीकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण इस बात का प्रमाण है।
उपरोक्त वर्णित आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि ने 750 से 1200 ई. के बीच दक्षिण भारतीय मंदिरों की स्थापना रूप विधान एवं वर्ण्य विषय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते मंदिरों का प्रभाव मंदिरों की विशालता एवं कलात्मक विन्यास में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। इस काल में मंदिरों का निर्माण वृहदाकार में होने लगा और मंदिरों के चारों ओर काफी बड़ी जमीन को खाली रखा जाता था। साथ ही यह प्रयास किया जाता था कि मंदिर का शिखर एवं गोपुरम उस शहर में सबसे ऊंचा हो, जिससे मंदिर की श्रेष्ठता स्वयंसिद्ध हो। अब मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, तीर्थस्थल एवं व्यापारिक केन्द्र की भूमिका भी निभाने लगे थे। इसके कारण मंदिरों के ताम-झाम, कलाकृतियों एवं बनावट में काफी शानोशौकत का पदार्पण हो गया था।
द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषतायें, यथा-पिरामिड आकार का शिखर, जो कलाकृतियों से भरा रहता था एवं गोपुरम (प्रवेश द्वार) सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में स्थापित मंदिरों में मिलते हैं, लेकिन उनका रूप-विन्यास अलग-अलग है। कहीं पत्थरों का तो कहीं पर्वत काट कर तो कहीं ईंटों का प्रयोग किया गया है। हर राज्य अपनी एक अलग शैली विकसित करने के लिए कृतसंकल्प दिखता है और इसी का प्रभाव दक्षिण भारतीय मंदिरों में देखा जा सकता है।
दक्षिण भारत के सभी राज्यों के प्रमुख राजाओं ने अपनी महानता को दर्शाने के लिए मंदिर का निर्माण ही नहीं करवाया बल्कि इन मंदिरों को विशाल आकार देने का भी प्रयास किया। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण इसी सोच से कराया लगता है। इस मंदिर का प्रांगण 300 फीट लंबा तथा 200 फीट चौड़ा है। इसमें 95 फीट ऊंचा विमान तथा समतल मंडप है। सामने एक अलग मंडप में नंदि स्थापित है, जिसके दोनों ओर 50 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ है। दूसरी ओर राजराज (985-1014
ई.) द्वारा प्रसिद्ध वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चतुष्कोण प्रांगण में किया गया है। इसके भव्य विमान (शिखर) पर तेरह तल्लों (खंडों) में पिरामिडानुरूप ऊपर उठता हुआ शीर्ष भाग है, जिस पर आकर्षक स्तूपिका स्थापित है। इसकी ऊंचाई 192 फीट है जो द्रविड़ स्थापत्य में सबसे विशाल है। अतः अंत में यह कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत की 750 से 1200 ई. के बीच की आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि ने मंदिर स्थापत्य के रूप विधान एवं वर्ण्य विषय को काफी प्रभावित किया था और एक विविधता लिए हुए द्रविड़ शैली का मार्ग प्रशस्त किया था।
Question : मनसबदारी व्यवस्था के गुण और दोषों का विश्लेषण कीजिये। अकबर के उत्तराधिकारियों के अधीन यह किस प्रकार चला?
(1993)
Answer : अकबर द्वारा शुरू की गयी मनसबदारी प्रथा मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की अनुपम विशेषता थी। मुगल प्रशासन में मनसब (अर्थात् पद, स्थिति या प्रतिष्ठा) शब्द सरकारी पदानुक्रम में इसके धारक (मनसबदार) की प्रतिष्ठा का सूचक था। मनसबदारी प्रथा का उद्भव मध्य एशिया में हुआ था। एक विचारधारा के अनुसार बाबर इसे उत्तर भारत में लाया था। लेकिन इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को जाता है, जिसने इसे मुगल सैनिक संगठन और नागरिक प्रशासन का मूलाधार बनाया। मुगल साम्राज्य में मनसबदार शासक समूह में आते थे। प्रायः समूचे अमीर वर्ग, नौकरशाही तथा सैनिक ओहदेदारों को मनसब प्राप्त होते थे। परिणामस्वरूप, विभिन्न कालों में मनसबदारों की संख्या तथा उनके संगठन ने भौतिक दृष्टि से न केवल राजनीति और प्रशासन को, बल्कि साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य के मनसबदार अपना वेतन या तो नकद या जागीरों के रूप में प्राप्त करते थे। इससे वे भू-राजस्व तथा सम्राट द्वारा अनुमत अन्य सभी करों की वसूली करने के अधिकारी होते थे, मनसबदारी प्रथा कृषि तथा जागीरदारी प्रथा का भी एक अभिन्न अंग थी।
मूलभूत विशेषताएं: मनसबदार नागरिक तथा सैनिक दोनों ही विभागों से सम्बद्ध होते थे। उन्हें नागरिक विभाग से सैनिक विभाग में और प्रतिक्रम से स्थानान्तरित किया जाता था। मुगल मनसब का दोहरा स्वरूप होता था और यह दो स्थितियों का परिचायक था, एक का नाम जात (वैयक्तिक पद) तथा दूसरे का नाम सवार (अश्वरोही पद) था। जात का मुख्य उद्देश्य शासकीय पदक्रम में मनसबदार की स्थिति को इंगित करना था। नकद पाने वाले मनसबदार नकदी तथा निर्धारित जागीरों के जरिए वेतन लेने वाले जागीरदार कहलाते थे। जागीरें सहज रूप से हस्तांतरणीय होती थीं और किसी मनसबदार को लम्बे समय तक एक ही जागीर को अपने पास रखने की अनुमति नहीं होती थी। सामान्यतया गृह प्रदेशों (जागीर-ए-वतन) में जागीरें प्रदान की जाती थीं और यह केवल उन्ही जमींदारों को प्राप्त होती थीं, जिनके पास मुगल साम्राज्य की स्थापना से पूर्व अपने राज्य होते थे और मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के उपरान्त उन्हें जागीर-ए-वतन के रूप में अपने मूूल राज्य प्रदान कर दिये जाते थे। उदाहरणार्थ, राजपूत राजाओं को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के उपरान्त उन्हें उनके ही राज्य जागीर-ए-वतन के रूप में प्रदान किये गये।
मनसब आनुवंशिक नहीं होते थे तथा मनसबदार की मृत्यु या पदच्युति के उपरान्त यह स्वतः समाप्त हो जाता था। मनसबदार के पुत्र को नया मनसब प्रदान किये जाने पर नए सिरे से कार्य आरम्भ करना पड़ता था। दूसरी विशेषता ‘जब्ती’ प्रणाली थी, जिसके अनुसार जब किसी मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी, तब उसकी सारी सम्पत्ति सम्राट द्वारा जब्त कर ली जाती थी। यह युक्ति इसलिए शुरू की गयी थी कि मनसबदार जनता का मनमाने ढंग से शोषण न कर सकें। मनसबदारी प्रथा ने मुगल सम्राट को साम्राज्य के दूर-दूर के क्षेत्रों पर आवश्यक नियंत्रण, कृषि का विकास करने, आवश्यक सैनिकों की उपस्थिति एवं महत्वाकांक्षी लोगों को नियंत्रण में रखने का अवसर प्रदान किया था।
इस प्रथा के कई दोष भी थे। इस प्रथा के कारण एक वर्ग सुविधाभोगी वर्ग के रूप में उभरा और लगातार अधिक-से-अधिक सुविधा पाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाता रहा। मनसबदारों के एक जगह निश्चित नहीं रहने और मृत्यु के बाद सम्पत्ति जब्त हो जाने की बात ने उन्हें विलासी, उपभोगी एवं जनमानस का शोषक भी बना दिया था। जनता की कमाई बेहिसाब रूप से विलासिता पर खर्च होती थी। महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों ने मनसबदार बनकर सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने का भी प्रयास किया।
हालांकि अकबर द्वारा प्रचलित मनसबदारी व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के साथ अपने मूल रूप में उसके उत्तरराधिकारियों के काल में प्रचलित रही, किन्तु उसमें समय-समय पर कुछ परिवर्तन और संशोधन किये गये। जैसे कि जहांगीर के शासनकाल में दो अस्पा और सिह अस्पा पदों को मनसब के साथ जोड़ा गया। दो अस्पा और सिह अस्पा के शाब्दिक अर्थ थे- प्रति मनसबदार सैनिक के ऊपर दो या दो से अधिक घोड़े रखना। दो अस्पा और सिह अस्पा पद प्राप्त होने वाले मनसबदारों को अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाता था। शाहजहां के शासन काल में मनसबदारों के नए वेतनमान, भत्ते, उनके द्वारा गठित की जाने वाली सेना की संख्या आदि के सम्बन्ध में कुछ नवीन नियम प्रतिपादित किये गये। मनसबदारों को जागीरें प्रदान करने के उद्देश्य से दीवान-ए-विजारत द्वारा प्रत्येक भू-क्षेत्र से प्राप्त होने वाले राजस्व को एक बही में इंगित किया जाता था। इस बही में विभिन्न भू-क्षेत्रों की निर्धारित आय (जमा) का उल्लेख किया जाता था, जिन्हें रुपयों में नहीं, बल्कि दामों में निर्दिष्ट किया जाता था। इसकी गणना एक रुपये के लिए 40 दामों के हिसाब से की जाती थी। यह दस्तावेज जमादामी, अर्थात् दामों पर आधारित क्षेत्र की निर्धारित आय का प्रलेख कहलाता था। औरंगजेब के शासन काल में विशेषकर उच्च श्रेणियों के मनसबदारों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। मनसबदारों की संख्या इतनी अधिक हो गयी कि ऐसी शिकायतें होने लगीं कि उन्हें प्रदान करने के लिए कोई जागीरें शेष नहीं रह गयी हैं। संकट इतना विकट हो गया कि सम्राट और उसके मंत्री बार-बार सभी नई भर्तियां रोकने की सोचने लगे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। मनसबदारों की संख्या में अतिशय वृद्धि और जागीरों के अभाव ने जागीरदारी और कृषिजन्य संकट को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप औरंगजेब के शासन के परवर्ती दिनों में मनसबदारी व्यवस्था भी पतनोन्मुख हो गयी।
Question : हिन्द महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण और इसका प्रभाव।
(1993)
Answer : 1948 ई. में वास्को डी-गामा के कालीकट आगमन के उपरांत हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का नियंत्रण क्रमशः बढ़ता गया। राज्य संरक्षण, सुदृढ़ नौ सेना तथा चतुर कूटनीति के माध्यम से उन्होंने शीघ्र ही इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। सोलहवीं शताब्दी में पुर्तगालियों का मूल उद्देश्य सैन्य बल के प्रयोग द्वारा अपने देश और अपने आपको समृद्ध करना था। उनका स्पष्ट, लेकिन दुहरा लक्ष्य था- यूरोप भेजे जाने वाले मसालों पर एकाधिकार और अन्य एशियाई व्यापार पर नियंत्रण और उससे कर वसूलना। हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने शुरू से ही बल प्रयोग का तरीका अपनाया। पुर्तगाली स्वयं को सागर के स्वामी कहते थे। उन्होंने हिंद महासागर के अन्य देशों के साथ व्यापार करने पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। वे मानते थे कि मसालों के व्यापार पर पूर्णतया पुर्तगाली सम्राट और उसके अभिकर्त्ताओं का ही एकाधिकार है। कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना उनकी अनुमति के नहीं जा सकता था।
पंद्रहवीं एवं सोलहवीं शताब्दी में पुर्तगाली शासकों का उद्देश्य केवल व्यापार में लाभ कमाना ही नहीं था, अपितु अपने धर्म की सेवा करना भी था। इसी कारण उक्त अवधि में उनकी नृशंसता के शिकार प्रायः मुसलमान हुए। भारत में धर्म-परिवर्तन की दिशा में भी वे काफी सक्रिय रहे। जहां-जहां पुर्तगाली बस्तियां थीं, वहां पुर्तगालियों एवं भारतीयों के बीच सामाजिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक संकरण तथा आर्थिक, सैन्य एवं राजनीतिक सहयोग का सम्बन्ध विकसित हुआ। हिंद महासागर में पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण विशिष्ट बंदरगाहों और उनसे संबद्ध भू-भागों की समृद्धि में भी तीव्र परिवर्तन आया। 16 वीं शताब्दी के अंत तक समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों के नियंत्रण का यह भी परिणाम हुआ कि कोई भी भारतीय जहाज बिना उनकी अनुमति के पूर्वी अफ्रीका या मसाला द्वीपों में जाने का साहस नहीं कर सकता था। समुद्र में अन्य लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के अधिकार की धारणा को लाकर, पुर्तगलियों ने एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति का समावेश कर दिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिंद महसागार पर पुर्तगाली आधिपत्य का, न केवल व्यापार पर ही प्रभाव पड़ा वरन् तत्कालीन राजनीति तथा धार्मिक-सामाजिक स्थिति भी इससे प्रभावित हुए बिना न रह सकी।
Question : पूर्वकालीन वैदिक और उत्तरकालीन वैदिक संस्कृतियों के बीच परिवर्तन और सातत्य के तत्त्वों को स्पष्ट कीजिये।
(1993)
Answer : ऋग्वैदिक-उत्तर वैदिक साहित्य की रचना के लगभग 500 वर्ष एक महत्वपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वह काल था, जबकि लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में एक निश्चित दिशा में परिवर्तन हो रहा था। यह सत्य है कि इस काल का तथाकथित राजनीतिक इतिहास एक कथात्मक-परंपरा से आच्छादित है और किसी प्रकार के पुरातात्विक-साक्ष्य से दोषित नहीं है, किन्तु फिर भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में एक ऐसे ढांचे का आविर्भाव हुआ, जो छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ सदियों तक चला। इस काल में आविर्भूत ढांचे की प्रमुख विशेषताएं थीं- कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार पड़ना और वर्णव्यवस्था का जन्म तथा क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय।
तकनीकी विकास की दृष्टि से यही वह काल है, जबकि उत्तरी-भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। इसने धीरे-धीरे जीवन के विभिन्न पहलुओं-आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक, को प्रभावित किया। कबायली संगठन में दरार का एक प्रमाण तो इस बात से मिलता है कि ऋग्वेद कालीन अनेक छोटे कबीले एक-दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्रगत जनपदों को जन्म दे रहे थे। उदाहरणार्थ- पुरू एवं भरत मिलकर कुरू और तुर्वश एवं क्रिवि मिलकर पंचाल कहलाए। अनेक ब्राह्मण ग्रंथों में तो स्वयं कुरू-पंचाल युग्म के भी अनेक उल्लेख हैं। वास्तविकता तो यह है कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक गतिविधियों में कुरू-पंचाल और इनके जैसे बड़े-बड़े जनपदों का ही बोलबाला था। यह असंभव नहीं कि इस प्रक्रिया में लौह तकनीक ने भी सहयोग दिया हो। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, नोह, अतरंजीखेड़ा, बटेसर आदि स्थानों से, जो कुरू-पंचाल प्रदेश में ही पड़ते हैं, बरछी-शीर्ष एवं बाणाग्र जैसी अधिकांश लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह भी मात्र संयोग नहीं है कि उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में ही कुरू-पंचाल वंशी अनेक राजाओं द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का उल्लेख मिलता है, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि ऐसे राष्ट्रों की सैन्य शक्ति, उनके विकास का एक महत्वपूर्ण कारक थी। क्षेत्रीयता का तत्त्व अब उभर रहा था- यह इस बात से पता चलता है कि पैतृक राजतंत्र और राष्ट्र की अवधारणा के स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, फ्राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा वरुण, बृहस्पतिदेव, इन्द्र एवं अग्नि उसे दृढ़ बनाएं।य् राजत्व की दैवी उत्पति के सिद्धान्त की चर्चा भी इसी काल में शुरू हुई। हालांकि सभा, समिति, विदथ, परिषद आदि संस्थानों की गतिविधियों में कबायली जीवन की कुछ झलक मिल जाती है। समिति एवं परिषद की पहचान कबीले के लोगों से होती थी, जैसे, ‘पंचालों की समिति’। राजा की घोषणा ‘कबीले में होती थी। भूमि का दान भी राजा कबीले की अनुमति के बिना नहीं कर सकता था। इसी काल में भावी स्थायी सेना की अवधारणा के बीज भी (ऐतरेय ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण में) सीमित रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि वह सजातीयता के नियम पर आधारित थी।
लोगों के आर्थिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके स्थायित्व में दृष्टिगोचर होता है, जो कृषि के अधिकाधिक प्रसार का परिणाम था। चित्रित धूसर एवं उत्तरी काली पॉलिश मृद्भांडीय पुरातात्विक संस्कृतियों से, जिन्हें हम विभिन्न सीमाओं के बावजूद उत्तर वैदिक काल की कृतियां बताते हैं, लोगों के स्थायी जीवन की पुष्टि होती है। यद्यपि अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं किंतु उत्तर वैदिक काल में कृषि ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में तो जुताई से संबंधित कर्मकांडों पर एक पूरा-का-पूरा अध्याय (टप्प्ण्2ण्2ण्) दिया गया है। ऋग्वेद की तुलना में उत्तर वैदिक साहित्य में विभिन्न अनाजों का वर्णन है और सौभाग्यवश अतरंजीखेड़ा से जौ, चावल एवं गेहूं के प्रमाण भी मिल गये हैं। कृषि के अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय भी उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता थी। इन विभिन्न व्यवसायों के अनेक विवरण हमें पुरुषमेध के विवेचन में मिलते हैं जिनमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि उल्लेखनीय हैं।
उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टतः वर्णव्यवस्था पर आधारित हो गया, जिसमें ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को विशेष स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में ब्रह्म एवं क्षत्र तथा मित्र एवं वरुण के जिस द्वंद्व का उल्लेख है, वह ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के पारस्परिक मनमुटाव का ही द्योतक है, लेकिन अन्य वर्णों के मामले में ये दोनों अपने विशेषाधिकार की रक्षा के लिए एक भी हो जाते थे। इस काल में वैश्यों एवं शूद्रों का शोषण धीरे-धीरे बढ़ने लगा था एवं वर्ण-व्यवस्था कठोरतम रूप ग्रहण करने लगी थी।
सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं में ‘कुल’ का उल्लेख दृष्टव्य है, जो कि ऋग्वेद में अप्राप्य है। यद्यपि एक पत्नी विवाह के आदर्श को अब भी मान्यता प्राप्त थी, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बहुपत्नी विवाह काफी प्रचलित था और सबसे पहली पत्नी को मुख्य पत्नी होने का विशेषाधिकार प्राप्त होता था। ऋग्वैदिक काल की नारी की तुलना में अब उसके स्थान में कुछ गिरावट आ गयी। मैत्रयणी संहिता में तो उसे पासा एवं सुरा के साथ-साथ तीन प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। उत्तर वैदिक कालीन जैसे पितृप्रधान समाज में पुत्र जन्म की लालसा स्वाभाविक थी, किन्तु यह सुझाव उस समय अपनी सारी सीमाओं को पार कर जाता है, जबकि हम ऐतरेय ब्राह्मण में यह पढ़ते हैं कि पुत्री ही सभी दुःखों का स्रोत तथा पुत्र ही परिवार का रक्षक है।
ऋग्वेदकालीन धार्मिक जीवन की भांति उत्तर वैदिक काल के लोगों की धार्मिक आस्थाएं एवं गतिविधियां भी तत्कालीन भौतिक पृष्ठभूमि से कुछ कम प्रभावित न थीं। इस युग में एक ओर तो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित एवं पोषित यज्ञ अनुष्ठान एवं कर्मकांडीय व्यवस्था थी, तो दूसरी और इसके विरुद्ध उठाई गयी उपनिषदों की आवाजें। यों तो यज्ञादि का आभास ऋग्वेद में भी मिलता है, किन्तु एक स्वतंत्र प्रथा के रूप में इसका विकास इसी युग में हुआ। चूंकि ब्राह्मण एक अनुत्पादी वर्ग था, अतः अपने को विशेषाधिकार संपन्न वर्ग बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह लोगों के मस्तिष्क पर अपनी धार्मिक श्रेष्ठता की छाप बनाए रखे। इसीलिए कर्मकांडाें का जो विकास इस युग में दृष्टिगोचर होता है, उसमें ब्राह्मणों का हित निहित था। इस काल में ऋग्वेद कालीन बहुत से देवताओं, यथा- इन्द्र, वरुण एवं अग्नि आदि का महत्व कुछ कम होने लगा था। अब प्रमुख देवताओं में प्रजापत्य, विष्णु, शिव (ऋग्वेद कालीन रूद्र) एवं ब्रह्मा प्रमुख हो गये थे। अब यज्ञों एवं कर्मकाण्डों का महत्व बेहद बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदीय अद्वैत सिद्धान्त में दृष्टिगोचर होती है। यह ब्राह्मणों के कर्मकांड पर एक गहरा आघात था।
इस तरह कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में पूर्वकालीन वैदिक काल की अपेक्षा काफी परिवर्तन हुआ, लेकिन वस्तुतः ये सारे परिवर्तन पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं पर ही आधारित थे।
Question : चोल साम्राज्य के विकास के लिए राजराजा प्रथम और राजेन्द्र प्रथम के योगदान की विवेचना कीजिये। चोलों के नौसेनिक अभियानों के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिये।
(1993)
Answer : चोल साम्राज्य के विकास के लिए राजराजा प्रथम और राजेन्द्र प्रथम के योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। चोल राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजराजा प्रथम था, जिसने 985 में 1014 ई- तक राज्य किया। उसके तंजौर अभिलेख में उसकी युद्ध सम्बन्धी सफलताओं का वर्णन इस प्रकार दिया गया हैः "उसने कन्दलपुर सलाई में जहाजों को नष्ट किया और महान् युद्धों में सफल अपनी सेना (साढ़े सात लाख सैनिकों) द्वारा वेंगयी-नादु, गंगपदी, तदिगौपदी, नोलम्बपदी, कुदामलाई-नादु, कोललम कलिंगम् और समुद्र के बारह हजार प्राचीन द्वीपों के स्वामी महाशक्तिशाली सिंहलों के प्रदेश इलामपडलम् तथा इस्तपदी को जीता और शेलियों के गौरव को उस समय नष्ट किया, जब उनकी सर्वत्र पूजा होती थी।" उसने चेरों की नौसेना को त्रिवेन्द्रम के निकट नष्ट किया, मदुरा को जीता, कुर्ग एवं उदागयी के किले को जीता, लंका के उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिला लिया और वहां एक शिव मन्दिर बनवाया, पश्चिमी गंगों को 991 ई. में हराया। राजराजा ने पश्चिमी चालुक्यों के प्रदेशों, 12000 प्राचीन द्वीपों अर्थात् मालदीव द्वीपों को भी जीता था। राजराजा एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था।
राजराजा योग्य प्रशासक, धार्मिक और सहिष्णु व्यक्ति भी था। वह कला और विद्वता का संरक्षक था। 1000 ई. में उसने भूमि सर्वेक्षण आरम्भ किया। अपने राज्य में उसने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। उसने उत्तराधिकारियों में संघर्ष रोकने के लिए युवराज नियुक्त करने की प्रथा शुरू की। राजराज ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर एवं चूड़ामणि विहार का निर्माण करवाया। इस तरह राजराजा ने अपने प्रयास से चोल राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक महान एवं विकसित राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसके इस कार्य को उसके योग्य पुत्र राजेन्द्र प्रथम (1012-1044 ई.) ने योग्यता से आगे बढ़ाया।
राजेन्द्र प्रथम ने सिंहासनारोहण के कुछ वर्ष बाद सम्पूर्ण लंका को ही अपने राज्य में मिला लिया। केरल, पाण्ड्यों, पश्चिमी चालुक्यों आदि राजाओं के प्रदेशों को जीता। पूर्वी भारत की ओर अपने अभियान में उसकी सेना गोदावरी, बस्तर और उड़ीसा को पार कर पश्चिम बंगाल पहुंची और वहां के राजा महिपाल को हरा, गंगा का पवित्र जल लेकर लौटी। उसने काड़रम (दक्षिण-पूर्व एशिया) के राजा संग्राम विजयोतुंग वर्मा के विरुद्ध भी नौसैनिक अभियान भेजा था। इसी के साथ राजेन्द्र प्रथम ने गंगयीकोण्डचोलपुरम् में नई राजधानी बनाई, जिसमें सिंचाई व्यवस्था, मन्दिर और महल थे, जिनके अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं। उसने चीनी सम्राट के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये और 1016 तथा 1033 ई. में राजदूत भेजे। कहा जाता है कि उसने एक वैष्णव केन्द्र में 340 विद्यार्थियों के लिए एक वैदिक महाविद्यालय की व्यवस्था की। उसमें चौदह आचार्य नियुक्त किये। राजेन्द्र प्रथम ने स्थानीय स्वशासन, व्यापार एवं प्रशासन में सुधार के लिए कई कदम उठाए थे।
चोल शासक शक्तिशाली नौसेना के गठन के लिए सर्वप्रसिद्ध हैं। नौसेना की सहायता से ही उन्होंने समुद्र पार विजयें कीं। उनके द्वारा शक्तिशाली नौसेना बनाने के पीछे प्रमुख कारण था-व्यापार का विकास एवं साम्राज्यवादी सोच को पूरा करना। राजराजा प्रथम ने कन्दलूर के समीप चेरों का नाविक बेड़ा नष्ट किया था तथा लंका एवं मालदीव पर अधिकार किया था। राजेन्द्र प्रथम ने समस्त लंका को ही अपने राज्य में मिला लिया। उसने सुमात्र और मलाया प्रायद्वीप के लिए एक समुद्री अभियान भी भेजा। कुलोतुंग चोल के समय भी चोल नौ सेना काफी मजबूत थी।
इस शक्तिशाली नौसेना होने के कारण ही बंगाल की खाड़ी को ‘चोल झील’ कहा जाता था। शक्तिशाली नौसेना ने चोलों को बंगाल की खाड़ी एवं हिन्द महासागर की एक शक्ति बना दिया था। नौसेना के विकास के कारण ही इस क्षेत्र में काफी मदद मिली। इसी काल में चीन-भारत व्यापार में काफी तेजी आई। साथ ही, भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक योगदान एवं प्रभाव काफी तेज हुआ। चोलों की नौसैनिक शक्ति के प्रभाव स्वरूप ही दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों पर भारतीय संस्कृति का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उस क्षेत्र को बाद में वृहत्तर भारत ही कहा जाने लगा।
Question : अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के महत्व का परीक्षण कीजिये। क्या वह इन उपायों को लागू करने में सफल हुआ था?
(1993)
Answer : अलाउद्दीन एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, व्यावहारिक राजनेता तथा महान प्रशासक था। उसने अपने शासन के पूर्व प्रचलित शासन व्यवस्था का बारीकी से मूल्यांकन किया और इसमें व्यापक सुधार किये। उसके द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण सुधार इस प्रकार हैं:
(I)विद्रोहों को रोकने के उपाय: अलाउद्दीन को अपने शासन के प्रारम्भिक दिनों में अकत खां, मलिक उमर और मंगू खां तथा हाजी मौला के नेतृत्व में तीन विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहों से आशंकित होकर सुल्तान ने यह निश्चय किया कि भविष्य में ऐसे विद्रोहों या उपद्रवों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जायें। उसने मूलभूत निरोधात्मक उपाय किये। प्रथमतः, उसने अमीरों तथा अधिकारियों द्वारा संचित धन पर प्रहार किया। राज्य द्वारा वक्फ या धार्मिक कार्यों के लिए प्रदत्त इक्ताओं एवं अनुदानों को रद्द कर दिया गया।
द्वितीयतः, एक कुशल एवं व्यापक गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया गया। तृतीयतः, दिल्ली में शराब एवं नशीले पदार्थों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया। चतुर्थतः, सामाजिक समारोहों एवं प्रीतिभोजों के आयोजन, अमीरों के परिवारों के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध तय करने आदि पर भी कठोर प्रतिबन्ध लगाए गये और इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाने लगी। अमीरों के परिवारों के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध निश्चित करने से पूर्व सुल्तान की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक बना दिया गया। अमीरों एवं अधिकारियों के मध्य आपसी मेलजोल और अन्तर्सम्बन्धों पर विभिन्न प्रतिबन्ध लगाए गये।
(II) लगान व्यवस्था में सुधार: उसने भू-राजस्व या लगान व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यापक सुधार कियेः
(क) राजस्व विषयक उसका पहला अधिनियम (जाबिता) कृषि योग्य भूमि की माप से सम्बन्धित था, जिससे कि भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया जा सके। बिस्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया गया।
(ख) प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में निर्धारित किया गया।
(ग) सुल्तान ने मुखियों और लगान वसूल करने वाले हिन्दू अधिकारियों, जैसे- खुत, मुकद्दम एवं चौधरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इन्हें अन्य सामान्य कृषकों की भांति समान दर पर लगान एवं करों को अदा करने के लिए बाध्य किया गया।
(घ) लगान या भू-राजस्व के अतिरिक्त कृषक जनता पर गृह कर (घरी) एवं चरागाह कर (चरी) भी आरोपित किये गये।
(घ) अधिकांश छोटी इक्ताओं को समाप्त कर दिया गया और इनसे प्राप्त जमीनों को खालसा (राजभूमि या केन्द्र द्वारा नियंत्रित भूमि) के अंतर्गत लाया गया।
(च) खालसा भू-क्षेत्रों से लगान सीधे राज्य द्वारा वसूल किया जाने लगा।
(छ)बाजार-नियंत्रण व्यवस्था की सफलता के लिए लगान को फसल या जिंस के रूप में वसूल किया जाने लगा और किसानों को अपनी शेष उपज को खेतों में ही बेचने के लिए बाध्य किया गया, जिससे कि वे अनाज की जमाखोरी न कर सकें।
(III) बाजार नियंत्रण व्यवस्था: अलाउद्दीन खिलजी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण व्यवस्था था। चूंकि सुल्तान ने समकालीन बाजारों पर राज्य के पूर्ण नियन्त्रण की स्थापना की, अतः तत्सम्बन्धी सुधारों को बाजार नियंत्रण व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम लागू किये गये, वे आर्थिक अधिनियम कहलाते हैं। इन क्रान्तिकारी एवं अनूठे सुधारों को लागू करने के पीछे सुल्तान के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के कारणों के बारे में विवाद है। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के अनुसार, इन सुधारों को लागू करने के पीछे मूलभूत उद्देश्य मंगोलों का मुकाबला करने के लिए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना खड़ी करना था। इतनी विशाल सेना को बहुत अधिक वेतन देना कठिन था, अतः कम वेतन पर रहने वाले सैनिकों को सस्ते में जरूरत के सामान दिलवाने के लिए ही बाजार नियंत्रण किया गया था। जबकि अमीर खुसरो के अनुसार, इन सुधारों का लक्ष्य सामान्य लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति तथा साथ ही, अकाल का सामना करने के लिए निर्धारित दरों पर शाही गोदामों के लिए खाद्यान्न संग्रह सुनिश्चित करना था। जो भी हो, अलाउद्दीन के प्रयास से बाजार में एक व्यवस्था, मूल्यों में नियन्त्रण में एक व्यवस्था, मूल्यों में नियन्त्रण एवं स्थिरता एवं व्यापक सुधार आया।
(IV) अलाउद्दीन ने सेना में सुधार की प्रक्रिया भी आरम्भ की थी। ‘दाग’ और ‘चेहरा’ पद्धति को आरम्भ कर उसने सेना में काफी सुधार किया और एक शक्तिशाली सेना का गठन किया।
अलाउद्दीन इन प्रशासनिक सुधारों को अपने शासन काल में लागू करवाने में एक हद तक सफल भी रहा था। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये सारे सुधार राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही सही मायने में सफलतापूर्वक लागू हो सकते थे। अन्य क्षेत्रों में पूर्व की व्यवस्था ही चलती रही थी। अलाउद्दीन ने अपने जिस साम्राज्य का इतनी शक्ति एवं निर्ममतापूर्वक निर्माण किया था, वह उसके जीवन के अन्तिम दिनों में ही धराशायी होने लगा। जिस मलिक काफूर को उसने मलिक नायब (रीजेन्ट) के उच्च पद पर नियुक्त किया था, वह सभी संभावित प्रतिद्वन्द्वियों को मिलाकर राज्य पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास करने लगा। अलाउद्दीन के उत्तरा -धिकारी के कमजोर होने के कारण भी अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार उसकी मृत्यु के बाद एकदम से समाप्त हो गये थे।
Question : मुगल चित्रकला
(2007)
Answer : भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली, वह एक उन्नतिशील एवं शक्तिशाली कला आंदोलन के रूप में विकसित हुई। हालांकि मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी लेकिन मुगल चित्रकला का विकास हुमायूं के समय आरंभ हुआ, जब हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर ईरान में निवास कर रहा था। उसी समय ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अबदुस्समद की सेवाएं प्राप्त हुईं। ये दोनों चित्रकार हुमायूं की अस्थाई राजधानी काबुल में काम शुरू किये। बाद में जब हुमायूं दिल्ली को जीता तो ये दोनों कलाकार दिल्ली आ गए। इन परिस्थितियों में मुगल चित्रकला पर ईरानी प्रभाव का होना स्वाभाविक था।
हालांकि सल्तनत काल में ही ईरानी कला का प्रभाव भारत में महसूस किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय चित्रकार जहां अधिकतर धार्मिक विषयों का चित्रण करते थे, वहीं ईरानी चित्रकारों ने राजदरबार के जीवन, युद्ध के दृश्य आदि का चित्रण किया। मुगल चित्रकला के आरंभिक काल से ही ईरानियों के विषय और विधि का प्रभाव तो पड़ा ही, इसके अलावा चित्रण में भी ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से था। फूल-पौधे और पशु-पक्षी, वेश-भूषा आदि सभी पर ईरानी प्रभाव था।
अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने नया रूप धारण किया उस पर भारतीय प्रभाव की झलक मिलती है। चूंकि अकबर ने भारत में समन्वित संस्कृति के विकास की नीति अपनायी। उदार धार्मिक नीति, राजपूतों से मित्रता तथा विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों के भौगोलिक प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं एक-दूसरे के संपर्क में आईं। विशेषकर राजपूत चित्रकला ने मुगल शैली को प्रभावित किया। इनकी प्रमुख विशेषताओं यथा गोल ब्रश का प्रयोग गहरे नीले और गहरे लाल रंग का अधिक प्रयोग आदि का समावेश मुगल चित्रें में देखी जा सकती है। इसके अलावा लोगों के चेहरे, रंग-रूप, वेश-भूषा, फूल-पौधे, पशु-पक्षी इत्यादि अब भारतीय हैं न कि ईरानी। राजपूत शैली का इतना अधिक प्रभाव अकबर द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय चित्रकारों को नियुक्त करने के कारण हुआ। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में दसवंत एवं बसावन को नाम उल्लेखनीय हैं।
इसी समय पुर्तगालियों के माध्यम से यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूना अकबर के दरबार में पहुंचा, जिससे मुगल शैली पर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी पड़ा। मुगल चित्रकारों ने व्यक्ति विशेष के चित्र बनाने तथा अग्रसंक्षेपण की विशेषता यूरोपीय चित्रकला से ग्रहण किया। इस प्रकार अकबर के काल में मुगल चित्रकला में विभिन्न शैलियों का मिश्रण हुआ तथा एक नई और अधिक समुन्नत शैली का विकास हुआ। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। इस समय हम दो नई विशेषताओं को देखते हैं। पहली मोरक्का के रूप में है। इसमें चित्रें का संकलन एक जगह, पक्षियों का एक जगह तथा फूलों का एक जगह संकलन इत्यादि।
दूसरी विशेषता कमबवतंजमक उंतहपदे के रूप में मिलती है। जहांगीर को चित्रो का बड़ा पारखी भी माना जाता है। चित्रकारी की यह परंपरा शाहजहां के समय भी जारी रही। परंतु इसे हम चित्रकला के दृष्टिकोण से शिथिल काल ही कह सकते हैं। इसके बाद औरंगजेब के समय दरबार में कट्टरपंथी प्रभाव के कारण चित्रकला का पतन हो गया तथा अनेक मुगल चित्रकार राजपूत राजघराने में चले गए। मुगल शैली की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें राजनीतिक एवं दरबारी जीवन का चित्रण ही मुख्य रूप से हुआ। जन सामान्य के जीवन की झलक मुगल शैली में नहीं मिलती।
Question : दर्शाइए की भारत में प्रशासनिक तंत्र चोल काल के दौरान एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था।
(2007)
Answer : सामान्यतः चोलकाल सैन्यविजयों, विस्तृत साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया एवं दक्षिण भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना के युग के तौर पर जानी जाती है। लेकिन विद्वानों का एक विशाल समूह चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं इसकी अद्भूत विशेषताओं को चोल काल की वास्तविक उपलब्धि मानते हैं। हालांकि बर्टेन स्टीन जैसे कई इतिहासकार चोलकालीन प्रशासनीक पद्धति को बहुत महत्व प्रदान न करते हुए इसे एक ‘खंडित राज्य’ ही मानते हैं। परन्तु वास्तव में, चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत सुनियोजित एवं प्रभावी थी, विशेषकर ग्रामीण स्वायत्तता व्यवस्था ने चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। चोल प्रशासन के शीर्ष पर स्वयं राजा होता था जिसकी तुलना देवता से की जाती थी। ‘देवत्व के सिद्धान्त’ को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मृत राजाओं की पूजा मंदिरों में की जाने की प्रथा को प्रोत्साहित किया गया था। सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें ‘मंडलम’ कहा जाता था। प्रान्तों की संख्या संभवतः 8 या 9 थी।
प्रत्येक मंडल कई कोट्टमों (वलनाडु) में विभक्त थे एवं कोट्टम कई नाडुओं में विभक्त था। प्रत्येक नाडु में अनेक ग्राम-संघ थे, जिन्हें ‘कुर्रम’ एवं ‘तार-कुर्रम’ कहा जाता था। इस प्रकार प्रशासन की इकाइयां पूर्णतः श्रेणीबद्ध थीं। सामान्यतः मंडलम् का प्रमुख राज परिवार का व्यक्ति ही होता था। इसके अतिरिक्त चोल प्रशासन में अधिकारों का विशाल समूह और एक शक्तिशाली नौकरशाही तंत्र, प्रशासनिक सुव्यवस्था हेतु जिम्मेदार थे। सामान्यतः उच्च अधिकारियों का वर्ग पेरूदारम एवं निम्नाधिकारियों का वर्ग सेरूदारम कहलाते थे। अधिकारियों की नियुक्ति में जन्म, जाति एवं योग्यता के बीच उचित संतुलन बनाया जाता था। केन्द्रीय प्रशासन में प्रशासकीय विभाग थे। इन सबसे बीच बेहतर तालमेल था एवं प्रशासकीय अभिलेखों (रिकार्ड) को नियमित ढंग से रखा जाता था।
चोल काल में राजस्व प्रशासन व्यवस्थित था। भूमि की पैमाइश की जाती थी एवं कर योग्य भूमि को निश्चित श्रेणियों में बांटा जाता था। साधारणतः भू-राजस्व (मकमई) कुल उत्पादन का 1/3 होती थी। अन्य कई प्रकार के ‘कर’ लगाए गये थे, यथा व्यवसाय कर, गृह एवं उत्सव कर आदि। चोलकाल में न्यायिक पद्धति भी केन्द्रीय न्यायालय से ग्राम न्यायालय तक संगठित रूप से स्थापित की गई थी। उपरोक्त तथ्य किसी भी साम्राज्य के उन्नत प्रशासनिक प्रणाली को अभिव्यक्त करती है। यद्यपि आलोचक प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं कि चोल प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय शक्तियों पर केंद्र का नियंत्रण अतिन्यून था।
साथ ही चोलों की कोई समान वित्तीय पद्धति नहीं थी एवं स्थानीय संस्थाओं ने वह स्थिति उत्पन्न कर दी थी, जिसके कारण सम्राट (राजा) अपनी शक्तियों का केन्द्रीकरण करने में असफल रहे। किन्तु इन तथ्यों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता एवं न ही इन तथ्यों के आधार पर चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है।
चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की सर्वोच्च उपलब्धि इसकी प्रभावी स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली थी। यद्यपि आलोचकों का मानना है कि ग्रामीण स्वायत्त शासन प्रणाली वस्तुतः पांड्य-पल्लव शासन व्यवस्था की देन है।
लेकिन इस प्रमाणिक तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि ग्रामीण स्वायत्त शासन प्रणाली चोल काल में जितनी प्रभावी एवं कार्यक्षम रही, उसने चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को अत्यंत उन्नत दर्जा प्रदान किया।
चोल काल में उर, सभा एवं नगरम जैसे स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का गठन किया जाता था। निचले स्तर पर सत्ता इन संस्थाओं में निहित कर दी जाती थी। सामान्य गांवों में उर नामक संस्था का गठन किया जाता था। इसके सदस्य संबंधित गांव के सभी करदाता पुरुष होते थे। बड़े गांवों में एक से अधिक उर का भी गठन किया जाता था। 1227-1247 के अभिलेखों में दो उरों के गठन की चर्चा की गई है। दूसरी तरफ अग्रहार गांव में सभा या महासभा नामक संस्था गठित की जाती थी। उन क्षेत्रें में जहां व्यापारी निवास करते थे, नगरम जैसी संस्था थी। नगरम ग्रामीण क्षेत्रें एवं नगरों के बीच मध्यस्थ का कार्य भी करते थे। उर एवं सभा नामक संस्थाएं अपने कार्योर्ं का संपादन विभिन्न समितियों के माध्यम से करते थे।
उर नामक संस्था में अलूंग्नम नामक समिति गठित होती थी। समकालीन साक्ष्यों से उर के कार्यसम्पादन पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, परंतु प्रथम के काल के उत्तरमेरूर अभिलेख से सभा के गठन, उसके सदस्यों के चुनाव एवं कार्यप्रणाली पर विशेष प्रकाश पड़ता है। सभा द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जो वरीयम कहलाते थे। इस समिति के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई थी, यथा उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच हो, उसके पास लगभग डेढ़ एकड़ भूमि एवं अपना मकान हो, साथ ही वह वैदिक मंत्रें का ज्ञाता हो। उसी प्रकार कुछ अयोग्यताएं भी निर्धारित की गई थीं। उदाहरण के लिए चोरी, व्याभिचार अथवा वित्तीय अनियमितता में संलिप्त सिद्ध व्यक्ति को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता था। समितियों के सदस्यों का चुनाव लाटरी पद्धति से होता था।
विभिन्न प्रकार की समितियां आवश्यकतानुसार गठित की जाती थीं, जैसे उपवन समिति (तोट्टðा वारियम) एरीवारियम (जलाशय), पनवारियम (स्वर्ण संबंधी समिति) आदि। ‘सभा’ को व्यापक उत्तरदायित्व एवं शक्तियां प्रदान की गई थीं। सभा के निम्नलिखित कार्य थे-
राजा और गांव के मध्य संबंध बनाए रखने के लिए चोल शासकों के अपने सामन्त होते थे। संपूर्ण चोल काल के दौरान ऐसे उदाहरण कम ही प्राप्त होते हैं जब सामंत एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा निरंकुश व्यवहार किया गया हो अथवा स्वायत्त शासन प्रणाली को क्षति पहुंचाई गई हो। रोमिला थापर के अनुसार, ग्राम स्तर पर स्वायत्तता इतनी थी कि प्रशासन के उच्च स्तरों और राजनीतिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन गांव के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे।
इन स्वशासित व्यवस्थाओं में केंद्रीय सत्ता द्वारा असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप होता था। कुल मिलाकर इन ग्राम सभाओं तथा सर्वसाधारण लोगों की उर नामक संस्थाओं को लघु गणतंत्र कहना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। कुल मिलाकर तत्कालीन युग में स्वायत्त शासन की सफल व्यवस्था ही चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की श्रेष्ठता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। आने वाले समय में कभी भी स्वायत्त शासन व्यवस्था इतनी प्रभावशाली नहीं रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया।
वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा स्थानीय एवं ग्रामीण व्यवस्था को स्वायत्तता एवं सुदृढ़ता प्रदान की जा रही है। यह आधुनिक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से चोल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण कर रही है और यह चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के उच्च स्तर का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है।
Question : “हिन्दू और मूसलमान रहस्यवादियों के धार्मिक सिद्धान्त इतने अधिक समान थे कि दोनों धमों के अनुयायियों की समत्वयी गतियों के लिए भूमि परिपक्व थी।” इस बात को स्पष्ट कीजिए।
(2007)
Answer : संतों और सूफियों के प्रयासों से जो भक्ति और सूफी आंदोलन आरंभ हुए उससे मध्य भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में एक नवीन शक्ति एवं गतिशीलता का संचार हुआ। इन दोनों आंदोलनों ने सामाजिक तनाव एवं प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त किया जिसके कारण इस्लाम के साथ सहयोग और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। इस सहयोग और सहिष्णुता के कारण जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई और विचार एवं कर्म के स्तर पर मध्यकालीन भारतीय समाज का उन्नयन हुआ। जहां तक सूफीवाद का संबंध है इसने उन तत्वों को अपनी ओर आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के वाहक के रूप में उभरकर सामने आए। तुर्की आधिपत्य के काल में जब देश का जनजीवन घुटन का अनुभव कर रहा था तो इन सूफियों तथा भक्तों ने सामाजिक संदेश फैलाने एवं सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया।
इतिहासकारों ने जब यह प्रश्न उठाया कि भक्ति आंदोलन पर इस्लाम अथवा सूफी विचारधारा का प्रभाव कहां तक था तो इसके पीछे हिंदू और मुसलमान रहस्यवादियों के धार्मिक सिद्धांतों में समानता ही मुख्य वजह थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि इन दोनों रहस्यवादियों के धार्मिक सिद्धांतों में अनेक तत्व समान थे। ताराचंद, युसूफ हुसैन आदि कुछ इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानंद की भक्ति भावना पर इस्लाम के संपर्क का गहरा प्रभाव था।
हालांकि इतिहासकारों का एक वर्ग इसका विरोध करते हुए यह कहता है कि 12वीं शताब्दी से पहले दो भिन्न संस्कृतियों का संपर्क इतना निकटतम नहीं था कि आध्यात्मिक तौर पर वे एक-दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूफियों एवं संतों में (ये दोनों ही रहस्यवादी थे) बहुत ही समानताएं थी, जैसे-गुरु का महत्व, नाम स्मरण, प्रार्थना, ईश्वर के प्रति प्रेम, व्याकुलता एवं विरह की स्थिति, संसार की क्षणभंगुरता, जीवन की सरलता, सच्ची साधना, मानवता से प्रेम, ईश्वर की एकता और व्यापकता आदि। ये सभी तत्व दोनों ही आंदोलनों का आधार थे।
सूफियों एवं संतों की आस्था धर्म तथा समाज में प्रचलित कर्मकांडों में न होकर ईश्वर के प्रति भावनात्मक प्रेम तथा साधनात्मक रहस्यवाद में थी। अजीज अहमद का मानना है कि सूफीवाद और भक्ति आंदोलन में जो समानताएं हैं, उनके आधार पर एक-दूसरे का प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन के संत नानक और कबीर सूफी विचारों से स्पष्टतः प्रभावित थे। आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के शब्द आज भी सुरक्षित हैं।
सिख धर्म की कई परंपराएं जैसे-गुरुपद का धार्मिक एवं राजनैतिक नेतृत्व से संबंध होना, मसनद की व्यवस्था इत्यादि इस्लाम से स्पष्ट प्रभावित है। कबीर के शब्दावली और उनके द्वारा निर्गुण, निराकार ईश्वर की अराधना आदि पर सूफीवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। भक्ति आंदोलन के संतों और सूफियों के संबंध में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि दोनों ने ही ईश्वरीय प्रेम के द्वारा मानवता का पथ प्रशस्त किया है। भारतीय संस्कृति एवं साधना के संपर्क में आने पर सूफियों ने इस संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण कर लिया। नाथपंथी साधकों, योगियों आदि का प्रभाव तो इन पर जगह-जगह देखा जा सकता है।
भावों के मिश्रण के साथ-साथ उन्होंने भारतीय भाषा एवं बालियों को अपनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा फरीद ने पंजाबी साहित्य को अनूठी देन दी है। कुतुबन मंझन, जायसी तथा नूर मुहम्मद जैसे सूफी कवियों ने अपनी साहित्य के लिए अवधी भाषा को अपनाया। शेख गेसूदराज के समय तक हिंदी कविता, भजन तथा संगीत के मिश्रण से एक नया आकर्षण प्राप्त करती है। बाबा फरीद तथा निजामुद्दीन औलिया का योगियों से संपर्क हमेशा रहा तथा शेख निजामुद्दीन ने योगियों की साधना पद्धति को मुक्त मन से स्वीकार किया। सूफियों ने भारत में धार्मिक उदारता को बढ़ावा दिया और भारत में प्रचलित अनेक हिंदू परंपराओं को इस्लाम में स्वीकृति दिलायी। उन्होंने संगीत को भक्ति के माध्यम के रूप में ग्रहण किया। चिश्ती खानकाहों में नियमित रूप से संगीत सभाओं का आयोजन होता था जिन्हें ‘समा’ कहा जाता था। इन सभाओं में भक्ति भावना से प्रेरित काव्य वाद्ययंत्रें के साथ गाये जाते थे। चूंकि सूफियों पर पहले भी ईरानी संगीत का प्रभाव था, इसलिए भारत में इन संगीत सभाओं के माध्यम से ईरानी राग एवं रागनियों का विस्तार हुआ जिससे भारतीय संगीत प्रभावित हुआ।
भाषा और सूफियों के क्षेत्र में सूफियों ने काफी योगदान किया। सूफियों के खानकाहों में ही उर्दू भाषा का जन्म हुआ। सूफियों को भारत आने पर एक संपर्क भाषा की आवश्यकता थी ताकि वे भारतीय प्रजा के बीच अपने विचारों को प्रचार कर सकें। इस प्रकार आपसी संपर्क और विचारों के आदान-प्रदान से एक ऐसी भाषा विकसित हुई जिसमें अरबी और फारसी के साथ भारतीय भाषाओं के कुछ शब्द मिले हुए हैं। उर्दू भाषा के आरंभिक ग्रंथ भी सुफियों द्वारा ही लिखे गए।
दूसरी तरफ भारतीय भाषाओं में सूफियों की रचनाएं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए शेख अहमद खट्टू ने गुजराती भाषा, कुतुबन, मंझन, जायसी आदि ने अवधी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया। बाबा फरीद, बुल्ले शाह ने पंजाबी भाषा में अपने विचारों का प्रचार किया। इस भाषिक अंतःक्रिया के कारण भारतीय भाषाएं संपन्न हुईं। धार्मिक उदारता के क्षेत्र में इन दोनों रहस्यवादियों ने काफी योगदान किया। सूफियों ने यदि मुस्लिम समाज की रूढि़वादिता तथा कट्टरता को दूर किया तो हिंदू संतों ने यही काम हिंदू समाज के संदर्भ में किया। यह उल्लेखनीय है कि अधिकतर सूफी शासक वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे ताकि शासकों के अत्याचार में साझेदार न समझा जाए। इसके विपरीत सूफी लोग दलित एवं शोषित वर्ग को समर्थन देने में विश्वास रखते थे।
इनका आम जन से संपर्क में हिंदू या मुस्लिम धर्म आड़े नहीं आते थे। इस प्रकार उन्होंने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें सभी मनुष्य समान थे तथा सभी के प्रति उनका व्यवहार एक जैसा था। धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। भक्तिकाल के संतों ने भी इस प्रकार के भेदभाव की तीखी आलोचना की। उन्होंने भी अपने शिष्यों तथा आम जनता के बीच उदार विचारों का प्रचार किया। इससे समाज में सहिष्णुता का वातावरण तैयार हुआ। आगे चलकर अकबर जैसे महान शासक ने इसी सहिष्णुता को अपनी धार्मिक नीति का आधार बनाया। इस प्रकार सूफियों एवं भक्त संतों ने सामाजिक तथा पारस्परिक वैमनस्य को दूर करते हुए आपसी एकता पर जोर दिया। कभी-कभी तो योगियों एवं सूफियों के बीच पारस्परिक शास्त्रर्थ के प्रमाण मिलते हैं।
भारत में खानकाहों एवं संतों का उदार वातावरण हिंदू और मुसलमान दोनों को प्यार देने में सफल रहा तो खानकाहों एवं संतों ने दोनों से प्यार पाने में भी सफल रहे। सूफियों एवं रहस्यवादी संतों ने अहिंसा एवं शांति से भारतीय जनता की समस्याएं सुलझाने का प्रयत्न किया। मध्यकालीन युग में बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बहुत सी बुराईयां उत्पन्न हुईं। अमीर खुसरो तथा बरनी ने जमाखोरी, दास प्रथा, काला बाजारी, शराब, वेश्यावृत्ति आदि अनेक सामाजिक बुराईयों का वर्णन किया है, जो शायद अमीर वर्गों के धन से बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में सूफी संतों एवं हिंदू रहस्यवादियों ने अपने विचारों तथा सादगी पूर्ण जीवन के माध्यम से लोगों को इन बुराईयों से बचने के लिए प्रेरित किया।
इस प्रकार इन रहस्यवादियों ने अपने कार्यों, उपदेशों और विचारों के माध्यम से दो भिन्न सांस्कृतिक आधार वाले समाज के बीच जो विरोध था उसे समाप्त करके ऐसा वातावरण तैयार किया कि दोनों समुदायों ने एक-दूसरे के समाज से बहुत कुछ ग्रहण किया तथा एक समन्वित समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हुए। इसी वातावरण के कारण आगे चलकर इन दोनों महान संस्कृति का प्रभाव भारतीय कला, साहित्य, धर्म, सामाजिक रीति-रिवाज आदि पर दिखाई देता है।Question : बहमनी राज्य।
(2007)
Answer : बहमनी राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में तुगलक साम्राज्य के अवशेषों पर किया गया। मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में निरंतर विद्रोह और अशांति के कारण दक्षिण भारत के तुर्क सरदारों को भी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की प्रेरणा मिली। तुगलक साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए पश्चिम और दक्षिणी प्रांतों में ऐसे सैनिक सरदारों की नियुक्ति की गई थी जो ‘अमीराने सदा’ कहलाते थे। ये लगभग सौ गांवों के समूह के प्रशासक थे। ये पूर्वकालीन इक्त्तेदारों की तरह थे जो राजस्व वसूलने के साथ-साथ सैनिक टुकडि़यां रखते थे तथा स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस प्रकार प्रशासन, वित्त एवं सेना पर इनका पूर्ण अधिकार था। सबसे पहले गुजरात के सदा अमीरों ने विद्रोह किया, जिससे प्रेरणा पाकर दौलताबाद में उसे विशेष सफलता नहीं मिली। बाद में इस्माइल ने जफर खां को सत्ता सौंप दिया, जिसने 1346-47 ई. में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ग्रहण कर स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किया। सत्ता ग्रहण करने के बाद इसने अपने सीमावर्ती क्षेत्रें - कोटगिरी, कल्याणी और बीदर को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। वारंगल के शासक को अपना आधिपत्य स्वीकार करने पर मजबूर किया।
इसने व्यापार तथा वाणिज्य के विकास पर भी ध्यान दिया तथा राज्य के आंतरिक प्रशासन को मजबूत बनाया। इसने हिंदू प्रजा के प्रति उदार नीति का पालन करते हुए जजिया की वसूली पर रोक लगाया।
अपने स्थापना के समय से ही बहमनी राज्य को पड़ोस के शक्तिशाली विजय नगर से संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष दोनों के बीच प्रभुता का था जो भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक कारण से प्रेरित हुआ। इस संघर्ष का अंत 1565 ई. के तालिकोटा के रक्त-रंजित युद्ध के रूप में हुआ, जिसके बाद विजय नगर साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि इस युद्ध के पूर्व ही बहमनी साम्राज्य अपने आंतरिक कलह तथा प्रशासनिक अंतर्विरोधों के कारण पांच राज्यों में विभाजित हो गया था। ये पांच राज्य बीजापुर के आदिलशाही, अहमदनगर के निजामशाही, बरार का इमादशाही, गोलकुंडा का कुतुबशाही तथा बीदर का बरीदशाही थे। बाद में बीजापुर ने बीदर को अपने राज्य में मिला लिया था।
बहमनी राज्य ने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया तथा दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारत तथा विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम के समर्थक बहमनी राज्य में गए। बहमनी के विभिन्न शासकों ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया तथा विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया। हालांकि इस कार्य से सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ लेकिन इन विद्वानों ने मुस्लिम संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया। बहमनी शासकों ने मदरसा, मस्जिदें आदि इमारतों का निर्माण किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में बहमनी राज्य और विशेषकर उसके उत्तराधिकारी राज्य को सबसे महत्वपूर्ण योगदान दक्खिणी हिंदी का विकास है। इस क्षेत्र में गोलकुण्डा का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार बहमनी राज्य ने दक्षिण भारत के राजनीति और संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Question : मराठा
चौथ और सरदेशमुखी
(2007)
Answer : मराठा शासक शिवाजी के शासन काल में मराठा राज्य की आय के दो अन्य स्रोत थेः चौथ तथा सरदेशमुखी।
चौथः चौथ किसी भी क्षेत्र से प्राप्त कुल भूमि आय का एक चौथाई होता था। चौथ उस क्षेत्र से वसूला जाता था, जिस क्षेत्र पर मराठा आक्रमण नहीं करते थे और यदि उस क्षेत्र पर किसी अन्य बाहरी शक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है तो चौथ देने वाले क्षेत्र की रक्षा मराठा सैनिक करते थे। इतिहासकार रानाडे के अनुसार यह ‘सेना के लिए दिया जाने वाला अंशदान मात्र नहीं था। जिसमें कोई नैतिक और कानूनी मान्यता न होती, अपितु बाहृय शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले लिया जाने वाला कर था। दक्षिण के सुल्तानों और मुगलों ने मराठों को अपने इलाकों से ये कर वसूलने का अधिकार दिया था जिसने इस उदीयमान राज्य को बड़ी सीमा तक बैधता प्रदान की थी। चौथ का 3/4 भाग मराठा सरदार ‘सरंजाम’ के रूप में स्वयं के और अपने सैनिकों के खर्च के लिए प्राप्त करते थे।
चौथ का 6 प्रतिशत भाग ‘सहोत्र’ (कर) के रूप में पंत सचिव के लिए सुरक्षित रख लिया जाता था। चौथ का 3 प्रतिशत भाग, जो नादगौंदा कहलाता था, उसे मराठा राजा अपनी इच्छानुसार वितरित करता था। 16 प्रतिशत भाग राजा स्वयं अपने लिए रखता था। इस भाग को पेशवा या ‘प्रतिनिधि’ एकत्र करते थे। इस अधिकार से पेशवा के हाथों में अर्थव्यवस्था का नियंत्रण आ गया। चौथ पहली बार पुरंदर की संधि (1665) के बाद मांगी गयी थी।
सरदेशमुखीः यह कर मराठा राजा को उसके देशस्वामी (देशमुख) होने के नाते दिया जाने वाला एक पुराना कर था। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख और सबसे बड़ा होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार था। कुतुबशाही राज्य (गोलकुंडा) में देशमुख कर वसूलने वाले एक अधिकारी होता था।
सरदेशमुखी 10 प्रतिशत भूमिकर के बराबर होती थी, जिसकी वसूली मराठा शासक स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से करता था। यह कर उन क्षेत्रें पर मराठा राज्य में सम्मिलित कर लिये गये थे। सरदारों द्वारा गुमाश्ता नियुक्त किया जाता था, जो उनके लिए 10 प्रतिशत सरदेशमुखी एकत्रित करता था।
Question : “अकबर ने राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने के द्वारा मुगल साम्राज्य का निर्माण किया था, औरंगजेब ने राजपूतों को अपने से अलग करने के द्वारा उसी को ध्वस्त कर दिया था।” समालोचनात्मक रूप से चर्चा कीजिए।
(2007)
Answer : अकबर ने सिंहासन पर अपने अधिकार को सुदृढ़, स्थिर और प्रारंभिक समस्याओं का समाधान करने के पश्चात अपने साम्राज्य के विस्तार करने की नीति को सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया। उस काल में राजपूत एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। उन्हें अकबर ने उदारनीति के द्वारा अपना सहयोगी बना लिया।
उनके शक्ति एवं सहयोग से अकबर ने न केवल एक विशाल मुगल साम्राज्य का निर्माण किया अपितु परवर्ती काल में मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए उनके सहयोग की भूमिका को सुनिश्चित रूप भी प्रदान किया। मुगल काल में भारत के सशक्त वर्ग राजपूत के साथ मधुर संबंधों की शुरुआत अकबर के शासन काल में हुई। इससे शासक वर्ग के स्तर पर धार्मिक एवं राजनीतिक आधार पर होने वाला संघर्ष कम हो गया। मित्रता एवं सहयोग के युग की शुरुआत हुई जिससे दोनों पक्षों को लाभ हुआ। दिल्ली सल्तनत में पहले से ही भारतीय राजनीति में राजपूतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। अकबर ने राजपूतों की शक्ति के महत्व को समझते हुए राजपूतों को अपने साम्राज्य का सहायक बनाने के उद्देश्य से राजपूतों के प्रति एक सकारात्मक सहयोगी और उदारवादी नीति का अनुपालन किया। इस नीति से राजपूत शासक न केवल उसके समर्थक हो गये, बल्कि मुगल साम्राज्य के विस्तार में भी उन्होंने सक्रिय योगदान किया। राजपूतों के विद्रोह में कमी आने से अकबर का शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। इसलिए वह अपने प्रशासनिक सुधारों पर पर्याप्त समय देकर एक स्थायी साम्राज्य का निर्माण भी कर सका।
अकबर द्वारा सुझायी गयी राजपूत नीति उसके उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां कमोबेश पालन करते रहे। परन्तु औरंगजेब के काल में अकबर द्वारा अपनायी गयी राजपूत नीति में परिवर्तन आ गया। आरंभ में औरंगजेब को भी राजपूतों का सहयोग एवं समर्थन मिल रहा था। औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्ध के समय जसवंत सिंह ने औरंगजेब को सैन्य सहयोग दिया। इसी काल में अंबेर के शासक राजा जयसिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। किन्तु 1679 ई. औरंगजेब को राजपूतों के विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी औरंगजेब की राजपूतों के साथ संबंध समाप्त नहीं हुए थे। परन्तु कटुता जरूर आ गयी थी।
सामान्य धारणा यह है कि औरंगजेब ने धार्मिक बरहता की नीति अपनाकर हिंदू सामंतों और सामान्य प्रजा को अपना विरोधी बना लिया। उसकी धर्मांधता से असंतुष्ट होकर हिंदू विद्रोह और उपद्रव करने लगे। इससे साम्राज्य में अराजकता फैली और इसका पतन अवश्यंभावी था। यह भी कि औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार करने का अनुचित प्रयास किया। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु (1678ई.) के पश्चात मारवाड़ के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप कर औरंगजेब ने राठौर राजपूतों के साथ दुश्मनी मोल ले लिया। उसका राजपूतों से युद्ध भी हुआ। मारवाड़ युद्ध के समय औरंगजेब ने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगाया, तीर्थयात्र कर वसूला तथा मंदिरों को ध्वस्त भी कर दिया। इससे समस्त हिन्दू वर्ग में औरंगजेब के प्रति द्वेष की भावना उभर गयी।
मारवाड़ युद्ध कालांतर में और अधिक फैल गया। मेवाड़ के शासक भी औरंगजेब के विरुद्ध राठौरों के साथ हो गया। राजपूतों ने औरंगजेब के असंतुष्ट तथा विद्रोही पुत्र अकबर को भी सहायता प्रदान की परन्तु औरंगजेब ने कूटनीति के द्वारा इस समस्या को हल कर दिया। उसके समय राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी कायम नहीं हुए। उसने राजपूतों के आपसी वैवाहिक समझौतों में भी हस्तक्षेप किया। परंतु इन सब अवरोधों के बावजूद औरंगजेब के राजपूतों के साथ संबंध समाप्त नहीं हुए थे। मेवाड़ और मारवाड़ से संबंध विच्छेद होने के बावजूद बीकानेर, कोटा, बूंदी आदि राजपूत राज्यों से उसके संबंध बने रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड से भी बहादुरशाह ने संधि कर ली और राजपूतों का सहयोग मुगलों को प्राप्त होता रहा।
फर्रुखशियर के साथ अजीत सिंह की एक बहन का विवाह भी हुआ। अतः यह उचित प्रतीत नहीं होता कि औरंगजेब ने राजपूतों का असयोग खो दिया था और इस कारण साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। वस्तुतः दक्षिण में शिवाजी के दमन हेतु राजा जयसिंह को नियुक्त किया गया और काबुल में उसने अफगान विद्रोह के दमन हेतु जसतंब सिंह को नियुक्त किया गया। लेकिन पूर्व मुगल शासकों के काल की तरह उन्हें ऊंचा मनसब नहीं दिया गया। इस प्रकार औरंगजेब राजपूतों से पूरी तरह विमुख नहीं हुआ था। औरंगजेब के काल तक मुगल उत्तर भारत में मजबूत हो चुके थे तथा अब दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मराठों का सहयोग चाहते थे इसलिए राजपूतों पर विशेष ध्यान नहीं दे सका। उसकी राजपूत नीति में उसकी कट्टरपंथी नीति के अलावा तत्कालीन परिस्थितियों का भी योगदान था, जबकि मनसबों में सर्वाधिक हिन्दुओं की संख्या औरंगजेब के ही काल में थी। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए मूल रूप से आर्थिक एवं जागीरदारी संकट उत्तरदायी थे न कि औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब ने राजपूतों को विमुख करके अपने लिए एक अतिरिक्त समस्या पाल ली। इसलिए उसकी राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के पतन के सहायक कारणों में से एक थी।
Question : दारा शिकोह
(2006)
Answer : शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का जन्म 1615 ई. में हुआ था। मुगलकालीन इतिहास में अपने उदार धार्मिक दृष्टिकोण तथा साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के कारण वह चर्चित रहा। यद्यपि दारा उच्च आदर्शवादी व्यक्ति था, तथापि प्रशासन के निमित्त वह अयोग्य था। वह युवराज था तथा इलाहाबाद, पंजाब एवं मुल्तान जैसे संपन्न प्रांतों का गवर्नर भी रहा। शाहजहां ने उसे 40,000 का मनसब और शाह बुलन्द इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। सिंहासन के समीप एक स्वर्ण कुर्सी पर उसे बैठने की अनुमति थी, परन्तु उसमें सैनिक गुणों तथा राजनीतिक तकनीकों का अभाव था। वह संकल्पशून्य, अहंकारी तथा अव्यावहारिक भी था। उसे शाहजहां तथा कुछ राजपूत सरदारों का समर्थन प्राप्त था, परन्तु धरमट तथा सामूगढ़ की लड़ाइयों में वह औरंगजेब से पराजित हो गया। वह सिंध भाग गया, परन्तु जीवन खां के विश्वासघात के कारण गिरफ्रतार कर लिया गया। अंततः विधर्मी होने के आरोप में औरंगजेब ने उसे मृत्युदंड दे दिया। शासकीय गुणों का अभाव होने के बावजूद दारा एक उदार व प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति था।
वह सर्वेश्वरवादी दर्शन में विश्वास करता था। दारा एक शासक की अपेक्षा विद्वान, कवि और दार्शनिक की भूमिका में उपयुक्त था। उसने अपने ग्रंथ सफीनत-उल-औलिया में विभिन्न परंपराओं के सूफियों का जीवनवृत प्रस्तुत किया है। हिन्दू धर्म में उसे काफी रूचि थी। मजमा-उल-बहरीन (दो समुद्रों का संगम) नामक ग्रंथ में उसे हिन्दू और सूफीमत का तुलनात्मक वर्णन किया है। इसमें हिन्दू-मुस्लिम धर्म में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। 52 उपनिषदों का सिर्र-ए-अकबर नाम से उसने फारसी अनुवाद किया। भागवत गीता और योगवशिष्ठ का भी फारसी अनुवाद उसकी देखरेख में हुआ। वस्तुतः उसने रहस्यवादी संकलन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। वह हिन्दू-मुस्लिम संश्लेषणात्मक संस्कृति तथा समन्वयवादी नीतियों का प्रबल समर्थक था।
Question : अकबर की धार्मिक सहिष्णुता
(2006)
Answer : अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के विकास में उसके पूर्वजों, शिक्षकों, राजपूतों के साथ संबंधों तथा स्वयं उसके व्यक्तित्व का विशेष योगदान रहा। उसने यह चिंतन किया कि धर्म एवं जाति का भेद-भाव किये बिना प्रजा का कल्याण ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। संभवतः इसी से प्रेरित होकर 1562 ई. में उसने युद्धबंदियों को दास बनाने तथा बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार कराने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 1563 ई. में तीर्थयात्र कर तथा 1564 ई. में जजिया कर समाप्त कर दिया। धार्मिक भेद-भाव किये बिना योग्यता के आधार पर लोगों के लिये सेवाओं के द्वार खोल दिये गये।
राजा टोडरमल, भगवानदास, मानसिंह, बीरबल इत्यादि को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किये गये। उसने धार्मिक चर्चा के लिए 1575 ई. में फतेहपुर सीकरी में एक ‘इबादतखाना’ के निर्माण का आदेश दिया। उलेमा के असहिष्णुता से उनके प्रति अकबर की श्रद्धा कम होने लगी। अतः 1578 ई. में इबादतखाना का द्वार सभी के लिए खोल दिया गया। वह ईसाई, जैन, पारसी तथा हिंदू विद्वानों के संपर्क में भी आया। पुरूषोत्तम तथा देवी जैसे हिन्दू धर्मशास्त्रियों के संपर्क में आकर उसने हिंदुओें के कर्म एवं जीवागमन के सिद्धातों में भरपूर विश्वास जताया।
जैन अहिंसा के सिद्धांत से प्रभावित होकर उसने मांस खाना तथा शिकार खेलना छोड़ दिया। विभिन्न धर्मों में सत्यता है और सभी का उद्देश्य एक ही है, ऐसा उसने विश्वास किया। संभवतः वह धार्मिक सहिष्णुता लाकर अपनी प्रशासनिक एवं राजनीतिक पकड़ मजबूत भी करना चाहता था। उसने कुछ कुप्रथाओं पर रोक भी लगाई। दी-ए-इलाही में उसने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया।
संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए उसने अन्य धर्म के लोगों को भी उच्च पद प्रदान किया, कुछ धार्मिक करों से मुक्त कर दिया, अन्य धर्म के अपनी पत्नियों को राजमहल में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी, सभी धर्मावलम्बियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया तथा दीन-ए-इलाही में विभिन्न धर्माें के मूल सिद्धांत को अपना लिया। उसी इस नीति का उद्देश्य सुलहेकुल (सबके लिए शांति) था।
Question : उत्तरी भारत में सूफीवाद
(2006)
Answer : सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सफा से हुई है, जिसका अर्थ पवित्रता है। अर्थात् जो लोग आध्यात्मिक रूप से तथा आचार-विचार से पवित्र थे, वे सूफी कहलाए। सूफीवाद इस्लाम में रहस्यवादी विचारों और उदार प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है।
उत्तरी भारत में सूफीवाद का प्रारंभ मुख्यतः ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर में आकर बसने के साथ होता है। इनके अनेक अनुयायी बने, जिन्होंने चिश्ती सिलसिले को उत्तरी भारत में प्रमुखता प्रदान की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में, फरीद ने पंजाब में तथा निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में अपना खानकाह बनाया। चिश्ती संत अत्यंत उदार थे। उन्होंने शासक वर्ग से यहां अपने-आप को दूर रखा तथा समा (संगीत-सभा) का आयोजन किया।
सुहारावर्दी सम्प्रदाय के प्रमुख संत शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। इनका प्रभाव मुख्यतः सिंध, पंजाब एवं गुजरात में था। इनके अनुयायी पूर्वी भारत, बंगाल तथा बिहार में भी थे। बिहार में सुहारावर्दी सम्प्रदाय के फिरदौसी शाखा का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त कादिरी, नक्शबंदी, सत्तारी आदि सम्प्रदायों ने भी उत्तरी भारत में अपना खानकाह स्थापित किया था। उत्तरी भारत में सूफीवाद का व्यापक प्रचार तथा प्रसार हुआ। सूफी सन्तों ने सामाजिक तथा पारस्परिक वैमनस्य को दूर करते हुए आपसी एकता पर जोर दिया। इन्होंने उत्तरी भारत में शासक वर्ग के नीतियों को प्रभावित किया। उत्तरी भारत में प्रचलित हिन्दू परम्पराओं को इस्लाम में स्वीकृति सूफियों ने ही दिलाई। विशेषकर उत्तरी भारत में सूफीवाद तथा भक्ति-आंदोलन ने मिलकर हिन्दू-मुस्लिम सामंजस्य उत्पन्न किया। सूफीवाद ने उत्तर भारत में क्षेत्रीय भाषा, संगीत, साहित्य आदि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तरी भारत के शासक वर्ग भी उनके उदार विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।
Question : मुगलकाल में साहित्य के विकास पर संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
(2006)
Answer : मुगल बादशाहों ने साहित्य की विभिन्न शाखाओं के विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया। तैमूरी बादशाह विद्वानों के पोषक तो थे ही, स्वयं भी साहित्य-सर्जन करते थे। यही कारण है कि मुगलकाल में फारसी, तुर्की, संस्कृत, हिन्दी, बंगला और पंजाबी साहित्य का विकास हुआ।
तुर्की और फारसी साहित्यः बाबर अपनी मातृ भाषा तुर्की के साथ-साथ फारसी भाषा का भी एक उच्च कोटि का कवि एवं लेखक था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा की रचना की जो ‘तुजके-बाबरी’ या ‘बाबरनामा’ के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक उच्च कोटि की रचना है। उसने फारसी में एक नई शैली (मुजरियान या बाबरी शैली) का आविष्कार किया।
बाबर के साथ अब्दुल वाहिद फारीगी, नादिर समरकन्दी, ताहिर ख्वान्दी आदि कवि एवं मिर्जा हैदर दौगलत एवं जैनुल-आबिदीन ख्वाफी आदि इतिहासकार भारत आए।
दौगलत ने तारीखे-रशीदी की रचना की। हुमायूं पुस्तकों का प्रेमी था। उसकी मृत्यु भी पुस्तकालय के सीढि़यों से गिरकर हुई थी। खोंदमीर, अब्दुल लतीफ और शेख हुसैन जैसे विद्वानों को उसने संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिया। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी में हुमायूंनामा की रचना की।
खोंदमीर ने ‘कानूने हुमायूंनी’ की रचना की। खोंदमीर को हुमायूं ने ‘अमीरे अख्बार’ की उपाधि प्रदान की थी। जौहर आफतावची ने ‘तजकिरातुल वाकियात’ की रचना की। अकबर का काल शांति और समृद्धि का काल था, जिसके कारण साहित्य को विकास का अवसर प्राप्त हुआ।
अकबर के समय के फारसी साहित्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है। (i) ऐतिहासिक साहित्य (ii) अनुदित साहित्य (iii) काव्य और पद्य। आइने-अकबरी या अकबरनामा, अकबर के समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना अबुलफजल ने की। वह एक विद्वान, निबन्धकार, कवि, समालोचक और इतिहासकार भी था। उसके अनुसार अकबर के दरबार में 59 कवि थे। इनमें से अनेक ने अपने ‘दीवान’ पूरे कर लिए थे।
मुल्ला दाउद द्वारा अकबरनामा, अब्बास खां शेरवानी द्वारा तोहफा-ए-अकबरीशाही या तारीखे-शेरशाही आदि अनेक ग्रंथों की रचना अकबर के काल में हुई। संस्कृत एवं अन्य भाषाओं की अनेक पुस्तकों का इस काल में फारसी में अनुवाद किया गया। महाभारत का अनुवाद ‘रज्मनामा’ के नाम से किया गया।
बदायूंनी ने रामायण का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का, हाजी सरहिन्दी ने अथर्ववेद का, मुक्कमल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक तजक का तथा मौलाना शाह मुहम्मद शाहाबादी ने कश्मीर के इतिहास का फारसी अनुवाद किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद ‘अनवर-ए-सुहेली’ के नाम से किया। पद्य लिखने वालों में गिजाली तथा फैजी का नाम सर्वप्रथम है। निशापुर का मुहम्मद हुसैन नाजिरी ग़ज़लें लिखता था।
अब्दुर्रहीम खानखाना भी फारसी में रचना करते थे। जहांगीर स्वयं उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा ‘तुजके-जहांगीरी’ के नाम से फारसी में लिखी, जिसमें अपने शासनकाल के 17 वर्षों तक का इतिहास उसने प्रस्तुत किया है। मुतमिद खां ने‘इकबालनामा-ए-जहांगीरी’ की रचना की। शाहजहां ने ‘कलीम’ को राजकवि नियुक्त किया। चन्द्रभान ब्राह्मण पहला हिन्दू कवि था, जिसने अबुल फजल की शैली को समन्वित कर एक नई शैली प्रस्तुत की। चन्द्रभान एक गद्य लेखक भी था।
उसने ‘चार चमन’ की रचना की। कजवीनी की पादशाहनामा, इनायत खां की शाहजहांनामा, मोहम्मद सालेह की अमले-सालेह, सादिक खां की शाहजहांनामा आदि शाहजहां के काल की ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। दारा शिकोह ने सफीनत-उल-औलिया, सकीनत-उल-औलिया तथा मज्म-उल-बहरीन नामक सूफी तथा दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। औरंगजेब मुस्लिम धर्मशास्त्र तथा न्यायशास्त्र का ज्ञाता था। उसके आदेश पर उलेमाओं ने ‘फतवा-ए-आलमगीरी’ नामक इस्लामी कानून ग्रंथ की रचना की।
यद्यपि कविता तथा इतिहास लेखन में औरंगजेब की रुचि नहीं थी, फिर भी साकी मुस्तइद खां की मुआसिरे आलमगीरी, ईश्वरदास नागर की ‘फतुहाते-आलमगीरी, भीमसेन कायस्थ की’ नुस्खा-ए-दिलकुशां’, खाफी खां की गुप्त रूप से लिखी गई मुन्तखाब-उल-लुवाब तथा औरंगजेब के काल के सरकारी इतिहासकार काजिम शिराजी की आलमगीरनामा इस काल की प्रमुख ऐतिहासिक रचनाएं हैं। मुहम्मदशाह की मृत्यु के बाद फारसी का स्थान उर्दू ने ग्रहण कर लिया तथा फारसी का विकास अवरूद्ध हो गया।
हिन्दी साहित्यः मुगलकाल में हिन्दी साहित्य का विकास तीव्र गति से हुआ। अकबर के काल को हिन्दी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। इस काल में तुलसी, सूर, रहीम, रसखान तथा बीरबल जैसे कवियों का आविर्भाव हुआ। इनकी कृतियां शैली, माधुर्य, ग्राह्यता तथा सहजता के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट हैं। उस समय का अधिकतर काव्य-साहित्य धार्मिक (भक्ति-साहित्य) था तथा रामभक्ति एवं कृष्ण-पूजा की व्याख्या करता था। रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास का यद्यपि अकबर से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था तथापि वे उस युग की विभूति थे। उनकी 25 अन्य कृतियां हैं।
ब्रजभाषा के कवि सूरदास बालवर्णन में सर्वाधिक प्रवीण थे। उन्होंने सूर-सागर, सूर सरावली एवं साहित्य लहरी की रचना की। जायसी का दार्शनिक महाकाव्य पद्मावत भी इसी काल की रचना है। बीरबल को अकबर ने ‘कविप्रिय’ की उपाधि प्रदान की थी। मानसिंह विद्या का पोषक था तथा पद्य रचना करता था। हिन्दी पर सिर्फ हिन्दुओं का ही नहीं, बल्कि मुसलमानों का भी सम्यक् अधिकार था। रहीम के दोहे तथा रसखान की प्रेमवाटिका इसके प्रमाण हैं। जहांगीर ने भी हिन्दी साहित्य के तत्कालीन विभूतियों राममनोहर लाल, किशनदास, जद्रुप गोसाई, बूटा तथा वृक्षराज को संरक्षण प्रदान किया।
जहांगीर का भाई दानियाल हिन्दी का एक अच्छा कवि था। शाहजहां का काल रीतिकाल का शैशवकाल कहा जा सकता है। चिंतामणि, सुन्दर कविराय तथा कविन्द्राचार्य ने मिलकर ‘कवीन्द्र कल्पतरू’ नामक मिश्रित काव्य में सम्राट की प्रशस्ति लिखी। बिहारी, दादू तथा कवि-प्रिया एवं अलंकार मंजरी के रचयिता केशव शाहजहां काल के कवि थे, यद्यपि औरंगजेब ने हिन्दी के विकास में रूचि नहीं ली, तथापि भूषण, मतिराम तथा वृन्द उसके काल के प्रमुख कवि हैं। 18वीं सदी में पर्याप्त संरक्षण के अभाव में हिन्दी का विकास अवरुद्ध हो गया।
संस्कृत साहित्यः अकबर के समय महेश ने संस्कृत में अकबर कालीन इतिहास को लेखबद्ध किया। पद्यसुन्दर जैन ने ‘अकबरशाही शृंगार दर्पण’ तथा सिद्धिचन्द्र ने ‘भानुचन्द्र चरित्र’ नामक ग्रंथ की रचना की। ‘फारसी-प्रकाश’ नामक फारसी-संस्कृत शब्दकोष का संकलन किया गया। शाहजहां के दरबारी कवि जगन्नाथ ने ‘रस गंगाधर’ तथा ‘गंगालहरी’ की रचना की। औरंगजेब के समय हिन्दू राजाओं ने संस्कृत को प्रोत्साहन दिया।
उर्दू साहित्यः बाबर ने तुजके-बाबरी में हिन्दवी अर्थात् उर्दू शब्दों का प्रयोग किया। अकबर के काल में रेख्ता (उर्दू) बोलचाल की सीमा को पार कर भाषा की सीमा में प्रविष्ट कर चुकी थी। शाहजहां तथा औरंगजेब के काल में उर्दू शायरी की परम्परा का उत्तरोत्तर विकास हुआ। शाहजहां के चन्द्रभान ब्राह्मण तथा अब्दुल गनी कश्मीरी ने उर्दू कविता के विकास में योगदान दिया।
‘आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता’ वली दकनी 1700 ई- में दिल्ली आए, जहां प्रसिद्ध सूफी कवि शाह शादुल्ला ‘गुलशन’ से उनकी मुलाकात हुई। उनके निर्देशों का पालन कर वली ने एक दीवान (पद्य-संग्रह) की रचना की। मुहम्मदशाह के निमंत्रण पर 1772 ई- में वली पुनः दिल्ली पधारे, जहां अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर उन्हें विशेष ख्याति मिली। आबरू, मीरदर्द, सौदा महजर जाने जाना और आरजू ने वली के मार्ग पर चलकर उर्दू साहित्य को समृद्ध बनाया।
Question : 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापार के प्रारंभ एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए।
(2006)
Answer : प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध रहे थे। 1453 ई. में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों द्वारा अधिकार स्थापित कर लेने से यूरोपी देशों को एशियाई व्यापारिक माल मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। यूरोप के अनेक देश अब स्थलमार्ग की अपेक्षा भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। वास्कोडिगामा 1498 ई- में आशा अंतरीप के रास्ते अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचने में सफल हुआ।
पुर्तगाल में वास्कोडिगामा द्वारा लाया गया माल सारे अभियान के व्यय से साठ गुणा अधिक मूल्य पर बिका। इसके पूर्व यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार था और वे पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्रों, खासकर स्पेन और पुर्तगाल को पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे।
15वीं सदी में जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए नए समुद्री मार्गों की खोज ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना भर दी थी। कुतुबनुमा का भी आविष्कार हो चुका था।
16वीं 17वीं सदी के दौरान यूरोपीय व्यापार के प्रारंभ तथा विकास में इस नए व्यापारिक मार्ग ने जिसकी खोज वास्कोडिगामा ने की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।
यूरोपीय शक्तियों की नौसैनिक उत्कृष्टता ने एशियाई सामुद्रिक शक्ति को पीछे छोड़ दिया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी नौसैनिक क्षेत्र में एशियाई शक्तियों से श्रेष्ठ थे। फलतः हिन्द महासागर के व्यापरिक गतिविधियों पर यूरोपीयों का अधिकार स्थापित हो गया।
यह एक महत्वपूर्ण कारक था- 16वीं17वीं सदी में भारत में यूरोपीय व्यापार के प्रारंभ तथा विकास के लिए। यूरोप में मसालों की मांग निरंतर रहती थी। शीतकाल में चारे के अभाव में बड़ी संख्या में पशुओं को मारकर उनके मांस पर नमक लगाकर सुरक्षित कर लिया जाता था, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। भारतीय मसालों को प्राप्त करने की होड़ ने यूरोपीयों को व्यापार के लिए आकृष्ट किया।
अत्यधिक लाभांश प्राप्ति की उम्मीदों न भी यूरोपीय व्यापार के प्रारंभ तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17वीं सदी के आरंभ में अनेक व्यापारिक कम्पनियों का जन्म हुआ। अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनी (1600 ई.), डचों द्वारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पनी (1602 ई.) स्थापित की गई और बाद में फ्रांसीसियों द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनी (1964 ई.) की स्थापना ने यूरोपीय व्यापार के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।
16वीं-17वीं सदी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापार के प्रारंभ तथा विकास के लिए राज्य संरक्षण भी उत्तरदायी था। शासक वर्ग को व्यापारियों से कर के रूप में पर्याप्त धन प्राप्त होता था, जिसके बदले व्यापारी वर्ग तथा कम्पनियों को राज्य सुरक्षा प्रदान करती थी।
यूरोप तथा एशिया के बीच इसी व्यापारिक प्रणाली के अंतर्गत ही पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। पुर्तगालियों ने व्यापारिक व राजनीति प्रभुत्व स्थापित करने के साथ-साथ पोप से एक विशेष विज्ञप्ति जारी कर सभी नई खोजों व विजित प्रदेशों का स्वामित्व हासिल किया। आरंभ में पुर्तगालियों ने लाल सागर व भारतीय तटों के बीच चलने वाले जहाजों को अपनी लूट का शिकार बनाया, परंतु बाद में एक नियोजित ढंग से लाइसेंस प्रथा प्रारंभ करके अन्य देशों के जहाजों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यहां तक कि भारतीय शासकों के जहाज भी, अब बिना पुर्तगाली लाइसेंस के समुद्र में नहीं उतर सकते थे।
पुर्तगालियों ने हिन्द महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। अपनी कार्ट्ज-आर्मेडा-काफिला व्यवस्था द्वारा उन्होंने भारतीय व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। उनका मुख्य साधन था- कार्ट्ज या परमिट, जिसके पीछे आर्मडा का बल होता था। इस व्यवस्था ने यूरोपीय व्यापार के प्रारंभ तथा विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया तथा एशियाई व्यापारियों को हतोत्साहित किया।
भारत के बन्दरगाह नगरों पर यूरोपीय नियंत्रण से भी यूरोपीय व्यापार फला-फूला। 1530 ई. में गोआ भारत में पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी हो गई। 1535 ई. में दीव पर व 1559 ई. में दमन पर भी उनका अधिकार हो गया। इसके पूर्व 1503 ई. में कोचीन में उन्होंने एक छोटा-सा दुर्ग बनाया, जो भारत में उनका पहला दुर्ग था।
आरंभ से ही बल प्रयोग तथा दुर्गीकरण द्वारा यूरोपीय कम्पनियों ने भारत में यूरोपीय व्यापार को सुदृढ़ किया। पुर्तगालियों के नक्शेकदम पर चलते हुए डचों, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने भी अपने फैक्ट्रियों को दुर्गीकृत किया। दुर्गीकरण से यूरोपीय व्यापार को सुरक्षा प्राप्त हुई। व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए कम्पनियों ने बल का भी प्रयोग किया। व्यापार के विकास के लिए कम्पनियों ने अपनी चतुर कूटनीति का भी सहारा लिया। समय-समय पर भारतीय शासकों के समक्ष दूत भेजकर कम्पनी ने रियायतें प्राप्त कीं। पुर्तगालियों ने कोचीन एवं कालीकट के राजाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देकर कोचीन को अपना अधीनस्थ बना लिया।
अंग्रेजों ने हाकिंग्स तथा टामस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा तथा अनेक शासकों से भी रियायतें प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस चतुर कूटनीति से उन्होंने व्यापारिक फैक्ट्रियों का निर्माण भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर किया। अंततः किलेबन्दी तथा बल प्रयोग से इसे सुदृढ़ किया।
तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दुर्व्यवस्था ने कंपनी को राज्य विस्तार के लिए प्रेरित किया। अनेक महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्रें पर अधिकार कर लेने से यूरोपीय कम्पनियों को व्यापार के लिए आवश्यक माल सस्ता व सरलता से उपलब्ध होने लगा। उदाहरणार्थ बंगाल ने ब्रिटिश कम्पनी के व्यापार को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र-विजय से जुड़ जाने के बाद कम्पनियों को अधिकाधिक धन की आवश्यकता हुई।
सोलहवीं सदी में उत्तर भारत में मुगलों का शासन था। मुगल बादशाहों ने सुदृढ़ नौसेना निर्माण पर बल नहीं दिया तथा समुद्री व्यापार में उनकी विशेष रूचि नहीं थी।
इससे विदेशी शक्तियों को अरब सागर के व्यापार पर नियंत्रण का अवसर भी प्राप्त हो गया। पुर्तगाली व्यापार के फलते-फूलते रूप को देखकर अन्य यूरोपीय देश भी आकर्षित हुए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंततः नौसैनिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्कृष्ट ब्रिटिश कम्पनी ने भारत में यूरोपीय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया।
Question : खिलजी क्रांति
(2006)
Answer : सामान्यतः खिलजियों द्वारा सत्ता पर नियंत्रण, तुर्की शासन की समाप्ति, एक नए शासन की शुरुआत तथा प्रतिष्ठित इल्बरी वंश की समाप्ति को खिलजी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। यह इस मिथ्या धारणा की समाप्ति से संबंधित है कि राज्य पर केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का ही एकाधिकार है। खिलजी क्रांति ने शाही रक्त की तुलना में सर्वसाधारण के जनमत का आधिपत्य स्थापित किया। यह शासक वर्ग के सामाजिक आधार के विस्तार को प्रदर्शित करता है। शासन में गैर तुर्कों का सम्मिलित होना इस विस्तार को दर्शाता है। तात्कालिक अर्थों में यह सैन्यवाद को प्रोत्साहन देने का परिचायक है, अर्थात् राजव्यवस्था में नागरिक पहलू के स्थान पर सैनिक पहलू पर बल प्रदान करने से संबंधित है।
वास्तव में खिलजी क्रांति उदारवादी राज्य की दिशा में एक प्रयास था। इसने इस बात को साबित किया कि धार्मिक समर्थन के बिना राज्य न केवल जीवित रह सकता है, बल्कि सफलतापूर्वक कार्य भी कर सकता है। खिलजियों ने धर्म को राजनीति से अलग रखने का प्रयास भी किया। वृहत् अर्थों में यह अलाउद्दीन के द्वारा लाए गए परिवर्तनों का भी द्योतक है। इसमें राज्यहितों को सर्वोपरि समझा गया है। अनवरत विजयों, कूटनीति में असाधारण प्रयोगों, देश के सुदूरतम भागों में मुस्लिम सेनाओं के प्रवेश, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, नवीन आर्थिक प्रयोगों, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि से खिलजी क्रांति संबंधित है। अनेक आकस्मिक वंशीय क्रांतियों के कारण सत्ता का हस्तांतरण जनसाधारण के लिए अधिक महत्व का नहीं था, परंतु खिलजी क्रांति के दूरगामी परिणाम हुए। खिलजी विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि जातीय निरंकुशता और अधिक समय तक राज्य नहीं कर सकती। खिलजी क्रांति योग्यता को महत्व प्रदान करने से भी संबंधित है। इसने जनमत की शक्ति को भी प्रदर्शित किया है, क्योंकि जनसाधारण के भय से जलालुद्दीन एक लम्बे समय तक दिल्ली में आने का साहस नहीं कर पाया।
Question : तुर्क-अफगान काल के दौरान दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक तंत्र के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए।
(2006)
Answer : हिन्दुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की नींव तुर्की शासकों द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण करने के साथ शुरू होती है। सुल्तान राजनीतिक तथा धार्मिक मामलों दोनों का श्रेष्ठ अधिपति है। राज्य की सम्पूर्ण शक्तियां उसके हाथ में संकेन्द्रित थीं। यद्यपि इस्लामी राजसत्ता का रूप लोकतांत्रिक था, परन्तु तुर्क-अफगान काल में प्रशासनिक-तंत्र परिस्थितियों के कारण केन्द्रीकृत था।
सिद्धान्ततः धर्मिक मामलों में उसकी शक्ति कुरान के पवित्र कानून द्वारा सीमित थी, परन्तु व्यावहारिक रूप में तुर्क अफगान शासकों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। केन्द्रीय शासन में सर्वाधिक प्रभाव सुल्तान के व्यक्तित्व का पड़ता था। इस काल में आधुनिक काल की तरह कोई नियमित मंत्रिपरिषद् नहीं थी। शासन में सुल्तान की सहायता करने के लिए मंत्री होते थे, जिनकी नियुक्ति सुल्तान के इच्छानुसार होती थी। ये मंत्री सुल्तान को सिर्फ सलाह दे सकते थे, किन्तु सुल्तान की नीति को प्रभावित नहीं कर सकते थे। यद्यपि निर्बल शासकों के समय अमीर वर्ग का प्रभाव सुल्तान पर रहा, किन्तु अलाउद्दीन जैसे शक्तिशाली सुल्तान ने अमीर और उलेमा दोनों पर अंकुश लगा रखा था। इस निरंकुश राज्य शासन तंत्र में परामर्शदात्री सभा को मजलिस-ए-खलवत कहा गया।
केन्द्रीय सरकार में सर्वोच्च अधिकारी को वजीर कहा जाता था, जिसके नियंत्रण में राज्य के अन्य विभाग भी थे। वजीर राज्य के चार स्तम्भों अर्थात् वजीर, आरिजे मुमालिक, दीवाने इंशा तथा दीवाने रसालत में से एक था, किन्तु अन्य मंत्रियों से उसका पद थोड़ा ऊंचा था। प्रारंभ में वजीर का पद उतना महत्वपूर्ण नहीं था। परन्तु, इल्तुतमिश के समय वित्त और सैनिक दोनों कार्य वजीर करता था, परन्तु बलवन के समय वजीर की शक्तियां निम्नतम बिंदु पर जा पहुंची थीं।
तुगलक काल ‘विजारत का स्वर्णकाल’ था, जबकि अफगानों के अधीन वजीर का पद अप्रसिद्ध हो गया। वजीर का कार्यालय दीवाने-विजारत कहलाता था। नायब वजीर, मुशरिफ (महालेखाकार) तथा मुस्तौफी (महालेखा परीक्षक) वजीर के नीचे कार्य करते थे। केन्द्रीय प्रशासन में दीवान-ए-मुमालिक सैनिक विभाग का प्रधान दीवान-ए-इंशा शाही पत्र-व्यवहार का प्रधान, दीवान-ए-रसालत विदेश मंत्री, वकील-ए-दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधकर्ता था। व्यय के कागजातों की देखभाल के लिए जलालुद्दीन द्वारा दीवान-ए-वकूफ, बकाया कर वसूली के लिए अलाउद्दीन द्वारा दीवान-ए-मुस्तखराज तथा कृषि विभाग की देखरेख के लिए मु- तुगलक द्वारा दीवाने-ए-अमीरकोही आदि पदों का सृजन केन्द्रीय प्रशासनिक तंत्र में किया गया।
न्याय का प्रमुख काजी-उल-कुजात था, जिसे कानून की व्याख्या में मुफ्रती सहायता करता था। कानून कुरान के आदेशों पर आधारित था, यद्यपि अलाउद्दीन तथा मुहम्मद तुगलक जैसे शासक न्याय करने में नीति का विचार करते थे। मुहतासिब लोगों के आचरण पर नजर रखता था। कोतवाल शान्ति-व्यवस्था का संरक्षक था। दण्ड विधान कठोर था। अपराध स्वीकार करने के लिए यातना दी जाती थी। इस काल में न्याय प्रशासन व्यवस्था व्यवस्थित नहीं मालूम होता है। तुर्क-अफगान काल में प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा भाग कर वसूली से जुड़ा हुआ था। खिराज़, खुम्स, ज़जिया, जकात आदि करों को एकत्र करने के लिए विभिन्न विभागों तथा पदों का सृजन हुआ। अक्ता एक महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसका इस काल के प्रशासनिक तंत्र में विशेष महत्व था। अक्ता प्राप्त करने वाले को मुक्ता कहा जाता था। अक्ता के प्रशासकीय ढांचे के अन्तर्गत किसी क्षे से स्थायी संबंध न होते हुए भी शासक वर्ग के लिए वहां से आय की व्यवस्था हो जाती थी।
साथ ही यह प्रणाली शासक वर्ग की सामाजिक स्थिति तथा उनके राजनीतिक प्रभाव निर्धारण का आधार भी बनी रहती थी। तुर्की शासक वर्ग की धन लिप्सा की तुष्टि के साथ-साथ इक्ता व्यवस्था से नए प्रदेशों में कानून तथा व्यवस्था की स्थापना के साथ ही राजस्व वसूली की आवश्यक समस्या का समाधान भी हुआ। मुक्ता या बली, खराज व अन्य कर वसूल करके अपना तथा अपने सैनिकों का भरण-पोषण करते थे और बची हुई राशि सुल्तान के कोष में भेज देते थे। इस प्रकार उपलब्ध विपुल राजस्व के कारण ही मुस्लिम राज्य बड़ी सेना रखने में समर्थ हुए तथा इन राज्यों में अनेक नगरों का विकास हुआ। लोदी काल में मुक्ता को वजहदार कहा जाने लगा। तुर्की प्रशासन में सैनिक संगठन का विशेष महत्व था। सल्तनत की सेना को हश्म-ए-कल्ब या कल्ब-ए-सुल्तानी कहा जाता था। सैन्य संगठन में दासों का महत्वपूर्ण स्थान था। प्रांतीय सेना हश्म-ए-अतरफ कही जाती थी। सेना का कोई स्थायी सेनापति न था। सुल्तान ही मुख्य सेनापति होता था तथा नायब या मलिक नायब उसकी सहायता करता था। समय-समय पर सुल्तान विभिन्न आक्रमणों के लिए सेनापति स्वयं नियुक्त करता था।
सेनापति की नियुक्ति केवल विशिष्ट समय तक ही होती थी। सल्तनत के सैन्य संगठन में अमीर-ए-आखूर का विशेष महत्व था। वह अश्वशाला अध्यक्ष था। हाथियों से सम्बन्धित विभाग शहना-ए-पील के अधीन था। सैनिक प्रशासन में किलों की सुरक्षा का भार कोतवाल के पास था। नावों की बेड़ा का अध्यक्ष अमीर-ए-बहरी कहलाता था। तुर्क-अफगान काल में प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का प्रतिरूप था। प्रांतपति प्रांतीय शासन का केन्द्र था। उसे वल कहा जाता था।
प्रांत कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा था, जो मुक्तों या आमिलों के अधीन था। जिले को शिक कहा जाता था। शिकदार उसका अध्यक्ष होता था। जिले परगनों में विभाजित थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव मुकद्दम, खोत या चौधरी के अधीन होता था। प्रांतीय कानून-व्यवस्था, सेना का प्रबंध, कर-वसूली एवं न्याय-व्यवस्था प्रांतपति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते थे। प्रांतपति अपने कार्यों के संबंध में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय न्यायपालिका में चार प्रकार के न्यायालय थे-वल, काजी-ए-सूबा, दीवान-ए-सूबा तथा सद्र-ए-सूबा। राज्य के कर्मचारी लोगों के आम जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे। ग्राम-पंचायत अपना शासन करने में पूर्ण स्वतंत्र थी। सल्तनतकालीन शासन-प्रबंध तथा शासकों के प्रशासकीय दृष्टिकोण में निरंतर प्रगति होती रही।
भारत के तुर्क-अफगान प्रशासकों ने प्रशासन के कार्यों में हिन्दुओं की योग्यता को भी पहचाना। करों की वसूली से संबंधित अपनी समझ के कारण भूमिकर विभाग अधिकतर हिन्दू अधिकारियों के ही हाथ लगे। मुस्लिम सरदारों का राज्य में सेनापतियों, शासकों तथा कभी-कभी राजा बनाने वालों के रूप में बहुत प्रभाव था।
शासक वर्ग तथा जनसमुदाय के बीच पारस्परिक प्रेम के बन्धन का अभाव था। राज्य तंत्र सैनिक शक्ति पर विकसित हुआ। सरदार बिना किसी स्थिर नीति के स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे। जब सुल्तान पर्याप्त शक्ति रखने में विफल हो गये तथा सरदार अधिक महत्वाकांक्षी एवं उपद्रवी बन गये, तब इसका पतन अनिवार्य हो गया।
Question : मुगल चित्रकला
(2005)
Answer : भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली, वह एक उन्नतिशील एवं शक्तिशाली कला आंदोलन के रूप में विकसित हुई। हालांकि मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी लेकिन मुगल चित्रकला का विकास हुमायूं के समय आरंभ हुआ, जब हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर ईरान में निवास कर रहा था।उसी समय ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अबदुस्समद की सेवाएं प्राप्त हुईं। ये दोनों चित्रकार हुमायूं की अस्थाई राजधानी काबुल में काम शुरू किये। बाद में जब हुमायूं दिल्ली को जीता तो ये दोनों कलाकार दिल्ली आ गए। इन परिस्थितियों में मुगल चित्रकला पर ईरानी प्रभाव का होना स्वाभाविक था। हालांकि सल्तनत काल में ही ईरानी कला का प्रभाव भारत में महसूस किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय चित्रकार जहां अधिकतर धार्मिक विषयों का चित्रण करते थे, वहीं ईरानी चित्रकारों ने राजदरबार के जीवन, युद्ध के दृश्य आदि का चित्रण किया। मुगल चित्रकला के आरंभिक काल से ही ईरानियों के विषय और विधि का प्रभाव तो पड़ा ही, इसके अलावा चित्रण में भी ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से था। फूल-पौधे और पशु-पक्षी, वेश-भूषा आदि सभी पर ईरानी प्रभाव था।
अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने नया रूप धारण किया उस पर भारतीय प्रभाव की झलक मिलती है। चूंकि अकबर ने भारत में समन्वित संस्कृति के विकास की नीति अपनायी। उदार धार्मिक नीति, राजपूतों से मित्रता तथा विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों के भौगोलिक प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं एक-दूसरे के संपर्क में आईं। विशेषकर राजपूत चित्रकला ने मुगल शैली को प्रभावित किया। इनकी प्रमुख विशेषताओं यथा गोल ब्रश का प्रयोग गहरे नीले और गहरे लाल रंग का अधिक प्रयोग आदि का समावेश मुगल चित्रों में देखी जा सकती है। इसके अलावा लोगों के चेहरे, रंग-रूप, वेश-भूषा, फूल-पौधे, पशु-पक्षी इत्यादि अब भारतीय हैं न कि ईरानी। राजपूत शैली का इतना अधिक प्रभाव अकबर द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय चित्रकारों को नियुक्त करने के कारण हुआ। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में दसवंत एवं बसावन को नाम उल्लेखनीय हैं। इसी समय पुर्तगालियों के माध्यम से यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूना अकबर के दरबार में पहुंचा, जिससे मुगल शैली पर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी पड़ा। मुगल चित्रकारों ने व्यक्ति विशेष के चित्र बनाने तथा अग्रसंक्षेपण की विशेषता यूरोपीय चित्रकला से ग्रहण किया। इस प्रकार अकबर के काल में मुगल चित्रकला में विभिन्न शैलियों का मिश्रण हुआ तथा एक नई और अधिक समुन्नत शैली का विकास हुआ।
जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। इस समय हम दो नई विशेषताओं को देखते हैं। पहली मोरक्का के रूप में है। इसमें चित्रों का संकलन एक जगह, पक्षियों का एक जगह तथा फूलों का एक जगह संकलन इत्यादि। दूसरी विशेषताकमबवतंजमक उंतहपदे के रूप में मिलती है। जहांगीर को चित्रों का बड़ा पारखी भी माना जाता है।
चित्रकारी की यह परंपरा शाहजहां के समय भी जारी रही। परंतु इसे हम चित्रकला के दृष्टिकोण से शिथिल काल ही कह सकते हैं। इसके बाद औरंगजेब के समय दरबार में कट्टरपंथी प्रभाव के कारण चित्रकला का पतन हो गया तथा अनेक मुगल चित्रकार राजपूत राजघराने में चले गए। मुगल शैली की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें राजनीतिक एवं दरबारी जीवन का चित्रण ही मुख्य रूप से हुआ। जन सामान्य के जीवन की झलक मुगल शैली में नहीं मिलती।
Question : मुगल काल के दौरान शहरी विकास पर अपना मत प्रस्तुत कीजिए।
(2005)
Answer : प्राचीन काल या मध्यकाल में जब हम शहर की बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है कि उस समय के शहर या नगर आज के शहरों या नगरों की तरह नहीं होते थे। इन नगरों की दो प्रमुख विशेषताएं होती थीं- पहला, एक सीमित स्थान पर आबादी का उच्च घनत्व और दूसरा जनसंख्या का मुख्यतः गैर-कृषक खासकर गैर-खेतीहर स्वरूप।
इन्हीं दो विशेषताओं के कारण ये शहर गांवों से भिन्न होते थे। ये विशेषताएं मुगलकालीन शहरों के संबंध में भी सही हैं। अतः मुगल काल के दौरान शहरी विकास के संबंध में चर्चा करते समय भी इसे ध्यान में रखना जरूरी है। भारत में तुर्कों के आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही शहरीकरण की प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया मुगल साम्राज्य की स्थापना के कारण और भी तीव्र हो जाती है तथा काफी बड़े-बड़े शहरों का उदय होता है। प्रमाणों से पता चलता है कि कुछ पुराने शहरी केंद्रों जैसे दिल्ली, लाहौर आदि का विस्तार हुआ और कुछ नए शहरी केंद्रों जैसे- इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, गुजरात, बनारस आदि की स्थापना हुई। उत्तर मुगल काल में शहरी केंद्रों के विकास की यह प्रक्रिया मुगल साम्राज्य के अंदर तथा बाहर भी जारी रही। इस साम्राज्य के बाहर भी गोलकुंडा, बीजापुर और कोचीन तथा कालिकट आदि शहरों का विकास हुआ। हालांकि गोलकुंडा और बीजापुर को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया, लेकिन ये दोनों इस साम्राज्य में शामिल किए जाने से पूर्व ही शहरी केंद्र के रूप में विकसित हो चुके थे। इस काल में विकसित होने वाले शहरी केंद्रों में कुछ छोटे होते थे तथा कुछ काफी बड़े होते थे। ये छोटे-छोटे शहरी केंद्र स्थानीय शिल्प एवं व्यापार के केंद्र होते थे। इन केंद्रों से स्थानीय आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं का नियंत्रण होता था। मगर बड़े-बड़े शहरी केंद्रों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व था तथा इन केंद्रों से दक्षिण-पूर्वी एशिया, मध्य-पूर्व एशिया और पश्चिम यूरोप से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण होता था। इन बड़े शहरी केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार की शिल्प सामग्री का उत्पादन होता था। यहां विकसित बाजार होते थे तथा अनेक प्रकार की ऋणों की सुविधा भी उपलब्ध थी। जल एवं स्थल मार्ग से ये केंद्र आपस में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े हुए थे। विदेशी यात्रियों ने मुगल काल के बड़े शहरों की संपदा एवं समृद्धि से प्रभावित होकर काफी कुछ लिखा है।
मुगल काल में शहरीकरण के विकास में अनेक कारणों ने मदद पहुंचाई। मुगलों ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर संपूर्ण भारत को प्रशासनिक एवं राजनीतिक एकता प्रदान किया। इससे राजनीतिक अराजकता का दौर समाप्त हो गया तथा व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा मिला। इस व्यापार विकास ने गांवों को कस्बों में तथा कस्बे को शहरों में विकसित करने में सहायता पहुंचाया।
इसके अलावा मुगलकालीन प्रशासनिक ढांचे ने भी शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। जिन स्थानों को मुगलों ने अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया वह भी शहर के रूप में विकसित हो गए। मुगल काल में तकनीकी परिवर्तन के कारण भी शहरों की संख्या एवं आकार में वृद्धि हुई। चूंकि शहर के लोग स्वयं कृषि कार्य नहीं करते, इस कारण शहर का अस्तित्व कृषि के अधिशेष उत्पादन पर निर्भर करता है। इस काल में नवीन तकनीक के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।
प्रमाणों से पता चलता है कि मुगल काल में किसान बीजों की बुवाई के लिए गड्ढा खोदने की विधि को प्रयोग में लाते थे। वर्षा और बाढ़ से प्राप्त जल की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की नई प्रणालियों का प्रयोग करते थे। कुओं से पानी निकालने के लिए लीवर प्रणाली पर कार्य करने वाले ‘धकेली’ तथा फारसी जल यंत्र ‘साकिया’ का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि ने अधिशेष कृषि अधिशेष में वृद्धि किया। यह अधिशेष शहरों के गैर कृषक जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया।
मुगल शासक वर्ग नगरोन्मुखी थे। अतः शासक वर्ग के नगरों में निवास के कारण शिल्पकारों और दस्तकारों का वर्ग इन नगरों की ओर आकर्षित हुए। इसके कारण शहरों की आबादी में वृद्धि हुई तथा नगरों का विस्तार हुआ। मुगल शासकों को अपने दरबारों, अंतःपुर की साज-सज्जा एवं शानोशौकत के लिए अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी। इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनेक सरकारी कारखाने की स्थापना की गई। ये कारखाने काफी बड़े होते थे। इसके आकार का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मुगल पादशाह अपने आय का 40 प्रतिशत इस पर खर्च करता था। मुगल पादशाह द्वारा इन बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना ने भी शहरी विस्तार को बढ़ावा दिया होगा, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है।
मुगल काल में अनेक यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। ये कंपनियां भारतीय शिल्प-उत्पादों तथा मसालों का यूरोपीय बाजार में निर्यात करते थे। इसके कारण इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। फलस्वरूप अनेक शहरों का विकास शिल्प एवं लघु उद्योग के केंद्र के रूप में हुआ। इन कंपनियों ने जिन स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, वे भी नगर के रूप में परिणत हो गए। इसके अलावा सूफी संतों की गतिविधियां तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं ने भी शहरीकरण के विकास में सहायता पहुंचाई। अनेक नगरों का विकास शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी हुआ। इस प्रकार विभिन्न कारणों ने मुगल काल में शहरीकरण को बढ़ावा दिया।
ऐसा माना जाता है कि उत्तर मुगल काल या 18वीं शताब्दी में शहरीकरण की प्रवृत्ति में ”ास हुई तथा शहरी जीवन में भी गिरावट आई। उर्दू शायर सौदा के ‘शार अशोब’ में दिल्ली की अवनति का रोना रोया गया है। परंतु प्रमाण इसके विपरीत मिलते हैं। मासीर उल उमरा का लेख (1772 ई-) दिल्ली के बारे में कहता है कि वह खूब फलफूल रहा था। इन दोनों स्रोतों का सावधानी से विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि वास्तव में दिल्ली की अवनति इस अर्थ में हुई कि वह प्रशासन की राजधानी नहीं रही। लेकिन दिल्ली की इस कमी की पूर्ति उसके आस-पास कृषि क्षेत्र के विस्तार और संचार व्यवस्था के स्थापित होने से पूरी हुई। यूरोपीय यात्रियों के विवरण से भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि इस काल में नगरों का ”ास हुआ तथा नगरीय जीवन में गिरावट आई।
वास्तव में 18वीं शताब्दी में अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ जिसके कारण प्रशासनिक केंद्र के रूप में अनेक नए शहरों का उदय हुआ। जैसे- मुर्शिदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद आदि। इसके अलावा इन क्षेत्रीय शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों, विद्वानों तथा शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान किया। इस कारण कला एवं शिल्प के केंद्र के रूप में इन केंद्रों का विकास हुआ। एक अन्य बात जो 18वीं शताब्दी में नगरीकरण के हास की मान्यता को खंडित करता है। वह है - व्यापार और वाणिज्य की प्रगति। किसी भी प्रमाण से यह नहीं पता चलता कि व्यापार का ”ास इस काल में हुआ हो, बल्कि इस समय तक विदेशी व्यापारिक कंपनियों की गतिविधियों में वृद्धि के कारण व्यापार और शिल्प उद्योग में वृद्धि ही हुई और जैसा कि हम जानते हैं कि नगरों का विकास किसी भी कारण से हुआ हो उनकी समृद्धि तथा आर्थिक महत्व व्यापार एवं शिल्पों पर ही निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूरे मुगल काल में शहरी जीवन में कोई गिरावट नहीं आयी।
मुगलकाल में शहरों एवं कस्बों की संख्या तथा इसमें रहने वाले लोगों की संख्या से संबंधित आंकड़ें के समय मुगल साम्राज्य में 120 नगरों तथा 3200 कस्बों का उल्लेख मिलता है। इसमें आबादी के दृष्टिकोण से आगरा और दिल्ली सबसे विशाल थे। फिच नामक यूरोपीय यात्री के अनुसार आगरा और लाहौर तत्कालीन लंदन और पेरिस से बड़े शहर थे। मैनरीक ने तत्कालीन पटना की आबादी 2 लाख बतायी है। स्मरणीय है कि यह आबादी यूरोपीय नगरों की आबादी की तुलना में कई गुणा अधिक थे। मुगलकालीन नगरों में प्रशासनिक केंद्र (शाही व प्रांतीय राजधानियां), व्यापारिक केंद्र (पत्तन एवं अंतर्देशीय नगर), धार्मिक एवं शैक्षणिक केंद्र शामिल थे। इनकी आबादी में विभिन्न संप्रदाय के लोग शामिल थे, जिसमें भारतीय और विदेशी, हिंदू और मुसलमान आदि थे।
इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगलकालीन भारत में शहरों की संख्या, आकार और उनकी धन-संपदा में तेजी से वृद्धि हुई। उसमें कुछ की आबादी यूरोप और इंग्लैंड के समकालीन शहरों से भी अधिक थी। लेकिन उनकी वृद्धि से गांवों के जीवन का कुछ भी अहित नहीं हुआ। कुछ शहर पुनर्जीवित हुए और कुछ नए शहर बने। कुछ शहर अफसरशाहों ने बनवाए और कुछ अभिजात वर्ग के लोगों ने। इसके विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे तथा ये शहर आर्थिकगतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। इस कारण इसका विश्वव्यापी महत्व स्थापित हुआ। हालांकि ये शहरी केंद्र विभिन्न श्रेणियों के थे तथा उनका प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक भूमिकाएं भिन्न-भिन्न थी।
Question : ‘हिंदू एवं मुसलमान रहस्यवादियों के धार्मिक सिद्धांत इतने अधिक समान थे कि दोनों धर्मों के अनुयायियों के बीच सहक्रियात्मक आवाजाही के लिए भूमि तैयार हो चुकी थी।’ इसको सुस्पष्ट कीजिए।
(2005)
Answer : बहमनी राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में तुगलक साम्राज्य के अवशेषों पर किया गया। मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में निरंतर विद्रोह और अशांति के कारण दक्षिण भारत के तुर्क सरदारों को भी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की प्रेरणा मिली। तुगलक साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए पश्चिम और दक्षिणी प्रांतों में ऐसे सैनिक सरदारों की नियुक्ति की गई थी जो ‘अमीराने सदा’ कहलाते थे। ये लगभग सौ गांवों के समूह के प्रशासक थे। ये पूर्वकालीन इक्त्तेदारों की तरह थे जो राजस्व वसूलने के साथ-साथ सैनिक टुकडि़यां रखते थे तथा स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस प्रकार प्रशासन, वित्त एवं सेना पर इनका पूर्ण अधिकार था। सबसे पहले गुजरात के सदा अमीरों ने विद्रोह किया, जिससे प्रेरणा पाकर दौलताबाद में उसे विशेष सफलता नहीं मिली। बाद में इस्माइल ने जफर खां को सत्ता सौंप दिया, जिसने 1346-47 ई. में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ग्रहण कर स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किया। सत्ता ग्रहण करने के बाद इसने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों - कोटगिरी, कल्याणी और बीदर को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। वारंगल के शासक को अपना आधिपत्य स्वीकार करने पर मजबूर किया। इसने व्यापार तथा वाणिज्य के विकास पर भी ध्यान दिया तथा राज्य के आंतरिक प्रशासन को मजबूत बनाया। इसने हिंदू प्रजा के प्रति उदार नीति का पालन करते हुए जजिया की वसूली पर रोक लगाया।
अपने स्थापना के समय से ही बहमनी राज्य को पड़ोस के शक्तिशाली विजय नगर से संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष दोनों के बीच प्रभुता का था जो भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक कारण से प्रेरित हुआ। इस संघर्ष का अंत 1565 ई. के तालिकोटा के रक्त-रंजित युद्ध के रूप में हुआ, जिसके बाद विजय नगर साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि इस युद्ध के पूर्व ही बहमनी साम्राज्य अपने आंतरिक कलह तथा प्रशासनिक अंतर्विरोधों के कारण पांच राज्यों में विभाजित हो गया था। ये पांच राज्य बीजापुर के आदिलशाही, अहमदनगर के निजामशाही, बरार का इमादशाही, गोलकुंडा का कुतुबशाही तथा बीदर का बरीदशाही थे। बाद में बीजापुर ने बीदर को अपने राज्य में मिला लिया था।
बहमनी राज्य ने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया तथा दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारत तथा विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम के समर्थक बहमनी राज्य में गए। बहमनी के विभिन्न शासकों ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया तथा विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया। हालांकि इस कार्य से सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ लेकिन इन विद्वानों ने मुस्लिम संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया। बहमनी शासकों ने मदरसा, मस्जिदें आदि इमारतों का निर्माण किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में बहमनी राज्य और विशेषकर उसके उत्तराधिकारी राज्य को सबसे महत्वपूर्ण योगदान दक्खिणी हिंदी का विकास है। इस क्षेत्र में गोलकुण्डा का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार बहमनी राज्य ने दक्षिण भारत के राजनीति और संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Question : चैतन्यदेव और वैष्णववाद
(2005)
Answer : चैतन्यदेव का जन्म बंगाल के नदिया में 1486 ई. में हुआ था। उन्होंने बंगाल एवं पूर्वी भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक हलचल और भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। चैतन्य ने भक्ति के माध्यम से ब्रह्मा की उपासना का उपदेश दिया। उनका कहना था कि जिस प्रकार राधा और कृष्ण के बीच प्रेम था, वैसा ही प्रेम भक्तों को अपने प्रभु के लिए प्रकट करना चाहिए। चैतन्य के धर्मोंपदेश में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए समाज के सभी वर्ग और जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। वे ईश्वर भक्ति के लिए संन्यास को आवश्यक नहीं मानते थे। चैतन्य ने तत्कालीन समाज की बुराईयों पर प्रहार करते हुए एक अति सरल मार्ग की शिक्षा दी। उनके धर्म का केंद्रीय विषय भावनात्मक प्रेम था। चैतन्यदेव के धर्म का यह स्वरूप उनके बाद भी जीवित रहा क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों एवं अनुयायियों में अत्यंत कड़ा अनुशासन लागू किया था और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को सख्ती से दंडित किया जाता था।
चैतन्य बंगाल के वैष्णववादी आंदोलन के एक पश्चातकालीन संत एवं नेता थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन एवं भक्ति संप्रदाय की शुरुआत वैष्णव मतालंबियों एवं सहजिया संप्रदाय दोनों से हुई थी। 12वीं शताब्दी में महान कवि जयदेव का गीत गोविन्द पहले ही लिखा जा चुका था तथा चण्डीदास अपने भक्ति-भजनों एवं विद्यापति नेअपने गीत-काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त कर चुके थे। चैतन्य से काफी समय पहले माधवेन्दुपरी ने बंगाल में भक्ति का संदेश दिया था और भक्ति संप्रदाय की नींव रखी थी। भक्ति का मूल स्रोत श्रीमद्भागवत पंरपरा में था किंतु बाद में यह अपने मार्ग से विचिलित हो गया क्योंकि इसने अनेकों विचारधाराओं को स्वयं में शामिल कर लिया था, विशेषकर तांत्रिक, सहजिया संप्रदाय आदि।
इसके अलावा ब्राह्मणवाद एक धर्म के रूप में कर्मकाण्डी होने के कारण पतनोन्मुखी हो गया था। चैतन्य ने बाह्मणवादी धर्म को दुरावस्था से बचाया तथा वैष्णववादी भक्ति परंपरा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने स्वयं एक मौलिक सुधारकर्ता की भूमिका निभाई तथा बंगाल के हिंदू समाज को पुनर्जीवित कर हिंदू धर्म को त्रण दिया। उन्होंने बड़ी संख्या में शिष्यों को आकर्षित किया जिसमें कुछ मुसलमान एवं निम्न जाति के लोग भी शामिल थे। उन्होंने धर्मशास्त्रें या मूर्तिपूजा का पूरी तरह परित्याग नहीं किया वरन् संकीर्तन को काफी प्रोत्साहित किया।
चैतन्य और उनका वैष्णववाद बंगाल में सामाजिक पुनरुत्थान के लिए भी विशेष रूप से याद किये जाते हैं। इसके अलावा बंगाली साहित्य एवं भाषा के विकास के लिए भी चैतन्य एवं उनके शिष्यों को जाना जाता है। चैतन्य के अनुयायियों ने वृहदकार साहित्य रचा जिसमें इस महान संत के जीवन चरित्र का वर्णन है। बंगाल के सुल्तानों ने इस साहित्यिक क्रियाकलापों को और अधिक प्रोत्साहित किया तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का बांग्ला में अनुवाद करवाया। चैतन्यवाद सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। यह संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में फैल गया। इनके वैष्णववाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इसने मध्यकालीन बंगाल के हिंदू समाज में नई चेतना फैलाई।
Question : भारत के इतिहास में अठारहवीं शताब्दी का आप किस प्रकार से लक्षण-वर्णन करना चाहेंगे?
(2005)
Answer : 18वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में संक्रमण का काल था। इस समय भारत का महान मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया तथा इस शताब्दी के अंत होते-होते वह दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों तक ही अपनी सत्ता को बनाए रख सका। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह (1719-1748) के शासन काल में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हुई तथा हैदराबाद, बंगाल और अवध में प्रायः स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। मराठों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना तो 18वीं शताब्दी से पूर्व ही कर लिया था, किंतु 18वीं शताब्दी में वह मुगलों के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक समय तो ऐसा लगा कि मुगलों का उत्तराधिकार मराठे ही प्राप्त करेंगे परंतु पानीपत की पराजय ने उन्हें भारत में साम्राज्य के निर्माण का स्वप्न तोड़ दिया। इधर मुगल बादशाहत तो 1858 ई. तक रही जब तक कि अंग्रेजों ने 1857 ई. के विद्रोह को दबाने के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह द्वितीय को सिंहासन से हटाकर रंगून नहीं भेज दिया। परंतु मुगल बादशाहत बहुत पहले ही नष्ट हो गई थी और 18वीं शताब्दी में ही विभिन्न शक्तियों का उदय हो गया था। ये नवीन शक्तियां सत्ता और राज्य विस्तार के लिए आपस में संघर्ष कर रही थीं। राजस्थान में राजपूत शक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की। पंजाब में सिखों ने अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिए। दक्षिण भारत में हैदरअली ने मैसूर के स्वतंत्र राज्य की नींव डालीं। मराठों ने भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति होने का दावा किया। राजनीतिक विभक्तिकरण की इन परिस्थितियों में अनेक विदेशी शक्तियों ने हस्तक्षेप किया। इन विदेशी शक्तियों में ईरानी, अफगानी तथा यूरोपीय शक्तियां प्रमुख थीं। ईरानी तथा अफगानी शक्तियां जहां कमजोर होते मुगल साम्राज्य को और भी कमजोर किया, वहीं मराठों के उभरते साम्राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया। इधर यूरोपीय शक्तियों ने भी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में तथा भारतीय शक्तियों से संघर्ष किया। इस प्रकार के पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता में अंग्रेजों ने स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध किया तथा 1757 ई. में प्लासी के युद्ध और 1764 ई. में बक्सर के युद्ध को जीतकर उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वास्तविक सत्ता अपने हाथों में ले लिया। 1799 ई. में उन्होंने एक शक्तिशाली शत्रु टीपू को परास्त कर मैसूर राज्य के विरोध को सदा के लिए समाप्त कर दिया और मराठों से प्रथम युद्ध करके सम्मानित शर्तों पर सालबाई की संधि की। इस प्रकार 18वीं शताब्दी भारत में मुगल साम्राज्य के पतन और उसके परिणामस्वरूप उसके विभिन्न भागों में बने स्वतंत्र राज्यों तथा भारत में आयी हुई यूरोपियन जातियों के पारस्परिक संघर्ष की सदी रही।
18वीं शताब्दी के आर्थिक स्थिति के संबंध में ऐसा माना जाता है कि यह पतन की सदी थी। राजनीतिक एकता और स्थायित्व के अभाव में भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ गया जिसका अंतिम परिणाम भारत में विदेशी सत्ता के स्थापना के रूप में हुआ। परंतु वास्तविक स्थिति कुछ और ही थी। साक्ष्यों से पता चलता है कि कपड़ा उद्योग तथा व्यापार में उन्नति हुई। गांव में भीमुद्रा का प्रचलन था। प्राथमिक बैंक व्यवस्था ददनी प्रथा और हुण्डियों को जारी किए जाने के रूप में प्रगति पर थी और नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि 18वीं सदी के भारत में परिवर्तन की काफी संभावनाएं थीं और उसकी स्थिति आर्थिक जड़ता की नहीं थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने से भारत के व्यापार में उन्नति हुई। लेकिन यह भी सत्य है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, तब से भारत का आर्थिक शोषण आरंभ हो गया। इसी शोषण का परिणाम था कि बंगाल जैसे धनी प्रांत में 1770 में अकाल पड़ा।
18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही था। इस काल में कृषि के उत्पादन तकनीक में पूर्वकाल की तुलना में कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि व्यापार की प्रगति इस काल में हुई तथा इससे लघु उद्योगों के विकास में सहायता भी मिली लेकिन वस्तुओं के निर्माण विधि यथावत ही रही। इससे स्पष्ट है कि तकनीकी परिवर्तन के दृष्टिकोण से 18वीं शताब्दी अपने पूर्वकाल से भिन्न नहीं है। नवीन तकनीकों के प्रयोग न होने के बाद भी कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन आदि में गिरावट नहीं आई। जैसा कि स्रोतों से पता चलता है कि इस काल में कृषि और उद्योग देश की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो किया ही विदेशों में निर्यात के लिए भी अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध कराया। इसी कारण विदेश व्यापार इस काल में न केवल सुरक्षित रहा बल्कि उसमें वृद्धि ही हुई। भारत इस काल में भी प्रचुर मात्र में कपास, रेशम, शक्कर, जूट, नील, अफीम, जड़ी-बूटियां, कीमती पत्थर, मोती आदि वस्तुओं का उत्पादन करता था। सूती वस्त्र उद्योग में तो भारत विश्व प्रसिद्ध था ही, यहां उच्च कोटि का और विभिन्न किस्मों एवं रंगों का सूती कपड़ा तैयार किया जाता था जिसकी मांग संसार के सभी देशों में थी। इस काल में अनेक ऐसे नगरों का विकास हुआ जो सूती वस्त्र या अन्य शिल्पों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। इन औद्योगिक नगरों में उत्पादितवस्तुओं की मांग यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों में थी। भारत का विदेशी व्यापार भी इसी सदी के आरंभ में भारत के पक्ष में रही, लेकिन 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में विदेश व्यापार का संतुलन भारत के विपरीत होती गई तथा सदी के अंत तक विदेश व्यापार भारत के प्रतिकूल हो गया। ऐसा अंग्रेजों द्वारा भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के कारण हुआ।
सामाजिक दृष्टि से 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में काफी विभिन्नता एवं असमानता थी। आर्थिक आधार पर भारत विभिन्न वर्गों जैसे शासक, जागीरदार, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर, कारीगर, मध्यम वर्ग में बंटा हुआ था। इन विभिन्न वर्गों में काफी प्रतिस्पर्द्धा तथा विरोध था। इसके अतिरिक्त धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भी भारतीय समाज में तीव्र विभाजन था।
भारत में बहुसंख्यक वर्ग हिंदू था। यह वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्णों में विभाजित था। इसके अलावा प्रत्येक वर्ण की सैकड़ों जातियां और उप-जातियां थीं। जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर थी और विभिन्न जातियों में पारस्परिक खान-पान और विवाह संबंध नहीं होते थे। जातियों की अपनी पंचायतें होती थी जो जातीय नियमों का कठोरता से पालन करती थी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड देती थी। व्यक्ति की जाति ही उसके व्यवसाय का निर्धारण करती थी। जाति परिवर्तन असंभव था। हिंदूओं में बाल विवाह, दहेज, सती, बहु विवाह, देवदासी प्रथा, बालिकाहत्या, विधवा विवाह का न होना आदि कुप्रथाएं भी इस काल में प्रचलित थीं। हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति काफी खराब थी।
भारतीय समाज का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमानों का था। मुसलमानों में भी धर्म, धन, व्यवसाय आदि के आधार पर विभाजन था। विदेशी मुसलमान भी विभिन्न राज्यों के आधार पर बंटे हुए थे। ईरानी, तूरानी, अफगान आदि आपस में अंतर मानते थे। हिंदुओं की जाति प्रथा का मुसलमानों पर भी कुछ प्रभाव पड़ा तथा मुस्लिम समाज के विभाजन में भूमिका निभाई। मुसलमानों में शिया, सुन्नी, सूफी आदि धार्मिक संप्रदाय भी थे। मुसलमानों में भी पर्दा, बहु-विवाह आदि सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थीं। इस प्रकार इस समाज में भी स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। भारत में सिख, पारसी, जैन आदि अन्य सामाजिक वर्ग भी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज विभाजित, प्रतिस्पर्धापूर्ण और विभिन्न कुरीतियों से ग्रस्त था। यह समाज दुर्बल और गतिहीन था।
भारत में 18वीं शताब्दी में सांस्कृतिक दृष्टि से गिरावट आई। महान मुगल बादशाहों, कुलीनों, जागीरदारों एवं हिंदू-नरेशों ने भारत की राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि के समय में शिक्षा, साहित्य और ललित कलाओं को संरक्षण प्रदान किया तथा उन्नति में सहयोग दिया था। परंतु 18वीं शताब्दी में राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं, जिसके कारण सांस्कृतिक विकास प्रभावित हुआ। इस सदी में अनेक छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों के शासक ने राज्य के संसाधनों का उपभोग व्यक्तिगत विलासिता एवं स्वार्थ पूर्ति में किया। उन्होंने सांस्कृतिक प्रगति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। स्थापत्य कला की दृष्टि से इस काल में निर्मित उत्कृष्ट इमारत नहीं मिलते और मुगल चित्रकला तो सदा के लिए लुप्त ही हो गया। हालांकि कांगड़ा और राजस्थान के राजपूत शासकों ने अपने सीमित संसाधनों से कला को कुछ प्रोत्साहन दिया, विशेषकर चित्रकला में इन शासकों ने विशेष रुचि लिया। इसी प्रकार उत्तरकालीन मुगल शासकों तथा कुछ क्षेत्रीय नवाबों के विलासितापूर्ण जीवन में योग देने के लिए नृत्य एवं संगीत कला को संरक्षण दिया गया। साहित्यिक दृष्टि से फारसी साहित्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हालांकि इस काल में कुछ क्षेत्रीय भाषाओं एवं साहित्य की उन्नति हुई। उर्दू के कुछ विद्वान जैसे मीर, सौदा, नजीर आदि इस काल में हुए और उर्दू मुगल दरबार की लोकप्रिय भाषा बन गई। तमिल, मलयालम दरबारऔर बांग्ला भाषा में भी कुछ ग्रंथों की रचना की गई।
इस काल में शिक्षा का अभाव रहा। हालांकि शिक्षा के लिए मुसलमानों के मकतब तथा मदरसे थे तथा हिंदुओं के पाठशालाओं तथा मंदिरों से जुड़े हुए विद्यालय थे, किंतु ये संस्थाएं निजी या सामूहिक प्रयत्नों से चलती थीं। सरकार की तरफ से शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती थी।
शिक्षा के अभाव के कारण विज्ञान एवं तकनीकी का समुचित विकास नहीं हो पाया। इस काल तथा इस पूर्व भी किसी शासक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और न यह जानने का प्रयत्न किया कि विदेशों में इस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है। इस कारण भारत आर्थिक एवं सैनिक साधनों के क्षेत्र में पिछड़ गया। इसके अलावा शिक्षा के अभाव ने भारतीयों को मानसिक पिछड़ापन दिया, जिससे व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों की प्रगति अवरुद्ध हो गई तथा भारत विदेशी शासन के अधीन हो गया।
Question : सामंत प्रणाली
(2005)
Answer : भारत में सामंती प्रणाली का आरंभ गुप्त काल में देखते हैं, लेकिन इसका पूर्ण विकास पूर्व मध्य काल में ही हुआ। इस प्रणाली के विकास में तत्कालीन राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण केंद्रीय सत्ता निर्बल हुई तथा चारों ओर राजनीतिक अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई। केंद्रीय शक्ति की कमजोरी ने समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया, जिन पर स्थानीय सुरक्षा का भार आ पड़ा। अरबों तथा तुर्कों के आक्रमणों ने शक्तिशाली राजवंशों को समाप्त कर दिया। इस कारण उत्तर भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ। इससे सामंती प्रणाली को बढ़ावा मिला। प्राचीन भारतीय शासक के धर्मविजय की अवधारणा ने इस प्रणाली के विकास में मदद किया।
सामंती प्रणाली के विकास में आर्थिक तत्वों ने भी मदद किया। पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक अव्यवस्था के कारण व्यापार-वाणिज्य का पतन हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था मुख्यतः भूमि और कृषि पर निर्भर हो गयी। इससे बड़े-बड़े भू-स्वामी कुलीन वर्ग का उदय हुआ जो आर्थिक स्रोतों के केंद्र बन गए। आर्थिक परिवर्तन की यह क्रिया सामंतवाद के लिए उपयुक्त वातावरण दिया। इसके अलावा इस प्रणाली के विकास में शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि और ग्राम अनुदान तथा राजाओं द्वारा अपने कुल के व्यक्तियों तथा संबंधियों को विभिन्न प्रांतों में उपराजा अथवा राज्यपाल बनाने की प्रथा ने भी सामंती प्रणाली को मजबूत बनाया। आर.एस. शर्मा की मान्यता है कि सामंती प्रणाली का उदय राजाअों द्वारा ब्राह्मणों तथा प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को भूमि और ग्राम दान देने के कारण हुआ।
सामंत जागीरों के स्वामी होते थे तथा वे विशेष अधिकारों और सुविधाओं का उपभोग करते थे। सामंतों की अनेक श्रेणियां थीं। कुछ बड़े सामंत अपने अधीन कई छोटे सामंत रखते थे। वे अपने-अपने क्षेत्र में राजाओं जैसी सुख-सुविधाओं का उपयोग करते थे। सामंती व्यवस्था पैतृक थी तथा सामंत भूमि पर बिना काम किए ही काफी आमदनी प्राप्त कर लेते थे। राजपूत काल में अनेक छोटे-छोटे सामंतों ने राज्य स्थापित किया तथा अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए परस्पर संघर्ष करने लगे।
इस प्रणाली के कारण व्यापार, वाणिज्य का ”ास हुआ तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा इस प्रणाली से स्थानीयकरण की भावना काविकास हुआ तथा सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध हो गई। सामंतों को राज्य के बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त किया गया। पूर्व मध्यकाल में अधिकाधिक सामंत रखना गौरव की बात माने जाना लगा। राजपूत शासक तो अपने अधीन इतना सामंत रखते थे कि हम कह सकते हैं कि वे सामंतों पर ही शासन करते थे। कभी-कभी सामंतों के प्रभाव में आकर शासक मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा भी कर देते थे। पूर्व मध्यकाल तक प्रशासन का पूर्णतः सामंतीकरण हो गया तथा प्रशासन में सामंतों की नियुक्ति आनुवंशिक रूप से होने लगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि सामंती प्रणाली ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया तथा इससे जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल हुए। समाज के उच्च एवं निम्न वर्गों का अंतर समाप्त हो गया। परंतु यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। वस्तुतः सामंतवाद का विकास चातुर्वर्ण की अव्यवस्थित स्थिति में ही हुआ।
Question : औरंगजेब की राजपूत तथा धार्मिक नीतियां उसके पूर्वजों की नीतियों से किस प्रकार भिन्न थीं? उसके द्वारा किये गये परिवर्तनों के क्या परिणाम हुए?
(2004)
Answer : मुगलों द्वारा अपनायी गयी विभिन्न नीतियों में राजपूत नीति का विशेष महत्व है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम मुगल-राजपूत नीति को सुनिश्चित रूप मिला। अकबर ने राजपूत वर्ग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर न केवल उन्हें सहयोगी बनाया बल्कि सांप्रदायिक असहिष्णुता को भी कम करने का प्रयास किया।
अकबर के काल में अनेक समस्याएं थीं। जैसे अफगान समस्या, हिंदू जनता का विरोध आदि। भारत में राजपूत शासकों का वर्ग सबसे शक्तिशाली था। उनसे सहयोग प्राप्त कर ही अकबर भारत में शासन कर सकता था तथा अपने वंश को स्थायित्व प्रदान कर सकता था। इसलिए अकबर ने राजपूतों को अपने अधीन लाकर मित्र बनाया। उसके उत्तराधिकारी जहांगीर एवं शाहजहां भी कमोबेश इसी नीति पर चलते रहे। परंतु औरंगजेब के काल में साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव, राजपूतों के आंतरिक झगड़ों तथा विभिन्न दलों द्वारा क्षेत्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की उद्घोषणा की पृष्ठभूमि में मुगल-राजपूत संबंधों को धक्का पहुंचा।
औरंगजेब के साथ राजपूत संबंध को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम काल का दौर 1658 से 1678 ई. तक था। पहले दौर में औरंगजेब ने अपने पूर्वजों की राजपूत नीति को समर्थन दिया।उत्तराधिकार के युद्ध में उसे राजपूत शासकों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। यद्यपि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपने पूर्वजों की भांति राजपूतों से वैवाहिक संबंध तो कायम नहीं किया परंतु प्रथम दौर में उन्हें पदोन्नति प्रदान करता रहा।
औरंगजेब के राजपूतों के संबंध के दूसरे दौर (1679-1707 ई.) में कटु हो गये। अपने पूर्वजों की नीति के विपरीत उसने अपने सहयोगी सामंत मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप कर राजपूतों को नाराज कर दिया।मुगलों ने मेवाड़ के कुछ इलाके छीन लिये थे।
मेवाड़ का शासन उन इलाकों को वापस न मिलने के कारण औरंगजेब से नाखुश था। इस दौर में औरंगजेब ने राजपूतों को कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा। उसने राजपूतों के आपसी वैवाहिक समझौतों में भी हस्तक्षेप किया। बीकानेर, कोटा, बूंदी आदि राजपूत राज्यों से अच्छे संबंध रहने के बावजूद उन्हें ऊंचा पद नहीं दिया। उसने राजपूतों की बजाए दक्षिण में पैर जमाने के लिए मराठों का सहयोग लिया। यह सब कार्य उसने अपने पूर्वजों की राजपूत नीति के विपरीत किया।
मुगलों की धार्मिक नीति का विकास भी अकबर के शासनकाल में हुआ। उसके काल में एक नयी और उदार धार्मिक नीति का विकास हुआ। जिसमें साम्राज्य की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को सम्मानपूर्ण स्थान मिला। उसने सुलह-कुल अथवा सबके प्रति सद्भाव की नीति अपनायी और समस्त प्रजा को एक समान समझा। उसके काल में धार्मिक आधार पर पदों पर नियुक्ति नहीं की जाती थी। सरकारी नौकरियों में सभी धर्म के लोगों की नियुक्ति की जाती थी। उसने मुस्लिम कट्टरपंथियों का प्रभाव काफी बढ़ गया। इसके बावजूद हिंदुओं का धार्मिक आधार पर उत्पीड़ननहीं हुआ। परंतु औरंगजेब के काल में उसके पूर्वजों की धार्मिक नीति की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं।
औरंगजेब दकियानूसी तथा संकुचित धार्मिक विचारों का था। उसके शासनकाल के आरंभ में दकियानूसी इस्लामी तत्व धीरे-धीरे प्रबल बन गये। अकबर के विपरीत वह दार्शनिक तर्क-वितर्क अथवा आध्यात्म में जरा भी रूचि नहीं रखता था। उसने 1679 ई. में पुनः जजिया कर लागू कर दिया। 1665 ई. में हिंदू व्यापारियों से भेदभाव वाला कानून लागू किया गया। अपने पूर्वजों के विपरीत औरंगजेब ने ऐसे नियम भी जारी किये जो राज्य नीति के रूप में पूरे साम्राज्य के हिंदुओं को सीधे प्रभावित करते थे।
इन नियमों में था- मंदिरों को तोड़ना और पुराने मंदिरों की मरम्मत पर प्रतिबंध, सरकारी नौकरियों में मुस्लिम वर्ग को प्राथमिकता देना आदि। ये सब कार्य उसने मुस्लिम कट्टपंथियों का समर्थन पाने के लिए किया।
उसने इस्लाम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अनेक प्रथाओं जैसे झरोखा दर्शन, सिक्कों पर कलमा अंकित करना आदि को बंद करवा दिया। लेकिन ये कार्य किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं थे। औरंगजेब की कट्टरता के पीछे उसकी व्यक्तिगत सोच और अंदर छिपी कुंठा और ग्लानि काम कर रही थी।
अपने पूर्वजों की राजपूत एवं धार्मिक नीति में परिवर्तन करने के कारण औरंगजेब को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह सम्राज्य को स्थायी रखने में राजपूतों का सहयोग नहीं पा सका जबकि दक्षिण में राज्य प्रसार के समय मराठों के विरुद्ध राजपूतों का अधिकतम सहयोग प्राप्त कर सकता था। उसे अन्य विद्रोह के अलावा राजपूतों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। उसके पुत्र राजकुमार आजम के विद्रोह के समय मेवाड़ के राजपूतों ने औरंगजेब की सहायता के बजाए आजम का साथ दिया। राजपूतों से संघर्ष के कारण साम्राज्य की सैन्य शक्ति एवं प्रतिष्ठा को हानि पहुंची।
धार्मिक नीति में परिवर्तन के कारण उसे हिंदू वर्ग का सहयोग मिलना बंद हो गया। मंदिरों को तोड़ने तथा जजिया कर को लगाने के कारण बहुसंख्यक हिंदू प्रजा उसकी विरोधी बन गयी। उसके समय हुए जाट, सिक्ख आदि विद्रोह यद्यपि आरंभ तो हुए आर्थिक कारणों से परंतु औरंगजेब के कट्टरपंथी नीति के कारण उनका स्वरूप बाद में सांप्रदायिक हो गया। इससे विद्रोहों का स्वरूप अधिक कठोर हो गया। साम्राज्य की सैन्य शक्ति में ”ास हुआ। उससे राजपूत वर्ग तो विमुख थे ही बहुसंख्यक प्रजा भी विरुद्ध हो गयी। इन सबका प्रभाव मुगल साम्राज्य के स्थायित्व पर पड़ा। साम्राज्य कमजोर पड़ गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् मुगल साम्राज्य का क्षरण भी आरंभ हो गया।
Question : क्या दीन-ए-इलाही ‘अकबर की मूर्खता का स्मारक’ था?
(2004)
Answer : मुगल सम्राट अकबर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सांस्कृतिक एवं सामाजिक समन्वय के क्षेत्र में थी। उस युग में भारत में सांप्रदायिक सौहार्द्र की कमी थी। हिंदू एवं मुस्लिम वर्गों के मध्य धार्मिक आधार पर वैमनष्यता व्याप्त थी। मध्यकाल में शासक वर्ग का धर्म मुस्लिम था और उनके द्वारा मुस्लिम धर्म को प्रश्रय देने के कारण राजदरबार एवं समाज में मुस्लिम कट्टरपंथियों का बोलबाला था। ऐसे समय में परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अकबर ने भारत में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सद्भाव एवं सम्मान की नीति अपनायी जिसे ‘सुलह कुल’ कहा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में अकबर एक श्रद्धावान मुसलमान था। इस्लाम धर्म सिद्धांत पर बहस के लिए 1575 में उसने ‘इबादत खाना’ की स्थापना की। 1578 में ‘इबादत खाना’ का दरवाजा समस्त धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया। सभी धर्मों के विद्वानों से बहस के उपरांत अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में अच्छे तत्व हैं। इससे अकबर की विचारधारा को एक नई दिशा मिली।
1581-82 में अकबर ने सभी धर्मों के उपदेशों का संकलन करने ‘दीन-ए-इलाही’ के रूप में एक ऐसी आचार संहिता प्रस्तुत की जिस पर सभी धर्मों के अनुयायी अपने-अपने धर्मों के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए भी कार्य कर सकते थे। ‘दीन-ए-इलाही’ विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच एकता और सद्भावना लाने का एक सराहनीय प्रयास था। यह कोई धर्म नहीं था बल्कि एक प्रकार की सूफी व्यवस्था थी। इस पंथ का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, पुजारी की व्यवस्था नहीं थी, उपासना स्थल नहीं था, केवल दीक्षा की व्यवस्था थी। अकबर अपने चारों और एक निष्ठावान वर्ग खड़ा करना चाहता था जिन्हें वह आध्यात्मिक दिशा प्रदान कर सके। ‘दीन-ए-इलाही’ का अकबर की धार्मिक या राजनैतिक नीति से संबंध नहीं था।
मौजूदा परिस्थितियों में अकबर ने यह समझ लिया था कि न तो सभी धर्मों को एक में मिलाना संभव है और न ही एक नया धर्म बनाना संभव है, परंतु उसने सुनने वालों तक अपनी बात पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की। इसी उद्देश्य से उसने ‘दीन-ए-इलाही’ पंथ की स्थापना की। ताकि सभी धर्मों के लोगों को अच्छे आचरण की शिक्षा देकर सांप्रदायिकता से मुक्त एक समाज का निर्माण कर सके। इसलिए ‘दीन-ए-इलाही’ ‘अकबर की मूर्खता का स्मारक’ नहीं था बल्कि सामाजिक समन्वय के क्षेत्र में एक सराहनीय प्रयास था।Question : कहा जाता है कि चोल राजाओं ने एक शक्तिशाली तथा सुसंगठित प्रशासन की स्थापना की, जिसमें स्थानीय स्तर पर स्वशासन का तत्व विद्यमान था। क्या आप सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए।
(2004)
Answer : चोल शासकों ने सैन्य विजयों द्वारा दक्षिण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की और इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उन्होंने एक मजबूत और स्थिर प्रशासन भी दिया जो कि अनेक विशेषताओं वाली थी। प्रशासन के क्षेत्र में उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि स्थानीय स्वशासन की पद्धति थी। अपने आप में यह अद्वितीय थी। इन सबकी जानकारी उनके शिलालेखों से होती है। चोलों की राजनीतिक पद्धति ऐसी थी जिसने केंद्रीय प्रशासन की विशिष्टताओं को सुरक्षित तथा कृषकों बड़े पैमाने पर संपर्क बनाये रखा।
चोल शासकों ने अपने साम्राज्य के अनुरूप ‘चक्रवर्तीगल’ जैसी बड़ी-बड़ी उपाधियां ग्रहण कीं। दिवंगत राजाओं की मूर्तियों की पूजा-उपासना एवं उनकी स्मृति में निर्मित मंदिरों ने जनमानस में इस भावना को प्रोत्साहित किया कि राजा में ईश्वरीय गुण निहित रहते हैं।
चोलों ने एक अत्यंत कार्य कुशल प्रशासन की स्थापना की। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें ‘मंडलम’ कहा जाता था। प्रांतों की संख्या बदलती रहती थी। कभी यह संख्या छः थी और कभी आठ थी। प्रत्येक ‘मंडल’ कई ‘कोट्टमों में विभक्त थे। ‘कोट्टम’ कई ‘नाडुओं’ में विभक्त था। प्रत्येक ‘नाडु’ में अनेक ग्राम-संघ थे जिन्हें ‘कुर्रम’ और ‘तार-कुर्रम’ कहा जाता था। वे प्रशासन की इकाइयां थे। राजा प्रशासन का प्रमुख था परंतु उसकी निरंकुशता, मंत्रिपरिषद और सुव्यवस्थित प्रशासनिक कर्मचारी-मंडल के कारण सीमित थी। ‘मण्डल’ का प्रमुख अधिकतर राजा का संबंधी होता था। वह केंद्रीय सरकार से निरंतर सम्पर्क बनाए रखता था। प्रशासकीय कार्य में बहुत से कर्मचारी उसके अधीन होते थे। रिकार्ड नियमित ढंग से रखे जाते थे। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अनेक विभाग थे। विभागों के प्रमुख राजा के निकट होते थे और राजा प्रायः उनसे परामर्श लिया करता था।
चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय एवं ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की पद्धति थी। ग्राम और नगर परिषदें प्रारंभिक परिषदें थीं और ‘नाडु’ परिषदें प्रतिनिधि परिषदें थीं। चोलों के काल में ग्राम एक प्रशासनिक इकाई थे और उस समय में गांवों को दी गयी स्वायत्तता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चोल अधिकारी गांवों के मामलों में प्रशासकों के रूप में नहीं बल्कि परामर्शदाताओं और प्रेक्षकों के रूप में भाग लेते थे। गांवों में ‘ग्राम सभा’ नामक संगठन होता था और इसी सभा में सत्ता निहित होती थी। बड़े गांवों में जहां ग्रामीण संगठन जटिल होता था, विभिन्न प्रकार की सभाएं होती थीं, जिनमें सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुसार एक ग्रामीण दो या अधिक सभाओं का सदस्य हो सकता था। गांव हलकों में बांटा जा सकता था और प्रत्येक हलका अपने सदस्यों की एक सभा बुला सकता था। ग्राम सभा अनेक वारियमों (समितियों) के माध्यम से स्वशासन का संचालन करती थी।
प्रशासन की विभिन्न इकाइयां जैसे नाडु, कुर्रम तथा ग्राम में विभिन्न प्रकार की सभाएं होतीथीं। पूरे प्रांत की जन सभा के अनेक संदर्भ मिलते हैं। जिलों और नगरों की अपनी सभाएं थीं।
ग्राम स्तर पर एक ‘महासभा’ भी होती थी। अधिकांश स्थानीय निवासी इस महासभा के सदस्य होते थे। इन सभाओं की तीन श्रेणियां होती थीं-उर, सभा अथवा महासभा, तथा नगरम् ‘उर’ साधारण लोगों की संस्था थी। ‘सभा’ के सदस्य गांव के केवल ब्राह्मण लोग होते थे। यह ‘सभा’ केवल उन ग्रामों में होती थी जो ब्राह्मणों को दान में दिये गये थे। इसे ‘अग्रहार’ भी कहा जाता था। तोंडमंडलम् तथा चोलमंडलम् में प्राप्त चोल अभिलेखों में अग्रहार तथा ब्राह्मणों की सभा के विशेष उल्लेख हैं। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कांची और मद्रास क्षेत्रों में ऐसी अनेक सभाएं थीं। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत नगरम् आते थे, जो सामान्यतः व्यापारिक केंद्रों में होती थी क्योंकि ये पूर्णतः व्यापारिक हितों की रक्षा के निमित्त होती थी। कुछ गांवों में ‘उर’ तथा ‘सभा’ दोनों ही होती थी। बहुत बड़े गांवों में प्रशासनिक सुविधा के लिए दो ‘उर’ होते थे। ‘उर’ तथा ‘सभा’ अथवा ‘महासभा’ में ग्राम के समस्त वयस्क पुरुष भाग ले सकते थे लेकिन व्यावहारिक रूप में प्रौढ़ सदस्य अधिक सक्रिय भाग लेते थे। ‘उत्तरमेरूर’ के मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख में स्थानीय ‘सभा’ की कार्य प्रणाली का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है।
‘सभा’ के वारियम (कार्यकारिणी समिति) की सदस्यता के लिए कुछ शर्तें थीं जैसे पैंतीस से सत्तर वर्ष की आयु सीमा, अपना मकान, एक-डेढ़ एकड़ भूमि, वैदिक मंत्रों की जानकारी, आदि। 1190ई- के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि कभी कभी चुनाव के नियम सम्राट द्वारा निर्धारित किये जाते थे, किंतु अधिकतर ग्राम-सभा ही इसका निर्धारण करती थी। सभा की बैठक सामन्तया मंदिरों में अथवा पेड़ के नीचे होती थी। वारियम (कार्यकारिणी समिति) के तीस सदस्यों में से उपवन (तोट्टवारियम्), जलाशय (एरिवारियम) आदि समितियां निर्मित होती थीं। ‘महासभा’ अथवा ‘सभा’ को ‘पेरू गुर्रि, इसके सदस्यों को ‘पेरू-मक्कल’ तथा समिति के सदस्यों को ‘वारियपेरूमक्कल’ कहा जाता था।’
सरकार के लिए कर-निर्धारण का दायित्व ग्राम सभा का होता था। कभी-कभी समस्त गांव से संयुक्त कर एकत्रित किया जाता था। किसी विशेष कार्य जैसे जलाशय का निर्माण कराने के लिए, सभा को कर-निर्धारण का अधिकार था। दान तथा करों से संबंधित आय-व्यय का विस्तृत ब्यौरा रखना ग्राम सभा का कार्य था। सार्वजनिक भूमि पर ग्राम सभा का स्वामित्व होता था। साथ ही व्यक्तिगत भूमि पर भी इसका न्यायिक अधिकार था। जंगल को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाना, राजस्व वसूल करना, कर न देने वाले की भूमि नीलाम करना, भूमि तथा सिंचाई संबंधी झगड़ों का फैसला करना भी ग्राम सभा का कार्य था। न्याय समिति (न्यायवत्तर) अपने अधिकारियों के माध्यम से अपराध का पता लगाती थी। धर्म वारियम न्यस्त संपत्ति की देखभाल करती थी। बड़ी ग्राम सभाओं में वैतनिक अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी परंतु छोटे गांवों की ग्राम सभाओं में सदस्य अवैतनिक थे। राजा और गांव के मध्य संबंध बनाये रखने के लिए चोल शासकों के अपने सामन्त होते थे लेकिन सामन्तों और राजाओं के परस्पर संबंधों से ग्राम सभा का कोई संबंध नहीं था।
रोमिला थापर के अनुसार ‘ग्राम स्तर पर स्वायत्तता इतनी थी कि प्रशासन के उच्च स्तरों और राजनीतिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन गांव के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे।’ कभी-कभी चोल सामंत कर एकत्रित करने में बहुत कठोरता बरतते थे। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि जब केंद्रीय नियंत्रण बहुत निर्बल हो गया तब स्थानीय संग्रहकर्ता एवं अधिकारी निरंकुश एवं अनियंत्रित हो गये तब पूरे जिले की समस्त गांवों ने सामूहिक रूप से सभा करके निरंकुश एवं अत्याचारी प्रवृत्तियों का सामूहिक रूप से विरोध करने का निश्चय किया। इन ग्राम-सभाओं तथा सर्वसाधारण लोगों की ‘उर’ नामक संस्थाओं को लघु-गणतंत्र कहना सर्वथा उपयुक्त है। इन स्वशासित व्यवस्थाओं में केंद्रीय सत्ता द्वारा असाधारण परिस्थिति में ही हस्तक्षेप होता था।
Question : वातापी के चालुक्यों के उत्थान तथा उनके अन्य शासकों से संघर्ष का विवरण दीजिए। उनके द्वारा कलाओं के संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए।
(2004)
Answer : छठी शताब्दी में दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्यों की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण घटना थी। लगभग 550 से 750 ई- के काल में न केवल दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत की राजनीति को भी वातापी के चालुक्यों ने प्रभावित किया। वातापी के चालुक्यों के संबंध में बहुत कम ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। विक्रमांक देवचरित के लेखन एवं विक्रमादित्य छठे के दरबारी कवि बिल्हण और परवर्ती चालुक्य वंश के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि चालुक्य शासक (बादामी/वातापी, पश्चिमी चालुक्य) अयोध्या को अपने पूर्वजों का मूल निवास मानते थे।
चालुक्य वंश का संस्थापक वैसे तो जयसिंह था, परंतु वातापी के आस-पास के क्षेत्रों को मिलाकर एक छोटे राज्य की स्थापना कर वंश की वास्तविक नींव डालने वाला ‘पुलकेशिन प्रथम’ था। उसने वातापी अथवा बादामी को अपनी राजधानी बनाया। उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। उसके पुत्र ‘कीर्तिवर्मन प्रथम’ ने बनवासी के कदंबों, कोंकण के मौर्यों एवं बेलारी तथा, कार्नूलों को युद्ध में पराजित किया। कीर्तिवर्मन का भाई ‘मंगलेश’ अगला शासक बना। उसके कलचुरियों तथा कदंबों को पराजित किया। उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा पुलकेशिन द्वितीय बना। एहोल स्थित पुलकेशिन द्वितीय के शिलालेख में इस वंश का पूर्ण इतिहास प्राप्त होता है। उसने सन् 609 से 642 ई. तक शासन किया। उसके शासन काल में चालुक्यों की शक्ति, वैभव एवं ऐश्वर्य की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर पहुंच गयी। प्रारंभ में उसने विद्रोही सामन्तों एवं निकटवर्ती राज्यों पर अपनी सत्ता स्थापित की। उसने कदंबों की राजधानी पर अधिकार कर लिया। मैसूर के गंगों को आतंकित किया और उत्तरी कोंकण के मौर्यों को पराजित किया। इसी के समय से चालुक्यों एवं पल्लवों के बीच युद्ध आरंभ हुआ, जो लगभग 150 वर्षों तक चलता रहा। सर्वप्रथम पल्लव शासक ‘महेन्द्रवर्मन प्रथम’ से इसका युद्ध हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चालुक्य और पल्लव दोनों ही दक्षिण में अपना आधिपत्य चाहते थे तथा दोनों ही वंश के शासन शक्तिशाली थे। अतः संघर्ष का होना अवश्यंभावी था। एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों से वेंगी को छीन लिया और अपने भाई को वहां का गर्वनर बना दिया।
यद्यपि चालुक्यों के अभिलेखों में चालुक्यों की विजय का उल्लेख है परंतु दूसरी ओर पल्लवों के अभिलेखों में महेंद्रवर्मन प्रथम की पुल्ललूर विजय का वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय ने चोल, केरल और पांड्य शासकों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर भारत के महान सम्राट ‘हर्षवर्धन’ पर विजय थी।
हर्षवर्धन नर्मदा के दक्षिणी राज्यों पर भी अपना आधिपत्य चाहता था। इसी कारण नर्मदा के तट पर उन दोनों का युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई और उसने दक्षिण भारत पर आधिपत्य का विचार त्याग दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में पुलकेशिन द्वितीय ने ‘परमेश्वर’ की उपाधि धारण की। इसके बाद लाट, मालवा और गुजरात भी उसके राज्य के अंग बन गये। लेकिन 642 ई. में पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम चालुक्य सेना को पराजित कर वातापी तक पहुंच गया। इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हुई।
पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात् चालुक्य वंश कुछ काल के लिए लुप्त हो गया। पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने ‘वेंगी के चालुक्य वंश’ की स्थापना की। पुलकेशिन के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम 654-55 में गद्दी पर बैठा। उसके काल में चोलों, पांडयों और केरलों ने स्वयं का स्वतंत्र घोषित कर विद्रोह कर दिया। विक्रमादित्य ने इन तीनों को समाप्त करने के अलावा पल्लवों के राज्य कांची को हस्तगत कर लिया। विक्रमादित्य प्रथम के उत्तराधिकारी विनयादित्य और विजयादित्य भी शक्तिशाली शासक थे। विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों को पुनः पराजित किया। सम्भवतः उसने अरबों के आक्रमण का प्रतिरोध करके उन्हें दक्षिण गुजरात तक भगा दिया था। उसके पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय को 753 में उन्हीं के राष्ट्रकूट वंश के सामान्त दन्तिदुर्ग ने पराजित किया और इस प्रकार चालुक्य वंश का अंत हो गया।
वातापी के चालुक्य शासक शक्तिशाली होने के अतिरिक्त कला के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने विष्णु, शिव एवं अन्य देवताओं के सम्मान में मंदिरों के निर्माण कार्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। पाषाण वास्तुशिल्प कला की भी बहुत उन्नति हुई। पत्थरों को बिना गारे और चूने से जोड़ा जाता था। चालुक्यों के तत्वाधान में बौद्धों और ब्राह्मणाें ने गुफा मंदिर बनवाये। इन विशाल गुफाओं में पर्याप्त प्रकाश तथा काम करने के लिए आवश्यक सुविधाओं के अभाव में गहरी कटी हुई गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुऐ हैं।
अजन्ता की सर्वश्रेष्ठ कला कृतियां पांचवीं और छठी शताब्दियों में वाकाटकों तथा चालुक्यों के समय की हैं। अजंता के प्रथम विहारीय विशालकक्ष में एक भित्ति चित्र में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारस के शिष्टमंडल के भव्य स्वागत को अभिव्यक्त किया गया है। चालुक्यों द्वारा निर्मित बादामी तथा एहोल के मंदिर दक्षिण भारतीय शैली के प्रतीक हैं। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था। लेकिन इस मंदिर में यह शैली पराकाष्ठा पर पहुुंच गयी थी।
चालुक्यों द्वारा निर्मितवातापी का विष्णु का गुफा मंदिर बौद्ध गुफामंदिर के अनुरूप है। इसी प्रकार अनेक गुफा मंदिर भी बौद्धों के गुफा मंदिरों के समान ही है। चालुक्यों के मंदिर पत्थरों के बने हैं। मेगुति स्थित शिव मंदिर इस कला का साक्ष्य है। इस मंदिर में पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित रविकीर्ति द्वारा रचित एक प्रशस्ति भी है। चालुक्यों के समस्त मंदिरों में एहोल का विष्णु मंदिर सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित मंदिर है। यह मंदिर उड़ते हुए देवताओं की सुन्दर मूर्तियों के लिए प्रख्यात है। पट्टदकल स्थित विरुपाक्ष मंदिर में स्तंभों परआधारित लोगों के लिए एक विशाल मंडपम् अथवा सभाभवन भी है। एहोल में 70 मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासकों ने किया। उनके काल में जैन मतावलम्बियों ने कर्नाटक में कुछ मंदिर का निर्माण करवाया था।
Question : ‘चालीस अमीरों का दल’ तथा उसके सुल्तानों से संबंध।
(2004)
Answer : इल्तुतमिश ने एक ‘चालीस गुलामों’ के दल का निर्माण किया और लगभग सभी ऊंचे पद इन्हीं लोगों को दिये। मुईजुद्दीन अथवा कुत्बुद्दीन के समय के अमीरों में से विरोधी अमीर पदच्युत कर दिये गये अथवा मार डाले गये। इस कारण शेष अमीर इल्तुमिश के अधीन हो गये। ‘चालीस अमीरों के दल’ ने इल्तुतमिश का अठत तक साथ दिया। सल्तनत के राज्य विस्तार तथा स्थायित्व में इन्होंने योगदान दिया। अंतिम समय में इल्तुतमिश अपने पुत्रों की अयोग्यता के कारण अपनी बुद्धिमान एवं योग्य पुत्री ‘रजिया’ को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था लेकिन अमीरों के दल ने इसका विरोध किया और उसके पुत्र रूक्नुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया। फिरोज एवं उसकी मां शाह तुर्कान के विरोधी कार्यों के कारण अमीरों के दल ने उसे युद्ध में पराजित किया। इसी बीच ‘रजिया’ दिल्ली के जनता के सहयोग से दिल्ली की शासिका बन गयी।
‘चालीस अमीरों के दल’ ने ‘रजिया’ का विरोध करने के लिए रजिया से युद्ध किया परंतु आरंभ में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में उन्होंने एक युद्ध में ‘रजिया’ को युद्ध में हराकर मुईजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बनाया। बहराम शाह पूरी तरह इन अमीरों पर आश्रित था। राज्य के सभी उच्च पदों पर इन्हीं अमीरों का वर्चस्व था। 1242 ई. में अमीरों ने मसूद शाह को सुल्तान बनाया। ‘चालीस अमीरों के दल’ के एक अमीर अथवा गुलाम बलबन इस समय काफी मजबूत हो चुका था। उसने मसूद शाह को हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। उसके शासन काल में राज्य सत्ता की डोर बलबन के हाथों में थी। वास्तविक शासक बलबन ही था। नासिरुद्दीन बलबन की स्वामिभक्ति देखकर उसकी सहायता से अन्य अमीरों को कुचलना चाहता था। उसे ‘नायब’ भी नियुक्त किया। परंतु बलबन एवं नासिरुद्दीन को अन्य विद्रोही अमीरों के भयंकर विद्रोह का सामना करना पड़ा। अंत में बलबन अपनी योग्यता के बल पर नासिरुद्दीन के बाद 1266ई. में दिल्ली का सुल्तान बनने में कामयाब हुआ।
Question : कबीर तथा नानक के योगदान पर बल देते हुए भक्ति आंदोलन के निर्गुण संप्रदाय के विकास की विवेचना कीजिए।
(2004)
Answer : मध्यकालीन भारत में धार्मिक विचारों के क्षेत्र में एक महान आंदोलन का विकास 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुआ, जिसका संबंध मुख्य रूप से हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार के साथ-साथ धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने से था। इसे ‘भक्ति आंदोलन’ के नाम से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन आंतरिक रूप से वैविध्यपरक था और इसमें दो भिन्न-भिन्न धारणाएं दृष्टिगोचर होती है प्रथम है सगुण संत-परंपरा तथा द्वितीय निर्गुण-संत परंपरा।
निर्गुण भक्ति धारा के संतों में कबीर और नानक का नाम प्रमुख है। निर्गुण भक्ति परंपरा के विकास में कबीर एवं नानक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि निर्गुण परंपरा का नाथ-पंथी संतों की रचनाओं में वर्णन मिलता है परंतु उसका सच्चा क्रियात्मक रूप मध्यकाल में कबीर के बाद आया। ऐसा माना जाता है कि चौदहवीं शताब्दी से बहुत पहले ही निर्गुण भक्ति तथा निराकार प्रभु की आस्था का भाव प्रकट हो चुका था और इस संबंध में भारत के अधिकांश भागों में यत्र-तत्र कुछ रचनाएं भी प्रस्तुत की जाने लगी थी। परंतु जो कुछ मध्यकालीन संत कबीर, नानक, दादू आदि ने कहा और जिस रूप में कहा उसकी एक पृथक ऐतिहासिक तथा निर्गुण परंपरा उभरी तथा बहुत समय तक थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ समाज और धर्म को प्रभावित करती रही।
निर्गुण संतों ने प्रभु की भक्ति निराकार रूप में करने पर जोर दिया, जबकि तुलसी, सूर, चैतन्य आदि ने राम या कृष्ण की पूजा या सगुणोपासना पर बल दिया। निर्गुण संतों की विचार धाराएं उपनिषदों से प्रेरित थीं। कबीर एवं नानक जैसे संतों ने सरल भाषा के माध्यम से जन-साधारण को महसूस कराया कि इस संसार की मूल सत्ता अवश्य है परंतु उसका कोई रूप नाम नहीं है।
मध्यकालीन भारतीय समाज विभिन्न प्रकार के धार्मिक मत-मतांतरों के रूढि़वादिता से ग्रसित था। एक नये धर्म-मुस्लिम धर्म का भी समाज में प्रवेश हो चुका था। मुस्लिम धर्म शासक वर्ग का भी धर्म था। विभिन्न कारणों से हिंदू धर्म में आन्तरिक द्वंद्वता तो थी ही, हिंदू एवं मुस्लिम धर्म में भी साम्प्रदायिक असहिष्णुता की स्थिति थी। उस काल में सगुण भक्ति आंदोलन का प्रचलन जोरों पर था। इसमें मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन उपासना आदि को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। इससे मंदिरों की संस्कृति तथा ब्राह्मणों के कर्मकांडों को अनजाने में ही महत्व मिल गया और धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा मिला। समाज में जाति-प्रथा, ऊंच-नीच का भेदभाव तो पहले से ही था। निर्गुण संतों ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निराकार प्रभु की भक्ति का मार्ग आम-जन को दिखाया। जिसमें बाह्य साधना से ध्यान हटाकर वैयक्तिक साधना पर जोर दिया गया। उन्होंने अधिक प्रगतिशील विचारधारा का प्रचार किया तथा डटकर आडंबरों का विरोध किया। परिणामस्वरूप निर्गुण भक्ति आंदोलन को व्यापक सामाजिक आधार भी प्राप्त हुआ।
कबीर दास मात्र भक्त ही नहीं, बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। अंधविश्वासों, दकियानूसी अमानवीय मान्यताओं तथा गली-सड़ी रूढि़यों की कटु आलोचना की। उन्होंने समाज, धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचारधारा को प्रोत्साहित किया। कबीर ने जिन ‘राम’ की भक्ति का उपदेश दिया वे ‘राम’ सगुणोपासक के ‘आराध्यदेव राम’ नहीं थे बल्कि निराधार प्रभु को ‘राम’ का नाम दिया था। उन्होंने किसी ईश्वर विशेष की उपासना पर बल नहीं दिया। उन्होंने जनसाधारण के लिए धर्म की सहजता या भक्ति की सुगमता पर बल दिया। जनसाधारण की ही भाषा में उन्होंने बताया कि निर्गुण प्रभु सबका है, उस पर किसी वर्ग, व्यक्ति तथा धर्म-जाति का अधिकार नहीं है। निर्गुण भक्ति-धारा में कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक शुद्ध गृहस्थ बने रहे एवं शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को मानव की सफलताओं का आधार बताया। इससे काफी हद तक कबीर तत्कालीन स्थितियों को प्रभावित करने में सफल रहे।
उन्होंने पहली बार धर्म को अकर्मण्यता की भूमि से हटाकर कर्मयोगी की भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। कबीर ने पौराणिक हिंदू-मत के साथ-साथ मुल्लाओं और काजियों की रूढि़वादी धार्मिक-परंपराओं का भी डटकर विरोध किया। कबीर ने मध्यकालीन विषम सामाजिक परिस्थितियों में इस प्रथा का डटकर-विरोध किया और बिखरे समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दैवी एकता के तर्क से कबीर ने एक ऐसा रंग दिखाया कि उनकी शिष्य-परंपरा में हिंदू और मुसलमान सभी शिक्षित होने लगे।
कबीर ने समाज के आर्थिक ढांचे पर भी प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि समाज तथा राष्ट्र में अधिकतर विवाद अर्थव्यवस्था की असमानता से उपजते हैं। उन्होंने शारीरिक परिश्रम द्वारा आवश्यकता के अनुकूल धन अर्जित करने एवं उपभोग करने का संदेश दिया। सारांश में कबीर ने जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विचारधारा का बीजारोपण किया। समकालीन समाज एवं धर्म के क्षेत्र में उनकी तीन बातों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ये बातें हैं वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात, सांप्रदायिक तत्वों का बहिष्कार तथा भक्ति की सादगी एवं व्यापकता का प्रचलन।
कबीर के बाद निर्गुण भक्ति धारा पर प्रभाव डालने और प्रचार-प्रसार करने मे नानक का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है विचारों और सामाजिक आचारों की दुनिया में परिवर्तन लाने वाले गुरु नानक ने किसी का दिल दुखाए बिना तथा किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को नाश करने का प्रयास किया। उनका उपचार प्रेम, मैत्री, सहानुभूति और सर्वहितचिंतन था। भेदभाव से उठकर वे हिंदू-मुसलमानों को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने आम जन को समन्वय का मार्ग बताया। इस्लाम के उत्तम सिद्धांतों को भी उन्होंने सहज भाव से अपनाया। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में एकेश्वरवाद, मूर्तिपूजा का विरोध, हिंदू-मुस्लिम एकता अैर सच्ची पवित्र-भक्ति उनका ध्येय रहा है। विषम परिस्थितियों में उन्होंने मनुष्य की अंतनिर्हित शक्ति को जगाया और एक सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में विश्वास द्वारा भक्ति-भावना को विशाल पृष्ठभूमि में स्थापित कर दिया। उनकी भाषा सीधी और सरल थी। ऐसी स्थिति में शताब्दियों से पददलित निम्न जातियों को बंधनों से मुक्त होने की अपार प्रेरणा नानक से मिली क्योंकि कबीर की तरह ही नानक ने भी जाति-प्रथा के विविध पहलुओं पर कसकर प्रहार किया।
प्रायः मध्ययुग के अन्य संतों का संदेश धार्मिक और सामाजिक जीवन तक ही सीमित रहा, परंतु नानक इस दृष्टि की व्यापकता में भी आगे रहे और परवर्ती कालों में प्रभावशाली सिक्ख-संप्रदाय के प्रवर्तक बने। नानक ने जिस धार्मिक आंदोलन का आरंभ किया था उसे उनके अनुयायियों ने आगे बढ़ाया। नानक के प्रभाव से पंजाब की जनता के साथ-साथ देश को भी नयी दिशा मिली तथा समानता, बंधुता ईमानदारी तथा सृजनात्मक शारीरिक श्रम के द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नयी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई।
कबीर, नानक, दादू आदि संतों ने निर्गुण विचार धारा को समस्त भारत में फैलाया। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक सुधार के क्षेत्र में था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से मध्यकालीन निर्गुण संत निम्न वर्ग से संबंध रखते थे और इसी में इनको लोकप्रियता मिली।
Question : मराठा शासकों के द्वारा चौथ तथा सरदेश मुखी की वसूली की व्यवस्था।
(2004)
Answer : ‘चौथ’ किसी भी क्षेत्र से प्राप्त कुल भूमि आय का एक चौथाई होता था। चौथ उस क्षेत्र से वसूला जाता था, जिस क्षेत्र पर मराठा आक्रमण की पूर्ण संभावना होती थी। चौथ देने वाले क्षेत्रों पर ब्राह्य आक्रमण से रक्षा मराठा सैनिक करते थे। चौथ का 3/4 भाग मराठा सरदार ‘सरंजाम’ के रूप में स्वयं के और अपने सैनिकों के खर्च के लिए प्राप्त करते थे। चौथ का 6 प्रतिशत भाग ‘सहोत्र’ (कर) के रूप में पंत सचिव के लिए सुरक्षित कर लिया जाता था। चौथ का 3 प्रतिशत भाग, जो ‘नातगौंदा’ कहलाता था। उसे मराठा राजा अपनी इच्छानुसार वितरित करता था। 16 प्रतिशत भाग राजा स्वयं अपने लिए रखता था। इस भाग को ‘पेशवा’ या ‘प्रतिनिधि’ एकत्रित करते थे।
‘सरदेशमुखी’ नामक कर मराठा राजा को उसके ‘देशस्वामी (देशमुख)’ होने के नाते दिया जाने वाला एक पुराना कर था। ‘सरदेशमुखी’ 10 प्रतिशत भूमि के बराबर होता था, जिसकी वसूली मराठा शासक स्वयं अथवा अपने अधिकारियों के माध्यम से करता था। यह कर उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था, जो मराठा राज्य के बाहर थे और विजय द्वारा मराठा राज्य में सम्मिलित कर लिए गये थे।
वसूली की व्यवस्था में स्थानीय बिचौलियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इनकी संख्या काफी थी। इसलिए काश्तकारों को बहुत से कर्मचारियों से संपर्क में आना पड़ता था। प्रत्येक महल मेंमराठों के दो प्रकार के अधिकारी तैनात होते थे- ‘कामविसदार’ जिनका कार्य चौथ वसूल करना था तथा ‘गुमाश्ता’ जो सरदेशमुखी की वसूली करते थे। इसकी वसूली सीधे काश्तकारों से की जाती थी। वसूली के कागजात पर सरिश्तेदार के हस्ताक्षर भी आवश्यक होते थे।
Question : मुहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित सांकेतिक मुद्रा प्रणाली।
(2004)
Answer : मुहम्मद बिन तुगलक 1327-30 ई. में चांदी के टंके बराबर कांसे के रूप में सांकेतिक मुद्रा को प्रचलन में लाया। इस प्रयोग के संबंध में बरनी का विचार है कि सुल्तान ने विदेश विजय की इच्छा से प्रेरित होकर तथा राजकोष की दयनीय स्थिति के कारण सांकेतिक मुद्रा को प्रचलित किया। परंतु इसमें सत्यता का अभाव हैै। नैल्सन राइट ने सुल्तान के सिक्कों की व्याख्या के आधार पर अपना विचार व्यक्त किया है कि 1327-30 ई. में सांकेतिक मुद्रा जारी होने के समय भारत में ही नहीं, अपितु संसार भर में चांदी की कमी हो गयी थी। अतः सुल्तान ने इस बहुमूल्य धातु को पचाने के लिए तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किये। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के समान रखा गया। यद्यपि 13वीं सदी के अंत में चीन के मंगोल सम्राट कुबलय खां ने चीन में कागज का सिक्का चलाया था तथा फारस के शासक गैखातू ने 1294 ई. में इसका प्रयोग किया था, परंतु मुहम्मद तुगलक का यह प्रयोग असफल रहा। असफलता का प्रथम कारण यह था कि यह समय से बहुत आगे था तथा लोग इसका वास्तविक महत्व नहीं समझ सके। दूसरा, यह कि सुल्तान ने प्रतीक मुद्रा चलाने पर राज्य का एकाधिकार स्थापित नहीं किया तथा नकली सिक्का ढालने के विरुद्ध उचित सावधानी बरतने में असफल रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में जाली सिक्के बाजार में आ गये तथा उसका भारी अवमूल्यन हो गया। फलतः व्यापार एवं व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा। अंततः सुल्तान ने आरंभ करने के चार वर्ष बाद प्रतीक मुद्रा वापस ले लिया। उसने कांस्य सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के देना मंजूर किया। इस प्रकार बहुत से लोगों ने कांस्य सिक्कों को बदल लिया। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची।
Question : इतिहास कार के रूप में कल्हण
(2003)
Answer : भारतीय इतिहास में एक इतिहासकार के रूप में कल्हण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके द्वारा संस्कृति में रचित ग्रंथ ‘राजतरंगिणी’ अपने ढंग की अकेली रचना है। यह संस्कृत में उपलब्ध उन रचनाओं में सर्वाधिक पहली महत्वपूर्ण रचना है जिसमें ऐतिहासकि की विशेषताएं पायी जाती है। इसमें कल्हण ने भू-वैज्ञानिक युग से लेकर स्वयं अपने युग तक के (बारहवीं शदी) कश्मीर के इतिहास का विवरण दिया है। कल्हण ने अपने कृति में केवल एक महान वीर के क्रिया-कलापों का उल्लेख ही नहीं किया बल्कि उसने उस स्थिति को समझने और उनकी व्याख्या करने की कोशिश भी की है जिसमें वे रह रहे थे।
कल्हण एक मंत्री के पुत्र थे तथा ग्यारहवीं सदी में कश्मीर के लोहार वंशीय शासक हर्ष के सलाहकार थे। वे और उन्हें राजनीतिक सत्ता के काफी निकट थे जिससे उन्हें राजनीतिक गतिविधियों को सूक्ष्मता से देखने का मौका मिला था और उन्हें इस क्षेत्र के इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग के शासकों के काल में उन्हें राजकीय संरक्षण नहीं मिला। इन सब तथ्यों का प्रभाव उनकी रचना पर पड़ा और वे प्रशस्ति परक रचना के स्थान पर ऐतिहासिक कृति रचने में सफल रहे।
कल्हण की राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम स्तुत्य प्रयास है। उसके वर्णन में स्पष्टता एवं निष्पक्षता है। अपनी रचनाओं के लिए उन्होंने काव्य की विधा को अपनाया था। इतिहास के द्वारा वे सांसारिक जीवन तथा भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को प्रकट करना चाहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि लोग अपने अतीत की गलतियों से सबक लें। इतिहास से सीख या सबक लेने के लिए उन्हें स्थितियों एवं घटनाओं का विश्लेषण करना पड़ा। यह विश्लेषण ही उनकी कृति को अन्य कृतियों की तुलना में विशिष्ट बना देता है।उन्होंने मंदिरों तथा अन्य अभिलेखों का भी उपयोग किया। इतिहास के तर्क-संगत ड्डोत के रूप में अभिलेखों का उपयोग निश्चय ही एक महान योगदान था। वे सभी महत्वपूर्ण राजाओं (जैसे मौर्य राजाओं) को कश्मीर के शासक के रूप में शामिल कर लेते हैं। इसके बावजूद कोई भी समकालीन इतिहासकार सूक्ष्म अंतर्दृष्टि या महत्ता की दृष्टि से कल्हण की बराबरी नहीं कर सकता।
Question : कबीर और नानक ने भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव छोड़ा था?
(2003)
Answer : संतों की ओर से सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक बा“य आडम्बरों तथा अंधविश्वासों को चुनौती बहुत पुराने समय से मिल रही थी। कबीर और नानक भी इसी परंपरा के प्रमुख संत थे। वे मध्यकालीन निर्गुण भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। भक्ति आंदोलन का उद्भव भी सामाजिक कुरीतियों तथा धार्मिक बा“यों आडम्बरों के विरोध में हुआ था। 14वीं-15वीं शताब्दी के लगभग जन सामान्य की आस्था तथा भक्ति के भीतर से एक व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ जो समस्त भारत में फैल गया। भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक जीवन में यही आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन ने संतों के एक नये वर्ग को जन्म दिया, जिसके अगुआ कबीरदास थे। मध्य युगीनसंतों में कबीरदास की साहित्यिक एवं ऐतिहासिक देन अविस्मरणीय है। वे मात्र भक्त ही नहीं, बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का डटकर विरोध किया। अंधविश्वासों, दकियानूसी, अमानवीय मान्यताओं तथा सड़ी गली रूढि़यों की कटु आलोचना की। कबीर ने जनसाधारण के लिए धर्म की सहजता या भक्ति की सुगमता पर बल दिया। जनसाधारण की ही भाषा में उन्होंने बताया कि निर्गुण प्रभु सबका है, उस पर किसी वर्ग व्यक्ति तथा धर्म जाति का अधिकार नहीं है। कबीर ने जहां एक ओर बौद्धों, सिद्धों और नाथों की साधना और सुधार परंपरा के साथ वैष्णव संप्रदायों की भक्ति भावना को ग्रहण किया वहां दूसरी ओर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक असमानता के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। इस प्रकार मध्यकाल में कबीर ने प्रगतिशील तथा क्रांतिकारी विचारधारा को स्थापित किया।
धर्म के संबंध में कबीर ने अत्यंत महत्वपूर्ण विचार उपस्थित किये हैं। उन्होंने किसी धार्मिक विश्वास को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वह धर्म का अंग बन चुका है, इसके अतिरिक्त अंध विश्वासों, व्रत, ब्राह्मणों के कर्मकांड आदि पर भी जोरदार व्यंग्य किये। उन्होंने पहली बार धर्म को अकर्मण्यता की भूमि से हटाकर कर्मयोगी की भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। कबीर ने मध्यकालीन विषम सामाजिक परिस्थितियों में जाति प्रथा का डटकर विरोध किया और बिखरे हिंदू समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। शुभचिंतक व वक्ता होने के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां कबीर को कठोर-कर्कश जानते हुए भी प्यार से अपनाना चाहती थीं। यह उनके मानवतावाद की विजय थी। कबीर का मानना था कि समाज और राष्ट्र में अधिकतर विवाद अर्थव्यवस्था की असमानता से उपजते हैं। परन्तु धन संचय एवं वैभव की उन्होंने निंदा की तथा लोकहितार्थ धनोपार्जन को श्रेयस्कर बताया। यह एक प्रमुख तथ्य है कि निर्गुण भक्तिधारा में कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे एवं शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को मानव की सफलताओं का आधार बताया। अहंकार को त्याग नश्वर संसार के मायाजाल से विमुख हो भक्ति करने का अभिप्राय प्रस्तुत कर कबीर ने अकसर यह बताया कि कोई किसी का आर्थिक शोषण न कर सके।
कबीर की यह विचारधारा वर्तमान में प्रचलित साम्यवादी विचारधारा के समान थी। आधुनिक काल में साम्यवादी विचाराधारा को मनुष्य की समानता को स्थापित करने के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी विचारधारा माना जाता है। कबीर ने इस विचारधारा को मध्यकाल में प्रचारित एवं प्रसारित किया। कबीर की समाज को यह बहुत बड़ी देन है। कबीर ने युग-युग से पीडि़त समाज के निम्न वर्गों को आत्म सम्मान दिया। उनके द्वारा कही गयी ‘बानिया’ ऐतिहासिक एवं साहित्यिक धरोहर है। यह हमारी संस्कृति की अमूल्य विद्या है।
कबीर के बाद मध्ययुगीन समाज को प्रभावित करने वाले संतों में नानक का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। विचारों एवं सामाजिक आचारों की दुनिया में परिवर्तन लाने वाले गुरु नानक किसी का दिल दुखाये बिना तथा किसी पर आघात किये बिना कुसंस्कारों को नष्ट करने का प्रयास किया। उनका उपचार प्रेम, मैत्री, सहानुभूति और सर्वहित चिंतन था। नानक ने जहां एक ओर मानव के सामाजिक दुखों का अनुभव किया वहां दूसरी ओर अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं को दूर करने का प्रयास भी किया। भेदभाव से ऊपर उठकर उन्होंने हिंदू-मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखा। कबीर की तरह नानक ने भी सीधी बात बात सीधी भाषा में कहा। पंजाब की जनता के साथ-साथ देश को भी नयी दिशा मिली तथा समानता, बंधुता, ईमानदारी तथा सृजनात्मक शारीरिक काम के द्वारा जीवकोपार्जन पर आधारित नयी समाज व्यवस्था स्थापित हुई। उन्होंने पारंपरिक समाज और धर्म की भर्त्सना या विरोध का मार्ग नहीं अपनाया बल्कि आध्यात्मिक साधना वाली भक्ति और सूफी परंपरा की मध्यकालीन भारतीय जीवन तथा सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में व्याख्या की। सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध हिंदू-मुस्लिम एकता और सच्ची पवित्र भक्ति का उन्होंने संदेश दिया। विषम परिस्थितियों में उन्होंने मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को जगाया तथा एक सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में विश्वास द्वारा भक्ति की भावना को विशाल पृष्ठभूमि में स्थापित कर दिया। उनके विचारों में कहीं भी संकीर्णता या क्षुद्रता नहीं थी। ऐसी स्थिति में शताब्दियों से पद्दलित निम्न जातियों को बंधनों से मुक्त होने की अपार प्रेरणा नानक से मिली क्योंकि कबीर की तरह ही नानक ने भी जाति प्रथा के विविध पहलुओं पर कसकर प्रहार किया। प्रायः मध्ययुग के अन्य संतों का उपदेश धार्मिक एवं सामाजिक जीवन तक ही सीमित रहा। परंतु नानक इस दृष्टि की व्यापकता से भी आगे रहे और परवर्ती कालों में प्रभावशालीसिख प्रवर्तक बने।
Question : सूफी आंदोलन
(2003)
Answer : इस्लामी इतिहास में सूफी रहस्यवाद की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी के आस-पास हुई। मुस्लिम रहस्यवादियों का जन्म इस्लाम के अंतर्गत बहुत पहले हो गया था। यही बाद में सूफी कहलाये। सूफी मत इस्लाम में रहस्यवादी विचारों तथा उदार प्रवृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। कुरान के उपदेशों की उदार व्याख्या का आधार तरीकत है जो सूफी मत का आधार है। कलांतर में सूफी मत अनेक संप्रदायों में बंट गया तथा इन संप्रदायों ने संगठित होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने मत का प्रचार-प्रसार किया।
भारत में सूफियों का अगमन तुर्क आक्रमण के काल से ही आरंभ होता है और सूफी संतों में पहला महत्वपूर्ण नाम शेख अली हुज्वीरी है जो महमूद के आक्रमण काल में लाहौर में आकर बस गये। उनका प्रभाव बहुत सीमित था। 12 वीं सदी के अंत में मोईनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी। सूफी आंदोलन के वास्तविक संस्थापक यही थे। चिश्ती संप्रदाय ने धर्म-जाति, संप्रदाय के भेदभाव शासक वर्ग से अपने-आपको अलग रखा। कलांतर में सूफी मत अनेक संप्रदायों में बंट गया इनमें प्रमुख थे- सुहरावर्दी, कादरी, शत्तारी, मदारी एवं नक्शबंदी। 17 वीं सदी तक भारत में 14 प्रमुख सूफी संप्रदाय अस्तित्व में थे।
सुहरावर्दी संप्रदाय पश्चिमी भारत, सिंध तथा पंजाब में केंद्रित था। बिहार में फिरदौसी शाखा का विकास हुआ। सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रमुख संत बहाउद्दीन जकरिया थे। कादरी संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल कादिर गिलानी थे। नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। इस संप्रदाय के संत अपेक्षाकृत अधिक कट्टरपंथी थे। सुहरावर्दी संप्रदाय के संतों ने बाद में शासन का आश्रय लेना स्वीकार कर लिया। दक्षिण भारत में सूफी मत फैलाने का श्रेय शेख बुरहानुद्दीन जकारिया तथा गेसूदराज को जाता है। शेख अहमद सरिहिंदी नक्शबंदी सिलसिला के शेख थे। वे सूफी आंदोलन के सर्वाधिक कट्टर शेख थे। उन्होंने ऐसे रीति-रिवाजों और विश्वासों का विरोध किया जो हिंदुत्व से प्रभावित था। किंतु उनके विचारधाराओं का प्रभाव तत्कालीन राजनीति और समाज पर कम ही पड़ा। जहांगीर ने उन्हें अपने को मुहम्मद साहब से भी बड़ा बताने के लिए बंदी बना लिया था। सूफी आंदोलन ने भारत के हिंदू धर्म पर कुछ प्रभाव भी डाला तथा प्रभाव ग्रहण भी किये। इसने भारत में धार्मिक उदारता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया और उत्तरी भारत में प्रचलित हिंदू परंपराओं को इस्लाम में स्वीकृति दिलायी। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र सूफी संतों का योगदान अविस्मरणीय है। सूफियों की खानकाहों में ही उर्दू भाषा का जन्म हुआ।
Question : मुहम्मद तुगलक के प्रयोग
(2003)
Answer : मध्यकालीन भारतीय इतिहस में मुहम्मद तुगलकअपने नये तथा क्रांतिकारी प्रयोगों के कारण जाना जाता है। उसने पांच योजनाएं बनायी और उनकों पूरा करने का प्रयास किया। परंतु योजनाओं के क्रियान्वयन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाया तथा उस समय प्राकृतिक विपदा आ जाने के कारण उसके प्रयोग सफल नहीं हो पाये। इतिहासकारों के अनुसार वस्तुतः उसके प्रयोग गलत नहीं थे। बल्कि वे समय से आगे थे तथा गलत समय पर किया गया था।
1. राजधानी परिवर्तनः 1327 में मुहम्मद तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरि स्थानांतरित कर दिया तथा उसका नया नाम दौलताबाद रखा। बरनी के कथनानुसार देवगिरि साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। इब्नबतूता के अनुसार सुल्तान दिल्ली-वासियों को सजा देने के लिए ऐसा किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत पर प्रभावशाली ढंग से शासन करने के लिए वह देवगिरि को दूसरी राजधानी बनाना चाहता था। वस्तुतः दक्षिण परिवर्तन ग्रीष्म ऋतु में किया गया इसलिए लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुनः दो वर्ष पश्चात राजधानी दिल्ली को बनाया और दौलताबाद का परित्याग कर दिया।
2. सांकेतिक मुद्रा का प्रचलनः सुल्तान ने 1327-30 में चांदी के टंके के बराबर कांसे के रूप में सांकेतिक मुद्रा को प्रचलन में लाया। यह प्रयोग उसने चीन के सम्राट कुबलय खान द्वारा प्रचालित कागज के मुद्रा के सफल प्रयोग से प्रेरित हो कर किया। चौदहवीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी हो गयी थी। योजना तो अच्छी थी परंतु प्रतीक मुद्रा की ढलाई पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाया, फलस्वरूप नकली मुद्रा की भरमार हो गयी और उसका भारी अवमूल्यन होने लगा और प्रयोग असफल हो गया।
3. खुरासान अभियानः बरनी के अनुसार सुल्तान ने खुरासान तथा इराक पर विजय के लिए 3,70000 सैनिकों को इकट्ठा किया, परंतु उस समय ट्रांसआक्सियाना में राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन और उथलपुथल के कारण योजना का परित्याग करना पड़ा।
4- कराचिल अभियानः मध्य हिमाचल में स्थित कराचिल पर अभियान हेतु सुल्तान खुरासन अभियान के लिए गठित सेना का उपयोग किया। तत्कालीन इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान चीन से लगे इस क्षेत्र पर कब्जा कर सीमा को मजबूत करना चाहता था। परंतु मौसम संबंधी परिवर्तन के कारण अधिकांश सैनिक मारे गये। कहा जाता है कि दस हजार सैनिकों में से केवल दस लोग जीवित लौटे।
5. दोआब में कर वृद्धिः उपरोक्त योजनाओं से साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा इसलिए सुल्तान ने उपजाऊ प्रदेश दोआब में भू-राजस्व की दर को बढ़ा दिया। किंतु दुर्भाग्यवश उसी वर्ष वहां अकाल पड़ गया। अधिकारियों ने जबरदस्ती कर वसूलने का प्रयास किया। परणिामस्वरूप वहां के किसानों तथा वहां बसे सैनिक किसानों ने विद्रोह कर दिया। इससे सुल्तान की अलोकप्रियता बढ़ गयी।
Question : अलबरुनी के लेखनों के प्रकाश में भारतीय विज्ञान एवं सभ्यता पर एक समालोचनात्मक निबंध लिखिए। उसके विवरण से आप कौन से गुण-अवगुण और त्रुटियां पाते हैं?
(2003)
Answer : अलबरुनी मध्यकाल में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरुनी 1017 से 1030 ई- के बीच भारत के जीवन एवं पद्धति का निरीक्षण कर भारतीय विज्ञान एवं सभ्यता के बारे में लिखा। अलबरुनी की अभिरुचि विविध विषयों में थी और भारतीय ज्ञान-विज्ञान की सम्पदा से वह परिचित था। उसने कई भारतीय रचनाओं का अनुवाद पढ़ा था और गणित, विज्ञान, दर्शन, खगोल विद्या ज्योतिष शास्त्र आदि के क्षेत्रों में वह भारतीय ज्ञान की सम्पदा से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। वह लिखता है कि हिंदू दर्शन और विज्ञान यद्यपि बहुत उन्नत दशा में नहीं था, लेकिन वह उसक समय प्रचलित था और आवश्यक भी था। अंक विचार (अंकों के प्रतीकों का प्रयोग) दशमलव प्रणाली एवं शून्य के आविष्कार का उसने उल्लेख किया है। अलबरुनी ने आर्यभट्ट के सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। अरबवासियों ने बीजगणित का ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया था। अलबरुनी ने भास्कर एवं ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों के कार्यों जैसे वर्गमूल, घनमूल तथा द्विघाती समीकरणों का उल्लेख किया है। अलबरुनी के अनुसार गणित की विभिन्न शाखाओं में हिन्दुओं ने खगोल शास्त्र को सर्वोच्च स्थान दिया। आर्यभट्ट ने चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण के कारणों का पता लगाया था। उन्होंने अनुमानों के आधार पर पृथ्वी की परिधिको मापा जो आज भी सही मानी जाती है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वराहमिहिर के अनुसार चन्द्रमा, जो पृथ्वी का एक उपग्रह है पृथ्वी के चारों और चक्कर लगाती है और पृथ्वी स्थिर है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। औषधिशास्त्र के क्षेत्र में आयुर्वेद की पद्वति का उसने उल्लेख करते हुए बताया कि भारतीयों को रोगों के सामान्य तथा शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। भारतीयों को विश्वास था कि विश्व की सृष्टि विभिन्न तत्वों से जैसे-पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से मिलकर हुई है। भारतीयों को सीमित परमाणु ज्ञान था। ध्वनिशास्त्र के क्षेत्र में भी भारतीयों ने महत्वपूर्ण खोजे की थीं। रसायन एवं धातुशोधन का क्षेत्र भारत में प्राचीन काल से ही विकसित था। अलबरुनी ने भारतीय रसायनशास्त्र के ज्ञान का उल्लेख एक अलग पुस्तक में किया है। प्रशंसा के अतिरिक्त वह भारतीयों की आलोचना भी करता था। वह लिखता है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई ऐसा राजा उनके राजा के समान नहीं है तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है।
अलबरुनी ने भारतीयों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। मुख्य रूप से उसने जाति प्रथा, विवाह व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, पारिवारिक और उत्तराधिकार संबंधी नियम, त्यौहार एवं उत्सव, रीति-रिवाज एवं संस्कार तथा सामान्य धारणाओं और अंधविश्वासों की चर्चा की है। उसके अनुसार हिंदू मुसलमानों से पूर्णतः भिन्न थे। सामाजिक दृष्टि से जाति व उपजातियों में बंटे होने से समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य तीक्ष्ण विभाजन था और इससे समाज कमजोर हो रहा था। चार पारंपरिक वर्ग-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के अतिरिक्त एक बड़े वर्ग को ‘अन्त्यज’ पुकारा जाता था।
इन्हें समाज के किसी भी वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं था। उन्हें नगरों और गांवों से बाहर रहना पड़ता था। केवल निर्धारित समय पर ही वे नगर या गांव में प्रवेश कर सकते थे और वह भी केवल सफाई का काम करने के लिए। चीनी यात्री फाहियान ने भी अश्पृश्यों के बारे में ऐसा ही उल्लेख किया। चमार, जुलाहे, मछली पकड़ने वाले, बुनकर, शिकारी आदि इसी वर्ग में सम्मिलित थे। इनकी स्थिति शूद्रों से निम्न थी। वैश्यों और शूद्रों को वेद और धार्मिक शास्त्रें को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यदि वे ऐसा करने का साहस या प्रयास करते थे तो उनकी जबान काट ली जाती थी। छुआछूत की भावना के कारण समाज की दशा और भी शोचनीय हो गयी। समाज में ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा था। ब्राह्मणों के मुख्य कर्तव्य दया दिखाना, दान देना और लेना तथा अध्ययन-अध्यापन और यज्ञ करना था। अलबरुनी के अनुसार प्रत्येक काम में ब्राह्मण का अधिकार है। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता था। केवल ब्राह्मण को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार था।
अलबरुनी के अनुसार समाज में क्षत्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परंतु राजपूतों का उल्लेख नहीं करता है जो ग्यारहवीं में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे। ब्राह्मणों के समान क्षत्रिय भी वेदपाठ करते थे तथा यज्ञोपवीत धारण करते थे। वैश्यों का मुख्य कार्य कृषि, पशुपालन एवं ब्राह्मणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।प्रत्येक वर्ण के लिए अपने निश्चित व्यवसाय से बाहर काम करना अपराध या पाप समझा जाता था। सभी गैर-हिन्दुओं को मलेच्छ माना जाता था।
अलबरुनी भारतीयों के सामाजिक जीवन विविध पक्षों का वर्णन करता है। इसके अनुसार सामान्यतः समाज में पशुवध प्रतिबंधित था। परंतु मांस खाने के लिए कुछ पशुओं का वध किया जाता था। हिंदू समाज में विवाह एक जीवन पर्यंत संबंध था तथा तलाक की कोई परिकल्पना नहीं थी। बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा उच्च वर्गों में विद्यमान थी। स्त्रियों की स्थिति काफी खराब हो गयी थी और उसे सिर्फ पुरुषों के मनोरंजन व विलास की वस्तु ही माना जाता था। विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी। परन्तु अपनी जाति से उपर की जाति की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता था। (प्रतिलोम)। ब्राह्मण सामान्यतः अपनी ही जाति में विवाह करते थे। गर्भाधान, जातकर्म और नामकरण संस्कार प्रचलित थे। अलबरुनी ने रामनवमी एवं शिवरात्री की चर्चा की है। हिंदुओं में परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे एवं हर व्यक्ति बचा हुआ खाना फेंक देता था।
धर्म के संबंध में अलबरुनी ने लिखा है कि हिन्दू धर्म ने परस्पर संपर्क के अभाव में जिसने सामाजिक, व्यवस्था को हिला दिया, अपने ऊपर आवरण को परिष्कृत और परिमार्जित कर लिया है। हिन्दु अनेक देवी-देवताओं की पूजा उपासना करते थें।
प्रशासनिक न्याय के संबंध में अलबरुनी कहता है कि मौखिक आरोपों के साथ लिखित आरोप को स्वीकार किया जाता था, शपथ दिलाई जाती थी और विवादों का साक्ष्यों के अनुसार निर्णय किया जाता था।
अलबरुनी के अनुसार दक्षिण के भारत में लोग ताड़ के पन्नों पर तथा उत्तरी भारत में लोग भोजपत्र पर लेखन कार्य करते थे। अलबरुनी के अनुसार कुल उत्पादन का छठा भाग भू-राजस्व के रूप में लिया जाता था। समस्त श्रमिक, व्यापारी अपनी आय पर कर देते थे।
अलबरुनी की जानकारी केवल शास्त्रें में प्रस्तुत विवरण पर ही आधारित है, जिससे वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है। व्यावहारिक जीवन में इन सिद्धान्तों का सदैव पालन नहीं होता था। अलबरुनी भारत के पश्चिमी भाग में आया था। वहां जो देखा, सुना तथा पढ़ा उसी के आधार पर उसने लिखा। उसने भारत के समाज तथा व्यवस्था का केवल आलोचनात्मक निरीक्षण किया। उसने अधिकांशतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में नकारात्मक विवरण ही दिया है, जबकि समाज में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रवृतियां पायी जाती हैं। उसने भारतीय समाज के सकारात्मक पक्ष को नहीं उभारा है। उसने जाति व्यवस्था का आलोचनात्मक विवरण तो दिया है पर उस समय कायस्थ जाति भी समाज में मौजूद था जिसका उल्लेख उसने नहीं किया है।
Question : हड़प्पा संस्कृति में नगर सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण कीजिये। उसके पतन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे?
(2002)
Answer : हड़प्पा क्षेत्र में होने वाली कृषि अधिशेषों ने यहां नगर सभ्यता को जन्म दिया। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली। नगर मुख्यतः दो भागों में विभक्त थे। उच्च नगर को किला नगर भी कहा गया है सामान्यतः यह ऊंचे टीले या चबूतरे पर स्थित है। यह क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत है और इसके लिए प्रवेशद्वार एवं वाच टावर का भी निर्माण हुआ था। निम्न नगर सामान्यतः छोटे मकानों वाला अधिवासीय क्षेत्र था। उच्च नगर की भांती यहां सार्वजनिक स्थल नहीं है। कई विद्वानों ने इसे इसे मजदूरों का निवास की संज्ञा दी है, हालांकि यह उचित प्रतीत नहीं होता। संभव है यहां श्रमिकों के साथ-साथ छोटे व्यापारी आदि रहते थे।
भवनों के निर्माण में पकी ईंटों का बहुतायत प्रयोग हुआ है। ईंटों की चुनाई अच्छी तरह हुई है। हड़प्पा के स्थापत्य काल में सीढि़यों औरमकानों के कोनों पर स् और ज्प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पावासी दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने ईंटों का प्रयोग शुरू किया। बड़े-बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता हैं। मोहनजोदड़ो में कई सार्वजनिक भवन स्थित थे, यथा- अÂभंडार, पुरोहितवास, मंदिर, स्नानागार आदि।
हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है- जल निकास प्रणाली। घर से निष्कासित जल के लिए कहीं-कहीं ईंटों के बने हुए छोटे शॉकपिट (गड्ढे़)का भी निर्माण किया गया था। घरों से निकलने वाली नालियां, गली की मुख्य नाली से जुड़ी रहती थी और गली की मुख्य नाली शहर की मुख्य नाली से जुड़ी थी। गुजरात में स्थित लोथल का नक्शा बिल्कुल अलग-सा है। यह बस्ती आयताकार थी और चारों तरफ ईंटों की दीवारों का घेरा था। शहर के पूर्वी हिस्से में ईंटों से निर्मित कुंड सा पाया गया है, जिसे बंदरगाह के रूप में पहचाना गया है।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारकों का सूक्ष्म विश्लेषण कर विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। मार्टिमम ह्नीलर पहला इतिहासकार था जिसने इस सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डाला। ब्रिटिश इतिहासकारों का मत था कि जब-जब भारत पर विदेशी जाति का आक्रमण होता था तब-तब भारत का उत्थान होता था और अपने इस तर्क के आधार पर इन विद्वानों ने आर्य आक्रमण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और ऋग्वेद में वर्णित इंद्र जो कि आर्यों के सेनापति थे, को हड़प्पायी सभ्यता का विनाशक बताया। उनका मानना है कि इंद्र का नाम पुरंदर है, क्योंकि वह किलों को ध्वस्त करने वाला है। परंतु, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर आर्य आक्रमण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोहनजोदड़ो से सिर्फ 9 नरकंकाल मिले हैं, जबकि अनुमानतः वहां 35000 लोग रहते थे। युद्ध में प्रयुक्त युद्धास्त्रें के भी प्रमाण नहीं मिलता है और यदि युद्ध होता तो कुछ आर्यों के भी नर कंकाल अवश्य मिलते, पर सभी 9 कंकाल हड़प्पाई लोगों के ही हैं।
फेयर सर्विस ने पारिस्थितिक असंतुलन को इस सभ्यता के ”ास का कारक माना है। उसके अनुसार नगर और ग्राम के लोग इस क्षेत्र की सघन वनस्पति पर आश्रित थे। इन वनस्पतियों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इनका धीरे-धीरे हास होने लगा। इसके कारण पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो गया। पर अनुसंधानों से यह पता चलता है कि वनस्पति संपदा के दोहन के बावजूद जमीन की उर्वरता नहीं गई। फेयर सर्विस का मत कुछ हद तक सही हो सकता है।
जॉन मार्शल जो इस सभ्यता के उत्खनन के सर्वेक्षक थे, ने कहा कि 2500 ई.पू. के उपरांत यहां की अर्थव्यवस्था में एक ठहराव सा आ गया। नगरीय जीवन में 2500 ई.पू. के बाद ज्यादा प्रगति नहीं देखी गयी। वे अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट हो गये। 2250 ई.पू. के पश्चात् तो ऐसा निश्चित तौर पर लगता है कि विघटन के लिए उत्तरदायी कारण जन्म लेने लगे थे। बड़े मकानों का बनना बंद हो गया। मनको के कारखाने बंद हो गये, लिपि का प्रयोग बंद हो गया, माप तौल का मानकीकरण बंद हो गया। नगर नियोजन में भी नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलते हैं।
सारगौन/मेसोपोटामिया के पतन ने सिंधु सभ्यता के आर्थिक हितों को काफी नुकसान पहुंचाया। विदेशी व्यापार वह कारक था जिसने इस कृषि अधिशेष वाली सभ्यता को नगरीय जीवन के उच्चतम आदर्शों तक पहुंचाया था, पर जब वही सभ्यता समाप्त हो गयी तो शिल्पकार, व्यापारी आदि बेकार हो गये और पुनः कृषि की ओर वापस लौट गये। संभवतः हड़प्पा वासियों ने एक संपूर्ण विकसित प्रशासनिक पद्धति का निर्माण नहीं किया था। आर्थिक विखराव की स्थिति में यह प्रशासनिक व्यवस्था भी बिखर गयी।
इस प्रकार विद्वान-जन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विघटन का कोई एक कारक नहीं था, कई कारकों ने मिलकर इस सभ्यता के नगरीय जीवन को ग्रामों की ओर पलायन करने पर मजबूर कर दिया। अंत केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नगरीय जीवन का हुआ उनकी सभ्यता का नहीं, उनके कुछ तत्व आज भी हमारे जीवन में मौजूद हैं।
Question : मनसबदारी व्यवस्था
(2002)
Answer : मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा दिया गया था। यह व्यवस्था मुगल साम्राज्य की सैन्य व सिविल सेवाओं का आधार बनी रही। अकबर के शासन काल के 11वें वर्ष में पहली बार हमें मनसब प्रदान किये जाने का संदर्भ प्राप्त होता है। यह कोई पदवी या पद-संज्ञा नहीं थी, प्रत्युत इसमें मुगल प्रशासनिक सेवा अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता था। इस प्रकार मनसब का अर्थ पद या श्रेणी इस व्यवस्था के मूलभूत तत्वों के अध्ययन का कार्य, सर्वप्रथम, मोरलैंड तथा अब्दुल अजीज ने किया। इनके अनुसार एकल संख्यात्मक पद अकबर के काल के पहले से ही प्रचलित था। जब मोरलैंड को सैनिक टुकड़ी के वेतन की अदायगी के लिए तीन विशिष्ट श्रेणियों का संदर्भ मिला तो उसने इस सूचना को सवार पद के प्रचलन का साक्ष्य माना। प्रथम से जात अर्थात व्यक्ति के वेतन तथा पद स्थिति का बोध होता था जबकि सवार पद से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। सवार पद से मनसब की श्रेणी का बोध होता था। प्रथम श्रेणी के मनसबदार को अपने जात पद के बराबर सैनिकों की व्यवस्था करनी होती थी। द्वितीय श्रेणी के मनसबदार को अपने जात पद से कुछ कम या आधे घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था करनी होती थी जबकि तृतीय श्रेणी के मनसबदार को अपने जात मनसब के आधे से भी कम घुड़सवार सैनिक रखने होते थे।
आइने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख किया गया है। किंतु व्यवहार में 33 मनसब ही प्रदान किये जाते थे। सभी मनसब, यहां तक कि 10/10 जात व सवार भी बादशाह द्वारा प्रदान किये जाते थे। सभी मनसबदारों द्वारा अपने सैनिक दस्तों की व्यवस्था स्वयं ही व अलग-अलग की जाती थी। निम्न श्रेणी के मनसबदारों को उच्च श्रेणी के मनसबदारों के निर्देशन में काम करना होता था किंतु वे उसके अधीन नहीं थे। सबसे बड़ा मनसब 5000/5000 जात व सवार होता था जो राजकुमारों या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में अकबर के उत्तराधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। किंतु जात व सवार पदों की युगल व्यवस्था इसी प्रकार बनी रही। जहांगीर के काल में सवार पद में संशोधन हुआ तथा दु-अस्पा, सिह-अस्पा की व्यवस्था की गयी। इस व्यवस्था द्वारा सवार पद में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करके किसी मनसबदार के पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाती थी। कालांतर में शहजादों के मनसबों को 5000 से बढ़ाकर 20,000 तक कर दिया गया। अकबर के काल से ही यह शिकायत चली आ रही थी कि जागीरों का अनुमानित तथा वास्तविक आय में अंतर होता था अर्थात् जागीरों से होने वाली आय वास्तव में कम होती थी। शाहजहां ने जागीरों की वास्तविक वसूली के आधार पर माहीना जागीरों (शिश माहा, सीमाहा) की व्यवस्था शुरू की। इसके अनुसार यदि किसी जागीर से राजस्व की वसूली 50 प्रतिशत होती थी तो उसको शिशमाहा जागीर माना जाता था तथा वसूली यदि कुल जमा एक-चौथाई होती थी, तो जागीर सीमाही मानी जाती थी।
यह सच है कि मनसबदारों की मुगल साम्राज्य के विस्तार में प्रमुख भुमिका रही थी किंतु यह भी एक सत्य है कि उनके कारण राजस्व ड्डोतों का अपवाह हुआ। मनसबदारों के निर्वाह पर होने वाले व्यय के कारण कृषि उत्पादन अधिशेष की अधिकाधिक वसूली की गई। वस्तुतः काश्तकारों के पास कृषि को उन्नत बनाने या उसका विस्तार करने की संभावना ही नहीं रह गयी थी।
Question : अकबर के शासनकाल की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। शाहजहां ने उनमें क्या परिवर्तन किए?
(2002)
Answer : अकबर के काल में मुगल स्थापत्य को जहां एक नवीन आयाम प्राप्त हुआ, वहीं शाहजहां के काल में यह चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। अकबर काल की प्रथम महत्वपूर्ण इमारत तो वस्तुतः हुमायुं का मकबरा है, जिसमें चार बाग प्रणाली एवं कृत्रिम फव्वारा की योजना के साथ-साथ डबल-डोम का सुंदर प्रयोग हुआ है। यह मकबरा ऊंचे चबूतरे के ऊपर लाल बलुआ पत्थर एवं सफेद संगमरमर के मिश्रित प्रयोग से बना है। इसे शाहजहां कालीन ताजमहल का पूर्ववर्ती भी माना जाता है। अकबर के काल में दिल्ली स्थित ताज-ऊल मनाजिल नामक मस्जिद का निर्माण भी हुआ। इस मस्जिद में अफगान शैली की भांति ड्रम पर स्थित गुंबद का निर्माण हुआ है एवं मस्जिद की मुख्य भिति पर नीले रंग वाले ईरानी टाइल्स का सुंदर प्रयोग हुआ है। अकबर के काल के स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट पक्ष हिदू एवं ईरानी शैलियों का परस्पर सम्मिश्रण था। अकबर ने आगरा के लाल किला का निर्माण कराया एवं उसके मुख्य द्वार पर दो गजारोही राजपूत योद्धाओं की मूर्तियों को प्रतिस्थापित करवाया। इस काल में बने दुर्गों का अब बहुत कम अवशेष ही बचा है। शाहजहां के काल में इस संपूर्ण दुर्ग में व्यापक परिवर्तन करवाये गये। शाहजहां ने वस्तुतः जहांगीरी महल को छोड़कर संपूर्ण महल की स्थापत्य योजना में व्यापक परिवर्तन किये। अकबर के काल में ही इलाहाबाद एवं लाहौर में भी दो सुविशाल दुर्गों का निर्माण हुआ, जिससे स्थापत्य की शक्ति एवं दृढ़ता का पता चलता है। ये महल विशाल वैस्टिमन एवं ऊपरी भाग में कंगूरे से युक्त हैं।
अकबरकालीन भवनों में फतेहपुर सीकरी की वृह्द वास्तु योजना सर्वप्रमुख है। यहां हिद-ईरानी परंपरा का अपूर्व संगम दिखाई पड़ता है। यहां भारत का सबसे बड़ा विशाल आर्क वाले बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया है। पंचमहल की योजना में बौद्ध विहारों की प्रणाली का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
जोधाबाई का महल राजस्थान की क्षेत्रीय हवेली जैसे भवनों वाली योजना को प्रकट करता है। बीरबल का महल यहां की दूसरी प्रमुख संरचना है। यहां की इमारतों में सर्वाधिक सौंदर्यशाली मकबरा शेख सलीमशाह चिश्ती का है।
शाहजहां के काल में भवनों के निर्माण में अपूर्व विशिष्टता आई। एक ओर जहां सफेद संगमरमर का प्रयोग व्यापक रूप से बढ़ गया वहीं दूसरी ओर पिंट्रा-ड्यूरा के प्रयोग में भी व्यापकता आई। अब भवनों की भीतियों को अलंकृत बनाने के लिये बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। पत्थरों की उत्कृष्ट कटाई कर उनके द्वारा भितियों के उपर सुंदर पुष्प सज्जा एवं ज्यामितिक संरचनायें बनायी गयीं। शाहजहां के काल में गुंबद की संरचना और अधिक प्रभावी बन गयी। इस युग की गुंबद को अमरूदी गुंबद कहा जाता है। गुंबद के ऊपर बना अवांगमुखी कमल भी अत्यंत प्रभावी जान पड़ता है। इस काल में स्तंभों का निर्माण भी बड़े सुंदर प्राकार से हुआ। फ्रलुटेड पिलर एवं पायर, जिसका आधार कलश के समान है, शिल्प कला का अत्यंत ही सुंदर उदाहरण है। मेहराब के ऊपर स्पैंड्रल्स भी सौंदर्य की अपूर्व योजना को प्रकट करते हैं। विशेषकर शाहजहां कालीन दांतेदार मेहराब शाहजहां के काल के स्थापत्य के सर्व प्रमुख उदाहरण हैं।
एक ओर जहां अकबर कालीन भवनों में शक्ति एवं दृढ़ता प्रकट होती है, वहीं शाहजहां कालीन इमारत शक्ति एवं सौंदर्य दोनों को ही रूपायित करते हैं। शाहजहां कालीन आगरा एवं लाल किला दोनों का स्थापत्य कई दृष्टियों से एकरूपता रखते हैं। दोनों जगह दीवाने-खास एवं दीवाने-आम जहां वृह्दता को प्रकट करता है दीवाने-खास में लावण्य एवं सौंदर्य की प्रधानता है।
शाहजहां युग मोती मस्जिद, आगरा अलंकरण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वहीं दिल्ली का जामी मस्जिद अलंकरण से ज्यादा संतुलन, सादगी एवं अद्भुत समाकर्षण को प्रकट करती हैं। जामी मस्जिद की गुंबदों में मध्यवर्ती गुंबद सुविशाल है एवं तीनों गुंबदों पर पुष्पालंकरण अत्यंत प्रभावी रूप से हुआ है।
शाहजहां कालीन भवनों में मकबरों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक प्रमुख मकबरा आगरा का ताजमहल हैं। जो श्वेत संगमरमर की अतुलनीय कृति है। इसके चारों कोणों पर मीनारों को बनाया गया है तथा मकबरे की आंतरिक रचना अपने पिंट्रा-ड्यूरा कार्य के कारण प्रभावोत्पादक है।
तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहा जाये तो अकबर का काल मुगल शैली के विकास का प्रारंभिक काल है, जिसमें हिदू-पर्शियन शैली एक नवीन स्वरूप का परिग्रहण करती है, वहीं, सुंदर बल्बर डोम, दांतेदार मेहराब, अलंकृत स्पैंड्रसस, फ्रलुटेड स्तंभ आदि संरचनाओं के साथ शाहजहां कालीन भवन मुगल स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को प्रकट करते हैं।
Question : पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम
(2002)
Answer : उत्तर में मराठों के अलाभकारी अभियानों से क्षुब्ध होकर पेशवा ने सदा शिवराव को उत्तरी अभियान का नेतृत्व सौंपा था। किंतु यह उसकी भूल थी क्योंकि सदाशिव उत्तर की राजनीति तथा युद्ध प्रणाली से परिचित नहीं था। पानीपत के तृतीय युद्ध में राजपूतों की भूमिका तटस्थ थी। सूरजमल से अपमानजनक व्यवहार के कारण उसने जाटों की मित्रता खो दी थी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 29 अक्टूबर 1761 को मराठे और अब्दाली के सैनिक पानीपत के मैदान में आ जमें। इस युद्ध में मराठों ने अपनी परंपरागत युद्ध प्रणाली को भी नहीं अपनाया। पानीपत में युद्ध से हार के कारण मराठों की प्रतिष्ठा को भारी क्षति हुई। पानीपत के मैदान की तबाही कुछ कम हो सकती थी यदि भाऊ ने किसी सुनिश्चित योजना के अंतर्गत काम किया होता या सेना के सभी दस्तों में कुछ सामंजस्य होता। रिजर्व सेना की व्यवस्था किये बिना ही उसने अपनी सारी की सारी सेनाओं को युद्ध की भट्टी में झोंक दिया। इस युद्ध में भाऊ के अतिरिक्त तुकाजी सिधिया, यशवंत राव पवार, पिल्लैजी जादव जैसे 27 महान सरदार, सैकड़ों की संख्या में छोटे सरदार तथा 28,000 मराठा सिपाही काम आए।
बंगाल विजय के पश्चात् अंग्रेजों का ध्यान इस युद्ध की ओर लगा था। अंग्रेजों को लगता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में मराठे सबसे बड़े बाधक हैं। अंग्रेज अभी खुद इतने सबल नहीं थे कि मराठों की लगातार बढ़ती शक्ति को रोक पाते। दिल्ली पर भी मराठों का प्रभुत्व कायम था। अंग्रेज किसी भी कीमत पर मराठों की शक्ति का ”ास देखना चाहते थे। यदि पानीपत के युद्ध में मराठे जीत जाते तो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी सोंच को भारी धक्का लगता। पर मराठों की हार ने अंग्रेजों को वह अवसर प्रदान कर दिया जिसकी ताक में वे बैठे थे। इस युद्ध में मराठों की हार से यह स्पष्ट हो गया कि भारत पर शासन कौन नहीं करने जा रहा है। पानीपत के युद्ध में मराठों के हारने के बाद अंग्रेजों ने मराठों के क्षेत्र में भी दखल देनी शुरू कर दी जिसका परिणाम आंल-मराठा युद्ध थी और अंततः मराठों के पूर्ण समर्पण के बाद भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं बची जो अंग्रेजों को सशक्त चुनौती दे सके।
Question : अकबर के धार्मिक विचारों के विकास की रूपरेखा दीजिये। उसकी सुलहे कुल की नीति पर एक टिप्पणी लिखिये।
(2002)
Answer : इतिहासकारों में अकबर की धार्मिक नीति के स्वरूप तथा प्रेरक उद्देश्यों को ले कर भारी मतभेद है। स्मिथ तथा निजामी के मत में वह पैगंबर का रुतबा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था। अहतर अली के अनुसार अकबर का उद्देश्य एक धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य अभिजात प्रशासक वर्ग में, जिसका गठन विभिन्न जातियों वर्गों तथा धर्मों के लोगों द्वारा हुआ था, संतुलन पैदा करना था। अकबर ने संप्रभुता के एक ऐसे सिद्धांत की स्थापना का प्रयास किया जिसमें भारत की धार्मिक तथा जातिगत विषमताओं का पूरा ध्यान रखा गया था ताकि मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ आधार मिल सके। उस युग में जबकि धर्म और जाति को अलग-अलग रखना प्रायः असंभव ही था, अकबर द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को केवल राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य से ही प्रेरित नहीं माना जा सकता। उसमें धर्म और राजनीति दोनों के ही तत्व विद्यमान हैं, जिनको अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता।
शासन के आरंभिक वर्षों में अकबर राज्य के परम्परावादी इस्लामप्रधान स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता था, पर बाद के वर्षों में उसने तीर्थकर और जजिया कर को हटाकर यह दर्शाया कि वह धर्मों के मध्य भेदभाव नहीं करता था। 1568 में चित्तौड़ विजय को उसने काफिरों के प्रति जेहाद कहा तथा कश्मीर के मीर याकूब को उलेमा की सम्मति से शिया-सुन्नी के आधार पर 1569 में मौत की सजा दी। ये दोनों उदाहरण अकबर के उदार तथा मानवतावादी दृष्टिकोण को गलत ठहराते हैं।
1575 में इबादतखाना की स्थापना का उसका उद्देश्य धार्मिक विषयों पर वाद-विवाद करवाना था। अकबर की रुचि सूफी मत से संबंधित प्रश्नों, विद्वतापूर्ण चर्चा, दर्शन आदि की गूढ़ताओं के विषय में जिज्ञासा-समाधान आदि में अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। इबादतखाने में शुरू में वाद-विवाद केवल सुन्नीमत के इर्द-गिर्द तथा उसके अनुयायियों तक ही सीमित था, किंतु बाद में शिया मत के अनुयायियों को शामिल होने का मौका मिलने लगा। बाद में भारतीय भौतिकतावादी दार्शनिकों तथा संशयवादियों, ईसाइयों, यहूदियों तथा स्त्रियों आदि के लिए भी इबादतखाने के द्वार खोल दिये गये। इबादतखाने में होने वाले वाद-विवाद ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में गहरी भूमिका निभायी। वाद-विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि अकबर की दृढ़ धारणा बन गयी कि ज्ञानी पुरुष सभी-धर्मों में पाये जाते हैं तथा यह भी कि सत्य किसी एक धर्म की व विशेषकर इस्लाम की बपौती नहीं है। अकबर द्वारा धार्मिक व भौतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने का विधिवत कार्य अगस्त-सितंबर 1579 ई. में महजर नामक दस्तावेज द्वारा हुआ। महजर ने अकबर को यह अधिकार दिया कि उलेमाओं में किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में वह साम्राज्य की जरूरतों को ध्यान रखते हुए किसी एक विचार को, जिसे वह सर्वोत्तम समझे, मान्यता दे सकता है।
1579 ई. के वर्ष की घटनाएं अकबर के इस्लाम द्वारा अनुमोदित दायरे के अंतर्गत अपने हाथों में आध्यात्मिक व लौकिक शक्ति सन्निहित करने के निश्चय की परिचायक थीं। अबुल फजल की सैद्धांतिक योजना में अकबर को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया था, जो सांप्रदायिक दायरों से परे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं अकबर ने अपने धार्मिक विचारों का भी अंततः यही निष्कर्ष निकाला होगा। उसके धार्मिक विचारों के नियंत्रण में सूफी मत व सर्वेश्वरवाद का गहरा प्रभाव था। सूफी मत के प्रति अकबर की आस्था का पता इस बात से चलता है कि उसने चिश्ती को प्रश्रय दिया।
1562-79 ई. के मध्य में उसने अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अनेकों बार जियारत की थी। उसने बाद में फतेहपुर सीकरी में भी एक दरगाह का निर्माण कराया था। उसने बाद में फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह का भी निर्माण करवाया था। अकबर के सूफी धर्म के प्रति झुकाव ने ही विश्व के प्रति उसे एक विशद् व उदार दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित किया। अकबर के विचारों का मुख्य आधार यह था कि सभी धार्मिक विषयों में अनुकरण की अपेक्षा तर्क का अधिक महत्व है। उसका विश्वास था कि आस्था तथा आचरण में अंतर के कारण ही धर्मों में भ्रामक विभिन्नताएं पैदा हो गयी हैं। इसलिए उसने हिदुओं की मूर्ति पूजा तथा मुस्लिमों की उपासना के तरीकों की आलोचना की थी। अकबर का विचार एक ऐसी उपासना पद्धति का निर्माण करना था, जो कट्टरपंथी इस्लाम तथा हिदू धर्म की पद्धतियों से भिन्न हो। उसके अनुसार ईश्वर की उपासना का सबसे सच्चा मार्ग एक ऐसे जागरूक हृदय का अधिकारी होना था, जो प्रकाश को से प्रेम करता है।
तौहीद-ए इलाही सर्वेश्वरवाद पर आधारित विचार पद्धति थी जिसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था अर्थात यह कट्टरपंथी इस्लाम तथा हिदू धर्म दोनों के ही प्रभाव से मुक्त थी। इसमें प्रकाश को एकल वास्तविकता का शुद्धतम प्रकट रूप माना गया था। उसने तौहीदे इलाही की सदस्यता केवल उन चंद लोगों के लिए सीमित कर दी, जो उसके विश्वस्त थे। अकबर की व्यक्तिगत धार्मिक विचार पद्धति मुगल साम्राज्य के उदार सिद्धांतों में अर्थात सार्वलौकिक सहिष्णुता (सुलह- ए-कुल) में समाविष्ट हो गयी।
अकबर के धार्मिक विचार तथा संस्थाएं उन समस्याओं के समाधान के रूप में सामने आयीं, जिनका सामना अकबर को मुगल साम्राज्य की स्थापना व सुदृढ़ आधार प्राप्त करने के दौरान करना पड़ा था। उसे एक नयी विचार पद्धति की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा राज्य में धार्मिक तथा जातिगत क्षेत्रों में पक्षपात-रहित नीतियों का प्रतिपादन हो। साथ ही बादशाह के प्रति सामान्य जन के मन में आस्था का भाव उत्पन्न हो। अबुल फजल द्वारा अकबर के विचारों के परिप्रेक्ष्य में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, उनसे उसके उद्देश्य व दृष्टिकोण भली-भांति निरुपित होते थे। इनके द्वारा एक ओर सुलह-ए-कुल या सार्वलौकिक शांति मुगल साम्राज्य की सर्वप्रमुख की नीति बनी रही, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक क्षेत्रों में मुगल पादशाहों व विशेष रूप से अकबर की विशिष्ट स्थिति की भी पुष्टि हुई। नवीन प्रशासनिक प्रणाली के मूल में यही सिद्धांत थे। इनका कार्यान्यन मनसबदारी व्यवस्था के रूप में हुआ जिनमें विभिन्न धर्म, जाति व कुलों के लोग बादशाह के प्रति स्वामिभक्ति के सूत्र में बंध कर एक थे। दूसरी ओर बादशाह भी उनके प्रति भेदभाव-रहित तथा सामंजस्य पूर्ण नीति अपनाने के लिए कट्टिðबध था, उनके धर्म व जातीयता का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं था।
Question : ऐतिहासिक ड्डोत के रूप में बाबरनामा
(2002)
Answer : ऐतिहासिक ड्डोत के रूप में बाबरनामा की महत्ता दो प्रमुख बातों में निहित थी। प्रथमतः बाबर का अपने पूर्वजों एवं अपने निवास फरगना के संदर्भ में विवरण एवं द्वितीय उसका भारत में अनुभव। बाबर ने वस्तुतः अपनी डायरी में अपने अनुभवों एवं मनोदशाओं का वर्णन किया है। उसकी इस डायरी को तुर्की काव्य शैली का एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इसे सामान्यतः तुजुक-ए-बाबरी के नाम से जाना जाता था। जब अकबर के काल में इसका पर्शियन भाषा में अनुवाद हुआ तो इसे बाबरनामा के नाम से जाना गया। विशेष बात यह है कि बाबर ने अपनी डायरी में जीवन की प्रारंभिक कठिनाईयों का वर्णन किया है। साथ ही उसने फरगना के वातावरण एवं प्राकृतिक सौंदर्य को भी उद्धृत किया है। भारत में आना बाबर के लिए विदेश गमन जैसा है। वह यहां की जलवायु, विशेष रूप से गर्म वातावरण की निदा की है। उसे भारत में उद्यानों एवं कृत्रिम फब्वारों का सर्वथा अभाव दिखता है। वह यहां की गरीब जनता को भी देखकर परेशान है। उसे भारतीय लोगों को कम से कम कपड़ों में देखना तथा उनकी शारीरिक संरचना किसी भी प्रकार से आकर्षण का विषय मालूम नहीं पड़ा। बाबर ने अगर किसी भारतीय वस्तु का विवरण प्रस्तुत किया है तो वह है ग्वालियर में बना राजा मान सिह तोमर का दुर्ग। जिसकी मजबूत वास्तु रचना को देखकर बाबर निस्संदेह प्रभावित होता है।
अगर मुगलकालीन राजकीय संरक्षण में लिखे गये इतिहास से बाबरनामा की तुलना की जाये तो इतिहासपरकता इसका प्रमुख विषय जान नहीं पड़ता परंतु यदि एक बादशाह की भारत में अनुभूतियों एवं उसके कवित्व शक्ति की समालोचना का प्रश्न है तो यह रचना निस्संदेह महत्वपूर्ण है।
Question : बलबन के राजत्व की संकल्पना की विवेचना कीजिये। अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें क्या परिवर्तन किए थे?
(2002)
Answer : संभवतः बलबन दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जिसने राजत्व से संबंधित अपने विचारों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। सुल्तान के उच्च पद और शासक के कर्तव्यों के विषय में उसने अपने स्पष्ट व विस्तृत विचार प्रकट किये। राज मुकुट को उच्च व सम्मानित स्तर पर स्थापित करने के लिये यह आवश्यक था कि राजा के पद को अधिक प्रतिष्ठित बनाया जाये। हिदू विद्रोहियों एवं मंगोल आक्रमणों के विरुद्ध एक संगठित शासन की आवश्यकता थी, जिसमें शासक की शक्ति सर्वोपरि और निर्विवाद रूप से स्वीकार की जाए। इल्तुतमिश ने राजा के पद की केवल रूपरेखा खींची थी, परंतु बलबन ने उसे पूर्ण उच्चता व नवीन शक्ति प्रदान की। अपने वसीयत के दूसरे भाग में उसने अपने पौत्रों को राजत्व के संबंध में निर्देश दिये हैं। उसके अनुसार व्यक्तियों के ऊपर शासन करने को एक मामूली और महत्वहीन कार्य न समझो। यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिये। बलबन का राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि ‘नियाबते खुदाई’ माना गया। दिखावटी मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा को बलबन ने राजत्व के लिए आवश्यक बना दिया। वह साधारण व्यक्तियों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। उसने राजा के पद को जीवित रखने के लिए राजकीय प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव और आचार-व्यवहार आदि तत्वों को आवश्यक समझा। वह किसी भी शर्त पर राजत्व के आदर्श की महानता बनाये रखना चाहता था। वंशावली के महत्व पर बलबन ने अत्याधिक बल दिया उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब के वंश से संबंधित घोषित किया। गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद उसने अपनी जीवनचर्चा व आदतों में परिवर्तन किया। अपनी सामाजिक सभाओं में होने वाले नृत्य, संगीत, मद्यपान सभी पर उसने पूर्ण प्रतिबंध लगाया। उसने फारसी परंपरा का अनुकरण करते हुए अपने दरबार में सिजदा और पायबोस को अपनाया, जिसका पालन उन लोगों को पूरी तरह करना पड़ता था, जिन्हें उसके समझ आने का विशेषाधिकार प्राप्त होता था। दरबार में केवल वजीर ही उससे वार्तालाप कर सकता था। बलबन ने कठोरतापूर्वक अपने व्यक्तित्व को अपने राजत्व के लिए बलिदान किया। अपने निजी सेवकों के समक्ष भी वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता था।
बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। उसका उद्देश्य था सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रभुत्व रखना। वह इल्तुतमिश के समान केवल अभिजात वर्ग का मुखिया बनकर रहने से संतुष्ट नहीं था। वह राजा के पद को एक विशेष स्थान प्रदान करना चाहता था, जो अपनी शक्ति व सत्ता के लिए अभिजात वर्ग पर निर्भर न रहकर अपनी व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित हो। उसने जिस निरंकुश राजत्व की नींव रखी थी, उसके लिए सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। उसने सेना में वृद्धि करने के साथ निष्ठावान व योग्य अधिकारी नियुक्त किये। उसके राजत्व की सबसे प्रमुख विशेषता यही थी कि उसने जनहित को शासक का मुख्य कर्तव्य समझ था। शांति और व्यवस्था उसके राजतंत्र के मूल मंत्र थे।
अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष सत्ता प्राप्त करने के पश्चात प्रथम समस्या यह थी कि हड़पे हुए राजत्व को जनता की दृष्टि में उचित सिद्ध किया जाये, जिससे वह उस वास्तविक राजत्व के समकक्ष हो जाये जिसके लिए जनता के हृदय में प्रेम, लगाव व भक्ति थी। यह सोचने-विचारने के बाद ही अलाउद्दीन के समय में राजत्व के सिद्धांत का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। वह जलालुद्दीन एवं कैकुबाद के समान मानवीय प्रवृतियों पर आधारित राजत्व का समर्थक नहीं था। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उसने अपने कार्यों के लिए धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं थी। वह किसी दैव-शक्ति पर आधारित राजत्व नहीं था, वरन ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके।
अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के लिए राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें अलाउद्दीन के राजत्व को न्यायसंगत बनाने और ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया गया। खुसरो के दृष्टिकोण में अलाउद्दीन एक महान विजेता था, परंतु विजेता होने से भी अधिक उसकी महत्ता एक कुशल एवं कर्मठ प्रशासक के रूप में थी। इसी महान गुण ने उसके राजत्व को पवित्रता देनी चाही। अमीर खुसरो ने ईश्वरीय गुणों से समानता देकर उसके पद को पवित्र तथा दिव्य बना दिया। अलाउद्दीन को ईश्वर की छाया माना गया। किंतु यह शरीयत में दिये गये सिद्धांत पर आधारित नहीं था और इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा भी नहीं लिया गया। वह राजनीति में धन के महत्व को समझता था। उसे ज्ञात था कि धन एक ऐसी शक्ति थी जिसका कोई मुकाबला नहीं है। धन का उदारतापूर्वक वितरण कर उसने राजत्व को सुरक्षित व संगठित कर लिया। वह समझता था कि उसका राजत्व जनता के स्नेह और भक्ति के बिना संभव नहीं है। उसे अपने राजत्व को जनता की दृष्टि में पवित्र और न्यायसंगत बनाना था। यही कारण है कि अपने पद के स्थायित्व के लिए अलाउद्दीन ने जनमत का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक समझा। उसने अपने राजत्व को धर्म के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त करने का प्रयास किया और उसे अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। इतना होने के बावजूद जन-कल्याण को सुल्तान ने प्रमुख कर्तव्य माना।
मूलतः अलाउद्दीन का दृष्टिकोण एक मध्यकालीन निरंकुश शासक का था और वह राज्य की राजनीति में धर्मांध उलेमा की सलाहको अव्यावहारिक समझता था। उसके अनुसार राजनीति तथा धर्म बिल्कुल ही भिन्न तथा विपरीत कार्यक्षेत्र हैं। वह जानता था कि वह उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित शासन कर सकता था, जिसे हिदू जनता स्वीकार करती हो। इसी कारण उसने बलबन की जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग किया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। उसने किसी धर्मयुद्ध की कल्पना भी नहीं की और धार्मिक उद्देश्यों पर बल न देकर समयानुकूल और व्यावहारिक शासन व्यवस्था की विवेकपूर्ण ढंग से स्थापना की।
Question : भक्ति आंदोलन का उद्गम
(2002)
Answer : सामान्यतः यह माना जाता रहा है कि भक्ति आंदोलन का उद्गम सूफी सिलसिला के प्रभाव में हुआ। परंतु यह बात सर्व स्वीकृत नहीं है क्योंकि मध्यकालीन भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में देश के पश्चिम सीमा क्षेत्र में सूफी संतों के आगमन के पूर्व हुआ। यह भी माना जाता रहा है कि प्रपति मार्ग वाली भक्ति शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग वाले अद्वैतवादी दर्शन के विरुद्ध एक वैचारिक प्रतिक्रिया थी। यह मत भी केवल आंशिक रूप में ही सत्य प्रतीत होता है क्योंकि रामानुजाचार्य के पूर्व भी दक्षिण में अलवार एवं नयनार संतों ने नालारियम एवं तिरुवासगम जैसे पुस्तकों में भक्तिवादी भावना को सबलता से उद्घाटित किया। नामालवार एवं अप्पार स्वामी जैसे तमिल भक्ति-संतों के गीतों में भक्तिवाद पूर्णतः परिलक्षित होता है। इतना ही नहीं प्राचीन भारतीय ग्रंथों यथा भगवद्गीता एवं श्रीमद्भगवद् पुराण में भक्ति मार्ग की व्यापक चर्चा हुई है। इन्हीं पुस्तकों को वस्तुतः आधार मानकर अनेकानेक कवि-संतों ने भक्तिवादी उपदेश दिये एवं उनकी काव्यधारा भी इन्हीं प्रमुख रचनाओं पर आधारित हैं। भक्तिवादी जयदेव का गीत-गोविन्द भी कल्पना के साथ-साथ श्रीमद् भागवत से अभिप्रेरित है।
दक्षिण में भक्तिधारा को नवीन दिशा यमुनाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य ने दिया जो अद्वैतवादी दर्शन से अलग हटकर जगत को ईश्वर की रचना मानते हुये विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें आत्मा एवं परमात्मा का ऐक्य एक विशिष्ट अवस्था है जिसे भक्ति मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है।
निम्बार्क एवं माध्वाचार्य जैसे संतों ने भी मूलतः भक्तिवादी धर्म का ही प्रचार एवं प्रसार किया। बल्लभाचार्य का पुष्टिमार्ग भक्ति का एक नया स्वरूप था जिसमें उपमा के रूप में भक्त के प्रेम भाव को नार्योचित अनुराग मान लिया गया। उत्तर भारत में भक्तिवादी धारा रामानंद द्वारा प्रचारित हुआ। जिसके शिष्यों ने क्रमशः सांकारोपासना एवं निराकारोपासना के आधार पर सगुण एवं निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। इन दोनों धाराओं के अतिरिक्त कृष्ण एवं राम भी भक्ति के दो प्रमुख आराध्य देव बने। 15वीं शताब्दी के पश्चात भक्ति एक संपूर्ण भारतव्यापी आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ जिसके अलग-अलग क्षेत्रों में उन्नायक चैतन्य, सरलादास, शंकरदेव, सूर, तुलसी एवं विद्यापति जैसे भक्त कवि थे।
Question : क्या राष्ट्रकूट, गुर्जर-प्रतिहार, पाल त्रिकोणात्मक संघर्ष ने उत्तर भारत में राजनैतिक शून्य उत्पन्न करके महमूद गजनवी के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त कर दिया था?
(2001)
Answer : सम्राट हर्षवर्द्धन की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया और उसका स्थान छोटे-छोटे राज्यों ने ले लिया। उत्तर भारत के सम्राट की राजधानी होने का गौरव पाटलिपुत्र के स्थान पर अब कन्नौज ने ले लिया था। आगे भारत के यशस्वी शासकों ने कन्नौज को राजधानी बनाने अथवा उसे अपने अधिपत्य में लेने के लिए संघर्ष किये। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए मुख्यतः तीन वंश के शासकों- पश्चिम भारत के गुर्जर-प्रतिहार, दक्षिण के राष्ट्रकूट तथा पूर्व के पाल वंश में एक त्रिदलीय संघर्ष हुआ। इस त्रिदलीय संघर्ष ने एक तरफ तो इन्हें उत्तर-पश्चिमी सीमा की तरफ ध्यान देने का अवसर नहीं दिया वहीं, दूसरी तरफ तीनों ही दलों ने अपनी शक्ति नष्ट कर ली। इस प्रकार इस त्रिकोणात्मक संघर्ष ने उत्तर भारत में राजनैतिक शून्य उत्पन्न करके महमूद गजनवी के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
कन्नौज को अपने आधिपत्य में लेने का प्रथम प्रयास प्रतिहार शासक वत्सराज (770-805) ने किया। उसका आशय कन्नौज को विजित करकेसंपूर्ण गंगा की घाटी पर अधिकार करना था। कन्नौज का शासक इन्द्रायुद्ध ने वत्सराज के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। उसी समय पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव भी कन्नौज और गंगा की घाटी को अपने अधिकार में करने के लिए उत्सुक हुए। वत्सराज ने धर्मपाल को तो परास्त कर दिया, परन्तु वह ध्रुव से खुद परास्त हो गया। किन्तु ध्रुव को तुरंत ही दक्षिण लौट जाना पड़ा। ध्रुव के वापस चले जाने और प्रतिहारों की शक्ति के दुर्बल हो जाने से धर्मपाल को कन्नौज पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। उसने इन्द्रायुद्ध हो हटाकर उसके भाई चक्रायुद्ध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया, जिसने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। जब नागभट्ट प्रतिहार शासक बना तो उसने अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और निकट के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने धर्मपाल पर भी आक्रमण किया। परंतु नागभट्ट द्वितीय भी अधिक समय तक अपनी सफलता का उपयाोग नहीं कर सका, क्योंकि इसी समय राष्ट्रकूट शासक गोविन्द तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया। चक्रायुद्ध और धर्मपाल ने बिना युद्ध किये ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कन्नौज पर गोविन्द तृतीय का प्रभाव स्थापित हो गया। परंतु गोविन्द तृतीय भी अधिक समय तक उत्तर भारत में नहीं रहा। इस कारण प्रतिहार और पाल शासकों में कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पुनः प्रतिस्पर्धा हो गयी। यद्यपि दोनों में कोई संघर्ष नहीं हुआ और कन्नौज पर संभवतया नागभट्ट का अधिकार हो गया।
धर्मपाल के उत्तरधिकारी देवपाल (810- 850) के शासन काल में यह संघर्ष पुनः आरंभ हो गया। देवपाल ने नागभट्ट द्वितीय को पीछे हटने के लिए बाध्य किया, उत्तर भारत में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित किया तथा नवीन प्रतिहार शासक मिहिरभोज को भी युद्ध में परास्त किया। परन्तु देवपाल के उत्तराधिकारी निर्बल और अयोग्य सिद्ध हुए। पाल शासकों की शाक्ति का विकास एक बार पुनः महिपाल प्रथम के शासनकाल में हुआ, परन्तु कन्नौज के लिए प्रतिद्वंद्वी बने रहने की स्थिति में वे देवपाल के शासन काल के पश्चात कभी नहीं आये। मिहिरभोज ने देवपाल की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर ही नहीं अपितु बिहार पर भी अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। मिहिरभोज ने दक्षिण भारत में भी बढ़ने का प्रयत्न किया, जिसके कारण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से उसका दो बार संघर्ष हुआ। प्रथम युद्ध में उसे सफलता मिली परन्तु इस युद्ध में उसकी पराजय हुई। तब भी मिहिरभोज ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।
इस प्रकार गांगेयघाटी और कन्नौज को अधिकार में करने के प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों में जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ उसमें प्रतिहारों को सफलता प्राप्त हुई। निस्संदेह राष्ट्रकूट शासक इन्द्र तृतीय ने 915 से 918 ई. के मध्य एक बार पुनः उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासक महिपाल को परास्त किया और कन्नौज को भी लूटने में सफलता पायी, परन्तु सदैव की भांति राष्ट्रकूटों की यह सफलता भी अस्थायी रही। उत्तर भारत में वे और अधिक न बढ़ सके।
इस संघर्ष का अन्तिम परिणाम पाल वंश का बंगाल तक सीमित हो जाना तथा प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की शक्ति का दुर्बल हो जाना था। दसवीं सदी के प्रारंभिक काल में ही ये तीनों राजवंश पर्याप्त दुर्बल हो गये थे, जिसका परिणाम इन तीनों का पतन और भारत का विभिन्न राज्यों में बंट जाने के रूप में सामने आया। प्रतिहारों के पश्चात उत्तर भारत को एक साम्राज्य में संगठित करने का प्रयत्न भी किसी ने नहीं किया, जिसका लाभ 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करके उठाया।
Question : क्या मराठे भौगोलिक-राजनीतिक सीमाओं के कारण भारत की सार्वभौम शक्ति बनने में असमर्थ रहे?
(2001)
Answer : मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठे सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रीय शक्ति बनकर उभरे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ (1713-20) ने दक्कन में मराठा शक्ति को सुदृढ़ किया, जबकि उसके उत्तराधिकारी बाजीराव (1720-40) ने मराठा संघ के अन्य शक्तिशाली सरदारों, जिन्होंने अपने लिए स्वतंत्र राज्य बना लिये थे, की सशक्त हिस्सेदारी से मालवा और गुजरात को जीत लिया; वे मराठा सरदार थे- नागपुर के राघोजी भोंसले, बड़ौदा के पिल्लाजी गायकवाड़, इंदौर के मल्हार राव होल्कर और ग्वालियर के राणोजी सिंधिया। मराठा सेनाएं दिल्ली के दरवाजों पर गरजती थीं और उत्तर-पश्चिम भारत को रौंदती थीं। सन् 1740 ई. में बाजीराव की मृत्यु के पहले ही मराठा पताका कृष्णा से सिंधु तक लहरा रही थी। मराठों का दुर्भाग्य ही था कि अहमद शाह अब्दाली ने उन्हें 1761 ई. में पानीपत की तीसरी लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया और प्रतापी मुगलों के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने के उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा शक्ति के पतन को रोकने का अंतिम प्रयास पेशवा माधव राव (1761-72) ने किया।
उसने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। हैदरअली को नजराना देने के लिए बाध्य किया। दक्षिण भारत में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के बाद उसने उत्तर भारत के रूहेला सरदारों, राजपूत राजाओं और जाटों को भी पराजित किया। 1771 में उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। उसने नागपुर के जानोजी भोंसले और इन्दौर की रानी अहिल्या बाई पर नियंत्रण बनाये रखा और महादजी सिंधिया पर भी अपनी औपचारिक संप्रभुता बनाये रखी। किन्तु माधव राव के बाद कोई भी मराठा शासक इतना सशक्त नहीं हो पाया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मराठा शक्ति का पतन होने लगा, जिस कारण भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। मराठा शक्ति के पतन के लिए कई कारण उत्तदायी थे।
कई इतिहासकारों का मानना है कि मराठे अपनी भौगोलिक राजनयिक सीमाओं के कारण भारत की सार्वभौम शक्ति बनने में असफल रहे। मराठों का मूल निवास क्षेत्र ‘मराठवाड़’ एक त्रिभुजात्मक भू क्षेत्र है, जो भारत के पश्चिमी सागर तट पर स्थित है। इसकी एक सीमा सहयाद्रि पर्वतमाला और दमन के कारवाड़ तक सागर तट पर विस्तृत है। दूसरी सीमा नागपुर तक सतपुरा पर्वतमाला और गोदावरी के रूप में तथा तीसरी सीमा नागपुर से कारवाड़ तक विस्तृत क्षेत्र के रूप में देखी जा सकती है। इसे तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है- (1) सहयाद्री पर्वत से दक्षिण तटवर्तीभाग, जो कोंकण कहलाता है। (2) सहयाद्री का पर्वतीय क्षेत्र जो मालवा कहलाता है। (3) पूर्व का मैदानी क्षेत्र जो देश कहलाता है। इस क्षेत्र में समुद्र तट और पश्चिमी घाट के क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग जंगलों और पहाडि़यों से भरा है। इसलिए इस क्षेत्र में कृषि कार्य कठिन था।
अतः मराठे अपनी आजीविका के लिए शांतिपूर्ण उपायों पर ही निर्भर नहीं रह सकते थे। प्राकृतिक कठिनाइयों ने एक ओर उनमें साहस, कठोर परिश्रम, आत्म संयम जैसे गुणों का विकास किया तो दूसरी ओर वे पड़ोस के उर्वर क्षेत्रों को लूटने और वहां से धन अर्जित करने पर बाध्य हुए। इन लूटमार के अभियानों ने मराठों में सैनिक प्रतिभा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मराठों द्वारा छापामार युद्ध नीति का प्रयोग भी सफल ढंग से हुआ। भौगोलिक परिस्थितियों ने मराठों में एकता की भावना भी जगायी। किन्तु जब मराठों ने साम्राज्य विस्तार का सिलसिला शुरू किया तो उनकी शक्ति क्षीण पड़ने लगी। आरंभ में मराठों ने दक्कन में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। पेशवाओं के प्रभुत्व काल में विशेषकर बाजीराव प्रथम के अधीन मराठों ने मध्य भारत और उत्तर की ओर विस्तार प्रारंभ किया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दक्कन में अपनी सत्ता पूरी तरह सुदृढ़ किये बिना ही मराठे उत्तर में विस्तार करने लगे। उत्तर भारत में तो वे अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं पर पाये जबकि दक्कन में भी उनके विरुद्ध शक्तियां संगठित होने लगीं और कालांतर में उनकी शक्ति का आधार दोनों ही क्षेत्रों में कमजोर बना रहा।
उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार के प्रयास ने मराठों को कुछ नयी समस्याओं में उलझाया। अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक वे राजपूताना, बुंदेलखंड, मालवा, गुजरात आदि को जीतते हुए मुगल दरबार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की अवस्था में आ गये। थे। 1752 में एक संधि के द्वारा उन्होंने मुगल सम्राट से पंजाब की सुरक्षा का दायित्व भी ग्रहण कर लिया था। उस समय पंजाब पर काबुल का शासक अहमद शाह अब्दाली भी अधिकार करने का इच्छुक था।
अतः मराठा शक्ति का पंजाब तक विस्तार उसके लिए अप्रिय था। मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव से मुगल दरबार के अनेक सामंत भी असंतुष्ट थे। इन लोगों ने भी अहमदशाह अब्दाली को मराठों पर चढ़ाई करने के लिए आमंत्रित किया। फलतः 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमदशाह अब्दाली के हाथों मराठों की निर्णायक हार हुई। मराठों की सैनिक शक्ति को भीषण क्षति पहुंची और भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका अब निर्णायक नहीं रही। मराठों को राष्ट्रीय मोर्च पर असफल होना ही था, क्योंकि वे पूरे देश पर मराठों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। उनके नेताओं ने राजपूतों, जाटों और सिक्खों जैसे नये उभरते राजनीतिक बलों का समर्थन पाने अथवा उनके साथ सहयोग करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार मराठे अपनी भौगोलिक-राजनयिक सीमाओं के कारण भारत की सार्वभौम शक्ति बनने में असमर्थ रहें, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उन्हें उत्तर और दक्षिण दोनों ही जगहों पर सशक्त विरोध का सामना करना पड़ता था।
उपर्युक्त कारणों के अलावा इतिहाकारों ने मराठों की अन्य कई कमजोरियों की तरफ इंगित किया है। जैसे- सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था को विकसित करने का पर्याप्त उपाय नहीं करना, पड़ोसी भारतीय शासकों से संबंध न सुधारना आदि। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मराठा सरदारों की अदूरदर्शिता और राजनैतिक परिपक्वता के अभाव ने ही मराठा शक्ति को मुगलों का उत्तराधिकारी बनने से रोक दिया।
Question : समसामयिक अर्थ-व्यवस्था एवं समाज पर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।
(2001)
Answer : अलाउद्दीन द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लागू किये गये, जिनका संबंध राजस्व प्रणाली एवं व्यापार-वाणिज्य से था। अलाउद्दीन द्वारा आर्थिक सुधारों को अपनाने की प्रेरणा उसके राजनैतिक सिद्धांत में निहित थी। वह बाह्य नीति में साम्राज्य विस्तार और आंतरिक नीति में शक्तिशाली शासन प्रबंध का इच्छुक था। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति आर्थिक सुधारों के बिना संभव नहीं थी। उसके आर्थिक सुधारों में सबसे विलक्षण और महत्वपूर्ण उसकी मूल्य निर्धारण योजना या बाजार नियंत्रण की नीति मानी जाती है। इतिहासकारों में इस योजना के उद्देश्य, क्षेत्र एवं प्रभाव के संबंध में मतभेद हैं।
इस योजना के संबंध में मुख्य रूप से जानकारी बरनी की ‘तारिख-ए-फिरोजशाही’ में मिलती है। बरनी के अनुसार यह योजना सैनिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर लागू की गयी थी। अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार के लिए विशाल सेना संगठित की थी। इस सेना पर होने वाले खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर दिया था। अतः यह आवश्यक था कि इसी निर्धारित वेतन में ही सैनिकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अतः वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना आवश्यक हो गया था। इसके विपरीत अमीर खुसरो की रचना ‘ख्वाजाएनुल फतुह’ के अनुसार अलाउद्दीनका उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। इसकी पुष्टि ‘खैरुल मजलिस’ से भी होती है। बरनी की एक अन्य रचना ‘फतवा-ए-जहांदारी’ में भी शासक को दिये जाने वाले सुझावों में जन कल्याण के लिए मूल्यों को निर्धारित करने का सुझाव शामिल है।
इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने इस योजना का उद्देश्य मूल्य वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति की समस्या पर नियंत्रण करना बताया है। यह भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन अपनी निरंकुश शासन प्रणाली को सुदृढ़ आधार देना चाहता है, जिसके लिए प्रजा को आर्थिक रूप से राहत देना अनिवार्य था, ताकि वे अपने राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों पर हो रहे आक्षेप पर आपत्ति न करें। इन विभिन्न विचारों में सैनिक आवश्यकता से प्रेरित योजना का विचार ही अधिक मान्य है। इतिहासकारों में इस पर भी विवाद है कि इस योजना को केवल दिल्ली में लागू किया गया या साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी। बरनी के विवरण से स्पष्ट होता है कि यह योजना केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू हुई थी।
अलाउद्दीन ने अनेक उपायों द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया और अपने शासन काल की पूरी अवधि में इनमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होने दी। यह एक प्रशंसनीय सफलता थी। इस व्यवस्था से सामान्य जन को क्या लाभ हुआ या यह योजना सभी वर्गेां के लिए किस हद तक लाभदायक सिद्ध हुई, इस पर मतभेद हैं। इस सन्दर्भ में अमीर खुसरो स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि इस योजना का लाभ समस्त प्रजा को हुआ। खैरुल मजलिस से भी स्पष्ट होता है कि आम प्रजा सुखी थी। मोहम्मद हबीब ने भी इस योजना को सभी वर्गों के लिए हितकारी माना है, क्योंकि अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिये थे तथा मुनाफाखोरों और बेइमान व्यापारियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था कर दी थी। यदि किसी को निर्धारित मूल्यों पर सामान बेचना होता था तो उसे कोई हानि नहीं थी, क्योंकि उसे अन्य समान निर्धारित मूल्य पर प्राप्त हो रहे थे। ऐसी स्थिति में क्रय शक्ति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी स्मरणीय है कि मूल्यों का निर्धारण मनमाने या अत्याचारपूर्ण ढंग से नहीं, बल्कि उत्पादन के लागत के अनुसार किया गया था। हां, यह सत्य है कि मुनाफा की दर न्यूनतम कर दी गयी थी। अतः यह कहना कि इस योजना से व्यापारियों, शिल्पियों और किसानों का शोषण हुआ, सही नहीं है।
इरफान हबीब ने बरनी के वर्णन के आधार पर अलाउद्दीन के उपायों से उत्पन्न धन के अभाव की समस्या की ओर संकेत किया है। उन्होंने अलाउद्दीन और उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल की परिस्थितियों की तुलना करते हुए स्पष्ट किया है कि मुबारक की तुलना में अलाउद्दीन के समय मजदूरी की दर एक-चौथाई थी। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन के समय में सामंतों, सैनिकों, बड़े अधिकारियों और धनी व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के पास धन नहीं था। मूल्यों में गिरावट से इनकी क्रयशक्ति में वृद्धि हुई, जबकि मजदूरी पर आश्रित वर्ग कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सका। इरफान हबीब के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को राहत पहुंचाने से अधिक सैनिक खर्च में कमी लाकर राजकोष की स्थिति को संपन्न बनाये रखना था। उनके अनुसार सैनिक कार्यों पर देने वाला खर्च मुख्यतः मूल्य निर्धारण से प्रभावित क्षेत्र में ही रहा था, अतः मूल्यों में गिरावट से इस खर्च की मात्र में कमी लायी जा सकती थी। दूसरी ओर मूल्य निर्धारण से अप्रभावित क्षेत्र से राज्य को जो धन प्राप्त हो रहा था, उसके वास्तविक मूल्य में वृद्धि हुई। इससे राज्य को पर्याप्त बचत हुई और राजकोष की स्थिति सुदृढ़ हुई।
कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि अलाउद्दीन का उद्देश्य केवल सैनिक और सामंत वर्ग को ही संतुष्ट रखना था, ताकि इनके समर्थन से वह अपनी निरंकुश सत्ता को मजबूत बना सके। उसने सभी वर्गों के शोषण पर इस व्यवस्था को विकसित किया और किसान, शिल्पकार एवं व्यापारी इससे असंतुष्ट रहे। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अलाउद्दीन के इन उपायों का उद्देश्य केवल दिल्ली की प्रजा को संतुष्ट करना था, ताकि वे उसके निरंकुश शासन के विरुद्ध आवाज न उठायें। इसके लिए उसने सभी समीपवर्ती क्षेत्रों की प्रजा का शोषण किया।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल्य निर्धारण की योजना अलाउद्दीन खिलजी की एक विशिष्ट उपलब्धि थी, जो उसकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत करती है। इस योजना के लिए उसकी प्रशंसा समकालीन, मुगलकालीन और आधुनिक इतिहासकारों ने भी की है। दुर्भायवश यह सारी उपलब्धि एक व्यक्ति की प्रतिभा पर आधारित थी और उस व्यक्ति अर्थात अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात इस योजना का कार्यान्वयन कारगर रूप से संभव नहीं रहा।
Question : शंकराचार्य का वेदान्त
(2001)
Answer : पूर्व मध्य कालीन भारत में हिन्दू धर्म और दर्शन के क्षेत्र में जिन लोगों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें आदि शंकराचार्य सबसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने वेदान्त दर्शन की एक नयी व्याख्या प्रस्तुत की और उसके माध्यम से बौद्ध धर्म और दर्शन द्वारा प्रस्तुत चुनौती का न केवल तार्किक निदान प्रस्तुत किया, बल्कि हिन्दू धर्म के जीर्णोद्धार में तथा उसे व्यापक लोकप्रियता प्रदान कराने में निर्णायक योगदान दिया। अपने 32 वर्ष के छोटे से जीवन काल में ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं और अपने धार्मिक दर्शन एवं विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए सारे भारत का भ्रमण किया और चार प्रमुख मठों की स्थापना की। इन मठों के माध्यम से उनके विचारों का प्रचार-प्रसार उनके मरणोपरांत भी होता रहा। उन्होंने उपनिषदों में प्रस्तुत धार्मिक दर्शन को एक नयी व्याख्या प्रदान की। यह दर्शन ‘वेदान्त दर्शन’ कहलाया और इसकी प्रस्तुत व्याख्या ‘अद्वैतवाद’ कहलायी। शंकराचार्य द्वारा उपनिषदों तथा भागवद्गीता पर अनेक भाष्यों की रचना की गयी। उन्होंने ‘ब्रह्मसूत्र’ को अपने दर्शन का आधार माना जो उनके अद्वैत सिद्धांत का आधार है। उनकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत थी और उनके विचार तार्किक एवं सुस्पष्ट थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की शब्दावली को अपनाया और उसी के सन्दर्भ में वेदान्त दर्शन की पुनर्व्याख्या की।
शंकराचार्य ने यह माना कि वेदों और उपनिषदों में जो ज्ञान प्रस्तुत हुआ है, वही वास्तविक ज्ञान है। उन्होंने संसार के अस्तित्व को तीन तत्वों पर आधारित माना जो ‘सत, चित और आनंद’ थे। ये तीनों अनन्त ब्रह्म से जुड़े हैं। ब्रह्म ही सत्य है और यही अस्तित्व का आधार है। चित्र चेतना है और आनन्द सांसारिक अनुभूतियां हैं। शंकराचार्य के अनुसार मानवात्मा का परमात्मा ब्रह्म या सत्य का ही एक अंग है, परन्तु इससे पृथक होकर मानव आत्मा एक जीवन या प्राणी का रूप धारण कर लेती है।
अज्ञानता के कारण जीव इसी पृथक् अस्तित्व को अर्थात सांसारिक जीवन को सत्य या वास्तविकता समझ लेता है। यद्यपि सांसारिक जीवन एक मिथ्या या माया है, जिसका वास्तविक अस्तित्व कुछ भी नहीं। पुनः अज्ञानता के ही कारण सांसारिक जीवन से लगाव और सांसारिक इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। इन्हीं इच्छाओं से तृष्णा उत्पन्न होती है, जिस कारण मानवात्मा पुनर्जन्म के बंधन में बंधी रहती है। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो तो वह शास्त्रें के अध्ययन से ही हो सकती है, और मोह की प्राप्ति तभी संभव है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति से संसार के मायावी रूप और ब्रह्म से मानवात्मा का अनिवार्य संबंध स्पष्ट हो जाता है। तब सांसारिक इच्छाओं का अंत हो जाता है और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है; बूंद सागर में मिलकर अमरत्व प्राप्त कर लेती है यही मोक्ष की प्राप्ति है।
शंकराचार्य केवल दार्शनिक तथ्यों को प्रस्तुत करने वाले विचारक ही नहीं, बल्कि एक सक्रिय धर्म प्रचारक भी थे। उन्होंने भारत के विस्तृत क्षेत्र की यात्र की और तर्क-वितर्क द्वारा अनेक विद्वानों को अपने विचारों से प्रभावित किया। वे महान संगठनकर्ता भी थे। उन्होंने दक्षिण भारत मेंशृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और उत्तर में बद्रीनाथ सहित चार पीठों की स्थापना
की जो आज भी सक्रिय हैं। इस प्रकार वैचारिक से व्यवहारिक स्तर पर हिन्दू धर्म को पुष्टि प्रदान करने में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा।
Question : सवाई जयसिंह ज्योतिषाचार्य।
(2001)
Answer : अपने पिता किशन सिंह की मृत्यु के पश्चात 1700 ई. में जयसिंह शासक बना। 12 वर्ष की उम्र में जब वह सिंहासन पर बैठा ही था, औरंगजेब ने उसे दक्षिण भारत बुला भेजा। दक्षिण भारत के युद्धों में साहसपूर्वक भाग लेने के कारण उसे मालवा का नायब सूबेदार बनाया गया। बादशाह जहांदारशाह ने 1712 ई. में जयसिंह को मिर्जा राजा का पद दिया। 1713 ई. में बादशाह फर्रुखसियर ने इसे ‘सवाई’ का पद और मालवा की सूबेदारी दी। उस समय से वह सवाई राजा जयसिंह के नाम से विख्यात हुआ। 1743 ई. में जयसिंह की मृत्यु हुई। जयसिंह तत्कालीन राजपूत शासकों में सर्वाधिक योग्य साबित हुआ और उसने अपने राज्य के सम्मान और शक्ति को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। राजनीतिक सफलता के अतिरिक्त जयसिंह ने अपने समय में सांस्कृतिक विकास में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। वह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था। परंतु सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में चमका। ध्यान रहे कि जिस युग में वह था, उसमें अधिकांश भारतीयों को वैज्ञानिक प्रगति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने जाटों से लिए गये इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का महान केंन्द्र बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर और एक नियमित योजना के तहत हुआ। उसकी चौड़ी सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती है।
जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोलशास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनवायी। कुछ उपकरण तो खुद जयसिंह ने स्वयं बनाये थे। उसके खगोलशास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण आश्चर्यजक रूप से सही होते थे। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोलशास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिली। इसका नाम जिन मुहम्मदशाही था। उसने युक्लिड की ‘रेखागणित के तत्व’ का अनुवाद संस्कृत में कराया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघुगणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपीयर की रचना का भी अनुवाद संस्कृत में कराया। उसके द्वारा निर्मित वेधशालाएं आज भी देखी जा सकती हैं। उसने अपने दरबार में हिन्दू, मुसलमान और विभिन्न यूरोपीयन विद्वानों को एकत्र किया। उसके शासन काल के प्रारंभिक वर्षों में एक प्रसिद्ध विद्वान भट्ट पौंडरिक थे। उनके भतीजे ब्रजनाथ भट्ट भी एक प्रमुख विद्वान हुए। उसके समय में प्रमुख विद्वानों में श्री कृष्ण भट्ट, हरिकृष्ण, मायाराम, जगन्नाथ, प्रियदास, केवलराम आदि थे। इन विद्वानों ने ज्ञान के सभी क्षेत्रों की उन्नति में सहयोग दिया। जयसिंह ने सामाजिक कुरीतियों को रोकने का भी प्रपबंध किया।
इस प्रकार जयसिंह ने अनेक कठिनाइयों और राजनीतिक दावपेंचों में व्यस्त रहते हुये भी भारत की सांस्कृतिक प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दिया। इस कारण, उसका स्थान अपने समय के राजस्थान के शासकों में ही नहीं, अपितु भारत के योग्यतम शासकों में आता है।
Question : शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष
(2001)
Answer : भारत में मुगल स्थापत्य काविकास वास्तव में अकबर के साथ ही आरंभ हो सका। यद्यपि बाबर और हुमायूं द्वारा कुछ भवनों का निर्माण हुआ, परन्तु उनकी शैली में कोई विशिष्टता प्रतीत नहीं हुई। यद्यपि अकबर के काल में ही स्थापत्य की एक नयी शैली का पूर्ण विकास हो चुका था, तथापि इसकी क्रमिक उन्नति जहांगीर एवं शाहजहां के काल में हुई और शाहजहां के अधीन मुगल स्थापत्य कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। यह स्थापत्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, किन्तु उसके बाद पतन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल स्थापत्य कला का भी पतन हो गया।
शाहजहां के शासन काल में मुगल स्थापत्य कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गयी। शाहजहां को भवनों का निर्माण करने में विशेष रुचि थी और उसने स्थापत्य कला को अत्यधिक प्रश्रय दिया। आगरा और दिल्ली में उसके द्वारा अनेक भवनों का निर्माण कराया गया। अकबर की इमारतों की तुलना में शाहजहां की इमारतें चमक दमक एवं मौलिकता में घटिया है, परन्तु अति व्ययपूर्ण प्रदर्शन एवं समृद्ध और कौशलपूर्ण सजावट में बढ़ी हुई है, जिससे शाहजहां की वास्तुकला ‘एक अधिक बड़े पैमाने पर रत्नों के सजाने की कला बन जाती है।’
आगरा में निर्मित भवनों में दीवाने खास, रंग महल, शीश महल, नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज एवं मोती मस्जिद अधिक विख्यात हैं। ये सभी आगरे के किले में स्थित है।
दिल्ली में उसके द्वारा निर्मित भवनों में जामा मस्जिद तथा लाल किला प्रमुख हैं और उसने लाहौर में भी अनेक भवन बनवाये हैं, जो अपनी सुन्दरता एवं सजीवता के लिए प्रसिद्ध हैं।
शाहजहां का शासनकाल संगमरमर के भवनों का काल है। राजपूताना, मकराना एवं बलुचिस्तान से उपलब्ध सफेद संगमरमर का उपयोग अब भवन निर्माण सामग्री के रूप में होने लगा। इसी के साथ भवनों की सजावट की कला में भी परिवर्तन आया। अब संगमरमर में रंगीन पत्थरों को भरकर सजावट का काम किया जाने लगा। इस कला को पितरा-दुरा कहा जाता है। इसका पहला उपयोग एत्मादुदौला के मकबरे में हुआ है। अधिकतर फूल-पत्तियों की डिजाइनों को बनाकर भवनों को सजाया गया। इसी काल में कई स्तरीय मेहराबों का निर्माण प्रारंभ हुआ। एक मेहराब में सात या नौ छोटी मेहराबों का निर्माण हुआ, इसका उदाहरण लाल किले के दीवाने खास में है। इस काल में गुम्बद की कलाकारी भी अधिक सुन्दर हो गयी, जो कि ईरानी प्रभाव का परिणाम थी। इस काल की सबसे महान उपलब्धि आगरा का ताजमहल है। इसे शाजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र पर बनवाया। कई इतिहासकार ताजमहल की योजना और डिजाइन को ‘यूरोपीय और एशियाई प्रतिभा के सम्मिश्रण की उपज’ मानते हैं जबकि कई इतिहासकार इसका श्रेय उस्ताद इसा को देते हैं। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग शाहजहां के साथ ही समाप्त हो जाता है।
Question : क्षेत्रीय भाषाओं एवं जन-सामान्य के लिए जीवन एवं चिंतन पर सूफी एवं भक्ति आन्दोलनों के प्रभाव की समीक्षा कीजिये।
(2001)
Answer : मुस्लिम आक्रमणों के साथ इस देश में ऐसे निश्चित सामाजिक एवं धार्मिक विचारों ने प्रवेश किया, जो मौलिक रूप से भारतीय विचारों से भिन्न थे। जब कभी दो सभ्यताएं सदियों तक एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ संपर्क में आती हैं, तब दोनों का एक-दूसरे से प्रभावित होना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार लंबी अवधि तक संसर्ग, स्वधर्म छोड़ मुसलमान बनने वाले भारतीयों की संख्या वृद्धि हुई तथा भारत में अनेक उदार आन्दोलनों के प्रभाव वफ़े कारण हिन्दू तथा मुस्लिम समुदायों ने एक-दूसरे के विचारों तथा रीति-रिवाजों को अपना लिया। तूफान और दबाव के आंदोलित धरातल के नीचे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक एकता एवं सहिष्णुता की सुखद धारा बहने लगी। इस काल की प्रमुख विशेषता थी मुसलमानों में सूफी संप्रदाय तथा हिन्दुओं में भक्ति आन्दोलन की प्रगति। इन दोनों ही धाराओं ने भारतीय जन जीवन के सभी पक्षों धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, कला, साहित्य आदि को प्रभावित किया।
मध्यकालीन भारत में सामाजिक-धार्मिक जीवन के क्षेत्र में एक नयी और महत्वपूर्ण चेतना का विकास हिन्दू समाज में हुआ, जिसकी मूल प्रेरणा भक्ति के सिद्धांत से ली गयी थी। इसे भक्ति आन्दोलन कहा जाता है। अपने पहले चरण में यह आन्दोलन मूल रूप से एक धार्मिक आन्दोलन था जिसका उद्देश्य हिन्दू धर्म की व्याख्या इस ढंग से करना था जिससे इसे जन साधारण के बीच लोकप्रियता प्राप्त हो सके। दूसरे चरण में इसका रूप धर्म एवं समाज सुधार आन्दोलन का रहा जिसमें जाति-प्रथा की जटिलताओं का विरोध किया गया और ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी गयी। तीसरे चरण में इसका स्वरूप एक समन्वयवादी चिंतन का हो गया, जिसके माध्यम से हिन्दू धर्म और इस्लाम के बीच एक मिश्रित परंपरा का विकास हुआ और रूढि़वादी एवं कट्टरपंथी विचारों के विपरीत एक उदार और सहिष्णुतापूर्ण विचारधारा विकसित हुई। व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस आन्दोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। प्रथम, इसने हिन्दू धर्म में सुधार का प्रयत्न किया। मूर्तिपूजा और जाति प्रथा का विरोध इस प्रयत्न के मुख्य आधार थे। तत्कालीन युग में इस आन्दोलन ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में कुछ सफलता प्राप्त की। परन्तु वह सफलता न तो स्थायी थी और न ही सर्वव्यापी। हिन्दू धर्म की सुदृढ़ प्राचीरों को (चाहे वे लाभ के लिए अथवा हानि के लिए रही हों) यह आन्दोलन न तोड़ सका। विभिन्न धर्म प्रचारकों के न चाहते हुए भी उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके शिष्यों ने छोटे-छोटे धार्मिक संप्रदायों का निर्माण करके अपने लक्ष्य और कार्यक्षमता को सीमित कर लिया, जिसके कारण न तो वे हिन्दू धर्म में कोई स्थायी सुधार कर सके और न हिन्दूओं के जन जीवन में सम्मिलित ही रहे सके। परन्तु फिर भी यह आन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण था। मध्य युग में हिंदुत्व को जीवित रखने और शक्ति प्रदान करने में उसका योगदान अमूल्य रहा।
इस आन्दोलन का द्वितीय लक्ष्य हिन्दू मुस्लिम एकता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में यह आन्दोलन पूर्णतया असफल रहा। तत्कालीन समय में भी उसका प्रभाव बहुत सीमित रहा और स्थायी प्रभाव तो उसका हुआ ही नहीं। परन्तु एक अन्य दृष्टि से यह आन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण रहा। विभिन्न संतों ने अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अपने उपदेश दिये तथा कविताओं आदि की रचना की। इससे प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य के निर्माण में सहायता मिली। हिन्दी, बंगला, मराठी, मैथिली आदि सभी भाषाओं के साहित्य का निर्माण संभव हुआ। इस प्रकार मध्य युग का यह भक्ति आन्दोलन काफी महत्वपूर्ण था।
लेकिन उनकी उपलब्धियों को कठोरतापूर्वक आंकना भी अनुचित है। महान संतों को सफलता अवश्य मिली, किन्तु उन्होंने समाज के लोगों के दिमाग में या सामाजिक चेतना में क्रांतिकारी मूल्य या प्राथमिकताएं उत्पन्न कर दीं। इसका सर्वाधिक लाभ मुगल शासकों को मिला, क्योंकि देश के जनमानस में महान संतों की ऐसी शिक्षाएं विद्यमान थीं जिन्होंने जाति और धर्म के दुराव की समाप्त कर दिया था। अकबर के विचारों की यही सैद्धांतिक पृष्ठभूमि थी और ‘तौर्हिद इलाही’ या एकेश्वरवाद की उसकी अवधारणा इसी पृष्ठभूमि में फलीभूत हुई थी।
सूफियों ने भारत में धार्मिक उदारता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभायी और उत्तर भारत में प्रचलित हिन्दू परंपराओं को इस्लाम में स्वीकृति दिलायी। उन्होंने संगीत को भक्ति के माध्यम के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने नयी राग-रागनियों को लोकप्रिय बनाया और नये वाद्य यंत्र विकसित किये। धार्मिक उदारता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सूफियों ने शासक वर्ग के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर दिया। अधिकतम सूफी संत शासक वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे, ताकि शासकों के अत्याचार में साझीदार न समझे जायें। इसके विपरीत वे दलित एवं शोषित वर्ग को समर्थन देने में विश्वास रखते थे। मुस्लिम समाज के प्रति भी सूफियों को देन उल्लेखनीय है। भारत में इस्लाम का प्रचार वस्तुतः इन्होंने ही किया। इन्होंने यह सिद्ध किया कि इस्लाम धर्म केवल हिंसा और कट्टरता पर ही आधारित नहीं है। उन्होंने उदारता एवं सहिष्णुता पर भी बल दिया। भारत में मुस्लिम शासक वर्ग धन और विलासिता के वातावरण में नैतिक आचरण के स्तर से गिरता जा रहा था। ऐसी स्थिति में धन को हीन बताने और दरिद्रता के जीवन को ही महत्व देने का विचार सूफियों ने प्रस्तुत किया। मध्य काल में नगरीय जीवन के कारण जो बुराइयां आ गयी थीं जैसे- मुनाफाखोरी, दासप्रथा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, इनके विरुद्ध नयी चेतना जगाने में इन सूफियों का महत्वपूर्ण हाथ था। इन्होंने मनुष्य की कमजोरी और सांसारिक आकर्षण की निंदा करते हुए समाज सुधार के प्रयास किये।
भाषा और साहित्य के क्षेत्र में सूफियों का योगदान अविस्मरणीय है। निजामी के शब्दों में सूफियों की खानकहों में ही उर्दू भाषा का जन्म हुआ। उनका तर्क यह है कि सूफियों को भारत में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता थी, जिससे कि वे भारतीय प्रजा के बीच अपने विचारों का प्रचार कर सके। इस प्रकार आपसी सम्पर्क और विचारों के आदान-प्रदान से एक ऐसी भाषा विकसित हुई जिसमें अरबी और फारसी के साथ भारतीय भाषाओं के शब्द मिले हुए थे। उर्दू भाषा के आरंभिक ग्रंथ भी सूफियों द्वारा ही लिखे गये। दूसरी ओर भारतीय भाषाओं में भी सूफियों की रचनाएं लिखी गयीं। बाबा फरीद और अनेक संतों ने जैसे- हुसैन शाह, बुल्लेशाह आदि ने पंजाबी भाषा का प्रयोग अपने विचारों के प्रचार के लिए किया। शेख अहमद खट्टु ने गुजराती भाषा, कुतबन मंझन, जायसी आदि ने अवधि एवं ब्रजभाषा का प्रयोग किया। इससे भारतीय भाषा भी संपन्न हुयी।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास एवं जनसामान्य के जीवन एवं चिन्तन को प्रभावित करने में सूफी एवं भक्ति आन्दोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।Question : ‘तुर्क, अफगान एवं मुगलों द्वारा राजपूतों की पराजय का एकमात्र कारण निम्नकोटि की अश्वारोही सेना ही नहीं थी।’ विवेचना कीजिये।
(2001)
Answer : भारत ने इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला प्रायः तीन सौ वर्षों तक अपनी उत्तर-पश्चिम सीमा पर किया। अरबों का भारत पर आक्रमण सिंध और मुल्तान तक सीमित रहाऔर तुर्कों द्वारा काबुल, अफगानिस्तान तथा पंजाब पर विजय आसानी से नहीं हुई। यह एक गौरवपूर्ण बात थी कि जिस इस्लाम ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अधिकांश भाग को जीतकर अपना अंग बना लिया, उसका मुकाबला हिन्दू एक लंबे समय तक कर सके थे। 11वीं और 12वीं सदी में हिन्दू राज्य जिस प्रकार महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी से पराजित हुए, वह अस्वाभाविक था। हिन्दू राजाओं के सैनिकों की संख्या तुर्की आक्रमणकारियों की सेना की संख्या से कम न थी तथा उनकी शक्ति भी कम न थी, जैसा कि गोरी के अन्हिलवाड़ तथा तराइन के युद्धों की पराजय से स्पष्ट होता है। शौर्य एवं साहस की दृष्टि से भी भारतीय दुर्बल न थे, परन्तु तब भी अंत में विजय तुर्कों की ही हुई, यह इतिहासकारों की जिज्ञासा का कारण रहा है। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और मिन्हाज उस सिराज ने उनकी पराजय के कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला। फक्र-ए-मुदब्बिर ने अपने ग्रंथ में यह संकेत अवश्य दिया कि राजपूतों की सामन्ती-सैनिक व्यवस्था तथा तुर्की घुड़सवार सेना की गतिशीलता तुर्कों की सफलता के कारण थी। डॉ. के.ए. निजामी ने लिखा है- ‘उस युग में गतिशीलता तुर्की सैनिक संगठन का मूल आधार थी। वह युग घोड़ों का युग था और अद्वितीय गतिशील तथा शस्त्र-सुसज्जित घुड़सवार सेना उस युग की एक महान आवश्यकता थी।’ डॉ. यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि उस युग में तुर्की घुड़सवार एशिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। वह लिखते हैं- ‘सीमापार के इन आक्रमणकारियों के शस्त्रें और घोड़ों ने उनको भारतीयों पर विवादरहित सैनिक श्रेष्ठता प्रदान की।’ इस प्रकार बहुत से इतिहासकार तुर्क, अफगान एवं मुगलों द्वारा राजपूतों की पराजय का एक मुख्य कारण इनकी सैन्य दुर्बलताओं को मानते हुए निम्नकोटि के अश्वारोही सेना को जिम्मेदार ठहराते हैं। किन्तु गहन विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि राजपूतों की पराजय का एकमात्र कारण निम्न कोटि की अश्वारोही सेना नहीं थी। वस्तुतः राजपूतों के पराजय में कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य कारणों का सम्मिलित योगदान रहा था।
सर्वप्रथम भारत में राजनीतिक एकता का पूर्ण अभाव था। सारा देश छोटे-छोटे क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त था। इनके शासक क्षेत्रीय विस्तार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना के कारण एक-दूसरे से परस्पर संघर्ष में लगे रहते थे। राजनीतिक एकता के अभाव में सामन्तीकरण की प्रक्रिया का भी योगदान था। शासकों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण संयुक्त रूप से विदेशी आक्रमण का सामना करना कठिन था। यद्यपि कुछ अवसरों पर महमूद के विरुद्ध भारतीय शासकों ने एकजुट होकर संघर्ष का प्रयास किया, परंतु वे इसमें सफल नहीं हो पाये और मुहम्मद गोरी के समय ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रयास हुआ भी नहीं। उसी प्रकार अफगानों और मुगलों के विरुद्ध भी भारतीय शासक एक संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल रहे।
राजनीतिक अनेकता का एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम यह भी हुआ कि सीमांत क्षेत्र की रक्षा का समुचित प्रबंध नहीं हो सका। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों के शासक सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा में सक्रिय रूप से योगदान देने में रुचि नहीं लेते थेे। सीमांत क्षेत्र के असुरक्षित होने के कारण आक्रमणकारियों के लिए भारत में प्रवेश का मार्ग सदा खुला रहा।
राजनैतिक अनेकता और सामंती प्रथा का दुष्परिणाम आर्थिक जीवन के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। उस समय राज्य की आय का मुख्य साधन लगान अथवा भू-राजस्व के रूप में था। परंतु सामंती प्रथा के कारण यह आमदनी राजा के हाथ में केन्द्रित न होकर अनेक सामतों के बीच विभाजित थी। इसका परिणाम यह हुआ कि शासक के हाथ में आर्थिक साधन सीमित थे और राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैनिक संगठन का बोझ उठाना उसकी क्षमता से परे था। सैनिक दायित्व सांमतों पर ही डाल दिया गया था जो युद्ध के समय शासक को सहायता प्रदान करता था, परंतु इस सेना का रूप एक संगठित केन्द्रित सेना के समान नहीं था।
तुर्कों की रणपद्धति भी अधिक उन्नत थी और अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में भी उन्हें अग्रता प्राप्त थी। हाथी की तुलना में घोड़ों की तेज गति के कारण तुर्कों को सदा सुविधा होती थी। जीतने पर वे भारतीय सेना को अधिक दूर तक खदेड़ सकते थे और हारने पर सुरक्षित स्थान पर जल्दी ही पहुंच सकते थे। भारतीय अश्वारोहियों को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। तुर्क चमड़े की जीन का प्रयोग करते थे, जबकि भारतीय चमड़े को अपवित्र मानकर कपड़े या बोरे की जीन इस्तेमाल करते थे। इसी प्रकार तुर्कों द्वारा प्रयोग की गयी रकाब अधिक मजबूत और सुविधाजनक होती थी। तुर्क सैनिकों के लिए लंबी यात्र करना और चलते घोड़े पर खड़े होकर हथियार चलाना संभव था, जबकि भारतीय सैनिकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तुर्की घोड़ों में नाल का प्रयोग होता था जिससे घोड़ों के खुर सुरक्षित रहते थे और कठिन क्षेत्र में यात्र के समय या अन्य परिस्थितियों में घोड़े के घायल होने और मरने की संभावना कम होती थी। उपर्युक्त के अलावा भारत में अच्छी नस्ल के घोड़े उपलब्ध न होने के कारण ऐसी क्षति को पूरा करना भी कठिन था।
भारतीय शासकों और तुर्क शासकों के दृष्टिकोण में भी व्यापक अंतर था। भारतीय शासक युद्ध में हार को व्यक्तिगत अपमान मानकर कभी-कभी आत्महत्या भी कर लेते थे, जबकि तुर्क शासक युद्ध में पराजय से हतोत्साहित न होकर हार के कारणों को समझने और उनका निदान करने का प्रयास करते थे। इसलिए भी अंततः वे विजयी रहे।
कुछ इतिहासकारों ने भारतीय शासकों की हार के लिए सामाजिक परिस्थितियों को भी उत्तरदायी माना है। वर्ण तथा जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज कई वर्गों में बंटा था। छुआछूत की भावना तथा भू-स्वामियों द्वारा निम्न वर्ग के खेतीहर तथा अन्य श्रमिकों के शोषण के कारण समाज दुर्बल हो रहा था। शोषित वर्ग में देश या राज्य की सुरक्षा अथवा विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध की भावना का होना संभव नहीं था। उच्चवर्ग की श्रेष्ठता की धारणा के कारण वे विदेशों से भी समुचित संपर्क स्थापित न कर सके और देश में पृथकतावादी प्रवृत्ति ने घर कर लिया। इस पृथकतावादी प्रवृत्ति के कारण बाहरी देशों के नवीन राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा रण कौशल संबंधी विकास के ज्ञान से भारतीय समाज लाभ नहीं उठा सका, जबकि विदेशों से भारत का व्यापार पर्याप्त मात्र में होता था और भारत की धन संपदा तथा अन्य बलों को विदेशी आक्रमणकारियों का निश्चित ज्ञान था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूतों की पराजय के मूल में सिर्फ निम्न कोटी की अश्वारोही सेना नहीं थी, बल्कि इसके लिए कई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य कारक उत्तरदायी थे।
Question : अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी था।
(1999)
Answer : अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के महानतम शासकों में से एक था। उसका शासनकाल साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासनिक सुधार दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उसने एक शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था का गठन किया और उसकी सहायता से अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ की एवं पड़ोसी क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्यवादी विस्तार को संभव बनाया। उसके अनुसार सुल्तान का पद वहीं व्यक्ति प्राप्त करता है, जो इसके लिए सक्षम हो। शासक बनने का अधिकार उसे ही है, जो सत्ता पर अधिकार अपने बाहुबल द्वारा कर सके।उसका विश्वास था कि संसार में विभिन्न राज्य एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। अतः अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए हर राज्य को अपना विस्तार करना और अपने साधनों में वृद्धि करना अनिवार्य है। जो राज्य ऐसा नहीं करता है, वह अंततः कमजोर और पराजित होता है। इसी सिद्धांत ने उसे साम्राज्यवादी विस्तार के लिए प्रेरित किया। उसने शीघ्र ही गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरि, वारंगल, मदुरै एवं होयसल राज्य को जीतकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया। साथ ही, उसने आक्रामक मंगोल नीति अपनाकर उस साम्राज्य की रक्षा भी की। उसका साम्राज्यवाद सिद्धांत और व्यवहार में अलग-अलग था। सिद्धांततः अलाउद्दीन विश्व विजय का इच्छुक था, परंतु व्यवहार में उसे केवल भारतीय उपमहाद्वीप के राज्यों की विजय का ही अवसर मिल सका। वह एक व्यावहारिक साम्राज्यवादी था। उसकी सर्वोच्च उपलब्धि यह भी थी कि दक्षिणी प्रदेशों को साम्राज्य में विलीन किये बिना ही उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गयी। अपनी विस्तारवादी नीति के कारण वह लगभग संपूर्ण भारत का स्वामी बन गया। उसने धर्म के प्रभाव से राजनीति को मुक्त रखने में निर्णायक सफलता प्राप्त की। उसकी सत्ता के अधीन सुल्तान की निरंकुशता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गयी और सल्तनत का कोई दूसरा शासक उसके जैसा शक्ति संपन्न शासक नहीं बन सका। वास्तव में वह एक अनोखा साम्राज्यवादी था।
Question : शिवाजी के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की समीक्षा कीजिये। शिवाजी की देन पर भी प्रकाश डालिये।
(1999)
Answer : मराठों के राजनीतिक उत्कर्ष एवं मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी का बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने शाहजी भोंसले द्वारा आरंभ किये गये कार्य को आगे बढ़ाया तथा दक्षिणी रियासतों एवं मुगलों से संघर्ष कर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी भारतीय इतिहास में एक वीर योद्धा, विजेता, कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक के रूप में विख्यात हैं। इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार, शिवाजी का व्यक्तित्व अपने युग में ही नहीं बल्कि संपूर्ण आधुनिक युग में भी असाधारण है। अंधकार के बीच में वह एक ऐसे नक्षत्र के समान चमकते हैं, जो अपने समय से बहुत आगे था। शिवाजी के उत्कर्ष के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार थीं:
भौगोलिक स्थिति: शिवाजी के उत्थान में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। महाराष्ट्र का इलाका पर्वतों से घिरा एवं सुरक्षित था। यह स्थान बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था। खेती की सुविधा और उपज अधिक नहीं होने तथा कम वर्षा होने के कारण मराठों को कठिन परिश्रम करना पड़ता था, जिसने उसे साहसी और वीर बना दिया।
लूटमार को मराठों ने जीविकोपार्जन का साधन बना लिया, जिससे उनमें सैनिक गुणों का विकास हुआ। दुर्गम स्थानों में दुर्ग बनाकर मराठों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इन दुर्गों को भेदना तथा उन तक सेना एवं रसद पहुंचाना आक्रमणकारियों के लिए आसान नहीं था। इसका लाभ मराठों ने अपने दुश्मनों को हराने एवं लूटमार करने में किया। वे इच्छानुसार दक्षिण में आक्रमण कर सुरक्षित वापस लौट जाते थे। पहाड़ों में रहने के कारण मराठे छापामार युद्ध करने में प्रवीण हो गये एवं दक्षिणी रियासतों एवं मुगलों से अपनी सुरक्षा करने में सफल हुए।
मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव: मराठों में स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जगाने में मराठी धर्म सुधारकों का प्रमुख योगदान था। वहां संत ज्ञानेश्वर एकनाथ, तुकाराम, रामदास और वामन पंडित जैसे विचारक और सुधारक हुए, जिन्होंने मराठों में जागृति ला दी। इन लोगों ने सामाजिक कुरीतियां मिटाने तथा सबके साथ समान बर्ताव करने का उपदेश दिया। जन साधारण की भाषा का सहारा लेकर इन लोगों ने घर-घर में अपनी बात पहुंचा दी। इनका मराठों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वे संगठित होने लगे।
भाषा एवं साहित्य का योगदान: मराठी संतों ने बोलचाल की भाषा के माध्यम से अपने संदेशों का प्रचार किया। उन्होंने मराठी भाषा में गीत एवं कवितायें लिखीं तथा साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। वे सुगमता से सभी को उपलब्ध थे। इनके माध्यम से मराठों में आपसी एकता, समानता एवं राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई।
तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति: मराठों का सामाजिक जीवन विषमताओं और वर्ग संघर्ष से अपेक्षाकृत कम प्रभावित था। छुआछूत, जाति व्यवस्था, ऊंच-नीच का विभेद धर्म सुधारकों और विचारकों के प्रभाव से कमजोर पड़ गया। इसके विपरीत मराठों में एक जाति और एक राष्ट्र की भावना घर करने लगी। उनके बीच आर्थिक विषमता अधिक नहीं थी। सामाजिक-आर्थिक एकता और नवचेतना ने उनमें राष्ट्रीयता की भावना भी जगा दी।
प्रशासनिक एवं राजनीतिक अनुभव: अपने सैनिक गुणों के कारण मराठों ने पर्याप्त प्रशासनिक एवं राजनीतिक अनुभव प्राप्त कर इसका लाभ उठाया। इससे मराठों ने विभिन्न राजनीतिक स्थितियों को समझा एवं इसका लाभ मराठों को संगठित करने में किया।
शाहजी भोंसले का योगदान: इन सारी परिस्थितियों का लाभ उठाकर मराठों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय लखजी जाधव नामक मराठा सरदार के दामाद और मौलजी के पुत्र शाहजी भोंसले को दिया जाता है। उन्होंने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर मराठों की एकता एवं राजनीतिक उत्कर्ष को नेतृत्व प्रदान किया।
शिवाजी का कर्मठ व्यक्तित्वः शिवाजी एक सेनापति ही नहीं, वरन् महान राष्ट्र निर्माता भी थे। जिस समय शिवाजी का उत्कर्ष हुआ, उस समय हिंदू राष्ट्र समाप्त हो गया था। महाराष्ट्र में यद्यपि धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी, परंतु राजनीतिक एकता या राष्ट्रीयता की भावना शून्य थी। ऐसी स्थिति में शिवाजी ने अपनी व्यक्तिगत वीरता, साहसपूर्ण सुयोग्य नेतृत्व, कुशल व्यवहार तथा अपने अनवरत प्रयत्नों से बिखरी मराठा जाति को समान रूप में संगठित एवं एकत्रित करके एक संयुक्त जाति बना दिया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। शिवाजी ने मराठों में आत्मसम्मान तथा आत्मगौरव के भाव जगाकर उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया तथा अपने देश, अपनी जाति और अपने धर्म के लिए मर मिटना सिखाया। अपनी राष्ट्रीय सेना की सहायता से उन्होंने महाराष्ट्र में जिस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, उसका नाम उन्होंने स्वराज्य रखा। शिवाजी के उत्कर्ष में उनके अधीनस्थ सहयोगियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जिनमें मोरी पिंगले, अन्ना जी दत्ता, प्रीांद नीराजी, रावजी, मुरारबाजी, आबाजी सोनदेव, निम्बालकर, सूर्याजी मलूसरे तथा नेता जी पालकर आदि प्रमुख थे। ये सहयोगी स्वार्थहीन, स्वामीभक्त एवं कर्तव्यनिष्ठ थे। शिवाजी को एक महान पुरुष, न्यायप्रिय, प्रजा वत्सल तथा राष्ट्र निर्माता कहा गया है। शिवाजी के देन को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता हैः
मानव के रूप में: शिवाजी असाधारण चरित्र एवं व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके आदर्श उच्च थे। अपने माता-पिता के प्रति उनके मन में अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति थी। शिवाजी बलिष्ठ, साहसी और पराक्रमी थे और कठिन संकटापÂ स्थिति में अपने व्यक्तिगत कार्यों द्वारा अपने अनुयायियों में उत्साह एवं नया जीवन फूंक देते थे। शिवाजी दीन-दुखियों, संन्यासियों एवं विद्वानों के संरक्षक भी थे तथा उनमें धार्मिक सहिष्णुता भी थी।
सेनानायक के रूप में: शिवाजी एक वीर सैनिक, वीर योद्धा तथा सुयोग्य, रणनिपुण एवं सफल सेनानायक थे। अपनी सैनिक प्रतिभा से ही शिवाजी साधारण जागीरदार के पद से प्रगति करते हुए अपनी विजयों से विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गये। अनेक युद्धों में उन्होंने साहस से अपने जीवन को संकट में डालकर भी विजय पायी। अत्यंत सीमित साधनों के होते हुए भी शिवाजी ने प्रबल मुगल साम्राज्य से टक्कर ली। उनकी छापामार रणपद्धति अपने-आप में एक विशेष गुण था।
सफल एवं कुशल शासन प्रबंधक: वे एक कुशल एवं सफल शासक भी थे। उन्होंने जो प्रशासन स्थापित किया, वह दीर्घकाल तक टिका रहा। विशेषकर दुर्गों की शासन व्यवस्था में शिवाजी मुगलों की शासन व्यवस्था से भी अधिक श्रेष्ठ थे। शिवाजी का प्रशासन हिंदू धर्म के सिद्धांतों और परंपराओं के अनुरूप था। न्याय की व्यवस्था हिंदू स्मृतियों के आधार पर की गयी थी। उन्होंने आवश्यकतानुसार जनहित हेतु सुधार भी किये। सैनिक एवं असैनिक सेवाओं के लिए भूमि या जागीर देने के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। प्रशासन में उन्होंने सभी वर्गों और संप्रदायों के अनुयायियों के लिए समान अवसर प्रदान किये। शासन में योग्यता व प्रतिभा को ऊंचा स्थान दिया।
उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ: शिवाजी ने बिखरे हुए मराठों को उन्होंने संगठित किया। अपनी कुशलता के बल पर ही शिवाजी ने अत्याचारों और शोषण से संतप्त जनता को एक दृढ़ राजनीतिक शक्ति में संगठित कर दिया और अपनी सफलताओं से राजनीतिक क्षेत्र में मराठों के यश एवं सम्मान में वृद्धि की। शिवाजी महान दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ भी थे। अपनी कूटनीतिज्ञता के बल पर शिवाजी ने अपने शत्रुओं को कभी एक नहीं होने दिया। शिवाजी हमेशा शत्रुओं की शक्ति को छिन्न-भिन्न करके अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया करते थे।
राष्ट्र निर्माता: आधुनिक इतिहासकारों ने शिवाजी को महान राष्ट्र निर्माता माना है। वास्तव में जिस समय शिवाजी का उदय हुआ था, उस समय हिन्दू राष्ट्र समाप्त हो गया था। उत्तर भारत में तो राजपूतों का गौरव समाप्त ही हो गया था। उस समय महाराष्ट्र में सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकता के होते हुए भी राजनीतिक अथवा राष्ट्रीय एकता का पूर्णतः अभाव था। मराठा सरदार इधर-उधर बिखरे हुए थे और वे मुसलमान शासकों की सेवाओं में संलग्न थे। शिवाजी ही वह पहले मराठा सरदार थे, जिनमें बाल्य काल से ही राष्ट्रीयता की भावना उम्र के साथ-साथ बढ़ती गयी और यह स्वदेश प्रेम इतना प्रबल हो गया था कि उन्होंने एक हिंदवी स्वराज्य की पुनर्स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। सर जदुनाथ सरकार के शब्दों में, फ्वह भारत का अंतिम हिन्दू राष्ट्र निर्माता था", जिसने हिंदुओं के मस्तक को एक बार पुनः ऊँचा किया।
वस्तुतः एक राज्य संस्थापक एवं प्रशासक के रूप में उनकी तुलना किसी भी महान शासक से की जा सकती है। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था- मराठों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर उनमें राष्ट्रप्रेम की भावना जगाना। मराठा इतिहास इसके लिए सदैव ऋणी रहेगा। Question : आपको दिये गये मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 15 स्थानों पर निशान लगाइये एवं अंकित स्थानों पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखियेः
1. अंबक, 2. कान्यकुब्ज, 3. किष्किंधा, 4. कुंडलवन, 5. खजुराहो, 6. गिहलोट, 7. गोकुल, 8. चिदम्बरम, 9. जहाजपुर, 10. जैसलमेर, 11. तक्षशिला, 12. द्वारका, 13. जलालाबाद, 14. नालंदा, 15. पंचवटी, 16. पाटलिपुत्र, 17. फतेहपुर सीकरी, 18. बद्रीनाथ,19. बहमनाबाद, 20. बालब्रह्मेश्वर, 21. बीजापुर, 22. बुरहानपुर, 23. बैराठ, 24. भद्रावती, 25. भीतरगांव, 26. वारंगल, 27. विलासपुर, 28. शत्रुंजय, 29. श्रीपुर, 30. कारगिल
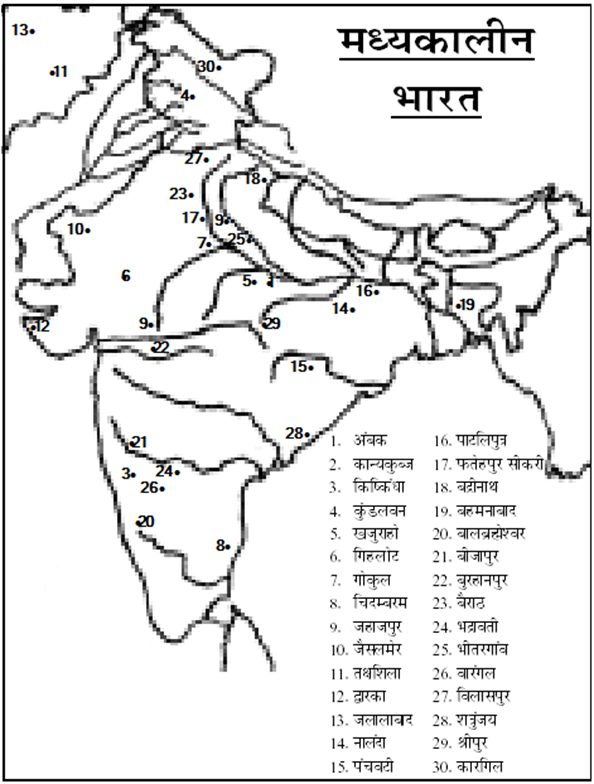
(1999)
Answer : 1. अबंक: चेदि महाजनपद की राजधानी शक्तिमती के निकट अंबक स्थित था। यहां से उत्तरवैदिक कालीन पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति हुई है। यहां से चित्रित धूसर मृद्भांड, लौह उपकरण एवं कुछ मृण्यमूर्तियां मिली हैं।
2. कान्यकुब्ज: महाभारत, रामायण तथा पतंजलि के ‘महाभाष्य’ में उल्लिखित कान्यकुब्ज के वैभव का युग सातवीं सदी से प्रारंभ हुआ, जब इसे पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्द्धन ने अपनी राजधानी बनाया। इसके पूर्व यह मौखरि वंश की राजधानी थी।
3. किष्किंधा: कर्नाटक राज्य के दावणगेरे जिले में स्थित किसिन्धा को किष्किंधा से समीकृत किया गया है। रामायण में इस स्थान का वर्णन है। यहीं पर राजा बालि और सुग्रीव राज करते थे। रामचंद्र की भक्त हनुमान से यहीं मुलाकात हुई थी।
4. कुंडलवन: आधुनिक श्रीनगर के निकट स्थित कुंडलवन एक विख्यात बौद्धस्थल है। यहीं पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तथा बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था।
5. खजुराहो: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी थी। यहां से मध्यकालीन वास्तुकला के अन्यतम नमूने प्राप्त होते हैं।
6. गिहलोट: राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित यह एक छोटा.सा गांव है। यहां से मेवाड़वंशी शासकों के अवशेष पाये गये हैं। यहीं पर एक प्राचीन शिवमंदिर भी स्थित है।
7. गोकुल: मथुरा के निकट स्थित गोकुल भागवत संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह स्थल श्रीकृष्ण एवं गोपियों की रासलीलाओं के लिए विख्यात रहा है।
8. चिदम्बरम: उत्तरी तमिलनाडु में स्थित चिदम्बरम चोल काल में अति विख्यात था। यहां चोल कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहां पर एक विख्यात शिवमंदिर स्थित है, जिसमें नटराज की मूर्ति स्थापित की गयी थी।
9. जहाजपुर: यह मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू के निकट स्थित है। यह मालवा राज्य के खिलजी राजवंश के अधीन विख्यात हुआ। यहां इस्लामी कला का एक प्रमुख केंद्र था। यह संगीत शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था।
10. जैसलमेर: राजस्थान की अरावली पहाडि़यों के पश्चिम में थार मरुस्थल के लगभग अंतिम छोर पर जैसलमेर नगर राजपूत. कालीन एक भव्य एवं दुर्गम नगर है। राव जैसल ने 1155 ई. में इसकी नींव रखी थी। यहां भाटी राजाओं का शासन रहा था।
11. तक्षशिला: प्राचीन महाजनपद गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो अपने सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व के कारण विख्यात था। यहां पर एक विश्व-विख्यात विश्वविद्यालय था, जहां पर विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। चाणक्य यहीं पर अध्यापन का कार्य करते थे।
12. द्वारका: गुजरात के पश्चिमी तट पर बसी द्वारका श्रीकृष्ण की राजधानी थी। श्रीकृष्ण ने जरासंध के आक्रमणों से बचने के लिए अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका बना ली थी। प्राचीन द्वारका जलमग्न हो गयी है। प्राचीन द्वारका के अवशेष समुद्र के अंदर खोज निकाले गये हैं।
13. जलालाबाद: जलालाबाद, अफगानिस्तान में काबुल के निकट स्थित है। प्राचीन बौद्ध स्थल बामियान इसी के निकट स्थित है। यहां पर गौतम बुद्ध की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गयी थी। यह गांधार कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था।
14. नालंदा: मध्य बिहार में स्थित नालंदा एक विख्यात शिक्षा केंंद्र एवं बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था, जहां देश-विदेश से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। चीनी पर्यटक ह्नेनसांग ने इस स्थल की अतिप्रशंसा की है।
15. पंचवटी: यह स्थल मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्थित है। इसे दंडकारण्य का ही एक भाग माना जाता है। राजा रामचंद्र ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय यहीं पर बिताया था।
16. पाटलिपुत्र: मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक विश्वविख्यात स्थल है। मौर्य काल में यह स्थान अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसकी प्रतिष्ठा आठवीं सदी तक बनी रही। बाद में इसका महत्व जाता रहा। फाह्यान एवं ह्नेनसांग ने इस स्थान का वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने यहीं रहकर अपनी विख्यात पुस्तक इंडिका की रचना की थी।
17. फतेहपुर सीकरी: आगरा के निकट स्थित फतेहपुर सीकरी अकबर के समय विख्यात हुआ। यहां अकबर ने अपनी राजधानी बनाया और इसे इंडो-इस्लामिक कला का महान केंद्र बना दिया। चिश्ती सूफी संत शेख सलीम चिश्ती यहीं रहते थे। बाद में यह स्थल उपेक्षित हो गया।
18. बद्रीनाथ: उत्तरांचल के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ हिन्दुओं का एक महान तीर्थस्थल है। यहां पर शंकराचार्य ने एक पीठ स्थापित किया था।
19. बहमनाबाद: बहमनाबाद बंगाल में पांडुआ के निकट स्थित है। हाजी इलियास शाह के काल में इसकी नींव डाली गयी थी। नुसरत शाह के समय यह इस्लामी कला का एक विख्यात केंद्र बन गया।
20. बाल ब्रह्मेश्वर: यह कर्नाटक मेंशृंगेरी के निकट स्थित है। कहा जाता है कि कौंडिन्य ऋषि ने यहीं पर अपना आश्रम स्थापित कर दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रसार किया था।
21. बीजापुर: बहमनी सल्तनत के विघटन के बाद बीजापुर राज्य का गठन हुआ था। यहां आदिलशाही राजवंश का शासन कायम हुआ। 1686 में मुगल साम्राज्य में इसका विलय हो गया। बीजापुर का गोल गुंबज विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है।
22. बुरहानपुर: मध्यकालीन स्थलों में बुरहानपुर का स्थान महत्वपूर्ण है। यह मालवा राज्य के अधीन विकसित हुआ था। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल की मृत्यु यहीं हुई थी। यह इस्लामी कला एवं संस्कृति का एक प्रसिद्ध केंद्र था।
23. बैराठ: बैराठ, आधुनिक जयपुर के निकटस्थित है। इसे प्राचीन विराटनगरी से समीकृत किया गया है। यहां से अशोक के दो अभिलेख पाये गये हैं। जिससे अशोक के प्रशासन एवं धम्म की जानकारी मिलती है।
24. भद्रावती: यह कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण जिला है। यहीं पर स्थित हम्पी से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह लौह उत्पादक स्थल होने के कारण प्राचीन काल में भी चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं परवर्तीचालुक्य जैसे राज्यों का उदय हुआ था।
25. भीतरगांव: यह उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बनवाया गया था। इस मंदिर में शिखर भी पाया गया है। यह काफी ऊंचे चबूतरे पर बना है।
26. वारंगल: यहां पर मध्य काल में ककातीय राजवंश का उदय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीता था और अधीनस्थ राज्य बनाया। बाद में मु- बिन तुगलक ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।
27. विलासपुर: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित विलासपुर पूर्व मध्यकाल में विख्यात हुआ। यहां हूणों के हमले हुए थे, परंतु प्रभाकरवर्द्धन ने हूणों को मार भगाया था।
28. शत्रुंजय: शत्रुंजय, देवराष्ट्र राज्य के अधीन प्रमुख बंदरगाह था। समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान के समय यहां के शासक ने समुद्रगुप्त को बड़ी चुनौती दी थी।
29. श्रीपुर: श्रीपुर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह पूर्व से पश्चिम जाने वाले व्यापारिक राजमार्ग पर स्थित था। इसकी स्थिति के कारण सातवीं-आठवीं सदी में इसका आर्थिक महत्व बढ़ गया था।
30. कारगिल: सियाचिन ग्लेशियर के निकट स्थित कारगिल होकर प्राचीन एवं मध्यकाल में आक्रमणकारियों ने भारत पर हमलाकिया था। यहीं पर स्थित मार्तंड होकर महमूद गजनवी ने कश्मीर राज्य पर हमला बोला था।
Question : भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर इस्लाम के प्रभाव का उल्लेख कीजिये।
(1999)
Answer : भारतीय जनजीवन पर इस्लाम का प्रभाव कोई एक ही रात में पड़ना शुरू नहीं हो गया था। यह प्रभाव तो एक सतत् प्रक्रिया के रूप में उभरकर सामने आया था, जिसमें विरोध और समन्वय दोनों ही शामिल थे, क्योंकि हिंदू धर्म और इस्लाम के मूल धार्मिक- सामाजिक आदर्शों में अंतर था। इस अंतर के कारण पहले-पहल इन दोनों धर्मों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। कुछ मुसलमान शासकों ने अपने शासक होने की स्थिति से फायदा उठा कर इस्लाम धर्म को हिन्दुओं पर थोपने की चेष्टा की। इसे हिन्दुओं ने अपने धर्म और समाज पर आक्रमण समझा और इससे अपनी रक्षा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की। इस रक्षात्मक प्रवृत्ति के कारण हिंदू समाज में संकीर्णता और रूढि़वादिता बढ़ने लगी। ब्राह्मणों ने अपने जातीय नियमों को और भी कठोर किया और तथाकथित रक्त की शुद्धता और पवित्रता को बनाये रखने के लिए विवाह आदि के प्रबन्धों को कठोरता से लागू किया, स्त्रियों की गतिशीलता पर रोक लगायी तथा छुआछूत की भावना को और भी बढ़ाया। यही कारण था कि इस युग में एक ओर जातीय संकीर्णता बढ़ी, तो दूसरी ओर स्त्रियों की स्थिति में और भी पतन हुआ। जातीय कठोरता और संकीर्णता के कारण ही निम्न जातियों के लोगों ने इस्लाम को अपनाया। परन्तु इन संकीर्णताओं की एक स्वस्थ प्रतिक्रिया यह हुई कि कबीर, नानक, रामानंद, चैतन्य आदि संत-महात्माओं द्वारा धर्म तथा समाज को सुधारने के प्रयत्न भी हुए। कालांतर में हिन्दुओं और मुसलमानों में सामंजस्य, सहयोग और सहिष्णुता की भावना बढ़ने लगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है।
स्थापत्य कला पर प्रभाव: इस्लामी स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं गुंबज, ऊंची मीनारें, मेहराब तथा तहखाना था। इस शैली को तुर्की विजेता अपने साथ भारत में लाये थे और यहां पर आने के बाद इसी शैली का भारतीय स्थापत्य कला के साथ समन्वय हुआ। विदेशी शासकों को भवन निर्माण कार्य में भारतीय कारीगरों को लगाना पड़ा, जिन्होंने हिन्दू स्थापत्य कला का प्रयोग किया। इससे जो स्थापत्य के नमूने बने वह न तो पूर्णतया विदेशी थी और न ही शुद्ध देशी। प्रारंभिक तुर्क विजेताओं ने यहां के हिन्दू तथा जैन मंदिरों को पहले नष्ट किया और फिर उन्हीं की सामग्री से अपनी मस्जिदों और कब्रों का निर्माण किया। इस प्रक्रिया में भी दोनों शैलियों का समन्वय हो गया। मुसलमान शासकों ने नये सिरे से मस्जिद बनाने के स्थान पर केवल हिन्दू तथा जैन मंदिरों के चौरस छतों को तोड़कर उनके स्थान पर गुंबज तथा मीनारें बनाकर उन्हें मस्जिदों का रूप दे दिया गया।
चित्रकला पर प्रभाव: चित्रकला में भी तुर्की, ईरानी तथा प्राचीन भारतीय शैलियों का समन्वय हुआ। सभी मुगल बादशाह चित्रकला प्रेमी थे। बाबर स्वयं चित्रकार था और टियूराइड चित्रकारी के बहुत से उत्तम नमूने अपने साथ ले आया था। हुमायूं ने भी दो कुशल चित्रकार को फारस से बुलाया था। अकबर के दरबार में 17 प्रमुख चित्रकार थे। उनमें मीर सैयद अली, अब्दुस्मद, फर्रूखबेग और जमशेद विदेशी चित्रकार थे। हिन्दू चित्रकारों में दसबंत, बसावन, सांवलदास, ताराचंद, मुकुंद, हरिवंश और जगन्नाथ प्रमुख थे। ये कलाकार मनुष्यों के चित्र बनाने, पुस्तकों को चित्रित करने तथा पशुओं के चित्र बनाने में बहुत ही निपुण थे। अकबर के समय में हिन्दू तथा चीनी-फारसी चित्रकला के तत्त्वों का समन्वय देखने को मिलता है। प्रारंभ में फारसी प्रभाव अधिक था, पर बाद में वह धीरे-धीरे कम होता गया और भारतीय तत्त्वों की प्रधानता हो गयी। जहांगीर के काल में धार्मिक चित्रों में इस्लाम धर्म संबंधी चित्रों का अभाव दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इस्लाम धर्म चित्रकला का विरोधी है। अतः जहांगीर के समय में रामायण, महाभारत आदि हिन्दू ग्रंथों के चित्रों को अंकित किया गया।
संगीत पर प्रभाव: परंपरागत दृष्टि से संगीत को इस्लाम में बुरा बताया गया है। लेकिन फारस में सूफियों के साथ मुसलमानों का संबंध होने पर और बाद में संगीत प्र्रेमी हिन्दुओं के साथ भी संपर्क स्थापित होने के कारण उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। एक ओर सूफी संगीत को आध्यात्मिक उन्नति का साधन समझते थे, तो दूसरी ओर हिन्दू भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर संगीत समारोह का आयोजन करते थे। दिल्ली सल्तनत के समय में ही कुछ उल्लेखनीय गायक हुए, जिनमें कवि अमीर खुसरो का प्रथम स्थान था। उसने अपनी कुछ कविताओं को भारतीय स्वरों में आबद्ध किया। शासकों के प्रयास से प्राचीन भारतीय तथा ईरानी संगीत कलाओं का समन्वय हुआ और एक नयी शैली का जन्म हुआ। सम्राट अकबर के शासन काल में भारतीय संगीत का विकास और भी तेजी के साथ हुआ। उसके शासनकाल में रागों के ऊपर विदेशी प्रभाव पड़ा, जिससे उत्तरी भारत के संगीत के रूप में परिवर्तन हुआ। हिन्दू और फारसी शैलियों के सम्मिश्रण से इस समय में गायन और संगीत की नयी रीतियों का जन्म हुआ। मुसलमानों तथा भारतीयों के सम्मिलित प्रयासों से संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसकी परंपरा आज भी स्पष्ट है।
धार्मिक जीवन पर प्रभाव: मुसलमानों के आने से पहले हिन्दुओं में धर्म के क्षेत्र में आडम्बर और छुआछूत का विचार प्रबल था। इस संबंध में मुसलमानों का प्रथम उल्लेखनीय प्रभाव एक ईश्वर के प्रति हिन्दुओं का झुकाव था। इस्लाम से प्रभावित होकर अनेक हिंदू साधु-संतों ने सब धर्मों की समानता और ईश्वर की एकता पर बल दिया, बाहरी दिखावा और छुआछूत की निंदा की, जन्म के स्थान पर कर्म को अधिक महत्वपूर्ण माना और सामाजिक अन्याय की कटु आलोचना की। इनके संरक्षण में इस्लाम की भांति समानता के सिद्धांत पर बल देने वाले भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। इस्लाम के कारण भक्ति आंदोलन को प्रेरणा मिली, क्योंकि कबीर, चैतन्य, नानक, रामानंद, तुकाराम, रामदास आदि के उपदेशों में इस्लामी तत्त्वों को देखा जा सकता है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने सांप्रदायिक तनाव को दूर करने का प्रयास किया, सभी धर्मों की समानता और ईश्वर की एकता पर बल दिया, बाहरी दिखावा और छुआछूत की निन्दा की, जन्म के स्थान पर कर्म को अधिक महत्वपूर्ण माना। हिन्दू धर्म ने भी इस्लाम को प्रभावित किया। जिन हिन्दुओं ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, वे अपने साथ अपने पूर्वजों के धार्मिक विचारों, संस्कारों तथा कृत्यों को लेते गये। मुसलमानों में फकीरों, पीरों तथा मकबरों की पूजा प्रचलित हो गयी। यह हिन्दुओं में प्रचलित स्थानीय तथा जातीय देवताओं की पूजा का ही दूसरा रूप था, जिससे भारतीय मुसलमान छुटकारा न पा सके।
जाति प्रथा पर प्रभाव: इस्लाम के प्रभावों से हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए हिन्दुओं ने धर्म संबंधी और जाति प्रथा संबंधी नियमों को बहुत कठोर बनाया और उन्हें दृढ़ता से लागू किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जातीय संरचना में और भी रूढि़वादिता और संकीर्णता पनपी। ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति ऊंची बनाये रखने के लिए भरसक प्रयत्न किया, परंतु उनका यह प्रयत्न पूर्णतया सफल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ विरोधी शक्तियां भी उस समय क्रियाशील थीं। कुछ जातियों को विशेषकर कायस्थ, खत्री और क्षत्रियों को मुसलमान शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण इन जातियों को अपनी स्थिति को ऊंचा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे सामाजिक जीवन में इनकी प्रतिष्ठा पहले से कहीं अधिक बढ़ गयी। दूसरी ओर हिन्दू जाति प्रथा ने स्वयं मुसलमानों को भी प्रभावित किया। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से सभी मुसलमान उस समय बराबर थे, परंतु व्यावहारिक रूप से जिस जातीय संस्तरण का प्रारंभ मुस्लिम युग में हुआ, वह आज भी मौजूद है। हिन्दू धर्म त्याग कर इस्लाम अपनाने वालों की संख्या मुस्लिम राज्य तथा सत्ता के प्रसार के साथ बढ़ती गयी। ऐसे लोगों को शासक वर्ग की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। इनकी सामाजिक स्थिति निम्न ही बनी रही।
विवाह पर प्रभाव: इस्लाम के प्रभाव से हिन्दुओं के विवाह नामक संस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। दोनों समूहों के मध्य वैवाहिक संबंधों को रोकने के लिए विविध उपाय किये गये। हिन्दुओं में बाल विवाह एक सामान्य नियम बन गया। उच्च तथा मध्य जातियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन तेजी से किया गया। इस समय स्त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव हो गया। अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने में लड़कियां एक प्रकार से असमर्थ हो गयीं। विधवाओं के पुनर्विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगा दिये गये। इस प्रतिबंध के साथ अनेक धार्मिक तथा नैतिक विचारों को जोड़ दिया गया। इस काल में सती प्रथा के आदर्श को और भी बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया। भारत के अधिकतर मुसलमान मूलतः हिन्दू ही थे, फलतः मुसलमानों में भी बाल विवाह का प्रचलन हो गया। हिन्दुओं की भांति कुछ मुसलमानों में दहेज की तरह वर मूल्य प्रथा का भी प्रचार हो गया।
अन्य प्रभावः हिन्दुओं के पारिवारिक जीवन की अनेक विशेषतायें मुसलमानों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर गयीं। इनमें संयुक्त परिवार भी एक थी, जिसे मुसलमानों ने अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों में शामिल कर लिया। वेश-भूषा में भी हिन्दू और मुसलमान संस्कृतियों का समन्वय हुआ। मुसलमानों के चूड़ीदार पाजामा तथा शेरवानी को हिन्दुओं ने अपना लिया। मुसलमानों ने हिन्दुओं की पगड़ी को अपना लिया।
मुसलमानों ने भारत में अनेक प्रकार की मिठाइयों को प्रचलित किया; जैसे- बालूशाही, कलाकंद, गुलाब-जामुन, बर्फी, हलवा, इमरती, जलेबी आदि। मुसलमानों के आने से मांसाहार का प्रचलन बढ़ता गया, विशेषकर उन हिन्दुओं में जिनका मुसलमानों से घनिष्ठ संबंध था। एक ओर पुरुषों में तुलनात्मक रूप से शिक्षा का विस्तार हुआ, तो दूसरी ओर बाल विवाह और पर्दा प्रथा चरम सीमा पर होने के कारण स्त्रियों की शिक्षा बिल्कुल समाप्त हो गयी।
वस्तुतः जिन विदेशी धर्मों व संस्कृतियों ने भारतीय जनजीवन व संस्थाओं को प्रभावित किया, उनमें इस्लाम सर्वप्रमुख है।Question : शेरशाह के व्यक्तित्व में शेर और लोमड़ी के स्वाभाव का सम्मिश्रण था।
(1999)
Answer : शेरशाह मध्यकालीन शासकों में एक विशेष स्थान रखता है। एक श्रेष्ठ सैनिक के गुण और विशेषतायें उसके अंदर थी और सैनिक कार्य को वह अच्छी तरह समझता भी था। एक सैनिक के रूप में उसके अंदर अमिट साहस, अपूर्व शक्ति और असाधारण शौर्य था। एक सेनापति के रूप में उसने प्रत्येक सैनिक कार्यवाही में अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा और चातुर्य का परिचय दिया था। किसी सैनिक अभियान में उसे जहां-जहां ठहरना पड़ता था, वहां वह व्यूह रचना करता था और अपने आस-पास खंदकें खुदवाता था, जिससे कभी किसी संभावित अचानक आक्रमण से पूर्व सुरक्षा रहे। सैनिक अभियानों की कठिनाइयों और अभावों को तथा भविष्य के सुख-दुखों को अपने सैनिकों के साथ भोगने के लिए वह सदा तैयार रहता था। वह अपने सैनिकों से अलग नहीं रहता था, बल्कि उनके साथ घनिष्ठता रखता था। दिल्ली विजय से पूर्व उसने बंगाल और बिहार का अपने अधिकार में कर लिया था। हुमायूं पर अंतिम विजय प्राप्तकरने के कुछ ही वर्षों के अंदर उसके साम्राज्य के अंतर्गत असम, कश्मीर और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत आ गया था। उसने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए स्थायी सेना गठित की। शेरशाह का उत्कर्ष और उसकी सफलतायें ऐसी चकाचौंध पैदा करने वाली थीं कि अधिकांश इतिहासकार उसके चरित्र के दूसरे पहलू को देखने में असमर्थ रहे हैं। सामान्य रूप से लोग यह अनुभव नहीं करते थे कि वह बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह चालबाजियों और धोखाधडि़यों को प्रायः व्यवहार में लाता था। उसने अपने शत्रुओं पर कभी सामने से आक्रमण नहीं किया। जो सैनिक चालें वह व्यवहार में लाता था, वे थीं शत्रु को बेखबर रखना, उस पर अचानक हमला बोल देना, उसे झांसा देकर किसी छिपे हुए मार्ग से सेना ले जाना और वहां उस पर कई ओर से आक्रमण करना। उसकी सैनिक कार्यवाहियां बड़ी शीघ्रता से संचालित होती थीं। उसका यह विश्वास था कि अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए बुरे-भले सभी साधन व्यवहार में लाने चाहिए। चुनार का दुर्ग उसने छल-कपट से ही अपने अधिकार में किया। अपनी वचनबद्धता को धता बताकर ही उसने रोहतासगढ़ पर कब्जा किया। अपने प्रतिद्वंद्वी मालदेव को उसने जाली पत्र तैयार करवा कर और उसके सरदारों में फूट डलवाकर ही पराजित किया था। एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से शेरशाह का उत्कर्ष न सिर्फ उसकी योग्यता अपितु उसकी चालाकी एवं सिद्धांतहीनता के कारण ही संभव हो पाया।
Question : राणा प्रताप की देशभक्ति ही उनका एकमात्र अपराध था।
(1999)
Answer : यद्यपि मेवाड़ पर फरवरी 1568 में मुगलों का अधिकार हो गया था, तथापि राज्य का एक बड़ा भाग अभी तक राणा उदय सिंह के अधिकार में रह गया था। उसके पराक्रमी पुत्र राणा प्रताप ने मुगलों का बड़ी दृढ़ता से सामना करने का निश्चय किया। महाराणा प्रताप ही राजपूताना का एक ऐसा सम्राट था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सब कुछ अर्पण कर अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर जंगल में भटकते रहे। राणा प्रताप ने एक बार आमेर के शासक मानसिंह के साथ भोजन करने से इंकार कर दिया, क्योंकि उसने अपनी बुआ का विवाह अकबर से कर दिया था। सीमित साधन, अपने ही आदमियों से असंतोष तथा अपने भाई शक्तिसिंह की शत्रुता की परवाह न करते हुए उसने उस आदमी का सामना करने का निश्चय किया, जो धरती के पर्दे पर सर्वाधिक शक्तिशाली और साधन संपन्न शासक के रूप में गिना जाता था। अकबर का भी इसी तरह मेवाड़ के शेष भाग को राणा के हाथों से छीन लेने का इतना ही दृढ़ निश्चय था। अपने श्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद अकबर मेवाड़ के उस भाग पर अधिकार नहीं कर सका, जो राणा के अधीन था। यह मेवाड़ का उत्तरी-पश्चिमी भाग था, जिसमें कुंभलगढ़ और देवसूरी के दुर्ग सम्मिलित थे। गोगुन्डा पर भी उसका अधिकार चिरकाल तक नहीं रह सका, क्योंकि मुगल सेना के पास रसद की कमी थी और वहां की जनता उसके विरुद्ध थी। न तो उसकी धमकियां और न ही उसके अत्याचार राणा को वस में कर सके। स्वाभिमानी और देशभक्त राणा को यद्यपि कई अवसरों पर भूखों मरना पड़ा, तथापि अकबर की अधीनता उसने स्वीकार नहीं की। अकबर द्वारा राणा को अधीन बनाने का सारा प्रयास असफल रहा। वास्तव में राणा प्रताप की देशभक्ति ही उसका एकमात्र अपराध था।
Question : राष्ट्रकूटों का कला एवं संस्कृति के लिए योगदान की विवेचना कीजिये।
(1999)
Answer : दक्षिण भारत के इतिहास में राष्ट्रकूटों का विशेष महत्व है। राष्ट्रकूटों ने लगभग 225 वर्षों तक राज्य किया। राष्ट्रकूटों ने भारतीय कला को अनुपम भेंट दी। चट्टान काटकर बनाये गये एलोरा और एलीफैण्टा के पवित्र स्थल इसी काल के हैं। जिस समय दंतिदुर्ग ने 753 ई. में चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया और उससे उसका राज्य छीन लिया; उस समय इस घटनाका केवल राजनीतिक प्रभाव ही नहीं पड़ा, बल्कि उसके द्वारा स्थापित नवीन राजवंश की रुचि के कारण स्थापत्य की शैलकर्तन शैली को और अधिक प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रकूटों के संरक्षण में एलोरा के खुदे हुए प्रसिद्ध मंडप तथा मंदिर शैलकर्तन शैली की उस अंतिम अवस्था से संबंधित है, जो 9वीं शताब्दी के अंत तक काफी लोकप्रिय हो गयी थी। एलोरा की पर्वतमाला संख्या 16 के पश्चिमी सिरे के आस-पास खोदकर हिंदू शैली में जो निर्माण किया गया था, उसमें ‘कैलाश मंदिर’, ‘रावण की खाई’, ‘दसावतार’, ‘रामेश्वर’ और ‘सीता की नाहिनी’ मुख्य हैं। इनमें एलोरा का कैलाश मंदिर अत्यधिक विस्तृत तथा बहुमूल्य है। इस मंदिर को आठवीं शताब्दी में कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी चट्टान काटकर बनवाया था। यह पट्टडकल के लोकेश्वर मंदिर के समान है। इसे एक वर्गाकार गुफा में काटकर बनाया गया है। यह 276 फीट लम्बा तथा 154 फीट चौड़ा तथा अंदर जाकर 107 फीट गहरा है। मंदिर के चार प्रमुख भाग हैं- मुख्य पवित्र स्थल, पश्चिम का प्रवेश द्वार, नंदि मंडप तथा अांगन के चारों ओर मठ। यह संभव है कि पूरक भवनों की बाद में खुदायी की गयी थी। मंदिर एक ऊंची कुर्सी पर बना है, जिसकी ऊंचाई 7-6 मीटर है और चोटी तथा तली दोनों पर ढलायी की गयी है। दोनों के बीच बहुत बड़े आकार के सिंहों तथा हाथियों की भव्य चित्र वल्लरी है। कुछ सीढि़यां स्तंभ वाली ड्योढ़ी तक जाती हैं। यह ड्योढ़ी भी कुर्सी पर खड़ी है। यह मंदिर भित्ति स्तंभों, आलों, कारनिसों तथा विमान जैसे मंदिर स्थापत्य के सुविदित तत्त्वों का सुव्यवस्थित सम्मिलन है। शिखर के आधार के चारों ओर पांच छोटे-छोटे पूजा गृहों के समूह हैं। प्रत्येक पूजा गृह मुख्य पूजा गृह का प्रतिरूप है। मंदिर के अंदरूनी भाग में गर्भगृह, अंतरालय तथा स्तंभों वाला मंडप है। मंडप तथा स्तंभों वाले मंडप के सामने 6 मीटर वर्गाकार का नंदि पूजागृह है। यह ऊंची कुर्सी पर खड़ा है और एक पुल से मुख्य मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। कैलाश मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार बड़े आकार वाली एक दोमंजिली इमारत है। नंदि पूजा गृह के समीप हर तरफ दो ‘ध्वज स्तंभ’ हैं। उनमें से प्रत्येक बड़े सुंदर समानुपात में हैं और बहुत सुंदर ढंग से परिष्कृत हैं।
यदि कैलाश मंदिर को उसके शैलकर्तन स्थापत्य के कारण विलक्षण माना जाता है, तो उसके शानदार तक्षित मूर्ति फलक के कारण वह उतना ही गौरवशाली भी है। दुर्गा का फलक, जिसमें देवी को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है, पौराणिक विषय वस्तु का एक प्रभावशाली चित्रण है। उसमें संघर्षरत शक्तियों की वीरता तथा उत्तेजना को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकला का एक इससे भी असाधारण उदाहरण वह फलक है, जो एक और पौराणिक विषय वस्तु से संबंधित है। इसमें राक्षस राजा रावण शिव के स्थान कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास करता है। इसमें दंभी व अभिमानी, दसानन राजा रावण को कैलाश पर्वत को उस समय हिलाते हुए चित्रित किया गया है, जिस समय शिव और पार्वती अपने कक्ष में एकांतवास कर रहे होते हैं। भयाक्रांत होकर पार्वती सुरक्षा के लिए अपने पति से लिपट जाती हैं। शांत और प्रकृतिस्थ शिव अपने पैर से पर्वत को दबाते हैं और उद्धत राक्षस को कैदी बना लेते हैं। इनमें आकृतियां यथार्थ रूप से व्यवस्थित तथा समानुपात में हैं और ये जीवन की मरीचिका को व्यक्त करती हैं।
अन्य मंदिरों में दसावतार सबसे सादा है। इसे बौद्ध विहार की तरह बनाया गया है। यह अनियमित आकार का एक खुला प्रांगण है और इसके केंद्र में एक अलग पूजागृह है। इसका प्रत्येक तल स्तंभों वाला मंडप है और चारों ओर की दीवारों पर बने आलों पर विशाल आकार की प्रतिमायें हैं, जिनमें शिव तथा विष्णु से संबंधित विषय वस्तुओं को चित्रित किया गया है। इनमें से ‘हिरण्य कश्यप’ वाला खंड सर्वोत्तम है। रावण की खाई का विन्यास सीधा-सादा है। यह आयताकार है और इसके अधिकांश स्थान में स्तंभों वाला मंडप है। शेष भाग में एक पूजा गृह है। मंडप के अंतर्गत मूर्तियां हैं, जिनमें द्वारपाल तथा दीवारों पर स्तंभ वाली गुफाओं की अन्य आकृतियां शामिल हैं। रामेश्वर गुफा का विन्यास भी समान रूप से सीधा-साधा है, परंतु इसकी दीवारों पर उत्तम नक्काशी होने के कारण यह अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध है। इसके शक्तिशाली स्तंभों के कारण यह अधिक प्रभावशाली लगता है। इन स्तंभों के शीर्ष पर सामान्य कलश तथा बेलबूटे बने हैं और उनमें वनदेवी तथा देवियों की शानदार सुसज्जित ब्रैकेट आकृतियां बनी हैं। गुफा के अंदर इस काल की कुछ सबसे शक्तिशाली मूर्तियां हैं, जिनमें ‘दुर्गा’ तथा ‘नृत्य देवता’ शिव के अद्भुत शांत नृत्य को चित्रित करने वाले फलक सबसे श्रेष्ठ हैं।
घूमर लेन एलीफेंटा गुफाओं से असाधारण रूप से मिलती-जुलती है। शिव को समर्पित मुख्य पूजा गृह एक चतुर्भुजाकार कमरा है, जो हाल के पीछे स्थित है और चारों किनारे पर महिलाओं की लघुमूर्तियों के साथ भीमकाय द्वारपालों के जोड़े पहरेदारों के रूप में बने हैं। अंदरूनी भाग में उत्तम तक्षित फलकों में से एक, जिसमें शिव एवं पार्वती के विवाह को चित्रित किया गया है, अत्यंत सुंदर है और वह एलोरा की सर्वोत्तम तक्षित आकृतियों में से एक है। एलोरा में चट्टानों को काटकर पांच जैन मंदिर भी बनाये गये हैं और उनमें ‘घोटा कैलाश’, ‘इंद्र सभा’ और ‘जगन्नाथ सभा’ प्रमुख हैं। एलिफैण्टा का प्रमुख स्थल एलोरा के स्थलों से श्रेष्ठ माना जाता है। यह बताया गया है कि एलोरा के भैरव की मूर्तिकला की अपेक्षा एलिफैण्टा की नटराज और सदाशिव की मूर्तिकला अधिक श्रेष्ठ है। एलोरा की मूर्तिकला की तकनीक में पूर्णता नहीं है, यद्यपि उसकी शैली अधिक प्रबल है। एलिफैण्टा की अर्द्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति या महेश्वर मूर्ति के आलेखन में ईश्वर को तीन रूपों में अंकित किया गया है, जो उसके तीन कार्यों को व्यक्त करते हैं: सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार।
राष्ट्रकूट शासक मुख्यतया हिंदू धर्म के अनुयायी थे, किन्तु वे धर्म सहिष्णु थे तथा उनके द्वारा बनवाये मंदिरों में विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमायें स्थापित की गयी थीं। पूजा के लिए मूर्तियों की स्थापना हेतु मंदिर बनवाये जाते थे। उन मूर्तियों की पूजा प्रतिदिन होती थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य में शिव और विष्णु की पूजा लोकप्रिय थी। अभिलेखों में उन देवताओं के अनेक उल्लेख हैं। उनकी मुहरों पर विष्णु के वाहन गरुड़ या योग मुद्रा में बैठे शिव का चित्र है। इस काल में बहुत से वैदिक यज्ञ किये गये।
दंतिदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। कई व्यक्तियों द्वारा ‘तुलादान’ या स्वयं अपने भार के बराबर सोने के दान के उल्लेख मिलते हैं। जैन धर्म को अमोघवर्ष प्रथम, इंद्र द्वितीय, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय ने संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म की इस काल में अधिक उन्नति नहीं हुई और इसका मुख्य केंद्र कन्हेरी था। अमोघवर्ष प्रथम संस्कृति प्रेमी शासक था। उसके शासनकाल की प्रमुख घटना मान्यखेत ही बनाया। वह जैन मतावलम्बी था। संजान अभिलेख में उसे देवी महालक्ष्मी का उपासक कहा गया है। अमोघ वर्ष साहित्य का संरक्षक था और उसने जिनसन, महावीराचार्य और शकटायन को संरक्षण प्रदान किया। जिनसेन ने ‘आदि पुराण’ लिखा। महावीराचार्य ने ‘गणित सार संग्रह’ की रचना की। शकटायन ने ‘अमोघवृत्ति’ की रचना की। स्वयं अमोघवर्ष ने ‘कविराजमार्ग’ लिखा, जो पद्य रचना पर पूर्वतम कन्नड़ कृति है। त्रिविक्रम भट्ट राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय (1915 ई.) का समकालीन था, जिसने ‘नल चंपू’ या ‘दयमंती कथा’ का प्रणयन किया, जो संस्कृत का सबसे प्रारंभिक चंपू है। इसमें पद्य एवं गद्य दोनों ही साधारण कोटि का है। ‘मदालसा चंपू’ भी त्रिविक्रम भट्ट का ही लिखा हुआ बतलाया गया है। राष्ट्रकूट शासन काल में कन्नड़ साहित्य को सर्वांग रूप से सुसज्जित कर रंगमंच पर लाने वाले तीन रत्न हैं- ‘पंप, पोन्न तथा रन्न। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के समकालीन ‘पंप’ ने ‘आदि पुराण’ नामक पुस्तक में प्रथम जैन तीर्थंकर की जीवन कथा का वर्णन किया है। अपनी दूसरी कृति ‘विक्रमार्जुन विजय’ में ‘पंप’ ने महाभारत की कथा को अपने ढंग से पेश किया है और इस कारण वह ‘पंप भारत’ कहलाता है। समालोचकों ने एक मत से ‘पंप’ को कन्नड़ कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना है। ‘पोन्न’ पंप का समकालीन था। उसकी मुख्य कृति ‘शांतिपुराण’ है, जिसमें उसने सोलहवें तीर्थंकर के उपाख्यानों पर आधारित इतिहास प्रस्तुत किया है। उसके द्वारा रचित ‘भुवनई करामाभ्युदय’ नामक पुस्तक अब उद्धरणों के रूप में ही उपलब्ध है। उसकी एक अन्य कृति है, ‘जिना क्षरमाले’, जिसमें जिनों की यशगाथा पद्यों में वर्णित है। कृष्ण द्वितीय ने उसे ‘उभय कवि चक्रवर्ती’ की उपाधि दी थी। तीसरा कन्नड़ रत्न ‘रन्ना’ था। उसका ‘अजीत पुराण’ द्वितीय तीर्थंकर जीवन पर बारह ‘आश्वासों’ में रचित चंपू हैं। ‘रन्ना’ की दो अन्य कृतियां ‘परशुराम चरित’ तथा ‘चक्रेश्वर चरित’ अब उपलब्ध नहीं हैं। ‘रन्न कण्ड’ नामक एक शब्दकोश भी, जिसमें साधारणतः प्रत्येक पद्य का अंत ‘कविरत्न’ शब्द से होता है, संभवतः उसी की रचना है। 978 ई. में ‘रन्न’ ने ‘त्रिशष्टिलक्षण महापुराण’ की रचना की। यह कन्नड़ भाषा की सबसे प्राचीन उपलब्ध पुस्तकों में से एक है।
Question : स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन बोनापार्ट को बर्बाद कर दिया, दक्षिण की समस्या ने औरंगजेब को बर्बाद किया था।
(1999)
Answer : औरंगजेब के शासन का उत्तरार्द्ध (1681-1707) दक्षिणी शक्तियों से युद्ध करने एवं दक्षिण में अपनी शक्ति सुदृढ़ करने में ही बीत गया। दक्षिण की समस्याओं में वह इस बुरी तरह घिर गया कि उसे उत्तरी भारत की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला, जिसके घातक परिणाम निकले। एक इतिहासकार के शब्दों में, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपालियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को नष्ट कर दिया। औरंगजेब के समय दक्षिण में तीन प्रमुख शक्तियां थीं- बीजापुर और गोलकुंडा के शिया राज्य तथा मराठे। दो बार दक्षिण का सूबेदार रहने के कारण औरंगजेब दक्षिण की राजनीति से पूरी तरह वाकिफ था। अपनी सूबेदारी के दौरान उसने इन राज्यों की शक्ति को नष्ट करना चाहा था, परंतु शाहजहां के हस्तक्षेप से वह ऐसा नहीं कर सका। अतः शासक बनने के बाद उसने दक्षिण में विस्तारवादी नीति अपनायी। उसका उद्देश्य इन राज्यों पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य में मिलाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना था। धार्मिक एवं आर्थिक कारणों ने भी औरंगजेब को दक्षिण में विस्तारवादी नीति अपनाने को प्रेरित किया। 1681 ई. में अपने विद्रोही पुत्र अकबर- II का पीछा करते हुए वह दक्षिण पहुंचा और अथक परिश्रम एवं संघर्ष के बाद 1686 में गोलकुंडा तथा 1687 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया तथा बाद में मराठा राज्य पर आक्रमण कर शिवाजी के पुत्र शंभू जी की हत्या कर दी। उपरोत्तफ़ कार्यों से मुगल साम्राज्य का चरम विकास हो गया एवं दक्षिणी अभियानों से बेहिसाब धन मिला, लेकिन वास्तव में औरंगजेब को दक्षिण अभियान से हानि ही उठानी पड़ी। मुगलों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को गहरी ठेस लगी। लंबे समय तक दक्षिण में रह जाने से उत्तरी भारत की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गयी। प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था नष्ट प्रायः हो गयी। क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास होने लगे। दक्षिण में रहने के बावजूद औरंगजेब दक्षिण पर पूर्व प्रभाव स्थापित नहीं कर सका। मराठा स्वतंत्रता संग्राम ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी और दक्षिण ही उसकी कब्रगाह बन गयी। वह दक्षिण के शक्ति संतुलन को नहीं समझ पाया और अपनी ही नीतियों में वह उलझकर रह गया।
Question : मुगलकालीन कला एवं स्थापत्य के विकास का निरूपण कीजिये तथा इनमें मिश्रित हिन्दू-तत्त्वों का निर्देश कीजिये।
(1998)
Answer : मुगलकालीन कला एवं स्थापत्य के विकास का अवलोकन करते हुए यह आसानी से देखा जा सकता है कि इनमें हिन्दू-तत्त्वों का मिश्रण बड़ी मात्र में था। चित्रकला की हिंदू और फारसी शैलियों के बीच आरंभिक आदान-प्रदान के अवशेष गुजरात में मिलते हैं। मुगलकाल से पूर्व के इन सूक्ष्म चित्रों का प्रयोग कल्पसूत्र और कालिकाचार्य कथा जैसे जैन धर्म ग्रंथों के चित्रण में किया गया है। सूक्ष्म चित्रकारी का प्रयोग बंसल विलास जैसे धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों को सज्जित करने के लिए भी हुआ है। मुगलकाल में अकबर के कला संरक्षण में हिंदू और फारसी शैलियों की एक मिली-जुली कला शैली का विकास हुआ। इस संबंध में अबुल फजल का कहना है कि, "अपनी युवावस्था से ही बादशाह सलामत का इस कला के प्रति रुझान रहा है और वे इसे पूरा प्रोत्साहन देेते हैं। अतः यह कला फली-फूली है और अनेक चित्रकारों ने बड़ा नाम कमाया है।"
अबुल फज़ल अकबर के दरबार के अनेक चित्रकारों का उल्लेख करता है, जिनमें दशवंत अग्रणी था और जिसे अबुल फजल उस युग का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार मानता है। अकबर की निगरानी में अनेक हिंदू और गैर-हिंदू विषयों से संबद्ध ग्रंथों की चित्र सज्जा की गयी, जिनमें प्रमुख हैं: हम्जानामा, चंगेजनामा, जफरनामा, रज़्मनामा (अर्थात् महाभारत), रामायण और नलमन। अकबर के संरक्षण में पनपने वाली एक अन्य कला थी- भित्ति चित्रकारी (Fresco Painting)। फतेहपुर सीकरी के कतिपय भवनों के भित्तिचित्रों में पारंपरिक विषयों के अतिरिक्त बौद्ध और मसीही विषय भी देखने को मिलते हैं, जो अकबर के सकलवादी धार्मिक दृष्टिकोण के परिचायक हैं।
जहांगीर के शासनकाल में देशी और विदेशी मिश्रशैलियों से बनी मुगल कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अपने संस्मरण ‘तूजुक-ए-जहांगीरी’ में वह अपने चित्रकारी प्रेम एवं चित्रकारी की जानकारी का विस्तार से उल्लेख करता है। जहांगीर के समय तक ग्रंथों को सूक्ष्म चित्रकारी से सज्जित करने की कला का स्थान धीरे-धीरे छवि चित्र बनाने की कला लेने लगी थी और वही मुगल कला की पहचान मानी जाने लगी थी। यूरोपीय कला के प्रभाव ने मुगल कला को और समृद्ध किया। छवि चित्र बनाने की कला शाहजहां और औरंगजब के शासनकाल में भी फलती-फूलती रही। सत्रहवीं सदी के अंत में दक्षिण में मुगलों के प्रवेश के साथ वहां चित्रकला की मुगल अथवा शाही शैली का एक आंचलिक रूप विकसित हुआ, जिसे ‘दक्कनी कलम’ कहा जाता है। बाद में मुगल शैली एवं हिन्दू शैली के मिश्रण से अन्य क्षेत्रों में राजपूत शैली एवं पहाड़ी शैली का विकास हुआ।
हिंदू-मुसलमानों की मिली-जुली संस्कृति का जैसा स्पष्ट विकास भारतीय संगीत के क्षेत्र में देखने को मिलता है, वैसा अन्यत्र नहीं। अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्त्वों के समावेश का श्रेय दिया जाता है, जिनमें क्वाल (जिसे कव्वाली का मूल भी माना जाता है) और तराना जैसी गायिकी के नये रूप सम्मिलित हैं। भारतीय राजाओं के दरबार में भारतीय संगीत के साथ-साथ विदेशी संगीत, विशेष रूप से ईरानी संगीत सुना जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय संगीत में परिवर्तन तो हुआ, किंतु उसका मूल स्वरूप बना रहा। मुगल सम्राटों- अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में संगीत अपने चरम पर था। दरबारी संगीतकारों के अतिरिक्त बड़े-बड़े नौबत भी बने, जिनमें वात एवं तालवाद्य होते थे। ये नौबत प्रायः नियमित अंतराल से नक्कारखानों या नौबतखानों में बजते रहते थे, जो प्रायः महलों और मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थित होते थे। अबुल फजल अकबर के दरबार के छत्तीस प्रमुख संगीतकारों की तालिका देता है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही सम्मिलित हैं। अबुल फजल की तालिका में अनेक यन्त्रें का भी उल्लेख है, ग्वालियर के मियां तानसेन को वह इनमें अग्रणी मानता है। इस तालिका में मालवा का भूतपूर्व शासक बहादुरशाह भी सम्मिलित है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में जिन वाद्य यंत्रों की सूची दी हैं-उनमें प्रमुख है बीन, तंबूरा, सरमंडल, रबाब और ने (बांसुरी)।
औरंगजेब के शासनकाल में संगीत का विकास थोड़े समय के लिए अवरुद्ध रहा, जिसका कारण औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता बताया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि संगीत को संरक्षण न देने के बावजूद भी औरंगजेब संगीत में रुचि रखता था और इसके सिद्धांत पक्ष को अच्छी तरह समझता था। बहादुरशाह (1707-1712) और विशेष रूप से मुहम्मदशाह (1719-48) के समय में संगीत का पुनरुद्धार हुआ। मुहम्मदशाह स्वयं भी प्रसिद्ध गायक था और उसने अनेक ख्याल’ रचे, जिनमें से कुछ आज भी प्रचलित हैं। मुहम्मदशाह के संरक्षण में सत्रहवीं सदी के एक महत्वपूर्ण संगीत संबंधी ग्रंथ ‘संगीत परिजात’ का संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ। मुगल साम्राज्य का पतन हो जाने पर संगीत आंचलिक राज्यों के दरबारों में परवरिश पाता रहा।
उत्तर भारत में तुर्कों के आगमन से पहले हिंदू वास्तुकला की शैलियों और विधियों की लंबी परंपरा विकसित हो चुकी थी। इसलिए जब तुर्क यहां आये, तो उनकी अलग वास्तुकला शैली होने के बावजूद वे हिंदू वास्तुकला से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। सल्तनत काल के स्थापत्य में इस मिश्रण के स्पष्ट प्रमाण परिलक्षित होते हैं।
मुगल काल में अकबर द्वारा निर्मित भवनों में इस्लामी, हिंदू, बौद्ध और जैन, अनेक वास्तुशैलियों का समावेश हुआ है। आगरा के किले के जहांगीरी महल में मुसलमानी और हिंदू वास्तु शैलियों का मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। इस भवन के बाहरी हिस्से में मेहराबों और मेहराबदार आलों की भरमार है, जो फारसी शैली के हैं और इनके भीतरी भाग का अलंकरण शुद्ध हिंदू शैली में किया गया है। फतेहपुर सीकरी की अनेक इमारतों के अलंकरण में भी हिंदू शैली की प्रेरणा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, विशेष रूप से जोधाबाई के महल, मरियम सुल्ताना एवं राजा बीरबल के आवास गृहों, दीवान-ए-खास और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में। पंचमहल की पिरामिड जैसी संरचना एवं सिकंदरा (आगरा) स्थित स्वयं अकबर के मकबरे में बौद्ध वास्तुशिल्प का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। इसके भीतरी भाग के अलंकरण में मुसलमानी, हिंदू और ईसाई प्रभाव देखने को मिलता है। यहां ईश्वर के निन्यानवे नामों के साथ-साथ ‘अल्लाहु अकबर’ और ‘जला जलालुह’ के साथ ही हिंदू स्वास्तिक एवं मसीही क्रास भी अंकित हैं, जो अकबर के सकलवादी धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। वैसे इस मकबरे को जहांगीर के काल में पूर्ण किया गया था।
अकबर की मृत्यु (1605 ई.) के पश्चात् मुगलों ने जिन भवनों का निर्माण कराया, उनमें से से कुछ को छोड़ कर बाकी सभी में इस्लामीकरण ही अधिक दिखायी देता है। उदाहरण के लिए नूरहजां द्वारा बनवाये गये एतमादउद्दौला के मकबरे में फारसी मेहराबों और मेहराबदार आलों के साथ हिंदू कलश और छतरियों का भी प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार, शाहजहां के समय में बनाये जाने वाले भवनों में संगमरमर में बंगाली छप्पर का प्रभाव उत्पन्न किया गया, जो किनारों से झुका हुआ होता है। शाहजहां के समय में ही नौ शिखरों वाले पर्णालकृत मेहराब का समावेश हुआ, जिनमें से प्रत्येक शिखर को अपने-आप में एक छोटी मेहराब कहा जा सकता है। यह शैली हिंदू मंदिरों का प्रभाव दर्शाती है, जिसमें शिखर का छोटा रूप स्वयं शिखर के मुख्य बाह्य अलंकरण का भाग होता है। कुल मिलाकर, आगरा, दिल्ली और लाहौर में शाहजहां द्वारा निर्मित भवनों में हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला के सुंदर समन्वय के दर्शन होते हैं। फिर भी, इनका मुख्य स्वरूप इस्लामिक ही रहा, भले ही ताजमहल हो या दिल्ली और आगरा की जामा मस्जिदें। औरंगजेब के समय इन भवनों का इस्लामिक स्वरूप अधिक दृढ़ होकर उभरा, किंतु यहां भी कहीं-कहीं हिंदू शैली आ गयी है, जैसा कि लाल किले, दिल्ली की मोती मस्जिद (1652 ई.) आदि के लंबे शिखरों और झुके हुए कोनों से ज्ञात होता है।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुगल कला और वास्तुकला अपने विकास के क्रम में हिंदू शैली की कई विशेषताओं को खुद में समाये हुए सही मायने में एक गंगा-यमुनी संस्कृति के रूप में सामने आई थी। इसी गंगा-यमुनी संस्कृति ने आने वाले दिनों की भारतीय कला को न केवल नया आधार दिया, बल्कि उसे और अधिक प्रभावित भी किया।Question : चोलों की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये?
(1998)
Answer : चोलों का शासनकाल द्रविड़ इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। चोल वंश पल्लवों का उत्तराधिकारी राजवंश था। अतः उन्हें पल्लवों की कला संपदा भी विरासत में मिली थी, जिसे चोल शासकों ने और अधिक समृद्ध किया। उनके शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला, शिल्प कला, साहित्य एवं प्रशासन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गये।
चोलकाल में तमिल साहित्य ने बहुत प्रगति की। वैष्णव तथा शैव संतों द्वारा भक्ति आंदोलन को बढ़ाने के कारण धार्मिक साहित्य के निर्माण को प्रेरणा मिली। मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति के विचार की प्रशंसा में पुस्तकें लिखी गयीं। प्रिय पूर्णम् या शेखर की ‘तिरुट्टोन्डपूर्णम’ इसी श्रेणी का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पांचवां वेद बताया जाता है। इस काल के अन्य प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों के नाम नन्दी का ‘तिरुविलाईयादल पूर्णम्’, नन्दी अन्दार नम्बी का ‘तिरुसुशई-कांड पूर्णम्’ तथा अमुदनार का ‘रामानुज नुरंदादि’ है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में 10वीं शताब्दी में तिरुकदेवर द्वारा लिखित ‘शिवकोशीन्दमाणि’ का उल्लेख किया जा सकता है। काम्बन ने 12वीं शताब्दी में तमिल भाषा में रामायण की रचना की। जयगोन्दर ने ‘कलिंग पट्टुपर्णी’ लिखी, जिसमें दूसरे कलिंग युद्ध में कुलोतुंग के पराक्रम का वर्णन है। बुद्ध मित्र का ‘विरासोलियम्’ तथा पवन्दी का ‘नन्नौर’ व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। जैन कवि अमृत सागर ने तमिल मे लिखा।
कला के क्षेत्र में द्रविड़ शैली का पूर्ण विकास चोलों के काल में ही हुआ। चोल वंशीय महान निर्माता थे और उन्होंने बड़े आकार के निर्माण कराये। पल्लवों की भांति चोलों ने विशाल सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कराया। पल्लवों की भांति चोलों ने भी कुछ विशाल तड़ागों का निर्माण कराने के साथ-साथ कावेरी तथा अन्य नदियों पर प्रस्तरों द्वारा विशाल बांध निर्मित कराये तथा विस्तृत क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए नहरों का निर्माण कराया। राजेन्द्र चोल प्रथम ने अपनी नवीन राजधानी ‘गंगैकोण्डचोलपुरम’ में एक विशाल तड़ाग खुदवाया, जिसे कोलेरून तथा वेल्लार नदियों के जल से आपूर्ति किया गया। इस विशाल तालाब के तटबंध सोलह मील तक फैले हुए थे और इसमें प्रस्तर की नालियों एवं नहरों की व्यवस्था की गयी थी।
चोलों ने वाणिज्य एवं संचार के साधनों का विकास करने के लिए विशाल राजमार्गों का भी निर्माण कराया। राजमार्गों पर निश्चित दूरी पर सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक टुकडि़यों को नियुक्त किया गया और नदी जलमार्गों पर सार्वजनिक नौकाओं की व्यवस्था की गयी।
पल्लवों द्वारा विकसित की गयी स्थापत्य कला का चरमोत्त्कर्ष चोल काल में ही हुआ। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में दसवीं शताब्दी तक निर्मित प्रारंभिक चोल मंदिर हैं, जिनमें तिरुकट्टलाई का सुन्दरेश्वर मंदिर, नरतामालै का विजयालय मंदिर एवं कदम्बरमलाई मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दूसरे वर्ग में चोल कालीन मंदिर स्थापत्य कला का युग तंजावूर के बृहदेश्वर मंदिर के साथ आरंभ होता है, जिसकी चरम स्थिति राजेन्द्र चोल-प्रथम द्वारा निर्मित गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर में परिलक्षित होती है। इस काल के मंदिरों का आकार बहुत विशाल है और इनका धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक प्रयोजनों के लिए भी उपयोग किया जाता था। गर्भगृह (देव स्थान) के ऊपर बने विमान (शिखर) एवं गोपुरम् (प्रवेश द्वार) को काफी विशाल एवं सजावट के साथ बनाया गया था। चोल कालीन मंदिरों में वास्तुकला एवं शिल्पकला का बहुत सुन्दर समन्वय मिलता है। इस काल में द्रविड़ शैली ने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया और इसी समय स्थापत्य की द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में हुआ।
चोल काल में प्रस्तर एवं धातु दोनों की अत्यंत सुन्दर मूतिर्यों की भी रचना की गयी। इस काल में विभिन्न देवी-देवताओं की अत्यंत आकर्षक मूर्तियों को निर्मित किया गया, परन्तु प्रस्तर मूर्त्तियों की तुलना में धातु या कांस्य की प्रतिमाएं कहीं अधिक सुन्दर हैं। चोलयुगीन मूर्तियों में नटराज या नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा कांस्य प्रतिमाओं में सर्वोत्कृष्ट है। नटराज एवं अन्य शिव मूर्तियों के साथ-साथ पार्वती, स्कन्द-कार्तिकेय, गणेश आदि की असंख्य प्रतिमाएं भी निर्मित की गयी, पर चोलयुगीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का ‘सांस्कृतिक निचोड़ या सार’ कहा जाता है। चोल काल की विकसित चित्रकारी कला का प्रमाण तंजौर के मंदिरों से प्राप्तहुआ है। देवताओं, अप्सराओं एवं राजपरिवार सेे संबंधित चित्रकारी बेहद ही उत्कृष्ट हैं।
चोल युग धार्मिक पुनरुत्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। इस काल में पौराणिक शैव एवं वैष्णव धर्मों का बड़ी तीव्रता से पुनर्जागरण हुआ। शैव नयनारों और वैष्णव आलवारों ने अपने भजनों, गीतों एवं प्रवचनों से संपूर्ण दक्षिण भारत को आप्लावित किया। शैव एवं वैष्णव संप्रदायों के पुनरूत्थान के परिणामस्वरूप सुदूर दक्षिण में बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रभाव कम हुआ। समकालीन वैष्णव या आलवार संतों में महान वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य उल्लेखनीय हैं। इसी काल में भारतीय धर्मों का प्रसार भारत के बाहर तेजी से होने लगा।
प्रशासन के क्षेत्र में भी चोलों की उपलब्धि उल्लेखनीय रही है। चोल अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि उनकी प्रशासन व्यवस्था अत्यंत सुगठित तथा कुशल थी। राजा वह धुरी था, जिस पर राज्य का संपूर्ण प्रशासन तंत्र अवस्थित था। सामान्यतया राजवंश के ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार प्रदान करने की परंपरा प्रचलित थी। अवरोही क्रम में चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां थीं - राज्य, मंडल, कोट्टम, नाडु एवं कुर्रम। राज्य की आय का प्रमुख साधन भू-राजस्व था, जिसे ग्राम-सभाएं वसूल करती थीं। भूराजस्व का निर्धारण सामान्यतः खेत की उर्वरता, सिंचाई की सुविधा एवं वार्षिक फसल चक्र को ध्यान में रख कर किया जाता था। चोल अभिलेखों में उपज के आधार पर खेतों को बारह श्रेणियों में विभाजित किया गया था।
चोल युग की प्रशंसा विशेष रूप से उस समय स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामसभाओं को प्रदान की गयी स्वायत्तता एवं उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण की जाती है। इस काल में विकसित एक सशक्त स्थानीय स्वशासन प्रणाली ने दक्षिण भारत की परंपराओं एवं जीवन शैली को अक्षुण्ण रखा तथा तमाम राजनीतिक परिवर्तनों एवं तूफानों के बीच समाज को संगठित बनाये रखा। ग्राम, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की प्राथमिक इकाई थे। आठवीं एवं नौवीं शताब्दी के प्रारंभ से ग्राम संस्थाओं का व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ होता है।
चोल सम्राट परान्तक के शासन के बारहवें एवं चौदहवें वर्ष (919 एवं 921 ई-) के प्रसिद्ध उत्तरमेरुर अभिलेखों से चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र विवरण उपलब्ध होता है। चोल सम्राटों ने स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में समिति प्रणाली को लागू किया, जिसे वरियम कहा जाता था। उत्तरमेरुर अभिलेखों में ग्राम समितियों या वरियम के संविधान में संशोधन का उल्लेख है। चोल अभिलेखों में मोटे-तौर पर तीन प्रकार की ग्रामसभाओं का उल्लेख प्राप्त होता है ये हैं: उर, सभा या महासभा और नगरम्। इनमें से उर, ग्राम सभा थी। सभा ब्राह्मणों की सभा थी और नगरम् व्यापारिक केंद्रों की सभा थीं। इन सभी सभाओं के सदस्यों का चुनाव लॉटरी द्वारा होता था। इन सभी सभाओं के कार्यों के लिए विभिन्न समितियां होती थीं। इन सभाओं के कार्यों में केंद्रीय शासन का हस्तक्षेप नहीं के बराबर ही था। इन सभाओं को केंद्रीय शासन द्वारा लगाया गया कर वसूल करके देना होता था।
चोलों का सैन्य संगठन बेहद विकसित और सुगठित था। चोल नरेशों ने साम्राज्य की सुरक्षा तथा विजय की दृष्टि से विशाल सेना गठित की थी। चोल सेना के तीन प्रमुख अंग थेµ पदाति, गजारोही एवं अश्वारोही। चोलों की अश्वसेना (मुनरूकैमहासनै) में अश्वों का अरब एवं खाड़ी देशों से आयात किया जाता था। कहा जाता है कि चोल गज सेना में लगभग 60,000 हाथी थे।
महान चोल नरेशों अर्थात् राजराज प्रथम एवं राजेन्द्र चोल प्रथम के शासनकाल में नौ-सेना की शक्ति में भी पर्याप्त विस्तार हुआ, जिसके बल पर चोलों ने श्रीलंका एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। इन नौसैनिक विजयों के फलस्वरूप बंगाल की खाड़ी तो ‘चोलों की झील’ ही बन गयी थी। चोल अभिलेखों में चोल सेना के सत्तर रेजीमेंटों का उल्लेख है। राजेन्द्र चोल अपनी सेना के साथ उत्तर भारत पर चढ़ाई करके तथा बंगाल के सेन राजाओं को पराजित कर उत्तर भारत में विजय हासिल करने वाला प्रथम दक्षिण भारतीय राजा बना था।
चोलों की नौ शक्ति एवं भारत के बाहर के क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के कारण विदेशी व्यापार को भी काफी प्रोत्साहन मिला था। चोल शासकों ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए चीन एवं दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से राजनयिक संबंध भी स्थापित किये थे। कुलोतुंग चोल ने 72 व्यापारियों का एक दल चीन भेजा था। चोल राज्य के कई नगर उस समय काफी प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बन गये थे, इनमें तंजावूर, गंगैकोंडचोलपुरम् एवं उरैयूर आदि प्रमुख थे।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चोलों ने अपने शासनकाल में हर क्षेत्र में काफी उपलब्धियां अर्जित की थीं। इसलिए इस युग को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाना उचित ही है। लेकिन इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चोल शासक अपनी उपलब्धियों को अधिक दिनों तक बनाये नहीं रख सके। स्थानीय ग्रामसभाओं को स्वायत्तता देने का प्रतिफल हुआ- सामंतों का उदय, जिसने केंद्र की शक्ति को कमजोर ही किया और जो अंततः चोल साम्राज्य के पतन का कारण बना।
Question : ‘अलबरुनी का भारत’ पर एक लेख लिखिये, जो 200 शब्दों से अधिक न हो।
(1998)
Answer : भारत आने वाले प्रमुख अरब यात्रियों में खीव में जन्मा अलबरुनी उर्फ अबूरैथन भी था। वह महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण (1025 ई.) के समय भारत आया था। यहां रहते हुए उसने खगोल विद्या, ज्योतिष-प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन किया। अलबरुनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिन्द अथवा किताबुल-हिन्द (हिन्दुतान का यथार्थ अथवा हिन्दुस्तान का परिचय) ग्यारहवीं शताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। अलबरुनी ने भारत को जैसा देखा, बिल्कुल वैसा ही वर्णन प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक वस्तुतः टंकार करती हुई तलवारों, जलते हुए नगरों तथा लूटे हुए मंदिरों के बीच निष्पक्ष शोध का जादुई द्वीप है। अलबरुनी की यह पुस्तक अस्सी अध्यायों में विभक्त एक बड़ा ग्रंथ है।
अलबरुनी हिन्दुओं के बारे में लिखता है कि ये लोग काफी घमंडी हैं और बाह्य जगत से बिल्कुल कटे हुए हैं। अलबरुनी लिखता है कि हिन्दुओं को अपने ज्ञान एवं विज्ञान पर बहुत घमंड है और वे बाहर से आये ज्ञान को नहीं सीखना चाहते हैं। उसके वर्णन के अनुसार देश कई राज्यों में बंटा हुआ था। ये राज्य थे-कश्मीर, सिन्ध, मालवा, कन्नौज आदि। भारतीय समाज का उल्लेख करते हुए वह जाति व्यवस्था, जाति प्रथा के आधार, कम उम्र में विवाह करने की प्रथा, पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों को विधवा के रूप में रहने आदि का वर्णन करता है। अलबरुनी के अनुसार लड़के-लड़कियों के विवाह को अभिभावकों द्वारा तय किया जाता था और लेन-देन निश्चित नहीं किया जाता था। पत्नियों को अपने पतियों द्वारा प्राप्त हुए धन को ‘स्त्रीधन’ कहा जाता था।
धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हुए अलबरुनी कहता है कि हिन्दू बहुत से देवताओं की पूजा करते हैं। यह प्रथा उनकी नासमझी का प्रमाण है। शिक्षित हिन्दू यह मानते हैं कि भगवान आंतरिक शक्ति हैं, जिसका न आदि है और न अंत। प्रशासनिक न्याय व्यवस्था का वर्णन करते हुए वह कहता है कि लिखित शिकायत करने की व्यवस्था थी। कभी-कभी मौखिक शिकायतों पर भी सुनवाई की जाती थी। शपथ और गवाही के आधार पर न्याय किया जाता था। आपराधिक मामलों में भी सजा बहुत कठोर नहीं थी, लेकिन सजा भी जाति
के आधार पर ही दी जाती थी। ब्राह्मणों को नकद जुर्माना नहीं देना पड़ता था।
भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए अलबरुनी लिखता है कि उपज का छठां भाग राजा द्वारा ले लिया जाता था। सभी मजदूरों, शिल्पकारों एवं व्यापारिक वर्गों को अपनी आय में से कर देना पड़ता था। सिर्फ ब्राह्मणों को ही कर देने से छूट प्रदान की गयी थी। मूर्तिपूजा पूरे देश में प्रचलित थी। सती जैसी क्रूर प्रथा अस्तित्व में थी और विधवाओं को कड़ाई से पुनर्विवाह से रोका जाता था तथा यातनापूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। अलबरुनी ने भारतीय समाज, यहां के रीति-रिवाजों, खान-पान, पहनावे आदि का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। अलबरुनी भारतीय विज्ञान, गणित, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि के ज्ञान की काफी प्रशंसा करते हुए विस्तारपूर्वक इनका उल्लेख करता है। उसने भारतीय नाप-तौल, भारतीय नगरों की दूरी, यहां की ऋतुओं, नदियों, पहाड़ों आदि का वर्णन भी किया है। उसके अनुसार, भारतीय राजाओं में आपसी एकता की कमी होने के कारण ही भारतीय राज्य आसानी से विदेशी आक्रमणकारियों से हार जाते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि अलबरुनी ने अपनी पुस्तक में अपने युग के भारत एवं भारतीय समाज की पूर्ण वास्तविक तस्वीर उतारने का अच्छा प्रयास किया है।
Question : राजपूतों की सामाजिक संरचना
(1998)
Answer : जाति प्रथा राजपूत क्षेत्र में प्रचलित थी। वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त कई नयी उपजातियां भी थीं। राजपूत समाज में ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा स्थान था और उनका सबसे अधिक सम्मान किया जाता था। वे समस्त आध्यात्मिक या लौकिक ज्ञान के एकमात्र अधिकारी होने का दावा करते थे। वे राजपूत राजाओं के सभासद और मंत्री होते थे। उनमें से अधिकांश अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, धार्मिक, संस्कार तथा अन्य पुण्य कर्म करने में ही अपना समय व्यतीत करते थे।
ब्राह्मण, पुरोहित और दार्शनिक समझे जाते थे। उन्हें ऐसे अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं, जो अन्य लोगों को प्राप्त नहीं थीं। ब्राह्मणों को प्राणदण्ड नहीं दिया जाता था। राजपूत शासक और सैनिक क्षत्रिय वर्ग के होते थे। व्यापार और उधार तथा लेन-देन का काम वैश्य करते थे। शूद्र खेती और शिल्प का काम करते थे। वे शेष तीन जातियों की सेवा भी करते थे। अछूत ग्राम या शहर से बाहर रहते थे।
राजपूत काल के आरंभ में तो जाति प्रथा इतनी कठोर नहीं थी, लेकिन उत्तर राजपूत काल में वह कठोर हो गयी। बाण कवि ने पार्श्व का उल्लेख किया है, जो ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री का पुत्र था। अन्तर्जातीय विवाह से उत्पन्न पुत्रों की जाति उनके पिता की मानी जाती थी। इस काल में कई नयी जातियां और उपजातियां बन गयीं। उपजातियां जन्म, व्यवसाय, निवास स्थान, रीतियों, धार्मिक संस्कारों, भोजन के अंतर आदि पर निर्भर थीं। उप-जातियां विशेषकर ब्राह्मणों में थीं। उस समय कन्नौज के ब्राह्मण, गौड़-ब्राह्मण, मालवी-ब्राह्मण, तेलुगू-ब्राह्मण, कोंकण-ब्राह्मण आदि अस्तित्व में आ गये। उसी प्रकार, क्षत्रियों और वैश्यों में भी उप-जातियां बन गयीं। अनेक व्यावसायिक जातियां भी बन गयीं, जैसे-बुनकर, जुलाहे, बढ़ई, मछुवारे, शराब बनाने वाले, तेली, ग्वाले आदि। एक नयी जाति भी बनी, जिसका नाम कायस्थ था। कायस्थों का मुख्य कार्य लेखन का था। संभवतः वे कई जातियों के थे। राजाओं के इतिहास का बखान करने वाले भाटों एवं चारणों की भी अपनी जाति थी।
राजपूत अपनी स्त्रियों का अत्यधिक सम्मान करते थे। उनमें पर्दे की प्रथा नहीं थी। राजपूत स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे अपना वर भी स्वयं चुन सकती थीं तथा शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। राजपूत स्त्रियों में सतीत्व और देशभक्ति के उच्च आदर्श थे। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए राजपूत स्त्रियां सामूहिक आत्महत्या (जौहर) करने से भी पीछे नहीं रहती थीं। विवाह की आयु कम होती जा रही थी और स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, फलस्वरूप युवा विधवाओं को कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बहुविवाह पद्धति प्रचलित थी। कन्या का जन्म राजपूतों में अच्छा नहीं समझा जाता था, क्योंकि कन्या के पिता को उसके विवाह के समय झुकना पड़ता था। अतः कई कन्याओं का जन्म के समय ही कत्ल कर दिया जाता था। कन्यायें अपने पति पर या पुरुष संबंधियों पर अधिक निर्भर होती जा रही थीं। परिवार में पिता का महत्व बहुत बढ़ गया था। अंधविश्वास भी काफी प्रचलित थे। पर्व-त्यौहारों का काफी महत्वपूर्ण स्थान हो गया था।
Question : पानीपत का तृतीय युद्ध
(1998)
Answer : पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के इतिहास के लिए मात्र इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसने मराठा शक्ति को तहस-नहस कर दिया था, बल्कि शिवाजी ने जिस नैतिक और रणनीतिक आधार पर मराठा शक्ति को संगठित किया था,उसके अंत का भी संकेत है। युद्ध में पराजय की घटना ने यह संकेत दे दिया था कि अब पेशवा एवं केंद्रीय सत्ता की पकड़ मराठा सामंतों पर पहले जैसी नहीं रहेगी और अब मराठा सामंत केन्द्र के मूल्य पर शक्तिशाली होंगे।
1759 में जब राव होल्कर और रघुनाथ राव ने दोआब तथा राजपूताना में मराठा प्रभुता को स्थापित किया तथा अहमदशाह अब्दाली के प्रतिनिधि को आत्मसमर्पण करवा कर लाहौर में सरहिन्द पर कब्जा कर लिया, तब अब्दाली ने पंजाब में प्रवेश कर पेशवा के प्रतिनिधि दत्ताजी सिन्धिया को मार दिया। अब्दाली को जहां रोहिल्लों का समर्थन प्राप्त था, वहीं मराठों को राजपूतों एवं सिखों की सहानुभूति तक प्राप्त नहीं थी। तब पेशवा ने अपने पुत्र विश्वास राव के साथ सदाशिव राव भाऊ को भेजा, जिन्होंने 1760 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन मल्हार राव होल्कर एवं सूरजमल जाट, सदाशिव के व्यवहार से उसके विरोधी हो गये थे। यमुना के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत कर भाऊ साहब कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े, किन्तु अब्दाली उससे पूर्व ही अपनी मुख्य सेना के साथ रवाना हो चुका था। पानीपत के मैदान में 19 अक्टूबर, 1960 को दोनों सेनायें आ जमीं।
शुरू में मराठों की स्थिति मजबूत थी, किंतु मराठा सेना के कुछ कमांडरों के मारे जाने के बाद मराठा सेना सभी ओर से घिर गयी व उसका रसद संबंध टूट गया। भाऊ साहब ने शत्रु से संधि करवाने की प्रार्थना की, किंतु नजीब खां के प्रभाव के कारण अब्दाली तैयार नहीं हुआ। वैसे ही अफगान सैनिक संख्या में अधिक थे और उसी दौरान श्रेष्ठ घुड़सवारों की एक और टुकड़ी के आ जाने से उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गयी थी। इसके विपरीत मराठे भुखमरी व ठंड के कारण बेहाल थे। उनके घोड़े कंकाल मात्र ही रह गये थे। समर्थ घुड़सवारों की सहायता के बिना मराठों की भारी तोपें भी बेकार हो गयी थीं, जिन पर भाऊ को बड़ा भरोसा था व सूरजमल द्वारा सलाह दिये जाने के बाद भी उसने उनको पीछे नहीं छोड़ा था। सूरजमल की मराठों की परंपरागत युद्ध प्रणाली को अपना कर शत्रु पर आक्रमण करने की सलाह को भी ठुकरा दिया था। अपने भतीजे विश्वास राव की मृत्यु के कारण भाऊ साहब के किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाने की स्थिति में मराठा सेना में भगदड़ मच गयी, जिसका फायदा उठा कर अब्दाली ने अपनी 1500 तोपों से हमला कर दिया। इस युद्ध में भाऊ साहब के अतिरिक्त तुकोजी सिंधिया, यशवंत राव पवार, पिल्लैजी यादव जैसे 27 महान सरदार, सैकड़ों की संख्या में छोटे सरदार तथा 28,000 मराठा सिपाही मारे गये। पानीपत के युद्ध में हार के कारण मराठों की प्रतिष्ठा को भारी क्षति हुई।
पानीपत के मैदान की तबाही कुछ कम हो सकती थी, यदि सदाशिव राव ने किसी सुनिश्चित योजना के अंतर्गत निर्णय लिया होता या सेना के सभी दस्तों में कुछ सामंजस्य हो पाता। रिजर्व सेना की व्यवस्था किये बिना ही उसने अपनी पूरी सेना को युद्ध की भट्ठी में झोंक दिया।
Question : सल्तनत काल की भूमि-राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिये?
(1998)
Answer : सल्तनत काल की भूमि-राजस्व व्यवस्था मुस्लिम विचारधारा और पूर्व प्रचलित देशी संस्थाओं का सम्मिश्रण थी। सुल्तानों ने इस प्रकार के भू-राजस्व संबंधी नियम स्थापित किये थे, जिनके द्वारा अधिशेष उत्पादन (Surplus) मुख्यतः इक्ता प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जाता था।
वैसे सामान्य रूप से तुर्कों ने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को अपनाया। यह व्यवस्था बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित ‘किताब-उल-खराज’में लिपिबद्ध है। इस व्यवस्था का आधार खराज और उस्र है, जो जमीनों की किस्म या भूमि की उत्पादनशीलता पर निर्भर करता है। उड्ड मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था।
जिस भूमि की सिंचाई प्राकृतिक साधनों से होती थी, वहां यह पैदावार का 1/10 प्रतिशत था और जहां कृत्रिम साधनों से होती थी, वहां यह उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। ख़राज वह भूमि कर था, जो हिंदू जमींदारों और किसानों से वसूल किया जाता था। इसकी दर निश्चित नहीं थी और इसे प्रायः अनुमान से अथवा पुराने हिंदू युग के राजस्व आलेखों के आधार पर तय किया जाता था। ख़राज कभी भी उपज का 1/3 से कम और 1/2 से अधिक नहीं लिया जाता था। केवल अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के समय में सल्तनत के कुछ भाग से उपज का 1/2 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। सल्तनत काल में भूमि की व्यवस्था की दृष्टि से उसे चार भागों में विभाजित कर दिया गया थाः (1) प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों (अक्तादार, मुक्ता) में बंटी हुई भूमि, (2) खालसा भूमि, (3) वह भूमि जो व्यक्तियों को दान के रूप में दी जाती थी, जैसे- मितक, वक्पफ़ और इनाम, जिस पर राज्य कोई लगान नहीं लेता था, और (4) वह जमीन जो अधीनस्थ हिंदू राजाओं के आधिपत्य में थी।
इस प्रकार के कृषक समाज में तीन बातों की प्रधानता दृष्टिगत होती हैः (1) जो जमींदार तुर्की शासकों द्वारा दबाये गये थे, उनमें विद्रोह की भावना बराबर रहती थी, (2) कृषक वर्ग की बदलती हुई परिस्थितियां, (3) शासक वर्ग के मध्य अधिशेष उत्पादन को अधिक से अधिक हड़पने के लिए आपस में लगातार संघर्ष।
सल्तनत काल में भू-राजस्व निर्धारण के मुख्यतः तीन तरीके प्रचलित थेः
1.बटाई: जिसमें खड़ी, कटाई की गयी फसल या वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था। बटाई प्रणाली को विभिन्न नामों, जैसे- किस्मत-ए-गल्ला, गल्ला बख्शी अथवा हासिल आदि नामों से पुकारा जाता था।
2.मसाहत: इसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था।
3.मुक्ताई: यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। तेरहवीं शताब्दी में मुक्ताई की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। यह हिस्सा-बाट प्रणाली पर आधारित थी।
कर निर्धारण के तरीकों में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन अलाउद्दीन के शासनकाल में हुआ। उसने भूमि की वास्तविक माप पर जोर दिया। राज्य का लगभग संपूर्ण केंद्रीय भाग पैमाइश द्वारा कर-निर्धारण नियम के अधीन आता था। अलाउद्दीन ने कराधान का मापदंड उच्चतम सीमा तक बढ़ा दिया। उसने चराई-कर भी लगाया था। अलाउद्दीन ने राजस्व बकाया की वसूली के लिए विजा़रत की एक शाखा स्थापित की, जिसे मुस्तखराज कहा जाता था। अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही उसकी यह प्रणाली भी समाप्त हो गयी।
सुल्तान गयासुद्दीन की नीति महान खिलजी शासन की नीति से पृथव्फ़ थी और वह किसानों को प्रसन्न तथा समृद्ध रखना चाहता था। उसने इक्ताओं और विलायतों का राजस्व निर्धारित किया तथा उसके धारकों अर्थात् इक्तादारों, मुक्ताओं और वलियों को राजस्व अदायगी के लिए केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाया। मुक्ता और वली किसानों से राजस्व की वसूली खुतों और मुकद्दमों के माध्यम से करते थे। अलाउद्दीन के विपरीत गयासुद्दीन ने खुतों और मुकद्दमों को कुछ रियायतें भी प्रदान की। गयासुद्दीन द्वारा उठाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम यह था कि उसने वास्तविक उत्पादन (हासिल) के आधार पर लगान निर्धारित करने का आदेश जारी किया। गयासुद्दीन द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से राजनेता जैसा था, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर फसल खराब हो जाने तथा ऐसी ही अन्य आकस्मिक आपदाओं की स्थिति में छूट देने की व्यवस्था की गयी थी। हिन्दू कृषकों के प्रति भी वह उदार था और निश्चित रूप से उसने यह आदेश जारी किया कि उन पर इतना अधिक कर नहीं लगाया जाना चाहिए कि वे अपनी भूमि छोड़ने के लिए मजबूर हो जायें।
सम्राट मुहम्मद बिन तुगलक की दोआब में कराधान बढ़ाने की नीति सफल नहीं हो सकी। उसने दोआब क्षेत्र को लगान वृद्धि के प्रयोग के लिए चुना था, क्योंकि वह उपजाऊ क्षेत्र था तथा केंद्र के निकट स्थित था। लेकिन वह निश्चित ही नये कर नहीं लगाना चाहता था। वह केवल अलाउद्दीन की नीति का ही अनुसरण करना चाहता था और वह भी केवल एक सीमित क्षेत्र अर्थात् दोआब में ही।
इक्ताएं प्रदान करने की प्रथाएं जारी रहीं तथा मुक्ती और आमिल राजस्व वसूली का कार्य करते थे। फिरोज तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही स्थायित्व और व्यवस्था कायम करने हेतु तत्काल आदेश जारी किये। उसने सभी समुदाय के व्यक्तियों का विश्वास जीतने का भरसक प्रयास किया। फिरोज ने कृषि कर के अतिरिक्त हक्कीशिर्व या सिंचाई कर (नहरों द्वारा सिचाई भूमि पर उपज के 1/10 भाग की दर से) के माध्यम से और उद्यानों की आय से अपनी आय बढ़ाने का प्रयास किया। सुल्तान को जजि़या से काफी राशि प्राप्त होती थी। जजि़या के अतिरिक्त खम्स, घरी आदि भी राज्य की आय के महत्वपूर्ण साधन थे।
सल्तनत काल में भू-राजस्व प्रशासन के लिए भी विभिन्न अधिकारी थे। वजीर सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसकी सहातया के लिए नायब वजीर होता था। वकूफ, व्यय के मामले देखता था, मुस्तौफी-ए-मुमालिक (महालेखा परीक्षक) तथा गुमाश्ता, सरहंग, नवीसंद आदि सभी राजस्व के कार्य से संबंधित थे। पटवारी गांव की भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखता था तथा कारकून (क्लर्क) पटवारी को अपने कर्त्तव्य निभाने में सहायता देता था।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्व की इस प्रक्रिया द्वारा राजस्व लेने का ढंग नियमित हो गया और मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। राजस्व के नकद भुगतान के कारण किसानों को अपना अनाज व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस संबंध में अनाज व्यापारियों का भी प्रसंग मिलता है, जैसे- कारवानी, बंजारा आदि। इसके साथ-साथ अनाज मंडी (जहां अनाज संग्रह करके बेचा जाता था) तथा साहूकार (महाजन, मुल्तानी, मारवाड़ी) इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। इस राजस्व ढांचे द्वारा मुद्रा-प्रचलन को भी काफी प्रोत्साहन मिला।
Question : अकबर की उदारता की नीति का सोदाहरण प्रतिपादन कीजिये।
(1997)
Answer : अकबर उत्तर मध्यकालीन भारत का एक महान शासक था। मुगल बादशाहों में वह सर्वश्रेष्ठ तो था ही, परंतु उसकी गणना विश्व के महानतम विभूतियों में भी होती है। लगभग सभी तत्कालीन एवं आधुनिक इतिहासकारों ने मुक्तकंठ से अकबर की प्रशंसा की है। वह अपनी उदारता की नीति से वह सभी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर पाया और अपने कार्यों से वह राष्ट्रीय सम्राट की दर्जा पा सका। उसने अपनी धार्मिक नीति में, सामाजिक अंतःक्रिया में, अन्य राज्यों के साथ संबंधों में, वास्तुकला, चित्रकला,- संगीतकला जैसी कलाओं में भी अत्यंत उदारता को प्रदर्शित किया। अपनी उदारता की नीति के लिए अकबर को सदा ही याद रखा जायेगा।
अकबर एक धार्मिक सहिष्णु, प्रवृत्ति का शासक था। भारत का सम्राट बनते ही उसने तुर्क-अफगान शासकों की धर्मांधता की नीति को तिलांजलि दे दी। वह जानता था कि भारत का सम्राट बनने के लिए संकीर्णता की नीति को त्यागना ही होगा। वह हिन्दुओं और मुसलमानों को एक ही धरातल पर खड़ा कर उसके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहता था। इसलिए उसने धार्मिक उदारता की नीति निर्धारित की। वह अपनी बाल्यावस्था से ही मुगलों, तुर्कों, अफगानों ईरानियों तथा राजपूतों के प्रभाव में रहा। इसी कारण उसमें सांप्रदायिकता की भावना का विकास न होकर उदारता की भावना का विकास हुआ। उसने सभी धर्मों को देखा-सुना और उसके अच्छे गुणों से प्रभावित हुआ। इसी कारण उसने ‘दीन-ए-इलाही’ नाम की एक नई जीवन पद्धति को संचालित करने का प्रयास किया। इस नई पद्धति में सभी धर्मों की मूलभूत बातों का समावेश किया गया था। इसका पालन करने वालों को एक प्रकार के आचरणिक अनुशासन में बंधे रहना पड़ता था। हालांकि ‘दीन-ए-इलाही’ के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन अकबर इसे स्वीकार करने के लिए किसी पर दबाव डालने के पक्ष में नहीं था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी इस धर्म को भयभीत होकर स्वीकार करे। उसकी इच्छा थी कि लोग अपनी खुशी से अगर चाहें तो इसके सदस्य बन जायें। इसके प्रचार-प्रसार के लिए अकबर ने धन या बल का प्रदर्शन नहीं किया। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि इसकी सदस्यता से इंकार करने वालों को दंडित किया गया ही।
हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने जजिया एवं तीर्थयात्र कर समाप्त कर दिया। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदुओं को मंदिरों के निर्माण का अधिकार मिला। इसी प्रकार अन्य सभी धर्मावलम्बियों सिखों, पारसियों, ईसाइयों को भी सभी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी। यह अकबर की उदारता की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था। इसके द्वारा साम्राज्य में रहने वाली प्रजा को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। इन उपायों के द्वारा अकबर ने वैमनस्य और द्वेष के स्थान पर आपसी सद्भाव, सहयोग एवं धर्म सहिष्णुता की भावना जगाकर राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया।
अकबर ने सामाजिक अंतर्क्रिया में भी अपनी उदार नीति का सहारा लिया। हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा एवं बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। आपसी घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के लिए उसने अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया। स्वयं भी उसने राजपूत लड़कियों से शादी की। उसने आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरखा बाई से शादी की। अकबर ने राजपूतों से संबंध स्थापित करने में भी उदारता दिखाई। जिन राजपूतों ने उसके साथ सहयोग किया, उन्हें ऊंचे-ऊंचे पदों पर बहाल किया गया, दरबार में सम्मानित स्थान मिला, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी तथा अनेक सामाजिक सुधार किये गये, जिससे राजपूतों की स्थिति में सुधार हुआ। कछवाहा नरेश भारमल, भगवानदास, मानसिंह, टोडरमल, बीरबल आदि को महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद प्रदान कर उनकी प्रशासनिक प्रतिभा का सम्मान किया गया। दरबार में भी उन्हें सम्मानजनक एवं उचित स्थान दिया गया। शाही महलों में हिन्दू रानियों को भी अपने धार्मिक विश्वास एवं प्रथा के अनुसार आचरण करने की छूट दी गयी। अकबर ने हिन्दू पर्वों जैसे दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, शिवरात्रि आदि को मनाना आरंभ किया। हिंदुओं के साथ न्याय करने के लिए हिन्दू न्यायाधीशों की बहाली की गयी। जिन हिन्दुओं को पहले धर्मांध शासकों ने जबरदस्ती अपना धर्म परिवर्तन करने को बाध्य किया था, उन्हें फिर से अकबर ने अपना पुराना धर्म स्वीकार करने की आज्ञा प्रदान कर दी। इसके साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर भी रोक लगा दी गयी। विधवाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया। अकबर ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उदारता की नीति लागू की। उसने संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद कराया। संस्कृत से अनूदित पुस्तकों में महाभारत, रामायण, लीलावती, अथर्ववेद, राजतरंगिणी, नलदयमंती, पंचतंत्र आदि महत्वपूर्ण है। संस्कृत के अतिरिक्त तुर्की, अरबी भाषाओं का भी फारसी अनुवाद कराया गया। स्थापत्य कला में उसने राजपूती कला शैली एवं तीरा-ब्रेकेट प्रणाली का भी काफी प्रयोग किया। अपना स्वयं का मकबरा उसने बौद्ध शैली में बनवाया। उसके काल में ईरानी और भारतीय चित्रकला के सम्मिश्रण से कला की एक नयी शैली पनपी, जिसे ‘मुगलशैली’ कहा गया। चित्रकला को उसने ईश्वर को जानने का साधन बताया और कट्टर इस्लाम समर्थकों की दलीलअनसुनी कर दी। अकबर के दरबार में बसावन, ताराचंद, सांवलदास, केशव, जगन्नाथ और दसंवत जैसे हिंदू चित्रकार उपस्थित थे। संगीतकला के क्षेत्र में भी उसने अपनी उदारता का परिचय दिया। उसके दरबार में हिन्दू-मुसलमान, देशी-विदेशी दोनों ही प्रकार के संगीतज्ञ रहते थे। अबुलफजल ने 36 संगीतज्ञों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें तानसेन, बैजू बावरा, अब्दुर्रहीम खानखाना, रामदास, सूरदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अबुलफजल गायिकाओं का भी उल्लेख करता है।
उसने विदेशी संबंधों में भी उदारता का परिचय दिया। अकबर सुन्नी धर्म को मानता था, जबकि उसके स्वजाति उजबेकों ने साथ मिलकर शिया मतावलंबी फारसी शासकों पर आक्रमण करना चाहा तो अकबर ने उजबेकों की मांग ठुकरा दी। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अकबर ने हर क्षेत्र में उदारता की नीति प्रदर्शित की। वह भारतीयों में यह भावना लाने में सफल रहा कि विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदयों तथा वर्गों के होते हुए भी वे भारतीय है और उनमें एकता, सहयोग, सद्भावना तथा देश प्रेम का होना आवश्यक है।
Question : "अपने उत्तरवर्ती युगों तक, सिंधु सभ्यता की अविच्छिÂ व्याप्ति मात्र धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी।य् इस वक्तव्य का विश्लेषण कीजिये।
(1997)
Answer : प्रायः प्रत्येक सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती संस्कृति का परिवर्तित एवं विकसित रूप होती है और अपने परवर्त्ती सभ्यताओं को कुछ देकर ही विलीन होती है। इसी क्रम में पुरातत्त्व की दृष्टि से किये गये अनुसंधानों से पता चलता है कि हड़प्पा चरण से अब तक एक शैलीगत निरंतरता बनी रही है। नगरों के अंत का अर्थ यह नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इसे तो शासन तंत्र और अर्थव्यवस्था में केन्द्रीयकृत व्यवस्था का अंत मात्र ही माना जा सकता है। बच रही लोक-संस्कृतियों ने धार्मिक परंपराओं को निश्चय ही बरकरार रखा। सिंधु सभ्यता के पुरोहित वर्ग आर्य समुदाय में मिल गये। लोक समुदायों ने शिल्पकारिता की परंपराओं को भी बनाए रखा। एक बार जब पुनः प्रारंभिक भारत में नगरीय साक्षर परंपरा उभरी तो उसने लोक संस्कृति के समस्त तत्त्वों को आत्मसात कर लिया।
सिंधु सभ्यता में जिस प्रकार से देवी-देवताओं का अंकन किया गया है, उसे बहुदेववाद का आरंभ माना जा सकता है तथा परवर्ती युगों में यह बहुदेववाद एक प्रचलित परंपरा रही। पशुपति, पार्वती और लिंगपूजन का मत सिंधु सभ्यता से ही चलता आ रहा है। कालीबंगा के अग्निपूजन ने संभवतः वैदिक पूजन-पद्धति में स्थान पाया। यजुर्वेद तक आते-आते लिंग को कर्मकाण्ड में स्थान मिलने लगा और बाद में यह शिव का विशेष प्रतीक बन गया। सिंधु घाटी के योनि पूजन ने ही परवर्ती काल में शाक्त धर्म का रूप ले लिया।
सिंधु सभ्यता में मिली योगी की मूर्ति से जिस योग क्रिया का ज्ञान होता है वह बाद के भी संप्रदायों में भी देखी गयी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जल एवं स्नान के धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करता है, जो आज भी प्रासंगिक है। सिंधु सभ्यता के पशु पूजा को बाद में व्यापक मान्यता मिली। नाग, बैल, बत्तख एवं गरुड़ पक्षी की पूजा हड़प्पाई परंपरा से प्रभावित प्रतीत होती है। विभिन्न पशु-पक्षियों को देवी-देवताओं का वाहन मानकर उसे मंदिरों में स्थापित किया गया। सिंधु सभ्यता की पशु बलि ऐतिहासिक काल में भी प्रचलित रही। सिंधु सभ्यता में प्रचलित स्वास्तिक एवं चक्र जैसे प्रतीक आज भी पर्याप्त धार्मिक महत्व रखते हैं। पीपल जैसे वृक्षों की पूजा करने की परंपरा का उद्भव सिंधु सभ्यता से ही हुआ। परवर्ती काल में प्रचलित जैन तीर्थंकारों की कायोत्सर्ग मुद्रा वाली मूर्तियां सिंधु सभ्यता की नग्न मूर्तियों से मिलती-जुलती हैं। परवर्ती काल में अत्यधिक लोकप्रिय ताबीज-गंडे का उपयोग भी सिंधु सभ्यता से ही प्रेरित था। परवर्ती काल में देवताओं के लिए ध्वज निर्माण की जिस परंपरा का प्रचलन हुआ, उस पर सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्रभाव था।
इसके अलावा सिंधु सभ्यता में प्रचलित कई घरेलू बातें भी परवर्ती सभ्यता का अंग बन गईं। पवित्र स्थलों, नदियों, वृक्षों, पवित्र पशुओं और मिथकों के प्रतीक में विश्वास इतिहास के परवर्ती चरणों में स्पष्ट रूप से चलता आ रहा है। आधुनिक भारत में भी कुंभकारों के चाक, बैलगाडि़यां और नौकाएं तैयार करने के तरीके ठीक वही हैं जो हड़प्पाई लोगों के थे।
कपास का प्रचलन, विविध प्रकार के आभूषणों का प्रचलन, स्त्रियों का केश विन्यास, हाथी दांत के कंघे, काजल, रूज, लिपिस्टिक जैसे प्रसाधनों का प्रचलन सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। बढ़ईगीरी, स्वर्णकारी, राजगीरी जैसे शिल्पों का प्रचलन सिंधु सभ्यता से ही हुआ है। हाथी, बकरियां, गधे, कुत्ते, मुर्गी जैसे पालतू पशुओं की परंपरा आज भी बनी हुई है। माप-तौल के बाटों का प्रयोग, 16 की इकाई में नाप-तौल, जल निकासी एवं नगर नियोजन की प्रणाली बाद में भी जारी रही। कुछ विद्वान सिंधु सभ्यता की ताम्र पट्टिकाओं को आहत सिक्कों का पूर्व रूप मानते हैं। उत्तर भारत में गेहूं हड़प्पा काल से लेकर आज तक मुख्य खाद्य पदार्थ बना हुआ है। पकाई ईंटों का प्रयोग आज भी जारी है। मोहनजोदड़ो के गढ़ी वाले टीले में स्तंभयुक्त भग्नावशेष मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के स्तंभों पर आधारित भवनों की याद दिलाते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर वृषभ का सजीव एवं प्रभावोत्पादक अंकन की ही पुनरावृत्ति अशोक द्वारा स्थापित रामपुरवा के स्तंभ में हुई है। मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी में भारतीय नारी सौंदर्य के आदर्शों का कुछ अंश मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित योगी की मूर्ति जिस तरह से बायां कंधा ढंके दायें के नीचे से होकर वस्त्र धारण किये दिखाया गया है, वही विधि हम परवर्ती बुद्धमूर्तियों में भी पाते हैं।
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने परवर्ती युगों तक सिंधु सभ्यता की अविछिÂ व्याप्ति धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों सहित सामाजिक-आर्थिक एवं कलात्मक गतिविधियों में भी थी। Question : दिये गये मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों पर निशान लगाइए और मानचित्र में अंकित स्थानों पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखियेः
1. अमरकोट, 2. असीरगढ़, 3. औरंगाबाद, 4. बेलूर, 5. बुरहानपुर, 6. चंदेरी 7. चंद्रनगर, 8. गोलकुंडा, 9. हांसी, 10. जंजीरा, 11. जौनपुर, 12. जूनागढ़, 13. कांची, 14. कंधार, 15. कन्नौज, 16. कड़ा, 17. कावेरीपत्तनम, 18. कोणार्क, 19. मुल्तान, 20. मुर्शिदाबाद, 21. नागपुर , 22. नासिक, 23. पुरी, 24. राजामुंदरी, 25. रत्नागिरी, 26. सतारा, 27. तालीकोटा, 28. तिरुचिरापल्ली, 29. वातापी, 30. वेंगी।
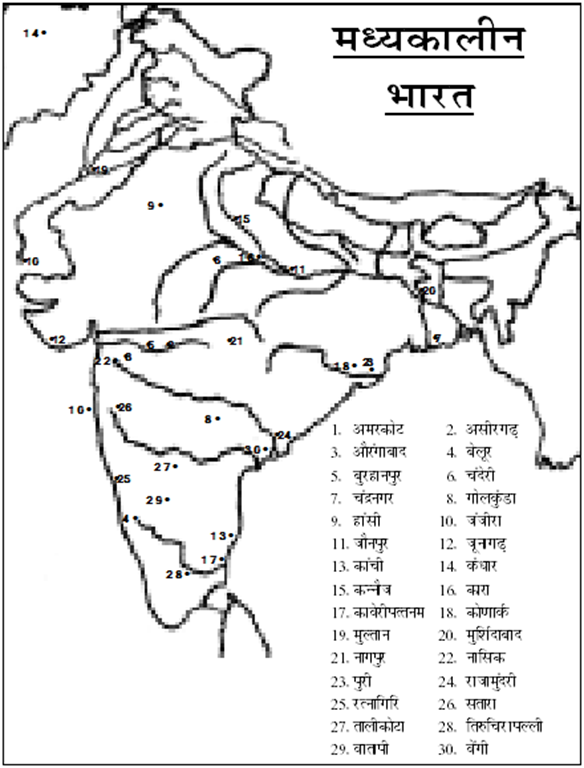
(1997)
Answer : 1. अमरकोट: पाकिस्तान में सिंध राज्य के थारपारकर जिले में स्थित अमरकोट में ही हुमायूं ने अपने निर्वासन के काल में शरण ली थी और यहीं के शासक वीरसाल के घर में महान मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था।
2. असीरगढ़: मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जि़ले में स्थित असीरगढ़ मध्यकाल में अपने मजबूत किले के कारण अतिविख्यात था। यह दिल्ली सल्तनत एवं फर्रूखी शासन के अधीन रहा था, लेकिन 1601 ई. में इसे अबकर ने जीत लिया। यह अकबर की अंतिम विजय थी।
3. औरंगाबादः मध्यकाल में यह बहमनी शासकों तथा अहमदनगर के निजाम शासन के अधीन रहा। जब औरंगजेब को दक्षिण का गवर्नर बनाया गया, तो उसने इसे अपना केंद्र बनाया। औरंगजेब ने अपनी बेगम राबिया उद्दौरानी की याद में यहां ‘बीवी का मकबरा’ भी बनवाया था।
4. बेलूर: होयसल राज्य की सीमा में स्थित बेलूर में स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने पाये जाते हैं। फारसी पर्यटक अब्दुर्रज्जाक ने यहां के केशव मंदिर की काफी प्रशंसा की थी। विजयनगर शासकों ने भी यहां स्थापत्य कला का विकास किया था।
5. बुरहानपुर: खानदेश के सुल्तान बुरहानुद्दीनवली के नाम पर बसाये गये बुरहानपुर में ही शाहजहां की बेगम मुमताज की मृत्यु हुई थी। मुगल काल में यह दक्कन सूबे का मुख्यालय था।
6. चंदेरी: आरंभ में यहां राजपूतों का और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। बाबर ने यहीं के शासक मेदनी राय को हराकर इसे जीत लिया और इसे मुगल राज्य में मिला लिया। बाद में यहां बुंदेलों का शासन रहा।
7. चंद्रनगर: 1674 ई. में शाइस्ता खां ने इसे फ्रेंच इंडिया कंपनी को दे दिया और 1690.92 के बीच यहां फ्रांसीसियों ने एक व्यापारिक केन्द्र की स्थापना की। 1950 में भारतीय गणतंत्र की स्थापना तक यह फ्रांसीसियों के अधिकार में ही रहा था।
8. गोलकुंडा: आरंभ में वारंगल के काकातीय शासन के अधीन रहने वाले गोलकुंडा पर बहमनी शासकों का अधिकार रहा। बाद में 1687 ई. में इसे औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
9. हांसीः 1192 ई. में इसे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं के किले में अर्कली खां को बंद किया था। यह सूफियों का एक महान केंद्र था।
10. जंजीरा: मध्यकाल में जंजीरा के पथरीले टापू पर सिद्दियों का अधिकार था। शिवाजी और इनके बीच संघर्ष हुआ था परंतु शिवाजी इन्हें परास्त नहीं कर पाये थे। बाजीराव प्रथम ने इन्हें हराया था।
11. जौनपुर: ‘पूर्व का शिराज’ कहे जाने वाले जौनपुर में शर्की वंश का शासन था। उस काल में यहां काफी सांस्कृतिक उन्नति हुई। अटाला मस्जिद, जामी मस्जिद, झंझरी मस्जिद यहां के प्रसिद्ध स्मारकों में से हैं।
12. जूनागढ़ः जूनागढ़ गुजरात के शासकों के अधीन रहा। यहां गुजरात के शासकों ने नौसेना एवं नौपरिवहन का विकास किया था। गुजराती शासक बहादुरशाह यहीं पर पुर्तगाली हमले में मारा गया था।
13. कांची: मध्यकाल में कांची पल्लवों एवं चोलों के अधीन रहा तथा बाद में यहां पांड्यों का भी शासन रहा। विजयनगर शासकों ने यहां स्थापत्यकला को विकसित किया था। यद्यपि पल्लवकालीन स्थापत्य कला यहां की वास्तविक प्रसिद्धि का कारण है।
14. कंधार: संप्रति अफगानिस्तान में स्थित कंधार का मध्यकाल में अत्यंत सामरिक महत्व था और इसी कारण सभी शासक इसे अपने अधीन रखना चाहते थे। भारत एंव ईरान के बीच यह शुरू से ही झगड़े का कारण रहा, परंतु जहांगीर के काल में ईरान ने इसे अपने राज्य में मिला लिया।
15. कन्नौज: त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी होकर प्रतिहारों ने यहां सत्ता स्थापित की, लेकिन बाद में यह गहड़वाल शासकों के अधीन हो गया। महमूद गजनवी ने इसे लूटा था।
16. कड़ा: इलाहाबाद के निकट स्थित कड़ा मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण इक्ता था। अलाउद्दीन खिलजी यहीं का सूबेदार था। यहीं पर जलालुद्दीन की हत्या हुई थी।
17. कावेरीपत्तनम्: चोल, पल्लव, विजयनगर शासकों के अधीन इसका विकास एक तटीय नगर एवं बंदरगाह के रूप में हुआ था। यहां से विदेशी व्यापार संचालित किये जाते थे।
18. कोणार्क: उड़ीसा में समुद्री तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के स्थित होने से विख्यात है। इसे ‘काला पैगोडा’ भी कहा गया है। इसे चोड़गंग शासकों के काल में बनवाया गया था।
19. मुल्तान: सिंध राज्य में मुल्तान स्थित था। यहां अरबों का आक्रमण हुआ था। यह बाद में दिल्ली सल्तनत एवं मुगलों की अधीनता में आ गया। यह एक विख्यात व्यापारिक केंद्र था।
20. मुर्शिदाबाद: इसकी स्थापना बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खां ने की थी तथा बाद में इसे बंगाल की राजधानी बनाया गया। जब कलकत्ता का विकास हो गया तो इसकी प्रसिद्धि जाती रही। यह एक विख्यात व्यापारिक केंद्र था।
21. नागपुर: आरंभ में यहां बहमनी तथा अहमदनगर के शासकों का शासन रहा। बाद में मराठा शक्ति के अधीन यहां भोंसले का शासन रहा। उस दौर में यहां काफी तरक्की देखी गयी।
22. नासिक: महाराष्ट्र में गोदावरी के उद्गम स्थल पर स्थित नासिक पर आरंभ में देवगिरि के शासकों का शासन रहा तथा बाद में दिल्ली सल्तनत, बहमनी, निजामशाही एवं मराठों का शासन रहा। यहां से कई ऐतिहासिक अभिलेख मिले हैं।
23. पुरी: मध्यकाल में पुरी एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित था। यहां का जगन्नाथ मंदिर आज भी श्रद्धालुओं का केंद्र है। अनंतवर्मन चोड़गंग ने पुरी का विकास कराया था।
24. राजामुंदरी: यह पहले वारंगल के काकातीय शासकों तथा बाद में विजयनगर के शासकों के अधीन रहा था। आधुनिक काल में यहीं फ्राजामुंदरी सोशल वर्क्स" नामक संस्था की स्थापना की गयी थी।
25. रत्नागिरि: महाराष्ट्र की पश्चिमी समुद्री सीमा पर स्थित रत्नागिरि मराठों के अधीन था। यहां कई प्राकृतिक किलों का विकास किया गया था। शिवाजी ने इस पर अधिकार कर लिया था।
26. सतारा: सतारा महाराष्ट्र में स्थित है। इसे शिवाजी ने जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। यहीं पर मराठों की दूसरी शाखा ने शासन किया।
27. तालीकोटा: रायचूर दोआब में स्थिततालीकोटा सदा ही बहमनी एवं विजयनगर के शासकों के मध्य संघर्ष का कारण बना रहा। 1565 ई. में हुए यहां के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा नष्ट हो गयी थी।
28. तिरुचिरापल्ली: तमिलनाडु में कावेरी तट पर स्थित तिरुचिरापल्ली पर आरंभ में चोल, पांड्य एवं विजयनगर के शासकों का शासन रहा। बाद में यह मद्रास प्रेसीडेंसी के अधीन हो गया।
29. वातापी: पूर्व मध्यकाल में वातापी में चालुक्यों का शासन रहा था। यह चालुक्यों की राजधानी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने वातापी को ही जीतकर ‘वातापीकोंडा’ की उपाधि ली थी।
30. वेंगी: वेंगी आरंभ में पल्लव शासन के अधीन था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीत लिया और विष्णुवर्द्धन के नेतृत्व में चालुक्यों की दूसरी शाखा को बसाया। बाद में यहां चोल एवं वारंगल के काकातीय शासकों का भी शासन रहा था।
Question : अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत प्रशासनिकऔरआर्थिक विनिमयों का भारतीय राज्य एवं जनता पर क्या प्रभाव पड़ा?
(1997)
Answer : अलाउद्दीन खिलजी एक प्रतिभा संपन्न एवं दूरदर्शी शासक था। वह सिर्फ अपनी निरंकुशता ही कायम नहीं करना चाहता था बल्कि जनसाधारण एवं सैनिकों के लिए कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराकर लोकप्रियता भी प्राप्त करना चाहता था। वह लोगों को निर्धन बनाकर उनकी षड्यंत्रकारी मनोवृत्तियों पर भी अंकुश लगाना चाहता था तथा मंगोलों से सुरक्षा के लिए एक विशाल सेना भी रखना चाहता था। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन ने अपनी प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियां निर्धारित कीं और
उसके मनोवांछित प्रभाव से वह अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा की पूर्ति कर पाया।
निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इच्छा को ही कानून का रूप दे दिया और अपने राजत्व सिद्धांत के माध्यम से अपने को उलेमा एवं अमीरों के नियंत्रण से मुक्त करा लिया। उसके राज्यारोहण के आरंभिक वर्षों में उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और कारणों का विश्लेषण कर उसे रोकने हेतु कुछ प्रशासनिक नीतियां बनाईं। उन प्रशासनिक नीतियों में निम्नलिखित प्रावधान किये गये थे:
उपरोक्त प्रशासनिक नीतियों से अलाउद्दीन को काफी आर्थिक लाभ हुआ। उसके पास काफी संपत्ति एकत्रित हो गयी और इसका उपयोग उसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने में किया। गुप्तचर व्यवस्था को संगठित कर देने से सरदार, अमीर एवं जनसाधारण भी सुल्तान के विषय में बातें करने से डरने लगे। मद्यपान पर निषेध तथा अमीरों के आपसी मेलजोल एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा देने से राज्य में फैले षड्यंत्रों का जाल सदा के लिए समाप्त हो गया, अपने जीवनपर्यंत सुल्तान को फिर किसी अन्य विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा।
अलाउद्दीन की राजस्व नीति भी राजनीति से प्रेरित थी। जमींदार वर्ग इस समय तक काफी शक्तिशाली हो चला था। वह किसानों से मनमाना लगान वसूल कर उसका कुछ हिस्सा ही राज्य को देता था और शेष स्वयं ही हजम कर जाता था। जमींदारों ने अनधिकृत तौर पर बहुत भूमि भी अपने कब्जे में ले रखी थी, जिस पर वे कर नहीं देते थे। इससे एक तरफ तो राज्य को आर्थिक क्षति होती थी एवं दूसरी तरफ अपने धन के बल पर जमींदार वर्ग हमेशा षड्यंत्रों में लगा रहता था। अलाउद्दीन ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वैसे सभी लोगों से जमीन वापस ले ली, जिन्हें पहले से ही मिल्क, इनाम, इन्द्रारात व वक्फ के रूप में जमीन मिली हुई थी, परंतु वे अब राज्य की सेवा करने के योग्य नहीं रह गये थे। अब भूमि वैसे लोगों को दी गयी जो राज्य की सेवा में कार्यरत थे और जो ठीक से इसकी देखभाल कर सकते थे। खुत, चौधरी एवं मुकद्दम जैसे राजस्व अधिकारियों से लगान वसूली का काम वापस ले लिया गया और उन्हें राज्य का वेतनभोगी कर्मचारी बना दिया गया। इसके चलते उनकी आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गयी। लेकिन इसके प्रभाव से सुल्तान के आर्थिक हितों के साथ-साथ राजनीतिक हितों की भी रक्षा हुई।
अलाउद्दीन की राजस्व संबंधी नीति काफी सफल रही। इसने उसके राजनीतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को पूरा कर दिया। परन्तु जनता पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। उसकी आर्थिक अवस्था दयनीय हो गयी। चूंकि उपज का अधिकांश हिस्सा राज्य ही ले लेती थी, इसलिए किसानों को उपज बढ़ाने की चिंता नहीं रही। लेकिन यह नीति राज्य के हित में लाभदायक सिद्ध हुई। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल एवं स्थायी सेना की व्यवस्था की थी। सेना को सस्ते दामों में आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए बाजार एवं मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू की गयी। बाजार की सारी व्यवस्था ‘दीवान-ए-रियासत’ नाम के अधिकारी को सौंप दी गयी। सभी व्यापारियों को ‘शहना-ए-मंडी’ में पंजीकृत कराने को कहा गया तथा सिर्फ पंजीकृत व्यापारियों को ही व्यापार करने की अनुमति दी गयी। इन्हें आवश्यक मात्र में सामानों की आपूर्ति करनी पड़ती थी एवं निश्चित मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचनी पड़ती थीं। प्रत्येक सामान की दर तय कर दी गयी थी। निर्धारित मूल्यों की सूची व्यापारियों एवं बाजार के अधिकारियों के पास रहती थी। बाजार के नियमों को भंग करने वालों को दंड देने के लिए ‘सराय-अदल’ नामक पदाधिकारी था। कीमती एवं दुर्लभ वस्तुओं की बिक्री पर भी नियंत्रण लगा दिया गया। इन उपायों का परिणाम संतोषप्रद निकला। बाजार में निश्चित मूल्य पर वस्तुएं मिलने लगीं। किसी सामान की कमी भी नहीं रही। दंड के भय से नाप-तौल की बेईमानी, चोर-बाजारी, सट्टे-बाजारी जैसे तत्त्व समाप्त हो गये। बाजार में अन्न की कमी नहीं होने देने के उद्देश्य से अनाज के रूप में ही लगान वसूल की जाने लगी, जिसे राजकीय गोदामों में सुरक्षित रखा जाता था।
किसानों को व्यापारियों के हाथों अनाज बेचने की मनाही कर दी गयी। सिर्फ अनुज्ञा प्राप्त व्यापारी ही किसानों से सीधे अनाज खरीद सकते थे। राजकीय गोदामों से अन्न की आपूर्ति किये जाने से अनाज का भाव काफी गिर गया एवं सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध हो गया।
इस बाजार नियंत्रण की नीति के परिणाम काफी लाभदायक हुए। इसके चलते अनाज एवं अन्य वस्तुओं की कीमत काफी सस्ती हो गयी। सैनिकों एवं अन्य नगर निवासियों को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होने लगीं। अलाउद्दीन के जीवनपर्यंत फिर वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ा।
वस्तुतः उपरोक्त सुधारों के द्वारा खिलजी ने मुख्यतः अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की। अपने राजत्व के सिद्धांत का सहारा लेकर उसने राज्य की सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उलेमा एवं अमीरों के प्रभाव से उसने अपने आपको मुक्त कर लिया। उसकी शक्ति को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। वह शासन का सर्वेसर्वा बन बैठा। विद्रोहियों की शक्ति समाप्त हो गयी। आर्थिक सुधारों से राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरी, जिसके आधार पर उसने एक विशाल सेना का संगठन किया एवं राज्य विजय की योजना बनाई। परंतु जनता पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और उसकी आर्थिक अवस्था दयनीय हो गयी।
Question : फ्विंध्याचल के दक्षिण पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेने भर से ही राष्ट्रकूटों की महत्त्वाकांक्षाओं का परितोष नहीं हुआ, उनकी इच्छा तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी प्रभुत्व प्राप्त करने की थी।" इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टिप्पणी कीजिये।
(1997)
Answer : दक्षिण भारत के इतिहास में राष्ट्रकूटों का विशेष महत्व है। राष्ट्रकूटों ने लगभग 225 वर्षों तक राज्य किया। बहुत कम हिन्दू राजवंशों को इतने लम्बे समय तक सम्मानपूर्वक राज्य करने का मौका मिला। दक्षिण भारत में 753 ई. से 975 ई. तक राष्ट्रकूट वंश की सर्वोच्चता का काल संभवतः उसके इतिहास का सर्वाधिक शोभनीय अध्याय है। दक्षिण में उनकी सफलताएं अपूर्व थी लेकिन ध्रुव, गोविन्द तृतीय एवं इंद्र तृतीय जैसे शासक अपना विजय अभियान उत्तरी भारत के मध्य तक ले गये तथा वहां के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों को परास्त करके उन्होंने उस क्षेत्र के इतिहास के रुख को बदल दिया।
राष्ट्रकूट साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने एवं स्वतंत्रता प्रदान कराने का श्रेय दंतिदुर्ग (735-755 ई.) को है। वह अत्यंत पराक्रमी होने के साथ-साथ कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी भी था। उसने शासक बनते ही तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया तथा उसके अनुरूप ही योजना बनाई। उसने पूर्व एवं पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयत्न किया। दंतिदुर्ग ने अपने शासनकाल में अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त की। उसकी विजयों का उल्लेख ‘समगंद प्लेट’ तथा एलोरा की ‘दशावतार गुफा’ के अभिलेखों से मिलता है।
दंतिदुर्ग ने दक्षिणी गुजरात में स्थित नन्दिपुरी को अपने राज्य में मिला लिया तथा अपने चचेरे भाई गोविन्द को वहां का शासक नियुक्त किया। नंदिपुरी तथा नौसारी पर विजय से उत्साहित होकर दंतिदुर्ग ने मालवा पर आक्रमण किया तथा उज्जैन पर अधिकार कर लिया। मालवा को उसने अपने राज्य में नहीं मिलाया, अपितु उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाकर ही संतुष्ट हो गया। मालवा विजय के पश्चात् दंतिदुर्ग ने महाकौशल एवं छत्तीसगढ़ का अभियान किया व विजय प्राप्त की। कोशल से लौटते समय दंतिदुर्ग ने कलिंग के कुछराजाओं को परास्त किया। इस प्रकार विभिन्न विजयों के माध्यम से दंतिदुर्ग ने संपूर्ण मध्य प्रदेश तथा मध्य एवं दक्षिणी गुजरात पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और राष्ट्रकूट साम्राज्य को शक्ति प्रदान की।
दंतिदुर्ग की मृत्यु के पश्चात् बने शासक कृष्ण प्रथम (756-772 ई.) ने गंग शासक श्रीपुरुष को पराजित किया तथा युवराज गोविन्द को वेंगी के चालुक्य शासक विष्णुवर्द्धन पर आक्रमण करने को भेजा। युवराज गोविन्द ने विष्णुवर्द्धन को पराजित करके हैदराबाद के विस्तृत भूभाग पर अधिकार कर लिया। कृष्ण प्रथम ने कोंकण पर भी विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। गोविंद द्वितीय (773-780 ई.) के पश्चात् ध्रुव (780-793 ई.) शासक बना। वह अत्यंत पराक्रमी शासक था। उसने अपने राज्याभिषेक के पश्चात् अनेक युद्ध किये व विजय प्राप्त की। ध्रुव ने संपूर्ण गंगवाड़ी को अधिकार में ले लिया और अपने पुत्र स्तंभ को वहां का शासक नियुक्त किया। गंगवाड़ी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् ध्रुव ने पल्लव शासक दंतिवर्मन को हराया। ध्रुव की इन विजयों से वह दक्कन का वास्तविक स्वामी बन गया। ध्रुव को चुनौती देने की शक्ति दक्षिण में किसी के पास नहीं थी। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वह इन विजयों से संतुष्ट नहीं हुआ व उत्तर भारत की राजनीति में भी उसने हस्तक्षेप किया।
जिस समय ध्रुव ने उत्तरी भारत का अभियान करने का निश्चय किया, उत्तर भारत में उज्जैन के प्रतिहार वंश व बंगाल के पाल वंश में अपनी-अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष चल रहा था। ध्रुव के समकालीन प्रतिहार व पाल शासक क्रमशः वत्सराज एवं धर्मपाल थे। ध्रुव ने अपने उत्तरी अभियान की योजना अत्यंत कुशलतापूर्वक बनाई। ध्रुव ने नर्मदा नदी के तट पर अपनी सेनाएं एकत्रित कीं। उस समय वत्सराज दोआब में आ चुका था। अतः ध्रुव ने मालवा पर सरलता से अधिकार कर लिया। तत्पश्चात् वत्सराज की मुख्य सेना का सामना करने के लिए ध्रुव ने कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। ‘राधनपुर’ अभिलेख से ज्ञात होता है कि ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर मरु देश में शरण लेने को विवश किया तथा वत्सराज के यश के साथ ही उन दो राजक्षत्रों को भी छीन लिया, जिन्हें उसने धर्मपाल से छीन लिया था। इस विजय से उत्साहित होकर ध्रुव ने धर्मपाल पर भी आक्रमण करने का निश्चय किया। अमोघवर्ष के ‘संजान अभिलेख’ से ज्ञात होता है कि ध्रुव ने पाल शासक धर्मपाल को भी परास्त किया। इस उत्तरी अभियान से यद्यपि उसके साम्राज्य का विस्तार तो न हुआ किंतु उसे अपार धन प्राप्त हुआ तथा उसकी प्रतिष्ठा में चार चांद लग गये। लेकिन अत्यंत सफल होने पर भी वह उत्तरी भारत में अपनी विजय को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका, क्योंकि विंध्याचल जैसी भौगोलिक बाधा को पार कर सुदूर प्रदेश को नियंत्रित करना सरल न था।
गोविंद तृतीय (793-814 ई.) ने भी अपने पिता ध्रुव के समान उत्तरी भारत पर अभियान किया। उसके समकालीन प्रतिहार व पाल शासक क्रमशः नागभट्ट द्वितीय व धर्मपाल थे। ‘संजन ताम्रपत्र’ से ज्ञात होता है कि गोविन्द तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। उसके पश्चात् उसने पाल शासक धर्मपाल को भी हराया। इस दिग्विजय से लौटते समय वह मालवा, कोशल, वेंगी, दाहल तथा औद्रक प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया।
चूंकि दक्षिणी प्रदेशों में भौगोलिक बाधाएं थोड़ी कम थीं और वह उनका परिचित प्रदेश था, इसी कारण वे दक्षिण में ही सिमट कर रह गये परंतु सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रकूट शासकों की इच्छा उत्तर भारत पर अधिकार करने की बनी रही। यद्यपि राष्ट्रकूटों को उत्तरी भारत में अपनी सफलता को बनाए रखने में सफलता नहीं मिली, परंतु संपूर्ण दक्षिण भारत पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। फिर भी इस वंश के तीन शासक ध्रुव, गोविन्द तृतीय तथा इंद्र तृतीय अपना विजय अभियान उत्तरी भारत के मध्य तक ले गये और वहां के सर्वाधिक प्रतापी शासकों को पराजित कर उस क्षेत्र के इतिहास के रुख को बदल दिया।
Question : निम्न ऐतिहासिक स्थलों को मानचित्र पर अंकित कीजिये तथा उन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिये
1. अजमेर, 2. अटक, 3. बनारस, 4. भटनेर, 5. चंपानेर, 6. कच्छ, 7. दौलताबाद, 8. दिल्ली, 9. देवगिरि, 10. दीव, 11. एलिचपुर, 12. एलोरा, 13. गजनी, 14. गोर, 15. ग्वालियर, 16. हम्पी, 17. हिसार, 18. जोधपुर, 19. काबुल, 20. कटनी, 21. खैबर का दर्रा, 22. लाहौर, 23. पेशावर, 24. रामेश्वरम, 25. रणथम्भौर, 26. सियालकोट, 27. थानेश्वर, 28. थट्टा, 29. उत्तर मेरुर, 30. वारंगल
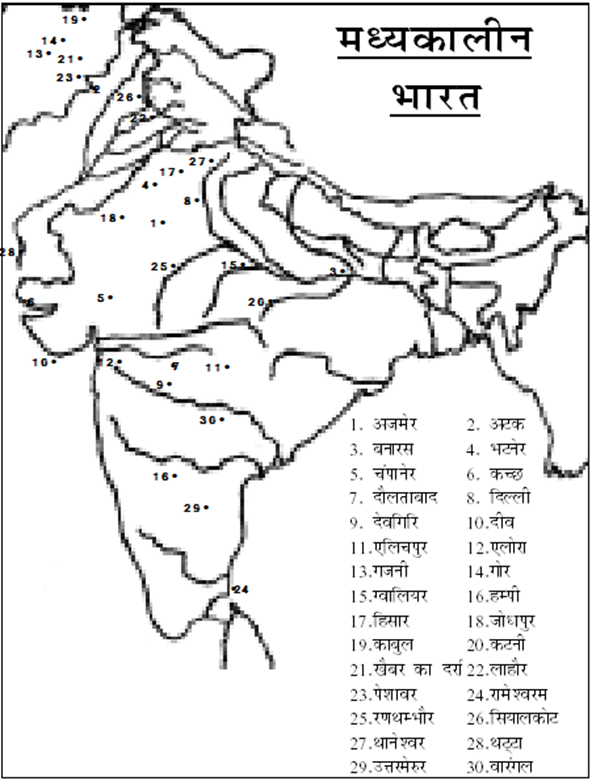
(1996)
Answer : 1. अजमेर: राजस्थान स्थित अजमेर मध्य युग में प्रमुख व्यापारिक मार्ग तथा उत्तर भारत से पश्चिम भारत की ओर जाने वाले मार्ग पर अवस्थित था। इसकी स्थापना शाकम्भरी के अजयदेव ने 1113 ई. में की थी। चौहान वंश के शासकों के अधीन अजमेर ने महानता प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान के समय भी अजमेर साम्राज्य का अंग था।
कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया मस्जिद अढाई दिन का झोंपड़ा यहीं है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर को महत्वपूर्ण स्थल के रूप में चित्रित करता है। शाहजहां ने आनासागर झील के पास संगमरमर झील का निर्माण कराया था। यह एक महत्वपूर्ण शोरा का केन्द्र भी था। मनूची ने अजमेर को ‘सफेद वस्त्र का केंद्र’ कहा है।
2. अटक: सम्प्रति अटक पाकिस्तान में सिंधु तट पर अवस्थित है। यह प्राचीनकाल में हाटक कहलाता था। कहा जाता है कि सिकन्दर ने अटक से 16 कि.मी. दूर ओहिन्द से सिंधु नदी को पार किया था। ओहिन्द के निकट ही महमूद गजनवी ने आनन्दपाल की सेना को हराया था। यहां पर एक सुदृढ़ किला नदी तट पर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था। अकबर ने अटक के पार युसुफजाइयों से लड़ने के लिए बीरबल, टोडरमल तथा मानसिंह को भेजा था। जुलाई 1758 ई. में बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव ने अटक पर मराठा झंडा फहराया था।
3. बनारस: पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित बनारस अन्य नामों-वाराणसी और काशी से भी अभिहित किया जाता है। हिन्दुओं का पवित्र स्थल बनारस वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य स्थित है। कहा जाता है कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच बहुचर्चित शास्त्रर्थ यहीं संपन्न हुआ था। प्राचीन काल से ही यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र भी रहा है। औरंगजेब ने यहां के मूल विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा कर मस्जिद की स्थापना कर दी थी। 1777 ई. में अहिल्याबाई ने पास में ही एक दूसरा मन्दिर बनवाया जो हिन्दुओं के लिए तीर्थ-स्थल बन गया है।
4. भटनेर: राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास स्थित भटनेर मध्यकालीन भारत में पश्चिमोत्तर सीमा का सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र था। प्रारंभिक मध्यकाल में जैसलमेर के भाटियों का अधिकार भटनेर पर था। बाहरी आक्रमणों के खतरे को भांपते हुए यहां एक सुदृढ़ किले का निर्माण करवाया गया था।
5. चंपानेर: गुजरात में बड़ौदा के पास वर्तमान पावागढ़ नगर ही मध्यकालीन चम्पानेर है। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने 1484 ई. में चम्पानेर पर अधिकार कर उसे ‘मुहम्मदाबाद’ नाम दिया। 1535 ई- में हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुरशाह को पराजित कर चम्पानेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। चम्पानेर दो कारणों से महत्वपूर्ण था- एक, यह उत्तरी भारत से गुजरात तथा खम्भात की खाड़ी तक पहुंचने के मार्ग पर था, दूसरे, यहां का दुर्ग अत्यंत मजबूत था। अकबर ने जब गुजरात विजय किया, तो यह फिर से मुगल राज्य का अंग बन गया।
6. कच्छ: वर्तमान में गुजरात में स्थित इस स्थल (कच्छ) का उल्लेख महाभारत एवं पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता हैं। ‘शिशुपालवध’ नामक काव्य में भी कच्छ का वर्णन है। इसमें श्रीकृष्ण के सैनिकों का लवंग पुष्पों की माला से विभूषित होने, नारियल का पानी पीने और कच्ची सुपारियां खाने का लालित्यपूर्ण वर्णन है। महमूद गजनवी ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया था, उनमें कच्छ भी एक था। मध्यकाल में सुल्तान फीरोज तुगलक ने जब 1361-62 में सिंध पर आक्रमण किया तो वह कच्छ के रन में फंस गया था।
7. दौलताबाद: महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरि था और यह यादवों की राजधानी थी। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की राजधानी देश के केन्द्र में करने के ख्याल से इसका विकास किया और 1327 ई. में देवगिरि का नाम दौलताबाद करके अपनी राजधानी बनायी। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण भी किया था। मुबारक खिलजी ने इसका विलय दिल्ली सल्तनत में किया था। मुगलकाल में यह अहमदनगर के एक मजबूत किले के रूप में जाना जाता था। 1760 ई. में मराठों ने इस पर अपना अधिकार बना लिया था।
8. दिल्ली: दिल्ली की स्थापना तोमर राजा अनंगपाल ने 933 ई. में ढिल्लिका नाम से की थी। 1192 ई- में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। विभिन्न मुस्लिम शासकों ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अपनी राजधानी बनायी। अलाउद्दीन ने सिरी, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद, मुहम्मद तुगलक ने जहांपनाह, फिरोजशाह तुगलक ने फिरोजाबाद, शेरशाह ने पुराना किला और शाहजहां ने शाहजहांनाबाद में अपनी राजधानी बनायी। अंग्रेजों ने भी 1911 के बाद दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। सांस्कृतिक-ऐतिहासिक महत्व के स्थापत्यों में कुतुबमीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, जन्तर-मन्तर आदि प्रमुख हैं।
9. देवगिरि: देवगिरि की स्थापना दक्षिण भारत के यादववंशीय शासक भिल्लम चतुर्थ ने की थी। सल्तनतकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने यहां के शासक रामचन्द्र देव को हराकर इस नगर को खूब लूटा। बाद में मुहम्मद बिन तुगलक ने इस नगर का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया और कुछ दिनों के लिए अपनी राजधानी बनाया। मुगल शासक औरंगजेब को यहीं दफनाया गया।
10. दीव: दीव वर्तमान केन्द्रशासित प्रदेश दमन एवं दीव का हिस्सा है। दीव या देवबन्दर भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। 16वीं शताब्दी ईस्वी में यह गुजरात के सुल्तानों के अधीन था। गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा ने यह द्वीप पुर्तगालियों को दे दिया था। यहां पुर्तगालियों ने अपनी आवासीय बस्तियां बसाईं, जिनके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र भारत में सन् 1961 में इसे गोवा और दमन के साथ भारत का हिस्सा बना लिया गया।
11. एलिचपुर: एलिचपुर महाराष्ट्र में बरार जिले में स्थित है। यह अमरावती के उत्तर में है। 13वीं शताब्दी ईस्वी में एलिचपुर यादवों के देवगिरि राज्यान्तर्गत आता था। 1296 ई. में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरि पर आक्रमण किया था, तब देवगिरि के शासक रामचन्द्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को एलिचपुर का वार्षिक खराज देना स्वीकार किया था। बाद में दिल्ली सल्तनत को वार्षिक खराज नियमित रूप से न देने पर अलाउद्दीन ने 1307 ई. में पुनः आक्रमण किया था।
12. एलोरा: महाराष्ट्र स्थित एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन एवं हिन्दुओं की सांस्कृतिक चेतना को आकर्षक मूर्तियों एवं भित्तिचित्रों में अभिव्यक्त करते हैं। यहां का भित्ति चित्रण उतना उत्कृष्ट नहीं, किन्तु मूर्ति वैभव दर्शकों को सहज ही आकृष्ट कर लेता है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम (748-775 ई.) द्वारा निर्मित एवं द्रविड़ शिल्पकला का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक कैलाश मन्दिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
13. गजनी: वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित गजनी एक अरब नेता याकूब इब्न लेस द्वारा स्थापित किया गया बताया जाता है। एक तुर्की जनरल अलप्तगीन ने 962 ई. में अंतिम अरब मुखिया अबू बकर लाविक से गजनी को जीता था। सोमनाथ मंदिर का प्रसिद्ध लुटेरा महमूद (998-1030) गजनी का ही शासक था। 1739 ई. में नादिरशाह ने गजनी पर अधिकार किया था।
14. गोर: गजनी और हेरात के मध्य पर्वतीय प्रदेश में यह स्थान अवस्थित है। 10वीं शताब्दी में यह स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर चुका था। महमूद गजनी ने 1009 ई. में यहां के शासक मुहम्मद बिन सूरी को परास्त किया था। बाद की घटनाओं में गजनी के शासक बहराम की आज्ञा से गोर वंश के राजकुमार मलिक कुतुबुद्दीन हसन का वध करवा दिया। गोर में शंसबानी वंश प्रधान वंश था। मुहम्मद गोरी भी वहीं का शासक था।
15. ग्वालियर: मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर राजपूताना क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण राजनैतिक- सामरिक महत्व रखता था। ऊंची पहाड़ी पर एक दुर्भेद्य दुर्ग बना हुआ है जो सामरिक स्थापत्य कला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 1398 ई. से 1518 ई. तक ग्वालियर तोमर शासकों के अधीन रहा। इन शासकों में राजा मानसिंह तोमर का नाम अग्रगण्य है। वे संगीतानुरागी थे। उनकी पत्नी मृगनयनी भी संगीत में अभिरुचि रखती थीं। अकबरी दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन भी ग्वालियर के दरबार के माध्यम से मुगल दरबार तक पहुंचा था। तानसेन का मकबरा भी यहीं है। मराठा शक्ति के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में यह सिन्धिया घराने के अन्दर रहा। प्रसिद्ध किले के अन्दर मानसिंह का शीश महल, सास-बहू का मन्दिर और तेली का मन्दिर प्रमुख स्थापत्य नमूने हैं।
16. हम्पी: कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। इस नगर का निर्माण 1343 ई. में हुआ था। विजयनगर के चार वंशों- संगम, सुलुव, तुलुव एवं अरविडु ने यहां से शासन किया। अब्दुर्रज्जाक नामक फारसी यात्री ने इस नगर को विश्व का एक अद्वितीय नगर बताया। विरुपाक्ष मंदिर अपने स्थापत्य को लेकर काफी विख्यात है।
17. हिसार: हरियाणा राज्य में अवस्थित हिसार की स्थापना फिरोजशाह तुगलक ने 1356 ई. में की थी। फिरोजशाह ने यहां यमुना से एक नहर निकाली थी, जिससे उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राजकीय संरक्षण में खेती शुरू की गयी और यह क्षेत्र समृद्ध होने लगा। यहां कपास एवं गन्ने जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। फिरोजशाह द्वारा बनवाये गये महल का अवशेष अब भी यहां देखा जा सकता है।
18. जोधपुर: लूनी नदी के किनारे अवस्थित जोधपुर राजस्थान का जिला-नगर है। इसकी स्थापना 1459 ई. में राठौर सरदार राव जोधा ने की थी। इस प्रकार, मंडोर के स्थान पर जोधपुर मारवाड़ की राजधानी बना। मालदेव यहां का प्रसिद्ध शासक था। उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करके 1570 ई. में अकबर ने उदयसिंह को मारवाड़ का शासक बनाया और बाद में, उदयसिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ शहजादा सलीम का विवाह हुआ। उदयसिंह के प्रतिद्वन्द्वी भाई चन्द्रसेन ने आजीवन मुगलों का विरोध किया। औरंगजेब के समय जोधपुर का शासक जसवंत सिंह था। 1678 ई. में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के उत्तराधिकार प्रश्न पर औरंगजेब ने हस्तक्षेप किया था। फलस्वरूप मारवाड़ की निष्ठा मुगल साम्राज्य के प्रति खत्म हो गयी।
19. काबुल: आधुनिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल ही मध्यकालीन काबुल है, जो कुभा अथवा काबुल नदी के किनारे स्थित है। मध्य युग में मध्य एवं पश्चिम एशिया से विदेशियों के भारत में आने के कारण, काबुल का बहुत महत्व था। काबुल को बाबर ने 1504 ई. में जीता था। 1526 ई. में भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद यह मुगल साम्राज्य का अंग हो गया था। 1545 ई. में हुमायूं, 1581 ई. में अकबर तथा 1739 ई. में नादिरशाह ने काबुल को जीता था।
20. कटनी: वैसे तो वर्तमान कटनी नगर मध्य प्रदेश के रायपुर-विलासपुर जिलों में अवस्थित है। लेकिन मध्यकाल में कटनी या कटनी नाला के नाम से प्रसिद्ध एक नगर का प्रमाण हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिला के एक प्रमुख नगर के रूप में मिलती है। इस नगर की नींव राजा दीपचंद्र ने 1653 ई. में डाली थी। यूरोपीय यात्री विग्ने ने 1838 ई. में इस नगर के सौंदर्य तथा वैभव के बारे में अपने संस्मरण लिखे थे। वैसे यह क्षेत्र भाखड़ा-नांगल बांध के कारण अब जलमग्न हो चुका है।
21. खैबर का दर्रा: यह वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर के उत्तर-पश्चिम में है। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का द्वार भी कहा जाता है। इसी दर्रा से सभी विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया।
22. लाहौर: रावी नदी के तट पर अवस्थित लाहौर वर्तमान पाकिस्तान का एक प्रमुख नगर है। मध्य काल में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां हिन्दूशाही वंश का शासन था। दिल्ली सल्तनत में लाहौर, स्थापना के समय से ही शामिल था। बाबर ने 1524 ई. में इस पर आक्रमण किया था। अकबर ने पश्चिमोत्तर सीमा की गड़बड़ी को देखते हुए इसे वर्षों तक राजधानी बनाए रखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद लाहौर पर से मुगलों का नियंत्रण जाता रहा। बाद में रणजीत सिंह के समय लाहौर सिखों की राज्य की राजधानी बन गया। लाहौर में कई उल्लेखनीय कलाकृत्तियां भी हैं, जिनमें बादशाही मस्जिद, जहांगीर का मकबरा, शालीमार बाग आदि प्रमुख हैं।
23. पेशावर: वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित पेशावर मध्यकालीन भारत में उत्तर-पश्चिम सीमा पर खैबर दर्रे के पास होने की वजह से सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। भारत एवं उत्तर-पश्चिम के देशों के बीच स्थल मार्ग से व्यापार का मार्ग भी पेशावर होकर ही गुजरता था। महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण कर अपने राज्य में मिला लिया था। तबसे सिखों के राज्य की स्थापना तक यह प्रायः भारत के नियंत्रण से बाहर ही रहा। वैसे, शेरशाह का इस पर आंशिक नियंत्रण था, जब उसने पेशावर होकर तक्षशिला से सोनार गांव तक व्यापारिक मार्ग का निर्माण करवाया था।
24. रामेश्वरम: मन्नार की खाड़ी में मदुरई से लगभग 100 मील की दूरी पर एक द्वीप का नाम रामेश्वरम है। यह तलइमन्नार (श्रीलंका) में सामान भेजने के लिए उपयुक्त बन्दरगाह भी है। यह उत्तरवर्त्ती द्राविड़ स्थापत्य की एक विख्यात मंदिर रामनाथस्वामी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अलंकार युक्त स्तंभों वाले गलियारे ने इसकी खूबसूरती और भी बढ़ा दी है। एक गलियारा 1220 मीटर लंबा है जो भारत में सबसे बड़ा है। 12वीं शताब्दी में इस मन्दिर का निर्माण किया गया। यह उत्तर भारत के वाराणसी की तरह एक पवित्र नगर है।
25. रणथम्भौर: सम्प्रति राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथम्भौर मध्यकाल के सबसे दुर्गम और दुर्जेय किले के रूप में प्रसिद्ध था। आरम्भ में इस पर चौहान शासकों का नियंत्रण था, बाद में मेवाड़ के हाड़ा शासक का नियंत्रण हो गया। इस पर पहली बार कई कोशिशों के बाद 1301 ई. में अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रण कर पाया था। मुगलों के शासनकाल में अकबर ने बूंदी के हाड़ा सरदार सुरजन सिंह से रणथम्भौर प्राप्त किया और अगली दो शताब्दी तक यह मुगल साम्राज्य का अंग रहा। यहां राजपूत शैली के ऐतिहासिक स्थापत्य के कई नमूने मिलते हैं।
26. सियालकोट: प्राचीन काल में साकल कहा जाने वाला सियालकोट सम्प्रति पाकिस्तान में है। मुहम्मद गोरी ने इसे जीता था और दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। बाबर ने भारत पर आक्रमण करते समय इसे आधार स्थल के रूप में प्रयोग किया। अकबर पश्चिमोत्तर सीमा की रक्षा के लिए यहां सेना रखता था।
27. थानेश्वर: संप्रति हरियाणा के करनाल जिले में स्थित ‘थानेसर’ ही प्राचीन काल में थानेश्वर के नाम से विख्यात था। यह धर्म एवं संस्कृति का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। हिन्दुओं के पवित्र तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध यह नगर बाद में पुष्यभूतियों की राजधानी बना। पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक प्रभाकर वर्द्धन ने इसे एक केन्द्रीय शहर के रूप में विकसित किया। बाद में हर्षवर्द्धन यहां का शासक बना। जब हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित कर दी तो इस स्थल की महत्ता कुछ कम हो गयी। महमूद गजनवी ने यहां पर आक्रमण करके अपार धन-संपदा लूटी थी।
28. थट्टा: आधुनिक पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त में सिन्धु नदी के तट पर स्थित थट्टा मध्य काल में महत्वपूर्ण स्थल था, क्योंकि यह लाहरी बन्दर बन्दरगाह को शेष भू-भाग से जोड़ने वाला केन्द्र था। सल्तनत काल में इस पर नियंत्रण के लिए सुल्तानों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुहम्मद बिन तुगलक की थट्टा अभियान में ही मृत्यु हुई थी। फिरोजशाह तुगलक कई आक्रमणों के बाद ही वहां के शासक से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सका। मुगलकाल में भी यह महत्वपूर्ण स्थल बना रहा। थट्टा महदवी आन्दोलन का भी केन्द्र रहा।
29. उत्तर मेरुर: उत्तर मेरुर वर्तमान तमिलनाडु में एक छोटा-सा ग्राम है, जहां से प्राप्त पल्लव एवं चोल अभिलेखों से दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन की विकास प्रक्रिया के विषय में पता चला है। उत्तर मेरूर से 919 ई. तथा 929 ई. के दो ऐसे अभिलेख मिले हैं, जिनसे ग्राम की स्थानीय सभा के संगठन, संरचना, स्वरूप तथा कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है। उक्त अभिलेख से पता चला है कि चोलों के समय स्थानीय ग्रामीण सभा स्वायत्त थी और इसका कार्य-सम्पादन ‘वरियम’ अथवा ‘समिति प्रणाली’द्वारा होता था। महासभा की संरचना का स्वरूप लोकतांत्रिक था तथा यह केन्द्रीय हस्तक्षेप से मुक्त था।
30. वारंगल: सम्प्रति वारंगल आन्ध्र प्रदेश का एक जिला है, जो गोदावरी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश की राजधानी के रूप में यह प्रसिद्ध हुआ। 1310 ई. में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक काफूर ने वारंगल पर चढ़ाई की, जिसमें उसे अथाह सम्पत्ति हाथ लगी। वहां के तत्कालीन शासक प्रताप रूद्रदेव ने नियमित रूप से दिल्ली सल्तनत को नजराना देना स्वीकार कर लिया। पर, इसमें अनियमितता आने पर तुगलक काल में फिर से वारंगल पर आक्रमण कर उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया।
Question : "प्राचीन भारत के लोगों की इतिहास लेखन में कोई रुचि नहीं थी। उस समय के विद्वानों ने धर्म, अध्यात्म और दर्शन के अध्ययन की ही अधिक चिन्ता की। भारतीय इतिहास लेखन वस्तुतः इस्लामी शासन की देन है।" भारतीय इतिहास में मध्यकाल के इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक होने वाले तत्कालीन लेखकों और उनकी रचनाओं का विशेष उल्लेख करते हुए इस कथन की समीक्षा कीजिये।
(1996)
Answer : प्राचीन भारत के लोगों पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उनमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। यह सही है कि उन्होंने वैसा इतिहास नहीं लिखा जैसा आजकल लिखा जाता है। यहां यूनान के हिरोडोटस या रोम के लिवी जैसे इतिहास लेखक नहीं हुए, इसलिए कुछ पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा बन गयी थी कि भारतीयों को इतिहास की ठीक संकल्पना ही नहीं थी। परंतु ऐसा समझना एक भूल है। वस्तुस्थिति यह है कि प्राचीन भारतीयों की इतिहास की संकल्पना आधुनिक इतिहासकारों की संकल्पना से पूर्णतया भिन्न थी। आजकल का इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में कार्य-कारण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है किन्तु प्राचीन इतिहासकार केवल उन घटनाओं का वर्णन करता था, जिनसे जनसाधारण को कुछ शिक्षा मिल सके। महाभारत में इतिहास की परिभाषा ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा से दी गयी है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके। प्राचीन काल में इन चार पुरुषार्थों को जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक समझा जाता था। इन पुरुषार्थों को करने की प्रेरणा देने में इतिहास भी एक साधन था, इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहासकार उन घटनाओं को कोई महत्व नहीं देते थे, जिनसे इन चारों पुरुषार्थों की शिक्षा न मिल सके। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास राजनीतिक कम और सांस्कृतिक अधिक है। भारतीय समाज के निर्माण में धर्म, अध्यात्म और दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आरंभिक ऐतिहासिक लेखन में कल्हण की राजतरंगिणी (राजाओं की धारा) को आज के अर्थ में इतिहास का ग्रन्थ कहा जा सकता है, परन्तु यह भी काफी उत्तरवर्ती काल अर्थात् 12वीं शताब्दी का है।
मध्यकालीन भारत के इतिहास को प्राचीन भारतीय इतिहास से जो तत्त्व अलग करते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण तत्त्व यह है कि मध्यकालीन भारत से संबंधित समसामयिक ऐतिहासिक साहित्य अपेक्षाकृत प्रचुर परिमाण में मिलता है। इसलिए यह कहा जाता है कि भारतीय इतिहास लेखन वस्तुतः इस्लामी शासन की देन है। हमें इस्लामी ऐतिहासिक लेखन सिंध पर अरबों की विजय अर्थात् आठवीं शताब्दी से ही मिलनी शुरू हो जाती है। ‘फतहनामा’ या ‘चचनामा’ सिंध के इतिहास पर ऐसी ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सही है कि लिखित विवरणों का उपलब्ध होना इतिहास लेखन के लिए लाभकर है किन्तु इनके मूल स्वरूप को जानना भी आवश्यक होता है अन्यथा यह उल्टे हानिकर हो सकता है। यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि इतिहास लेखक कौन है, उसके लेखन का उद्देश्य क्या है और किस कालखण्ड में इतिहास लिखा गया है। लेखक की सीमाएं भी जानी जानी चाहिए। मिन्हाज की पुस्तक तबकाते नासिरी में तुर्कों की विजय का वृत्तांत मिलता है। मिनहाज सत्ता के अधिक करीब था। वह खुद विभिन्न उच्च पदों पर कार्य करता रहा। ये ऐसी बातें हैं जो उसके इतिहास के स्वरूप को निर्धारित करने में सहायक हुईं। इतिहास इस्लाम के साथ-साथ उस राज्य के प्रति निष्ठा एवं उत्साह जगाने का तरीका था, जिसका वह सदस्य था और जिसको वह इस्लामी राज्य के रूप में चित्रित करता था। मिनहाज की कमी थी कि वह राजाओं और अमीरों के ही बारे में लिख पाया। उसने आम आदमी की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया।
जियाउद्दीन बरनी की रचनाएं तारीख-ए फिरोजशाही और फतवा-ए-जहांदारी थीं। बरनी मुहम्मद बिन तुगलक का मित्र था। फिरोजशाह तुगलक से उसके संबंध बिगड़ गये और उसे जेल की सजा भी काटनी पड़ी। अन्तिम समय में उसे सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा। फिर भी उसने तारीखे फिरोजशाही नामक ग्रन्थ फिरोज को समर्पित किया। बरनी भी इतिहास लेखन के समय मुख्य रूप से शासक वर्गों के हितों के प्रति आग्रहशील था। हां, मिनहाज की तरह उसने इस्लाम पर अधिक ध्यान केन्द्रित न करके भारत संबंधी घटनाओं को ही प्रमुखता दी। बरनी की खासियत थी कि वह प्रायः नैतिकता के संदेश देने पर उतर आता था। उसकी रचना में कालानुक्रम दोष भी है। अतः तारीख संबंधी विवरणों में वह भरोसेमंद इतिहासकार नहीं माना जा सकता।
शम्स-ए-सिराज अफीफ ने भी अपनी पुस्तक का नाम तारीखे फिरोजशाही रखा। अफीफ ने दरअसल मिनहाज और बरनी की रचनाओं के बाद के इतिहास क्रम को पूरा करने के लिए यह पुस्तक लिखी। अफीफ की खासियत है कि वह पहला इतिहासकार था, जिसने दरबारी क्षेत्र से बाहर निकलकर आम आदमी का इतिहास भी लिखा। अफीफ ने किसी बौद्धिक महत्त्वाकांक्षा के वशीभूत होकर इतिहास नहीं लिखा। वह लेखन के मामले में बहुत सीधा-साधा व्यक्ति
लगता था।
इन इतिहासकारों से काफी पहले अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘किताबुल हिन्द’ लिखी, जिसमें 1017 से 1030 ई. के बीच के भारतीय जीवन की झलक मिलती है। वह धार्मिक पूर्वाग्रह से दूर रहते हुए भारतीय परंपराओं, रीति-रिवाजों, त्यौहारों, उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों के विवरण देता है। तुर्कों के आक्रमण से ठीक पहले का इतिहास जानने के लिए यह एक भरोसेमंद कृति है।
एक और यात्री इब्नबतूता, मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। उसकी रचना का नाम ‘रेहला’ था। इब्नबतूता एक यात्री था, अतः उसकी रचना में ऊपरी जानकारी ही दी जा सकी। उसका विवरण छिछला और सतही लगता है।
इसामी बहमानशाह का दरबारी लेखक था और उसकी पुस्तक फुतूह-उस-सलातीन में मुहम्मद बिन तुगलक की कटु आलोचना है।
अमीर खुसरो हालांकि इतिहासकार नहीं था, परन्तु उसके लेखन से भी इतिहास संबंधी कुछ जानकारी इकट्ठी की जाती है। ‘नूह सिपिहर’ उसकी ऐसी रचना है जिसमें हिन्दुस्तान संबंधी अच्छा चित्रण देखने को मिलता है। सरहिंदी ने अपनी पुस्तक ‘तारीखे-मुबारकशाही’ में तैमूर के आक्रमण के बाद के हालातों का चित्रण किया है। उसकी दिलचस्पी केवल सैनिक और राजनीतिक इतिहास में है।
अंत में यह देखा जा सकता है कि जिन मध्यकालीन इतिहास लेखकों को आधुनिक अर्थ में इतिहास लेखक मानते हैं, उनकी रचनाओं को भी पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता और आवश्यक संशोधन जरूरी होते हैं। इसलिए केवल प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखकों पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। दरअसल, इतिहास लेखक अपने समय में जीता है जिसकी अनदेखी वह भी नहीं कर सकता।
Question : गयासुद्दीन बलबन का मूल्यांकन कीजिये।
(1996)
Answer : दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों में बलबन विशेष महत्व रखता है। उसी के अधीन दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करने का काम संपन्न हुआ और दिल्ली सल्तनत एक शक्तिशाली और सुसंगठित राज्य के रूप में प्रकट हुई। दास के रूप में जीवन शुरू करने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर जल्द ही पदोन्नति पाते हुए मशहूर ‘चालीसा’ के दल में शामिल हो गया। नासिरूद्दीन महमूद ने 20 वर्षों तक उसे अपना प्रधानमंत्री बनाए रखा और उसकी मृत्यु के बाद तो बलबन खुद सुल्तान बन बैठा।
दिल्ली का सुल्तान रहते हुए उसका सर्वाधिक मुख्य उद्देश्य हिन्दुस्तान में नव स्थापित तुर्की सल्तनत को सुसंगठित करना था। इसके लिए उसने पहले से जीते हुए प्रदेशों में ही सुव्यवस्था लाना श्रेयस्कर समझा। उसने नए क्षेत्रों को जीतने या पड़ोसी हिन्दू शासकों की स्वाधीनता हड़पने की नीति को अनुचित समझा। इसका कारण यह था कि उसे तुर्की साधनों की सीमा और जनसंख्या पर पड़ने वाले दबाव का अहसास था। यह एक नवोदित राज्य के लिए सूझ-बूझ भरा कदम कहना चाहिए। इसके बदले में उसने आन्तरिक शान्ति की पुनः स्थापना पर बल दिया और सल्तनत की उत्तर-पश्चिमी सीमाओं की रक्षा के लिए समुचित प्रबंध करके उसको मंगोलों के आक्रमण से बचाया। उसके पूर्वाधिकारियों के शासन काल में ताज की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आ गयी थी। बलबन ने इसकी पुनर्प्रतिष्ठा की। उसने बहुत सारे दबंग सामंतों की शक्ति को कुचलकर तुर्की शासन को एक नया रूप दिया। निस्संदेह वह योग्य तथा कठोर शासक और सफल सुल्तान था।
शासक की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए बलबन ने राजत्व का एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार सम्राट ईश्वर की छाया है। इसलिए सम्राट की इच्छा की अवहेलना ईश्वर की अवहेलना होगी। बलबन ने अपने दरबार को ईरानी शासकों की परिपाटी के अनुसार संगठित किया। दरबार में अनुशासन को सबसे अधिक प्रमुखता दी गयी। दरबार की गंभीरता का उल्लंघन अक्षम्य अपराध था। वह स्वयं गंभीर मुद्रा में दरबार में रहता था। उसके सामने सामन्त हंसी-मजाक या फिजूल की बातें करने की हिमाकत कभी नहीं करता था। बलबन का खुद का व्यक्तित्व इतना दबंग था कि उससे अपनी बात कहते हुए बड़े-बड़े सामन्तोंकी जुबान लड़खड़ा जाती थी। उसने अमीरों को नीचा दिखाने के लिए दरबार में ईरानी प्रथा ‘सिजदा’ और ‘पैबोस’ की शुरुआत की।
बलबन वृद्धावस्था में सुल्तान बना था, परन्तु उसमें अपूर्व उत्साह, स्फूर्ति एवं कार्य करने की क्षमता थी। वह दोषी अमीरों एवं राज्यपालों को कठोर-से-कठोर सजा देने से भी नहीं हिचकता था। उसने बदायूं के मलिक बकबक को अपने नौकर की हत्या के अपराध के लिए कोड़े मारने का दण्ड दिया था। इसी तरह के एक अन्य अपराध के लिए अवध के एक जागीरदार हैबत खान को 500 कोड़ों का दण्ड दिया गया था। अपने स्वभाव और कार्यकुशलता के बल पर ही उसने सामंतों पर पकड़ बनायी थी। बलबन पक्का सुन्नी मुसलमान था। इस्लाम द्वारा निर्धारित कर्त्तव्यों का वह बड़ी सावधानी से पालन करता था। वह सच्चरित्र मुस्लिम धर्माधीशों के साथ उठना-बैठना अधिक पसन्द करता था। अपनी बहुसंख्यक प्रजा के प्रति वह सहिष्णु नहीं था, क्योंकि वह धर्मान्ध भी था। वह कुलीन परिवार के सदस्य को ही शासन के उच्च पदों पर बैठाता था। वस्तुतः इसका अर्थ यह था कि भारतीय मुसलमान शासन में शक्ति और प्रभुत्व के पदों से वंचित रह जाते थे। इस मामले में वह अव्यावहारिक माना जायेगा, जब हमें पता चलता है कि एक बड़े व्यापारी से उसने मिलना इसलिए अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह उच्च कुल का नहीं था। बरनी लिखता है कि अकुलीन व्यक्ति को देखकर बलबन अपना आपा खो बैठता है। उसने खुद को कुलीन बतलाने के लिए कथाओं में प्रसिद्ध तुर्की योद्धा अफरासियाब से अपना संबंध जोड़ा।
बलबन ने केन्द्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे ‘दीवाने अर्ज’ कहते थे। ऐसा उसने सामन्तों पर सैनिक निर्भरता को समाप्त करने के लिए किया था। सुल्तान के पास अब अपनी निजी सेना थी, जिसका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता था। परवर्त्ती काल में अलाउद्दीन खिलजी ने इसी केन्द्रीय सेना का उपयोग करके साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया था। लेकिन बलबन ने इसका उपयोग तत्कालीन सामंतों के उच्छृंखल व्यवहार को रोकने के लिए किया और इस तरह एक व्यावहारिक नीति अपनायी। उसने ‘लौह और रक्त’ की नीति को अपनाते हुए मेवाती डाकुओं एवं राजपूत सरदारों की उपद्रवी गतिविधियों पर रोक लगायी। एक नवस्थापित तुर्की राज्य को दीर्घकालिक बनाने के लिए यह प्रारंभिक स्थिरता आवश्यक थी। बलबन ने तुर्की सल्तनत की रक्षा का सुप्रबन्ध किया और उसे नया जीवन प्रदान किया। यही उसका सबसे महान कार्य था। उसने ताज की पुनर्प्रतिष्ठा बहाल की। राज्य में सर्वत्र शांति और व्यवस्था स्थापित करना उसकी एक अन्य उपलब्धि थी। बलबन की ये उपलब्धियां दीर्घकाल तक प्रभाव छोड़ने वाली थीं। अतः बलबन सभी दास शासकों में महान समझा जाता है।
Question : शिवाजी के उदय को मराठा इतिहास की एक अलग घटना नहीं माना जा सकता। वह घटना शिवाजी के व्यक्तिगत साहस और शौर्य का जितना परिणाम थी, उतना ही दक्कन की भौगोलिक स्थिति और उन एकीकरण के कारक धार्मिक प्रभावों का भी परिणाम थी जो पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी की जनता में नई आशाओं और आकांक्षाओं का संचार कर रहे थे। स्पष्ट कीजिये।
(1996)
Answer : मुगल साम्राज्य के पतन के दिनों में शिवाजी का उदय उनके व्यक्तिगत साहस एवं शौर्य का परिणाम कही जाती है। उनके द्वारा नवस्थापित मराठा राज्य न केवल दक्षिण भारत की राजनीति वरन् उत्तर भारत की राजनीति को भी खासा प्रभावित करता रहा। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मराठा शक्ति के उदय की प्रक्रिया में कुछ तत्त्व ऐसे भी थे, जो काफी लम्बे समय से विकसित हो रहे थे। दूसरे शब्दों में, शिवाजी ने मराठा राज्य के उदय होने की प्रक्रिया को मुखरता दी।
आधुनिक इतिहासकारों- यदुनाथ सरकार, जी.एस. सरदेसाई और एम.जी. रानाडे ने शिवाजी के उत्थान को औरंगजेब के हिन्दू विरोधी राजनीति के रूप में देखने की कोशिश की है। शिवाजी ने ‘हिन्दू पादशाही’ अंगीकार किया, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया और ‘हिन्दुत्व-धर्मोद्धारक’ की पदवी धारण की। परन्तु सतीशचन्द्र इन तर्कों को नहीं मानते। वे कहते हैं कि मराठा शक्ति के विस्तार के पहले चरण में मुगल साम्राज्य पर शाहजहां का शासन था और यह ऐसा समय था, जब उसने मोटे तौर पर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनायी थी। स्पष्ट है कि शिवाजी के उदय के पीछे औरंगजेब की धार्मिक नीति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरे, मराठा इतिहास के आरंभिक चरण में संघर्ष मराठों और दक्षिणी सल्तनतों के बीच रहा था और मुगल उसमें काफी बाद में सम्मिलित हुए थे।
दक्षिण की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति भी शिवाजी के उदय में सहायक हुई। अहमदनगर राज्य के बिखराव और अकबर की मृत्यु के पश्चात् दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार की धीमी गति ने महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों को प्रोत्साहित किया। मराठे दक्षिणी सल्तनतों एवं मुगलों- दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न युद्धों में भाग लेकर सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर चुके थे। दक्षिणी भारत के कमजोर और बिखरी ताकत ने शिवाजी को मराठा राज्य स्थापित करने में सहायता की।
शिवाजी ने उदीयमान राज्य की राजस्व संबंधी गड़बडि़यों को दूर कर राज्य को एक विस्तृत सामाजिक आधार देने की कोशिश की। रानाडे के अनुसार, शिवाजी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी नागरिक या सैन्य प्रमुख को जागीरें नहीं देंगे। भारत में केन्द्र विमुख एवं बिखराव की प्रवृत्तियां सदैव बलवती रही हैं और जागीरें देने की प्रथा जागीरदारों को भू-कर से प्राप्त धन द्वारा अलग से अपनी सेना रखने की अनुमति देने से यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि सुव्यवस्थित शासन लगभग असंभव हो जाता है। अपने शासन काल में शिवाजी ने केवल मंदिरों को एवं दान धर्म की दिशा में ही भूमि प्रदान की। यदुनाथ सरकार इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी ने राजस्व प्रशासन के माध्यम से किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया। लेकिन ऐसा लगता है कि शिवाजी शांतिप्रिय जमींदारों के विरुद्ध नहीं थे, अपितु उनके राजनीतिक हितों के लिए जो गंभीर खतरा पैदा करते थे, ऐसे जमींदारों के विरुद्ध थे।
हम जानते हैं कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो बीजापुर के सामंत बने रहना अधिक पसन्द करते थे। उन्होंने इस नाजुक स्थिति से निबटने के लिए ‘भय और प्रीति’ की नीति अपनायी। कुछ बड़े देशमुखों को तो उन्होंने सैन्य शक्ति से पराजित किया और कुछ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किये। मोरे, शिर्के और निम्बालकर कुछ ऐसे देशमुख थे, जिनके परिवारों से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किये। छोटे देशमुखों ने बड़े देशमुखों के शोषक रवैये के विरुद्ध शिवाजी का साथ दिया।
शिवाजी के चरित्र एवं व्यक्तित्व ने भी एक सशक्त मराठा आन्दोलन खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संतों, विशेष रूप से दादाजी कोंडदेव के प्रभाव ने उन्हें अत्यन्त धार्मिक एवं अनुशासित बना दिया था और वे जाति के विधि निषेधों के परे देखते थे। उनमें नेतृत्व देने और कार्य करने, राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य से मराठा समाज के विभिन्न तत्त्वों को एक करने की क्षमता थी। इन्हीं योग्यताओं के बल पर वे एक शक्तिशाली और प्रभावशाली मराठा राज्य स्थापित कर सके।
परन्तु तात्कालिक परिस्थितियों एवं शिवाजी की योग्यता के अलावा, मराठा राज्य के उदय के कारक पहले से विद्यमान थे। महाराष्ट्र की उबड़-खाबड़ भौगोलिक स्थिति और वहां की जलवायु ने मराठों को दृढ़ परिश्रमी और लड़ाकू जाति बनाया और आने वाले समय में यही लक्षण उनकी पहचान बना। महाराष्ट्र प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है- महान पर्वतशृंखलाएं, जिन्होंने इसे दो तरफ से घेर रखा है-उत्तर से दक्षिण तक सह्याद्रि पर्वत मालाएं और पूर्व से पश्चिम तक सतपुड़ा एवं विन्ध्य पर्वत श्रेणियां। इन पर्वतशृंखलाओं से निकलने वाली छोटी श्रेणियां आड़ी-तिरछी रेखा बनाती हैं और अनेक नदियों के जल-विभाजक का निर्माण करती हैं जो अन्ततः गोदावरी और कृष्णा में जाकर गिरती हैं। ये सब मिलकर प्रदेश को ऐसा उबड़-खाबड़ और असीम रूप प्रदान कर देता है जो देश के किसी भी अन्य भाग में इतने बड़े स्तर पर दिखायी नहीं देता। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है और बस्तियां छितरी हुई हैं, जिनमें कष्टसहिष्णु और संयमी लोग बसे हुए हैं। प्राकृतिक कठिनाइयों ने एक ओर उनमें साहस, कठोर परिश्रम, आत्मसंयम जैसे गुणों का विकास किया तो दूसरी ओर वे पड़ोस के उर्वर क्षेत्रों को लूटने और वहां से धन अर्जित करने पर विवश हुए। इन लूट-पाट के अभियानों ने मराठों में सैनिक प्रतिभा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कीं। पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मराठों द्वारा छापामार युद्ध नीति का प्रयोग भी सफल ढंग से हुआ। उनके दुर्ग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मुगलों के प्रहार से सुरक्षित थे।
दक्कन की अनुकूल भौगोलिक स्थिति के अलावा 15वीं और 16वीं शताब्दी में धार्मिक संतों और दार्शनिकों द्वारा एकता और मानवता के जो पाठ पढ़ाये जा रहे थे, उनका भी मराठा राज्य के निर्माण में कुछ योगदान माना जा सकता है। ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और चक्रधर से लेकर एकनाथ, तुकाराम और रामदास तक, महाराष्ट्र के सभी संतों और दार्शनिकों ने भक्ति के सिद्धान्तों पर एवं इस बात पर बल दिया कि सभी मनुष्य परमपिता ईश्वर की संतान हैं और इस कारण समान हैं। उनके जाति प्रथा का विरोध करने के कारण मराठा और कुन्बी जैसी निम्न जाति के लोग उनके अनुयायी बन गये। ये संत स्थानीय मराठी भाषा में ही उपदेश देते थे, जिससे इस भाषा को इच्छित गौरव प्राप्त हुआ और इसे एक साहित्य भी मिला। एक विशिष्ट मराठा पहचान उभर कर सामने आयी, जिसने यहां के लोगों को एकता एवं लक्ष्य की भावना से प्रेरित किया।
Question : दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों के महत्व का मूल्यांकन कीजिये।
(1996)
Answer : चोल शासकों ने सैन्य विजयों द्वारा दक्षिण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की और इससे भी महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि उन्होंनेतमिल संस्कृति को एक निश्चित आकार व रूप दिया। प्रत्येक क्षेत्र में-चाहे वे सामाजिक संस्थाएं हों, धर्म हो या ललित कलाएं-इस काल में जो मानक स्थापित हुए, वे अत्यन्त ऊंचे माने गये। वे दक्षिण के जीवन पर छा गये। इसी काल में दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में चोल संस्कृति का विस्तार हुआ और इस क्षेत्र के व्यापार में दक्षिण भारत का राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही प्रकार का हस्तक्षेप पहले की अपेक्षा कहीं अधिक और सक्रिय रहा।
चोल वंश के दो प्रतापी राजाओं-राजराजा और उसका पुत्र राजेन्द्र प्रथम ने अनेक सैन्य विजयें हासिल कीं। राजराजा ने त्रिवेन्द्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया और कुइलोन पर आक्रमण किया। पाण्ड्यों की राजधानी मदुरई को जीता तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य का अंग बनाया। मालदीव को जीतकर अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता सिद्ध की। कर्नाटक के गंगा क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी भाग को अपने राज्य में मिला लिया।
राजेन्द्र प्रथम ने सैन्य विजय की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए पाण्ड्य और चेर राज्यों को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य का अंग बनाया। श्रीलंका की विजय को भी पूर्ण किया गया। राजेन्द्र प्रथम ने अपनी साम्राज्यवादी ताकत का अनुभव उत्तर-पूर्व भारत के दो स्थानीय राजाओं की पराजय से कराया, जिस घटना की याद में उसने ‘गंगयीकोंडचोल’ की उपाधि धारण की और अपने साम्राज्य की नयी राजधानी कावेरी तट पर ‘गंगयीकोण्डचोलपुरम’ की स्थापना की। राजेन्द्र ने श्रीविजय के राज्य (दक्षिणी मलाया प्रायद्वीप और सुमात्र) पर जीत हासिल की, ताकि उसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक हित अक्षुण्ण रहें। चोल राजाओं ने अपनी नौसेना का इस तरह प्रदर्शन किया, मानो बंगाल की खाड़ी उनके लिए झील-समान हो।
परवर्ती चोल शासक कुलोतुंग ने सन् 1077 ई- में सत्तर व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को चीन भेजा। चोल राजाओं ने चीन के साथ व्यापार को अत्यधिक महत्व दिया। चीन को निर्यात किये जाने वाले सामानों में कपड़ा, मसाले, औषधियां, जवाहरात, हाथी दांत, सींग, आबनूस की लकड़ी तथा कपूर प्रमुख होते थे। पश्चिम में मुख्य रूप से फारस और अरब के साथ व्यापार होते थे। विदेश व्यापार के लिए पूर्वी तट पर महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, शालीयूर तथा कोरकई और मालाबार (पश्चिमी) तट पर क्वीलोन में बड़े-बड़े प्रतिष्ठान थे। मार्कोपोलो बताता है कि भारत में आयात के लिए सर्वाधिक व्यय घोड़ों पर किया जाता था।
चोलों के प्रशासन की सर्वाधिक मुख्य विशेषता थी- स्थानीय स्वशासन। हमें ‘ऊर’ और ‘सभा’ या ‘महासभा’ नामक दो समितियों की जानकारी मिलती है। ऊर गांव की प्रधान समिति होती थी, जबकि महासभा गांवों के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी, जिन्हें ‘अग्रहार’ कहा जाता था। ये गांव अधिकांशतः स्वायत्तता का उपभोग करते थे। गांव के कारोबार की देख-रेख एक प्रबंधकारिणी समिति करती थी और इनका संचालन प्रजातांत्रिक रीति से कुशलतापूर्वक किया जाता था।
चोलों के वैभव एवं संपन्नता की एक झलक स्थापत्य के क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों के निर्माण में भी देखी जा सकती है। इन्होंने स्थापत्य की जिस शैली का प्रयोग किया, वह द्रविड़ शैली कहलाती है। इसके अन्तर्गत मुख्य प्रतिमा कक्ष के ऊपर एक के ऊपर एक मंजिल का निर्माण होता था, जिनकी संख्या पांच से सात तक होती थी। ये एक विशेष शैली में बनी होती थीं, जिन्हें ‘विमान’ कहते थे। प्रतिमा कक्ष के सामने स्तम्भयुक्त मंडप होता था, जिसका उपयोग सभाएं आयोजित करने या देवदासियों के आनुष्ठानिक नृत्य के लिए होता था। मन्दिर के गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणापथ हो सकता था। समग्र ढांचा एक प्रांगण के अन्दर ऊंची दीवारों से घिरा होता था, जिसमें ऊंचे प्रवेश द्वार थे, जिन्हें ‘गोपुरम्’ कहा जाता था। गोपुरम् में अलंकरण की संभावना अधिक थी। राजराजा द्वारा बनवाया गया वृहदेश्वर का मन्दिर तंजावुर में है। प्रसिद्ध वास्तुविद और इतिहासकार पर्सी ब्राउन का मत है कि यह मन्दिर द्रविड़ शिल्प कला की सर्वोत्तम कृति है। राजेन्द्र चोल द्वारा बनवाया गया एक अन्य मन्दिर गंगयीकोण्डचोलपुरम में है और इसमें तंजावुर के मन्दिर की अपेक्षा अलंकरण अधिक है।
चोलों का शासनकाल अपनी कांसे की मूर्तियों के लिए भी उल्लेखनीय है। इस काल की नटराज की मूर्तियां विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं जो अपनी उत्कृष्ट कारीगरी के लिए विश्व धरोहर की श्रेणी में आ गयी हैं।
साहित्य के क्षेत्र में तमिल और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रचित ग्रंथों की उत्कृष्टता देखी जा सकती है। बारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में ‘तीरूमुराई’ के नाम से ग्यारह खण्डों में संग्रहीत भक्ति संतों की रचनाओं को पावन और पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखकर तमिल साहित्य का गौरव बढ़ाया। अन्य कई साहित्यकारों ने रामायण और महाभारत को अपनी विषयवस्तु बनाकर इन गौरव ग्रन्थों को जनमानस तक पहुंचाया।
दर्शन के क्षेत्र में रामानुज ने शंकर के ज्ञान मार्ग की जगह भक्ति मार्ग का प्रचार किया। रामानुज के अनुसार, ज्ञान अनेक साधनों में से एक है। लेकिन पूर्णतया समर्पित भावना के साथ की गयी परम भक्ति के सदृश प्रभावशाली अथवा विश्वसनीय नहीं है। रामानुज के भक्ति मार्ग ने हिन्दू धर्म में एक ऐसे तत्त्व का प्रवेश कराया, जिसके अनुसार ईश्वर के पास पहुंचने का बहुत ही सरल उपाय बतलाया गया और वह था- भक्ति और प्रेम।
धर्म के क्षेत्र में लिंगायत सम्प्रदाय के उदय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शैव मतावलम्बी थे। इन्होंने धार्मिक पाखण्डों पर तीव्र प्रहार किया। उन्हाेंने पुनर्जन्म के साथ ही वेदों की प्रामाणिकता पर भी संदेह किया। लिंगायतों में सामाजिक चेतना की भावना प्रबल थी। अधिक उम्र की लड़कियों के विवाह और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। लिंगायतों के उदार सामाजिक विचारों एवं भावनाओं के कारण निम्न जातियों ने भी इसको समर्थन दिया। इन प्रमुख धार्मिक प्रवृत्तियों एवं पद्धतियों के अतिरिक्त स्थानीय देवताओं एवं आस्थाओं को भी मान्यता दी गयी।
इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल शासकों ने दक्षिण भारत की राजनीतिक एकता, व्यापारिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देकर भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय स्थान बनाया है।
Question : हर्ष की मृत्यु से लेकर उत्तर भारत की मुस्लिम विजय तक की अवधि के उत्तर भारत और मध्य भारत के समाज का विवरण दीजिए।
(1996)
Answer : हर्षोत्तर भारत की सामाजिक अवस्था मध्यकाल के प्रारंभ को अभिव्यक्त करती है। पहले से ही स्थापित जाति व्यवस्था सामाजिक ढांचे का मूलाधार बन गयी। हिन्दू धर्म का बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा था। इसी के अनुरूप सामाजिक व्यवस्थाकारों ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों पर काफी बल दिया। अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मणों की सच्चरित्रता और महानता को उजागर किया गया है। शूद्रों की छाया तक से उसे दूर रहने के लिए कहा गया है। गंभीर अपराध के लिए ब्राह्मण को मृत्युदंड से वर्जित करते हुए देश निकाला तथा विशिष्ट चिह्नों से दागने की व्यवस्था दी गयी। मेघातिथि ने विद्वान एवं सच्चरित्र ब्राह्मणों को तो इससे भी मुक्त कर दिया है।
इस युग की महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय है, जिन्होंने प्राचीन क्षत्रियों का स्थान ले लिया था। प्राचीन ग्रंथों में राजवंश के कुमारों को राजपुत्र कहा गया है, किन्तु इस काल में यह शब्द लड़ाकू जातियों तथा सामंत वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। 12वीं शताब्दी तक राजपूतों की 36 जातियां प्रसिद्ध होे चुकी थीं। इनकी उत्पत्ति संबंधी विविध विचार रखे गये हैं। अपने वंशगत स्वाभिमान के लिए ये प्रसिद्ध थे। इनमें बलिदान तथा उच्च आदर्श के अपूर्व उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिसकी छाप इस काल के इतिहास पर पूर्ण रूप से दृष्टिगत होती है।
राजपूत स्त्रियों ने भी ऐसी ही मिसाल कायम की है। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस काल को ‘राजपूत काल’ की संज्ञा दी जाती है, किन्तु एक शक्तिशाली सैनिक वर्ग होने के कारण धर्म, समाज, काव्य-साहित्य, कला तथा स्थापत्य, आर्थिक व्यवस्था आदि जीवन के सभी क्षेत्रों पर इनका गहरा प्रभाव है।
वैश्य वर्ण के लोग सदैव की भांति व्यापार, कृषि, पशुपालन आदि में संलग्न थे। किन्तु इस काल में वैश्य वर्ग अधिकतर व्यापार में ही संलग्न रहे। पशुपालन तथा कृषि व्यवसाय में लगे हुए लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती जा रही थी। इस काल में भी व्यापारी, संघों तथा शिल्पकार, श्रेणियों में संगठित थे। देश की समृद्धि में इनका मूलभूत योगदान था। हालांकि शास्त्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक शिल्पकारों की गणना शूद्र वर्ण में होती थी।
यह ध्यान देने योग्य है कि जाति वर्गीकरण बहुत अधिक कठोर नहीं था। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक तौर पर लोग उच्च वर्ण में शामिल हो सकते थे और निम्न जाति में गिर भी सकते थे। कभी-कभी नयी जातियों को वर्ण की श्रेणी में रखना कठिन हो जाता था। गुप्तकाल के अंतिम समय में जिन प्रशासकीय अधिकारियों का करण या लिपिक के रूप में उल्लेख हुआ है, वे नवीं शताब्दी तक कायस्थ जाति के रूप में संगठित हो चुके थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ में विविध जातियों के लोग, जिनमें ब्राह्मण और शूद्र भी शामिल थे और जिन्होंने राजकीय व्यवस्था में हाथ बंटाया था, कायस्थ नाम से पुकारे गये।
पूर्ववर्त्ती काल की भांति साधारण रूप से शास्त्रीय व्यवस्था शूद्र वर्ण के प्रति अनुदार ही रही। हालांकि शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया था। विभिन्न स्मृतिकारों ने शूद्र के लिए सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शिल्प जैसे विस्तृत क्षेत्र निर्धारित किये। स्मृतियों में शूद्र के हाथ का भोजन तथा उनसे संपर्क वर्जित माना गया। वैश्यों की स्थिति भी निरन्तर गिर रही थी और वे शूद्रों के अधिक करीब हो गये थे। स्मृतिकारों ने समाज की तस्वीर सामान्य रूप से शोषकों एवं शोषितों की बनायी है। परन्तु व्यावहारिक रूप में इसके कुछ अपवाद भी देखे जा सकते हैं।
मेघातिथि ने ब्राह्मण का क्षत्रिय तथा वैश्य से अनुलोम विवाह अपवाद रूप में स्वीकार किया है, जबकि नारदीय पुराण में इसे कलिवर्ज्य माना जाता था। मेघातिथि के अनुसार अनुलोम विवाह की संतान माता की जाति की होगी और प्रतिलोम विवाह की संतान पिता की जाति में होगी। अन्तर्जातीय विवाहों को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति सामाजिक व्यवस्थाकारों के विचारों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसके पीछे रक्तशुद्धि की भावना थी। इस काल में स्वयंवर (विशेषकर राजवंशों में) के उदाहरण प्राप्त होते हैं। स्त्रियों का पुनर्विवाह या विधवा विवाह, पति के लापता होने पर, मृत्यु पर, संन्यासी होने पर या जाति बहिष्कृत होने पर संभव था। कुछ विशेष परिस्थितियों में तथा अनेक बंधनों के साथ ‘नियोग’ शास्त्रीय व्यवस्था में मान्य था। बाल विवाह तथा बहुविवाह स्त्रियों की स्थिति निर्बल ही बनाता था। विभिन्न स्मृतियों में स्त्री विवाह की उम्र घटाकर आठ से 10 वर्ष कर दी गयी। आठ वर्ष की लड़की ‘गोरी’ तथा 10 वर्ष की लड़की ‘कन्या’ कहलाती थी। इनका विवाह किसी भी हाल में रजस्वला होने से पूर्व करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके कारण उनकी समुचित शिक्षा भी संभव नहीं हो पाती थी। साथ ही, सती तथा जौहर प्रथा, पुत्री की बाल हत्या, बहुपति विवाह और देवदासी तथा वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं ने स्त्रियों की दशा को कमजोर करने में ही योगदान किया। हालांकि माता और बहन के रूप में स्त्रियां सामान्य आदर की पात्र थीं, किन्तु पत्नी के रूप में उन्हें पति की हर प्रकार से सेवा प्रदान करने का शास्त्रीय निर्देश था।
भू-सम्पत्ति अधिकार के विकास के साथ-साथ स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकार में वृद्धि हुई। पारिवारिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्त्रियों को अपनी संपत्ति किसी पुरुष संबंधियों को उत्तराधिकार में देने का अधिकार प्रदान किया गया। यदि किसी पुरुष की मृत्यु बिना पुत्र प्राप्ति के हो जाती थी तो कुछ मामलों को छोड़कर उसकी पत्नी को अपने पति की पूरी जायदाद का अधिकार मिल जाता था। किसी विधवा की संपत्ति पर उसकी पुत्रियों का अधिकार होता था। इस प्रकार सामंती समाज ने निजी संपत्ति की धारणा को मजबूत बनाया।
Question : क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में तुर्कों एवं मुगलों के आगमन ने उत्पादन साधनों में अनेक परिवर्तनों का सूत्रपात किया? अपने उत्तर के समर्थन में कारण प्रस्तुत कीजिये।
(1995)
Answer : कुछ समय पहले तक यह समझा जाता रहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले तक भारतीय समाज की अपरिवर्तनशीलता ने प्रौद्योगिकी और उत्पादन साधनों के मामले में पिछड़ापन को बरकरार रखा था। लेकिन मुहम्मद हबीब और इरफान हबीब जैसे आधुनिक इतिहासकारों के सावधान अध्ययन ने यह तथ्य प्रतिपादित किया कि तुर्कों और मुगलों के काल में ही कई प्रौद्योगिक परिवर्तन हुए। नवीन उत्पादन साधनों ने मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये। ‘शहरी क्रान्ति’ और ‘ग्रामीण क्रान्ति’ इसी संदर्भ में गढ़े दो मुहावरे हैं। अगर शहरी अर्थव्यवस्था के विकास को देखें तो इसमें तीन परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं देखी जा सकती हैः
इरफान हबीब ने इस विकास के पीछे तीन कारण गिनाये हैं: (क) भारत में पूर्वी इस्लामी देशों से दस्तकारों तथा व्यापारियों का भारी संख्या में आप्रवासन जो अपने-अपने शिल्प, तकनीकें तथा पेशे अपने साथ लेते आये थे; (ख) व्यापक स्तर पर दास बनाने की प्रक्रिया से विनीत एवं प्रशिक्षित योग्य श्रमिक वर्ग की आपूर्ति; और (ग) इक्ता और खराज की प्रणाली द्वारा कृषि-अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा शहरों के लिए हस्तगत करना। यह बात दीगर है कि तुर्कों के आने से नवीन आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ लेकिन इरफान हबीब इस व्यवस्था को शोषक ही मानता है।
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का सीधा संबंध सल्तनत काल की तकनीकी उन्नति से है। कृषि समाज के अधिकतर वर्गों की आय का प्रमुख स्रोत थी। खेती की उपज बढ़ाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार तो नहीं हुए, लेकिन सिंचाई के क्षेत्र में रहट का उपयोग महत्वपूर्ण अवश्य है। प्राचीन भारत में रहट के उपयोग के संबंध में अस्पष्ट उल्लेख है; परन्तु इसका पहला विस्तृत लिखित विवरण 16वीं शताब्दी के बाबरनामा में मिलता है। यह रहट गहरे कुंए से पानी निकालने में समर्थ था और इस तरह पूर्व के रहट से भिन्न था जो केवल खुले तल वाले जलाशय जैसे नदी, तालाब से ही पानी निकाल सकता था। रहट के प्रयोग को इस बात से आंका जा सकता है कि पंजाब में, जो कि परंपरागत धारणा के अनुसार निर्जन क्षेत्र था, 15वीं शताब्दी के आसपास आर्थिक सुधारों की गति तीव्र होने लगी। परवर्ती कालों में पंजाब की कृषि-संपन्नता रहट के प्रवेश और प्रसार के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है।
वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में चरखे का यांत्रिक उपकरण के रूप में बहुत महत्व रहा है। भारत में चरखा संभवतः ईरान से आया। भारत में इसका पहला लिखित उल्लेख इसामी की फुतूह-उस-सलातीन (1305 ई.) में मिलता है। इरफान हबीब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत में चरखे के वास्तविक प्रादुर्भाव का समय 12वीं-14वीं शताब्दी ही मानना चाहिए और धुनिया की कमान भी संभवतः इसी समय बाहर से भारत में आयी होगी। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि इन आयातित उपकरणों ने कई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सूत्रपात किया। चूंकि चरखा कपड़े की किस्म में गुणात्मक सुधार के बदले, कातने की गति बढ़ाता है इसलिए यह हिसाब लगाना कठिन नहीं है कि सूती कपड़े के उत्पादन में बड़ी भारी वृद्धि हुई होगी।
सूती कपड़े के अतिरिक्त, रेशमी कपड़े की बुनाई में भी विकास हुआ था क्योंकि रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में ही प्रचलित हुई। इसका सीधा प्रभाव संभवतः भारतीय रेशम वस्त्र-उद्योग पर पड़ा होगा क्योंकि इससे पहले कच्चा माल बाहर से आयात किया जाता था। इस काल में तकनीकी विकास का एक और उदाहरण कालीन बनाने के उद्योग में मिलता है।
कागज निर्माण एक अन्य क्षेत्र है, जिसका इस्तेमाल तुर्की लोगों के आगमन के बाद तेरहवीं शताब्दी में व्यापक रूप से होने लगा था। भारत में इस समय भी आमतौर पर ताड़ के पत्तों और छाल पर लिखाई होती थी। अमीर खुसरो ने तेरहवीं शताब्दी के अंत में इसका उल्लेख किया है कि कागज का प्रसार भारत में हो चुका है। इस तकनीकी विकास के दूरगामी प्रभाव न केवल शिक्षा के प्रसार पर, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी देखे जा सकते हैं। सस्ते कागज की उपलब्धि से हुंडियों से लेन-देन के व्यापारिक कागज, राज्य को निर्देश आदि भेजना अधिक सुगम हो जाता था और इससे विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संपर्क अधिक दृढ़ हो जाने की संभावना भी बढ़ जाती थी।
समुद्री जहाजों में चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग, समय-सूचक उपकरणों के रूप में नक्षत्र घडि़यां, धूप घड़ी और जल-घड़ी अन्य ऐसे उत्पाद हैं जिन्होंने निश्चय ही जीवन के विभिन्न पहलूओं को छूआ और उन्हें संवारा भी। शस्त्रस्त्रें में धातु का प्रयोग भारत में प्राचीनकाल से ही किया जाता रहा है। मुगलों के आगमन से पूर्व भारत में तोपों, बंदूकों और बारूद का प्रयोग अज्ञात था। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में किया था। तोपों ने भारतीय युद्ध कला में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया।
मुगलकाल में नगर उत्पादन और व्यापार के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित हुए। नगरों में केन्द्रित उद्योग हस्तशिल्प-उत्पादन पर आधारित थे और इनमें सबसे अधिक महत्व वस्त्र उद्योग का था। सल्तनतकाल से चले आ रहे उद्योगों ने काफी तकनीकी प्रगति कर ली थी। मुगलकाल में खनिज पदार्थों की निकासी और धातु-उत्पादन के उद्योग भी विकसित अवस्था में था। धातु-उद्योग में प्रमुख स्थान लौह एवं इस्पात का था। इस्पात का उपयोग हथियारों के निर्माण के लिए होता था जिनमें तलवारें, तीर और भालों की नोक, तोप और बंदूकों की नाल के अतिरिक्त कवच भी बनाए जाते थे। लोहे का उपयोग घोड़ों की नाल, कांटी, छोटे-छोटे औजार और सामान्य उपयोग की वस्तुओं के निर्माण में होता था। सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों के निर्माण में होता था। समकालीन ईरानी और यूरोपीय यात्रियों ने भारतीय आभूषण-निर्माताओं की दक्षता और उनके सुन्दर उत्पादनों का वर्णन किया है। मुगल काल में लकड़ी, चमड़े, शीशे और हाथी-दांत की वस्तुएं भी बड़ी संख्या में बनायी जाती थीं। इन सबके अतिरिक्त कपड़ों में माड़ी देना, रंगना, कढ़ाई का काम भी प्रमुख व्यवसायों में थे।
ऐसे अनेक उत्पादन और व्यवसाय इस काल में विकसित हुए जो इनके तकनीकी विकास की कहानी बताते हैं। तुर्कों और मुगलों के आगमन ने उत्पादन के जो नवीन साधन उपलब्ध कराए वह भारतीय अर्थ व्यवस्था में बदलाव लाने में सहायक हुए। मुगलकाल में भारत की आर्थिक प्रगति पूरे विश्व में ईर्ष्या का विषय बन गया था।Question : उत्तर भारत के भूमि अनुदान-पत्र (लगभग 750 से 1200 ई)
(1995)
Answer : भूमि अनुदान-पत्र विशेष रूप से ऐसे आलेख हैं जो पत्थर या तांबे की पट्टिका पर उत्कीर्ण हैं। सामान्यतः इनसे दाता, दानग्राही, राजवित्तीय कर, दान की गयी भूमि, अनुदान के अवसर और उद्देश्यों का पता चलता है। अनुदान-पत्र में उसकी विजयों और उसके नाम के साथ कई विशेषण लगे रहते हैं जो उसकी राजनीतिक स्थिति, धार्मिक संबंध और उसकी कुछ उपलब्धियों को व्यक्त करते हैं। चूंकि दानग्राहियों में आमतौर पर ब्राह्मण होते थे, अतः वे अपने गोत्र और प्रवर से पहचाने जाते हैं। जिन करों से दानग्राही या दान की गयी जमीन अथवा गांव को छूट दी जाती थी वे भी भूमि अनुदान की विषय वस्तु का अविभाज्य अंग होते थे। करों की सूची एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और एक काल से दूसरे काल में बदलती रहती है। कुछ अधिकार-पत्रों में गांव में रहने वाले किसानों और शिल्पियों के साथ-साथ भूमिखण्डों पर काबिज काश्तकारों को सीधे स्थानान्तरित कर देने की व्यवस्था है।
आरंभिक मध्यकाल में यह एक आम प्रथा थी कि राजा जब तीर्थ स्थानों की यात्र पर जाते थे तो वे इसका शुभारंभ भूमि अनुदान से करते थे। कई बार यज्ञ और तीर्थ यात्रएं युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु किया जाता था। अनेक भूमि-अनुदानों में गांव के वयोवृद्ध जनों और विभिन्न प्रकार के निवासियों के अनुसार पहचान की गयी है। दाता स्वयं अपने और साथ ही पूर्वजों व पारिवारिक सदस्यों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए भूमिदान करता था। धर्म के लाभ एवं वृद्धि और पूर्वजों की प्रतिष्ठा को बार-बार अनुदान के मूल अभिप्राय के रूप में पेश किया गया है। अनेक भूमि-अनुदानों में उन राजस्वगत एवं प्रशासनिक इकाइयों के नाम भी दिये रहते हैं जिनमें वह भूमि व गांव स्थित है। भूमि-अनुदानों में यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अमुक कर्त्तव्यों का पालन करे या फिर इसकी वापसी के लिए तैयार रहें। दूसरी ओर, उत्तराधिकारी राजकुमारों को यह कहकर डराया धमकाया भी गया है कि यदि उन्होंने भूमि-अनुदान पत्रों को छीन लिया तो उन पर सभी तरह की विपत्तियां टूट पड़ेंगी।
अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर पहले-पहल भूमि-अनुदान प्रथम शताब्दी ई.पू. दक्कन में सातवाहनों द्वारा जारी किये गये हैं। इन अनुदान-पत्रों के बारे में कहा गया है कि जब तक सूरज और चांद है तब तक वे बने रहेंगे। किंतु गुर्जर-प्रतीहारों के शासन काल में हमें इनके प्रतिग्रहण एवं नवीकरण के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। आरंभिक मध्यकालीन अनुदानों में लाभ भोगियों को कुछ कृषि अधिकार के इस्तेमाल के अधिकार भी हस्तांतरित किये गये हैं। जहां तब ब्राह्मणों को अनुदान देने की बात है, उनसे निजी स्वामित्व की प्रक्रिया को ही बढ़ावा मिला। उनका भू-धारण अधिकार राजकीय अधिकार पत्र पर आश्रित था जिसके द्वारा उन्हें फलोपभोग का अधिकार हस्तांतरित किया जाता था। किंतु चूंकि यह अनुदान वंशानुगत था और साथ ही राज्य कर से मुक्त भी; अतः व्यवहार में यह भूमि मिलकियत जैसा ही था।
अनेक अनुदानों में ऐसे संसाधनों और उत्पादकों के नाम भी दिये गये हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की खास विशेषताएं हैं। इस समय के अनुदानों में संबद्ध भूमि की माप भी दी गयी है। 11वीं-12वीं सदी के दौरान लोगों की क्रय-शक्ति का भी अनुदानों से पता चलता है। सिक्कों के बारे में भी इसमें उल्लेख है। इस सदी के भूमि अधिकार-पत्रों में उल्लिखित शहरों के स्वरूप से पता चलता है कि तुर्क-अफगानों ने ही शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू की।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूमि अनुदान-पत्र न केवल भूमि-व्यवस्था बल्कि फसलों, हस्तशिल्पों, व्यापार, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था व बस्तियों के इतिहास की भी जानकारी देने में सहायक है।
Question : भारत में अरबों के आगमन के ऐतिहासिक महत्व पर एक लघु लेख लिखिये। इसका उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
(1995)
Answer : भारत में अरबों के आगमन का राजनीतिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं है, जितना अन्य पक्षों का है। अरब भारत में उस प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाये, जैसा कि उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। यहां तक कि सिंध में भी उनकी शक्ति अधिक दिनों तक नहीं बनी रही। किंतु दीर्घकालिक परिणामों की दृष्टि से प्रतीत होता है कि अरबों ने भारतीय जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुए।
अरबों ने चिकित्सा, दर्शनशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ली। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अलफजारी ने अरबी में अनुवाद किया। अलबरूनी कहता है कि पंचतंत्र का अनुवाद भी अरबी में हो चुका था। सूफी धार्मिक संप्रदाय का उद्भव स्थल सिंध ही था, जहां अरब लोग रहते थे। सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। दशमलव प्रणाली अरबों ने नवीं सदी में भारत से ही ग्रहण की थी।
यदि तात्कालिक राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाये तो कहा जा सकता है कि अरबों ने एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत की, जिसका सामना करने के लिए ऐसी शक्तियां उदित हुईं, जो भारत में आगामी 300 वर्षों तक व्याप्त रहीं। गुर्जर-प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, चालुक्यों की प्रतिष्ठा की स्थापना उनके द्वारा अरबों का विरोध करने के कारण हुई। दीर्घकालिक दृष्टि से भी अरबों ने राजनीतिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण नीति का प्रचलन किया। भारत में उन्होंने धर्म राज्य की स्थापना न करके धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। हालांकि जजिया संग्रहीत किये जाते थे। यह भी अरबों के भारत आगमन का एक उल्लेखनीय महत्व था।
अरबों के भारत आगमन का आर्थिक महत्व व्यापार के क्षेत्र में देखा जा सकता है। अरब व्यापारियों के समुद्री एकाधिकार के साथ भारतीय व्यापारियों ने तालमेल बनाया और पश्चिमी जगत तथा अफ्रीकी प्रदेशों में अपनी व्यापारिक गतिविधियां जारी रखीं।
Question : ‘बलबन के राजत्व सिद्धांत’ पर 200 शब्दों में एक लेख लिखिये।
(1995)
Answer : दिल्ली के सुल्तानों में बलबन पहला शासक था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धान्तों पर विस्तारपूर्वक विचार किया था। इसके पीछे निहित कारण पिछले 30 वर्षों में इल्तुतमिश के कमजोर उत्तराधिकारियों द्वारा सुल्तान के पद के गौरव और मर्यादा को बनाये रखने में असमर्थता थी। इसके अतिरिक्त बलबन को सत्ता-हरण का औचित्य भी सिद्ध करना था। इस सबके लिए आवश्यक था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा सुल्तान न केवल शक्तिशाली होता वरन् प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी अप्रतिम होता।
बलबन का राजत्व सिद्धान्त प्राचीन ईरान के सासानी शासकों के सिद्धान्त पर आधारित था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता राजत्व का अर्द्धदैवी स्वरूप था। बलबन ने राजत्व को ‘नियाबते खुदाई’ अर्थात् ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में माना और खुद के लिए ‘जिल्ले इलाही’ अर्थात् ईश्वर की छाया शब्द का प्रयोग किया। इसका तात्पर्य यह सिद्ध करना था कि शासक कोई साधारण मनुष्य नहीं, वरन् ईश्वर द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, जिसकी आज्ञा का पालन ईश्वर की आज्ञा-पालन के बराबर है और जिसकी अवज्ञा अपराध ही नहीं वरन् पाप भी है। इस प्रकार धार्मिक भावना के आधार पर शासक की सत्ता को बलबन ने सुदृढ़ किया।
राजत्व संबंधी एक दूसरी विशेषता निरंकुशता थी। बलबन मानता था कि ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते सुल्तान के ऊपर अंकुश लगाने की क्षमता किसी भी मानव में नहीं है, चाहे वह उलेमा हो या सामन्त। और इसी कारण यह इन लोगों के राजनीतिक हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करता था।
शासक की दैवी छवि और निरंकुशता ने सुल्तान के पद की गौरव और शक्ति को पुनसर््थापित कर दिया। निरंकुश राजतंत्र की कल्पना शासक की शक्ति में वृद्धि का कारण सिद्ध हुई, जबकि अर्द्धदैवी स्वरूप के कारण राजत्व की प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ़ गयी। इसके साथ ही साथ बलबन ने न्यायप्रियता का गुण भी राजत्व सिद्धान्त में सम्मिलित किया। उसने प्रजा को शासक की निरंकुश शक्तियों से सुरक्षा का आश्वासन दिया। किसी सामन्त या प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा उन पर अत्याचार भी समाप्त किया गया।
पर ऐसा नहीं कि बलबन प्रजा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का समर्थक रहा हो। इसके विपरीत वह प्रजा से दूरी बनाए रखना अच्छा समझता था ताकि प्रजा के मन में शासक का भय बना रहे। वह कुलीनवाद का भी समर्थक था। उसके सामन्त उच्च कुल के होते थे। वह निम्न कुल के व्यक्ति से मिलना भी पसन्द नहीं करता था। उसने खुद को महान ‘अफरासियाब’ का वंशज कहा और अपने वंशजों के नाम प्राचीन तूरान के महान शासकों के नाम पर रखा।
अपने राजत्व सिद्धान्त को कार्यरूप देने के लिए राजदरबार का उसने पुनर्गठन किया। ‘सिजदा’ और ‘पायबोस’ की ईरानी प्रथा को लागू किया। दरबार में उपस्थित होने के लिए सामन्तों के लिए निर्धारित पोशाक निश्चित किया। दरबार में हंसी-मजाक पर रोक लगा दी। बलबन राजसी ठाठ-बाट के साथ दरबार में आता और दरबार में पूरी गंभीरता का ख्याल रखता था। ये कुछ ऐसे उपाय थे जिन्होंने राजा की शक्ति और पद की मर्यादा को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया।
Question : अलाउद्दीन खिलजी एवं शेरशाह सूरी द्वारा किये गये कृषि संबंधी सुधारों की तुलनात्मक पुनरीक्षा कीजिये।
(1995)
Answer : अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी दो ऐसे मध्यकालीन शासक हुए जो भारतीय इतिहास में अपने सुधारों के लिए ही सबसे अधिक याद किये जाते हैं। जहां तक इनके कृषि संबंधी सुधारों का सवाल है तो सच्चे मायनों में ये कृषि सुधार नहीं कहे जा सकते। यहां कृषि संबंधी सुधार का अर्थ भू-राजस्व या लगान संबंधी सुधारों से ली जाती है।इन दोनों शासकों के लगान संबंधी सुधार परवर्ती शासकों के लिए दिशा-निर्देशक हो गये और इसलिए भी इनके सुधारों का महत्व है। वैसे तत्कालीन प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप इनके कृषि संबंधी सुधार प्रशंसनीय हैं।
अलाउद्दीन के समय लगान राज्य की आमदनी का प्रमुख साधन था जिसमें वह पर्याप्त वृद्धि करना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह मध्यस्थ भूमिपति वर्ग का दमन भी करना चाहता था जो राज्य में विद्रोहों का एक प्रमुख कारण था। इस प्रकार अलाउद्दीन के राजस्व-सुधार दो उद्देश्यों से प्रेरित थे- राज्य की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि, जिससे कि साम्राज्य-विस्तार के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया जा सके तथा मध्यस्थ भूमिपति वर्ग का दमन और उसका धन छीनना ताकि इस वर्ग द्वारा विद्रोह एवं उपद्रव की समस्या का समाधान हो सके।
जबकि शेरशाह सूरी द्वारा अपनाये गये भू-राजस्व नीति के नियामक सिद्धान्तों के बारे में अब्बास खां दो बातों की चर्चा करते हैं; एक, रैयत अर्थात् प्रजा की भलाई की चिंता मुख्य थी। इसलिए निर्धारित भू-राजस्व की मात्र साधारण होती थी, किन्तु निर्धारण के बाद उसकी वसूली पूरी मात्र में होती थी; दूसरी, वसूली करने वाले अमले पर उचित नियंत्रण रखा जाता था, किन्तु कर-निर्धारण और वसूली के शुल्क के रूप में तथा जमींदारों को नियंत्रित रखने के लिए उनका देय हिस्सा भी उन्हें अवश्य दिया जाता था।
अलाउद्दीन ने भू-राजस्व वसूली में वृद्धि के लिए तीन महत्वपूर्ण उपाय किये। उसने दोआब-गंगा और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में लगान की दर में वृद्धि के आदेश दिये। अब किसानों को उपज के एक-तिहाई के स्थान पर आधा हिस्सा लगान के रूप में देना था। दूसरी ओर, अलाउद्दीन ने दोआब क्षेत्र में कर-मुक्त भूमि पर केन्द्रीय नियंत्रण स्थापित कर दिया और सारे भूमि-अनुदान वापस ले लिए। इक्ता, इनाम, मिल्क, वक्फ आदि के रूप में सामन्तों, अधिकारियों और उलेमा के पास जो भूमि थी उसे खालसा (सुल्तान के प्रत्यक्ष शासन के अधीन) भूमि में परिवर्तित करने के आदेश दिये गये। इस प्रकार राज्य की आमदनी में और अधिक वृद्धि संभव हुई।
अलाउद्दीन ने संभवतः लगान निर्धारण की पद्धति में भी सुधार लाया। बरनी के अनुसार, उसने भूमि की माप के आधार पर लगान वेफ़ निर्धारण के आदेश दिये। इस पद्धति के लिए ‘मसाहत’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। परन्तु बरनी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। उसने मात्र इतना ही लिखा है कि अलाउद्दीन ने प्रति ‘बिस्वा’ में उपज के आधार पर लगान निर्धारित करने का आदेश दिया। लगान वसूली के कार्य में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने एक नये विभाग ‘दीवाने मुस्तखराज’ की स्थापना की।
शेरशाह का रुझान भी मापन की प्रथा की ओर था और अलाउद्दीन खिलजी की तरह वह भी इसका जितना हो सके, उतना विस्तार करना चाहता था। जमीनों का आम सर्वेक्षण करवाया जाना नई ‘जमा’ को तय करने के लिए लाभकारी हो सकता था किंतु उसका शासन काल छोटा होने के कारण संतोषप्रद नहीं हो सका।
अलाउद्दीन ने दोआब क्षेत्र में भू-राजस्व की दर आधी कर दी थी, जबकि अबुल फजल कहता है कि शेरशाह की दरें सबसे कम थी; शायद यह एक-चौथाई था जिसे अकबर ने बढ़ाकर एक-तिहाई कर दिया था। लेकिन मोरलैंड का मानना है कि शेरशाह के समय भू-राजस्व की दर एक-तिहाई थी। परमात्मा सरन भी ‘राई’ शब्द की व्याख्या करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुचंते हैं कि राज्य की मांग 1/3 थी।
शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि को तीन श्रेणियों- उत्तम, मध्यम और निम्न में विभक्त कर दिया था। इनकी औसत उपज का एक-तिहाई भाग लगान के रूप में लिया जाता था। इस व्यवस्था की आलोचना यह कह कर की जाती है कि खराब भूमि से अधिक और अच्छी भूमि से कम लगान प्राप्त होता था।
किसानों को नकदी या अनाज किसी एक माध्यम से लगान देने की छूट दी गयी। लगान के निर्धारण में नरमी बरती गयी लेकिन वसूली ठीक समय पर कड़ाई के साथ की जाती थी। जबकि अलाउद्दीन ने दोनों ही मामलों में कड़ाई का रुख अपनाया। उसने किसानों को अधिशेष अनाज राज्य द्वारा निश्चित किये गये मूल्य पर बेचने के लिए भी बाध्य किया। कभी-कभी किसानों को वही अनाज बाजार में अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता था। किसानों को दरअसल हमेशा रोटी की चिन्ता में ही समय गुजारना पड़ता था। अलाउद्दीन में वह मानवीयता भी नहीं थी जो शेरशाह में थी। शेरशाह काश्तकारों पर जुल्म के विरुद्ध था।
अलाउद्दीन की कृषि नीति के पीछे उसकी महत्त्वाकांक्षी बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था थी जिसमें सैनिकों के हित को प्रमुखता दी गयी थी। शेरशाह ने अपने पिता की जागीर का काम अनेक वर्षों तक संभाला था; अतः उसमें व्यवस्थापकीय गुण आ चुका था। यही कारण है कि उसकी कृषि नीति में प्रवीणता स्पष्ट दिखलायी पड़ती है। शेेरशाह का परवर्त्ती मुगल शासक अकबर अपने पूर्ववर्ती शासक की आर्थिक नीति का अनुसरण करके साम्राज्य में समृद्धि ला सका। दूसरी ओर, अलाउद्दीन का परवर्त्ती शासक मुहम्मद बिन तुगलक ने उसकी कृषि नीति का अनुसरण करते हुए दोआब में कर की दर बढ़ाकर आधा कर दिया तो इसके विरुद्ध विद्रोह हो गया।
अलाउद्दीन ने मध्यस्थ भूमिपतियों, यथा-खूत, मुकद्दम एवं चौधरी के दमन के लिए कड़े उपाय किये। अलाउद्दीन विभिन्न बगावतों के पीछे इनका हाथ मानता था; अतः उसने इस वर्ग का खात्मा कर देना अपना कर्त्तव्य समझा। इस वर्ग के सदस्यों पर कई बंदिशें लगायी गयी। ये बहुत जल्द ही गरीबी के कगार पर पहुंचा दिये गये। शेरशाह ने भी भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवायी की। लेकिन भ्रष्टाचार इन दोनों शासन काल में पूरी तरह समाप्त नहीं किये जा सके।
अलाउद्दीन का भू-राजस्व, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ निकट का संबंध स्थापित करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। इन सुधारों के कुछ उपायों को उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा जो बाद में शेरशाह के कृषि सुधारों का भी आधार बने।
Question : दिये गये मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिये और केवल अंकित स्थानों में से ही प्रत्येक पर लगभग 50 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखियेः
1. अहमदनगर, 2. अन्हिलवाड़ा, 3. बाद्गारा, 4. बालासोर, 5. बयाना 6. बीदर, 7. चिंसुरा 8. चित्तौड़, 9. दमन, 10. धर्मत, 11. दीपालपुर, 12. गंगैकोण्डचोलपुरम, 13. गौर, 14. धारगांव, 15. कामतापुर, 16. कटेहर, 17. किशनगढ़, 18. लखनावती, 19. मदुरै, 20. माण्डू, 21. नवसारी, 22. ओरछा, 23. पण्ठरपुर, 24. पानीपत, 25. पाटण, 26. कमरनगर, 27. रायचूर, 28. सिरोही, 29. सोमनाथ, 30. तिरहुत।

(1995)
Answer : 1. अहमदनगर: वर्तमान में यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जिसकी स्थापना 1490 ई. में अहमद निजामशाह ने बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद की थी। यह राज्य दक्षिण भारत की राजनीति में प्रमुख स्थान रखता था लेकिन विजयनगर के साथ 1565 ई. के तालीकोटा के युद्ध के बाद इसकी स्थिति बदलने लगी। अकबर ने 1597 ई. में ही अहमदनगर के विरुद्ध सैनिक अभियान का आदेश दिया था लेकिन मुगल साम्राज्य में विलय नहीं कर सका था। चांद बीबी ने इसका डटकर मुकाबला किया था लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। अहमदनगर के किले पर अकबर ने 1600 ई. में अधिकार कर लिया था लेकिन पूर्णतः विलय शाहजहां ने 1637 ई. में की।
2. अन्हिलवाड़ा: यह गुजरात राज्य में स्थित है जिसकी पहचान प्राचीन पाटन नगर के रूप में की गयी है। इसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने गुजरात के एक बड़े भू-भाग को जीतकर किया था तथा इसको अपनी राजधानी बनाया। महमूद गजनवी ने 1025 ई. में इसपर आक्रमण किया था। 1178 ई. में यहां का शासक मूलराज द्वितीय ने आबू के निकट मुहम्मद गोरी को हराया था। 1299 ई. में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अन्हिलबाड़ा के राजा कर्ण को पराजित किया था और तभी से 1401 तक यह दिल्ली सल्तनत का अंग बना रहा। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक अन्हिलवाड़ा एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बना रहा।
3. बाद्गारा: मध्यकाल में, विशेषतः सेन नरेशों के समय में बंगाल का एक महत्वपूर्ण प्रांत था।
4. बालासोर: उड़ीसा में समुद्र तट पर बालासोर मुगलकाल में एक व्यापारिक केन्द्र था। 1658 ई. में डचों ने बालासोर में एक फैक्टरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने 1633 ई. में ही यहां अपनी फैक्टरी खोल ली थी। बंगाल में औरंगजेब के वायसराय शाईस्ता खां ने अंग्रेजों के अनाप-शनाप मांगों पर रोक लगा दिया और 1686 में उनके कई फैक्ट्रियों को जब्त कर लिया। अंग्रेजों ने विरोधस्वरूप बालासोर को खूब लूटा। 1803 ई. के देवगांव संधि के तहत भोंसले राजा ने बालासोर अंग्रेजों को सौंप दिया।
5. बयाना: यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है जो मध्यकालीन भारत में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। करावली राजवंश के प्रथम राजा विजयपाल ने मथुरा से आकर विजय मंदिर गढ़ बनाया था जिसका बाद में नाम बदलकर बयाना हो गया। 1196 ई. में यहां के किले पर मुहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया था। मध्य और उत्तर मुगल काल में यह स्थान भरतपुर के जाट राजाओं की एक रियासत बन गया था। आगरा के निकट होने के कारण भी इसका सामरिक महत्व बहुत था।
6. बीदर: वर्तमान में यह स्थान आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के निकट स्थित है। हालांकि इसका स्वतंत्र अस्तित्व 1526-27 में स्थापित हुआ जब बहमनी राज्य का विघटन हुआ। इसकी स्थापना अली बरीद ने की थी। बहमन शासक अहमदशाह ने 1425 ई. में इसको अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर के विरुद्ध सम्मिलित अभियान में बीदर भी शामिल था। यहां सबसे प्रसिद्ध इमारत महमूद गवां द्वारा बनाया गया मदरसा है जिससे ईरानी निर्माण शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 1619 ई. में बीजापुर ने बीदर पर अधिकार कर उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया।
7. चिंसुरा: वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित चिंसुरा में 1653 ई. में डचों ने अपनी कोठी बनायी। डचों का यहां आगमन व्यापारिक उद्देश्यों, खास कर कपड़े और सिल्क के व्यापार को बढ़ाने हेतु हुआ था। चिंसुरा के डच बंगाल में अंग्रेजी प्रभाव से ईर्ष्या रखते थे। 1698 ई. में शहजादा अजीमुश्शान के वर्दमान प्रवास के दौरान चिंसुरा के डचों ने अंग्रेजों को चुंगी संबंधी मिली छूटों का विरोध किया था। डचों ने कानून बनाकर चिंसुरा में घृणित सती प्रथा पर रोक लगायी थी।
8. चित्तौड़: यह राजस्थान के उदयपुर में चम्बल की सहायक नदी गम्भीरा नदी के तट पर अवस्थित है। यह मेवाड़ के राजपुताना क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र था। 7वीं-8वीं सदी में बप्पारावल ने इसको अपनी राजधानी बनाया जो संभवतः 16वीं सदी तक अपनी अस्मिता बनाये रखी। राणा रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ई. में इस पर आक्रमण कर दिया। सात महीने के कठिन संघर्ष के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने छल से चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लिया। कहा जाता है कि राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने वह आक्रमण किया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम खिज्राबाद रख दिया। गुजरात के शासक बहादुरशाह ने 1534-35 ई. में एवं अकबर ने 1567 में इस पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ के प्रमुख शासकों में राणा कुम्भा, राणा सांगा, उदयसिंह एवं महाराणा प्रताप ने ख्याति अर्जित की। चित्तौड़ गढ़ का किला राजा चित्रंगद ने बनवाया था तथा चित्तौड़ का कीर्ति स्तम्भ एवं विजय स्तम्भ का निर्माण राणा कुम्भा ने करवाया था।
9. दमन: यह गुजरात राज्य में दक्षिणी सीमा पर स्थित है। 1531 ई. में पुर्तगालियों ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। 1559 में पुर्तगालियों ने इस पर पुनः आक्रमण कर इस पर व्यापारिक बस्ती स्थापित की। भारत ने 1961 ई. में उसे अपने अधिकार में लिया। वर्तमान दमन नगर दो हिस्सों-प्रथम तटीय भाग और दूसरा थोड़ी दूर स्थित नगर हवेली में विभाजित है।
10. धर्मत: यह मध्य प्रदेश में उज्जैन के समीप स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां के बीमार होने पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारम्भ हो गया। इसी उत्तराधिकार के संघर्ष की एक कड़ी धरमत की लड़ाई भी है। यह युद्ध 25 अप्रैल, 1658 ई. में औरंगजेब और मुरादबख्श की सम्मिलित सेना एवं दारा के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व जसवंत सिंह एवं कासिम खां कर रहा था। इस युद्ध में दारा की सेना पराजित हुई और औरंगजेब के लिए मुगल बादशाह की गद्दी प्राप्त करने में सहायता की।
11. दीपालपुर: वर्तमान में यह नगर पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में सिन्धु नदी के तट पर अवस्थित है। पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से मंगोलों द्वारा किये जाने वाले आक्रमणों से रक्षा के लिए बलबन ने कुछ क्षेत्रों को सामरिक महत्व का क्षेत्र घोषित कर दिया था। इन सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में दीपालपुर भी प्रमुख था। यहां बलबन ने दुर्ग का निर्माण कराया तथा सीमा की रक्षा हेतु विशाल सेना नियुक्त कर दी।
12. गंगैकोण्डचोलपुरमः यह पूर्व मध्यकालीन स्थल तमिलनाडु के त्रिचिनापल्ली में अवस्थित है। इसकी स्थापना परवर्ती चोल शासक राजेन्द्र प्रथम (1014-44 ई.) ने गंगा घाटी की सफलता पर किया था। कावेरी नदी तट पर निर्मित इस नगर को राजेन्द्र प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया। यहां इसने वृहदेश्वर मन्दिर का निर्माण कराया तथा चोलगंगन नामक तालाब का निर्माण कराया जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तम्भ भी बनवाया था।
13. गौड़: मध्यकाल में गौड़ बंगाल की राजधानी थी। 14वीं शताब्दी की परम्परा वाली ईंटों के मेहराब का निर्माण यहां विकसित हुआ। हिन्दू एवं मुस्लिम तरीकों का अजीब घालमेल पाया गया। यह फिरोज शाह मिनार, छोटा सोना और बड़ा सोना मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है।
14. धारगांव: यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवस्थित है। यहां मालवा के परमारों ने शासन किया। राजा मुंज के समय धार शिक्षा एवं संस्कृति का केन्द्र थी लेकिन इसकी पराकाष्ठा राजा भोज के समय देखने को मिलती है। 1305 ई. में मालवा नरेश महलकदेव को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने धार पर अधिकार कर लिया तथा धार समेत मालवा को भी दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। यहां मध्यकाल में गेहूं की अच्छी पैदावार होती थी। यहां से दिल्ली के लिए पान भी भेजे जाते थे।
15. कामतापुर: वर्तमान पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में कामतापुर ने पंद्रहवीं सदी के प्रारंभ में प्रमुखता हासिल की थी। इस समय सेन शासकों ने एक प्रबल राजतंत्री राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी कूचबिहार से कुछ मील दक्षिण कामतापुर में थी। सेन शासकों ने कामत पर लगभग पचहत्तर वर्षों तक राज किया। उनके अन्तिम शासक नीलाम्बर को बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह ने 1498 ई. में हरा दिया और कामतापुर पर अधिकार कर लिया।
16. कटेहर: वर्तमान उत्तर प्रदेश में रोहिलखंडक्षेत्र ही मध्यकालीन कटेहर है। इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। लम्बे संघर्ष और काफी खून-खराबा के बाद इल्तुतमिश कटेहर को जीत पाया था, जहां राजपूत शासक राज्य कर रहे थे। कटेहर के राजपूतों ने जब सुल्तान को कर देना बंद कर दिया तो 1254 में बलबन उनका दमन भारी मारकाट के बाद ही कर सका। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कटेहर साम्राज्य का अनुशासित अंग बना रहा। खिज्रखां (1414-1421) और मुबारक शाह (1421-1434) के समय पुनः विद्रोह शुरू हुए। 1748 में अफगान अली मुहम्मद खां रूहेला ने कटेहर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कटेहर का नाम रूहेलखंड हो गया।
17. किशनगढ़: यह राजस्थान के जयपुर और अजमेर के मध्य स्थित है। इसकी स्थापना 1575 ई. में जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। इसकी प्रसिद्धि चित्रकला की विशिष्ट शैली के कारण मानी जाती है, इस चित्रकला शैली के विकास की शुरुआत सहसमल ने 1615-18 ई. के बीच की थी। निहालचन्द द्वारा निर्मित बणी-ठणी का चित्र इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इसकी विशेषताओं में अत्यन्त नुकीली बादामनुमा आंखें, ऊपर उठी हुई भवें, नुकीली ठोढ़ी एवं नाक इत्यादि हैं।
18. लखनावती: यह प. बंगाल राज्य में माल्दा जिले में स्थित है। लखनौती सेन वंश के शासकों के समय बंगाल की राजधानी थी। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के नाम पर इसका नाम लखनौती (लखनावती) रखा गया। 1204-05 ई. में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की पूर्व राजधानी नदिया पर आक्रमण कर अधिकार में ले लिया, उसके बाद लक्ष्मण सेन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। 1538 ई. में शेरशाह के नेतृत्व में अफगानों ने इस पर अधिकार कर लिया जो अन्ततः 1575 ई. में अकबर के अधीन हो गया।
19. मदुरै: तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भाग में वैगेई नदी के किनारे स्थित यह नगर प्राचीन काल में पांड्य राज्य की राजधानी हुआ करती थी। 1311 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने मदुरै पर आक्रमण कर वहां से बड़ी मात्र में सामरिक एवं आर्थिक महत्व की चीजें हासिल कर दिल्ली लाया। इसमें प्रमुख रूप से हाथी एवं कीमती पत्थर विशेष उल्लेखनीय है। 1370 ई. में मदुरै को विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। अराविडु वंश के पतन के बाद यहां नायक वंश का शासन स्थापित हो गया। यहां की मीनाक्षी मंदिर अपनी सौन्दर्य एवं वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।
20. माण्डु: माण्डु मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मालवा के शासक हुशंगशाह ने धार के स्थान पर मांडु को अपनी राजधानी बनाया जिसने इसे पूर्ण कलात्मक ढंग से सुसज्जित कर दिया। गुजरात के शासक बहादुरशाह ने भी 1531 ई. में मांडु को जीता था। बाज बहादुर संगीत एवं कला का प्रेमी था तथा अपनी पत्नी रूपमती के साथ नृत्य-संगीत के सागर में हमेशा डूबा रहता था। यहां के हिंडोला महल, जहाज महल, रूपमती एवं बाज बहादुर के महल एवं अन्य प्रमुख स्थापत्य सुन्दर, सजीव एवं रोचक दृश्य प्रस्तुत करते हैं।
21. नवसारी: नवसारी अरब सागर में गुजरात तट पर स्थित था। मध्यकाल में यह स्थल व्यापारिक क्रियाकलापों के कारण विख्यात हुआ। यह आरंभ में एक निर्जन द्वीप था। इसे अरबी व्यापारियों ने आबाद किया, जो बाद में पुर्तगालियों के अधीन हो गया। जब मराठों ने सूरत की लूट की तो नवसारी पर शिवाजी का अधिकार हो गया। इस स्थल को लेकर जंजीरा के सिद्दियों एवं मराठों के बीच बहुत दिनों तक संघर्ष होता रहा। बाद में पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय इस पर मराठों का अधिकार हो गया।
22. ओरछा: यह मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बेतवा नदी के समीप स्थित है। यहां परिहारों एवं चंदेल वंश के शासकों ने शासन किया। ओरछा की स्थापना 1531 ई. में राजा रूद्रप्रताप ने की थी। भारतीचन्द ने 1539 में गढ़कुंडार के स्थान पर ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। यहीं परवीर सिंह बुन्देला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। बुन्देलखंड के स्थानीय ओरछा शासकों ने कला एवं साहित्य को भरपूर प्रोत्साहन दिया। वीर सिंह द्वारा निर्मित जहांगीर महल, केशवदेव भवन इत्यादि के अवशेष सुरक्षित हैं।
23. पण्ढरपुर: विठ्ठल या विठोबा मन्दिर के लिये प्रसिद्ध पश्चिमी भारत में स्थित पण्ढरपुर 13वीं शताब्दी में पाण्डुरंग या श्री विठ्ठल के सम्प्रदाय का केन्द्र बना। यह देवीमाता के पंच से संबंधित था। प्रारंभ में इसे विष्णु का रूप माना गया। यह दक्षिण में भक्ति आन्दोलन का एक केन्द्र बन गया जिसने नामदेव, जनोबई, सेन तथा नरहरि को आकृष्ट किया। इन्होंने मराठी में भजन लिखे और स्थानीय जनता को आकृष्ट किया। संत तूकाराम पण्ढरपुर के विठ्ठल स्वामी के बड़े भक्त थे। ज्ञानेश्वर वर्ष में दो बार पंढरपुर के विठोबा के पास आते थे। यह स्थानीय व्यापार का एक प्रसिद्ध केन्द्र भी था।
24. पानीपत: यह स्थान हरियाणा में स्थित है जो मुख्यतः तीन ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। 1526 ई में बाबर और अफगानी शासक एवं लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहीम लोदी के बीच प्रथम युद्ध हुआ था। इसी से बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। 1556 ई. में दूसरी बार अकबर और बैरम खां के बीच युद्ध हुआ जिसमें अकबर ने अफगानी चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर मुगल साम्राज्य को और सुदृढ़ किया। 1761 ई. में तीसरा युद्ध मराठों एवं अहमदशाह अब्दाली के बीच हुआ जिससे अहमदशाह अब्दाली ने हिन्दुस्तान के शासक बनने के मराठों के सपने को तोड़ दिया।
25. पाटन: सम्प्रति पाटन गुजरात राज्य के महसाणा जिले का नगर है। प्राचीन काल में इसे निहिलवाड़ या अनहिलपुर (अनहिलवाड़) कहा जाता था। माना जाता है कि इसकी स्थापना लगभग 746 ई. में रानी रूप सुन्दरी के पुत्र वनराज ने की थी जो चावड़ा वंश का प्रथम राजा था। मुहम्मद गोरी के आक्रमण (1178 ई.) के समय इसने अपनी मजबूती पेश की, भीमदेव द्वितीय ने उसे हराया। यहां के अन्तिम बघेला राजा कर्णघेलो को सन् 1298 में उलुग खान ने पराजित किया। आधुनिक पाटन उलुग के आक्रमणों से बने खण्डहरों की नींव पर बना जहां राजा भीम की रानी उदयमती का बनवाया हुआ कुआं निशान के तौर पर मौजूद है। हुमायूं और अकबर के मंत्री बैरम खां की हत्या यहीं पर हुई थी। यहां लगभग 110 जैन मन्दिर हैं।
26. कमरनगर: लैटिन भाषा के भूगोल ग्रंथ पेरिप्लस में दक्षिण भारत के काकंदी नगर को ही संभवतः कमर कहा गया है। यह ई. सन् की प्रारंभिक शताब्दियों में प्रसिद्ध बंदरगाह था। इस बंदरगाह को पुहार (मद्रास) के नाम से भी जाना जाता है। यह बंदरगाह चोल काल में विदेशी व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। माना जाता है कि इस बंदरगाह का निर्माण चोल सम्राट करिकाल ने श्रीलंका से लाए गये दासों के द्वारा बनवाया था।
27. रायचूर: यह कर्नाटक राज्य में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है जो उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध रहा है। रायचूर दुर्ग का निर्माण 1294 ई. में वारंगल राजा के मंत्री गंगायरूड्डी वारू ने करवाया था। बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच सामरिक महत्व के कारण संघर्ष का कारण बना रहा। हालांकि अधिकांश समय तक बहमनी सुल्तान का इस पर अधिकार रहा लेकिन 1520 ई. में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आदिलशाह को पराजित करके इस पर अधिकार कर लिया। अन्ततः मुगल शासक औरंगजेब ने इस पर अधिकार कर लिया।
28. सिरोही: वर्तमान राजस्थान में उदयपुर के पश्चिम में सिरोही एक मध्यकालीन स्थल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान शासकों को दिल्ली एवं अजमेर छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। इन चौहान शासकों ने अजमेर के और दक्षिण में बूंदी, कोटा और सिरोही राज्यों की स्थापना की। मुगलकाल में औरंगजेब ने सैनिक सहायता प्राप्त करने की गरज से मेवाड़ के राणा को सिरोही का राज्य दे दिया। ब्रिटिश काल में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1823 ई. में सिरोही के राज्य को ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करने संबंधी संधि करने को मजबूर कर दिया।
29. सोमनाथ: गुजरात में काठियावाड़ के प्रभासपट्टन नामक समुद्रतटीय क्षेत्र में स्थित है। यह शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। 1025-26 ई. में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। उस समय वहां का शासक भीमदेव प्रथम था। सोमनाथ मंदिर के आक्रमण में लगभग 50 हजार स्त्री-पुरुष मौत के घाट उतार दिये गये। उस समय इस मंदिर की गणना संसार की महान आचर्श्यजनक वस्तुओं में की जाती थी। कहा जाता है कि मंदिर की लूट से 20 लाख दीनार आक्रमणकारियों को प्राप्त हुआ जिसे महमूद गजनवी अपने साथ ले गया।
30. तिरहुत: गंगा के उत्तर में बिहार का यह क्षेत्र वर्तमान में मुजफ्रफरपुर और दरभंगा प्रमंडल के अन्तर्गत आता है। तिरहुत को मिथिला नाम से भी अभिहित किया जाता है। ग्यारहवीं सदी में कर्णाटवंशी शासक नान्यदेव ने इस राज्य की आधारशिला रखी। इसकी राजधानी सिमरांव थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तत्कालीन शासक हरीसिंह को हराकर इसे दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। हरीसिंह ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की और इसने नेपाल पर आक्रमण करके राजा जयरूद्र देव को हराया एवं वहां अपना शासन स्थापित किया। मुहम्मद बिन तुगलक के समय बार-बार के आक्रमणों एवं लूटपाट से तंग आकर उत्तर प्रदेश के बहुत-से ब्राह्मण मिथिला क्षेत्र में आ गये, जहां उन्होंने शांतिपूर्वक रहते हुए संस्कृत ग्रंथों की रचना की जिनमें कई पुराण उल्लेखनीय हैं। तिरहुत या मिथिला बंगाल जाने के रास्ते में पड़ता था अतः इसका सामरिक महत्व भी था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसे जीत कर इसका नया नाम तुगलकपुर रखा। इब्राहिम शाह शर्की ने यहां एक मस्जिद बनवाई। 1352 ई. में शम्सुद्दीन इलियास ने यहां के राजा से कर वसूल किया था। 1500 ई. में सिकन्दर शाह ने भी तिरहुत पर अधिकार कर यहां के राजा से कर वसूला था। 1519 ई. में यहां के राजा कंसनारायण को नसीब खां ने पराजित कर मार डाला।
Question : ‘मध्य युग में क्षेत्रीय भाषाओं एवं साहित्य के विकास’ पर टिप्पणी कीजिये। यह टिप्पणी लगभग 200 शब्दों में होनी चाहिए।
(1995)
Answer : आज हमारे देश में जिन भाषाओं के प्रयोग बहुतायत से हो रहे हैं उनमें से अधिकांश का जन्म मध्य युग में ही हुआ था। हिन्दी, बंगाली और मराठी भाषाओं की उत्पत्ति आठवीं शताब्दी में हुई थी। उर्दू का उद्भव एक मिश्रित भाषा के रूप में हुआ जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की के अलावा हरियाणवी, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली के अंश मिले हुए हैं। इसकी उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई। इन भाषाओं का विकास और साहित्यिक भाषाओं के रूप में उनका प्रयोग मध्यकाल की विशेषता है। इस समय संस्कृत का महत्व क्वचित कम हो चला था जबकि भक्त-कवियों द्वारा जन-भाषा के प्रयोग से इन क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में सहूलियत हुई। वस्तुतः देश के अनेक हिस्सों में संतों ने इन भाषाओं को साहित्यिक भाषा के रूप में ढ़ालने का काम किया था।
हिन्दी भाषा का विकास राजपूत शासनकाल से माना जाता है। इसका मूल खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी आदि बोलियों में देखा जा सकता है। इस भाषा के आरंभिक उदाहरण वीरगाथा काव्य के रूप में देखा जा सकता है, जैसे चन्दबरदायी की पृथ्वीराज रासो, जगनिक की अल्हाखण्ड, सारंगधर की हम्मीर रासो आदि। इसके अलावा अमीर खुसरो और सूफी सन्तों की रचनाओं में भी हिन्दी भाषा के आरंभिक उदाहरण देखे जा सकते हैं क्योंकि उर्दू एवं हिन्दी का मूल रूप एक ही था। हिन्दी को समृद्ध बनाने में भक्तिकाल के सन्त कवियों का उल्लेखनीय योगदान रहा। कबीरदास, सूरदास एवं भक्ति-रस के कवियों में जयदेव तथा विद्यापति का योगदान इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। मुगलकाल में अकबर के समकालीन रहे तुलसीदास द्वारा लिखित ‘रामचरित मानस’ हिन्दी के अवधी अपभ्रंश का उत्कृष्ट उदाहरण है। रहीम के दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। मध्य युग में मुगल सम्राटों तथा हिन्दू राजाओं ने आगरा तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को काफी प्रोत्साहित किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में जान फूंक दिया।
बंगला भाषा की उत्पत्ति गौड़ प्राकृत से मानी जाती है। तुर्क शासकों ने इसे संपन्न बनाने में अच्छा योगदान किया। बंगाल के नुसरत शाह ने ‘महाभारत’ और ‘रामायण’ का बंगाली भाषा में अनुवाद करवाया। भक्त संत चैतन्य के अनुयायियों ने बंगला में अनेक रचनाएं रचीं। मुगलकाल में अलाउल ने बंगला में रचना कर इसे सम्पÂ बनाने में योगदान दिया।
पंजाबी भाषा के विकास में सूफी संतों, विशेषकर संत फरीदुद्दीन गंज-ए-शकर अथवा बाबा फरीद ने उल्लेखनीय योगदान दिया। बुल्लेशाह व अन्य सूफी कवियों के अलावे सिख धर्म के प्रवर्त्तक गुरु नानकदेव ने विशेषकर पंजाबी भाषा को संपन्न बनाया। मुगलकाल में अन्य समकालीन सिख गुरुओं ने भी पंजाबी को समृद्ध करने में उल्लेखनीय योगदान किया।
मराठी के विकास में भक्त-संतों जैसे नामदेव एवं तूकाराम का विशेष योगदान रहा। बहमनी साम्राज्य में मराठी प्रशासन की एक भाषा रही और बाद में बीजापुर के दरबार की भाषा बनी। राजस्थानी भाषा के विकास में मीराबाई ने प्रभूत योगदान दिया। गुजराती भाषा के विकास में नरसी मेहता और संत वल्लभाचार्य के अनुयायियों का योगदान रहा। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में तेलुगू साहित्य पनपा। कन्नड़ और मलयालम में भी साहित्यिक परंपरा का आरंभ एवं प्रगति भी इस काल में द्रष्टव्य है। उर्दू का विकास बीजापुर एवं गोलकुंडा के शासनकाल में उल्लेखनीय रही।
इस प्रकार हम देखते है कि मध्य युग में बाहरी भाषाओं के हस्तक्षेप एवं प्रचलित अपभ्रंश की आन्तरिक शक्ति से नयी-नयी भाषाओं की उत्पत्ति हुई और जनसामान्य के लगाव एवं शासक वर्ग के सहयोग से इन भाषाओं ने जीवन्त साहित्य की एक लंबी दूरी तय की।
Question : अकबर से औरंगजेब काल पर्यन्त कुलीन वर्ग की संरचना में हुए परिवर्तन
(1995)
Answer : मुगलकाल में कुलीन वर्ग या अमीर वर्ग (छवइसम) में वे मनसबदार आतेे थे जो एक हजार या उससे अधिक मनसब के हकदार थे। मुगलिया प्रशासनिक व्यवस्था का प्रचलन राज्य के राजनीतिक और सैनिक दायित्वों का भली-भांति निर्वहन, सामाजिक मानकों का अनुरक्षण और यहां तब कि स्वयं मुगल साम्राज्य का अस्तित्व एक बड़ी सीमा तक संस्था के सुव्यवस्थित प्रचलन पर आधारित था। मुगल बादशाह इस दिशा में यथोचित रूप से सफल हुए कि वे कुलीन वर्ग के दिलों में एक समान उद्देश्य की भावना तथा शासक राजवंश के प्रति िनष्ठा की भावना भर सकें। यह भावना जब तक बनी रही और कुलीन वर्ग की संस्था पर पादशाह की जब तक अच्छी पकड़ रही, मुगल साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर रहा।
इस संस्था के कमजोर होते ही मुगल साम्राज्य पतन के गर्त्त में गिरने लगा।
सैद्धान्तिक रूप से मुगल कुलीन वर्ग के दरवाजे हर योग्य व्यक्ति के लिए खुले हुए थे पर वास्तव में उच्च घरानों को, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, विशेष सुविधा थी। अधिकतर मुगल कुलीन मुगलों के स्वदेश, तूरान तथा ताजिकिस्तान, खुरासान, ईरान आदि क्षेत्रों से आये थे। अकबर के समय से कुलीन वर्ग में हिन्दुओं की भर्ती भी होने लगी। इनमें सबसे बड़ा वर्ग राजपूतों का था और इन राजपूतों में कछवाहा सबसे अधिक थे। कुलीन वर्ग में शामिल किये गये राजपूत या तो वंशगत राजा थे या फिर किसी राजा से संबंधित उच्च खानदान के थे।
जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में कुलीन वर्ग में काफी स्थिरता आई। इन दोनों सम्राटों ने कुलीन वर्ग के संगठन (मनसबदारी व्यवस्था), पदोन्नति के नियमों, अनुशासन तथा राजकीय सेवा के योग्य व्यक्तियों की भर्ती की ओर काफी ध्यान दिया। इनके शासन काल में अधिकतर मनसबदार ऐसे थे जिनका जन्म भारत में ही हुआ था। अफगानों को कुलीन वर्ग में सम्मिलित किये जाने की बाबर के समय से चली आ रही कोशिश आखिरकार जहांगीर के समय फलीभूत हुआ। जहांगीर और शाहजहां के समय अफगानों, भारतीय मुसलमानों (हिन्दुस्तानियों) तथा हिन्दुओं का कुलीन वर्ग में अनुपात बढ़ता गया। जहांगीर पहला मुगल सम्राट था जिसने इस बात का अनुभव किया कि दक्कन के मामलों में मराठे बहुत महत्वपूर्ण थे और उसने उन्हें अपने पक्ष में जीतने की चेष्टा की। शाहजहां ने भी इस नीति को जारी रखा।
औरंगजेब ने भी मराठों और दक्कनी मुसलमानों को कुलीन वर्ग में अच्छा स्थान दिया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि शाहजहां के शासन काल में जहां हिन्दू मनसबदारों की संख्या 24 प्रतिशत थी वह औरंगजेब के शासनकाल में बढ़कर 33 प्रतिशत हो गयी। साथ में हिन्दू मनसबदारों की कुल संख्या डेढ़ गुनी से भी अधिक हो गयी। हिंदू मनसबदारों में आधी से अधिक संख्या मराठों की थी।
मुगलकालीन कुलीन वर्ग विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह बहुनस्ली और बहुधार्मिक समाज को एकीकृत बनाये रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा। औरंगजेब के काल तक आते-आते वाणिज्य-व्यापार में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी थी। कुलीन वर्ग के कमजोर पड़ते ही मुगल साम्राज्य का ढ़ांचा चरमराने लग गया।