Question : आपको दिये गये मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिये और उन पर ही संक्षिप्त टिप्पणियां लिखियेः 1. अखनूर, 2. अरिकमेडु, 3. बराबर, 4. बाघ, 5. भूमा, 6. बोधगया, 7. भगतराव, 8. चन्द्रकेतुगढ़, 9. धाम्नेर, 10. एलीफैंटा, 11. एरण, 12. गोप, 13. ग्यासपुर, 14. हड़प्पा 15. हरवान, 16. कार्ले, 17. मोहनजोदड़ो, 18. मार्तंड, 19. मास्की, 20. महेन्द्रगिरि, 21. मुखलिंगम, 22. नचना, 23. पिपरहवा, 24. राजिम, 25. संघोल, 26. शिशुपालगढ़, 27. सिरपुर, 28. सोंख, 29. सुतकागेन्डोर, 30. तिगवा
(1994)
Answer : 1. अखनूर: यह कश्मीर में स्थित है। आठवीं से दसवीं शताब्दी के बीच यह स्थल सामंती मुख्यालय एवं धार्मिक केन्द्र के रूप में विख्यात था। यहां मिट्टी की मूर्तियों का एक बहुत बड़ा भण्डार मिला है, जिसकी समीक्षा करने के बाद इतिहासकारों का मानना है, कि ये मूर्तियां सामंतवादी कला का अर्थात् समृद्ध वर्ग की कला का प्रतिनिधित्व करती हैं।
2. अरिकमेडुः वर्तमान समय में अरिकमेडु तमिलनाडु में कोरोमण्डल तट पर पाण्डिचेरी के निकट स्थित है। यह मौर्योत्तर युग में भारत-रोमन व्यापार का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख स्थल है। मौर्योत्तर युग में अरिकमेडु का व्यावसायिक-व्यापारिक महत्व था। यह मलाया-चीन-भारत व्यापारिक मार्ग से जुड़ा हुआ था। ‘पेरिप्लस’ में इसकी चर्चा है। अरिकमेडु के पुरातात्विक उत्खनन से जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, उनमें प्रमुख हैं- ईंटों से बना रंगाई हौज, रोमन बस्ती, रोमन बर्तन, कांच और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, मनके तथा बड़ा मालगोदाम। अवशेषों से पता चलता है कि यहां करघे पर वस्त्र-बुनाई का व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता था। मलमल जैसी महीन बुनाई के कपड़े भी यहां बनाए जाते थे। यहां से प्राचीन चोलों की मुद्राएं मिली हैं। रोमन शासक ऑगस्टस तथा टाइबेरियस के भी सिक्के मिले हैं।
3. बराबरः यह बिहार राज्य में गया जिले में स्थित है। बराबर की पहाडि़यों में सात गुफाएं हैं, जो गुफा कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से हैं। इन सात में से तीन को अशोक ने आजीविकों को दान कर दिया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी एक गुफा आजीविकों को दी थी। यहां की गुफाओं में से नागार्जुनी गुफा एवं सप्तपर्णी गुफा काफी उत्कृष्ट हैं। बराबर की पहाड़ी से प्राप्त एक अभिलेख में मौखरि शासक अनन्तिवर्मन का वर्णन है।
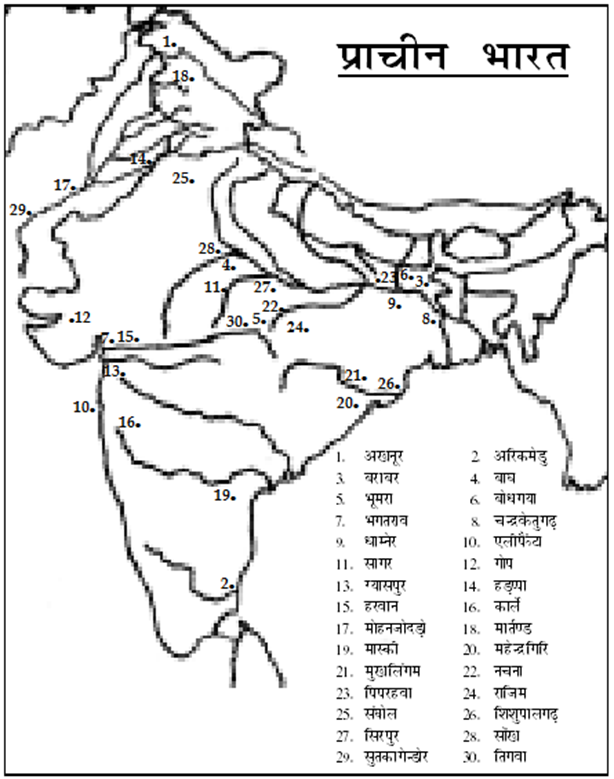
4. बाघः भूतपूर्व ग्वालियर राज्य में बाघ नदी के तट पर स्थित छोटा-सा गांव है, जिसके चारों ओर विन्ध्य पर्वतमाला फैली हुई है। इन्हीं पर्वतमालाओं पर गुप्तकालीन 9 गुफायें हैं। सन् 1818 में लेफ्रिटनेण्ट डेजफील्ड ने इनको खोजा था। बाघ की चौथी एवं पांचवीं गुफायें अपनी टेम्पेरा पेन्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं में लौकिक एवं धार्मिक दोनों विषयों पर नाना प्रकार के चित्र चित्रित हैं।
5. भूमा: यह स्थल मध्य प्रदेश के भूतपूर्व नागोड़ राज्य में, जबलपुर के पास स्थित है। यहां गुप्तकालीन शिव का मन्दिर प्राप्त हुआ है। नागर शैली में बना यह मन्दिर काफी उत्कृष्ट है। यहां से गुप्त काल के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं।
6. बोधगया: यह स्थान हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ गया (बिहार) से 7 मील दक्षिण की ओर स्थित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अशोक ने यहां पर बौद्ध मन्दिर का निर्माण करवाया था, जो ह्नेनसांग के समय तक विद्यमान था। इस मन्दिर के पास सात प्रसिद्ध बौद्धस्थल हैं, जहां बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद 7 रातें व्यतीत की थीं। इस मन्दिर की वेदिकाओं पर बौद्ध जातक कथाओं, यक्ष एवं यक्षिणियों, शाल-भञ्जिका नारियों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। बोधगया की कला में भरहुत की कला अपने संक्षिप्त रूप में पायी जाती है। यहां की आकृतियां सजीव एवं भावपूर्ण हैं।
7. भगतराव: यह स्थल गुजरात-महाराष्ट्र की सीमा के पास गुजरात में स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम हिस्से का सीमास्थल कहा जाता है। यह किम नदी के किनारे स्थित है।
8. चन्द्रकेतुगढ़: चन्द्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस स्थल की प्रसिद्धि यहां से प्राप्त उत्तरी काले रंगे पात्र (NBPW) मिलने के कारण है। इस तरह के पात्र अधिकतर उत्तरी हिस्सों में ही मिले हैं या मिलते हैं, अतः इनका चन्द्रकेतुगढ़ में पाया जाना एक उल्लेखनीय बात थी। यह स्थल मौर्योत्तर काल में काफी महत्वपूर्ण हो गया था।
9. धाम्नेरः बिहार राज्य के गया जिले में था, इस स्थल को बोधगया भी कहा जाता है। यहां एक बौद्ध स्तूप था जिसे शायद अशोक ने बनवाया था।
10. एलीफैंटाः मुम्बई से सात मील उत्तर-पूर्व में स्थित एक छोटे-से द्वीप अपोलोबन्दर से एलीफैण्टा की पहचान की गयी है। इसका प्राचीन नाम धारापुरी था। एलीफैण्टा की गुफाओं में 500-600 ई. में भगवान शंकर की लीलाओं का चित्रंकन किया गया है। उत्कीर्ण नटराज शिव से गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशिष्टता के संकेत मिलते हैं। यहां शक बौद्ध चैत्य के अवशेष भी मिले हैं। 1600 ई. में पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। यहां अवस्थित हाथी की मूर्ति के कारण पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र को एलीफैण्टा नाम दिया।
11. एरणः यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। मालवा की ताम्र-पाषाण संस्कृति से लेकर गुप्तकाल तक के ऐतिहासिक साक्ष्य यहां मिले हैं। समुद्रगुप्त के शिलालेख में यह एरिकण नाम से अंकित है।
एरण में ताम्र-पाषाण संस्कृति का परिपक्व विकास हुआ था, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, किन्तु असम्बद्ध थी। यहां से बड़ी संख्या में आहत सिक्के मिले हैं। एरण की व्यापारिक-आर्थिक श्रेणियों ने मुद्रा जारी की थी। एरण से बुद्धगुप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। सबसे प्रमुख 510 ई. का भानुगुप्त अभिलेख है, जिससे प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। एरण से जो वराहमूर्ति मिली है, उससे तोरमाण तथा हूणों के अधीन एरण के शासित होने के प्रमाण मिलते हैं। एरण से गुप्तकालीन मंदिर भी मिले हैं, यथा- नरसिंह मंदिर इत्यादि।
12. गोपः गोप गुजरात में स्थित है। यहां पांचवीं से सातवीं शताब्दी में उत्तर शैली में निर्मित विष्णु का मंदिर प्राप्त हुआ है, जो काफी उत्कृष्ट ढंग का है।
13. ग्यासपुरः ग्यासपुर आधुनिक महाराष्ट्र में ताम्रकालीन स्थल इमामगांव के पास स्थित था। यहां ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं।
14. हड़प्पाः हड़प्पा पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब में रावी नदी में सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। सैन्धव सभ्यता के क्षेत्र में सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा में ही हुआ था। सैन्धव सभ्यता का एक अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता का कारण भी यही है। हड़प्पा सैन्धव सभ्यता का एक विकसित नगर था। हड़प्पा से विशाल धान्यकोठार, लिंग-योनि तथा कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं। नगर-निर्माण योजना के समस्त लक्षण यहां के अवशेषों में मिले हैं। यहां से पकी मिट्टी से बनी स्त्रियों की मूर्त्तियां भी बड़ी संख्या में मिली हैं।
15. हरवान: हरवान महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। यहां से परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं।
16. कार्ले: कार्ले अथवा कार्ली पश्चिमी दक्कन में महाराष्ट्र में पुणे से 50 कि.मी. दूर उत्तर-पश्चिम में अवस्थित है। सातवाहन-युग में पश्चिमी दक्कन में ठोस चट्टानों को काटकर बौद्ध चैत्य एवं विहार के निर्माण की शिला वास्तुकला विकसित हुई थी, कार्ले की चर्चा उसी संदर्भ में होती है। कार्ले का चैत्य उस शिला वास्तुकला के विकास का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी शुरुआत दूसरी-पहली शताब्दी ई.पू. से भी मानी जाती है। यह लगभग 40 मीटर लम्बा और 15 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है। कार्ले का चैत्य कई स्तम्भों से युक्त एक विशाल कक्ष है। इसमें बाहर से सूर्य की रोशनी के आने की समुचित व्यवस्था है।
17. मोहनजोदड़ोः वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिन्ध प्रांत में सिन्धु नदी के किनारे स्थित है। यह सैन्धव सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो से ही पुजारी का सिर, एक कांस्य स्त्री मूर्ति, योगी की आकृतिवाली मुद्रा, विशाल स्नानागार तथा विशाल अन्न भण्डार के अवशेष मिले हैं। यहां की जल निकासी-प्रणाली उत्कृष्टतम है। मोहनजोदड़ो से ही बुने हुए सूती वस्त्र का एक टुकड़ा भी मिला है। यहां से मातृदेवी की मूर्ति भी मिली है।
18. मार्तण्डः यह स्थल कश्मीर में स्थित है। यहां कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा आठवीं-नौवीं शताब्दी में बनवाया गया सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर में कश्मीर की कला के सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। छत त्रिकोणीय बनी हुई है और लकड़ी से बनाई गयी है। छत पर रोशनदान बना हुआ है।
19. मास्कीः यह आंध्र प्रदेश राज्य में रायचूर जिले में तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी मास्की के समीप स्थित एक छोटा गांव है। यहां से ताम्र-पाषाण संस्कृति के ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। मास्की से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। मास्की के अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहीं से पता चलता है कि अभिलेखों में उत्कीर्ण देवनां प्रिय प्रियदर्शी मौर्य शासक अशोक ही है। इसी अभिलेख में देवानां प्रिय प्रियदस्सिन् राजा तथा असोकस दोनों ही पद अंकित हैं।
20. महेन्द्रगिरि: उडी़सा में स्थित है। यहां से अशोक के दो कलिंग लेख (12वें एवं 13वें लेख) मिले हैं। इन दो शिलालेखों में नव-विजित कलिंग राज्य के प्रशासन को चलाने के नियम लिखे गये थे। ये दो शिलालेख धौली और जौगढ़ में पाये गये हैं। सम्भवतः इनका निर्माण काल 250 ई.पू. है।
21. मुखलिंगमः इसकी पहचान उड़ीसा राज्य के गंजाम जिला में अवस्थित प्राचीन कलिगनगर से की गयी है। यहां उड़ीसा की प्राचीनतम राजधानी थी। 10वीं-11वीं सदी ई. में भी गंगवंशीय नरेशों में अनंतवर्मन चौड़गंग (1076-1147 ई.) सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इसी ने पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। मुखलिगम वंशधारा नदी के तट पर स्थित है। यह भी संभावना व्यक्त की गयी है कि मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तम्भ भी स्थापित किया था।
22. नचना: यह स्थल मध्य प्रदेश के भूतपूर्व अजयगढ़ राज्य में स्थित है। इसे नचना-कुठार के नाम से भी जाना जाता है। यहां से गुप्त काल में बनाया गया पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर मिला है, जो अपनी नागर शैली की खूबसूरती के लिए विख्यात है। यहां अन्य मंदिरों के अलावा महादेव का मंदिर भी मिला है।
23. पिपरहवाः नेपाल की सीमा पर पिपरहवा के खण्डरों में एक स्तूप मिला है, जो पत्थर के एक विशाल कक्ष के चारों ओर तथा उसके ऊपर ईंटों के एक ठोस गुम्बद के रूप में बनाया गया है। इस स्तूप में ईंटों की जुड़ाई बहुत ही श्रेष्ठ कोटि की है, ईंटें बहुत अच्छी तरह जमाकर लगाई गयी थीं। पत्थर का विशाल कक्ष इससे अच्छा नहीं बनाया जा सकता था। पुण्य अस्थियों के सम्मान में कई तरह के बहुमूल्य पत्थर रखे मिले हैं।
24. राजिमः जिला रायपुर, म.प्र. में अवस्थित है। यहां राजिम या राजीवलोचन भगवान रामचंद्र का प्राचीन मंदिर है, जो शायद 8 वीं या 9वीं सदी का है। यहां से प्राप्त दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस मंदिर के निर्माता राजा जगतपाल थे। इनमें से एक अभिलेख से विदित होता है कि इस मंदिर को मगध नरेश सूर्यवर्मा (8वीं शती ई.) की पुत्री तथा शिवगुप्त की माता ‘वासटा’ ने बनवाया था। मंदिर के स्तंभ पर चालुक्य नरेशों के समय में निर्मित नखराह की चतुर्भुज मूर्ति उल्लेखनीय है। वराह के वामहस्त पर भू-देवी अवस्थित है। शायद यह मध्य प्रदेश से प्राप्त प्राचीनतम मूर्ति है। राजिम से पांडुवंशीय कोसल नरेश तीवरदेव का ताम्रदानपट्ट प्राप्त हुआ था, जिसमें तीवरदेव द्वारा पैठामभुक्ति में स्थित पिपरिवद्रक ग्राम के निवासी किसी ब्राह्मण को दिये गये दान का वर्णन है।
25. संघोलः संघोल वर्तमान पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में स्थित है। यहां से उत्तर-हड़प्पा युग से मौर्योत्तर युग तक के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। संघोल एक उत्तर-हड़प्पा स्थल है। यहां से हिन्द-पहलवों, गोंदोफरनीज, विम कडफिसस सहित कुषाणों तथा अर्द्धजनजातीय लोगों से सम्बद्ध मुद्राएं मिली हैं। प्रतीत होता है कि संघोल में एक टकसाल था। संघोल मथुरा कला का एक केन्द्र भी था।
26. शिशुपालगढ़ः यह उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के निकट पुरी जिले में स्थित है। यहां से 300 ई.पू. से 300 ई. के मध्य की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। शिशुपालगढ़ से 3 मील दूर धौली स्थित है जहां से अशोक का अभिलेख मिला है जो कि उसके अभिलेखों में तोसाली के रूप में वर्णित है। शिशुपालगढ़ की पहचान खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी से की गयी है। यहां से कनिष्क, हुविष्क के सिक्के, रोम की वस्तुयें, हाथी दांत आदि मिले हैं।
27. सिरपुरः मध्य भारत में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर गुप्तकालीन नचना कुठार के महादेव तथा ग्वालियर के पठारी मंदिरों के अनुरूप ही नागर शैली का है। इसमें गर्भगृह, अंतराल तथा मंडप है। इसका गर्भगृह पंच रथ में नियोजित है, जो शिखर की ऊंचाई तक प्रकर्षित (उन्न्त) है। ईंटों से निर्मित यह मंदिर सामने की ओर त्रिकोणात्मक रूप से बना है।
28. सोंख: मथुरा जिले में सोंख नामक स्थान में कांसे का एक कुषाणकालीन फलक मिला है, जिसमें एक सिह शिरा मातृदेवी को एक देवता के साथ दिखाया गया है और जिसमें इस देवी ने अपनी बायीं गोद में एक शिशु को ले रखा है। यहीं से प्राप्त एक अन्य कुषाण कालीन मूर्ति में जो टूटी-फूटी अवस्था में मिली है, तीन देवियों का चित्रण किया गया है, जिनमें से दो वाराही और नारसिही मानी गयी हैं, क्योंकि उनमें से एक का चेहरा सूअर का है और दूसरे का सिह का। कितु इन्हें शक्तियां या वराह तथा नरसिह की पत्नियां मानने में बाधा यह है कि इसके पक्ष में इनमें और कोई पहचान नहीं मिली।
29. सुतकागेन्डोरः यह अरब सागर तट से 30 मील की दूरी पर मकरान तट पर स्थित है। यह सैन्धव सभ्यता का प्राकृतिक बंदरगाह नगर था। यह दाश्क नदी के मुहाने पर अवस्थित था। यह क्षेत्र फारस की खाड़ी से सम्बद्ध था। यहां तक विशाल दुर्ग और परकोटों से घिरा हुआ आवास-स्थल मिला है।
30. तिगवाः तिगवा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यहां एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें आर्य शैली के अनेक गुण दर्शित होते हैं। इस मन्दिर का निर्माण भी सम्भवतः गुप्तकाल में ही हुआ था। यहां एक ऊंचे टीले पर स्थित चौकोर गर्भगृह है, जिसमें शिवलिंग प्रतिष्ठित है। मन्दिर की छत चपटी है। बाहरी भाग में कलात्मक ढंग से बेलबूटों से सुसज्जित स्तम्भ बना है, जिसमें पूर्ण कलश के अतिरिक्त चार सिंह पीठ से पीठ लगाए बैठे हुए हैं।
Question : लगभग 750 ई. तक भारत में हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकासक्रम का निरूपण कीजिये।
(1994)
Answer : सिंधु घाटी की सभ्यता के काल से लेकर आठवीं सदी के मध्य तक भारत ने तकनीकी तथा विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में निरंतर अद्वितीय उन्नति की, जिसका आधार एक व्यवस्थित शिक्षा पद्धति थी। इससे प्रभावित होकर विभिन्न विदेशी भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भरत आते रहते थे। आधुनिक इतिहास के लेखक इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि वेद सभी प्रकार यहां तक कि विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के भी स्रोत हैं यद्यपि उनके विचार न्यायसंगत नहीं हैं, परन्तु यह स्वीकार किया जाता है कि वैदिक आर्य केवल संस्कृत साहित्य और धार्मिक दर्शन में ही ज्ञानवान नहीं थे, अपितु उन्हें चिकित्सा विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष आदि शिक्षा और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों का भी ज्ञान और अनुभव था।
यह कहना गलत होगा कि प्राचीन भारतीयों ने भौतिक संस्कृति में कोई प्रगति नहीं की। उन्होंने उत्पादन के कई क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त की। भारतीय शिल्पी रंगाई करने तथा अनेक प्रकार के रंग बनाने में परम दक्ष थे। उन लोगों द्वारा बनाये गये मूल रंग इतने चमकीले और पक्के होते थे कि ‘अजंता’ एवं ‘एलोरा’ के मोहक चित्रों में प्रयुक्त किये रंग आज भी ज्यों-के-त्यों हैं।
उस समय तक भारतीय, लौह धातु के उपयोग से भी पूर्णतया परिचित हो चुके थे। इस्पात बनाने की कला सबसे पहले भारत में ही विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसका उपयोग कृषि, उपयोगी यंत्रों और विभिन्न नवीन शस्त्रें के निर्माण के लिए किया। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने समय में दो नवीन आयुधों का निर्माण कराया था, जिसमें से एक ‘महाशिलाकन्टक’ था, जो दूर से शत्रुओं पर पत्थर फेंकने का कार्य करता था एवं दूसरा ‘रथमुसल’ था, जिसमें योद्धा की सुरक्षा के लिए रथ के पहियों और किनारों पर तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र लगे हुए थे, जिसके चलने पर शत्रुओं को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। भारतीय इस्पात का अन्य देशों में निर्यात ई.पू. चौथी सदी से होने लगा और बाद में आकर यह ‘उट्ज’ कहलाने लगा। विश्व का कोई अन्य देश इस्पात की वैसी तलवारें नहीं बना सकता था, जैसी भारतीय शिल्पी बनाते थे। पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक में इन तलवारों की भारी मांग थी। जिसका अर्थ यह था कि भारतीयों ने उस काल में धातुविज्ञान में पर्याप्त उन्नति करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस काल में भारतीय उत्तर-पश्चिम दिशा में ईरानी और ग्रीक निवासियों के संपर्क में आये, जिसके फलस्वरूप उन्होंने नक्षत्र विज्ञान और सिक्के बनाने की कला के साथ ही साथ एक नवीन लिपि, खरोष्ठी का विकास किया।
प्राचीन भारत में विज्ञान ने काफी उन्नति कर ली थी।प्राचीन काल में धर्म और विज्ञान आपस में बंधे हुए थे, जिसके चलते धर्म के साथ-ही-साथ विज्ञान की भी अत्यधिक उन्नति हुई। ई.पू. तीसरी सदी में आकर गणित, खगोल विद्या और आयुर्विज्ञान तीनों का विकास अलग-अलग आरंभ हुआ। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने तीन विशिष्ट योगदान-अंकनपद्धति, दाशमिक पद्धति और शून्य के प्रयोग की शुरुआत की। दाशमिक पद्धति के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ई. की 5वीं सदी के आरंभ का है। भारतीय अंकनपद्धति को अरबों ने अपनाया और उसको पश्चिमी दूनिया में फैलाया। ‘अरेबिक न्यूमरल्स’, जिसे अरबी ‘हिन्दसा’ के नाम से जानते हैं, का पश्चिम में प्रचार होने के सदियों पहले भारत में प्रयोग हुआ, जो क्रमशः अशोक के शिलालेखों में पाया जाता है एवं जो ई. पूर्व तीसरी सदी में लिखा गया।
दाशमिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया क्योंकि सिंधु घाटी के अवशेषों में से 16-8 सेंटीमीटर लंबी और 9 स्पष्ट भागों में विभाजित नापने हेतु प्रयोग में आने वाली एक ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है जो संकेत देती है कि वे सम्भवतः नापने के साधनों को जानते थे और दशमलव प्रणाली के प्रयोग से परिचित थे। दाशमिक पद्धति को चीनियों ने बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखा और पश्चिमी जगत ने अरबों से। ई. पूर्व दूसरी सदी में भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप गणितज्ञ इसको एक पृथक् अंक समझने लगे और इसका प्रयोग अंकगणना में करने लगे। ई. पूर्व पांचवीं सदी के आसपास के शुल्व सूत्रों से ज्ञात होता है कि पश्चिमोत्तर भारत के लोगों में मापन और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था। ई. पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आपस्तम्ब ने एक व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की थी, जिसमें न्यूनकोण, अधिककोण और समकोण का वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके चलते त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। ‘सूर्य सिद्धांत’प्राचीन काल की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। आर्यभट्ट ने बेबिलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की। उन्होंने चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के कारणों का पता लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला जो आज भी शुद्ध माना जाता है। वे ही पहले भारतीय थे, जिन्होंने यह पता लगाया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ‘आर्यभट्टीय’ नामक पुस्तक की रचना की।
ई. की छठीं सदी में वराहमिहिर ने सुविख्यात कृति वृहत्संहिता की रचना की। उन्होंने बताया कि चन्द्र पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय शिल्पियों ने रसायन विद्या की प्रगति में बहुत योगदान दिया। भारतीय रंगरेजों ने टिकाऊ रंगों का विकास किया और ‘नील’ का आविष्कार किया।
प्राचीन भारत के वैद्यों को शरीर रचना का ज्ञान था। उन्होंने रोगों के निदान की विधियां विकसित कीं और इलाज के लिए दवा बनाई। ई. की दूसरी सदी में भारत में आयुर्वेद के दो महान विद्वान उत्पन्न हुए- सुश्रुत और चरक। अपनी सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिन्द, पथरी तथा और कई रोगों का शल्योपचार बताया। उन्होंने शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। ‘चरक संहिता’ भारतीय चिकित्साशास्त्र का विश्वकोश है, इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिरगी और यक्ष्मा के अनेक भेदोपभेदों का वर्णन है। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़-पौधों का वर्णन है, जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है। इस प्रकार यह पुस्तक भारतीय आयुर्विज्ञान के अध्ययन के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के वनस्पति और रसायन के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्राचीन भारत से लेकर 750 ई. तक ही नहीं, अपितु उसके पश्चात् भी भारतीयों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी सम्भव प्रयत्न किये थे। यह प्रयत्न केवल धर्मिक शिक्षा तक ही सीमित न था बल्कि विज्ञान तकनीक, ललितकला, चिकित्सा, गणित आदि सभी क्षेत्रों में प्रदान की जाती थी। यदि ऐसा न होता तो भारतीय, जीवन के सभी क्षेत्रों में इतनी उन्नति न कर पाते जो उन्होंने प्राप्त की थी।
Question : भू-प्रदेश के वैदिक देव।
(1993)
Answer : भू-प्रदेश के वैदिक देवों में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां आते हैं। वैदिक देवों का यह वर्गीकरण प्राकृतिक आधार पर आधारित है। देवता प्रकृति के जिस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी रूप में उन्हें वर्णित किया गया है। वैसे त्वस्त्रि (या त्वस्त) और पृथ्वी को तीनों वर्गों (भू, वायु एवं द्वि आकाशीय) में रख दिया गया है। अग्नि और उषस् को पृथ्वी स्थान एवं वायु स्थान, दोनों में रखा गया है। पृथ्वी को देवताओं की श्रेणी में रख वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वैदिक देवों में इन्द्र एवं वरुण के बाद अग्नि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में अग्नि से सम्बन्धित 200 स्तुतियां हैं, इसे अग्नि आहुति करने वाले पुरोहितों को देवता, घर के चूल्हे में निवास, भगवान और व्यक्ति के बीच मध्यस्थ, जो भगवान तक व्यक्ति की आहुति ले जाता है, जो स्वर्ग में बिजली के रूप में और पृथ्वी पर तितली में रहता है और जिसे रहस्यवाद एवं चिन्तन की मुख्य वस्तु माना गया है। ऋग्वेद के नवें ग्रंथ में सोम को एक अद्वितीय पौधा (भांग), जिससे पवित्र पेय बनता था और ब्राह्मणों का संरक्षक एवं कई बार देवताओं का राजा कहा गया है। ऋग्वेद के दसवें ग्रंथ की नदी- स्तुति खंड में गोमती (आधुनिक गोमल), क्रुमु (आधुनिक कुर्रम), कुभा (आधुनिक काबुल), सुवास्तु (आधुनिक स्वात), सिन्धु (इन्डस), शतुद्रि (सतलज), विपासा (व्यास), परूष्णी (रावी), असिक्नी (चेनाब), वितस्ता (झेलम), सरस्वती (सरसुती) एवं दृषद्वति (घग्गर) का उल्लेख है। इसमें से सरस्वती सर्वाधिक पवित्र एवं सिन्धु दूसरी प्रशंसित नदी थी।
Question : मौर्य स्तम्भों और अखमानी लाटों में समानतायें और अंतर।
(1993)
Answer : सर जॉन मार्शल ने लिखा है कि अशोक के स्तम्भों पर अखमानी लाटों का प्रभाव था, क्योंकि अशोक के राज्यकाल में ईरान से बुलाए गये कलाकारों द्वारा भारतीय कलाकारों का प्रशिक्षण हुआ। हैवेल इस मत को अस्वीकार करते हैं। अशोक के स्तम्भों पर घण्टी के आकार का ईरानी शीर्ष दिखाई देता है। यह शीर्ष भारतीय कला की वस्तुओं पर साधारणतः पाया जाता है। इसलिए इस आकार को ईरानी कला की घण्टी का आकार समझना गलत है। स्तम्भ पर यह आकार फूल का संकेत है न कि घण्टी का। यह भगवान विष्णु सम्बन्धी आकाश का नील-कमल है। कमल सम्बन्धी सांकेतिकता भारतीय विशेषता है, ईरानी नहीं। इसके अतिरिक्त अखमानी स्तम्भ किसी बड़े भवन आदि के अंग हैं, परन्तु अशोक के स्तम्भ पूर्णतः स्मरणीय हैं। अशोक के स्तम्भ उन राजसी ध्वजों या जातीय पताकाओं के प्रतिरूप हैं, जिन्हें वैदिक संस्कार करने के स्थान को सीमाबद्ध करने के लिए लगाया जाता था। मौर्य स्तम्भ पूर्णतः गोलाकार हैं जब कि ईरान के स्तम्भों में कंगूरे हैं। मौर्य स्तम्भ एक चट्टान से काटकर बनाया गया है, जबकि ईरान का स्तम्भ बहुत-से पत्थरो को जोड़कर बनाया गया है। मौर्य स्तम्भ एक बढ़ई का बनाया हुआ प्रतीत होता है, जबकि ईरानी (अखमानी) स्तम्भ राज का बनाया हुआ। मौर्य स्तम्भ में कोई आधार नहीं है किन्तु ईरानी स्तम्भ की आधारशिला उल्टे कमल के फूल के समान है। मौर्य स्तम्भ में ईरानी और यूनानी कला का अनुकरण अवश्य दिखाई देता है परन्तु उसमें भारतीय कला की देन भी बहुत स्पष्ट है।
Question : मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के निर्धारण के लिये अशोक के तेरहवें शिलालेख के महत्व का परीक्षण कीजिये। क्या अशोक की नीतियों और सुधारों ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया?
(1993)
Answer : मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के निर्धारण के लिऐ अशोक के तेरहवें शिलालेख का महत्वपूर्ण योगदान है। तेरहवें शिलालेख में उत्कीर्णित हैं कि, "अपने शासन के नवें वर्ष में कलिंग को जीता, जिसमें एक लाख लोग मारे गये और इससे भी अधिक घायल हुएतथा डेढ़ लाख लोग निर्वासित हो गये, यह जब देखकर देवनांप्रिय को पश्चाताप हुआ। जंगली जनजाति ठीक से रहें वरना मारे जाएंगे। ‘धम्मविजय’ ही सर्वोत्तम विजय है जिसे उसने सीरिया के एंटीकुश प्प् थियोस, मिस्र के टोलमी प्प् फिलाडेलफियस, सिरिन के मॅगास, मेसोडोनिया के एंटीगोनस, एपिरस के एलेक्जेन्डर, चोलों, पाण्ड्यों, सिलोन, कम्बोजों, नाभकों, नाभापंकित्सों, भोजों, पितिन्कों, आंध्रों, केरलपुत्रों, सत्यपुत्रों एवं पिरिंडों के क्षेत्रों में प्राप्त किया था। उत्तराधिकारियों को चाहिए कि वे अब भविष्य में विजय के लिए न सोचें।" इस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में सैनिक विजय नहीं वस्तुतः धम्मविजय प्राप्त की थी और यह सभी उसकी राज्य सीमा से बाहर थे। लेकिन इस शिलालेख के आधार पर मौर्य साम्राज्य की सीमा निर्धारण थोड़ी कठिन हो सकती है इसलिए जिन-जिन क्षेत्रों से अशोक के शिलालेख या स्तम्भ मिले हैं इतिहासकारों ने उनको उसके राज्य के अंतर्गत मानते हुए सीमा निर्धारण किया है। इस आधार पर अशोक के राज्य की सीमा उत्तर-पश्चिम में कांधार तक, जहां गांधार, कम्बोज एवं योन उसकी सीमा पर थे। दक्षिण में अशोक के सुदूर दक्षिण में प्राप्त अभिलेख रायचूर जिला से मिले हैं अतः चोल, पाण्डय, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्रों का राज्य उसकी सीमा से बाहर था। दक्षिण सीमा का स्पष्टतः उल्लेख नहीं हो पाता है। पेन्नार नदी की घाटी शायद एक प्राकृतिक सीमा हो दक्षिणावर्ती सीमा के पूर्वी भाग में। पूर्व में साम्राज्य का विस्तार गंगा के डेल्टा तक था और तामुलक साम्राज्य के अंतर्गत था।
इतिहासकारों में अब तक यह विवाद का विषय बना हुआ है कि क्या अशोक की नीतियां मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का विचार है कि मौर्य वंश के प्रति ब्राह्मणों के विद्रोह ने ही मौर्यवंश को जड़ से उखाड़ फेंका। लेखक मौर्यवंश के पतन का कारण अशोक के उन शिलालेखों को समझता है, जिनमें पशुवध को वर्जित ठहराया गया है। ब्राह्मणों के लिए यह विशेष रूप से आपत्तिजनक बात थी कि वे शिलालेख एक शूद्र राजा अशोक द्वारा लगाये गये थे। यह भी कहा गया है कि अशोक द्वारा महामात्रों की नियुक्ति भी ब्राह्मण वर्ग पर एक कड़ी चोट थी। यह कार्य ब्राह्मणों को सौंपा जाना चाहिए था, किन्तु अशोक ने ऐसा नहीं किया। ‘दण्ड-समंत’ और ‘व्यवहार-समत’ के सिद्धान्तों को अपने कर्मचारियों द्वारा बलपूर्वक लागू करना भी अपने आप में एक कारण हो सकता है।
इसका अर्थ यह है कि सभी से समान व्यवहार किया जाए और सभी को समान दण्ड दिया जाए। इन सिद्धान्तों के अनुसार जाति, रंग और वंश की चिन्ता नहीं की जाती थी। इससे ब्राह्मण विक्षुब्ध हो उठे, क्योंकि वे अनेक विशेषाधिकारों का, जिनमें मृत्युदण्ड से मुक्ति भी सम्मिलित थी, दावा करते थे। डॉ- रायचौधरी जैसे विद्वानों ने इस मत का खंडन किया है। उनका विचार है कि अशोक द्वारा पशु बलि को वर्जित घोषित करने का अर्थ यह कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि अशोक की यह क्रिया ब्राह्मणों पर सीधा आक्रमण था। मौर्यों को शूद्र कह कर तो पण्डित शास्त्री ने भारी गलती की है। विशेष बात यह है कि इस बात का प्रमाण भी तो नहीं मिलता कि अशोक द्वारा नियुक्त धर्म-महामात्रों को ब्राह्मण वर्ग में से नहीं चुना जाता था या ब्राह्मणों को धर्म महामात्र बनने की मनाही थी। अशोक द्वारा लगाए गये ‘समत’ सिद्धान्त ने रज्जुकों की शक्ति को तो सीमित किया किन्तु ब्राह्मणों के दण्ड से मुक्ति पाने के विशेषाधिकार को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई। अशोक ने तो अपने शिलालेखों में से एक शिलालेख में ब्राह्मणों के प्रति उदार भाव दर्शाया है। एक अन्य शिलालेख में अशोक ने घोषित किया है कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार एक अन्य शिलालेख में लिखा है कि धर्म महामात्रों का धर्म है कि वे ब्राह्मणों के सुख-दुःख की चिन्ता करें। अशोक के उत्तराधिकारी और ब्राह्मणों के बीच किसी प्रकार का मन-मुटाव रहा होगा, इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता। अशोक ने पशु-बलि पर पूर्ण अंकूश भी नहीं लगाया था।
इस दिशा में प्रो- नीलकंठ शास्त्री ने रायचौधरी की धारणा का समर्थन किया है। डॉ- शास्त्री ने इस विचार की भी आलोचना की है कि अशोक की बौद्धधर्म-पक्षी और उसके उत्तराधिकारी की जैनधर्म-पक्षी नीति के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी। इस बात का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है कि विश्व-बन्धुत्व और विभिन्न धर्मों की पारस्परिक मित्रता को बढ़ावा देने वाला अशोक तनिक भी ब्राह्मणों के विरुद्ध था।
हेमचन्द्र रायचौधरी का मत है कि अशोक की शान्तिवादी नीतियां ही साम्राज्य की शक्ति को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी थीं। उनका कहना है फ्बिम्बिसार के शासनकाल से लेकर कलिंग युद्ध तक का भारत का इतिहास दक्षिण बिहार में मगध के एक छोटे से राज्य का हिन्दुकूश गिरिपाद से लेकर तमिल प्रदेश की सीमाओं तक फैले हुए एक वृहतकाय साम्राज्य के विस्तार की कहानी है।" कलिंग युद्ध के बाद गतिहीनता के उस युग का जन्म हुआ, जिसके अन्तिम चरण में सम्पूर्ण प्रक्रिया ही परिवर्तित हो गयी। साम्राज्य का विस्तार धीरे-धीरे पतनोन्मुख होकर उस स्थिति में पहुंच गया जहां से बिम्बिसार और उसके उत्तराधिकारियों ने इसका उत्थान किया था। तथापि, रायचौधरी का विचार तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद भी अशोक पूर्णरूपेण शान्तिवादी नहीं बन पाया था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि उसने न तो मौर्य सेवा का सैन्य-वियोजन किया और न ही प्राणदण्ड को समाप्त किया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात् केवल अपनी साम्राज्यवादी नीति का ही परित्याग किया था और अहिंसा का प्रचार किया था। ऐसा व्यावहारिक शान्तिवाद मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता था।
अतः यह कहना कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक की नीतियां थी, गलत होगा। होे सकता है ये नीतियां साम्राज्य के पतन के कई कारणों में से एक हों। पर महत्वपूर्ण नहीं है। डी-डी- कौशाम्बी के अनुसार परवर्ती मौर्य राजाओं के अधीन मौर्य अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव बढ़ना, डॉ- रोमिला थापर के अनुसार परवर्ती कमजोर मौर्य शासकों द्वारा अत्यधिक केन्द्रीभूत प्रशासन को नहीं सम्हाल पाना, एवं राष्ट्रीय एकता का अभाव मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं।
Question : मौर्योत्तर काल में संस्कृत में लिखी बौद्ध रचनायें।
(1993)
Answer : महायान सम्प्रदाय के उदय के बाद महायानियों ने संस्कृत को अपने अनेक ग्रन्थों की भाषा बनाया। हीनयानियों (थेरवादियों) ने भी संस्कृत में अपने कुछ ग्रन्थ लिखे। परन्तु संस्कृत में लिखित अधिकांश बौद्ध धर्मग्रन्थ महायान संप्रदाय से सम्बन्धित हैं। महायान सूत्रों में वैपुल्यू सूत्रों के रूप में प्रसिद्ध कुछ धर्मग्रन्थ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं: (1) अष्ट सहस्त्रिका-प्रज्ञा पारमिता, (2) सधर्म पुण्डरीक, (3) ललित विस्तार, (4) सुवर्ण प्रभास, (5) गौड़व्यूह, (6) तथागत गुहगक, (7) सम्माधिराज, एवं (8) दशभूमिस्वर।
कनिष्क के समकालीन अश्वघोष ने भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रन्थ ‘बुद्ध चरित’ की एक महाकाव्य के रूप में रचना की। गुप्त काल में असंग ने योगाचार भूमिशास्त्र, प्रकरण आर्यवाचा, महायान सूत्रलंकार, वज्रघेटिका टीका, महायान सम्परिग्रह और महायानभिधर्म संगीत शास्त्र आदि ग्रंथ लिखे। वह महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। वसुबंधु ने हीनयान और महायान दर्शन पर अनेक ग्रंथ लिखे। अभिधर्मकोष में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। दिघ्नाग ने बौद्ध तर्कशास्त्र पर ग्रंथ लिखा। बुद्धघोष ने त्रिपिटकों पर अनेक भाष्य लिखे। विसुद्धिमग्ग उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अश्वघोष द्वारा लिखित सौन्दर्यानन्द भी बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित है। अश्वघोष के ही समय नागार्जुन ने प्रज्ञापारामिता-सूत्रशास्त्र लिखा। वसुमित्र ने महाविभाग शास्त्र लिखा। अश्वघोष सारिपुत्रप्रकरण का भी लेखक था।
Question : कलिंग के खारवेल के सैनिक क्रियाकलापों की विवेचना कीजिये। क्या आप यह सोचते हैं कि उसका राज्यकाल केवल सैनिक अभियानों के लिए ही महत्वपूर्ण है?
(1993)
Answer : खारवेल शुंगों (दूसरी-पहली शताब्दी ईसा-पूर्व) का समकालीन था एवं सौभाग्यवश हाथीगुंफा शिलालेखों (उड़ीसा में) से उसके विषय में बहुत कुछ ज्ञात होता है। के-पी- जायसवाल और आर-डी- बनर्जी ने इस शिलालेख को सुयोग्यता से सम्पादित किया है। वह कलिंग के तीसरे राजवंश से था और उसके वंश का नाम चेत (या चैत्र) था अपने शासन के दूसरे वर्ष में शातकर्णो की अवहेलना करते हुए उसने पश्चिम की ओर एक बड़ी सेना भेजी। उसने कशप (कश्यप) क्षत्रियों की सहायतार्थ भूषिकों की राजधानी को नष्ट कर दिया। आठवें वर्ष में उसने मगध पर आक्रमण किया और गया से पाटलिपुत्र के पुराने मार्ग पर बढ़ते हुए बराबर की पहाडि़यों (गोरथ-गिरि) तक बढ़ गया। किन्तु राजगृह के विरोधी राजा ने युद्ध नहीं किया और वह मथुरा तक पीछे हट गया। खारवेल ने आगे न बढ़ने में ही बुद्धिमता समझी। अपने शासन के दसवें वर्ष में उसने भारत वर्ष अथवा उत्तरी भारत के विरुद्ध अपनी सेनाएं भेजीं। इस वर्ष की अन्य घटनाऐं शिलालेख से मिट गयी हैं।
अपने शासन के 12वें वर्ष में खारवेल ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं (उत्तरापथ) पर आक्रमण किया। उसी वर्ष उसने मगध के लोगों को चिन्तित कर दिया और उनके राजा को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वह उससे भेंट करे। वह अंग और मगध के बहुमूल्य उपहारों तथा कलिंग की कुछ पैतृक सम्पत्ति तथा प्रथम जिन की एक प्रतिमा तथा पद-चिन्ह, जिसको राजा नन्द उठाकर ले गया था, अपने साथ लेकर कलिंग वापस लौटा। देश में उसने स्तम्भ बनवाए जिनके अन्दर अत्यन्त सुन्दर नक्काशी का काम देखने को मिलता है। उनके अन्दर उसने उपहार तथा भेंटें रखवाईं। उसी वर्ष उसने पाण्ड्य राजा से बड़े-बड़े हाथी-जहाज छीने या बलपूर्वक भेंट में लिये। इसके अतिरिक्त उसने हीरे, जवाहरात, हाथी, घोड़े तथा अन्य उपहार भी प्राप्त किये। इस समय तक वह अपने राज्य-विस्तार से सन्तुष्ट हो चुका था। अतः राज्य काल के तेरहवें वर्ष में उसका मन धर्म की ओर झुका। कुमारी पर्वत (उदयगिरि) पर उसने अर्हत देवालय के निर्माण की व्यवस्था की।
हालांकि यह सत्य है कि खारवेल का शासनकाल उसके महत्वपूर्ण सैनिक विजयों के कारण बेहद उल्लेखनीय हैं, लेकिन मात्र सैनिक विजय ही खारवेल का स्थान भारतीय इतिहास में निश्चित नहीं करते हैं, कलिंग क्षेत्र में खारवेल द्वारा जैन धर्म को समर्थन दिया गया। उसके कारण जैन धर्म के इतिहास में खारवेल का नाम अमिट हो गया। उदयगिरि पर्वत पर हाथीगुंफा अभिलेख एवं पत्थर का बना मन्दिर खारवेल को भारतीय कला के इतिहास में भी अमर बना देती है। ‘भिक्षु-सम्राट’ और ‘धर्मराज’ के रूप में वर्णित खारवेल ने अपना जीवन कल्याण के कार्यों में बिताया।
अपने राज्य के प्रथम वर्ष में उसने कलिंग के तूफान से क्षतिग्रस्त प्राचीरों, द्वारों और भवनों को ठीक करवाया। उसने सरोवर तथा बाग बनवाए। उसने अपनी 3,500,000 प्रजा को प्रसन्न रखा। अपने राज्य के तीसरे वर्ष में ‘गन्धर्व-वेद’ या संगीत-शास्त्र में निपुण खारवेल ने नृत्य, नाटक और अन्य उत्सव किये। पांचवें वर्ष में वह तनाशुल्य पथ से तीन सौ वर्ष पूर्व सम्राट नन्द की खोदी हुई नहर को अपनी राजधानी में लाया। छठे वर्ष में उसने ‘पौर’ तथा ‘जनपद’ परिषदों को कुछ सुविधाएं दीं। नौवें वर्ष में उसने ब्राह्मणों को बहुत से दान एवं उपहार दिये। इसी वर्ष खारवेल ने भुवनेश्वर के निकट प्राची नदी के दोनों तटों पर 35 लाख की रजत मुद्राओं की लागत का एक महल बनवाया, जिसका नाम उसने ‘विजय-प्रसाद’ रखा। उसने ग्यारहवें वर्ष में 13 सौ वर्ष पुरानी केतुभद्र की लकड़ी की प्रतिमा का जूलूस निकाला। इस तरह खारवेल को उसकी सैनिक विजयों के साथ-साथ उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं लोककल्याणकारी कार्यों के लिए भी महत्व दिया जाता है।
Question : सैन्धव सभ्यता की शवाधान रीतियां।
(1993)
Answer : सैन्धव सभ्यता की शवाधान रीतियां उसकी धार्मिक रीतियों की ही तरह विभिन्नता लिए हुए थीं। मॉर्टिमर व्हीलर द्वारा हड़प्पा में 67 समाधियों (कब्रों) से युक्त एक समाधि स्थान की खोज की गयी थी, जिससे प्रतीत होता है कि शवाधान या दफनाना अन्तिम संस्कार की सामान्य प्रथा थी। मोहनजोदड़ो से शवाधान के तीन प्रमुख रूप देखने को मिलते हैं अर्थात् पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और शव के दाह-संस्कार के बाद अस्थि अवशेषों
का शवाधान। पूर्ण शवाधान से तात्पर्य है पूरे शव को विभिन्न अनुष्ठानों सहित मृतक की सज्जा-सामग्री और अर्पण-योग्य वस्तुओं के साथ दफनाना।
आंशिक शवाधान में मृतक शरीर को वन्य पशुओं और पक्षियों द्वारा खाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था, तदुपरान्त बची हुई अस्थियों को दफना दिया जाता था, इस तरह के पांच शवाधान पाये गये हैं। दाह संस्कार के उपरान्त की गयी शवाधान क्रिया में चौड़े मुंह वाले अस्थि-कलशों के अंदर अनेक छोटे-छोटे पात्र, मेमने, बकरी आदि जैसे पशुओं, पक्षियों या मछलियों की हड्डियों के साथ चूडि़यां, मनके, छोटी मूर्त्तियां जैसी छोटी-छोटी वस्तुएं कोयले और राख के साथ मिली हुई प्राप्त होती हैं। हड़प्पा से एक कब्र में ताबूत में कफन से लिपटे शव के प्रमाण मिले। कालीबंगा से अंडाकार या आयताकार कब्रों में अस्थियों के साथ पात्रों या पात्रों में अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। लोथल के एक कब्र से युगल शवाधान का प्रमाण मिलता है।
Question : "शिलालेखों एवं सिक्कों की सहायता के बिना पूर्वकालीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण मुश्किल से ही संभव है।" चर्चा कीजिए।
(2007)
Answer : प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे पास विविध प्रकार के स्रोत हैं। स्थूल रूप से, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को दो मुख्य स्रोतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली साहित्यिक और दूसरी पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत और अन्य साहित्य को तथा इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे वृतांतों को शामिल किया जा सकता है। पुरात्व के स्थूल शीर्ष के अन्तर्गत हम पुरालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, पुरातात्विक अन्वेषणों तथा उत्खननों पर विचार कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, भारत के इतिहास से संबंधित प्राचीन भारतीय साहित्य की विश्वसनीयता के बारे में बहुत वाद-विवाद रहा है। यह मत प्रकट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसे जिस साहित्य के इतिहास होने के दावा किया जाता है, उनमें घटनाओं एवं राजाओं की कोई निश्चित तिथियां नहीं दी गई हैं, इसके कारण कालक्रम के अनुसार ऐतिहासिक विन्यास करना कठिन है। समान रूप से बौद्ध एवं जैन साहित्य द्वारा अपने सिद्धान्तों का औचित्य सिद्ध करने के लिए तथ्यों को विरूपित करके प्रस्तुत किया गया है। विदेशियों द्वारा लिखे गए वृतांत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों एवं धारणाओं के कारण निश्चित रूप से इसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। लौकिक साहित्य की समस्या ये है कि इसमें तथ्यों को कई बार ईमानदारी से प्रस्तुत नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, बाणभट्ट द्वारा हर्षवर्धन के काल का वर्णन अतिश्योक्तिपूर्ण है। पुरातत्वीय स्रोतों में स्थापत्य अवशेषों तथा उत्खननों के संदर्भ में अभी और खोज एवं विश्लेषण की आवश्यकता है।
उपरोक्त परिस्थितियों में प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अभिलेखशास्त्र एवं मुद्राशास्त्र जैसी शाखाओं से अत्यंत लाभांवित हुई है, जिसके बिना भारत के अतीत के बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित होता। मुद्राशास्त्रीय स्रोतों के बिना हमें अधिकतर भारतीय-यूनानी, शक-पार्थियन और कुषाण राजाओं के बारे में अशोक के विचार एवं समुद्रगुप्त तथा अन्य राजाओं की विजय गाथाओं के विवरण, उनके शिलालेखों के बिना अक्षात बने रहते।
शिलालेखः इतिहास लेखन का एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत शिलालेख हैं। चूंकि उत्कीर्ण लेख एक समकालीन अभिलेख होता है, इसलिए यह क्षेपकों से मुक्त होता है। यह उसी रूप में उपलब्ध होता है जिस रूप में उसकी रचना की गई थी। बाद की अवस्था में इसमें कुछ जोड़ना लगभग असंभव होता है।
भारत में प्राप्त हुए सबसे प्राचीन शिलालेख सम्राट अशोक के काल के हैं। इन शिलालेखों में वृहद् शिलालेख, लघु शिलालेख एवं स्तंभ लेख शामिल हैं। इन शिलालेखों में ब्राह्मी खरोष्ठी, अरमाईक एवं ग्रीक लिपियों का प्रयोग किया गया है। लंबे समय तक इन शिलालेखों का अध्ययन संभव नहीं हो सका था। लेकिन इन शिलालेखों के अध्ययन की शैली के विकास के साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में व्यापक जानकारियां लोगों के समक्ष आने लगीं। अशोक के शिलालेखों से मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण संभव हो सका, मौर्य साम्राज्य के वैदेशिक संबंध एवं विदेशी-राज्यों के बारे में सूचना प्राप्त हुआ। मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासकीय व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई।
सबसे बढ़कर अशोक की धम्म नीति एवं उसके राजकीय आदेशों एवं प्रजा हेतु उठाए गए कल्याणकारी कदमों की जानकारी शिलालेखों से ही प्राप्त होती है। शिलालेखों से ही स्पष्ट होता है कि भारतीय-यूनानी, शक-क्षत्रप ओर कुषाण राजाओं ने दो अथवा तीन शताब्दियों में भारतीय नाम एवं परम्परा को अपना लिया। इन शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि वे अन्य किसी भारतीय की तरह सामाजिक और धार्मिक कल्याण का कार्य करते थे। शिलालेखों में संस्कृत का भी प्रयोग किया जाने लगा था। रूद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो दूसरी शताब्दी ई- के मध्य में लिखा गया था, समकालीन इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना देता है। यह शिलालेख प्रांजिल संस्कृत का एक प्राचीन उदाहरण समझा जाता है।
गुप्तकाल के शिलालेख संस्कृत भाषा में है। इलाहाबाद के स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का सारांश दिया गया है। इस एकमेव उत्कीर्ण लेख के अभाव में यह महान गुप्त नरेश भारत के इतिहास में अज्ञात बना रहता। गुप्तकाल के अधिकतर पुरालेखों में वंशावलियों का वर्णन है। आगे आने वाले राजवंशों में इसका प्रयोग होने लगा। वे इन शिलालेखों पर अपनी विजय तथा अपनी पूर्वजों की उपलब्धियों और अपने पौराणिक मूल का विवरण देते थे। इसके कारण प्राचीन भारत का इतिहास विन्यास स्थापित करना एवं सही कालानुक्रम का ज्ञापन संभव हो सका। ये शिलालेख शुंग वंश, सातवाहन वंश से लेकर हर्ष के काल तक की जानकारियों के स्रोत हैं। शिलालेखों से हमें अग्रहार, देवदान, भूमिदान आदि के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है।
सिक्केः सिक्के इतिहास के पुनर्निर्माण का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। पहला स्थान उत्कीर्ण लेखों का है। लाखों की संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के बहुमूल्य हैं, क्योंकि इनके कालानुक्रम और सांस्कृतिक संदर्भ को सही-सही निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, चांदी और तांबे के हैं। कुछ सोने के भी आहत सिक्के मिले हैं, लेकिन इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं और उनके केवल प्रतीक अंकित हैं। प्रत्येक प्रतीक को अलग से अंकित (पंच) किया गया है। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तथा दूर दक्षिण में मिले हैं।
इन सिक्कों पर कोई शब्द या लेख अंकित नहीं है, लेकिन इन सिक्कों के विश्लेषण से प्राचीन भारत के आर्थिक-सामाजिक पहलू के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है।
भारतीय-यूनानी अथवा हिन्द-यवन सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, ये भी अधिकतर चांदी एवं तांबे के हैं। कुछ सिक्के सोने के भी प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के सुंदर एवं कलात्मक आकृतियों से युक्त हैं। इन सिक्कों के मुख्य भाग पर राजा की आकृति एवं पृष्ठ भाग पर देवता की मूर्ति अंकित है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें उन चालीस से अधिक भारतीय यूनानी शासकों का पता चला है, जिन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में शासन किया। इन सिक्कों से ही उन शक-पार्थियन राजाओं का पता चलता है, जिनके बारे में किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कुषाणों ने अधिकतर सोने और कुछ मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए, जो उत्तर-पश्चिम भारत से बिहार तक के विस्तृत क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। विम कडफिसिस के सिक्कों पर भगवान शिव की आकृति अंकित है। इन सिक्कों पर अंकित लेख में राजा ने अपना उल्लेख शिव भक्त के रूप में किया है। कनिष्क के सिक्कों पर भारतीय देवताओं के अलावा शकमुनी बुद्ध की आकृति अंकित है। ये सिक्के कुषाणकालीन धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था को जानने के मुख्य स्रोत हैं। गुप्त काल के सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के अश्वमेध, परशु सिंहहंता आदि के रूप मे प्रसिद्ध हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्के शासकों पर विजय की जानकारी देते हैं। इसके अलावा मौर्यात्तर काल से लेकर हर्ष के काल तक के सिक्के ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। अतः उपरोक्त विवेचना स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु सर्वप्रमुख स्रोत शिलालेख एवं सिक्के ही हैं।
Question : निम्नलिखित स्थानों में से किन्ही पंद्रह स्थानों को आपको दिए गए नक्शे पर चिन्हित कीजिए और चिन्हित किए गए स्थानों पर ही संक्षिप्त वर्णनात्मक टिप्पणियां भी लिखिएः
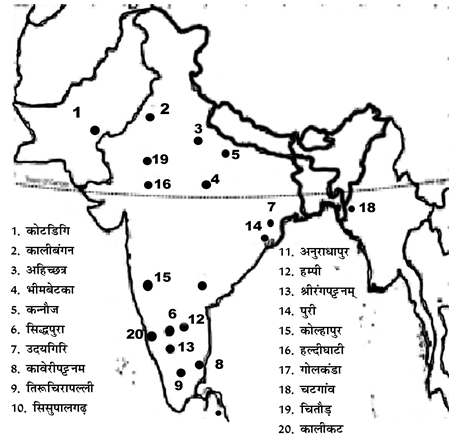
(2007)
Answer : 1. कोटडिगिः वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर के पास अवस्थित है। वहां से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के आघार पर प्राक्-हड़प्पीय, ताम्रपाषाण संस्कृति, स्थानीय कृषक समुदायों के प्रसार एवं हड़प्पा की नगर सभ्यता से उनके सम्बन्ध की जानकारी मिलती है। कोटदिजी में किलेबन्दी का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
2. कालीबंगनः यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के समीप स्थित है। हड़प्पा-युगीन संस्कृति के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राक-हड़प्पा चरण से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। इससे हड़प्पा-पूर्व काल में कृषि प्रसार के संकेत मिलते हैं। कालीबंगन के घरों में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है और न ही यहां कोई स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई है।
लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों के समान ही मुहरें, भार-माप, टेरीकोटा, धान्यकोठार, पत्थर एवं तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त अग्निवेदी यज्ञीय क्रिया-कलापों का संकेतक है।
3. अहिच्छत्रः अहिच्छत्र की समता उत्तर प्रदेश के बदेली जिले में स्थित रामनगर से की गई है। इस स्थान से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर गुप्तोत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं। यहां से चित्रित धूसर मृद्भाण्ड तथा लाल मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महाजनपद युग में यह उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। इस स्थान पर अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। यहां से कुषाणों से सिक्के इत्यादि भी मिले हैं। गुप्तकाल में अहिच्छत्र एक नगर के रूप में बसा हुआ था, जहां के शासक अच्युत को समुद्रगुप्त ने हटाया था।
4. भीमबेटकाः भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विन्ध्यपर्वतीय क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है।
यहां से पुरापाषाण तथा मध्यपाषाण दोनों ही संस्कृतियों से संबद्ध पुरातात्विक अवशेष मिले हैं।
भीमबेटका से उच्च पुरापाषाणीय अवस्था के मानव के उपयोग लायक गुफाएं एवं शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रय के चित्रों में हरे एवं लाल रंग का प्रयोग किया गया है एवं पशु, पक्षी, मनुष्यों को विषय बनाया गया है।
5. कन्नौजः प्राचीन भारत में कान्यकुब्ज के नाम से विख्यात कन्नौज वर्तमान समय में उत्तर-प्रदेश के फर्रूखाबाद जिले में गंगा के किनारे अवस्थित एक बस्ती है। कन्नौज से उत्तरी काले मृद्भाण्ड युग से लेकर कुषाण, गुप्त एवं मध्यकालीन युग तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज की सर्वार्ंगीण भव्यता कीमती थी, जिसका उल्लेख ह्नेनसांग ने किया है। उस समय कन्नौज ‘नगर-महोदयश्री’ कहलाता था। हर्षोत्तर काल में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए पालों, गुर्जर प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य विख्यात त्रि-दलीय संघर्ष चला था। जयचन्द के काल में इस नगर पर तुर्को ने अधिकार कर लिया।
6. सिद्धपुराः सिद्धपुरा वर्तमान में कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरि के समीप स्थित है। सिद्धपुरा से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो इस तथ्य का सूचक है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार इन क्षेत्रों तक था। वस्तुतः सिद्धपुर, गोविमढ़ और पालकीगुण्डु ऐसे दक्षिण भारतीय स्थल हैं, जो ब्रह्मगिरि में मिले अशोक के अभिलेख-समूह से संबंधित हैं।
7. उदयगिरिः उदयगिरि वर्तमान उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के समीप है। यहीं उदयगिरि पर्वत को काट कर कई गुफाओं का निर्माण किया गया था। इन गुफाओं में निर्मित चैत्यगृह जैन धर्म से संबंध रखते हैं। उदयगिरि चैत्यगृह का निर्माण शुंग काल में हुआ था। उदयगिरि से कुछ ही दूर कलिंग शासक खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख खुदा हुआ है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने उदयगिरि पहाड़ी क्षेत्र में शेवों के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था।
8. कावेरीपट्टनमः वर्तमान समय में कावेरीपट्टनम तमिलनाडु में कोरोमंडल पर तंजौर जिले में कावेरी नदी के किनारे स्थित है। समुद्री एवं स्थानीय जल मार्ग से जुड़े होने के कारण इस स्थान का आर्थिक-राजनैतिक महत्व था। यह प्राचीन चोलों की प्राचीन-पत्तन राजधानी थी। मौर्योत्तर युग में रोम के साथ व्यापारिक संबंध होने के कारण कावेरीपट्टनम की सम्पन्नता बहुत बढ़ गई थी। कावेरीपट्टनम एक विकसित बंदरगाह था, जहां चुंगी घर, प्रकाश स्तम्भ एवं माल गोदाम जैसी स्तरीय सुविधाएं थीं।
9. तिरूचिरापल्लीः तमिलनाडु में कावेरी तट पर स्थित तिरूचिरापल्ली पर प्रारंभ में चोल, पाण्ड्य एवं विजयनगर के शासकों का शासन रहा। कालांतर में यह मद्रास प्रेसीडेंसी के अधीन हो गया। आधुनिक काल में अंग्रेज-फ्रांसीसी संघर्ष (कर्नाटक युद्ध) के समय तिरूचिरापल्ली का विशेष महत्व हो गया।
10. सिसुपालगढ़ (शिशुपालगढ़): शिशुपालगढ़ उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के निकट पुरी जिले में स्थित है। यहां से 300 ई. पू. से 300 ई. के मध्य की संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शिशुपालगढ़ की पहचान खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी से की गई है। यहां से कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहां से रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जिससे रोमन व्यापारिक संपर्क के भी प्रमाण मिलते हैं। शिशुपालगढ़ के निकट ही अशोक के अभिलेखों में तोसली के रूप मे वर्णित स्थान धौली भी है।
11. अनुराधापुरः अनुराधापुर उत्तरी श्रीलंका में मलवतु ओय नदी के समीप स्थित है। अशोक युग में महेन्द्र एवं संघमित्र ने यहां बोधिवृक्ष की टहनी का रोपण किया था। यहां भगवान बुद्ध का एक दांत भी है। पूर्व मध्ययुग में चोल शासक राजरात प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को जीतकर उसे अपना एक प्रांत बनाया एवं उसे ‘पोलन्नरूआ’ का नाम दिया। अनुराधापुर उसी प्रांत की राजधानी थी।
12. हम्पीः दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सम्प्रति यह कर्नाटक के बेलारी जिले में है।
इस नगर का निर्माण 1343 ई. में हुआ और विजयनगर के पतन से पहले इस पर चार वंशों-संगम, सालुव, तुलुव और अरविडु ने शासन किया। 1565 ई. के तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य के राज्यों के संयुक्त कमान ने हंपी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया।
13. श्रीरंगपट्टनम्ः सम्प्रति कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर स्थित श्रीरंगपट्टनम् मध्यकाल में मैसूर के वोडेयार वंश के शासकों और फिर हैदर अली एवं टीपू के राज्य की राजधानी रही।
इस नगर का नामकरण यहां स्थित एक मंदिर के आधार पर हुआ है, जिसमें भगवान श्रीरंग (विष्णु) की प्रतिमा है। आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान यह सर्वाधिक प्रमुख केन्द्र था और चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान यहीं लड़ते-लड़ते शहीद हो गया था।
14. पुरीः वर्तमान में उड़ीसा राज्य का जिला प्राचीन काल से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रहा है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों में से एक पुरी भी है। पुरी में ही प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। पुरी जिले के अन्तर्गत ही शिशुपालगढ़ भी है, जो कालिंग नरेश खारवेल की राजधानी थी।
15. कोल्हापुरः कोल्हापुर महाराष्ट्र का जिला नगर है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के निकट है। यह मध्ययुग में मराठों के एक दल का प्रमुख केन्द्र था।
1707 ई. में ताराबाई ने कोल्हापुर को केन्द्र बनाकर शाहू के विरुद्ध संघर्ष किया था। बाद में शाहू ने ताराबाई के नेतृत्व में कोल्हापुर राज्य की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। इसके अतिरिक्त 1880 ई. में यहां से अशोककालीन लेखयुक्त एक विशाल स्तूप भी प्राप्त हुआ है।
16. हल्दीघाटीः आधुनिक राजस्थान में अरावली पर्वतों के पास स्थित हल्दीघाटी मध्यकालीन भारत में सिसोदिया राजपूतों की वीरता के लिए इतिहास प्रसिद्ध है।
1576 ई. के अकबर एवं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच यहां एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना को थोड़े से राजपूत सैनिकों ने नाको चने चबा दिए। राणा प्रताप ने अंततः हार नहीं मानी और आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों ने भी मुगलों का प्रतिकार जारी रखा।
17. गोलकुंडाः गोलकुण्डा आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के समीप स्थित है। गोलकुण्डा पर देवगिरि के यादवों एवं वारंगल के काकतीय लोगों का शासन रहा। 1424-25 ई. में गोलकुण्डा को बहमनी शासकों ने अपने राज्य में मिला लिया।
1518 ई. में कुली कुतुब शाह ने गोलकुण्डा में स्वतंत्र कुतुबशाही वंश की नींव डाली। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुण्डा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुण्डा हीरों के लिए प्रसिद्ध था। यहां बड़े स्तर पर मध्यकालीन दक्षिण-भारतीय स्थापत्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
18. चटगांग (चटगांव): बांग्लादेश में चटगांव बंगाल की खाड़ी में तटीय क्षेत्र से सटा हुआ है। मध्यकाल में यह एक प्रमुख व्यापारिक नगर था, जिसका राजनीतिक महत्व भी था। चटगांव पर 1415-18 तक बंगाल के राजा गणेश का और उसके बाद अराकानियों का अधिकार था। 1498 ई. बंगाल के शासक हुसैन शाह ने चटगांव पर अधिकार कर लिया। 1666 ई. में औरंगजेब के समय शाइस्ता खां ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
19. चित्तौड़ः राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित चित्तौड़ मध्यकालीन भारत में राजपुताना क्षेत्र की मेवाड़ रियासत का प्रमुख केन्द्र था। सातवीं-आठवीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बप्पारावल ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। चित्तौड़ के प्रमुख शासक सिसोदिया राजपूत थे, इनमें राणा कुम्भा, राणा सांगा और राणा प्रताप प्रमुख थे। अलाउद्दीन खिल्जी ने सर्वप्रथम 1302-03 ई- में चित्तौड़ को जीतकर इसका नामकरण किया था। अकबर ने 1567 ई. में चित्तौड़ पर अधिकार किया था।
20. कालीकटः केरल के मालाबार तट पर स्थित कालीकट अथवा कोजीकोड जिला नगर है। किसी समय कैलिको अथवा मलमल के उत्पाद केन्द्र होने के कारण कालीकट नाम पड़ा। मई 1798 में वास्कोडिगामा भारत में सर्वप्रथम यहीं आया था। कालीकट पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों एवं डेनिशों के प्रभाव में रहा। अंततः 1790 ई. में इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब्दुर्रज्जाक के अनुसार, कालीकट मालाबार तट का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र एवं बंदरगाह था। कालीकट से काली मिर्च आदि का निर्यात किया जाता था।
Question : प्रथम शताब्दी ई. से पूर्व बौद्ध धर्म के उत्थान और प्रसार के बारे में जो कुछ आप जानते हैं, वह लिखिए।
(2007)
Answer : छठी सदी ई. पू. में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उत्थान एक प्रमुख घटना थी। विद्वानों ने बौद्ध धर्म के उत्थान के कारणों पर विस्तारपूर्वक विचार किया है एवं बौद्ध धर्म के उत्थान के संदर्भ मे विविध पक्षों एवं मतों को प्रतिपादित किया है। बौद्ध धर्म के उत्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि इसने वर्ण व्यवस्था एवं कर्मकाण्डों पर आधारित ब्राह्मण धर्म का खंडन किया एवं एक अधिकाधिक संतुलित और स्वीकार करने योग्य समाधान प्रस्तुत किया, जो लोहे के उपयोग के फलस्वरूप समाज मे आये राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि समाज के मूल तत्व में आये परिवर्तनों के कारण जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उनके अनुसार, ये आन्दोलन उत्तर वैदिक समाज एवं यक्षों के शुद्धिकरण की ओर प्रेरित था, जो कठोर एवं शोषक प्रकृति का हो गया था तथा जिसके चलते धन की भारी हानि होती थी, वहीं एक अन्य मत यह स्थापित करता है कि बौद्ध आन्दोलन राजकीय नियंत्रण, वर्ग आधारित समाज एवं उस सामाजिक संरचना के विरुद्ध थी, जिसकी प्रकृति शोषण की थी। फलतः तात्कालिक व्यवस्था से असंतुष्ट विशाल जनसमूह का समर्थन बौद्ध धर्म को प्राप्त होने लगा। बौद्ध धर्म के उत्थान को तात्कालिक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है।
द्वितीय अवस्था में लोहे के प्रयोग से अर्थव्यवस्था में दूरगामी परिवर्तन आया। छठी सदी ई. पू. में कृषि कार्य में लोहे के उपयोग के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। लौह आधारित कृषि के कारण बड़ी संख्या में बैलों एवं अन्य पशुओं की आवश्यकता हुई, पर यज्ञों में दी जाने वाली बलि के कारण बड़ी संख्या में पशुओं की हत्या हो रही थी। यदि इस कृषि अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना था, तो इन हत्याओं को रोका जाना अनिवार्य था। ऐसी स्थिति में बुद्ध द्वारा अहिंसा एवं पशु सुरक्षा पर बल दिया गया, फलतः लोग बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। कृषि क्षेत्र में आये आमूल परिवर्तनों से अधिशेष उत्पादन संभव हो सका, जिससे व्यापार-वाणिज्य का विकास हुआ।
इससे स्वाभाविक रूप से नए शहरी केंद्रों का उदय हुआ। पंचमार्क सिक्कों के प्रचलन से इस प्रक्रिया में सुविधा होना स्वाभाविक था। इन सबके कारण वैश्यों की हैसियत बढ़ गई। वर्णाश्रम व्यवस्था आधारित समाज में वैश्यों की स्थिति तीसरे दर्जे की थी। अतः वैश्यों ने किसी ऐसे धर्म का सहारा लेने का प्रयास किया जो उनकी स्थिति को सुधारने में मदद दे।
फलस्वरूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी। बौद्ध धर्म तात्कालिक समय में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तनों को स्थिर रखने में भी सहयोग दिया। व्यापार-वाणिज्य की वृद्धि के कारण पैसा उधार देने के पेशे को बढ़ावा मिला। इसलिए वैश्यों को जो व्यापार-वाणिज्य की वृद्धि के कारण पैसा उधार देने लगे थे, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, क्योंकि ब्राह्ममण धर्म के धर्मसूत्र ने अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने को निंदनीय कहा गया है, जबकि बौद्ध धर्म ने अप्रत्यक्ष रूप से पैसा उधार देने का समर्थन किया। उसी प्रकार कर्जदार व्यक्ति को बौद्ध संघ में शामिल न करने का नियम था।
इसलिए स्वाभावतः इससे महाजनों एवं समाज के धनी वर्गो को लाभ प्राप्त हुआ एवं वे बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुए। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए अपने द्वार खुले रखे। ब्राह्मण धर्म में इन्हें यज्ञोपवित एवं वेदाध्ययन की अनुमति नहीं थी। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर उन्हें इन हीनताओं से मुक्ति मिल गई।
‘राधाकृष्णन’ जैसे विद्वानों के अनुसार, बौद्ध धर्म के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण बुद्ध का वास्तविक अर्थ में समकालीन समाज का प्रतिनिधित्व करना था। इन्होंने तत्कालीन सामाजिक स्थिति का अनुभव कर लोगों को उनके अपने विचारों के अनुसार परिवर्तित किया। बुद्ध तात्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक संधान को सही दिशा देने में सफल रहे। बौद्ध धर्म के सिद्धान्त ब्राह्मण धर्म के विपरीत सरल एवं बोधगम्य के साथ ही जनमानस के भाषा पालि में इसे प्रस्तुत किया गया था।
फलतः सत्य, अहिंसा एवं सदाचार संबंधी बौद्ध सिद्धान्तों से जन सामान्य अति प्रभावित हुए। सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले भिुक्षुओं द्वारा धर्म प्रचार करने से आम जनता प्रभावित हुई।
बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा था। सर्वप्रथम आर्यभूमि एवं ब्राह्मणीय प्रभावों से बाहर समझे जाने वाले मगध क्षेत्र के लोगों ने इसे अपनाया। अवन्ति, कोशल तथा काशी समेत अनेक गणतंत्रों की जनता भी बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुई। बिम्बिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु एवं उदयन जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को सरंक्षण एवं सहयोग प्रदान किया। अजातशत्रु के काल में राजगीर में (483 ई. पू.) एवं कालाशोक के समय वैशाली में (383 ई.) में आयोजित बौद्ध सम्मेलनों में बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों एवं आचार संहिता आदि को व्यवस्थित एवं परिष्कृत किया गया।
बौद्ध धर्म के इतिहास में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अंगीकार करना एक युगान्तकारी घटना थी। कलिंग युद्ध के तत्काल बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके उपरांत उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति एवं प्रजा की भौतिक प्रगति के लिए बौद्ध धर्म को आधार बनाया। बौद्ध धर्म के प्रचार में गति लाने एवं बौद्ध धर्म में एकता बनाये रखने के लिए उसने तृतीय बौद्ध संगीति (पाटलिपुत्र-251 ई. पू.) का आयोजित किया। इस तृतीय बौद्ध संगीति, जिसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्त तिस्स ने की थी, के उपरांत अशोक ने बुद्ध के संदेशों एवं शिक्षाओं का संपूर्ण भारत एवं पड़ोसी देशों में प्रचार करने हेतु धर्म प्रचारक मंडल भेजे।
उसने अपने व्यवस्थित एवं उत्साहपूर्ण प्रयासों द्वारा बुद्ध के संदेशों को गुफाओं एवं मठों से निकालकर इसे एक राष्ट्रीय धर्म बनाया।
अशोक महान के प्रयासों से बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ एवं बौद्ध धर्मानुयायियों में नवीन उत्साह का संचार हुआ। इसके परिणामस्वरूप बौद्ध समुदाय ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी बौद्ध संघ को उदार संरक्षण प्रदान किया। सांची और भरहुत में आज भी हम स्तूपों एवं उनके चारों ओर निर्मित वेदिकाओं को देखते हैं। वे अशोक के बाद लगभग 50-100 वर्षों में बुद्ध के धर्मपरायण अनुयायियों द्वारा निर्मित की गई हैं। यह कहा जाता है कि इन स्थानों पर वेदिकाओं के निर्माण के लिए बौद्ध समितियां बनाई गई थीं। इस प्रकार दूसरी शताब्दी ई. पू. तक बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया।
जब हिन्द-यूनानियों और कुषाणों ने क्रमशः दूसरी शताब्दी ई. पू. तथा प्रथम शताब्दी ई. पू. में उत्तर-पश्चिमी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया, तो इसके उपरांत बौद्ध धर्म का और तेजी से विस्तार हुआ। उन्होंने इस धर्म को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया। इसमें यवन नरेश मिनान्डर या मिलिन्द, जिन्होंने 160 ई. पू. के आसपास नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी एवं कुषाण शासक कनिष्क जिसने 78 ई. से 101 ई. तक शासन किया अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
भारत में अपने प्रसार के साथ-साथ बौद्ध धर्म ने भारत की सीमाओं को भी पार कर लिया और वहां इसे ठोस आधार मिला। तीसरी सदी ई. पू. में अशोक द्वारा तीव्रता से धर्म प्रचार किया गया। उसने महेन्द्र एवं संघमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। यह धर्म धीरे-धीरे एशिया के अधिकांश भागों में फैल गया।Question : गुप्त काल में आम आदमी की दशा पर प्रकाश डालिए।
(2007)
Answer : गुप्त काल में आम आदमी की दशा का सर्वश्रेष्ठ ज्ञापन तात्कालिक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की दशा का निर्धारण सामाजिक एवं आर्थिक तत्व ही करते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां एवं सांस्कृतिक परिदृश्य भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं।
गुप्तकालीन समाज में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्राथमिक इकाई थी, जिसमें जन्मजात उत्तराधिकार की परम्मरा प्रचलित थी। व्यक्ति अगर ज्येष्ठ पुत्र हो तो उसे बड़ा भाग मिलता था। उस काल में भूमि अनुदानों का परिणाम विखंडन के रूप में सामने आया, जिससे संयुक्त परिवार टूटकर छोटी इकाइयों मे विभक्त हो गये थे। एक आम व्यक्ति के तौर पर गुप्तकाल में स्त्रियों की दशा संतोषजनक नहीं कही जा सकती थी।
यदि स्त्री उच्चवर्गीय हो, तो उन्हें सीमित अधिकार प्राप्त थे तथा वे शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं एवं कुछ अवसरों पर दार्शनिक, अध्यापिका एवं चिकित्सक आदि की भूमिका भी निभा सकती थीं, किन्तु एक सामान्य स्त्री कई मूलभूत अधिकारों से वंचित थी। जैसे-उन्हें पैतृक संपति में हिस्सा प्राप्त नहीं होता था। उच्च शिक्षा प्रतिबंधित थी। लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता था एवं विधवाओं की दशा बुरी थी। सामान्य मामलों में पुनर्विवाह प्रतिबंधित था। यद्यपि गुप्तकालीन साहित्य में स्त्रियों को अवश्य आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया था, किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं था।
गुप्तकाल में एक सामान्य व्यक्ति को जाति संबंधी प्रतिबंधों एवं निर्योग्यताओं से एक हद तक राहत प्राप्त हुई। यद्यपि यदि व्यक्ति उच्च वर्ग का हो, उसे कई विशेषाधिकार अब भी प्राप्त थे, किन्तु अन्तर्जातीय विवाह एवं विभिन्न जाति के लोगों के बीच सहयोजन जाति व्यवस्था में सीमित उदारता को सूचित करती है।
गुप्तकाल में एक व्यक्ति को आर्थिक स्तर पर पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं। व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता था एवं व्यवसाय जाति के साथ कठोरता से नहीं जुड़ा हुआ था। यहां तक कि कई शूद्र वर्ग के व्यक्तियों को भी अब सैनिक, व्यापारी एवं कृषक कार्यो को अपनाने का मौका मिला। लेकिन ऐसा नहीं था कि सामाजिक व्यवस्था में बहुत व्यापक परिवर्तन आ गया था।
वर्णाश्रम व्यवस्था के सुदृढ़ होने के साथ ही अनेक पेशागत समूहों एवं जनजातियों की स्थिति में ह्रास हुआ था। अनेक अस्पृश्य जातियां थीं, इनमें चांडाल सबसे नीचे था। फाह्यान एवं ह्नेनसांग ने इन पर लगे प्रतिबंधों की चर्चा की है। सामान्यतः लोग अशुद्ध होने के भय से इनका बहिष्कार करते थे।
गुप्तकाल में दासों की स्थिति में गिरावट आई। इन्हें सामान्यतः अधिकार प्राप्त नहीं थे।
गुप्त काल में भू-राजस्व कुल उपज के 1/6 भाग के बराबर था। इसके अलावा व्यक्तियों को बलि, हिरण्य, उद्रंग एवं उपरिकर आदि अन्य कर देने होते थे। सामान्य ग्रामीणों को बेगार (बिष्टी) के लिए बाध्य किया जाता था। राजस्व वृद्धि एवं विशेष वर्गो को दी गई उन्मुक्तियों ने सामान्य जन की स्थिति को निश्चय ही दुष्प्रभावित किया। सूखा, बाढ़, फसल नष्ट होने एवं अकाल की स्थिति से आम आदमी की स्थिति तो निश्चय ही प्रभावित होती थी, लेकिन सबसे बढ़कर सामंतवादी विकास ने आम आदमी की स्थिति को दुष्प्रभावित किया।
गुप्त काल में उद्योगों एवं हस्तशिल्पों की स्थिति संतोषजनक थी। तांबा, कांसा, लोहा एवं सीसा उद्योगों के विकास के साथ-साथ सूती वस्त्र एवं रोशमी वस्त्र उद्योगों का भी विकास हुआ, फलतः व्यक्तियों के समक्ष रोजगार के पर्याप्त अवसर मौजूद थे। लुहारी, हाथी दांत का काम, पाषाण उद्योग, मूर्ति शिल्पकला, मिट्टी के बर्तन का निर्माण आदि व्यवसाय लागों के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका के स्रोत थे। यद्यपि गुप्तकाल के अंतिम दौर में उत्पादन एवं व्यापार में अवनति दृष्टिगोचर होती है। स्वभाविक रूप से इस स्थिति में व्यापारिक वर्ग के साथ-साथ जनसामान्य की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
गुप्त काल में आम आदमी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। हिन्दू धर्म में इस समय नई विशेषताओं का समावेश हुआ तथा देवी पूजा एवं तंत्रवाद का उद्भव हुआ। मूर्ति पूजा आम चलन में आ गया एवं अवतार की प्रतिष्ठा हुई। व्यक्तियों ने अपने विश्वासों के अनुरूप धार्मिक विचारों एवं क्रिया-कलापों को अपनाया।
हिन्दू धर्म के अंतर्गत शैव एवं वैष्णव सम्प्रदाय की उन्नति हुई एवं दोनों सम्प्रदाय के जन सामान्य के बीच संघर्ष अथवा मतभेद की स्थिाति नहीं थी। इस काल में बौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो गया था, लेकिन बौद्ध धर्मावलंबियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया था। पश्चिम भारत में जैन धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। इस समय जनसामान्य के बीच बौद्धिक स्तर पर शास्त्रर्थ लोकप्रिय था, जो सामान्यतः बौद्धों एवं ब्राह्मणों के बीच होता था। ब्राह्मण धर्म के अनुनायी गुप्त काल में पवित्र शास्त्र के प्रावधानों के अनुरूप व्यवहार करना ही उचित मानते थे।
गुप्त काल में आम व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका नगण्य थी। शासकों के परिवर्तन एवं राजनैतिक बदलावों से जनसामान्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। प्रारंभिक गुप्त शासकों ने साम्राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रखा था, फलतः जनसामान्य भी सुरक्षित थे। कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक होने के कारण आम तौर पर शान्ति थी। यद्यपि गुप्तकाल के अंतिम दौर में हुआ आक्रमण एवं राजनीतिक उथल-पुथल से जन सामान्य का प्रभावित होना आवश्यक था।
इस समय हिन्दू समाज शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। वात्सायन के कामसूत्र से हमें नागरिक दैनिक जीवन की कुछ जानकारी मिलती है। पता चलता है कि वे आरामदायक एवं विलासी जीवन जीते थे। व्यक्तियों की संगीत, चित्रकला एवं मूर्तिकला में रुचि थी, साथ ही जुए का भी चलन था। इस काल में जो महान सांस्कृतिक विकास हुआ उसमें जनसामान्य के योगदान से इंकार नहीं किया जा सकता। शैक्षणिक स्तर पर प्रगति हुई, प्रतिभाशाली एवं विद्वान व्यक्तियों को प्रर्याप्त सम्मान दिया जाता था।
कुल मिलाकर गुप्त काल में आम आदमी की दशा संतोषजनक थी। आजीविका के साधन उपलब्ध थे एवं उन्नति हेतु अवसर भी मौजूद थे। राजनीतिक रूप से गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ होने के कारण शांति और सुरक्षा का माहौल था एवं व्यक्ति का जीवन सुरक्षित था। किन्तु गुप्त काल में आम आदमी की दशा पर प्रकाश डालते हुए कुछ तथ्यों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। गुप्त काल से ही सामंतवाद का उत्थान प्रारंभ हुआ एवं सामंतवादी व्यवस्था के विकास के साथ ही जन सामान्य के अधिकारों में कटौती भी प्रारंभ हो गई। पुनः गुप्त काल में आम आदमी की स्थिति बहुत हद तक उसके वर्ग एवं जाति द्वारा भी निर्धारित होती थी।
Question : प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के बदलते हुए उपागमों पर चर्चा कीजिए।
(2006)
Answer : प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का आधुनिक अध्ययन 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यहां के रीति-रिवाजों, परम्पराओं और विधि-व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक प्रतीत हुआ। फलतः इतिहास के अध्ययन के साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। इसके अन्तर्गत औपनिवेशिक-प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर इतिहास को देखने का प्रयास किया गया।
इसके प्रतिक्रियास्वरूप 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास के संदर्भ में राष्ट्रवादी उपागम उभर कर सामने आया। पुनः 1960 ई. के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण उभरते हैं, जो अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत हैं। इनमें सामाजिक-आर्थिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल है तथा इतिहास को पुरातात्विक आधार पर समझे जाने का प्रयत्न भी है।
औपनिवेशिक उपागमः 18वीं शताब्दी में इतिहास का प्रस्तुतीकरण औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा औपनिवेशिक शासन को दृढ़ता प्रदान करने से संबद्ध था। आरंभिक चरण में प्राच्यविदों का प्रभाव रहा। 1784 ई. में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में संस्कृत, अरबी व फारसी ग्रंथों का संकलन व अनुवाद इस संस्था द्वारा किया गया।
प्राच्यविदों ने इतिहास लेखन के क्षेत्र में हमें एक नई दिशा दिखाई, ऐसा माना जा सकता है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर मौर्य राजवंश को सर्वव्यापी बनाया। इसी कारण भारतीय इतिहास के कालक्रम को विश्वसनीयता प्राप्त हो सकी तथा प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से संभव हो सका। प्राच्यविदों ने चीनी यात्रियों के वर्णनों को खोज निकाला, जिसमें निःसन्देह भारतीय इतिहास पर नई रोशनी पड़ी। कनिंघम ने अपनी पुरातात्विक खोजों से नवीन स्थानों को ढ़ूंढ़ा तथा ‘आर्कियोलोजिकल सर्वे रिपोटर्स’ के बीस खण्डों की रचना की।
प्राच्यविदों में से जिन लोगों ने संस्कृत का अध्ययन किया वे ‘आर्य संस्कृति’ के उत्साही प्रतिपादक बन गए। भारतीय-यूरोपीय मूलस्थान तथा संस्कृत और यूनानी संस्कृतियों की समान पूर्वज परंपरा का सिद्धांत उन्होंने विकसित किया। वैदिक युग को बढ़ा-चढ़ाकर आंका गया। मैक्समूलर ने भारतीय ग्राम्य-समाज का ऐसा वर्णन किया कि कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उन्होंने भारत की भूमि के दर्शन भी नहीं किए थे। तनाव भरी बातों को नजरअंदाज कर गौरव के पक्ष पर जोर दिया गया। भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में यद्यपि प्राच्यविदों की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता, किन्तु उन्होंने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया तथा उसका अति रोमांचकारी वर्णन किया। उन्होंने प्रमाणों की काल्पनिक और अपनी रूचि के अनुकूल व्याख्या की।
प्राच्यविद् उपयोगितावादियों के साथ संघर्ष में मात खा रहे थे। उपयोगितावादियों में जेम्स मिल और बेंथम प्रमुख थे। प्राच्यविदों के विपरीत उन्होंने भारतीय पद्धति को निकृष्ट करार दिया। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक व्याख्या की नींव डाली तथा द्विराष्ट्र के सिद्धांत के लिए ऐतिहासिक औचित्य प्रस्तुत किया। वह पहला इतिहासकार था, जिसने भारतीय इतिहास को तीन कालों में विभाजित करने का प्रयत्न किया-हिन्दू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश सभ्यता। यद्यपि भारतीय इतिहास में धर्म किसी भी दृष्टि से परिवर्तन का शक्तिशाली प्रेरक तत्व नहीं रहा, जैसा कि इन नामों से प्रतिध्वनित होता है। इस प्रकार औपनिवेशिक उपागम के अन्तर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रस्तुतीकरण के महत्वपूर्ण विषय हैं-भारत में निरंकुशवादी शासन, राजनीतिक एकता का अभाव, भारतीयों का आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों से जुड़ा रहना, भारत में एक राष्ट्र की संकल्पना का अभाव, भारतीयों की एहलौकिक विषयों के प्रति उदासीनता, भारतीय समाज में ठहराव की स्थिति एवं अप्रगतिशीलता, भारत में प्रजातांत्रिक संस्थानों का अभाव, भारतीयों की स्वशासन के प्रति अनुभवहीनता आदि। इस प्रकार औपनिवेशिक उपागम का प्रमुख उद्देश्य था, भारत में ब्रिटिश राज्य एवं भारतीय ड्डोतों के शोषण का ऐतिहासिक औचित्य सिद्ध करना तथा औपनिवेशिक शासन को वैधता प्रदान करना। इस उपागम में इतिहास की वास्तविकता को नकारा गया है, राजवंशों के इतिहास पर बल दिया गया है तथा बाह्य प्रभावों को अधिक महत्त्वपूर्ण बताया गया है।
राष्ट्रवादी उपागमः उपनिवेशवादी उपागम के विरोध में शीघ्र एक नीवन शैली का जन्म हुआ, जिसे राष्ट्रवादी उपागम की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गई है कि भारतवासियों की दुद्रशा के लिए साम्राज्यवादी प्रशासक ही उत्तरदायी थे। साम्राज्यवादी-राष्ट्रवादी विवाद के फलस्वरूप भारतीय आर्थिक इतिहास का एक नया विषय के रूप में जन्म हुआ।
इसी विषय के अन्तर्गत दादाभाई नौरोजी, आर. सी. दत्त आदि अनेक विद्वानों ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शैली की कटु आलोचना की। राष्ट्रवादी इतिहासकार प्राचीन भारत का काफी बढ़ा-चढ़ाकर गौरवगान करते थे। धर्मशास्त्रों जैसी रचनाओं को भारतीय जीवन की वास्तविकता के विवरण के रूप में स्वीकार कर लिया गया और प्राचीन भारतीय जीवन को निर्बन्ध खुशहाली का जीवन मान लिया गया। विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति, जनतांत्रिक संस्थाओं एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसी मूल्यों की खोज की जाती थी और प्राचीन भारत में इनका अस्तित्व था, ऐसा पहले ही मान लिया जाता था। ऐसे मूल्य राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए आवश्यक थे। इस उपागम में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि भारत का राजनीतिक इतिहास है तथा प्राचीन भारतीयों को प्रशासन का अनुभव था, परन्तु मिल के काल विभाजन को चुनौती नहीं दी गई तथा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अनजाने ही हिन्दू-पुनरूत्थानवाद से जुड़ गया।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणः साम्राज्यवादी इतिहास अध्ययन को वास्तविक चुनौती मार्क्सवादी चिंतकों द्वारा मिली। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन की नई दिशा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें अराजनीतिक इतिहास पर बल दिया जाने लगा। यह उपागम भारतीय इतिहास के भौतिकवादी स्वरूप को प्रतिबिम्बित करता है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र तथा संस्कृति को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं।
मार्क्सवादी उपागम में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर दिया जाता है तथा उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। मूलग्रंथों के पारम्परिक स्वरूप का मिलान नृवैज्ञानिक साक्ष्यों से किया जाता है तथा समसामयिक पुरातात्विक साक्ष्यों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। साथ-ही-साथ जलवायु व पर्यावरण संबंधी कारकों को भी महत्व दिया जाता है। इससे साहित्यिक ड्डोतों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में काफी वृद्धि हुई है तथा प्राचीन अतीत पर नया प्रकाश पड़ा है। प्राचीन भारत के अध्ययन में बहुत सारी परंपरागत मान्यताएं ध्वस्त हो गईं। इस उपागम में मगध साम्राज्यवाद के उद्भव के पीछे कतिपय शासकों के व्यक्तिगत पराक्रम के बदले सुस्पष्ट भौतिक कारणों में तलाशा गया। उसी प्रकार ईसा पूर्व छठी शताब्दी में धार्मिक पंथों के उद्भव को उत्पादन अधिशेष की स्थिति से जोड़कर देखा जाने लगा। अशोक की धम्म नीति को उसके उदार दृष्टिकोण का प्रतिफल न मानकर राज्य मशीनरी के सामाजिक दर्शन के रूप में मूल्यांकन किया जाने लगा तथा गुप्तकालीन स्वर्णयुग को कपोल कल्पित करार दिया गया। मिल का काल विभाजन संबंधी मान्यता खण्डित हो गई तथा नई मान्यता के अनुसार, मध्यकाल का उद्भव इस्लाम के आगमन के साथ नहीं, बल्कि छठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ हुआ। इस मध्ययुग की विशेषताए थीं- सामंतवाद, व्यापार-वाणिज्य का पतन, उपजातियों का विकास, ब्राह्मणवादी वर्चस्व में वृद्धि एवं वैश्यों की स्थिति में गिरावट, धर्म के क्षेत्र में तंत्रवाद एवं भक्ति का उद्भव, दर्शन के क्षेत्र में पारलौकिक दृष्टिकोण पर बल, भाषायी क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का उद्भव आदि।
इस प्रकार मार्क्सवादी उपागम ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन के नए परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण आयामों पर कार्य किया है। उदाहरणार्थ- सामाजिक-आर्थिक इतिहास, शहरी इतिहास, स्थानीय क्षेत्रीय इतिहास, पर्यावरण इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल का इतिहास तथा इतिहास लेखन का इतिहास आदि।
Question : निम्नलिखित स्थानों में से किन्हीं पंद्रह स्थानों के, आपको दिए गए नक्शे पर चिह्न लगाइए और अपने नक्शे पर जिन स्थानों के चिह्न लगाए हैं, उन्हीं के बारे में वर्णनात्मक टिप्पणियां लिखिएः
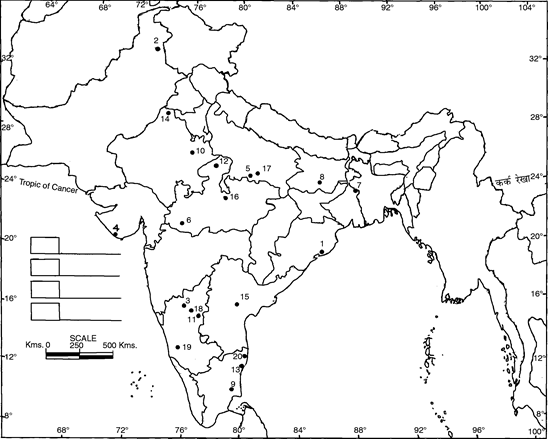
(2006)
Answer : 1. कोणार्कः उड़ीसा प्रान्त में पुरी के निकट, चिल्का झील से प्राची नदी तक फैली हुई रेतीली पट्टी के उत्तरी छोर के, समुद्रतट पर स्थित है। गंगनरेश नरसिंह देव (1238-1363 ई.) द्वारा निर्मित सूर्य मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मन्दिर ‘काले पैगोडा’ के नाम से विख्यात है। सम्पूर्ण मन्दिर पहियों वाले रथ की आकृति में है, जिसे सूर्य के सात घोड़े खींच रहे हैं। इसके 12 पहिये या चक्र 12 राशियों के व सात घोड़े सूर्य की किरणों के सात रंगों के प्रतीक हैं। अबुल फजल ने आईन-ए- अकबरी में मंदिर की स्थापत्य कला की प्रशंसा की है।
2. तक्षशिलाः पाकिस्तान में रावलपिंडी के निकट स्थित है। प्राचीन कालीन गंधार महाजनपद की राजधानी थी। रामायण के अनुसार, भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की। प्राचीन शिक्षा केन्द्र तक्षशिला में प्रसेनजीत, जीवक, चाणक्य, वसुबन्धु, पातंजलि आदि ने शिक्षा ग्रहण की। सिकन्दर के समय आम्भी यहां का राजा था। यह मौर्यकाल में उत्तरापथ की राजधानी थी। प्राचीन प्रसिद्ध व्यापार केन्द्र व मार्ग था। यहां से अशोक कालीन स्तूप व टाइबेरियस के सिक्के प्राप्त हुए हैं।
3. तालीकोटाः यह कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। मध्यकाल में रायचूर दोआब में स्थित होने के कारण इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बहमनी राज्यों की सम्मिलित सेना और विजयनगर के बीच निर्णायक युद्ध 1565 ई. में यहां हुआ, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। विजयनगर की सेना का नेतृत्व रामराजा कर रहा था। इस युद्ध को बन्नीहट्टी या राक्षसीटंगडी का युद्ध भी कहते हैं।
4. सोमनाथः गुजरात के प्रभासपट्टनम् नामक समुद्र तटीय स्थल पर स्थित सोमनाथ अपने प्रसिद्ध शिव मन्दिर के लिए एक हजार से अधिक वर्षों से प्रसिद्ध रहा है। इस मन्दिर का निर्माण गुजरात के चालुक्यों द्वारा करवाया गया था। 1025 ई. में महमूद गजनवी द्वारा इसे लूटा गया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण गुर्जर नरेश भोजदेव ने कराया, परंतु अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खां तथा नुसरत खां ने पुनः इसे तहस-नहस कर दिया।
5. कालिंजरः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला मध्यकाल में बहुत सुदृढ़ माना जाता था। 1022 ई. के अन्त में बुन्देलखंड के शासक गण्ड से कालिंजर लेने का प्रयास महमूद गजनवी ने किया, परन्तु वह सफल नहीं हो सका। 1202-03 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमार्दिदेव को पराजित कर कालिंजर को जीत लिया था। 1545 ई. में शेरशाह सूरी ने बुन्देलों से एक भारी संघर्ष के बाद इसे जीत लिया, परन्तु बारूद फटने से उसकी यहीं मौत हो गई। 1569 ई. में अकबर का इस पर अधिकार हो गया।
6. मांडुः यह मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक नगर है, जिसका प्राचीन नाम मण्डपदुर्ग या माण्डवगढ़ है। मालवा के सुल्तान हुशंगशाह ने धार के स्थान पर मांडू को राजधानी बनाया। 1531 ई. में गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह ने इसे जीत लिया। अकबर के समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। जामी मस्जिद, हिन्डोला महल, हुशंग की कब्र, जहाजमहल, बाजबहादुर और रानी रूपमती के महल मांडू दुर्ग में स्थित हैं। 1625 ई. में खुर्रम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर मांडू में शरण ली।
7. मुर्शिदाबादः आधुनिक पश्चिम बंगाल में भागीरथी के तट पर स्थित इस नगर का उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। मूलतः यह मखसूदाबाद था, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। 1704 ई. में मुर्शिद कुली खां ने इसका नाम मुर्शिदाबाद कर दिया और बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानान्तरित कर दी। 1773 ई. में कलकत्ता के राजधानी बनने तक मुर्शिदाबाद ही बंगाल की राजधानी रही। रेशमी वस्त्र, मिट्टी के बर्तन तथा हाथीदांत के सुन्दर काम के लिए प्रसिद्ध मुर्शिदाबाद नगर में नवाब का भव्य महल स्थित है।
8. नालन्दाः बिहार में राजगृह के पास स्थित यह बारागांव के नाम से भी जाना जाता है। नालन्दा में स्थित विश्वविद्यालय की स्थापना का क्षेत्र कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। हर्ष एवं पाल काल में यह विश्वविद्यालय चरमोत्कर्ष पर था। ह्नेनसांग ने यहां छः वर्षों तक रहकर अध्ययन किया। इस समय शीलभद्र इसके कुलपति थे। संभवतः कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने इसका विनाश कर दिया। इसके ध्वंसावशेष आज भी देखे जा सकते हैं।
9. तंजौरः तमिलनाडु में कावेरी तट पर स्थित तंजौर पूर्व मध्यकाल में चोल साम्राज्य की राजधानी था। राजराज प्रथम ने यहां वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका शिखर 190 फुट ऊंचा है। चोलों के बाद तंजौर पर होयसलों और पाण्ड्यों का राज्य हुआ। मलिक काफूर ने तंजौर को लूटा। तदन्तर विजयनगर साम्राज्य, नायकवंश तथा मराठों का इस पर अधिकार स्थापित हुआ।
10. अम्बर: राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर का पुराना नाम अम्बर या आमेर था। यह शीशमहल एवं भव्य किलों के लिए प्रसिद्ध है। 1128 ई. में ग्वालियर से आए कछवाहा राजपुत दुल्हा राय द्वारा इसे स्थापित किया गया। लगभग 700 वर्षो (1036 ई. से 1727 ई.) तक कछवाहा राज्यों की राजधानी रहने का इसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1727 ई. में सवाई जयसिंह ने जयपुर को लाल पत्थरों से निर्मित कराकर अपनी राजधानी बनाया। 1562 ई. में कछवाहा राजा भारमल ने स्वेच्छा से अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया। सिटी पैलेस, हवा महल तथा जंतर-मंतर यहां स्थित हैं।
11. अनेगोंडीः कर्नाटक के रायचूर जिला में तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर अवस्थित है। हरिहर प्रथम ने इसे विजयनगर की राजधानी बनाया था। नगर के दूसरी ओर हम्पी के खंडहर हैं, जहां सोलहवीं शताब्दी में ऐश्वर्यशाली विजयनगर स्थित था। तालिकोटा के युद्ध में हम्पी और अनेगोंडी दोनों का विनाश कर दिया गया। ‘ओंचा अप्पमठ’ के स्तम्भ तथा गणेश मन्दिर की पाषाण जालियां तथा सुन्दर उत्कीर्ण मूर्तियां कला के सुन्दर नमूने हैं।
12. चंदेरीः मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में मालवा और बुन्देलखण्ड की सीमा पर स्थित था। मालवा और उत्तरी भारतकी मुख्य सड़कों के पास से गुजरने के कारण चंदेरी का आर्थिक- राजनैतिक महत्व था। पूर्व मध्यकाल में चन्देरी मालवा के अधीन था, परन्तु मेदिनी राय ने मेवाड़ के राजा सांगा की अधीनता स्वीकार कर ली। बाबर ने 1528 ई. में चन्देरी के मेदिनी राय को पराजित किया। 18वीं सदी के अन्तिम चरण में यह सिंधिया के अधीन आ गया।
13. अरिकामेडूः अरिकामेडु पाण्डिचेरी के समीप कोरोमण्डल तट पर स्थित है। संगमकालीन इस प्रसिद्ध बन्दरगाह की खुदाई से रोम-भारत व्यापारिक संबंध प्रमाणित होता है। यहां से रोमन माल गोदाम, रोमन स्वर्ण सिक्के तथा रोमन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। विभिन्न वस्तुओं के बदले रोमन स्वर्ण भारत आता था। पेरिप्लस में इसे पेडोका कहा गया है।
14. कालीबंगनः यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घद्वघर नदी के तट पर स्थित है। पूर्व हड़प्पा काल और हड़प्पा काल के कुछ प्रमाण यहां से मिले हैं। हलकुण्ड, सात अग्निवेदिकाएं, अलंकृत ईंट, अधिकतम बुर्ज, गढ़ी के अन्दर भी विभाजन, नाली (लकड़ी निर्मित) आदि महत्वपूर्ण साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज अमलानन्द घोष ने की थी।
15. नागार्जुनीकोण्डाः आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित इस स्थल से नवपाषाणकालीन और महापाषाणकालीन चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सातवाहन शासक हाल ने श्रीपर्वत पर नागार्जुन के लिए एक विहार बनवाया था। इक्ष्वाकुओं ने अपनी राजधानी अमरावती से हटाकर यहां अपनी राजधानी बनायी और इसे ‘विजयपुरी’ कहा। बौद्ध धर्म के महासांघिक सम्प्रदाय के पूर्वशैल एवं अपरशैल पंथों का यह केन्द्र था।
16. एरणः मध्यप्रदेश के सागर जिले में स्थित एरण या एरिकिन भारत में सतीप्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है। भानुगुप्त के 510 ई. के एक अभिलेख में उसके सामन्त गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तोरमाण के समय एक सरदार धन्यविष्णु द्वारा वाराह प्रतिमा पर लेख अंकित करवाया गया। इसकेअतिरिक्त समुद्रगुप्त का लेख तथा रामगुप्त के सिक्के भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के अभिलेख को कनिंघम ने खोजा था, जो कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है।
17. कौशाम्बीः इलाहाबाद के दक्षिण-पश्चिम में 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। ई.पू. छठी शताब्दी में यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। यहां बुद्ध ने कई बार धर्मोपदेश दिए। घोषिताराम विहार तथा एक अशोक स्तम्भ यहां स्थित था। प्राचीन काल में यह व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था।
18. पट्टडकलः यह कर्नाटक प्रान्त के बीजापुर जिले में बादामी के नजदीक अवस्थित है। 992 ई. के एक लेख से ज्ञात होता है कि यह चालुक्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। चालुक्य वास्तु तथा तक्षणकला के इस केन्द्र से दस मन्दिर मिले हैं। विक्रमादित्य द्वितीय की रानी द्वारा 740 ई. में बनवाया गया विरूपाक्ष मन्दिर सर्वाधिक आकर्षक है। अन्य मन्दिरों में पापनाथ मन्दिर तथा संगमेश्वर मन्दिरप्रमुख हैं। पूर्णतया पाषाण निर्मित इन मन्दिरों को उत्तरी और दक्षिणी भारत के वास्तुकला के बीच की कड़ी कहा जा सकता है।
19. हेलिविडः कर्नाटक के हसन जिले में स्थित है। 1149 ई0 से 1339 ई. तक यहां होयसलों ने शासन किया। होयसल वास्तुकला के लिए स्थान प्रसिद्ध है। विष्णुवर्द्धन द्वारा होयसलेश्वर मन्दिर का निर्माण यहां करवाया गया। यह 160'×122' के आकार में है। पत्थरों पर संगतराशी का कार्य इसकी प्रमुख विशेषता है। मन्दिर की दीवारों पर देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि की सुन्दर एवं आकर्षक मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कई जैन मन्दिर भी यहां प्राप्त हुए हैं। इनमें पार्श्वनाथ का मन्दिर प्रमुख है, जिसमें उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा रखी हुई है। दो अन्य मन्दिरों में ऋषभदेव तथा शान्तिनाथ की प्रतिमायें भी हैं।
20. द्वारसमुद्रः द्वारसमुद्र होयसल शासक वीर वल्लाल तृतीय की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1310 ई. में मलिक काफूर को यहां भेजा गया जिसने वीर वल्लाल तृतीय को हराकर, द्वारसमुद्र को लूटा। यद्यपि द्वारसमुद्र का साम्य हेलेविड से स्थापित करने का प्रयत्न कुछ इतिहासकार करते हैं, परन्तु यह उचित प्रतीत नहीं होता है। संभवतः द्वारसमुद्र तमिलनाडु के उत्तर-पूर्व में स्थित था।
Question : समुद्रगुप्त के अधीन गुप्त साम्राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए।
(2006)
Answer : समुद्रगुप्त एक महान विजेता था, जिसने अपने बाहुबल से उत्तराधिकार में प्राप्त एक छोटे से राज्य को विस्तृत कर एक सुदृढ़ साम्राज्य में परिणत कर दिया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में चंबल नदी तक फैला हुआ था। दक्षिण के 12 राज्यों पर भी उसने विजय प्राप्त की और उनसे कर वसूला था। इसके अतिरिक्त उसके पड़ोसी राज्य, जैसे-सिंहलद्वीप, शक और कुषाण उसके आश्रित थे तथा समुद्रगुप्त के कृपा की आकांक्षा रखते थे। यद्यपि वे उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, तथापि उसकी सत्ता को मानते थे। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य और उसके प्रभुत्व का विस्तार दूर-दूर तक किया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार ‘धरणिबन्ध’ (सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतना) उसका उद्देश्य था।
समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार अपने दिग्विजय की नीति के आधार पर किया। उसकी नीति कुछ सिद्धांतों पर आधारित हैः
1. ‘प्रसभोद्धरण’: इस नीति का पालन उत्तरी भारत में किया गया, जिसमें विजय प्राप्ति के बाद विजित प्रदेशों का साम्राज्य में विलय कर लिया गया।
2. ‘ग्रहणमोक्षानुग्रह’: राज्यों को जीतकर स्वतंत्रता प्रदान कर देना। इस नीति का अनुसरण दक्षिण भारत में किया गया।
3. सेवक बनानाः ‘परिचारकीकृत सर्वाटविक राज्यस्य’ अर्थात् सभी आटविक राज्यों को उसने सेवक बना लिया।
4. ‘सर्वकरदान, आज्ञाकरण प्रणामागन’: उसकी आज्ञा का पालन करना, सभी कर देना तथा उसे प्रणाम करने राजसभा में उपस्थित होना। सीमावर्ती तथा गणतंत्रीय राज्यों के साथ इस नीति का पालन किया गया।
5. ‘आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरूत्मंदक-स्वविषय- भुक्ति-शासन याचनाः अर्थात् सम्राट के सामने स्वयं उपस्थित होकर अपनी कन्याओं का गुप्त राजघराने में विवाह तथा अपने राज्यों में शासन के निमित्त गरूड़ मुद्रा से अंकित राजाज्ञा के लिए प्रार्थना करना। विदेशी शक्तियों के साथ इस नीति का पालन किया गया। प्रयाग-प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में दो बार आक्रमण किया। पहले आक्रमण में उसने केवल तीन राजाओं को पराजित किया-
संभवतः अच्युत अहिच्छत्र (बरेली) का, नागसेन ग्वालियर के निकट का तथा कोतकुलज दिल्ली व पूर्वी पंजाब का शासक था।
आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के बाद दक्षिणापथ को जीतकर उसने स्वतंत्रता प्रदान कर दी। दक्षिणापथ का अर्थ विन्ध्यपर्वत से लेकर कृष्णा-तुंगभद्रा के बीच के प्रदेश से है।
समुद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य स्वीकार करवाने के बाद उनसे कर व उपहार प्राप्त किया। उन्मूलित राजवंशों को पुनः प्रतिष्ठित करने के कारण उसकी कीर्ति सम्पूर्ण जगत में फैल गई। रायचौधरी ने इस विजय की तुलना रघुवंश में वर्णित महाराज रघु के धर्म विजय से की है। दक्षिणापथ के पराजित शासकों के क्षेत्र थे-
(i) अवमुक्त (ii) एरण्डपल्ल (iii) देवराष्ट्र (iv) कच्ची (v) कौट्टूर (vi) कौसल (vii) कौराल (viii) कुस्थलपुर (ix) महाकान्तर (x) पालक्क (xi) पिष्टपुर तथा (xii) वेगी।
दक्षिणापथ के विजय द्वारा उसने अपने प्रभुत्व का विस्तार उड़ीसा के केन्द्रीय प्रान्तों के दक्षिणी-पूर्वी तट से होता हुआ पल्लव राज्य की राजधानी कांची तक कर दिया। दक्षिणापथ में उसकी नीति उसके दूरदर्शी एवं यथार्थवादी होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राज्य से अधिक दूरी के कारण इस पर प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं था।
दक्षिणापथ के अभियानों के बाद समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत पर पुनः विजय अभियान का संचालन किया। संभवतः आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में परास्त शासकों ने राजधानी से उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर पुनः स्वतंत्र होने की चेष्टा की। अतः उसने पुनः अभियान कर, इन्हें पूर्णतया उखाड़ फेंका। यहां उसने नौ राजाओं को पराजित किया- (i) अच्युत (ii) बलवर्मन (iii) चन्द्रवर्मन (iv) गणपतिनाग (v) मत्तिल (vi) नागसेन (vii) नागवर्मन (viii) नन्दिन तथा (ix) रूद्रदेव।
इनके राज्यों का साम्राज्य में विलय कर लिया गया। यद्यपि इन राज्यों की पहचान विवादित है, तथापि रूद्रदेव को कौशाम्बी, मत्तिल को बुलन्दशहर, चन्द्रवर्मा बांकुडा जिले का गणपतिनाग मथुरा का, नागसेन, पद्मावती का शासक माना जा सकता है।
अर्थात् समस्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक भाग तक साम्राज्य-विस्तार हो गया। संभवतः समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों के समय आटविक राज्यों ने उसके मार्ग में अवरोध पैदा किया था। अतः आटविक राज्यों को जीतकर उसने पूर्णतया अपने नियंत्रण में कर लिया। फ्रलीट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के वन प्रदेशों में ये राज्य फैले हुए थे।
समुद्रगुप्त से भयभीत होकर सीमावर्ती राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सीमावर्ती राज्यों को न तो उसने अपने राज्य में मिलाया और न ही भेंट स्वीकार कर उनको मुक्त किया बल्कि इन राजाओं पर उसने इस प्रकार का वर्चस्व स्थापित किया कि वे उसके आदेश का पालन करते थे, सभी कर देते थे तथा उसे प्रणाम करने राजधानी में उपस्थित होते थे।
उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी सीमा पर स्थित ऐसे सीमावर्ती राज्यों की संख्या पांच थी-
(i) समतट (ii) डबाक (iii) कामरूप (iv) कतृपुर (v) नेपाल इनमें समतट, डबाक और कामरूप का तात्पर्य पूर्वी बंगाल एवं असम से, कर्तृपुर का जालंधर, कुमायूं-गढ़वाल तथा रूहेलखंड से और नेपाल का तात्पर्य आधुनिक नेपाल से है।
इस प्रकार समुद्रगुप्त के नियंत्रण में पूर्वी बंगाल के बन्दरगाह भी आ गए, जिनमें ताम्रलिपि प्रमुख है। पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा स्थित नौ गणराज्यों के साथ भी इसी नीति का पालन
किया गया। इनके नाम हैं-(i) आर्जुनायन (ii) आभीर (iii) काक (iv) खर्परिक (v) मालव (vi) मद्रक (vii) प्रार्जुन (viii) सनकानिक और (ix) यौधेय। ये राज्य पंजाब, मालवा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के विभिन भागों में फैले हुए थे।
हरिषेण के अनुसार, समुद्रगुप्त के पराक्रम का भय विदेशी शासकों पर भी छा गया तथा कुछ विदेशी शासकों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की। ये शासक हैं-(i) दैवपुत्रषाहानुषाहि (ii) शक (iii) मुरूण्ड (iv) सिंघल
देवपुत्रषाहानुषाहि का तात्पर्य कुषाणों से है, जो पश्चिमी पंजाब व पेशावर में निवास करते थे। शक पश्चिमी मालवा, गुजरात व काठियावाड़ के शासक थे। सिंघल का तात्पर्य लंकाद्वीप से है, जिसके शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूतमंडल भेजा तथा बोधगया में विहार बनवाने की अनुमति प्राप्त की। इनके अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ द्वीपों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की ऐसा प्रतीत होता है।
अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के फलस्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो हिमालय से लेकर विंध्यपर्वत तक तथा बंगाल की खाड़ी से पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी राजपूताना, सिन्ध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। दक्षिणापथ तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता स्वीकार करती थी। विजय अभियानों के बाद उसने अवश्मेध यज्ञ का आयोजन किया, जो अभिलेखों और सिक्कों से प्रमाणित होता है। इस प्रकार अपने पिता से प्राप्त राज्य को उसने एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया।
Question : प्राचीनकाल के दौरान वास्तुकला के विकास में प्रमुख चरणों पर चर्चा कीजिए।
(2006)
Answer : प्राचीनकाल में वास्तुकला के विभिन्न विधाओं का विकास कई चरणों में हुआ। प्राचीन काल के वास्तुकला के विकास के इन चरणों के बीच एक सातत्य भी देखने को मिलता है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति के उपयोगी ईंटों के भवन दृढ़ एवं उपयुक्त थे, फिर भी उनमें सौन्दर्यात्मक महत्व का अभाव है। अतः यहां उनका वर्णन आवश्यक नहीं है। पुनः हड़प्पा काल और मौर्यकाल के बीच भी राजगृह के राजप्रसाद (जिसका भी कोई कलात्मक महत्व नहीं है) के अतिरिक्त कोई प्रसिद्ध वास्तुकला के अवशेष नहीं मिले हैं। अतः प्राचीन वास्तुकला के विकास के निम्नलिखित प्रमुख चरण हैं-
मौर्यकालीन वास्तुकलाः स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य-युग में ही सुसंगठित क्रिया-कलाप के दर्शन होते हैं। मौर्यकाल के पूर्व कलात्मक वस्तुओं का प्रयोग होता था। संभवतः इसी कारण वास्तुकला का मौर्य पूर्व साक्ष्य बहुत कम प्राप्त होता है। मौर्य युग में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग कि गया, फलतः कलाकृतियां चिरस्थायी हो गयीं। पाटलिपुत्र का राज प्रासाद, सूसा और एकबतना के राजप्रसाद से भी भव्य था। मौर्य वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है-नए क्षेत्रों में पहल व शुरुआत। उदाहरणार्थ-गुफाओं का निर्माण तथा स्तूपों का निर्माण ऐसे क्षेत्र हैं, जिनकी शुरुआत मौर्यों ने की। बौद्ध परम्परा अशोक को 84 हजार स्तूपों के निमार्ण का श्रेय प्रदान करती है। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों के बने थे। सांची के महास्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया।
इसके अतिरिक्त सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित धर्मराजिका स्तूप भी मूलतः अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया। विशालकाय तथा अलंकृत स्तूपों के निर्माण की परम्परा मौर्यो के बाद शुरू हुई। मौर्यकाल में गुहा स्थापत्य का पूर्ण विकास हुआ। बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी पर अशोक तथा दशरथ द्वारा बनवाई गई गुफाओं में चमकदार पालिश लगी हुई है। कालान्तर में इन्हीं गुफाओं के अनुकरण पर पश्चिमी भारत में अनेक चैत्यगृहों का निर्माण किया गया।
मौर्योत्तर काल में वास्तुकला का विकासः इस चरण में मुख्यतः गुफा कला तथा स्तूप कला का विकास हुआ। मौर्य काल में स्तूप के निर्माण की निरंतरता मौर्योत्तर काल में भी दृष्टिगोचर होती है। शुगों, कुषाणों, सातवाहनों और इक्ष्वाकुओं की स्तूप निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। शुंगों के समय पुराने स्तूपों को नया रूप प्रदान किया गया तथा भरहूत स्तूप का निर्माण भी हुआ। कुषाण शासक कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप का निर्माण करवाया था पर दक्षिणी क्षेत्र में सातवाहनों तथा इच्छवाकुओं ने अमरावती, नागार्जुनीकोंडा, घण्टशाला जग्यमपेट्ट आदि स्थानों में स्तूपों का निर्माण हुआ। इस चरण में स्तूप निर्माण कला अपने चरम पर था तथा विशालकाय महास्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूपों में अलंकरण की परम्परा की शुरुआत हुई, जिसमें समकालीन जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया। मौर्यकालीन स्तूपों में तीन क्षेत्रें की परम्परा थी, लेकिन इस काल में सात क्षेत्रों की परम्परा शुरू हुई।
यद्यपि इसकी वेदिका सादी तथा अलंकरण रहित है, परन्तु तोरण सुन्दर कलात्मक तथा आकर्षक है। भरहूत के स्तूप की वेदिका अलंकृत है। अमरावती स्तूप की वेदिका तथा गुम्बद में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। 200 ई. पू. से 300 ई. के काल में गुफा कला का विकास मुख्यतः पश्चिमी भारत से जुड़ा है। इस काल में गुफाओं का विकास मुख्यतः चैत्यों तथा विहारों के रूप में हुआ। यह काल गुफा कला के विस्तार, अलंकरण तथा बौद्ध प्रभाव का काल है। गुफा संरचना में एक परिवर्तन की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। इस चरण में पश्चिमी दक्कन में सातवाहन एवं उनके उत्तरावर्ती राजाओं ने बहुत सी बड़ी-बड़ी गुफाएं खुदवाईं। इनमें प्रमुख हैं-भज, कोण्डाने, पीतलखोरा, अजन्ता (9वीं-10वीं गुफा), बेदसा, नासिक, जुन्नार, कार्ले तथा कन्हेरी। कार्ले का चैत्य सर्वाधिक सुन्दर तथा भव्य प्राचीन स्मारकों में से एक है।
इन गुफाओं के आकार में धीरे-धीरे वृद्धि होती गई जैसा कि अजंता एवं एलौरा की गुफाओं से प्रतीत होता है। कार्ले के चैत्य में गुहा वास्तुकला अपने पूर्णता पर पहुंच गयी है। उड़ीसा में उदयगिरि और खण्डगिरि गुहाओं का निर्माण (खारवेल कालीन) इसी चरण में हुआ।
गुप्तकाल में वास्तुकला का विकासः गुप्तकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में मुख्यतः मन्दिर स्थापत्य तथा गुफा स्थापत्य का विकास हुआ। इस काल में संरचनात्मक मंदिरों का विकास नागर शैली के विकास के कुछ तत्वों को समेटे हुए था। जैसे-मंदिरों में गर्भगृह और शिखर का विकास। यही तत्व नागर शैली की परिपक्व अवस्था में तथा उत्तर गुप्तकाल में विशाल रूप धारण करते हैं। गुप्तकाल के मन्दिरों में मुख्यतः पत्थरों का प्रयोग किया गया यद्यपि भीतर गांव का मंदिर ईंटों से निर्मित था। मंदिरों के दरवाजों पर नक्काशी किया जाता था। मन्दिरों के स्तम्भ अलंकृत हैं। मन्दिरों के छत सपाट होते थे, यद्यपि शिखरों के निर्माण का उदाहरण देवगढ़ तथा भीतरगांव के मन्दिरों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
नचनाकुठार तथा भूमरा के मंदिरों में दूसरी मंजिल का विकास भी किया गया था। मंदिरों की योजना मुख्यतः चौकोर है, परन्तु देवगढ़ और भीतरगांती में अष्टभुजाकार योजना भी देखा जा सकता है। गुप्तकाल में वास्तुकला का विकास गुफा-कला के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। गुप्तकाल की महत्वपूर्ण गुफाएं हैं-बाघ, उदयगिरि तथा मंदारगिरि की गुफाएं। पश्चिमी भारत तथा मध्यभारत की गुफाशैली की निरंतरता गुप्तकाल में बनी रही, लेकिन अलंकरण के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही शिल्पकला तथा चित्रकला की बहुलता भी गुप्त गुहा कला की विशेषता है। बाघ की गुफाओं में गुफा नं. 2 का विशेष महत्व है। यह पांडव गुफा कहलाती है। यह सर्वाधिक विस्तृत है। गुफा नंम्बर- 4 को रंगमहल कहा जाता है तथा यह सौन्दर्य की दृष्टि से सर्वोत्तम है। गुप्तकालीन गुफाओं में सामान्यतः अलंकरण का अभाव है। अजन्ता की कई गुफाओं का निर्माण गुप्तकाल में हुआ। प्राचीनकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने इन गुफाओं में पाए गए हैं। सारनाथ का धामेख स्तूप गुप्तकालीन है। यह कल्पना, आकार और अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट है।
Question : मौर्य साम्राज्य के विस्तार का निर्धारण कीजिए।
(2005)
Answer : मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री एवं पुरोहित चाणक्य की सहायता से किया। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की स्थापना के क्रम में सर्वप्रथम पंजाब एवं सिंध को विदेशियों की दासता से मुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विवरण जस्टिन ने दिया है। जस्टिन कहता है-‘सिकंदर की मृत्यु के पश्चात् भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गर्वनरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सैंड्रोकोटस (चंद्रगुप्त) था।’ इस विवरण से चंद्रगुप्त द्वारा सिंध और पंजाब को जीतने तथा अपने साम्राज्य स्थापित करने का पता चलता है। चंद्रगुप्त ने सिंध और पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत कर मगध साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। हालांकि नंदों एवं मौर्यों के बीच होने वाले इस युद्ध का विवरण कहीं नहीं मिलता परंतु बौद्ध एवं जैन स्रोतों में मगध पर चंद्रगुप्त के अधिकार करने का विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस से आरकोसिया (कंधार) और पेरोपनिसडाई (काबुल) के प्रांत तथा एरिया (हेरात) एवं जेड्रोसिया के क्षत्रपियों का कुछ भाग प्राप्त किया। इस उपलब्धि से उसका साम्राज्य की सीमा का अतिक्रमण कर पारसीक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा तथा मौर्य साम्राज्य में अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग भी सम्मिलित हो गया। सेल्युकस से युद्ध तथा इन क्षेत्रों की प्राप्ति का विवरण अप्पिआनुस तथा स्ट्रेबो ने दिया है। शकमहाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से इस बात की सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीत कर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत ले आया था। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसने एक झील का निर्माण किया था।
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत की विजय कर साम्राज्य विस्तार करने के संबंध में जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, जैसे -सिद्धपुर, ब्रह्मगिरि, जटिंग-रामेश्वर पहाड़ी, मास्की आदि। अशोक के तेरहवें शिलालेख से ज्ञात होता है कि दक्षिण में उसने केवल कलिंग की ही विजय की थी, जिसके पश्चात उसने युद्ध कार्य पूर्णतया बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक की विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत की विजय की जानकारी जैन एवं तमिल स्रोतों से भी मिलती है। जैन परंपरा के अनुसार अपनी वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की तथा दोनों ‘श्रवणबेलगोला’ नामक स्थान पर आकर बस गए। यहीं चंद्रगिरि नामक पहाड़ी पर चंद्रगुप्त ने तपस्या किया।
यदि इस परंपरा पर विश्वास किया जाय तो श्रवणबेलगोला तक उसका अधिकार प्रमाणित होता है। तमिल परंपरा से भी पता चलता है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण क्षेत्र में ‘मोहर’ के राजा पर आक्रमण किया। इस प्रकार तमिल परंपरा से भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण विजय के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कलिंग प्रांत तथा सुदूर दक्षिण एवं सुदूर पूर्वी भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत शामिल था। इसकी पुष्टि प्लूटार्क तथा जस्टिन के विवरण से भी होती है। प्लूटार्क लिखता है कि -‘उसने छः लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। जस्टिन भी कुछ इसी प्रकार विवरण देता है। निष्कर्षतः चंद्रगुप्त के समय मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी तथा पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी।
बिंदुसार के समय साम्राज्य विस्तार के बारे में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती। ऐसा लगता है कि बिंदुसार ने अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। हालांकि बिंदुसार के समय कुछ प्रदेशों में विद्रोह हुए, जिसे उसने सफलतापूर्वक शांत कर दिया। जैसा कि दिव्यावदान से तक्षशिला में विद्रोह होने का विवरण मिलता है, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पुत्र अशोक को भेजा। संभव है कि इसी प्रकार के कुछ अन्य विद्रोह पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशों में भी हुए होंगे, लेकिन बिंदुसार ने इन विद्रोहों को शांत कर अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा।
अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण उसके अभिलेखों के आधार पर कर सकते हैं। उत्तर-पश्चिम में पेशावर जिले में स्थित शहबाजगढ़ी तथा हजारा जिले में स्थित मानसेहरा से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कंदहार के समीप शरेकुना तथा जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित लघमान से अशोक के अरामेइक लिपि के लेख मिले हैं। इन अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों से पता चलता है कि उसके साम्राज्य में हिंदूकुश, एरिया (हेरात), आरकोसिया (कंधार) तथा जेड्रोसिया सम्मिलित थे। चीनी यात्री हवेनसांग उल्लेख करता है कि कपिसा में उसने अशोक का स्तूप देखा था। स्पष्ट है कि अशोक के समय भी अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। उत्तर में कलसी (उत्तरांचल के देहरादून जिले में) रुम्मिनदेई तथा निग्लीवा के स्तंभ लेख इस बात का प्रमाण हैं कि हिमालय क्षेत्र का एक बड़ा भाग, जिसमें नेपाल की तराई शामिल है। मौर्य साम्राज्य का भाग था। ब्रह्मगिरि, मास्की, सिद्धपुर के अभिलेख कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुए हैं। इससे इस काल में मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा कर्नाटक राज्य तक पहुंच जाती है। अशोक ने अपने द्वितीय शिलालेख में चोल, पाण्ड्य, सत्तियपुत्त, केरलपुत्त साम्राज्य के दक्षिणी सीमा पर स्थित स्वतंत्र राज्य थे। इससे स्पष्ट है कि सुदूर दक्षिण के भाग को छोड़कर संपूर्ण भारत अशोक के अधिकार में था। पश्चिम में कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी तथा उसके दक्षिण में महाराष्ट्र में सोपारा नामक स्थान से उसका शिलालेख मिला है। इसके अलावा तेरहवें शिलालेख में पता चलता है कि अशोक ने अपने अभिषेक के आठवें वर्षकलिंग को जीता था।
इसके अलावा उड़ीसा के दो जगह धौली एवं जौगढ़ से भी उसके शिलालेख मिलते है। बंगाल में ताम्रलिप्ति से प्राप्त स्तूप उसके उस स्थान पर आधिपत्य होने का प्रमाण हैं। हवेनसांग हमें बताता हैकि अशोक के स्तूप समतट, पुण्ड्रवर्धन, कर्णसुवर्ण आदि में भी विद्यमान थे। इन सभी अभिलेखों की प्राप्ति स्थानों से स्पष्ट हो जाता है कि उसके समय मौर्य साम्राज्य उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता हैकि उसका कश्मीर पर भी अधिकार था। इसके अनुसार उसने वहां अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवायी थी। कल्हण अशोक को कश्मीर का प्रथम शासक बताता है। इस विवरण से अशोक के समय मौर्यों का कश्मीर पर अधिकार की पुष्टि होती है तथा मौर्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत तक जाती है।
अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा विस्तार के संबंध में हमारा ज्ञान अपर्याप्त तथा अनिश्चित है। पुराण, बौद्ध एवं जैन आदि अनुश्रुतियों के आधार पर साम्राज्य के विघटन की सूचना मिलती है। पुराणों के अनुसार अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। राजतरंगिणी हमें बताता है कि जालौक कश्मीर का स्वतंत्र शासक बन गया। तारानाथ के अनुसार गांधार का स्वतंत्र शासक वीरसेन बन गया। स्पष्ट है कि इस समय मौर्य साम्राज्य की विशाल सीमा छिन्न-भिन्न हो गयी। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुणाल का उत्तराधिकारी संप्रति के होने का पता चलता है। इधर पुराणों तथा नागार्जुनी पहाडि़यों की गुफाओं के शिलालेखों से दशरथ को कुणाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी होने का प्रमाण मिलता है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि इस समय मगध साम्राज्य का दो भागों में विभाजन हो गया। दशरथ का अधिकार साम्राज्य के पूर्वी भाग में तथा संप्रत्ति का साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार था। इस प्रकार विशाल मौर्य साम्राज्य का सीमा विस्तार अशोक के बाद सिमटने लगा तथा अंतिम मौर्य शासन बृहद्रथ की उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग द्वारा हत्या किए जाने के साथ ही इस विशाल साम्राज्य की भी समाप्ति हो गई और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के एक छोटे से भाग पर एक नवीन राजवंश शुंगों की सत्ता स्थापित हुई।
Question : गुप्त वंश की प्रशासनिक प्रणाली के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं?
(2005)
Answer : मौर्य वंश के पतन के पश्चात गुप्तों ने उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। गुप्तों ने अपने साम्राज्य में प्रशासन के लिए जो व्यवस्था स्थापित किया, वह पूर्ववर्ती मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था से भिन्न तथा विशिष्ट था। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के उन विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है जो पूर्ववर्ती मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ, वह इसके बाद के प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण बन गए।
गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था भी राजतंत्रत्मक थी। प्रशस्तिकारों ने गुप्त सम्राटों की महानता को दिखाने के लिए उनकी तुलना यम, कुबेर आदि देवताओं के साथ की है। लगता है कि मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी दैवी उत्पति में विश्वास करने लगे थे, लेकिन जनता में यह धारणा अभी तक ज्यादा मजबूत नहीं हुई थी। गुप्त शासकों ने स्वयं को अन्य छोटे शासकों पर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए बड़ी-बड़ी उपलब्धियां, जैसे महाराजाधिराज, परमभट्टरक, एकराट, परमेश्वर आदि धारण की तथा अश्वमेघ यज्ञ किया। इन सब बातों के होते हुए भी शासक को विधि नियमों के उल्लंघन की इजाजत नहीं थी। सम्राट प्रशासन का मुख्य स्रोत था। जिसके अधिकार और शक्तियां असीमित थीं। वह कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का प्रधान न्यायाधीश एवं सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। युद्ध के समय वह सेना का संचालन करता था। प्रशासन के सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाती थी और वे सभी उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार सिद्धांत में सम्राट की स्थिति एक निरंकुश शासक जैसी थी। परंतु व्यवहार में वह पर्याप्त अंशों में उदार तथा जनहितकारी होता था।
इस काल के प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता केंद्रीय नियंत्रण में कमी होना है। केंद्रीय शासन का जो नियंत्रण मौर्य युग में देखने को मिलता है, वह गुप्त युग में नहीं मिलता। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति गुप्त युग से ही बढ़ने लगी तथा हर्ष तथा उसके बाद यह प्रवृत्ति प्रमुख हो गई। समुद्रगुप्त ने अनेक शासकों को पराजित कर अपने अधीनता में शासन करने की छूट प्रदान की। उसने इन पराजित राज्यों को अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग नहीं बनाया। इन पराजित शासकों के अलावा भी सम्राट के अधीन अनेक छोटे-छोटे सामंत थे, जो अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे तथा नाममात्र के लिए सम्राट की अधीनता स्वीकार करते थे। इस प्रकार के छोटे शासकों में सनकानीक महाराज तथा परिव्राजक महाराज हस्तिन का उल्लेख किया जा सकता है।
सम्राट अपने शासन कार्य में अमात्यों, मंत्रियों एवं अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था। अमात्य प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग था जिसे योग्यता के आधार पर मंत्री नियुक्त किया जाता था। मंत्री का मुख्य कार्य राजा को मंत्रणा देना था तथा वह किसी गूढ़ विषय पर अपना निर्णय भी सम्राट को बता सकता था। कामंदक और कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि गुप्तकाल में मंत्रिपरिषद नामक संस्था मौजूद थी। प्रयाग प्रशस्ति में भी राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। राज्य का विभिन्न विभाग इन मंत्रियों के अधीन ही होते थे। गुप्तकालीन लेखों से तो ऐसा लगता है कि विभागीय अध्यक्षों और मंत्रियों में कोई खास अंतर नहीं था। सैनिक योग्यता मंत्रियों के लिए अनिवार्य थी। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त के युद्ध सचिव हरिषेण एवं वीरसेन उच्चकोटि के सेनानायक भी थे।
गुप्त प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि एक ही व्यक्ति को कभी-कभी कई पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था। जैसे कि प्रयाग-स्तंभ लेख से पता चलता है कि हरिषेण एक साथ कुमारामात्य, संधिविग्रहिक और महादंडनायक नामक तीनों पदों को धारण करता गया। कुछ पदों को आनुवंशिक रूप से भी दे दिया गया था। मध्य भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि एक ही परिवार की पांच पीढि़यों तक उच्च पदस्थ पदाधिकारी नियुक्त किए गए। करमदंडा अभिलेख के अनुसार पिता-पुत्र दोनों ने गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत मंत्री व कुमारामात्य का पद धारण किया। इसी प्रकार पर्णदत्त एवं चक्रपालित तथा शिखरस्वामी एवं पृथ्वीषेण का उदाहरण दिया जा सकता है। इस काल में राज्याधिकारियों में से कुछ को नकद वेतन के बदले भूमिदान दिया जाने लगा। इससे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला।
प्रशासनिक सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी ‘उपरिक’ था। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा वह सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। सीमांत प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारी ‘गोप्ता’ होता था तथा यह भी सम्राट द्वारा ही नियुक्त किया जाता था। सामान्यतः उपरिक पद पर राजकुमार अथवा राजकुल के किसी योग्य व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था पर इसके अपवाद भी मिलते हैं।
‘भुक्ति’ से छोटा प्रशासनिक इकाई विषय होता था। इसके प्रधान अधिकारी ‘विषयपति’ होता था। विषयपति की नियुक्ति प्रांत के उपरिक द्वारा ही किया जाता था। हालांकि कभी-कभी स्वयं सम्राट भी उसे नियुक्त करता था। विषयपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए विषय-परिषद होता था। इसके सदस्य नगर श्रेष्ठि, सार्थवाह, प्रथम कुलिक व प्रथम कायस्थ होते थे।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम का शासन ग्रामिक, ग्रामजनपद और ग्राम परिषद की सहायता से करते थे। एक अन्य प्रशासनिक इकाई ‘पेठ’ का उल्लेख मिलता है, जो कई ग्राम को मिलाकर बनायी गयी थी।
प्रमुख नगरों का प्रबंध नगरपालिकाओं के माध्यम से किया जाता था। ‘पुरपाल’ नगर का प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता था। ऐसा लगता है कि नगर प्रशासन में सहायता देने के लिए भी एक समिति होती थी।
गुप्तकालीन लेखों में न्याय-विभाग का उल्लेख नहीं है। किंतु इस काल के स्मृतियों विशेषकर नारद एवं बृहस्पति से गुप्तकालीन न्याय-व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। इस युग में न्याय व्यवस्था पूर्वकाल की तुलना में अत्यधिक विकसित थी। इस काल में प्रथम बार दीवानी तथा फौजदारी अपराधों से संबंधित कानूनों की व्याख्या की गई। उत्तराधिकार संबंधी विस्तृत कानूनों का निर्माण किया गया। सम्राट ही देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था जो सभी मामलों की सुनवाई कर सकता था। सम्राट के अलावा प्रांतों में भी न्यायालय होते थे जो अपने अधिकार क्षेत्र में न्याय का कार्य करते थे। व्यापारियों एवं व्यवसायियों की श्रेणियां भी अपने सदस्यों के संबंध में न्याय कार्य करती थीं। न्यायाधीशों को दण्डात्मक सर्वदण्डनायक, महादण्डनायक आदि कहा जाता था। फाहियान से पता चलता है कि दण्ड विधान अत्यंत कोमल थे। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और न ही शारीरिक यातनाएं मिलती थीं।
गुप्तकाल में सिद्धांततः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। राजकीय भूमि के अलावा निजी स्वामित्व की भूमि भी थे। मंदिर तथा ब्राह्मणों को दान में ‘अग्रहार’ नामक भूमि दी जाती थी। इस प्रकार की भूमि सभी करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के अनुदान को सम्राटग्रहीता के आचरण से अप्रसन्न होकर समाप्त कर सकता था तथा दूसरे योग्य व्यक्ति को दे सकता था। चूंकि राजा भूमि का मालिक था। अतः भूमि से प्राप्त उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस प्रकार भूमिकर को ‘भाग’ के नाम से जाना जाता था। एक दूसरा भूमिकर ‘भोग’ कहलाता था। यह राजा को प्रतिदिन फल-फूल, शल्यी आदि के रूप में दिया जाता था इसे ‘भोग’ कहा जाता था। ‘भाग’ एवं ‘भोग’ के अलावा गुप्त अभिलेखों में ‘उद्रंग’ और ‘उपरिकर’ नामक करों के नाम मिलते हैं। भूमिकर नकद या अनाज के रूप में लिया जाता था। भूमिकर संग्रह करने के लिए ‘ध्रुवाधिकरण’ नामक विभाग था जो महाक्षपाटलिक और करणिक नामक अधिकारी सेइस कार्य में सहायता प्राप्त करता था। राजस्व का दूसरा प्रमुख स्रोत चुंगी थी, जो नगर में आने वाली वस्तुओं के ऊपर लगायी जाती थी।
इस प्रकार गुप्त प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को देखने पर इसकी विशिष्टता स्पष्ट हो जाती है। गुप्त प्रशासन की मुख्य विशिष्टता विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का उदय होना है। ऐसा प्रशासन में सामंती तत्वों के उदय, विभिन्न उच्च पदों का आनुवांशिक बना देने तथा पदाधिकारियों को भूमिदान देने के कारण हुआ। गुप्त प्रशासन में उपर्युक्त नवीन प्रवृत्तियों का जो उदय हुआ। उसी का विकास हम हर्ष के समय तथा पूर्वमध्य काल में देखते हैं।
Question : ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से छठीं शताब्दी ईस्वी तक भारत में महिलाओं की परिस्थिति का आकलन कीजिए।
(2005)
Answer : वैदिक काल की समाप्ति के साथ स्त्रियों की दशा में निरंतर गिरावट आने लगी। उनके अधिकारों में जिस अनुपात से कटौती की गयी उसी अनुपात से कर्तव्यों में वृद्धि की गई। छठीं शताब्दी ई. तक स्त्रियों के अधिकार लगभग पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा समाज एवं परिवार के प्रति दायित्वों की बोझ लाद दी गई। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी तक कन्या का जन्म अभीष्ट नहीं रहा। स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया गया तथा विवाह के अलावा अन्य सभी संस्कारों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण बंद हो गया। कन्याओं के विवाह की आयु भी पूर्वकाल की तुलना में कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसका विधिवत शिक्षा पाना कठिन हो गया। ईसा की पहली शताब्दी से कन्याओं का विवाह 12-13 वर्ष की अवस्था में होने लगा। इस काल में अधिक आयु तक कन्याओं का अविवाहित रहना पाप समझा जाने लगा। इस धारणा के पीछे मुख्य कारण शायद स्त्रियों का बौद्ध और जैन संघों में शामिल होना रहा है क्योंकि अनेक स्त्रियां संघों में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मचर्य का यौवन नहीं बिता पाती थी, जिससे समाज में उनकी निंदा होती थी। इसके अलावा अविवाहित स्त्रियों को समाज में विवाहित स्त्रियों से अधिक जोखिम उठाना पड़ता था। इस कारण भी कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। जब कन्याओं का विवाह कम आयु में होने लगा तो पति का पत्नी के प्रति स्थिति आचार्य जैसी हो गई। मनु ने बिना किसी बड़े अपराध के पति को अपनी पत्नी का परित्याग करने की अनुमति देता है। हालांकि ई.पू. चौथी शताब्दी में स्त्रियों को यज्ञ तथा कर्मकांडों में अपने पति के साथ उपस्थिति औपचारिकता के रूप में बरकरार रही, लेकिन छठीं शताब्दी ई. तक यह औपचारिकता भी समाप्त हो गई। इस काल के आरंभ से ही स्त्रियों की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगना प्रारंभ हो गया तथा छठीं शताब्दी के पहले ही उनकी सारी स्वतंत्रता छीन ली गई। अब इस धारणा को बल मिला कि ‘स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं। उसे बचपन में पिता के युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए।’
ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक उत्तरी भारत में विदेशी आक्रमणों के कारण समाज में अव्यवस्था फैल गई। इससे स्त्रियों की स्थिति प्रभावित हुई। नियोग तथा पुनर्विवाह की प्रथाएं बंद हो गईं। प्राचीन काल में विधवा स्त्री संतानोत्पति के लिए देवर के साथ सहवास करती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। यह प्रथा ई. 300 तक जारी रही, किंतु इसके बाद के धर्म शास्त्रकारों ने इस प्रथा का विरोध किया। पुराणों में इस प्रथा को कालिवर्ज्य कहा गया। 600 ई. से पहले ही इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह के स्थापन पर संन्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कुछ समय बाद लगभग पांचवीं या छठीं शताब्दी से सती प्रथा का भी प्रचलन हुआ। इसके अनुसार स्त्रियों का संबंध उनके पति के साथ जन्म-जन्म का मानकर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि विधवा स्त्री को अपने मृत पति के साथ जल जाना चाहिए। इस प्रथा को महान धार्मिक यज्ञ माना गया। इस प्रथा से स्पष्ट है कि स्त्री का अपने पति के बाहर अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं था। इस प्रकार स्त्रियों की दशा और खराब हो गई। धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरता ने इस अमानवीय एवं बर्बर प्रथा को लोकप्रिय बनाया। इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस प्रथा का प्रचलन मुख्यत क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों में ही था। इससे जीमूतवाहन का यह कहना कि इस प्रथा का उद्देश्य स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित करना था, काफी तर्कसंगत लगता है।
ईसा की प्रथम शताब्दी से हम स्त्रियों में पर्दे की प्रथा का चलन देखते हैं। आरंभ में इसका चलन राजवंशों में पाते हैं, जहां महिलाओं को सार्वजनिक दृष्टि से बचाने के लिए पर्दा धारण करने की संस्तुति की गई है। बाद में समाज के सामान्य परिवारों ने भी इसका अनुकरण किया। हालांकि इस प्रथा का व्यापक चलन मुस्लिम आक्रमण के बाद हुआ। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से छठीं शताब्दी के बीच एक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। वैदिक काल तक स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं दिए गए थे। किंतु अब उन्हें संपत्ति में अधिकार दिया गया। इसके अलावा हम इस पूरे काल खंड में स्त्रीधन में क्रमशः विस्तार होते देखते हैं। उदाहरण के लिए मनु ने स्त्रीधन के रूप में विवाह के समय पिता, माता, भाई व अन्य संबंधियों द्वारा दिए गए उपहारों और विवाह के बाद प्रेम से पति द्वारा दिए गए उपहारों को शामिल किया है, तो विष्णु (100-300 ई.) ने स्त्रीधन का विस्तार करके इसमें तीन अन्य प्रकार के धन को शामिल किया है- विवाह के बाद पुत्र द्वारा दिया गया उपहार अन्य संबंधियों से प्राप्त उपहार तथा निर्वाह के लिए दिया गया धन। ऐसा लगता है कि पुनर्विवाह के अभाव में विधवा एवं पुत्रहीन स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। अतः उनके पोषण या जीवन निर्वाह के लिए व्यवस्थाकारों ने उसके धन संबंधी अधिकारों को मान्यता देना प्रारंभ किया।
इस काल खंड में हम स्त्रियों को कुछ व्यवसाय करते हुए भी पाते हैं। कुछ स्त्रियां साहित्य एवं व्याकरण पढ़ाने का कार्य करती थीं। कुछ बौद्ध तथा जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देती थी। भागवतपुराण में दाक्षायण की दो पुत्रियों का वर्णन है जो धर्म-विज्ञान एवं दर्शन में दक्ष थीं।
कुछ स्त्रियां वेश्या का कार्य भी करती थीं। मृच्छकटिकम की नायिका वसंतसेना वेश्या की पुत्री थी। इसी समय मंदिरों में हम देवदासी के रूप में स्त्रियों को कार्य करते देखते हैं। कुछ स्त्रियां राजनीति में भी भाग लेती थीं तथा राजकार्य वह सफलतापूर्वक चला लेती थीं। इसका उदाहरण नागनिका तथा प्रभावतीगुप्त हैं। परंतु इस प्रकार की स्त्रियों की संख्या समाज में काफी कम थी। इसके अलावा कामसूत्र से ज्ञात होता है कि धनी परिवार में कन्याओं को संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी।
एक महत्वपूर्ण बात जो इस कालखंड में हम पाते हैं, वह स्त्रियों और शूद्रों की स्थिति में समानता है। जहां तक नागरिक अधिकारों की बात है तो स्त्री और शूद्र के जीवन का मूल्य एक ही समझा गया। अग्निपुराण में कहा गया कि स्त्री हत्या करने वाले को शूद्र हत्या का व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार दोनों की सामाजिक स्थिति भी लगभग समान थी। इसी कारण संस्कृत नाटकों में ये दोनों संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते बल्कि अपभ्रंश बोलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज में दोनों की स्थिति निकृष्ठ थी।
उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वैदिक काल की समाप्ति के बाद विशेषतः ई.पू. 400 से स्त्रियों के प्रति व्यवस्थाकारों का रुख कठोर होता गया तथा उनके अनेक अधिकार जो पूर्ण काल में दिए गए थे, वह क्रमशः समाप्त करते गए तथा शूद्रों की निर्योग्यता स्त्रियों पर भी लाद दिया गया। हालांकि इन व्यवस्थाकारों ने माता के रूप में तथा पत्नी के रूप में स्त्रियों के गौरव का भी वर्णन किया है। मनु ने स्पष्ट लिखा है कि माता का पद पिता से बढ़कर है। परंतु पुरुषों से अलग एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में इन व्यवस्थाकारों ने स्त्रियों को कोई स्थान नहीं दिया। प्राचीन पितृप्रधान तथा वर्ग विभाजित समाज में स्त्रियों की यह अवस्था स्वाभाविक ही थी।
Question : परवर्ती वैदिक लोगों के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। यह जीवन ऋग्वैदिक जीवन से किन बातों में भिन्न था?
(2004)
Answer : बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों के आरंभ होने और स्थायी जीवन-यापन की नींव पड़ने के कारण परवर्ती वैदिककालीन आर्यों की सामाजिक दशा में ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की तुलना में काफी परिवर्तन आया। परवर्ती वैदिक कालीन समाज स्पष्टतः वर्ण-व्यवस्था पर आधारित था। अर्थात वर्ग इस प्रकार बंटे थे कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अनुत्पादी होते हुए भी विशेषाधिकार संपन्न थे, क्योंकि वे ही उत्पादन के नियंत्रणकर्ता थे। वैश्य एवं शूद्र निम्न वर्ग के थे और वे उत्पादन के लिए उत्तरदायी थे। जबकि ऋग्वैदिककालीन समाज कबीलाई समाज था तथा समाज जाति के आधार पर विभाजित नहीं था और विभिन्न व्यावसायिक गुट अर्थात मुखिया, पुरोहित, कारीगर आदि एक ही जन समुदाय के हिस्से थे।
यद्यपि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के थे, किन्तु इसके बावजूद उनमें आपस में तनाव की स्थितियों की झलक दृष्टिगोचर होती है। उत्तर-वैदिक साहित्य में ब्रह्म एवं क्षत्र तथा मित्र एवं वरुण के जिस द्वंद्व का उल्लेख है, वह ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के पारस्परिक मनमुटाव का ही द्योतक है। प्रायः यह माना जाता है कि इनमें संघर्ष समाज में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए था, मगर इतिहासकारों के अनुसार यह संघर्ष अधिशेष उत्पादन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ। सामान्यतः इस युग में ब्राह्मण वर्ग धार्मिक क्रिया-कलापों से जुड़ा हुआ था, क्षत्रिय वर्ग शासन के प्रबंधन से, वैश्य वर्ग कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और व्यापार से तथा शुद्र वर्ग उपरोक्त तीनों वर्णों के सेवा कार्य से जुड़ा था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इस युग में कृषकों/वैश्यों पर क्षत्रियों का दबाव बहुत बढ़ता जा रहा था और इसमें ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का साथ दिया। शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार शूद्र द्विजों द्वारा संबोधन किये जाने के योग्य नहीं था। उनका सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। सभी उच्च वर्गों की सेवा करना उनका कर्त्तव्य था।
सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं में ‘कुल’ का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। कुल या परिवार समाज की प्राथमिक इकाई था और ‘कुल’ अर्थात परिवार का सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया होता था। समाज पितृसत्तात्मक था। समाज में पुरुष को महत्व दिया जाता था और इसका पता उन श्लोकों से लगता है जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए लगातार प्रार्थना में प्रयोग किया जाता था। एक-पत्नी विवाह के आदर्श का अब भी मान्यता प्राप्त थी, किंतु बहुपत्नी विवाह भी काफी प्रचलित था और पहली पत्नी को मुख्य पत्नी होने का विशेषाधिकार प्राप्त था। यद्यपि पूरा समाज पितृसत्तात्मक था, फिर भी समाज में महिलाओं का काफी महत्व था। लेकिन अब महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आ गयी थी। वे शिक्षित थीं और वे सभाओं में भी भाग लेती थीं। कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने श्लोकों का संकलन भी किया। उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था। इन सबके बावजूद महिलाओं को पिताओं, भ्राताओं और पतियों पर सदैव निर्भर रहना पड़ता था। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य मैत्रयणी संहिता में स्त्री को पासा एवं सुरा के साथ-साथ तीन प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। विधवा विवाह का प्रचलन अब भी था।
इस काल में भी परिवार संयुक्त होते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् ज्येष्ठ पुत्र परिवार में मुखिया होता था। समाज में ‘नियोग’ प्रथा का भी प्रचलन था इसके अंतर्गत संतानहीन विधवा को अपने देवर के साथ संयोग कर पुत्र प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। समाज में अतिथि सत्कार पर विशेष बल दिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि भोजन महत्वपूर्ण अतिथि के आगमन पर अतिथि को गो-मांस अर्पित किया जाता था। इस काल में भी संगीत वैदिक आर्यों के मनोरंजन का प्रमुख माध्यम था। घुड़दौड़-रथदौड़ द्युतक्रीड़ा मनोरंजन के लोकप्रिय साधन थे। लेकिन समाज में द्युतक्रीड़ा को अच्छा नहीं माना जाता था।
शिक्षा का मौखिक रूप से आदान-प्रदान किया जाता था, परंतु शिक्षा की परम्परा इस काल में अधिक लोकप्रिय नहीं थी। विद्यार्थी गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस काल में अनेक स्त्री शिक्षकों का भी उल्लेख प्राप्त होता है जैसे मैत्रयी तथा गार्गीवाचक्नवी। उत्तर वैदिककाल में छात्रों को वेद, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा के अतिरिक्त शारीरिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता था।
उत्तर वैदिककालीन अथवा परवर्ती काल के आर्य लोगों का समाज कुछ अर्थों में ऋग्वैदिककालीन समाज से भिन्न था। समाज का संरचनात्मक ढांचा तो वही था परंतु विचारों में तथा सामाजिक प्रथाओं में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में कुछ-न कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें ज्यादा परिवर्तन आया। इनमें प्रमुख हैं- वर्ण व्यवस्था तथा नारियों की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में जन्म से व्यक्ति के कर्मों का निर्धारण नहीं होता था। यद्यपि इस काल में कुछ वर्ग तथा व्यवसाय अस्तित्व में थे किंतु वे वंशानुगत नहीं थे। रूचि एवं योग्यता के आधार पर कोई भी योद्धा बन सकता था, अथवा पुरोहित का कार्य कर सकता था। जबकि परवर्ती काल में जन्म के आधार पर वर्ण और कर्म का निर्धारण होता था। ऋग्वेद में विभिन्न वर्गों व व्यवसायों के बीच साथ भोजन ग्रहण करने तथा परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध नहीं मिलता। परंतु परवर्ती काल में इन सब पर कोई प्रतिबंध था। ऋग्वैदिक काल में मूलतः दो ही वर्ण थे- आर्य तथा दास। जबकि परवर्ती काल आर्य चार वर्णों में विभाजित हो गये और इनमें सामाजिक द्वंद्व भी था। जबकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के मध्य इस तरह का आपसी द्वंद्व नहीं था। द्वंद्व केवल आर्यों एवं दासों के मध्य था।
ऋग्वेद में स्त्रियों को उच्च स्थान प्रदान किया गया था। उन्हें पुरुषों की भांति शिक्षा प्राप्त करने एवं राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। उनका उपनयन संस्कार भी होता था। परंतु परवर्ती काल में उनकी स्थिति में गिरावट आयी। ब्राह्मण साहित्य में उल्लेख है कि स्त्री का वध करने का वही दंड था जो शूद्र का वध करने का। स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठान स्वयं नहीं कर सकती थीं। उनके राजनीतिक सभाओं में भाग लेने के निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते। अथर्ववेद तथा ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री का जन्म दुःख का कारण माने जाने का संदर्भ आया है।
Question : बौद्धमत के सामाजिक पक्षों को स्पष्ट कीजिए और भारत में उसकी अवनति के कारण बताइये।
(2004)
Answer : आर्यों के जीवन में विभिन्न भौतिक परिवर्तनों ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया। आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यावसायिक समूहों के सामाजिक स्तर में भी व्यापक परिवर्तन हुआ। वैश्यों और शूद्रों ने विभिन्न धातु शिल्प (कला) व्यापार और वाणिज्य को प्रमुख व्यवसाय बना लिया। एक तरह से समाज का चौथा वर्ग अर्थात शूद्रों का स्थान रिक्त हो गया। अनार्यों ने भूमि जोतने का कार्य आरंभ कर दिया और वे शूद्र बनकर सामाजिक व्यवस्था में मूल शूद्रों द्वारा रिक्त किये स्थान की पूर्ति करने लगे। वैश्य एवं शूद्र जो नयी आर्थिक व्यवस्था में नये व्यवसाय अपनाकर सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऊंचे उठ गये थे, उनको उचित एवं संतोषप्रद सामाजिक एवं धार्मिक आधार नहीं मिला। शहर में रहने वाले व्यापारियों तथा अमीर खेतिहर समुदायों के पास प्रचुर संपत्ति थी।ये समुदाय स्वयं को अन्य वर्गों के बराबर मानने लगे थे। इससे सामाजिक व्यवस्था का ढांचा भी हिलने लगा। पहले से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था पुरोहित प्रधान थी। सत्ता भी पुरोहितों में ही केन्द्रित थी। वैश्य वर्ग जो कि आर्थिकरूप से काफी समृद्ध था। उसे सामाजिक वास्तविकताओं ने अनुरूप अपेक्षित स्थान नहीं दिया था। क्षत्रिय समुदाय, चाहे वे राजतंत्र में हों या गणतंत्र में, के हाथ में अब पहले से अधिक राजनीतिक शक्ति थी। परंतु क्षत्रिय वर्ग की सामाजिक स्थिति ब्राह्मण वर्ग के बाद थी। ये सामाजिक समुदाय उस सामाजिक व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, जो ब्राह्मणों ने वंश के आधार पर निर्धारित की थी। बौद्ध मत ने जन्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को कोई महत्व नहीं दिया। इसने सामाजिक व्यवस्था में कठोर स्तरीकरण को अस्वीकार कर दिया था। इस कारण ब्राह्मण वर्ग से इतर वर्ग के लोगों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। बौद्ध धर्म मूलतः शहरी धार्मिक आन्दोलन था। इस कारण अधिकतर नगरवासी वैश्यों एवं शूद्रों को बौद्ध धर्म में आश्रय मिला।
नयी रूपान्तरित एवं परिपक्व आर्थिक व्यवस्था ने एक अन्य समस्या को जन्म दिया। आर्थिक दृष्टि से नवीनताओं की धर्म शास्त्रें ने कटु आलोचना की और खंडन किया। अस्तु नवोदित व्यापारी समुदाय, धनी और संपन्न होते हुए भी विचित्र द्विविधा की स्थिति में था। इतिहासकारों का मत है कि छठी शताब्दी ई.पू. में बौद्ध धर्म ने नवीन भौतिकवादी जीवन पद्धतिजन्य विभिन्न कुरीतियों और दूषित भावनाओं को नष्ट करने का प्रयास किया। इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तनों को स्थायित्व करने का भी प्रयास किया। बौद्ध धर्म के नियमों के अंतर्गत ऋणी व्यक्ति संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। इस नियम ने महाजनों, धनी एवं संपन्न वर्ग की परोक्ष रूप से बहुत सहायता की।
आर्थिक क्रांति की परिपक्वता से उपेक्षित एवं बहिष्कृत वर्गों की एक नयी समस्या सामने आयी वे तत्कालीन शहरी आर्थिक क्रियाओं से जो जुड़े थे परंतु समाज में अपनी पहचान बनाने में असमर्थ थे। इन्हें भी बौद्ध धर्म ने आश्रय प्रदान किया। बौद्ध धर्म ने लोगों की व्यवहारिक समस्याओं में भी गहन रूचि ली और लोगों को घृणा, निर्दयता, हिंसात्मक प्रवृत्तियों एवं धन संचय आदि से दूर रहने का उपदेश दिया। इससे सामाजिक असमानताओं में कमी आई।
पहले से चली आ रही वैदिक धर्म की पद्धतियां अब जटिल तथा अर्थ-विहीन हो गयी थीं। बलि-यज्ञों तथा अनुष्ठानों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया थ। इससे इसमें आम लोगोंकी भागीदारी कम हो गयी और रूचि भी समाप्त होने लगी थी। तत्कालीन कृषि व्यवस्था का आधार पशु थे जबकि वैदिक धर्म के अंतर्गत बलि प्रथा के चलते पशु-धन की हानि हो रही थी। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और पशुजीवन के महत्व और पवित्रता पर बल देते हुए देश में पशु सम्पत्ति की भावना को प्रोत्साहित किया। इससे समाज के कृषक वर्ग ने भी बौद्ध धर्म का समर्थन किया। इन सब तथ्यों के कारण बौद्ध मत के प्रसार में काफी सहायता मिली और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बौद्ध मत को अपनाया।
जिस द्रुत गति से बौद्ध धर्म का भारत में प्रसार हुआ, उसी गति से उसकी अवनति भी हुई। पांचवीं, छठी शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म भारत के कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गया। बौद्ध धर्म की अवनति के अनेक कारण थे।
महात्मा बुद्ध की मृत्यु के एक शताब्दी के अन्दर ही बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में विवाद और मतभेद आरंभ हो गये थे। परिणामस्वरूप बौद्ध मतावलम्बियों की चार सभायें हुईं और चौथी महासभा में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान सम्प्रदायों में विभक्त हो गया। विभाजन की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करने के सक्रिय प्रयासों ने बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया। जन्म और मरण के चक्र को मूलभूत सिद्धांत स्वीकार करना बहुत हानिकारक रहा। महायान मत के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तिपूजा भी आरंभ हो गयी।
वैदिक धर्म के अंतर्गत जन्म, मरण और कर्म का सिद्धांत पहले से ही अस्तित्व में था। मूर्तिपूजा की प्रथा भी थी। बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म के अनेक विशेषताओं को ग्रहण कर लिया। धीरे-धीरे बौद्ध धर्म और उत्तर वैदिक काल के आर्यों के बीच का अन्तर लगभग मिट ही गया और दोनों हिंदू धर्म के दो संप्रदाय मात्र रह गये जिनमें परस्पर कोई अंतर शेष नहीं रहा। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने शास्त्रर्थ में बौद्ध धर्म के महान दिग्गजों को परास्त कर बौद्ध धर्म की कमजोरियों को उजागर कर दिया। इससे जन-मानस में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची।
बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के साथ-साथ भोग विलास और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने की परंपरा भी बढ़ने लगी क्योंकि धनाढ्य वर्गों से बौद्ध मठों को अत्यधिक धन प्राप्त हो रहा था। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों में प्रमाद एवं आलस्य बढ़ गया और वे भोग विलास में लिप्त रहने लगे।
बौद्ध धर्म के विकास के साथ नये संप्रदायों का भी निरंतर अविर्भाव होता रहा। इनमें धर्म प्रचार और प्रसार की अपेक्षा परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिद्वंदिता की भावना अधिक थी। कालांतर में बौद्ध धर्म में तन्त्र एवं वाम मार्गी शाखा का भी विकास हुआ। हिंदु धर्म में भी यह शाखा विद्यमान थी। बौद्धों ने कलांतर में पाली भाषात्यागकर हिंदु धर्म की संस्कृत भाषा को ग्रहण कर लिया। इन समस्त तत्वों ने बौद्ध धर्म और हिन्दु धर्म के विलग अस्तित्व को लगभग समाप्त कर दिया। हिंदू धर्म में भी सुधार हो रहा था। इससे बौद्ध धर्म की ओर पलायन की प्रवृति में धीरे-धीरे कम होने लगी। कालांतर में महात्मा बुद्ध को भी हिंदुओं में भगवान विष्णु के अवतार की मान्यता मिल गयी। इस तरह मूल रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं संशोधन तथा बौद्ध धर्म का अपने मूल सिद्धांतों से पलायन और विकृति ही भारत में बौद्ध धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी है।
Question : ‘ई.पू.छठी शताब्दी भारत में धार्मिक एवं आर्थिक अशांति की अवधि थी’ टिप्पणी कीजिए।
(2003)
Answer : ई.पू. छठी शताब्दी में भारत के आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। ये परिवर्तन पूर्व के काल के क्रमिक विकास के परिणाम थे। छठी शताब्दी ई.पू. का काल पूर्व तथा आगामी काल के बीच एक संक्रमण काल था। इस काल में अर्थव्यवस्था अपने परिवर्तित स्वरूप में एक विस्तृत आकार ग्रहण कर रही थी। यह परिवर्तन सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में एक नयी सोच तथा व्यवहार को पोषित करने लगा था। यद्यपि अर्थव्यवस्था उत्तर वैदिक काल से क्रमिक गति से विकास कर रही थी तथा गतिशील थी, परन्तु कृषि अधिशेष इतना अधिक नहीं था कि वाणिज्य-व्यापार का विस्तार हो सके। इसके अतिरिक्त उद्योग धंधे, नगरीय अर्थव्यवस्था भी विकसित अवस्था में नहीं थी। इसलिए उस काल में अशांति के लक्षण परिलक्षित नहीं होते। परन्तु छठी शताब्दी ई.पू. के काल में धातुओं की प्रौद्योगिकी (शिल्पकला विज्ञान) में नयी क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। लोहे के प्रयोग ने सैन्य गतिविधियों तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कृषि क्षेत्र में लोहे के प्रयोग ने उत्पादन को बढ़ा दिया। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी अब पूर्व काल में प्रचलित कर्मकांड प्रधान धार्मिक गतिविधियों के स्थान पर भौतिकवादी, कर्मप्रधान तथा अनिश्वरीय धर्मों का उद्भव होने लगा था। आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्र में अशांति का वातावरण बन गया था। इस अशांति के वातावरण ने आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्र के परिवर्तनों को पूरा करने में सहायता प्रदान की तथा परवर्तीकाल के आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था को नयी दिशा प्रदान की।
इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। कृषि लोहे के फाल वाले हलों से की जाती थी। मध्य गंगा घाटी में बढ़ते हुए लोहे के औजारों के प्रयोग तथा रोपाई द्वारा धान की खेती ऐसे दो कारक थे, जिनसे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में काफी मदद मिली। लोहे के प्रयोग का अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। अधिक उपज के कारण व्यवसाय भी विकसित हुए। भरण-पोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था का बाजार की अर्थव्यवस्था में संक्रमण हो रहा था। सिक्कों के प्रचलन ने इस प्रक्रिया में विशेष योगदान किया। इसने अधिक गतिशीलता तथा व्यवसायों तथा व्यापारों को विकास प्रदान किया। अर्थव्यवस्था पर उन व्यापारियों तथा कारीगरों का प्रभाव था जो एक विस्तृत क्षेत्र के लिए वस्तुओं का भारी मात्र में उत्पादन और विनिमय करते थे। इस काल में देश के अंदर और विदेश से व्यापार काफी फल-फूल रहा था। क्रय-विक्रय के लिए कर्षापण नाम का सिक्का प्रचलन में आया गया था, जिस पर व्यापारी अथवा शिल्पी संघ की छाप रहती थी। विभिन्न व्यवसायियों के अपने-अपने संगठन थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियां कार्यकारी और न्यायिक अधिकारों से संपन्न रहती थीं। कुलीन और निर्धन व्यक्तियों के जीवन में स्पष्ट अंतर हो गया। इस प्रकार कृषि के प्रभूत उत्पादन तथा वाणिज्य व्यापार की अभूतपूर्व प्रगति ने मिलकर परम्परागत कबाइली आधार पर गठित सामाजिक आर्थिक संगठन को समाप्त कर दिया।
छठी शताब्दी ई.पू. जीवन के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन का युग था, चारों ओर सन्देह एवं निराशा का वातावरण था। गांगेय प्रदेश का आर्थिक रूपान्तर लगभग पूरा हो चुका था। आर्यों के जीवन में विभिन्न भौतिक परिवर्तनों ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया। आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यावसायिक समूहों के सामाजिक स्तर में भी व्यापक परिवर्तन हुआ। वैश्य वाणिज्य-व्यापार द्वारा तथा शूद्र कृषि कर्म द्वारा सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऊपर उठ गये थे। परन्तु उनको उचित एवं सन्तोषप्रद, सामाजिक एवं धार्मिक स्थान नहीं मिला। इसलिए इनमें असंतोष था। समाज के चार वर्णों में पुरोहित का सर्वोंच्च स्थान था और सत्ता भी पुरोहितों में ही केन्द्रित थी। धार्मिक आंदोलन का उदय हो रहा था। ये आंदोलन (बौद्ध और जैन धर्म) समाज के सभी व्यक्ति को समान महत्व दे रहे थे तथा इनमें कर्मकांड की जगह वैचिारिक शुद्धि पर बल दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त उनके अहिंसा आदि सिद्धांत व्यापारियों एवं कृषकों के लिए अनुकूल भी थे। इसलिए इन्होंने इस नये धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया। इससे वैदिक धर्म (ब्राह्मण धर्म) के वर्चस्व को चोट पहुंची। बौद्ध और जैन धर्म ने जाति व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों को अपने धर्म में स्वीकृत किया। युगों से समाज में ब्राह्मणों के स्थापित प्रभुत्व को यह एक महान चुनौती थी। इस चुनौती ने वैचारिक स्तर पर धार्मिक असंतोष को जन्म दिया।
Question : 2000 से 500 ई.पू. भारत में बसावत, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन और धर्म के प्रतिरूप का पुरातत्वीय साक्ष्यों के आधार पर आकलन कीजिए।
(2003)
Answer : पुरातत्वीय साक्ष्यों के अनुसार 2000 से 500 ई.पू. भारत में मुख्य रूप से चार प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान थीं- हड़प्पा संस्कृति (2000 ई.पू. से 1500 ई.पू.), वैदिक संस्कृति (1500 ई.पू. से 600 ई.पू.) ताम्रपाषाणीय संस्कृति तथा महाजनपदीय संस्कृति (600 ई.पू. से 500 ई.पू.) हड़प्पा संस्कृति को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया हैः विकसित हड़प्पा संस्कृति (2000 ई.पू. से 1800 ई.पू.) तथा उत्तर-हड़प्पा संस्कृति (1800 ई.पू. से 1500 ई.पू.)। वैदिक संस्कृति भी दो भागों में बॅटी है- प्रारंभिक वैदिक काल (1500 ई.पू. से 1000 ई.पू.) तथा उत्तर-वैदिक काल (1500 ई.पू. से 600 ई.पू.)। उत्तर वैदिक संस्कृति क्रमिक रूप से विकसित होती गयी परिणाम स्वरूप महाजनपदीय संस्कृति का उद्भव हुआ।
इन तीनों संस्कृतियों की बसावत, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन तथा धर्म के प्रतिरूपों में पुरातत्वीय साक्ष्यों के अनुसार विभिन्नताएं पायी गयी हैं। वर्तमान के पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत के क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र थे। अब तक 1000 से ज्यादा ऐसी बस्तियों की खोज की जा चुकी है जिनमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं। हड़प्पा, घग्घर और मोहनजोदड़ो का क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का केंद्र-बिंदु था। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता से संबंधित जिन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं इनमें 6 प्रमुख हैं- हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल तथा बनवाली। इस सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर तक थी, पश्चिमी सीमा सुतकांगेदोर तक, उत्तरी सीमा मांडा तक तथा दक्षिणी सीमा दैमाबाद तक थी। गंगा यमुना दोआब में स्थित प्रदेश बाद में उनके बसने के लिए काफी अनुकूल हो गयी क्योंकि जीवन-निर्वाह की व्यवस्था, उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुकूल थी।
हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी। यहां की बस्तियां सुनियोजित थी और जाल की तरह विन्यस्त थे। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश घरों का निर्माण ईंटों से किया गया था और ये ईंटें विशिष्ट रूप में एक ही माप के थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों के घरों के निर्माण में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। जल निकास हेतु नालियों का निर्माण किया गया था। सड़कों का निर्माण भी योजनानुरूप किया गया था। सड़कें सीधी दिशा में एक-दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगरों को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। हड़प्पा सभ्यता की ये सारी विशेषताएं इस तथ्य का द्योतक है कि वर्तमान नगरपालिका की तरह कोई संस्था तत्समय जरूर होगी। हड़प्पाई बस्ती की मुख्य विशेषता है किलेबंदी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में पश्चिमी बस्तियों की किलेबंदी की गयी थी जो संभवतः शासकों का आवास रहा होगा। जबकि कालीबंगा की पूरी बस्ती को सुरक्षा दीवार (किला) से घेरा गया।
बस्तियों की तरह हड़प्पाई अर्थव्यवस्था को विकसित कहा जा सकता है। इसमें कृषि तथा शिल्प के अतिरिक्त व्यापार की भी अहम भूमिका थी। प्रायः सभी हड़प्पाई स्थलों से अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो इस बात का सूचक है कि अधिशेष अनाज का उत्पादन होता था। मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में अन्नागार के ईंटों से निर्मित 27 प्रकोष्ठ प्राप्त हुए हैं। वहीं हड़प्पा के अनाज रखने हेतु छह कोठार मिले हैं। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल आदि अनाजों का उत्पादन करते थे। सर्वप्रथम कपास उतपादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। इसलिए इसे सिंडन कहा गया। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भी भूमिका रही है। कुछेक अपवादों को छोड़कर घोड़े के अस्तित्व अभी भी अंधेरे में है। कांस्ययुगीन सभ्यता होने के बावजूद अधिकांश शिल्पकार पत्थरों से किये गये हैं। किंतु इसका कतई यह अर्थ नहीं कि सिंधुवासी धातु शिल्पकारी से अनभिज्ञ थे। चन्हूदडो से मनके बनाने के कारखाने का मिलना इस बात की पुष्टि करता है। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया आदि से थ। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है, मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। लोथल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंधव के नगरों से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें तथा मेसोपोटामिया के उर, प्रिश, मूसा आदि से हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं तथा मुहरों का मिलना व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है।
मोहनजोदड़ों से प्राप्त वृहद इमारत के मंच पर एक मूर्ति मिली है। इस पुरुष की मूर्ति के चेहरे पर दाढ़ी और माथे पर पट्टी है। विद्वानों ने इसे पूज्यनीय पुरुष प्राप्त विशाल स्नानागार तथा इसके निकट से प्राप्त विशाल सभागार से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि संभवतः इसका कोई धार्मिक महत्व था। इन पवित्र धार्मिक इमारतों से हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक रीतियों का संकेत मिलता है। हड़प्पा की मुहरों एवं पकी मिट्टी की मूर्तियों से उनके अराध्य देव का पता चलता है। कई मुहरों में एक देवता जिसके सिर पर भैस के सींग का मुकुट है, योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। इस देवता की पहचान आदि-शिव के रूप में की गयी है। शिवलिंगनुमा पत्थर के अवशेष तथा योनि लिंग के अवशेष से उस काल में लिंग-पूजा के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। भारी संख्याओं में नारी मूर्तियों के मिलने से मातृदेवी की पूजा का पता चलता है। एक नारी मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। संभवतः उर्वरता देवी के रूप में इनकी पूजा होती थी। वृक्ष तथा अनेक प्रकार के जानवरों के चित्र मुहरों तथा मूर्तियों में मिले है। ताबीज बड़ी संख्या में मिले हैं। संभवतः हड़प्पाई लोक विश्वास करते थे कि भूत-प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं। इससे बचने हेतु वे ताबीज धारण करते थे। कालीबंगा तथा लोथल से अग्नि-वेदियों के प्रमाण मिले हैं। संभवतः यह स्थान पूजा क्रिया का केन्द्र रहा होगा। मृतक के अंतिम संस्कार में धार्मिक विश्वास का पुट मिलता है। लोथल से युग्म शवाधान के अवशेष प्राप्त हुआ है। मृतक के साथ बर्तन, शिल्प संबंधित वस्तुओं के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मृतकों को सावधानीपूर्वक रखकर अंतिम संस्कार करना तथा आभूषण की वस्तुओं को साथ रखना इस तथ्य का द्योतक है कि वे लोग मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे।
उत्तर-हड़प्पा काल में भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी क्षेत्र में एक ताम्र-पाषाण सभ्यता भी फैली हुई थी। राजस्थान में बनास संस्कृति, मध्य भारत में कायथा संस्कृति, मालवा क्षेत्र में मालवा संस्कृति तथा महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति फैली हुई थी। बनास संस्कृति के लोगों के आवास के साक्ष्य अहाड़ तथा गिलुंद से मिले है। कायथा संस्कृति तथा पश्चिमी भारत में अस्तित्व में थी।
ताम्र पाषाण काल की बस्तियों के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। हालांकि कच्ची ईंट के घर प्राप्त नहीं होते हैं किंतु अधिकतर घर गीली मिट्टी थोप कर बनाये जाते थे और घरों पर छापर भी दिये जाते थे। राजस्थान के आहार संस्कृति के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदनगर, नेवासा, दैमाबाद, इनामगांव आदि क्षेत्रों में विस्तृत थी। ये संस्कृतियां ग्रामीण थीं, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनामगांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गयी थी। उनकी अर्थव्यवस्था कृषि तथा पशुपालन पर आधारित थी। वे गाय, भेड़, बकरी तथा सुअर आदि जानवर पालते थे तथा गेहूं चावल, उड़द, मूंग मटर आदि पैदा करते थे। इनामगांव से पांच कमरों वाला आवास मिला है। मावला में चरखे और तकलियां मिली हैं। इनामगांव में कुम्भकार, धातुकार आदि के होने के साक्ष्य मिले हैं। किसी-किसी मृतक के साथ बहुत सारे आभूषण तथा बर्तन को रखकर दफनाया गया है तो किसी के साथ बहुत साधारण वस्तुएं मिली हैं।
ताम्रपाषाणिक स्थलों से प्राप्त मूर्तिकाओं में महिलाओं की पुतलियां हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मालवा या राजस्थान में मिली रूढ़ शैली की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ (सांड़) धार्मिक सम्प्रदाय का प्रतीक था। कब्र में दफनायी गयी इस्तेमाल की गयी वस्तुओं से ज्ञात होता है कि उन्हें परलोक जीवन के बारे में विश्वास था।
वैदिक कालीन लोग गेरुए रंग के मृद्भांड, चित्रित धूसर मृदभांड तथा काले और लाल मृदभांड इस्तेमाल करते थे। ये मृदभांड घग्गर नदियों के किनारे, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में पाये गये हैं। गंगा-यमुना के बीच के दोआब क्षेत्र में घने बसावत के साक्ष्य मिले हैं। इससे इन क्षेत्रों में वैदिक कालीन लोगों के रहने का संकेत मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार लोग कृषि पर आधारित स्थायी जीवन नहीं बिता रहे थे। प्रारंभिक वैदिककालीन स्थलों से पत्थर तथा ताम्र निर्मित औजारों से संकेत मिलता है कि वे लौह तकनीक से परिचित नहीं थे। अर्थात वे लोग युद्ध में ज्यादा संलग्न रहते थे। पक्के मकानों का साक्ष्य नहीं मिला है अर्थात वे लोग लकड़ी से निर्मित आवासों में रहते थे। उत्तर-वैदिक युग में वैदिक कबीले सप्त सैन्धव क्षेत्र में गंगा की उपरी घाटी तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों फैल गये थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तर-वैदिक कालीन लोगों से संबंधित चित्रित घूसर मृद्भाड़ पाए गये हैं। ऊपरी गंगा घाटी में 700 से अधिक घूसर मृदभांड के स्थलों की खुदायी की गयी है। इनमें प्रमुख हैं अतरंजीखेड़ा, नूह, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र आदि। इन क्षेत्रों से लोहे के हथियार और औजार भी मिले हैं। वैदिक काल में उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो गयी थी। उन्नत औजारों से जंगलों को साफ करने में सफल हुए। विभिन्न प्रकार के अनाज के दानों से उनके भोजन तथा अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। जैसे चावल, गेहूं आदि। उस काल के मन्दिर अथवा मूर्तियों के अवशेष नहीं मिले हैं। कार्यों के आधार पर उनका समाज बंटा हुआ था।
600 से 500 ई.पू. का काल जनपद और महाजनपदों के उदय का काल था। इनका उद्भव उत्तर-वैदिक काल के उत्तरार्ध में ही शुरू हो चुका था। इस काल के लोग किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं थे। अनेक महत्वपूर्ण महाजनपदों जैसे श्रावस्ती, वैशाली, हस्तिनापुर, उज्जैन आदि की खुदायी से, यहां के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, घरों, इमारतों तथा कस्बों आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्वीं छोर पर अंग, पश्चिमी छोर पर अवस्थित- मत्स्य, उत्तरी छोर पर गंधार तथा दक्षिणी छोर पर अश्मक महाजनपद थे। इस काल के लोग उत्तरी काले पालिश किये मृद्भाड़ का प्रयोग करते थे। इन बर्तनों के प्राप्ति स्थल से इनके बसावत का पता चलता है। इस काल के लोगों ने लौह का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करना आरंभ कर दिया था। लोहे के औजारों के कारण वनों की कटाई आसान हो गयी और कृषि के क्षेत्रों में विस्तार हुआ। अब अधिशेष उत्पादन से कृषि कार्य में संलग्न वर्ग भी समाज में उच्च स्थान पाने की आंकक्षा रखने लगा। इससे समाज में आंतरिक अशांति का प्रादुर्भाव हुआ और सामाजिक संगठन में परिवर्तन हुए। अर्थव्यवस्था कीगतिशीलता ने धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। कृषि में पशुओं के उपयोग के बढ़ोतरी ने बलि प्रथा के विरोध का मार्ग प्रशस्त किया। समाज के धनाढ्य वर्ग जो व्यापार-वाणिज्य में लगा था, ने जाति पर आधारित धार्मिक भेद-भाव का विरोध किया। सामाजिक भेद भाव का भी उसने विरोध किया। सैनिक वर्ग के सदस्य भी सामाजिक संगठन में अपने वर्चस्व का दावा करने लगे। अब कर्मकांडी धार्मिक आडम्बरों का विरोध भी होने लगा था।
Question : भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं के बारे में फाहयान द्वारा प्रदान की गयी जानकारी का परीक्षण कीजिए। उसके द्वारा दिये गये विवरण का हवेनसांग द्वारा दिये गये विवरण के साथ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।
(2003)
Answer : चीनी यात्री फाहयान ने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत की यात्र की थी। 399 ई. से 414 ई. तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसके द्वारा छोड़ा गया भ्रमण-वृत्तान्त चन्द्रगुप्तकालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं का सुन्दर निरुपण करता है। हवेनसांग भी एक चीनी यात्री थी, जिसने 630 और 644 ई. के बीच भारत की यात्र की थी। उस काल में भारत का सम्राट हर्षवर्धन था। फाहयान ने अपने समकालीन शासक का नाम नहीं लिखा है, जबकि “वेसांग ने लिखा है। दोनों यात्री बौद्ध थे। बौद्ध ग्रन्थों के गहन अध्ययन तथा बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थानों का भ्रमण करने के लिए भारत आये थे। फाहयान ने मथुरा से दक्षिण की ओर का प्रदेश ‘मध्यदेश’ (मालवा) के बारे में लिखा है कि वहां का प्रशासन प्रबुद्ध तथा कार्य कुशल था। लोग खुशहाल थे, उन्हें अपनी गृहस्थी के विषय में लिखवाना नहीं पड़ता, न ही न्यायाधीशों के सामने उपस्थित होना पड़ता और न ही उनके नियमों का पालन करना होता है। अपराधियों पर उनके अपराध की परिस्थितियों के अनुसार भारी या हल्का जुर्माना लगाया जाता है। वह लिखता है कि राजा बिना मृत्युदंड अथवा शारीरिक यंत्रणाओं का भय दिलते हुए ही शासन करता था। बार-बार विद्रोह करने पर भी केवल उनका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। सारे देश के लोग देश में जीव हत्या नहीं करते, न नशेदार पदार्थ पीते थे और प्याज या लहसन भी नहीं खाते थे। केवल चांडाल ही ऐसा करते हैं। क्रय-विक्रय में कौडि़यों का प्रयोग करते थे। परन्तु हमें तत्कालीन अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि लोग मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। फाहयान ने सारे देश के लोगों को अहिंसक बताया है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। फाहयान के विपरीत हवेनसांग तत्कालीन राजनीति स्थिति का विस्तार से वर्णन करता है। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध के बारे में भी वह लिखता है। उसके अनुसार पुलकेशिन ने हर्ष की अधीनता नहीं मानी। वह पुलकेशिन की शक्ति की प्रशंसा भी करता है। हवेनसांग ने भी भारतीयों के भोजन की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया। उसके अनुसार भी लोग प्याज और लहसुन का प्रयोग कम करते थे। हवेनसांग भी राज्य में अपराध और विद्रोह के कम होने की सूचना देता है। शारीरिक दण्ड नहीं देने की बात वह भी कहता है। “वेसांग भी राज्य में अपराध और विद्रोह के कम होने की सूचना देता है। स्वयं हवेनसांग को डाकुओं ने दो बार लूटा था। हवेनसांग ने भी यहां के लोगों की खुशहाली के बारे में लिखा है। दोनों ने यहां के लोगों के सहृदयता, सचरित्रता तथा अतिशय प्रेमके बारे में लिखा है।
फाहयान आर्थिक दृष्टि से भारत को सुखी और समृद्ध बताता है। समृद्धि के कारण ही धनपतियों ने मगध में चिकित्सालय बनवाये थे जहां रोगियों को मुफ्रत भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। किंतु वह बहुत से नगरों के उजाड़ होने का भी उल्लेख करता है जो व्यापार में पतन का द्योतक है। वह यह भी लिखता है कि क्रय-विक्रय में कौडि़यों का प्रयोग होता था। स्पष्टतः दैनिक जीवन में मुद्रा का प्रयोग कम होने लगा था। फाहयान के अनुसार सरकार की आय मुख्यतः राजभूमि के कर से प्राप्त की जाती थी जो कि उत्पादन का छठा भाग था। सरकारी कर्मचारियों को निश्चितवेतन दिये जाते थे और प्रजा से धन लेकर निर्वाह करने का उन्हें अवसर नहीं दिया जाता था। दान-धर्म की कई संस्थाएं थीं। सड़कों के किनारे पर या उनसे दूर लोग दान गृह बनवाते थे और यात्र करने वाले भिक्षुओं तथा यात्रियों को वहां बिस्तर और भोज्य पदार्थ दिये जाते थे। हवेनसांग भी भारत की समृद्धि का वर्णन करता है। उसके अनुसार अन्न तथा फलों का उत्पादत प्रचुर मात्र में होता था। वह कई नगरों तथा शहरों के निर्जन होने की सूचना देता है। हवेनसांग के अनुसार सरकार की आय का प्रमुख साधन भू-राजस्व था। परन्तु भिक्षुओं के लिए विहार, दानगृह, बनवाने का उल्लेख हवेनसांग ने भी किया है। फाहयान पाटलिपुत्र से और अशोक के भव्य महल से अत्यन्त प्रभावित हुआ था। हवेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र उत्तरी भारत का प्रमुख नगर नहीं रहा था और उसका स्थान कन्नौज ने ले लिया था। हवेनसांग ने सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। परन्तु फाहयान ने नहीं लिखा है। दोनों के अनुसार अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था।
सामाजिक विषमता का उल्लेख फाहयान तथा हवेनसांग दोनों के यात्र वृतांत में मिलता है। फाहयान के अनुसार चांडाल समाज से बहिष्कृत थे। वे गांवों तथा नगरों के बाहर निवास करते थे। गांवों तथा नगरों में प्रवेश करते समय लकड़ी पीटते हुए चलते थे ताकि लोग मार्ग से हट जायें और उनके स्पर्श से बच जायें। फाहयान के समान ही हवेनसांग तत्समय समाज में विद्यमान अश्पृश्यताओं का उल्लेख करता है। वह तत्कालीन समाज के बड़े जातियों तथा उपजातियों में विभाजित बताता है। उसके अनुसार कसाई, मछुवारे, भंगी, नट, जल्लाद आदि अछूत समझे जाते थे। वे गांवों तथा नगरों के बाहर निवास करते थे। हालांकि वह सिंध के राजा के रूप में एक शूद्र के आसीन होने का उल्लंघन करता है। वह ब्राह्मणों की प्रशंसा करता है। वह लिखता है कि वैश्यों के हाथ में देश की अर्थशक्ति थी। स्पष्टतः सामाजिक क्षेत्र में हवेनसांग का विवरण फाहयान से कहीं अधिक विस्तृत है।
फाहयान ने मध्यदेश को ब्राहमण धर्म का केन्द्र बताया है। वह एक बौद्ध तीर्थ यात्री था। उसने प्रत्येक वस्तु को बौद्ध धर्म की दृष्टि से ही देखा। गुप्तकाल में ब्राह्मण धर्म का केन्द्र बताया है। उसने इस धर्म का विस्तृत वर्णन नहीं किया है। उसने अधिकांश बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्र की थी। उस काल में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में बंटा हुआ था। उसने मथुरा में 20 बौद्ध बिहार देखे थे। उसने गया, कपिलवस्तु और कुशीनगर को उजाड़ खाली पाया था। उसने मध्य पद्रेश को शासक के विष्णु उपासक होने का उल्लेख किया है। उसके अनुसार हिन्दू और बौद्धों में परस्पर सद्भावना थी, हवेनसांग के अनुसार बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ रहा था। इसके बावजूद हजारों भिक्षु भारत में निवास कर रहे थे। हवेनसांग ने जैन धर्म की भी चर्चा की है जबकि फाहयान ने नहीं की है। हवेनसांग ने शैव और वैष्णव धर्म का भी उल्लेख किया है।
Question : मौर्य राज्य की प्रकृति का परीक्षण कीजिये। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये।
(2002)
Answer : मौर्य प्रशासन के बारे में हमें विशिष्ट जानकारी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विदेशी यात्रियों के विवरण एवं मौर्यकालीन अभिलेखों से मिलती है। मौर्य शासनकाल में भारत में पहली बार राजनीतिक एकता प्रतिस्थापित हुई। गणराज्यों का ”ास होने लगा और सत्ता अत्यधिक केंद्रित होने लगी। इस काल में परंपरागत मान्यताओं के विपरीत राजाज्ञा को प्रमुखता दी गयी। स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशाड्ड को माना गया है। अर्थशाड्ड की खोज पंडित श्यामजी शास्त्री ने सन् 1904 ई. में की थी। इसमें लेखक ने एक प्रबुद्ध राजतंत्र की चर्चा की है। वह एकराट या एकक्षत्र राज्य का पक्षधर है। उसने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है। ये हैं- राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। ये राज्य निर्माण के आवश्यक तत्व माने गये हैं। अर्थशास्त्र में राजा में विद्यमान कुछ आवश्यक गुण बताये गये हैं यथा- वह कुलीन हो, सत्यवादी हो, बुद्धिमान हो, धर्म का रक्षक हो। कौटिल्य ने एक निपुण शासक होने के लिए तीन बुनियादी शर्तें बताई हैं। यथा- राजा के लिए आवश्यक है कि वह हर समस्या पर यथेष्ठ ध्यान दे, वह सदा सचेत रहे एवं उसे अपनी दायित्वों का सदैव ज्ञान हो। उसने राजा को कुशल कूटनीतिज्ञ होने की बात कही है। उसका कहना है कि मित्र का शत्रु, शत्रु और शत्रु का शत्रु, मित्र होता है। राजा को इन सब बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। राजा को अन्वीच्छा अर्थात अन्वेषण, त्रयी अर्थात वेद, लोक अर्थात लोकधर्म, दंड अर्थात न्याय एवं वार्ता अर्थात कृषि-पशुपालन एवं व्यापार की विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए। वह एक प्रबुद्ध राजतंत्र का पक्षधर है। उसका कहना है कि राजा में क्षेत्र विजय का अदम्य साहस होना चाहिये। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। परंतु साथ ही साथ हम पाते हैं कि वह निरंकुशता के साथ लोक कल्याणकारी राजधर्म का भी समर्थक है। उसने लिखा है प्रजानाम हिते राज्ञं अर्थात प्रजा के हित में ही राजा का हित है।
मौर्यकाल में राजा को मंत्रियों की नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार था। अर्थशाड्ड में 18 महत्वपूर्ण तीर्थों या अमात्यों की चर्चा हुई है, परंतु ऐसा अहसास होता है उस काल में मंत्रीपरिषद काफी बड़ी होती थी। बिदुसार के 500 अमात्य थे। अर्थशाड्ड में मंत्री के लिए ईमानदारी, शास्त्रें का ज्ञाता, शीलवान, श्रेष्ठ कुलोत्पन्न एवं दंड नीति में पारंगत होना आवश्यक गुण माने गये हैं। अशोक के छठे शिलालेख जिसमें मंत्रीपरिषद से विचार-विमर्श की चर्चा आयी है इससे स्पष्ट होता है कि निर्णय बहुमत से लिये जाते थे।
मौर्यों के प्रशासन का स्वरूप केंद्रीय था। विभिन्न प्रकार के अमात्यों का उल्लेख एवं उद्योग- व्यवसाय आदि पर जिस प्रकार से नियंत्रण की चर्चा आयी है, उससे यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन के बड़े-बड़े विभागों में अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी एवं सभी को राजा द्वारा वेतन दिया जाता था। 500 पण से लेकर 48000 पण तक वेतन दिये जाने का उल्लेख हुआ है। इससे मौर्य प्रशासन के राजस्व का भी आभास मिलता है। अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि अशोक के काल में उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था।
यद्यपि मौर्य प्रशासन लोकतांत्रिक अवधारणा पर आधारित नहीं था, फिर भी इसके चरित्र में लोक कल्याण की भावना का समावेश
दिखायी पड़ता है। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में राजा को लोक कल्याण हेतु तत्पर रहने को कहा है। रूद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख आया है। धौली अभिलेख में अशोक अपने समस्त प्रजा को पुत्र-पुत्रियों कहता है। उसकी धम्म यात्र का उद्देश्य भी लोक कल्याण था। उसने प्रतिवेदक नामक अधिकारी की नियुक्ति मात्र इसलिए की कि वह उसे जनता की खबर सीधे पहुंचा सकेगा।
मौर्यकाल में सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सबसे नीचे ग्राम न्यायालय की, उसके बाद संग्रहण, दोशमुख खार्वटिक आदि स्थानीय अथवा जनपद स्तर के न्यायालय थे। राजा के न्यायालय के अलावा धर्मस्थीय एवं कंटकशोधन न्यायालय को जिसमें क्रमशः दीवानी ओर फौजदारी मामले देखे जाते थे, विवादों को पंजीकृत किया जाता था। न्याय का आधार धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। इस कार्य में वृद्ध, स्त्रियों, गणिकाओं आदि का भी सहयोग लिया जाता था। प्रतिवेदकों की चर्चा मिलती है जो किसी भी समय राजा से मिलने को स्वतंत्र था। संस्था और संचार दो अन्य प्रकार के गुप्तचरों की विशद् चर्चा मिलती है। इनमें संस्था स्थायी तौर पर और संचार परिचरण करते हुए कार्य करते थे। मेगास्थनीज ने गुप्तचरों को ओवरसियर की संज्ञा दी है। अर्थशास्त्र में चतुरंगिनी सेना की चर्चा मिलती है। मेगास्थनीज ने सेना के छः विभाग बताये हैं। इनके अलावा रसद, आयुद्धागार, रथाध्यक्ष की भी चर्चा आई है।
साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन पर यथोचित ध्यान दिया जाता था। अर्थशाड्ड में नगर प्रशासन को नागरक कहा गया है, जबकी मेगास्थनीज ने म्युनिसपिल जैसी संस्था बताया है। ये 30 वार्डों से निर्मित थे और पांच-पांच की संख्या में छः समितियों में विभक्त थे। ये जन्म मरण, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, शिल्पकला निर्मित वस्तुओं की बिक्री एवं कर वसूलने का कार्य करते थे। नगर में रात को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाता था।
अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मौर्य प्रशासन के सुदृढ़ केंद्रीकृत होने के बावजूद भी लोक कल्याण की भावनाओं से ओत प्रोत था। सिद्धांततः तो यह पूर्णतः राजतंत्र लगता है पर साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर यह कहा जा सयकता है कि राजा जन विचार के विपरीत कुछ नहीं करता था। कुछ प्रशासनिक कार्य भी जनता के हाथों सुपुर्द थे।
Question : प्राचीन भारतीयों की विभिन्न हस्त शिल्पों, विज्ञान एवं गणित में निपुणता का परीक्षण कीजिये।
(2002)
Answer : पाषाण कालीन सभ्यतायें जो कि सोहन घाटी, नर्मदा घाटी एवं बेलन घाटी जैसे स्थलों में विकसित हुई, से प्रस्तर कुठारों एवं लघु अश्मकों के विकास का प्रर्याप्त प्रमाण-पत्र होते हैं। भारत में नव पाषाण काल में कृषि की वैज्ञानिक पद्धति अस्तित्व में आई। इसका प्रमाण मेहरगढ़ (अब पाकिस्तान) से प्राप्त होता है। उल्लेखनीय बात यह है कि सिधु काल में ही सर्वप्रथम कपास की खेती का कार्य आरंभ हुआ। कालीबंगन के प्राग सैंधव स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण द्विफसली कृषि प्रणाली के विकास का द्योतक है।
हड़प्पा काल में विविध प्रकार के हस्तशिल्पों का समुÂत विकास हुआ। हड़प्पाई मृद्भांड अपनी संरचना एवं रंग के कारण विशिष्ट हैं। द्विरंगी और साथ ही बहुरंगी मृदभांड मत्स्य शल्क एवं पीपल के पत्ते जैसे सुंदर अलंकरणों से युक्त हैं। हड़प्पाई स्थल चन्हुदड़ो से मनकों के निर्माण के बारे में व्यापक पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि हड़प्पा के लोग कार्नेलियन, स्टेटाईट एमिथिस्ट एवं एमेट जैसे बहुमूल्य प्रस्तरों को सुंदर गोलाकार एवं ढ़ोलकाकार मनकों में परिणत करने की कला में निपुण थे। हड़प्पा के बने ऐसे मनके मेसोपोटामियाई स्थलों से भी प्राप्त हुए हैं। विशेषकर मुहरों के उपर अंकित चित्र व मूर्ति कला एवं शिल्प के यथार्थवादी स्वरूप के प्रतीक हैं। वैदिक काल में भी ज्ञान-विज्ञान का व्यापक विकास हुआ। शूल्व सूत्र से वेदिकाओं के निर्माण से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है।
मौर्यकाल में प्रस्तर शिल्प में अद्वितीय विकास संभव हुआ। राज्याश्रय में पल्लवित होने वाली प्रस्तर कला के प्रमाणों यथा अशोक कालीन स्तम्भों एवं बराबर के शैल गृहों में पत्थर के ऊपर एक विशिष्ट चमक देखी जाती है जो उस युग की महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि थी। साथ ही एकाश्मक स्तंभों की बेलनाकार संरचना एवं शीर्ष पर बनी पशु मूर्तियों से शिल्प में आई विशिष्ट प्रगति का पता चलता है। मौर्यों के पश्चात मथुरा, गांधार, अमरावती, नागार्जुनीकोंडा जैसे स्थलों पर मूर्तिकला का विकास हुआ एवं इन्हीं स्थानों पर पत्थर से आच्छादित स्तूप भी अस्तित्व में आये। इसी समय चरक जैसे विद्वान ने चरक संहिता की रचना की जो आयुर्वेद शास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ है।
गुप्त काल में कला-शिल्प एवं गणित आदि विज्ञानों का व्यापक विकास हुआ। धातु कर्म के क्षेत्र में भी विशिष्ट प्रगति हुई। जिसके प्रमुख उदाहरण मेहरौली का चंद्र लाट स्तंभ एवं सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र प्रतिमा है। स्थापत्य के क्षेत्र में इस युग में नागर शैली के मंदिरों का विकास हुआ, जो ईंट एवं पत्थर दोनों से ही बनाये गये। ईंट से बने मंदिर का सर्वप्रमुख उदाहरण भीतरगांव का मंदिर है, वही पत्थर के बने मंदिरों में पंचायतन शैली का बना देवगढ़ का दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। चैत्य गृहों के निर्माण में इस युग में ज्यादा परिपक्वता प्रकट होती है। अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19, 26 आदि इस काल की गुफा शैली के प्रमुख प्रमाण हैं। इस युग में ब्राह्मण धर्म में भी शैल गृहों के निर्माण की परंपरा चल पड़ी। इसके उदाहरण उदयगिरि से प्राप्त होते हैं। जिसमें भूदेवी उद्धार प्रतिमा का विराट अंकन हुआ है।
गुप्तकाल में ही आर्यभट्ट जैसे विद्वान ने गणित एवं ज्योतिष पर क्रमशः आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांतिक जैसी पुस्तकें लिखीं, जिसमें पृथ्वी के घूर्णन, दिन-रात एवं वर्ष तथा सूर्यग्रहण आदि से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी है। ऐसा पता चलता है कि आर्यभट्ट के समय भारतीयों को शून्य एवं दशमलव पद्धति का पूरा परिज्ञान था। आर्यभट्ट के परवर्ती खगोलविद वाराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, वृहत्संहिता, महाजातक, लघु जातक जैसे ग्रंथों में ज्योतिष एवं खगोल पर व्यापक परिचर्चा की है। चिकित्सा शाड्ड में सुश्रुत एवं धन्वतंरि के नाम भी प्रमुख हैं। खासकर सुश्रुत की संहिता शल्य चिकित्सा का रोचक वर्णन प्रस्तुत करती हैं। वाग्भट्ट के अवयंग हृदय से शरीर के आठ प्रमुख ग्रंथियों का पता चलता है।
गुप्तोत्तर युग में तो पशु चिकित्सा पर भी पुस्तकें लिखी गयी। इनमें पालकाप्य की जन चिकित्सा एवं शालिहाÂ की अश्व चिकित्सा प्रमुख हैं। गुप्तोतर काल में स्थापत्य विज्ञान ऊपर भी कार्य हुआ, जिससे संबंधित प्रमुख पुस्तकें हैं- मयमत, समरांगण सूत्रधार, शिल्पशाड्ड, ईशान विश्व गुरुदेव पद्धति आदि। इसी काल में प्रतिमा लक्षण एवं भिति चित्रकला के ऊपर विष्णु धर्मोतर पुराण की रचना हुई, जिसमें समुचित ताल-मान आदि का वर्णन भी हुआ है। भास्कराचार्य की लीलावती भी प्राचीन काल के गणित की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
यदि पश्चिमी एलोरा के कैलाश मंदिर का स्थापत्य एवं शिल्प को देखा जाय एवं दक्षिण भारत के चोल कालीन वृहदेश्वर मंदिर के विराट स्थापत्य में लय एवं संतुलन के सामंजस्य का अवलोकन किया जाये तो निःसंदेह ही प्राचीन भारत का शिल्प, गणित एवं विज्ञान गरिमा का विषय प्रतीत होते हैं।
Question : इस प्रश्न-पत्र के साथ दिए जा रहे मानचित्र में, निम्नलिखित स्थानों में से किन्हीं पंद्रह पर निशान लगाइए तथा मानचित्र में अंकित स्थानों पर संक्षिप्त वर्णनात्मक टिप्पणियां लिखिएः
1. अजन्ताः 2. बोधगयाः 3. धौलावीराः 4. द्वारकाः 5. गिरनारः 6. हस्तिनापुरः 7. कांचीपुरमः 8. कौशाम्बीः 9. मदुरैःकदंबन 10. मालखेड़ः 11. मोहनजोदड़ोः 12. नालंदाः 13. पुरुषपुरः 14. रोपड़ः 15. सांचीः 16. श्रवणबेलगोलाः 17. श्रावस्तीः 18. तंजोरः 19. थोनश्वरः 20. वाराणसीः
(2002)
Answer : 1. अजन्ताः यह वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। यह गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल में सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। यहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक गुफाऐं मिलती हैं जिनका निर्माण मुख्यतः वाकाटक शासकों ने कराया था।
2. बोधगयाः भगवान बुद्ध को यहीं पर बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ह्नेनसांग के अनुसार सिहल नरेश ने यहां महाबोधि संघाराम का निर्माण करवाया था।
3. धौलावीराः 1991 ई. में उत्खनित इस स्थल से 4500 ई.पू. के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां किले की दोहरी दीवार और रक्षक गृह बनाया गया है। यहां से हड़प्पा सभ्यता का अपारदर्शी शीशे के टुकड़े से बना 10 अक्षरों वाला शिलालेख मिला है।
4. द्वारकाः यह वर्तमान में गुजरात के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। यह भगवान कृष्ण से संबंधित स्थल है। इसे कुशस्थली भी कहा गया है।
5. गिरनारः गुजरात प्रांत के खेतक पर्वत के पास स्थित इस नगर को रूद्रदामन ने सातवाहनों से छीना था। यहां के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था।
6. हस्तिनापुरः प्राचीन भारत में यह सोलह जनपदों में से एक था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत में इसकी विस्तृत चर्चा आयी है।
7. कांचीपुरमः दक्षिण भारत की काशी कहलाने वाली यह नगरी तमिलनाडु में है। यह एक सुविकसित शिक्षा केंद्र एवं पल्लवों की राजधानी थी।
8. कौशाम्बीः इलाहाबाद से 48 कि.मी. दूर दक्षिण-पश्चिम में यमुना तट पर स्थित कौशाम्बी प्राचीनकाल में एक महत्वपूर्ण नगर था। सातवीं शती ई. में चीनी चात्री युवान च्यांग आया था। यहां पर 10 से अधिक बौद्ध विहार से जो अब जीर्णावस्था में हैं।
9. मदुरैः कदंबन नाम से भी जाना जाने वाला यह नगर प्राचीन काल में शिक्षा, धर्म और संस्कृति का दक्षिण भारतीय केंद्र था। मीनाक्षी देवी मंदिर यहां है। मलिक काफूर ने इसे 1310 ई. में मुस्लिम राज्य में मिला लिया था।
10. मालखेड़ः इस नगर को राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम ने बसाया था। अलमसूदी ने इसे मणिकर कहा है। इसके अन्य नाम हैं मान्यखेत, मान्यखेड़ तथा मलकुएर्र।
11. मोहनजोदड़ोः यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। यहां विशाल स्नानागार एवं अÂागार मिले हैं। इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है।
12. नालंदाः शक्रादित्य (कुमारगुप्त) ने राजगृह के निकट इस शहर को 5वीं सदी में बसाया और 11वीं सदी तक यह बौद्ध शिक्षा एवं धर्म का केंद्र बना रहा। बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में इसे तहस-नहस कर दिया।
13. पुरुषपुरः कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर नाम से विख्यात है। यहां कनिष्क द्वारा निर्मित सार्वजनिक भवन, स्मारक, बौद्ध विहार एवं 13 मंजिला स्तंभ जिसका ऊपरी भाग 400 फीट ऊंचा है।
14. रोपड़ः यह पंजाब में स्थित शहर है। उत्तरी भारतीय संस्कृति के विकास से इसका गहरा संबंध है। यहां के पुरातात्विक आन्वेषण से प्राप्त वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता से साम्य रखती हैं।
15. सांचीः भोपाल के निकट मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्तूप सांची को चेतियगिरि एवं काकनद के नाम से भी जाना जाता था। सांची भू-भाग एक चौराहा था जहां से उज्जैन, भड़ौंच, विदिशा, पाटलिपुत्र को मार्ग जाते थे। मौर्य या शुंगकालीन मंदिर संख्या 40 वहां का प्राचीनतम है।
16. श्रवणबेलगोलाः विंध्यगिरि एवं चंद्रगिरि पहाडि़यों पर स्थित जैनियों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। यह मंदिर जैनधर्म प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र भगवान बाहुबली की 17 मीटर ऊंची प्रतिमा गोमतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है।
17. श्रावस्तीः अचिरावती नदी, आधुनिक राप्ती के तट पर बसा यह नगर कोसल जनपद का प्रमुख शहर था। बौद्धों के अनुसार श्रावस्त ऋषि के नाम से इसका नामकरण हुआ।
18. तंजोरः यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह चोलों का एक प्रमुख नगर था जहां राजेन्द्र प्रथम ने वृहदारेश्वर का मंदिर बनवाया था। यह चोलों की राजधानी के रूप में भी प्रतिष्ठित था।
19. थोनश्वरः मध्य प्रदेश के इस नगर का पुराना नाम स्थाणेश्वर था। हर्षचरित में इसका वर्णन मिलता है। इसके अनुसार यह सरस्वती और दृषदुति नदियों के बीच में बसा हुआ था।
20. वाराणसीः भारत का प्राचीनतम नगर जिसे जातक कथा में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। वरूणा से अस्सी नदी के संगम पर स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा गया है जो काशी जनपद की राजधानी थी। प्रमुख प्राचीन व्यापारिक केंद्र था जहां हाथी दांत, सूती एवं रेशमी वस्त्र का कार्य होता था। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर शासक हर्ष ने यहां संन्यास लिया था।
Question : अशोक महान के समय तक मगध के साम्राज्यवाद की सफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिये।
(2001)
Answer : मगध के उत्थान में विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृितक और राजनीतिक परिस्थितियों का योगदान रहा। मगध की भौगोलिक परिस्थितियों ने मगध के उत्कर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। गंगा ओर उसके उत्तर में गंडक तथा घाघरा नदियों ने तथा दक्षिण में सोन नदी ने मगध को सुरक्षा तथा यातायात और व्यापारिक प्रगति के लिए साधन प्रदान किये। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह सात पहाडि़यों से घिरी हुई थी और बाद की राजधानी पाटलिपुत्र भी गंगा तथा सोन नदी के संगम पर स्थित होने के कारण न केवल सुरक्षित थी, अपितु उत्तर भारत के व्यापार का महान केन्द्र भी थी। मगध में गया के दक्षिण-पूर्व में बड़ी मात्र में लोहा और तांबा उपलब्ध था। उससे मगध न केवल समृद्धशाली हुआ, अपितु शस्त्र निर्माण में भी समकालीन राज्यों से आगे बढ़ गया। दक्षिण बिहार के घने जंगलों में पाये जाने वाले हाथियों का प्रयोग भी सैन्य कार्य में किया गया। जंगल में उपलब्ध लकड़ी मकान, शस्त्र और विभिन्न औजार बनाने में सहायक सिद्ध हुई। मगध की उर्वरा भूमि ने कृषि उत्पादन में वृद्धि सम्भव करके मगध की आर्थिक सम्पन्नता में सहयोग प्रदान किया। इससे राजकीय आय में पर्याप्त वृद्धि हुई। व्यापार और वाणिज्य के विकास तथा मुद्रा के प्रचलन से भी राजकीय आय में संवृद्धि आयी। इसी कारण मगध के शासकों को एक स्थायी सेना का निर्माण करने में सफलता मिली। निस्संदेह एक स्थायी सेना ने मगध के उत्थान और विस्तार में बहुत सहयोग दिया।
सांस्कृतिक दृष्टि से मगध में आर्यों एवं अनार्यों की सभ्यता का अद्भुत मिश्रण हुआ। मगध में आर्य सभ्यता का प्रसार देर से हुआ और वहां तक पहुंचते-पहुंचते उसकी शक्ति और श्रेष्ठता की भावना लुप्त हो गयी, जिसके कारण मगध में ब्राह्मणों के प्रतिक्रियावादी विचार श्रेष्ठता प्राप्त न करे सके और वहां उदारता तथा समन्वय का वातावरण बना रहा।
इसी उदारता के वातावरण में मगध में बौद्ध एवं जैन धर्मों का उत्थान हुआ। आर्यों एवं अनार्यों के मिश्रण से परिपूर्ण मगध के युद्धप्रिय निवासियों ने महात्मा बुद्ध और महावीर के अहिंसा के विचारों को सुना। जैसा कि डॉ. आर.के. मुखर्जी लिखते हैं: ‘रूढि़वादी ब्राह्मण सभ्यता द्वारा लगाये गये सामाजिक बंधनों में शिथिलता और बौद्ध तथा जैन धर्मों के सार्वजनिक दृष्टिकोण ने, जिन्हें मगध में सुखद स्थान प्राप्त हुआ था, इस क्षेत्र के राजनैतिक दृष्टिकोण को विस्तृत कर दिया और इस क्षेत्र को एक शक्तिशाली साम्राज्य का केन्द्र बिन्दु बना दिया।
मगध की शासन व्यवस्था भी जिसमें राजा का अधिकार पैतृक था और जिसमें राजा को अपनी शक्ति के विस्तार में सहायता मिली, मगध के उत्थान में सहायक सिद्ध हुई। राजतंत्र व्यवस्था में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। पहले भी कबायली व्यवस्था में राजा और उसके अधिकारी युद्ध में लूटे हुए धन का कुछ भाग ही प्राप्त करते थे। नवीन व्यवस्था में उस पर एकमात्र राजा का अधिकार हो गया। इस व्यवस्था से राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। मगध का शासक बिम्बिसार पहला व्यक्ति था, जो मगध की संपन्नता का लाभ उठाकर एक स्थायी सेना रख सका।
मगध के विभिन्न राजवंशों तथा शासकों कीव्यक्तिगत योग्यता एवं नीतियां भी मगध के उत्थान का एक प्रमुख कारण थीं। बिम्बिसार जो कि हिरयण्क वंश का था, के शासनकाल में मगध ने खूब उन्नति की। उसके द्वारा विजय और विस्तार की शुरू की गयी नीति अशोक की कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई। बिम्बिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया। उसने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। उसकी प्रथम पत्नी कोशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। कोशलदेवी के साथ दहेज में प्राप्त काशीग्राम से उसे 1 लाख की आय होती थी। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवि राजकुमारी चल्हना थी, और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। इस प्रकार बिम्बिसार को राजनीति प्रतिष्ठा प्राप्त होने के साथ-साथ उत्तर और पश्चिम में मगध के साम्राज्य विस्तार का द्वार भी मिल गया। मगध की असली शत्रुता अवन्ति से थी। इसके राजा चंडप्रद्योत महासेन की बिम्बिसार से लड़ाई हुई थी, किन्तु दोनों ने अंत में दोस्त बन जाना ही उपयुक्त समझा। गंधार के राजा के साथ हुए युद्ध में प्रद्योत को विजय नहीं मिली थी, किन्तु गंधार के इसी राजा ने बिम्बिसार के पास पत्र और दूतमंडल भेजा। इस प्रकार विजय और कूटनीति से बिम्बिसार ने मगध को ईसा पूर्व छठी सदी में सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया। बिम्बिसार की हत्या कर उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। अपने समूचे शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया। कोशल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने और अपने जमाई को काशी सौंपकर सुलह करने को बाध्य होना पड़ा। उसने रिश्तेदारी का लिहाज न करते हुए वैशाली पर हमला किया और उसके खिलाफ षडयंत्र रचे। इस प्रकार काशी और वैशाली के मिलने से मगध का और अधिक विस्तार हुआ। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उद्यन के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन शुरू हुआ। अवन्ति की शक्ति को तोड़ना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही अवन्ति और मगध के बीच की सौ साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया। शिशुनागों के बाद नन्दों का शासन शुरू हुआ। इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर, जो उस समय पंजाब पर हमला कर चुका था, पूर्व की और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। नन्दों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया। महापदम नंद ने अपने को ‘एकराट’ कहा। उसने न सिर्फ कलिंग पर कब्जा किया, बल्कि अपने खिलाफ विद्रोह करने वाले कोशल को भी हथिया लिया। बाद के नन्द शासक दुर्बल और अलोकप्रिय सिद्ध हुये। उनके शासन के स्थान पर मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। मौर्यवंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ दक्षिण में मगध का विस्तार किया, बल्कि उत्तर-पश्चिम में भी अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति के बल पर मगध की विजय पताका फहरायी। अशोक को अपने जीवन काल में सिर्फ कलिंग के साथ संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत पर मगध के साम्राज्य का आधिपत्य कायम था।
Question : इस प्रश्न-पत्र के साथ दिये जा रहे मानचित्र में, निम्नलिखित स्थानों में से किन्हीं पन्द्रह पर निशान लगाइये और मानचित्र में अंकित स्थानों पर वर्णनात्मक टिप्पणियां लिखिएः-
1. अजमेर, 2. अहमदनगर, 3. इलाहाबाद, 4. बादामी, 5. भुवनेश्वर, 6. चित्रकूट, 7. चित्तौड, 8. चंडीगढ़, 9. देहरादून, 10. धारा, 11. एलिफैन्टा, 12. एलोरा, 13. गुवाहाटी, 14. हैदराबाद, 15. हड़प्पा, 16. इन्द्रप्रस्थ, 17. जगन्नाथपुरी, 18. कल्याण, 19. कावेरीपट्टनम, 20. लोथल।
(2001)
Answer : 1. अजमेर: अजमेर अथवा अजयमेरू राजस्थान के तारागढ़ की प्रमुख तराई में स्थित एक प्रमुख नगर है। 1113 ई. में शाकंभरी के अजय देव ने अजमेर की स्थापना की थी। चौहान वंश के शासकों ने अजमेर को गौरवशाली बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। शेरशाह और अकबर के साम्राज्य में भी यह सम्मिलित था। अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहां अन्ना सागर झील के पास शाहजहां ने संगमरमर झील का निर्माण कराया था। मनुची ने अमजेर को सफेद वस्त्र का केन्द्र कहा है।
2. अहमदनगर: 1490 ई. में अहमद नगर की स्थापना मलिक अहमद निजामशाह ने की थी। 13वीं सदी में यह क्षेत्र बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत था। अहमद नगर यादववंश से लेकर मराठों की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा। मुगलों को अहमद नगर की स्वतंत्र सत्ता का बराबर प्रतिरोध झेलना पड़ा। अकबर के समय चांदबीवी का असफल प्रतिरोध हुआ। अंततः 1636 में शाहजहां ने अहमद नगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के बाद यह मराठों के अधीन आ गया।
3. इलाहाबादः उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के संगम पर बसे हुए इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग। यहां के अशोक स्तंभ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सैनिक एवं कलात्मक गतिविधियों के विषय में पता चलता है। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर उसे इलाहाबाद का नाम दिया था। प्रयाग का धार्मिक महत्व है और इसे तीर्थराज कहा जाता है। हर्षवर्द्धन प्रति पांचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था।
4. बादामीः बादामी आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत के चालुक्यों, विशेषकर कलात्मक गतिविधियों से संबद्ध है। इसका प्राचीन नाम वातापी था। इसकी स्थापना चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम ने की थी। चालुक्यों की राजधानी बादामी गुफा मंदिर प्राक द्रविड़- वस्तुशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह हिन्दुओं, बौद्धों एवं जैनों से संबंद्ध एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र था।
5. भुवनेश्वरः वर्तमान उड़ीसा प्रांत की राजधानी है जो मध्यकाल में भी उत्कल या कलिंग प्रांत की राजधानी थी। यहां आरंभिक कलिंग शैली जो कि आर्य नागर शैली का विकसित रूप थी, के कई आकर्षक मंदिर मिले हैं। यहां पर कड़ा अथवा कलिंग के शासकों ने कई मंदिर बनवाये जिनमें लिंगराज मंदिर सर्वोत्कृष्ट है। राजा-रानी मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर आदि यहां के अन्य मंदिर हैं।
6-7 चित्रकूट व चित्तौड़ः राजस्थान के उदयपुर जिले में चंबल की सहायक गम्भीरा नदी के किनारे स्थित चित्तौड़ का नाम प्राचीन काल में चित्रकूट था। यह मध्यकाल में मेवाड़ रियासत का प्रमुख केन्द्र था। यह उत्तरी भारत से गुजरात के तट तक पहुंचने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। सातवीं, आठवीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बप्पारावल ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था जो सोलहवीं शताब्दी तक बना रहा। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम तुर्क सुल्तान था, जिसने 1302-03 ई. में चित्तौड़ को जीतकर उसे खिज्राबाद का नाम दिया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा मुगल शासक अकबर ने भी चित्तौड़ पर क्रमशः 1536 तथा 1567 ई. में अधिकार किया था। चित्तौड़ की इमारतों में राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ और पदमिनी का महल उल्लेखनीय हैं।
8. चंडीगढ़ः चंडीगढ़ आधुनिक काल में वैज्ञानिक पद्धति से बसाया हुआ एक सुंदर नगर है। यह वर्तमान में हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ स्थित उच्च न्यायालय ही दोनों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का कार्य करता है।
9. देहरादूनः हिमालय की तराई में स्थित देहरादून काफी खूबसूरत शहर है। अभी हाल ही में बने नये राज्य उत्तरांचल की राजधानी देहरादून को ही बनाया गया है। भारत के प्रमुख हिल स्टेशन मसूरी का मार्ग देहरादून से ही गुजरता है।
10. धाराः धारा से मालवा के परमारों ने शासन किया था। राजा मुंज के समय से ही धारा नगरी शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र था। राजा भोज (1010-1055) ने उज्जैन के स्थान पर इसे मालवा की राजधानी बनाया था। ‘नवसहसांक चरित’ तथा ‘दशरूपक’ की रचना धारा नगरी में ही हुई थी। 1305 ई. में मालवा के महलकदेव को हराकर अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक ने धारा नगरी समेत मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया।
11. एलिफेंटाः मुंबई से सात मील उत्तर-पूर्व में स्थित एक छोटे से द्वीप अपोलोबंदर की पहचान एलीफैन्टा से की गयी है। इसका प्राचीन नाम धारापुरी था। एलीफैन्टा की गुफाओं में 500-600 ई. के नटराज (भगवान शंकर) की लीलाओं का चिंत्रकन किया गया है। यहां उत्कीर्ण नटराज शिव की मूर्ति से गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशिष्टता के संकेत मिलते हैं। 1600 ई. में पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। उन्होंने ही यहां हाथी की मूर्ति को देखकर इस क्षेत्र को एलीफैन्टा नाम दिया था। यहां से बौद्ध चैत्य के अवशेष भी मिले हैं।
12. एलोराः एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 25 किमी. पश्चिमोत्तर में स्थित है। यह क्षेत्र छठी शताब्दी से दसवीं शताब्दी के मध्य बने 34 शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटों ने करवाया था। गुफाएं ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मतों से संबंद्ध हैं। यहाँ 900 ई. में जैनियों का प्रभाव दिखाई देता है, ‘इन्द्रसभा’ भवन इसका उदाहरण है।
13. गुवाहाटीः असम के गुवाहाटी क्षेत्र में प्राचीन काल का प्राग्ज्योतिषपुर अथवा कामाख्या एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्र था। महाभारत के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने प्राग्ज्योतिषपुर के शासक नरकासुर का वध किया था। महाभारत युद्ध में प्राग्ज्योतिषपुर के शासक भगदत्त ने भाग लिया था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यह क्षेत्र गुप्तों के प्रभाव में भी था। रघुवंश में भी इस क्षेत्र की चर्चा है। यहां के शासक भास्कर वर्मन का हर्षवर्द्धन से मैत्री संबंध था।
14. हैदाराबादः हैदराबाद आधुनिक आंध्रप्रदेश की राजधानी है। इसकी स्थापना गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह ने 1591 में की था। बाद में इसी नाम से निजामउलमुल्क ने एक पृथक निजामशाही राज्य की स्थापना की। यह राज्य द. भारत की राजनीति का प्रमुख केन्द्र रहा और अंग्रेजों के साथ इसने बहुत निष्ठा दिखायी। इस नगर में अनेक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थापत्य हैं, जिनमें चारमीनार व सालारजंग संग्रहालय विश्व प्रसिद्ध हैं।
15. हड़प्पाः हड़प्पा पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। सिन्धु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्खनन 1921 में हड़प्पा में ही हुआ था। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक विकसित नगर था। यहां से विशाल धान्य कोठार, लिंग-योनि तथा कब्रिस्तान- H के अवशेष मिले हैं। नगर निर्माण योजना के समस्त लक्षण यहां के अवशेषों में मिले हैं।
16. इंद्रप्रस्थः दिल्ली के पुराना किला वाले क्षेत्र को इन्द्रप्रस्थ के नाम से ही जाना जाता है। महाभारत काल में यह काफी प्रसिद्ध था तथा यह पांडवों की राजधानी थी। इन्द्रप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ भगवान इन्द्र का निवास है। इन्द्रप्रस्थ का उल्लेख हमें कई पुराणों में भी मिलता है।
17. जगन्नाथपुरीः जगन्नाथपुरी वर्तमान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। मध्यकाल में धार्मिक केन्द्र के रूप में इसका काफी महत्व था। जगतगुरू शंकराचार्य ने धार्मिक एकता के लिए जो चार मठ देश के चारों कोनों में बनवाये, उनमें से एक जगन्नाथपुरी में स्थित है। यहां भगवान जगन्नाथ (विष्णु) की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं।
18. कल्याणः कल्याण वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी तट पर मुंबई के समीप थाणे जिले में स्थित है। प्राचीन काल में कल्याण का महत्व बहुत था। 14वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्कों ने इसका नाम इस्लामाबाद रखा था। 1536 ई. में पुर्तगालियों ने इस पर अधिकार कर लिया। बाद में शिवाजी ने कल्याण पर अधिकार कर लिया। 1674 ई. में शिवाजी ने अंग्रेजों को कल्याण में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी।
19. कावेरीपट्टनमः कावेरीपट्टनम तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर तंजौर जिले में कावेरी नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। तमिल काव्य, लैटिन एवं ग्रीक स्रोत तथा पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से ही कावेरीपट्टनम का महत्व बना हुआ था। कावेरीपट्टनम की पहचान मुहर अथवा पुगार से भी गयी है। यह चोलों की प्राचीन पत्तन राजधानी थी। चोल शासक करिकाल ने पुहार का निर्माण कराया तथा वहां बंदरगाह और बांध भी बनवाये। मौर्योत्तर युग में रोम के साथ व्यापारिक संबंध होने के कारण कावेरीपट्टनम काफी संपन्न था।
20. लोथल: लोथल गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में खंभात की खाड़ी के ऊपर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का अत्यंत विकसित चरण का एक व्यापारिक नगर था। यहां बंदरगाह, फारस की मुहर तथा अत्यंत सुंदर चित्रित मृद्भांड मिले हैं। यहां एक ऐसे कब्र का अवशेष मिला है जिसमें एक साथ स्त्री और पुरुष के शव हैं। यहां से चावल के भी अवशेष मिले हैं। यही से अग्निवेदी के भी अवशेष मिले हैं।
Question : मौर्यवंश के इतिहास जानने के साधनों का उल्लेख कीजिए। अशोक के शिलालेखों का ऐतिहासिक साधन के रूप में उनके महत्व का परीक्षण कीजिये।
(1999)
Answer : भारतीय इतिहास में मौर्यकाल का महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक एकता स्थापित की। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त (संस्थापक), बिंदुसार और अशोक के नाम उल्लेखनीय हैं। मौर्यों ने राजनीतिक एकीकरण के अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्रों के अभ्युदय तथा कला-कौशल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी हमें अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता हैः
1. संस्कृत साहित्य: मौर्य काल पर प्रकाश डालने वाले संस्कृत साहित्य में अर्थशास्त्र एवं पुराणों सहित कई नाटक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मौर्य वंश के इतिहास के लिए ‘अर्थशास्त्र’ सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य की कृति है। चंद्रगुप्त के शासनकाल की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर अर्थशास्त्र से प्रकाश पड़ता है। उसने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजा के कर्त्तव्यों, उसकी वैदेशिक नीति, गुप्तचर संगठन तथा तत्कालीन भू-व्यवस्था, वित्तीय नीति कानून आदि का भी वर्णन किया है।
पुराणों में अनेक ऐसे तथ्य वर्णित हैं, जिनकी ऐतिहासिकता एवं सत्यता संदेहास्पद है, तथापि मौर्य वंश के इतिहास के लिए पुराणों का अत्यधिक महत्व है। विष्णु पुराणों का अत्यधिक महत्व है। विष्णु पुराण में न केवल मौर्य वंशीय राजाओं के नाम वरन् उनसे संबंधित विभिन्न घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र व पुराणों के अतिरिक्त मुद्राराक्षस (विशाखदत्त), वृहत्कथामंजरी (क्षेमेन्द्र), कथासरित्सागर (सोमदेव) जैसे नाटकों से मौर्यवंश की जानकारी मिलती है। मुद्राराक्षस से मौर्यवंश की स्थापना पर प्रकाश पड़ता है। महाकवि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र से मौर्य वंश के पतन की जानकारी मिलती है। कल्हण की राजतरंगिणी में सम्राट अशोक व उनके उत्तराधिकारियों का भी वर्णन किया गया है। भास द्वारा रचित नाटक ‘स्वप्नवासवदत्ता’, ‘प्रतिज्ञा यौंगधरायण’ मौर्य काल पर ही आधारित है। कात्यायन द्वारा पाणिनि की ‘अष्टाध्यायी’ पर रचित वार्तिक भी मौर्यवंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं।
2. बौद्ध साहित्य: बौद्ध लेखकों ने अपनी रचनाओं में अशोक को प्रमुख स्थान दिया, इसी कारण बौद्ध साहित्य का मौर्यों के संबंध में विपुल सामग्री प्राप्त होती है। दीपवंश, महावंश, मिलिंदपन्हो, अट्ठकथा, दिव्यावदान, कुणालावदान, अशोकावदान सहित ‘मंजूश्री मूल कल्प’ जैसे बौद्ध साहित्य मौर्य वंश पर प्रकाश डालते हैं।
3- जैन साहित्य: कतिपय जैन ग्रंथों से भी मौर्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस संदर्भ में ‘परिशिष्ट पर्वन’ तथा ‘कल्पसूत्र’ विशेष महत्व के है। चंद्रगुप्त व अंतिम नंदशासक के संघर्ष की कहानी ‘परिशिष्ट पर्वन’ में उल्लिखित है। कल्पसूत्र से भी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। भद्रबाहुचरित से चंद्रगुप्त के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। हेमचंद्र की कृति ‘स्थविरावलिचरित’ भी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी देती है।
4. तमिल साहित्य: तमिल लेखकों ‘मामुलनार’ तथा ‘परणार’ के विवरणों से ऐसा ज्ञात होता है कि संभवतः चंद्रगुप्त ने दक्षिण में त्रिचनापल्ली की पोदियिल पहाड़ी तक आक्रमण किया था।
5. यूनानी व रोमन विवरण: मौर्यकाल से पूर्व के यूनानी लेखक स्काइलैक्स, हेरोडोटस, टेसियस, नियार्कस, ओनेसिक्रिटस एवं अरिस्टो-बुलस के ग्रंथों से उस युग की उन परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, जिन पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यूनानी शासक सेल्युकस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में तथा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था का आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक ‘इंडिका’ में किया है। यद्यपि मेगास्थनीज की पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, परन्तु बाद के यूनानी यात्र विवरणों में यह उद्धरण के रूप में वर्तमान है। बाद के जिन लेखकों ने प्राचीन यूनानी लेखकों की रचनाओं को उद्धृत किया है। उनमें डायोनीसस, स्ट्राबो, प्लिनी, टॉलमी, एरियन, जस्टिन, डायोडोरस एवं प्लूटार्क महत्वपूर्ण हैं।
6. चीनी व तिब्बती विवरण: फाह्यान और ह्नेनसांग के विवरणों से भी मौर्यकाल के विषय में जानकारी मिलती है। दोनों ही यात्री अशोक के हृदय परिवर्तन के पूर्व उसके क्रूर स्वभाव का उल्लेख करते हैं। तिब्बती लेखक लामा तारानाथ की रचनाओं में भी मौर्य वंश पर प्रकाश पड़ता है।
7. पुरातात्विक सामग्री: मौर्यवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली पुरातात्विक सामग्री में स्मारक, अभिलेख, कलाकृतियां एवं मिट्टी के बर्तन महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पाटलिपुत्र में हुए उत्खनन से प्राप्त होने वाले भग्नावशेषों से ज्ञात होता है कि मौर्यकालीन अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है।
उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मौर्यों पर प्रकाश डालने वाली प्रचुर सामग्री उपलब्ध है, जिनके अध्ययन से मौर्यकालीन इतिहास का सरलतापूर्वक निर्माण किया जा सकता है। अशोक के शासन एवं उसकी नीति की जानकारी उसके अभिलेखों से होती है। अशोक के अभिलेख न सिर्फ भारत में, बल्कि अफगानिस्तान में भी पाये गये हैं। इन अभिलेखों में प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कुछ अभिलेख खरोष्ठी एवं अरामाइक तथा यूनानी एवं आरामइक में लिखे गये हैं। सर्वप्रथम टीफेन्थैलर ने 1750 ई. में दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था, किन्तु अशोक के अभिलेखों को पढ़ने व उसका संबंध अशोक से जोड़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को 1837 में सफलता प्राप्त हुई। अशोक द्वारा इन अभिलेखों को महत्वपूर्ण स्थानों पर, नगरों के समीप, प्रसिद्ध व व्यस्त मार्गों पर व धार्मिक स्थानों पर उत्कीर्ण कराया गया था, जिससे अधिक से अधिक लोग उसके आदेशों से परिचित हो सकें। अशोक के अभिलेख भी कई प्रकार के हैं- शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुफा लेख। शिलाओं पर उत्कीर्ण अभिलेखों को बृहद् एवं लघु, शिलालेखों में वर्गीकृत किये गये हैं। बड़े शिलालेख संस्था में 14 हैं, जो कालसी, मानसेहरा शहबाजगढ़ी, गिरनार, सोपारा, येरेगुडी, धौली तथा जौगढ़ में पाये गये हैं। लघु शिलालेख बैराट, रूपनाथ, सहसराम, ब्रह्मगिरि, गाविमठ, जटिंगारामेश्वर, मास्की, पालकीगुण्डु, राजूल मंडागिरि, सिद्धपुर गुर्जरा, येरेगुडी व अहरौरा में पाये गये हैं।
स्तंभ लेख संख्या में सात हैं तथा इलाहाबाद, दिल्ली-टोपरा, दिल्ली-मेरठ, लौरिया-अरेराज, लौरिया-नंदनगढ़ तथा रामपुरवा में मिले हैं। इसके अतिरिक्त निग्गलीसागर, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, बैराट, रुम्मिनदेई व कंधार में भी मिले हैं। तीसरी श्रेणी गुहा अभिलेखों की है। ये अभिलेख गया के पास की बराबर पहाडि़यों में बनी गुफाओं में उत्कीर्ण हैं। इसकी संख्या तीन है- सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा एवं कर्ण चौपड़ गुफा।
अशोक के अध्ययन के लिए उसके अपने अभिलेख ही सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। सब कुछ होते हुए भी अशोक के अभिलेख व्यक्तिगत हैं, क्योंकि इनमें एकमात्र अशोक का ही विवरण है। सर्वप्रथम 1877 ई. में अशोक के अभिलेखों का एक प्रामाणिक संग्रह निकला था और फिर 1925 में दूसरा प्रामाणिक संग्रह प्रकाशित हुआ। प्रामाणिक एवं व्यक्तिगत होने के बावजूद अशोक के अभिलेखों से उसके प्रारंभिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। अशोक का नाम मास्की के प्रथम लघु शिलालेख में मिलता है। इसी अभिलेख में ‘पियदस्सी’ शब्द का समीकरण अशोक के साथ हुआ है। अफगानिस्तान से बंगाल और हिमालय से मैसूर तक फैला अशोक का विशाल साम्राज्य जम्बू द्वीप कहलाता था। इस शब्द का प्रयोग प्रथम लघु शिलालेख में हुआ है।
अशोक के पांचवें और तेरहवें अभिलेख में साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाली अनेक जातियों एवं जनपदों के नामों का उल्लेख किया गया है। इन जातियों में यवन, कम्बोज, गांधार, रिष्टिक, भोग, पितनिक, आंध्र, पुलिंद प्रमुख हैं। 13वें शिलालेख में अशोक के समकालीन विदेशी शासकों के नाम मिलते हैं। ये शासक थे- सीरिया का राजा एण्टियोकस द्वितीय थियोस, मिड्ड का राजा टॉलमी द्वितीय, मकदूनिया का शासक एण्टिगोनस गोनाटस, साइरीन का राजा मगस और एपिरस का राजा अलेक्जेंडर। ये शासक अशोक के प्र्रभाव क्षेत्र से बाहर थे। अशोक के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अशोक ने जिस नये ‘धम्म’ की कल्पना की वह बौद्धधर्म से भिन्न था। इसके अंतर्गत चार आर्य सत्य, आष्टांगिक मार्ग या निर्वाण की कल्पना नहीं की गई। अपने धम्म की व्याख्या अशोक ने स्वयं अपने अभिलेखों में की। अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों का इसमें समावेश किया गया था। यह वास्तव में नैतिक नियमों का संग्रह था। सातवें स्तंभाभिलेख द्वारा अशोक ने धर्मप्रचार के लिए जो कार्य किये, उसकी जानकारी मिलती है। धम्म से संबद्ध घोषणायें पत्थर के टुकड़ों और स्तम्भों पर लिपिबद्ध करवाकर महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित की गयीं। अभिलेखों द्वारा अशोक ने धार्मिक घोषणायें करवायी, धर्म स्तंभों का निर्माण करवाया तथा धम्ममहापात्रों की नियुक्ति की। उसने धर्म यात्रएं की तथा विदेशों में प्रचारकों को भेजा। उनके इन कार्यों से धर्म की अत्यधिक प्रगति हुई। उसने पुरुषों, राजुकों को धम्म संबंधी निर्देश दिये तथा युक्तों, राजुकों और प्रादेशिकों को आदेश दिया कि वे प्रति पांच वर्षों पर धर्मानुशासन के लिए निकलें। अशोक पहला शासक था, जिसने मानव कल्याण और मानव के नैतिक उत्थान के लिए इतना अधिक प्रयास किया। उसका धम्म सैद्धांतिक से ज्यादा व्यावहारिक था। इसका उद्देश्य नागरिकों में सामाजिक नैतिकता का विकास करना था। अशोक के अभिलेख से ही पता चलता है कि उसने अपनी प्रजा को अपनी संतान का दर्जा दिया और सदैव जनहित में लगा रहा। अशोक के जनकल्याणकारी प्रशासन की रूपरेखा तथा कलिंग युद्ध की भीषणता एवं उसके बाद हुए हृदय परिवर्तन जैसे तथ्यों की जानकारी, बौद्ध संघ में सुधार जैसी गतिविधियों पर उसके अभिलेख उल्लेखनीय प्रकाश डालते हैं।
Question : फ्हर्षवर्धन स्वयं महान था, परंतु उसे बाण एवं ह्नेनसांग ने महत्तर बना दिया।य् इस कथन की विवेचना कीजिए।
(1999)
Answer : हर्षवर्द्धन सातवीं शताब्दी की भारतीय राजनीति का श्रेष्ठतम नायक था। एक कुशल योद्धा, साम्राज्य निर्माता, प्रशासक, लोक कल्याणकारी और विद्यानुरागी शासक के रूप में सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। अनेक विद्वान उसे अंतिम हिंदू सम्राट एवं साम्राज्य निर्माता मानते हैं। परंतु उनकी उपलब्धियों को प्रकाश में लाने का श्रेय उसके दरबारी बाणभट्ट एवं चीनी पर्यटक ह्नेनसांग को जाता है।
हर्षवर्द्धन के दो महत्वपूर्ण अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं- मधुबन (आजमगढ़ उत्तर प्रदेश) तथा बांसखेड़ा (शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश) ताम्र पत्र अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों में हर्षवर्द्धन के राज्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। राज्यवर्द्धन की हत्या के पश्चात् 606 ई. में हर्षवर्द्धन थानेश्वर का राजा बना। उसकी राजधानी अब थानेश्वर से कन्नौज चली आयी। इसके साथ ही कन्नौज अब उत्तरी भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। अपने सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप हर्षवर्द्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हर्षवर्द्धन के साम्राज्य की वास्तविक जानकारी उसके अभिलेखों, हर्षचरित तथा ह्नेनसांग के विवरणों से प्राप्त होता है। समस्त उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के अतिरिक्त हर्ष का एक अन्य प्रमुख कार्य था-प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। हर्षवर्द्धन ने गुप्तों द्वारा स्थापित मूल प्रशासनिक व्यवस्था को बनाये रखा, परंतु आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन एवं परिवर्तन भी किया। राजतंत्रत्मक व्यवस्था के अनुकूल हर्षवर्द्धन राज्य और शासन का प्रधान था। राज्य की समस्त शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित थीं। सैद्धांतिक रूप से वह सर्वशक्तिशाली एवं निरंकुश शासक था, जिस पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं था, परंतु व्यवहारतः वह प्रजावत्सल शासक था। वह सदैव जनहित के कार्यों में लगा रहता था तथा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था। वह धर्म और दंड का समुचित व्यवहार करने वाला, शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला तथा प्रजा के आध्यात्मिक कल्याण के लिए काम करने वाला था। हर्ष शासक और विजेता के रूप में महान था, परंतु शांति के निर्माता के रूप में वह महत्तर था। शांति उसकी विजय युद्धों में अर्जित विजयों से कहीं अधिक व्यापक थी।
हर्ष ने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जितनी कुशलता से वह तलवार पकड़ता था, उतनी ही कुशलता से वह लेखनी भी संभालता था। इसी कारण उसके शासनकाल में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उÂति हुई। कन्नौज का सम्मेलन हर्ष के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ह्नेनसांग के महायान संबंधी तर्कों से प्रभावित होकर सम्राट हर्ष ने महायान संप्रदाय के प्रचार के लिए कन्नौज में अनेक धर्मों के अनुयायियों की सभा का आयोजन किया। 18 दिनों तक यह सभा चलती रही तथा ह्नेनसांग ने इस सभा में महायान की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। हर्ष के शासनकाल की एक प्रमुख उपलब्धि प्रत्येक पांच वर्ष बाद धार्मिक सभा का आयोजित होना था। हर्ष विद्वानों का महान आश्रयदाता था। उसके राज दरबार में अनेक प्रसिद्ध कवि एवं लेखक रहते थे। इन कवियों में प्रमुख ‘कादम्बरी’ तथा ‘हर्षचरित’ के रचयिता ‘बाणभट्ट’ थे। बाण के अतिरिक्त मातंग दिवाकर व मयूर नामक दो अन्य प्रमुख कवि थे। मयूर ने ‘सूर्य शतक’ की रचना की थी। शीलभद्र नामक विद्वान भी हर्ष के काल में ही हुआ था। हर्ष के राजदरबार में एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान जयसेन था, जो शब्द विद्या, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र तथा गणित का प्रकांड विद्वान था। हर्ष ने बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध केन्द्र नालंदा को भी खुले हाथों से दान दिये। हर्ष ने तीन उच्च कोटि के नाटकों ‘रत्नावली’, ‘प्रियदर्शिका’ तथा ‘नागानंद’ की रचना की थी। 11वीं शताब्दी के लेखक सोड्ढल ने अपनी ‘अवन्ति सुंदरी कथा’ में हर्ष को ‘कवीन्द्र’ कहा है। जयदेव ने हर्ष को कालिदास तथा भास के समान विद्वान माना है। हर्ष ने भी अनेक सार्वजनिक हित के कार्य किये। उसने अनेक परोपकारी और धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कराया। हर्ष के द्वारा अनेक स्तूप, चैत्य व विहारों का निर्माण कराया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए मार्ग व धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया। नालंदा विश्वविद्यालय आदि शिक्षा केंद्रों की उÂति के लिए हर्ष ने महत्वपूर्ण कार्य किये। हर्ष निःसंदेह प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। हर्ष जिस समय सिंहासनारूढ़ हुआ, उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी तथा उसके समक्ष अनेक कठिनाइयां थीं, परंतु हर्ष ने अत्यंत साहस व कुशलता से समस्त समस्याओं का सामना किया व उन पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। भारत, जो हर्ष से पूर्व बहुसंख्यक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, हर्ष के शासनकाल में एकता के सूत्र में आबद्ध हो गया।
हर्षवर्द्धन के इतिहास की जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोतों में उसके दरबारी कवि बाणभट्टद्वारा सात अध्यायों में लिखा गया
हर्षचरित उसके राज्य का इतिहास है। पहला अध्याय लेखक के जीवन व परिवार से संबंधित है। दूसरे, तीसरे एवं चौथे अध्यायों में हर्ष के पूर्वजों तथा थानेश्वर के राजवंश का वर्णन है। पांचवें और छठें अध्यायों में हर्ष के युद्धों एवं विजय का वर्णन है। अंतिम अध्याय में विंध्य के वनों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। हर्षचरित के अध्ययन से तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का पता चलता है। बाणभट्ट ने अलंकारपूर्ण शब्दों में प्रभाकर वर्द्धन के व्यक्तित्व, हर्षवर्द्धन के जन्म, उसकी बाल्यावस्था, राज्यश्री का विवाह, प्रभाकर वर्द्धन, राज्यवर्द्धन और ग्रहवर्मन की मृत्यु, हर्षवर्द्धन के राज्यारोहण, राज्यश्री की खोज एवं अन्य घटनाओं का वर्णन किया है। हर्षचरित में तत्कालीन महत्वपूर्ण राज्यों, प्रशासन और हर्ष की धार्मिक प्रवृत्तियों का भी उल्लेख है।
हर्ष के शासनकाल की एक प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्नेनसांग का भारत आगमन था। ह्नेनसांग का भारत भ्रमण-वृत्तांत तीन रूपों में उपलब्ध है। पहला तो ह्नेनसांग द्वारा रचित ‘सी-यू-की’ नामक ग्रंथ है और दूसरा ग्रंथ ह्नेनसांग की जीवनी है, जिसे उसके मित्र ‘शयन-ही-ली’ ने लिखा था। तीसरा ग्रंथ ह्नेनसांग की यात्र का सारांश है, जिसे उसके एक शिष्य एवं सहायक कार्यकर्ता ने तैयार किया था, जो ‘कांचू’ के नाम से प्रसिद्ध है। ह्नेनसांग के अनुसार हर्ष का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। राजा के परिश्रम तथा दानशीलता की भी ह्नेनसांग ने बहुत प्रशंसा की है। राजा के समय का विभाजन अत्यंत सतर्कता से किया गया था। उसका सारा समय धार्मिक कार्यों तथा शासन संबंधी मामलों में बंटा हुआ था। ह्नेनसांग के अनुसार हर्ष के काल में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी तथा उनसे बेगार नहीं लिया जाता था। जनता पर कर भी अधिक नहीं थे। भू-कर भी उपज का 1/6 भाग होता था। हर्ष राजकीय आय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से उसे चार भागों में विभक्त करता था। पहला भाग राजकीय कार्यों के लिए, दूसरा सरकारी कर्मचारियों के लिए, तीसरा विद्वानों की सहायता व चौथा दान के लिए रहता था। न्याय व्यवस्था अत्यंत सक्षम थी तथा अपराधियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। ह्नेनसांग ने लिखा है कि वैसे अपराध बहुत कम होते थे। हर्ष ने अनेक धर्मशालायें आदि बनवायी थीं। ह्नेनसांग के अनुसार राजधानी कन्नौज एक भव्य नगर था तथा उसका सम्मान हर्ष के समय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। उसने हर्ष की शक्तिशाली सेना का भी उल्लेख किया है। उसके अनुसार हर्ष की सेना में 60,000 हाथी व 1,00,000 घुड़सवार थे। ह्नेनसांग के वृत्तांत के अनुसार हर्षकालीन आर्थिक स्थिति में कृषि की प्रधानता थी। सिंचाई की उचित व्यवस्था करके कृषि की उन्नति की जाती थी। भारत से विदेशों को चंदन की लकड़ी, जड़ी-बूटियां, गर्म मसाले, कपड़े तथा अन्य वस्तुएं निर्यात होती थीं तथा भारत को घोड़े, धूप, हीरा व हाथी दांत आदि आयात किया जाता था। भारत में ऊनी, सूती, रेशमी व मलमल का कपड़ा बहुत अच्छा तैयार किया जाता था।
चीनी यात्री ने अनेक बौद्ध विहारों का वर्णन किया है, जो उस समय के प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र थे। उस समय व्याकरण, यांत्रिक, कला, वैद्यक, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध विहारों के अतिरिक्त गुरुकुलों में भी शिक्षा दी जाती थी। इन्हें राज्य की तरफ से अनुदान मिलता था। हर्ष के समय में उत्तरी भारत में शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र नालंदा महाविहार था। इस प्रकार चीनी यात्री के विवरण से हर्षकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। अतः स्पष्ट है कि हर्षवर्द्धन स्वयं तो महान था ही, परंतु उसे बाण एवं ह्नेनसांग ने महत्तर बना दिया।
Question : सिंधु घाटी सभ्यता की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिये। महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बताइये, जहां से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के नष्ट होने के कारणों का परीक्षण कीजिये।
(1999)
Answer : विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस सभ्यता के अवशेषों के प्रकाश में आने से अब निश्चित हो गया है कि आर्यों के आगमन के पूर्व ही भारत में पूर्ण विकसित नागरिक सभ्यता का उदय हो चुका था। अब यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत की सभ्यता भी मिड्ड और मेसोपोटमिया की सभ्यताओं की तरह ही अति प्राचीन है। इतना ही नहीं, भवन निर्माण और नगर निर्माण योजना के क्षेत्र में तो यह सभ्यता मिड्ड और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी अधिक विकसित थी। चारागाही, घुमंतू और खेतिहर समुदाय सिंधु के मैदान में आकर बसे। आगे चलकर इन्हीं खेतिहर समुदायों और छोटे-छोटे नगरों की नींव पर हड़प्पा सभ्यता पनपी। हड़प्पा युग में जीवन निर्वाह की व्यवस्था अनेक प्रकार की फसलों, पालतू पशुओं और जंगली जानवरों पर निर्भर थी। इस विविधता के कारण ही जीवन-निर्वाह व्यवस्था मजबूत बनी हुई थी। वे प्रति वर्ष एक साथ दो फसलें उगा रहे थे। इससे अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गयी थी कि नगरों में रहने वाली और अपने लिए खाद्या का उत्पादन खुद न करने वाली बड़ी जनसंख्या का भरण-पोषण किया जा सकता था। भौतिक विशेषताओं की एकरूपताओं के कारण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और घघ्घर क्षेत्र में जीवन-निर्वाह के एक जैसे तरीके सामने आये। किन्तु अन्य ऐसे स्थान भी थे, जहां जीविका के स्वरूप में वहां की परवर्ती भौगोलिक विशेषताओं के कारण विविधता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की नगर-योजना अत्यंत कुशल थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकान और वहां की अनोखी भौतिक उपलब्धियों का पता चलता है। हड़प्पा युग के मिट्टी के बर्तनों, औजारों और उपकरणों में काफी हद तक एकरूपता पायी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें और मनके कारीगरी के सुंदर नमूने हैं, लेकिन उनकी प्रस्तर मूर्तिकला और पकी मिट्टी की लघु मूर्तियां तकनीकी उत्कृष्टता में समकालीन मिड्ड और मेसोपोटामिया की कला का मुकाबला नहीं कर सकतीं। हड़प्पा सभ्यता की निर्वाह व्यवस्था अनेक फसलों की खेती और पालतू जानवरों पर निर्भर थी। इससे वहां की अर्थव्यवस्था नगरों में बसे लोगों का भरण-पोषण करने में समर्थ हो सकी। नगरों में रहने वाले लोग अपने खाद्या का उत्पादन स्वयं नहीं करते थे। उनके लिए खाद्या निकटवर्ती क्षेत्रों से आता था। हड़प्पा सभ्यता में बड़े-बड़े नगरों की मौजूदगी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ यह भी है कि उस समय कुशल कारीगर थे, दूर-दूर तक व्यापार होता था, समाज में धनी और निर्धन दोनों तरह के लोग रहते थे तथा वे शासक भी हुआ करते थे। हड़प्पाई लोग एक ही लिखित लिपि का प्रयोग कर रहे थे। हड़प्पा के सभी समुदाय एक ही तरह के बाट और तराजू का इस्तेमाल करते थे। वे तांबा और कांसे से निर्मित जिन औजारों का प्रयोग करते थे, वे बनावट, शक्ल और आकार में एक जैसे होते थे। उनके द्वारा प्रयोग में लायी गयी ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। उनके कुछ नगरों में बनी इमारतों, किलों आदि की बनावट में भी एकरूपतायें थीं। उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जहां हड़प्पा सभ्यता के नगर मौजूद थे, वहीं मोहरों, शंखों से बनी चूडि़यों, लाल पत्थर के बने मनकों और सेलखड़ी से बने गोल चपटे मानकों की बनावट एक-सी होती थी।
हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को अधिकतर गुलाबी रंग के मिट्टी के बर्तनों से पहचाना जाता है। इन मिट्टी के बर्तनों का ऊपरी भाग लाल रंग का होता था। मिट्टी के इन बर्तनों पर काले रंग से पेड़ों, पशु-पक्षियों के एक ही प्रकार के चित्र बने होते थे और ज्यामिति की आकृतियों को चित्रित किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की भौतिक विशेषताओं में पायी जाने वाली ये एकरूपतायें ही हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषतायें थीं।
सिंधु सभ्यता से संबद्ध सैकड़ों स्थलों में कुछ नगर, बड़े ग्राम एवं कस्बे थे। कस्बों की संख्या निश्चित रूप से नगरों से अधिक थी। कुछ नगर बंदरगाह के रूप में भी विकसित हुए। इस सभ्यता के समस्त क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए संभवतः एक से अधिक राजधानियां रही होंगी। कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी निम्न रूप से दी जा सकती हैः
हड़प्पाः रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा से नगर निर्माण योजना, अÂागार, भवन निर्माण योजना, मुहरों से लिपि, बर्तनों आदि की जानकारी मिलती है।
मोहनजोदड़ोः सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहां का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानागार है। यहां से अन्नागार और अन्य भवनों के अवशेष भी पाये गये हैं।
चन्हूदड़ोः मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित चन्हूदड़ो से पकायी गयी ईंटों के भवन एवं मनके बनाने का कारखाना प्रकाश में आया है। यहां से झूकर और झांगर संस्कृति के पुरावशेष भी मिले हैं।
लोथलः गुजरात में खंभात की खाड़ी के समीप स्थित लोथल से अनेक भवनों, दुकानों एवं गोदीबाड़े का प्रमाण मिला है।
कालीबंगाः राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से अग्निकुंड, जुते खेत एवं लकड़ी की नालियों सहित नगर नियोजन एवं मुहरों के प्रमाण मिले हैं।
बनावलीः हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित बनावली से किलेबंदी तथा हड़प्पा संस्कृति के नागरिक स्वरूप का प्रमाण मिलता है। यहां से मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र उपकरण, बाणाग्र, मनके, मृण्मूर्तियां, बाट-बटखरे और लिपियुक्त मुहरें मिली हैं।
सुत्कांगेनडोरः मकरान तट पर स्थित सुत्कांगेनडोर से एक बंदरगाह, दुर्ग और नगर योजना के प्रमाण मिले हैं।
कोटदीजीः सिंध राज्य में खैरपुर के निकट स्थित कोटदीजी से अच्छे बर्तनों, बाणाग्रों एवं प्राव्फ़ हड़प्पाई अवशेषों के प्रमाण मिलते हैं।
राखीगढ़ीः हरियाणा में जिंद के निकट स्थित राखीगढ़ी से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन पुरावशेष सहित एक लिपिबद्ध मुहर मिली है।
आलमगीरपुरः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर से चावल एवं हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
सुरकोतडाः गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोतडा से गढ़ी और आवासीय मकान, मिट्टी के बर्तन, अस्थि कलश और घोड़े के प्रमाण मिले हैं।
धौलावीराः गुजरात में स्थित धौलावीरा से मध्यमा नगर के प्रमाण मिले हैं, जो नयी प्रकार की विशेषता मानी जाती है।
दैमाबादः महाराष्ट्र में स्थित दैमारबाद को हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल माना जाता है, जहां से तांबे की वस्तुयें मिली हैं।
इसके अलावा सुत्काकोह, डाबरकोट, रोपड़, बाड़ा, संघोल, मिताथल, बड़गांव, अम्बखेड़ी, रंगपुर, रोजदी, मालवण, प्रभाष जैसे
स्थल भी यहां के महत्वपूर्ण स्थल है, जहां से हड़प्पाई पुरावशेष कीप्राप्ति हुई हैं।
हड़प्पा सभ्यता अपने विकसित स्वरूप में करीब 600 वर्षों (2300-1750 ई. पूर्व) तक चलती रही। 1700 ई. पूर्व के आस-पास इस सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखायी देने लगे। इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय तक नष्ट हो चुके थे। पुरातात्विक प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि उन्न्त हड़प्पा सभ्यता अब पतन के मार्ग पर बढ़ चली थी। इसका नागरिक स्वरूप नष्ट हो चुका था। यह सभ्यता पतनोन्मुखी स्वरूप में कुछ और दिनों तक बनी रही, परंतु इसकी विशिष्टता तथा इसकी प्राचीन गरिमा नष्ट हो चुकी थी। इस सभ्यता के पतन के लिए अनेक कारण सुझाये गये हैं। यहां हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें मात्र किसी एक कारण के परिणामस्वरूप इतनी विकसित सभ्यता का अंत अथवा पतन नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई एक कारण समान रूप से समस्त सभ्यता के अंत के लिए उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि विभिन्न हड़प्पा नगरों के पतन में भिन्न- भिन्न कारणों का योगदान रहा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए मुख्यतः निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं:
विदेशी आक्रमणः गॉर्डन चाइल्ड, मार्शल, ह्नीलर, पिग्गट जैसे अनेक पाश्चात्य विद्वानों की धारणा थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विनाश आर्य आक्रमणकारियों द्वारा किया गया। इस तर्क का आधार साहित्यिक एवं पुरातात्विक प्रमाण हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर (किले को तोड़ने वाला) कहा गया है तथा हरियूपिया को हड़प्पा मानकर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाहरी आक्रमण के कारण हुआ।
प्राकृतिक कारणः हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अनेक
विद्वानों ने प्राकृतिक कारणों को उत्तरदायी माना है। उनका मानना है कि प्राकृतिक प्रकोप जैसे बड़े पैमाने पर आग का लगना, भयंकर महामारी, बाढ़ के प्रकोप, नदियों की जलधारा में परिवर्तन, विवर्तनिक हलचलों, आर्द्रता का हास और भूमि की शुष्कता का विस्तार, जंगलों का नष्ट होना आदि ऐसे कारण थे, जिनका सैंधव सभ्यता के अस्तित्व पर गहरा प्रतिकूलप्रभाव पड़ा। फलतः हड़प्पा सभ्यता अपना मूल स्वरूप और आर्थिक आधार खो बैठी। इस परिस्थिति में इस नगरीय सभ्यता का बने रहना असंभव था।
मानवीय कारणः समय के साथ-साथ नगरों में बसने वाले लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। नगरों की आबादी पूर्ण विकसित काल में पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गयी। इससे प्राकृतिक और आर्थिक साधनों पर दबाव बढ़ने लगा। एक ओर तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, दूसरी ओर प्राकृतिक साधनों की कमी हो रही थी। परिणामस्वरूप आर्थिक स्थिति कमजोर होती गयी और नगरों का पतन सुनिश्चित हो गया।
प्रशासनिक शिथिलताः विभिन्न स्थलों की खुदाइयों से अंतिम प्रकाल के स्तरों में ”ास के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। इससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक संयंत्र ढीला और कमजोर पड़ गया था, जो नगर निर्माण एवं नागरीय जीवन की विशिष्टताओं को बनाये रख सके। फलतः उन स्थलों में शहरीपन का स्थान क्रमशः देहातीपन ने ले लिया।
आर्थिक कारणः विभिन्न कारणों से वहां के कृषि उत्पादन में कमी आयी तथा उद्योग-धंधों एवं विदेशी व्यापार में गिरावट आयी। सैंधव सभ्यता का मुख्य आधार व्यापार ही था, जिसमें कमी आने पर हड़प्पा की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी।
रूढि़वादिताः सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अनेक विद्वानों ने रूढि़वादिता विशेषतया आर्थिक स्थिरता को उत्तरदायी माना है। इस स्थिरता का सबसे बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार पर पड़ा।
इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के विनाश में विभिन्न कारणों का योगदान रहा है। कोई भी एक कारण इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं था। इसी प्रकार क्षेत्र विशेष की अलग-अलग परिस्थितियां और क्षेत्र विशेष में नगरों का पतन विशेष कारणों से हुआ। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के पतन को क्रमिक पतन की अवधारणा के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।
Question : दिये मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों पर निशान लगाइए और मानचित्र में अंकित स्थानों पर संक्षिप्त विवरणात्मक टिप्पणियां लिखिये:
1. ऐहोल, 2. अमरावती, 3. बेसनगर,4. भगवानपुर, 5. भरुकच्छ, 6. धौलावीरा, 7. दैमाबाद, 8. गिरिनगर, 9. इनामगांव, 10. कलिंगनगर, 11. कन्हेरी, 12. कार्ले, 13. कौशाम्बी, 14. कयथा, 15.किली-गुल-मुहम्मद, 16. कोटदिजी, 17. कुशीनगर, 18. मामल्लपुरम्, 19. मास्की, 20. मेहरगढ़, 21. प्रयाग, 22. पुष्कलावती, 23. सारनाथ, 24. सुर्पारक, 25. श्रुघ्न, 26. टेक्कलकोट्टा, 27. टोपरा, 28. उज्जयिनी, 29. उरैयर, 30. वल्लभी।
(1998)
Answer : 1. अयहोल/ऐहोलः अयहोल कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। अयहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला की पाठशाला कहा गया है। यहां से 70 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। चालुक्यों ने 610 ई. के आस-पास यहां अनेक मंदिर बनवाये, जिनमें प्रमुख थेः लाड खान मंदिर, दुर्गा मंदिर और हुचीमललीगुड़ी मंदिर। यहां से मेगुती के अधूरे जैन मंदिर का अवशेष भी मिला है। यहां के मंदिर द्रविड़, नागर एवं बेसर वास्तुकला की शैली में बने हुए हैं। दुर्गा मंदिर बौद्ध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यहां रविकीर्ति का पुलकेशिन प्प् के लिए 643 ई. में लिखा प्रशस्ति-लेख मिला है, जिसमें पुलकेशिन प्प् द्वारा हर्षवर्द्धन को हराये जाने का वर्णन है।
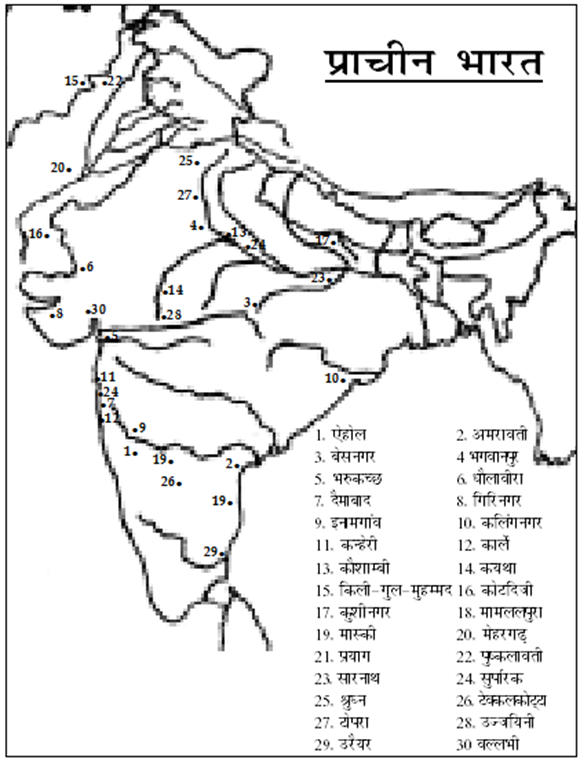
2. अमरावतीः अमरावती अथवा धान्यघट अथवा धान्यकटक अथवा धरणिकटक आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में कृष्णा-गोदावरी थाले में स्थित है। मृद्भाण्डीय संस्कृति से इक्ष्वाकुओं तक इसका महत्व बना हुआ था। अमरावती से आहत सिक्के मिले हैं। सातवाहनों के समय यह दक्षिण भारत में बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। अमरावती का स्तूप बहुत प्रसिद्ध है जो भित्ति-प्रतिमाओं से युक्त है, जिनमें से कुछ में जीवन के विभिन्न दृश्य उकेरे गये हैं। अमरावती में वास्तु एवं मूर्ति की एक स्वदेशी कला विकसित हुई थी। इक्ष्वाकुओं के समय भी अमरावती दक्षिण में बौद्ध संस्कृति का केन्द्र बना रहा। ह्वेनसांग के आगमन के समय अमरावती भग्नावस्था में था। प्राचीन काल में यह व्यापार का एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध केन्द्र था। यहां अपना माल बेचने और यहां से माल ले जाने के लिए बर्मा एवं इंडोनेशिया के जहाज आते थे।
3. बेसनगर: बेसनगर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। यहां से प्राप्त अवशेष यहां की मृदभाण्ड संस्कृति एवं मौर्योत्तर राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विवरण देते हैं। अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि यहां व्यापारिक सक्रियता थी। यहां का नागरिक प्रशासन भी निगमों द्वारा चलाया जाता था। यहां के एक हस्तदंत शिल्पी-संघ ने सांची-स्तूप का परिवर्द्धन कराया था। बेसनगर के ऐतिहासिक महत्व का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, यहां से प्राप्त हेलियोडोरस का गरूड़-स्तंभ। इस स्तंभाभिलेख से ई.पू. 100 में विदिशा क्षेत्र में शुंग-शासन तथा यूनानियों के भारत में आगमन का पता चलता है। इसी से दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है कि ई.पू. प्रथम शताब्दी में मालवा-क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रसार था। यहां तक कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने वैष्णव-भागवत मत स्वीकार कर लिया था। इस स्तंभ लेख में उसने स्वयं को वासुदेव का अनुयायी बताया है।
4. भगवानपुरः भगवानपुर, वर्तमान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यहां से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष उत्तर-हड़प्पा युग से संबंधित हैं। भगवानपुर से चित्रित धूसर मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहां तेरह कमरों वाला एक मिट्टी का घर मिला है, जिसमें पशुओं की हड्डियां भारी तादात में मिली हैं। इसे किसी बहुत बड़े परिवार अथवा कबीला-सरदार का आवास-गृह समझा जा रहा है। यहां से उत्तर-हड़प्पा युग की पकी ईंटें भी मिली हैं।
5. भरुकच्छः वर्तमान गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित भरुकच्छ अथवा भड़ौच एक बन्दरगाह नगर था। अब यह अरब सागर एवं भूमध्य सागर के माध्यम से पश्चिमी देशों से जुड़ा हुआ था। टॉलेमी ने भरुकच्छ को बेरीगाजा कहा है। भरुकच्छ में 300 ई.पू. से आबादी की शुरुआत के लक्षण मिले हैं, जिस समय मनका उद्योग प्रमुख उद्योग था। मौर्योत्तर युग में रेशम मार्ग का केंद्र होने के कारण भरुकच्छ अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था। यहां से सातवाहनों के सीसे के सिक्के तथा शक-क्षत्रपों के भी सिक्के मिले हैं। रोमन व्यापार का भरुकच्छ बहुत बड़ा केन्द्र था। ह्वेनसांग भरुकच्छ आया था और उसने यहां महायान स्थविर सम्प्रदाय के प्रभाव उल्लेख किया है।
6. धौलावीरा: यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हड़प्पा के सभ्यता के अब तक खोजे गये सभी स्थलों में धौलावीरा एक प्रमुख स्थल है। इसका उत्खनन आर-एस-बिष्ट द्वारा 1991 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के सिन्धु क्षेत्र के स्थलों में पायी जाने वाली सारी विशेषताएं यहां से प्राप्त अवशेषों से मिलती हैं। साथ ही, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का सबसे बड़ा अंश भी यहीं से प्राप्त हुआ है। इस स्थल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां अन्य हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में मिलने वाले दुर्ग नगर एवं बाह्य निम्न बस्ती के अलावा एक और नगर के अवशेष, दुर्ग और बस्ती के बीच में मिलेहैं।
7. दैमाबादः दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास अहमदनगर के समीप स्थित है। यह ताम्र-पाषाणयुगीन संस्कृति से संबद्ध है। दैमाबाद जोखे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व का सबसे बड़ा कारण है, यहां से बड़े पैमाने पर कांसे की वस्तुओं का मिलना। यहां से खिलौना-रथ तथा दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। यहां से हाथी, गैंडे, बैल एवं रथ की जो कांस्य मूर्तियां मिली हैं, उनका वजन 60-60 किलोग्राम तक है।
8. गिरिनगरः गिरिनगर गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में जूनागढ़ के निकट पर्वतीय क्षेत्र है, गिरिनगर या गिरनार। यहां से प्राप्त अवशेष, पश्चिम भारत में मौर्य शासन के विस्तार की पुष्टि करते हैं। गिरनार पर्वत या गिरिनगर से अशोक का चौदहवां शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय उसके गवर्नर पुष्यगुप्त ने इस क्षेत्र में सुदर्शन झील बनवायी थी। इस झील की मरम्मत अशोक के गवर्नर तुषाष्प ने करायी थी। गिरनार पर्वत से ही रूद्रदामन (शक शासक) प्रथम का 150 ई. का अभिलेख मिला है, जो संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। उसने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था।
9. इनामगांवः इनामगांव वर्तमान पश्चिम महाराष्ट्र में परभणी जिले तथा पुणे के मध्यवर्ती क्षेत्र के समीप स्थित है। यह ताम्र-पाषाण संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती है। यहां से नगरीकरण के अवशेष मिले भी हैं। यहां से दुर्गीकृत आवासीय क्षेत्र के भग्नावशेष मिले हैं। यहां से मातृदेवी की एक ऐसी प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में प्राप्त एक स्त्री मूर्ति के सदृश है। इनामगांव से विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। यहां से समुद्री मछली की हड्डी भी प्राप्त हुई है।
10. कलिंगनगरः आधुनिक उड़ीसा राज्य में स्थित यह नगर कलिंग राज्य में स्थित था और 200 ई.पू. से 300 ई. के बीच दक्षिणी बन्दरगाहों (दक्षिणापत्तन) को जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित था। यह शहर नगरीकरण और सम्पन्नता की अद्भुत झांकी प्रदर्शित करता था। यहां रहने वाले वाणिज्यिक वर्ग के लोगों का प्रमुख व्यवसाय आंतरिक और विदेशी व्यापार था। अपने राज्यकाल के आठवें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके इसे अपने राज्य में मिला लिया था।
11. कन्हेरीः कन्हेरी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह सातवाहन काल की गुफा वास्तुकला के कारण प्रसिद्ध है। यहां से यज्ञश्री शातकर्णी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें शकों एवं सातवाहनों के बीच के वैवाहिक संबंध का उल्लेख है। राष्ट्रकूटों के शासन काल के दौरान यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल था।
12. कार्ले: कार्ले अथवा कार्ली, पश्चिमी दक्कन में महाराष्ट्र में पुणे से 50 कि.मी. दूर उत्तर-पश्चिम में अवस्थित है। सातवाहन युग में पश्चिमी दक्कन में ठोस चट्टानों को काटकर बौद्ध चैत्य एवं विहारों के निर्माण की शिला-वास्तुकला विकसित हुई थी, कार्ले की चर्चा उसी संदर्भ में होती है। कार्ले का चैत्य उस शिला-वास्तुकला के विकास का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी शुरुआत दूसरी-पहली शताब्दी ई.पू. से भी मानी जाती है। यह लगभग 40 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है। कार्ले का चैत्य कई स्तंभों से युक्त एक विशाल कक्ष है। इसमें बाहर से सूर्य की रोशनी के आने की समुचित व्यवस्था है।
13. कौशाम्बी: कौशाम्बी की पहचान वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से दक्षिण-पश्चिम में यमुना नदी के किनारे स्थित कोसम नामक गांव से की गयी है। कौशाम्बी के अस्तित्व की वैदिक, जैन एवं बौद्ध साहित्य तथा पुरातात्विक अवशेषों से पुष्टि होती है। साथ ही फाह्यान तथा ह्वेनसांग के विवरण भी इसकी चर्चा करते हैं। कौशाम्बी को आद्य नगरीय-स्थल भी कहा जा सकता है। महाजनपद युग में कौशाम्बी, वत्स राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद कौशाम्बी आर्थिक तथा धार्मिक महत्व का केन्द्र बन गया। यहां उत्तरापथ और दक्षिणापथ का पड़ाव था। मोर्योत्तर युग तक यह महत्वपूर्ण नगर था। यहां से विम कडफिसस तथा कनिष्क के सिक्के मिले हैं। मगधों ने कौशाम्बी को राजधानी बनाकर, इस क्षेत्र में दूसरी और तीसरी शताब्दियों में शासन किया था। गुप्तों की राज्य-सीमा में कौशाम्बी था, किन्तु इसे हूण तोरमण के आक्रमण से बहुत क्षति पहुंची थी। 400-600 ई. के मध्य इसका तेजी से पतन हुआ। बुद्ध के महत्वपूर्ण कार्य-स्थलों में से यह एक था। यह थेरपंथ का केन्द्र था। घोषिता रामविहार, अशोक का प्रयाग स्तंभ इत्यादि इसके सांस्कृतिक महत्व की पुष्टि करते हैं।
14. कयथाः यह मध्य प्रदेश में उज्जैन से लगभग 24 कि.मी. पूर्व में स्थित है। यह स्थल ताम्र-पाषाण संस्कृति (2000-1800 ई.पू.) से संबद्ध है। कयथा संस्कृति हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन संस्कृति थी। वैसे यहां कुछ प्राक्-हड़प्पीय लक्षण भी दिखाई देते हैं। कयथा से ताम्र-पाषाणयुग की तांबे की चूडि़यां तथा दो कुल्हाडि़यां मिली हैं। इस युग का जल-निकास की व्यवस्था से युक्त स्नानगृह भी दिखता है। कयथा से नक्काशी की हुई हाथी दांत की बोतल भी मिली है। यहां से भुंग, कुषाण और गुप्त युग के भी अवशेष मिले हैं।
15. किली-गुल-मुहम्मदः यह एक नवपाषाण युगीन संस्कृति का एक स्थल था, जो बलूचिस्तान में स्थित है। इसका समय काल 5500 ई.पू. से 3500 ई.पू. के बीच का है। यहां सभ्यता की शुरुआत भेड़, बकरी एवं गायों के पालन से हुई थी। साथ ही, थोड़ी-बहुत खेती भी की जाती थी। मिट्टी के बने घरों, बर्तनों एवं शिल्पों के अवशेष यहां प्रमाणस्वरूप प्राप्त हुए हैं।
16. कोटदिजी: इस ऐतिहासिक स्थल का महत्व सैन्धव सभ्यता से संबद्ध है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर के पास अवस्थित है। यहां से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर प्राक्-हड़प्पीय ताम्र-पाषाण संस्कृति, स्थानीय कृषक समुदायों के प्रसार एवं हड़प्पा की नगर- सभ्यता से उनके संबंधों की जानकारी मिलती है। सैन्धव सभ्यता के अन्य स्थलों के प्रतिकूल कोटदिजी में किलेबंदी का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
17. कुशीनगरः कुशीनगर अथवा कुशीनारा की पहचान उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 35 मील पूरब पड़रौना जिले में स्थित कसिया नामक स्थल से की गयी है। दिव्यावदान, दीघ्घनिकाय, अशोक के आठवें बृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाह्यान एवं ह्वेनसांग के विवरणों से इस ऐतिहासिक स्थल के विषय में जानकारी मिलती है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानियों में से एक थी। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं हुआ था, जिसके कारण गुप्तकाल तक इसका धार्मिक महत्व बना रहा। इसी प्रकार, श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग पर स्थित होने के कारण कुशीनगर में आर्थिक गतिविधियां भी रहीं। प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल होने के कारण कुशीनगर में मौर्यकाल में बौद्ध इमारतें बनीं, जिनका निर्माण एवं पुनर्निर्माण गुप्तयुग तक चलता रहा। मौर्य शासक अशोक ने यहां स्तूपों एवं विहारों का निर्माण कराया था। कुमार गुप्त के समय हरिबल ने भी यहां स्तूप एवं विहार बनवाये थे। यहां के व्यापारियों एवं शिल्पियों द्वारा मुद्रा परिचालन के साक्ष्य मिले हैं। हूणों का आक्रमण कुशीनगर पर भी हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय यह अत्यंत पतनशील अवस्था में था। गुप्तोत्तर युग में कुशीनगर के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है।
18. मामल्लपुरमः मामल्लपुरम मद्रास के दक्षिणी समुद्री तट पर अवस्थित है। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन-प्रथम द्वारा करवाया गया था। यहां से एकाश्म पत्थरों को काटकर बनाये गये मंदिरों और रथों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हीं से दक्षिण में मंदिर वास्तुकला का आरंभ का संकेत प्राप्त होता है। लहर मंदिर और ईश्वर एवं मुकुन्द मंदिरों, जिनका निर्माण 8वीं शताब्दी ई. में राजसिह द्वारा करवाया गया था, के अलावा अन्य मंदिर भी यहां अवस्थित हैं, जो द्रविड़ वास्तुकला के अद्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।
19. मास्कीः यह आंध्र प्रदेश राज्य में रायचूर जिले में तुंगभद्रा की सहायक नदी मास्की के समीप स्थित एक छोटा गांव है। यहां से ताम्र-पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मास्की के अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता इसी लेख से यह पता चलना है कि अन्य अभिलेखों में उत्कीर्ण ‘देवानाम् प्रिय प्रियदर्शी’ मौर्य शासक अशोक ही है। इसी अभिलेख में देवानाम् प्रिय प्रियदस्सिन् राजा तथा असोकस-दोनों ही पद अंकित हैं।
20. मेहरगढ़ः मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में कच्छी मैदान में स्थित है। यहां पूर्व ताम्र-पाषाण संस्कृति एवं प्राक्-हड़प्पा सभ्यता के प्रथम स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। इसकी अवधि 7000 ई.पू. मानी गयी है। मेहरगढ़ में नगरीकरण के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। गेहूं, जौ तथा कपास की कई किस्में यहां से मिली हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि सिन्धु सभ्यता के लोगों ने जौ, गेहूं और कपास उपजाने की तकनीक मेहरगढ़ के लोगों से ही सीखी थी। यहां से कच्ची ईंटों से बने आयताकार मकानों एवं मृदभाण्डों के अवशेष भी मिले हैं।
21. प्रयागः उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के संगम पर बसा हुआ इलाहाबाद ही प्रयाग है। मौर्योत्तर युग के बाद के कालखण्ड में जब व्यापारिक ठहराव की स्थिति आई, तब दोआब की उपजाऊ भूमि में प्रयाग का महत्व बढ़ा। स्पष्टतः गुप्त युग से प्रयाग का धार्मिक- राजनैतिक महत्व सामने आने लगा। प्रयाग, गुप्तों के शासन क्षेत्र में आता था। यहां से अशोक-स्तंभ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सैनिक एवं कलात्मक गतिविधियों के विषय में पता चलता है। एस- आर- गोयल के अनुसार, पाटलिपुत्र के पहले ‘प्रयाग’ गुप्तों की राजधानी थी। उसके बाद हर्षवर्द्धन, गुर्जर-प्रतिहार, चंदेल और गहड़वाल वंशों का प्रभाव प्रयाग पर रहा। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर उसे इलाहाबाद नाम दिया था। प्रयाग का धार्मिक महत्व था और इसे तीर्थराज कहा जाता है। हर्षवर्द्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। कालिदास, कल्हण और अलबरूनी ने भी प्रयाग के धार्मिक महत्व का उल्लेख किया है।
22. पुष्कलावतीः वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर जिले के चारमुड्डा नामक स्थान को प्राचीन पुष्कलावती अथवा पुष्कल के रूप में पहचाना गया है। यह स्वात एवं काबुल नदियों के संगम पर बसा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि, कालिदास, टोलेमी, एरियन तथा ह्वेनसांग ने इस नगर की चर्चा की है। रामायण और रघुवंश के अनुसार, भरत के पुत्र पुष्कर ने पुष्कलावती नगरी का निर्माण कराया था। टॉलेमी और एरियन ने क्रमशः इसे पोक्लाइस एवं प्यूकेलाओटीज कहा है। पुष्कलावती सिकन्दरिया-काबुल मार्ग से संबद्ध नगर था। सिकन्दर के आक्रमण के समय हस्ति नामक भारतीय राजा पुष्कलावती पर शासन कर रहा था। अशोक ने यहां दो स्तूप बनवाये थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक-माउस यहां शासन कर रहा था। पुष्कलावती से गांधार शैली की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।
23. सारनाथः उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर से लगभग सात मील दूर स्थित सारनाथ ही प्राचीन इसिपतन मृगदाय अथवा ऋषिपतन मृगदाव है। यह बौद्ध सम्प्रदाय एवं मौर्यकला से संबद्ध स्थल है। भगवान बुद्ध का धर्मचक्रप्रवर्तन सारनाथ में ही हुआ था। मौर्य शासक अशोक ने सारनाथ में एक सिंह शीर्ष प्रस्तर-स्तंभ बनवाया था। स्वतंत्र भारत के राजचिह्न के रूप में इसी सिंह शीर्ष को अपनाया गया है। यह मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ के स्तंभ पर अशोक का लघु लेख भी उत्त्कीर्ण है। फाह्यान ने सारनाथ की यात्र की थी। ह्नेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का केंद्र था। मध्य युग में गहड़वाल शासक की रानी कुमारदेवी ने यहां विहार और संघाराम बनवाये थे। हाल में हुई खुदाई में सारनाथ से गुप्तकालीन धमेख स्तूप के अवशेष मिले हैं।
24. सुर्पारकः सुर्पारक अथवा शुर्पारक अथवा सोपारा महाराष्ट्र में थाने जिले में स्थित है। प्राचीन भारत में यह भृगुकच्छ क्षेत्र का प्रसिद्ध बंदरगाह था। अरब सागर का तटवर्ती बन्दरगाह होने के कारण पश्चिम की ओर के मार्ग का प्रमुख केन्द्र सुर्पारक ही था। हिब्रू साहित्य में वर्णित ओफीर पद से इसकी तुलना की गयी है। जातक साहित्य तथा महाभारत में भी सुर्पारक का वर्णन मिलता है। यहां से अशोक का आठवां अभिलेख मिला है। इससे अरब सागरीय क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर मौर्य प्रभुत्व का संकेत मिलता है। शक-सातवाहन युग में भी इसका व्यापारिक महत्व बना हुआ था। इसका उल्लेख टॉलेमी और पेरिप्लस दोनों ने ही किया है।
25. श्रुघ्नः भारत के उत्तरी हिस्से में अवस्थित यह क्षेत्र 200 ई.पू. से 300 ई. के बीच आंतरिक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। हस्तिनापुर एवं इन्द्रप्रस्थ से निकटता होने के कारण यह नगर काफी समृद्ध एवं सम्पन्न अवस्था में था।
26. टेक्कलकोट्टाः यह दक्षिण भारत में दक्कन के पठार के पहाड़ी एवं सूखे क्षेत्र पर अवस्थित एक नवपाषाण युगीन संस्कृति का स्थल था। यहां आवासों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त हस्तनिर्मित पात्र, लाल-कत्थई रंग के हैं, जिनका बाह्य हिस्सा चिकना है। पत्थर एवं स्लेटों के औजार यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां के लोगों को खेती का मात्र प्रारंभिक ज्ञान ही प्राप्त था। कार्बन-14 विधि से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार इस क्षेत्र के नवपाषाणकालीन संस्कृति का समय 2600 से 1000 ई.पू. के बीच निर्धारित किया गया है।
27. टोपरा: यह स्थल हरियाणा के अम्बाला जिले में अवस्थित है। फिरोजशाह तुगलक द्वारा अशोक का स्तंभ लेख, जो दिल्ली ले जाया गया था, वास्तव में टोपरा में ही था। इस स्तंभ लेख में सातों प्रमुख स्तंभलेख उत्कीर्ण हैं, जिन्हें प्रमुख शिलालेखों का परिशिष्ट माना जाता है।
28. उज्जयिनीः उज्जयिनी अथवा उज्जैन अथवा अवंतिका, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित मध्य प्रदेश का एक जिला नगर है। ‘पेरिप्लस’ में इसे ‘ओजीनी’ कहा गया है। इसके विषय में 708 ई.पू. से 11वीं शताब्दी ई. तक के विवरण मिलते हैं। बाद में यह क्षेत्र मालवा के रूप में जाना गया। उज्जैन महाजनपदयुग में अवन्ति की उत्तरी राजधानी थी। इसकी शक्ति का कारण इसकी लौह प्रचुरता थी। अजातशत्रु के बाद शिशुनाग ने अवन्ति को मगध जनपद में मिला लिया था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय अवन्ति प्रांत की राजधानी उज्जैन बनी रही। अशोक ने यहां स्थानांतरण की चक्रवत् प्रणाली अपनायी थी। अरब सागरीय तट के नजदीक होने के कारण उज्जैन, मौर्योत्तर युग में भी प्रभावी बना रहा। यह शुंगों की भी राजधानी थी। उज्जैन रेशम-मार्ग से संबद्ध था। यहां शक क्षत्रपों ने भी शासन किया था, जिन्हें चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने पराजित कर उज्जयिनी पर गुप्त प्रभुत्व स्थापित किया था। उज्जयिनी चन्द्रगुप्त-द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। ह्नेनसांग, बाणभट्ट, और अलबरुनी ने उज्जयिनी का उल्लेख किया है। कालिदास ने उज्जयिनी की विशेष चर्चा की है। उज्जयिनी का महाकालेश्वर शैव मंदिर कालिदास के समय से ही प्रख्यात है। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में यहां जंतर-मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था।
29. उरैयूरः वर्तमान समय में उरैयूर, कोरोमण्डल तट पर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी थाले पर स्थित है। इसका आर्थिक-राजनैतिक महत्व मौर्योत्तर युग से संबद्ध है। उरैयूर प्राचीन चोलों की बन्दरगाह-राजधानी थी। यहां से रोमन व्यापारिक संपर्क के भी प्रमाण मिले हैं। उरैयूर से ईंटों का बना हआ एक रंगाई हौज मिला है, जिसकी अवधि 100-300 ई. मानी गयी है। उरैयूर मौर्योत्तर-युग में दक्षिण भारत का एक प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्र था। यहां से बड़े पैमाने पर करघे पर कपड़े की बुनाई के साक्ष्य मिले हैं।
30. वल्लभीः गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में भावनगर जिले में बालाघाट गांव को वल्लभी के रूप मेंं पहचाना गया है। ह्वेनसांग ने वल्लभी को ‘फा-ल-पी’ कहा है। पांचवीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी मैत्रक वंश की राजधानी थी। इसकी स्थापना भट्टार्क मैत्रक ने की थी। वल्लभी में ही द्वितीय जैन महासभा हुई थी, जहां 600 ई. में प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन सुधर्मन की अध्यक्षता में हुआ था। वल्लभी के मैत्रकों के साथ सातवीं शती ई. के पूर्वार्द्ध में हर्षवर्द्धन के वैवाहिक संबंध स्थापित थे। वल्लभी में एक महान आवास-सह-शिक्षण संस्थान था। यहां प्रख्यात आवासीय बौद्ध विश्वविद्यालय भी था, जिसका अपभ्रंश-साहित्य में अनुपम योगदान था। इत्सिंग ने इस संस्थान की चर्चा की है।
Question : प्रशासन और कला के क्षेत्र में पल्लवों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिये।
(1997)
Answer : पल्लव शासन व्यवस्था का भारतीय इतिहास में विशिष्ट महत्व है। उसके इस महत्व का कारण उसकी समन्वयवादी प्रकृति है। पल्लव शासन व्यवस्था में एक ओर तो दक्षिण भारतीय शासन पद्धति का मूल तत्त्व स्थानीय स्वायत्तता सुरक्षित थी, तो दूसरी ओर उसमें उत्तरी भारत की मौर्य व गुप्त शासन व्यवस्था की केन्द्रीय प्रशासन व्यवस्था को भी स्थान दिया गया था। केन्द्रीयभूत प्रशासन का स्थानीय स्वायत्तता से मेल, यही समन्वय पल्लव शासन व्यवस्था को विशिष्ट रूप प्रदान करता है।
पल्लव शासन का चरित्र वंशानुगत राजतंत्र था। राजत्व को ईश्वरीय और वंशानुगत माना जाता था और वे अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते थे। राजत्व के ईश्वरीय सिद्धांत का अनुकरण करते हुए पल्लव सम्राट भी सर्वशक्तिमान होते थे। प्रशासन, वित्त, न्याय व सेना के क्षेत्र में अंतिम अधिकार उन्हीं के पास था। राजा का उत्तराधिकारी भी राजा के शासन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उसे ‘युवमहाराज’ कहा जाता था।
शासन कार्य में राजा की सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल भी होता था, जिसे ‘रहस्यादिकद’ कहा जाता था। मंत्रिमंडल की स्थिति मात्र सलाहकार की होती थी तथा जो भी प्रभाव वह रखते थे वह राजा और मंत्री के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता था। शासन को चलाने के लिए पल्लव राज्य में अधिकारी वर्ग भी होता था। न्याय के लिए पल्लव राज्य में न्यायालयों की स्थापना की गयी थी। उन न्यायालयों को ‘अधिकरण’ तथा ‘धर्मासन’ कहा जाता था। न्यायालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करता था। पल्लव साम्राज्य का विभाजन राष्ट्र, विषय, कोट्टम तथा ग्राम नामक इकाइयों में था। विषय का अधिकारी ‘विषयिक’ तथा कोट्टम का अधिकारी ‘देशाधिकृत’ कहलाता था। स्थानीय स्तर पर शासन की इकाइयों को व्यापक स्वायत्तता थी। इन स्थानीय इकाइयों के रूप में ‘सभा’ तथा ‘नाडु’ का उल्लेख मिलता है। इनमें शासन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता था। ग्राम भोजक नाम का अधिकारी केन्द्र व ग्राम के मध्य कड़ी के रूप में काम करता था। साथ ही वह ग्राम का नेता व मुखिया भी होता था। पल्लव राज्य में सैन्य संगठन का मुख्य अधिकारी ‘सेनापति’ था। उसके अधीन ‘नायक’ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। शक्तिशाली नौसेना का गठन पल्लव शासकों की एक मुख्य उपलब्धि थी।
पल्लव शासकों ने कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह योगदान उनके इतिहास के सांस्कृतिक महत्व का आधार बन जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में पल्लव शासकों ने सुदूर दक्षिण में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण कार्य आरंभ किया। पल्लवों के द्वारा बनवाए गये ये मंदिर कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजौर तथा पुड्डूकोराई में पाये जाते हैं। प्रारंभ के मंदिरों पर काष्ठकला तथा कंदरा कला का प्रभाव दिखाई देता है किंतु परवर्ती काल में ये मंदिर उन प्रभावों से मुक्त थे। निर्माण शैली की दृष्टि से पल्लवकालीन मंदिरों को कई शैलियों में बांटा गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः
1. महेन्द्र वर्मन शैली: महेन्द्रवर्मन के शासनकाल में जो मंदिर बनाए गये, उनमें स्तंभयुक्त बरामदा तथा अंदर की ओर एक या दो कमरे होते थे। ये सभी मंदिर शिला मंदिर के रूप में बने थे। इन्हें मंडप भी कहा गया है। इस शैली के प्रमुख मंदिरों में भैरवकोंड का मंदिर तथा नंदवल्लि का अनंतशयन मंदिर का स्थान है।
2. मामल्ल शैली: नरसिंहवर्मन के शासनकाल में निर्मित मंदिरों की शैली को ‘मामल्ल शैली’ कहा गया है। इस शैली में वराह मंडप, महिषमंडप, पंचपांडव मंडप सहित एकाश्म मंदिरों का भी निर्माण कराया गया था। एकाश्म मंदिरों को रथ मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, सहदेव रथ, पिंडार रथ, बलैयान कुट्टई रथ तथा गणेश रथ प्रमुख हैं।
3. राजसिंह शैली: आठवीं सदी में विकसित इस शैली में पत्थर एवं ईंटों के मंदिर निर्मित हुए। कांची का कैलाश मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर तथा महाबलीपुरम् के अन्य मंदिर इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कैलाश मंदिर में पल्लव राजा-रानियों की जीवितसम मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। महाबलीपुरम् में समुद्र तट पर दो गोपुरम् वाला लगभग 20 मीटर ऊंचा एक मंदिर भी निर्मित किया गया। छोटा होने पर भी यह बड़ा कलापूर्ण और सुंदर है।
4. अपराजित शैली: इसे नवीं सदी में अंतिम पल्लव नरेश अपराजित ने प्रारंभ किया था। इस शैली में पल्लव शैली, चोल शैली के समीप आ गयी है। यह शैली चोल शैली के अनुकरण पर निर्मित की गयी। इस शैली में अपराजितवर्मन ने पांडिचेरी के निकट बेलूर में मंदिरों का निर्माण कराया। इस शैली में मंदिरों के शिखर की गर्दन पहले की अपेक्षा अधिक स्थूल हो गयी तथा मंडपों के स्तंभों के शीर्ष के ऊपर का शीर्षफलक अधिक अलंकरणयुक्त और विशिष्ट हो गया। यह शैली काष्ठ कला से पूर्णतः मुक्त है।
मूर्तिकलाः पल्लव काल में मूर्तिकला का भी विकास हुआ, जो कि वास्तुकला का स्वाभाविक परिणाम था। पल्लव शैली की मूर्तिकला कहीं-कहीं गुप्त मूर्ति कला से साम्यता दर्शाती है तो कहीं-कहीं विभिन्नताएं भी प्रदर्शित करती है। पल्लव मूर्तिकला बौद्ध परंपरा की भी ऋणी थी। पल्लव मूर्तिकला में देवताओं और मनुष्यों की काया का अंकन अधिक गरिमामय है तथा पशुओं का अंकन करने में यह अन्य सभी शैलियों से श्रेष्ठ है। पल्लव शैली में ‘किरातार्जुनीयम’ मूर्तिफलक को 90’×50’ की शिला सतह पर उकेरा गया है। इसे बनाने के लिए शिलाखण्ड को पहाड़ से काटकर अलग नहीं किया गया। वह पूर्ववत् उसका अंग है। इस फलक में मूर्तिकार ने अपनी कल्पना की मौलिक उड़ान तथा सशक्त अभिव्यक्ति का परिचय दिया है। उस फलक में जीवधारियों का अंकन स्वाभाविक, यथार्थवादी तथा परंपरागत तीनों ही प्रकार से हुआ है।
Question : गुप्तकाल के दौरान दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार किस प्रकार हुआ?
(1997)
Answer : प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख विशेषता है कि इस काल में भारतीयों ने अपनी सर्जनात्मक शक्ति का उपयोग भारत के ही सांस्कृतिक विकास के लिए नहीं किया, अपितु विदेशों में जाकर वहां भी अपनी संस्कृति को स्थापित किया। दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय किसी एक स्थान से और एक साथ नहीं गये, अपितु वह वहां पर अलग-अलग समय में अलग-अलग क्षेत्रों से मानव लहर की तरह पहुंचे। परंतु गुप्तकाल में यह प्रक्रिया अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गयी थी। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में मुख्य भूमिका पुरोहित वर्ग, बौद्ध भिक्षु, व्यापारी वर्ग तथा योद्धाओं की रही। यह प्रसार युद्ध व बल प्रयोग द्वारा न होकर शांतिमय उपायों से भारतीयों व वहां के जन समुदाय के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के द्वारा हुआ।
दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में प्राचीन काल में चम्पा, कंबोज, फूनान, मलाया, जावा, सुमात्र, बोर्नियो, बाली, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, लाओस और इंडोचीन जैसे देश तथा अनेक छोटे-बड़े देश आते थे। गुप्तकाल में अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म को फैलाया। इन बौद्ध भिक्षुओं के अतिरिक्त अनेक हिन्दू संतों ने भी दक्षिण-पूर्व एशिया में हिन्दू धर्म का प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप यहां हिन्दू धर्म भी पल्लवित हुआ। जावा, कंबोडिया और फूनान में शैव और वैष्णव धर्मों ने अपनी जड़ें जमा लीं। इन बौद्ध और हिन्दू संतों के अतिरिक्त वे योद्धा भी दक्षिण-पूर्व एशिया पहुंचे, जिनका राज्य भारत में छिन गया था और वे कहीं भी अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे।
दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार में व्यापारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब चीन के साथ भारत का संपर्क बढ़ा, तो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बंदरगाहों की भी यात्रएं होने लगीं और इसी क्रम में भारतीय व्यापारी दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में रुचि लेने लगे। फाह्यान ने अपनी दक्षिण-पूर्व एशिया की सामुद्रिक यात्र के विवरण में अनेक कठिन और खतरनाक परिस्थितियों का वर्णन किया है। अन्य कई चीनी यात्रियों द्वारा दिये गये विवरणों में भी भारत एवं उन देशों के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। उनके अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया का भारतीयकरण यात्रियों एवं व्यापारियों के आवागमन के कारण, उन महत्वाकांक्षी भारतीयों के कारण जो वहां के राजाओं के सलाहकार बने या फिर स्वयं किसी राज्य के स्वामी बने, के कारण शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुआ। उन दिनों बर्मा को स्वर्णभूमि कहा जाता था। बर्मा में भारतीय संस्कृति का प्रसार बौद्ध धर्म के माध्यम से हुआ था। वहां से गुप्तकाल के बौद्ध अवशेष भारी मात्र में मिले हैं।
भड़ौंच, वाराणसी और चम्पा के व्यापारी बर्मा से व्यापार करते थे, उन दिनों स्वर्णद्वीप कहलाने वाले इंडोनेशिया (जावा, सुमात्र) में फाह्यान ने हिन्दू धर्म को फैला हुआ पाया। भारतीय संस्कृति के प्रभाव से ही सुमात्र का राज्य श्रीविजय साम्राज्य के रूप में उभर पाया और एक महत्वपूर्ण शक्ति और भारतीय संस्कृति का केंद्र बना रहा। जावा और सुमात्र की हिंदू बस्तियां भारतीय संस्कृति के प्रसार का द्वार बन गयीं तथा बस्तियों को स्थापित करने का सिलसिला आगे भी जारी रहा।
संप्रति उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के रूप में बंटे इंडोचीन में भारतीयों ने गुप्तकाल में कंबोज और चंपा नामक दो शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। कंबोज राज्य के शासक शैव वे। उन्होंने कंबोज को संस्कृत विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया और यहां असंख्य अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गये। कंबोज के निकट चम्पा में व्यापारियों ने अपने उपनिवेश बनाए। चम्पा का शासक भी शैव था। उसकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। यह देश वेदों एवं धर्मशास्त्रें की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था।
गुप्तकाल में थाईलैंड में भी भारतीय संस्कृति ने प्रवेश किया। यहां पर भी भारतीय राज्य की स्थापना हुई तथा यह देश भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र बन गया। इसका एक क्षेत्र गांधार तथा दूसरा विदेह कहलाता था। नगरों के नाम भारतीय थे। यहां बुद्ध व हिन्दू देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। बौद्ध धर्म का यहां अधिक प्रसार हुआ। गुप्तकाल में मलाया प्रायद्वीप में भी भारतीय बस्तियों की भी स्थापना हुई। यहां पर भारतीय संस्कृति के बौद्ध पक्ष का प्रभाव गहरा रहा। यहां पर भी नगरों व स्थानों के नाम में भारतीयता का पुट रहा। जावा के पूर्व में स्थित बाली द्वीप में भारतीय संस्कृति एक बड़ी सीमा तक आज भी उसी रूप में जीवित है, जिस रूप में वह प्राचीनकाल में वहां पहुंची थी। इस द्वीप पर हिन्दू धर्म की प्रधानता थी तथा वेद, रामायण, महाभारत का पठन-पाठन श्रद्धा व भक्ति भाव से किया जाता था। यहां का समाज भी चार वर्णों में विभाजित था। पूर्वी द्वीप समूहों में सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो से संस्कृत भाषा के अभिलेख तथा हिन्दू व बौद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि गुप्तकाल में किस प्रकार भारतीय संस्कृति का प्रसार दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में हुआ। धार्मिक संतों तथा व्यापारिक गतिविधियों के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की संस्कृति के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया। भाषा और धर्म किसी भी संस्कृति के मूल तत्त्व होते हैं और जब यह दोनों तत्त्व किसी अन्य संस्कृति से प्रभावित हो जाएं तो शायद ही संस्कृति का कोई भी भाग अछूता रहता हो। ऐसा ही दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ हुआ और उसका भारतीयकरण हो गया। वहां की अनेक भाषाओं पर भारतीय संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। थाई भाषा की लिपि भारतीय लिपि से ही प्रभावित है तथा थाईलैण्ड की राजधानी का नाम ‘अयूथिया’ अयोध्या के नाम पर रखा गया था।
Question : ‘नालंदा का महाविहार’ पर 200 शब्दों की सीमा में निबंध लिखिये?
(1997)
Answer : नालंदा का महाविहार गुप्तोत्तर काल का सर्वप्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां चीनी यात्री ह्नेनसांग ने उस महाविहार के अध्यक्ष शीलभद्र के चरणों में बैठकर योग का अध्ययन किया था। नालंदा एक स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय था, जिसमें 8,500 विद्यार्थी और 1,510 शिक्षक थे। शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात 1ः 5 था। इस अनुपात के अनुसार शिक्षकों और विद्यार्थियों का वैयक्तिक शिक्षा संपर्क था। नालंदा में कठिन परीक्षा के बाद प्रवेश मिलता था। यहां कोरिया, मंगोलिया, जापान, तिब्बत एवं लंका जैसे देशों से विद्यार्थी और विद्वान पढ़ने आते थे। ह्नेनसांग को वहां पर ऐसे 56 विद्यार्थी मिले, जिन्होंने भारतीय नाम रख लिये थे।
ह्नेनसांग के समय इस महाविहार में सात विहार और आठ प्रकोष्ठ थे। इस विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी, जिस पर फ्श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षुसंघस्यय् लेख उत्कीर्ण था। महाविहार का अपना बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र था, जहां की आय से महाविहार का व्यय चलता था। इस महाविहार की स्थापना कब और कैसे हुई, इसका निश्चित प्रमाण तो नहीं मिल पाया है परंतु हर्ष के युग में यह अपने चरमोत्कर्ष पर था।
हर्ष के बाद भी यह महाविहार बहुत बाद तक एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा था। पाल वंश के समय भी इस महाविहार को राज्य से पर्याप्त समर्थन मिलता था। सुमात्र के शासक बालपुत्र देव ने देवपाल की अनुमति से इस महाविहार में विदेशी विद्यार्थियों के लिए एक छात्रवास का निर्माण कराया था। यहां से जो पालकालीन अभिलेख मिले हैं, उससे ज्ञात होता है कि उस काल में भी यह उÂति के शिखर पर था।
Question : सांची के महान स्तूप की स्थापत्यात्मक एवं कलात्मक विशेषतायें।
(1997)
Answer : सांची एकमात्र ऐसा स्थल है जहां बौद्धकालीन शिल्प कला के सारे नमूने विद्यमान हैं। सांची में तीन स्तूप हैं जो अत्यंत सुंदर एवं प्राचीन हैं। इन तीनों स्तूपों में एक मुख्य स्तूप है, जिसका व्यास 36.5 मीटर का है और ऊंचाई 16.4 मीटर है। इस स्तूप के तोरण पर बुद्ध के जीवन की झलकियां उत्कीर्ण हैं। इस स्तूप का निर्माण महान् मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पश्चात् ईसा पूर्व तीसरी सदी में कराया था। इसी स्तूप के अंदर बुद्ध के शिष्यों में से सारिपुत्र एवं मौदग्यालन के अस्थि अवशेष कांच की मंजूषा में सुरक्षित रखे गये थे।
इस स्तूप में कला का उत्कृष्ट विकास दिखाई पड़ता है। यों तो इस स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, परंतु कलात्मक दृष्टि से इसका विकास बाद में हुआ। शुंग काल में इसका आकार बढ़ाया गया। स्तूप के ऊपर एक वर्गाकार वेदिका स्थापित की गयी। अपनी विशालता एवं गंभीरता के कारण यह वेदिका अत्यंत प्रभावोत्पादक है। इस स्तूप में चार तोरण हैं। स्थापत्य की जो मूर्तियां हैं, वे उत्कृष्ट कोटि की हैं। इस स्तूप के बाहरी दीवारों पर अंकित विभिन्न पशु-पक्षियों, पादपों, वामनों और यक्ष-यक्षिणियों की मूर्तियां कलाकारों के प्रकृति-प्रेम और वैभिन्य प्रेम की सूचना देती हैं। नागरिक एवं ग्राम्य जीवन की झांकी भी इस स्तूप से मिल जाती है। विभिन्न तरीकों से दर्शायी गयी जातक कथाएं, व्यक्तिगत मूर्तियां, उसके वर्गीकरण का ढंग, अभिव्यक्ति की प्रणाली तथा अलंकरण के तत्त्व सभी अत्यंत उच्च कोटि की शिल्पकला और कलात्मक भावना का प्रदर्शन करते हैं।
Question : सिन्धु सभ्यता का धर्म
(1996)
Answer : सिन्धु सभ्यता के धर्म के संबंध में जानकारी ध्वंस स्मारकों, मूर्तियों, मुहरों एवं ताबीजों आदि से प्राप्त की जाती है। अभाग्यवश सिन्धु लिपि अभी तक अपठनीय है और इसलिए निश्चित निष्कर्ष निकालना मुश्किल है।
हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री-मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है जो संभवतः पृथ्वी देवी की पूजा का संकेत देता है। इस तरह मालूम पड़ता है कि हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझ कर पूजते होंगे। अन्य मिट्टी के नारी मूर्तिकाओं के शरीर पर ढेर सारे गहने मिलते हैं। ये मूर्तिकाएं भी देवी की मानी जाती हैं, जिनकी पूजा-अर्चना होती थी। सींग वाले देवता का चित्र बड़ा प्रसिद्ध है, जो एक योगी की ध्यान-मुद्रा (पद्मासन लगाए) में दिखाया गया है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है, आसन के नीचे एक भैंसा है और पांवों के पास दो हिरण हैं। इस मुहर में अंकित चित्र पशुपति महादेव की याद दिलाता है। शिव प्रतिमा के अतिरिक्त लिंग पूजन भी संभवतः हड़प्पा में प्रचलित था, यह विभिन्न आकार के लिंग और योनि के बहुतायत मात्र में मिलने से पता चलता है। यह सांकेतिक पूजा-पद्धति को प्रकट करता है।
पीपल की डालों के बीच देवता का अंकन और बड़ी मात्र में कूबड़ वाले सांड़ का चित्रण वृक्षों और पशुओं के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। बड़ी तादात में ताबीज मिले हैं जो संभवतः भूत-प्रेत एवं जादू-टोने पर उनके विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। कालीबंगा में अग्नि-वेदी की संरचनाएं भी मिली हैं। उपर्युक्त लगभग सभी संकेत एवं मान्यताएं परवर्ती हिन्दू धर्म का किसी-न-किसी रूप में अंग रहे हैं। समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मन्दिर की संरचनाएं मिली हैं लेकिन भारत में ऐसी स्पष्ट संरचना नहीं मिली है। फिर भी सिन्धु सभ्यता के मिले संकेत एवं मान्यताओं के आधार पर धर्म के विकसित रूप में होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
Question : मौर्य-पूर्व काल (600-325 ई.पू.) में भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां।
(1996)
Answer : बुद्ध के समय से लोगों के जीवन में स्थायित्व के तत्त्व प्रकट रूप से सामने आये। कबीलाई समाज या समतामूलक समाज चार वर्णों में स्पष्टतः विभक्त हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्मसूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने-अपने कर्त्तव्य (पेशा) तय कर दिये गये। उच्च वर्णों से उच्च कोटि के नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती थी। शूद्रों पर हर प्रकार की अपात्रता लाद दी गयी थी। यहां तक कि जैन और बौद्ध संप्रदायों ने भी उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने की गंभीर कोशिश नहीं की। इस काल में स्त्रियों पर भी बदल रही अर्थव्यवस्था और समाज का कई रूपों में प्रभाव पड़ा। पैतृक वंश प्रणाली की व्यवस्था को बनाए रखने हेतु स्त्रियों की पतिव्रता पर विशेष बल दिया गया। सार्वजनिक सभा में बैठने या कोई व्यवसाय करने में स्त्रियां असमर्थ थीं और यह कहा गया कि उनको किसी न किसी के नियंत्रण में रहना चाहिए, यह पिता, पति या पुत्र के रूप में हो सकता है।
पुरातात्त्विक दृष्टि से मौर्य-पूर्व काल (600-325 ई.पू.) उत्तरी काली पॉलिश किये हुए बर्तन (एन-बी-पी- डब्ल्यू-) का युग था। यह बताया जाता है कि ई.पू. 750 से 700 के बीच लोहे के औजारों का उपयोग करके गंगा के मैदानी भाग के जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि में तब्दील कर दिया गया। लोहे की मुख्य भूमिका युद्ध में भी रही। यह इस बात से भी साबित होता है कि छोटानागपुर की खानों पर मगध के आधिपत्य ने उसे एक साम्राज्य निर्माण में सहायता पहुंचायी। इस युग की विशेषता अर्थव्यवस्था का विस्तार तथा उसके अन्तर्गत विशेषकर कृषि का प्रसार होना था। विभिन्नफसलों में धान प्रमुख अनाज था। कृषि के प्रसार ने जनसंख्या में क्रांतिकारी वृद्धि करायी। गंगा के बीच के मैदानों में बस्तियां नगरों एवं महानगरों में तब्दील होने लगीं, जहां व्यापारियों की प्रमुखता होने लगी। हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में यह दूसरा नगरीकरण माना जाता है। बौद्ध ग्रन्थों में ‘गहपति’ शब्द का उपयोग किया गया है। यह एक विशेष श्रेणी की ओर इंगित करता है जो कृषि के विस्तार में तथा स्वयं अपने लिए और पूरे समाज के लिए उत्पादनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। आहत मुद्राओं (च्नदबी डंतामक ब्वपदे) के प्रचलन से व्यापार में वृद्धि हुई। करों की नियमित वसूली से बड़े-बड़े जनपद राज्यों का निर्माण संभव हुआ।
Question : जिन घटनाओं का भारत के इतिहास पर अपूर्व प्रभाव पड़ा, उनमें 647 ई. में हुई हर्ष की मृत्यु का स्थान महत्वपूर्ण है, क्यों? स्पष्ट कीजिये।
(1996)
Answer : कई दृष्टि से भारतीय इतिहास में हर्ष का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। उसकी मृत्यु के बाद से मुसलमानों की विजय तक के युग को राजपूत युग की संज्ञा दी जाती है। इस काल-खंड में ऐसे-ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव आने लगे कि इसे एक युग का अन्त और दूसरे युग की शुरुआत के रूप में देखा जाने लगा। बहुत से इतिहासकार भारतीय इतिहास में मध्यकाल का पदार्पण हर्ष की मृत्यु के बाद ही मानते हैं। ये बदलाव राजनीतिक एकता, सामाजिक-आर्थिक संरचना, धार्मिक मान्यताओं, मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल एवं कला जैसे सभी क्षेत्रों में देखे गये। हर्ष का समय इस दृष्टिकोण से प्राचीन एवं मध्यकाल के बीच का सन्धिकाल माना गया है।
हर्ष भारत का अन्तिम हिन्दू सम्राट कहलाता है, जिसने समूचे उत्तर भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में बांधे रखा था। कश्मीर को छोड़कर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। पूर्व में गौड़ के राजा शशांक और दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्यों ने उसकी शक्ति पर अंकुश के कार्य किये। हर्ष के तिरोहित होते ही उत्तर भारत की यह एकता और बड़े साम्राज्य का युग समाप्त हो गया। उत्तर भारत में पाल, प्रतिहार और दक्कन में राष्ट्रकूट जैसी ताकतें आयीं जो देश को न तो राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध सके और न ही स्थिरता दे सके।
लगभग 1000 वर्षों से राजनीतिक सत्ता का केन्द्र बिन्दु पाटलिपुत्र बना रहा था, जिसे हर्ष ने बदलकर कन्नौज को कर दिया था। यह गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में था और अपनी उर्वर भूमि क्षेत्र, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होने तथा हर्ष की राजधानी बनने से उत्तर भारत का सर्वाधिक केन्द्रीकृत स्थल बन गया। आठवीं सदी के पूर्वार्द्ध में आरंभ होने वाला त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। ये तीन शक्तियां थीं- गुजरात राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। ये सभी हर्ष की मृत्यु से उत्पन्न उत्तरी भारत में हुई रिक्तता का लाभ उठाकर समृद्ध गंगा घाटी का स्वामित्व प्राप्त करना चाहते थे और कन्नौज इस संघर्ष के लक्ष्य का प्रतीक बन गया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि कन्नौज वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता एवं महानता का केन्द्र बन गया था।
हर्षवर्द्धन की मृत्यु के पश्चात् भारत में राजनीतिक उथल-पुथल थी। भारत छोटे-छोटे राज्यों में बंट चुका था। न केवल आन्तरिक अराजकता ही थी, अपितु बाह्य आक्रमण भी प्रारंभ हो चुके थे। अरबों की शक्ति तथा इस्लाम धर्म का उदय भी 7वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। राजनीतिक दृष्टि से भारत एक ‘भौगोलिक अभिव्यक्ति’ का चित्र मात्र प्रस्तुत करता है। इसके बावजूद, हर्ष की मृत्यु के बाद जिन महान् शक्तियों का उदय हुआ, उनमें से अधिकतर ‘राजपूत’ की श्रेणी में आती हैं। कुछ इतिहासकारों ने तो 7वीं से 12वीं सदी के काल को ‘राजपूत काल’ तक की संज्ञा दे दी। गुर्जर-प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमार, गहड़वाल आदि सभी राजपूत वंश के थे। हर्ष की मृत्यु के बाद इस ‘राजपूत कारक’ ने भारत के ‘राजनीतिक शून्यता के काल’ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपूतों ने वर्ण-व्यवस्था में क्षत्रियों के स्थानापन्न के रूप में जगह बनायी।
हर्ष के जीवन काल में ही भारतीय राजनीतिक गतिविधियों और संस्कृति के केन्द्र में बदलाव देखा जाने लगा। लगभग 550-750 ई. के काल में विभिन्न गतिविधियों का केन्द्र दक्षिण बन गया। इन दो शताब्दियों का दक्षिण भारत दो मुख्य राजवंशों के पारस्परिक संघर्ष का क्रीड़ास्थल था। ये दो वंश थे- वातापी का चालुक्य वंश और कांची का पल्लव वंश। चालुक्यों ने तो हर्ष के दक्षिण भारत में प्रसार को दृढ़तापूर्वक रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्ष की हार इसका सबूत है। हर्ष की मृत्यु के बाद किसी उत्तर भारतीय शासक ने दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह काल दक्षिण के उत्कर्ष का काल था।
गुप्तों के काल में ब्राह्मणों को भूमिदान (अग्रहार) देने की प्रथा जोरों पर थी। हर्ष ने अपने अधिकारियों को भी वेतन के बदले भूमिदान देने की प्रथा शुरू कर दी थी। यह प्रथा व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों की दुरावस्था एवं राज्य की आर्थिक विपÂता को प्रकट करती है। हालांकि राजा के पास भूमिदान को वापस लेने की सैद्धान्तिक सत्ता थी, परन्तु विरोध एवं विद्रोह के डर से ऐसा नहीं किया जाता था। सम्राट इसके बदले भेंट और उपहार पाने का हकदार था। उस भूमि से होने वाली आय ग्रहीता की होती थी। इस प्रथा ने सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दिया जो केन्द्रीय शक्ति को कमजोर करने में सहायक हुआ। हर्ष की मृत्यु के बाद इस प्रथा का सर्वत्र प्रचलन हो गया। भूमिदान की इस व्यवस्था ने भारत में प्राचीन काल की समाप्ति एवं मध्यकाल के प्रारंभ की घोषणा कर दी।
Question : हूणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध
(1996)
Answer : स्कंदगुप्त (455-469 ई.) के प्रारंभिक वर्ष अत्यंत ही संघर्ष के वर्ष थे। हूणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। हूण बर्बर योद्धा थे, जो मध्य एशिया के खानाबदोश लोग थे। अपनी बर्बरता एवं युद्धकौशल से हूणों ने यूरोप से लेकर भारत तक के क्षेत्र को आतंकित किया। परंतु स्कंदगुप्त ने अत्याचारी हूणों को परास्त कर न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की, वरन् आर्य सभ्यता एवं संस्कृति को भी नष्ट होने से बचाया। स्कंदगुप्त व हूणों के मध्य संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, चन्द्रगर्भ परिपृच्छा, चंद्र व्याकरण एवं कथा सरित्सागर जैसे ग्रंथों से प्रकाश पड़ता है। भितरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त हूणों के दर्प को चूर करने में पूर्णतः सफल रहा। हालांकि यह युद्ध किस स्थान पर हुआ था, इसका प्रमाण नहीं मिलता परंतु प्रतीत होता है कि यह युद्ध गंगा की उत्तरी घाटी में किसी स्थान पर हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त करने के पश्चात् ‘विक्रमादित्य’ व ‘क्रमादित्य’ की उपाधियां धारण कीं तथा इस विजय के उपलक्ष्य में उसने शारंग (सींग का बना धनुष) धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भितर गांव में स्थापित की। वास्तव में यह एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें विजयी होने से स्कंदगुप्त अपने विचलित वंश को पुनः स्थापित करने और शासन को सुप्रतिष्ठित करने में सफल हुआ।
Question : गुप्त साम्राज्य के उत्थान और पतन के कारक
(1996)
Answer : तीसरी सदी ईस्वी में कुषाणों के अवसान सत्र में उन्हीं के सामन्त गुप्तों ने साम्राज्य निर्माण की दिशा में कदम उठाया। गुप्तों के प्रारंभिक शक्ति स्थल बिहार और उत्तर प्रदेश थे। लगता है कि गुप्तों ने जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूतों का इस्तेमाल कुषाणों से सीखा। इन सभी से उनमें गतिशीलता आयी। अपने पूर्ववर्त्ती शासकों के नक्शे-कदम पर गुप्तों ने रथ और हाथी के स्थान पर घोड़ों को महत्व दिया। गुप्त शासकों के सिक्कों पर घुड़सवार अंकित हैं। घोड़े उनकी मूल शक्ति के आधार थे।
गुप्त राजाओं को कई भौतिक सुविधाएं भी प्राप्त थीं। उनके कार्यकलाप का मुख्य केन्द्र बिहार और उत्तर प्रदेश की उर्वर भूमि थी। साथ ही, वे मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लौह अयस्क का भी उपयोग कर सके। इसके अलावा, बिजेन्टाइन साम्राज्य अर्थात् पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार करने वाले उत्तर भारत के इलाके उनके पड़ोस में पड़ते थे, अतः वे इस निकटता का भी लाभ उठा सके। इन तमाम कारकों के सामूहिक प्रतिफलन के रूप में गुप्तों का उत्थान देखा जा सकता है।
गुप्त साम्राज्य का पतन अपनी आंतरिक कमजोरियों के फलस्वरूप हुआ, जिसे हूणों के आक्रमण ने और तेज कर दिया। आरंभ में स्कन्दगुप्त ने हूणों को आगे बढ़ने से रोका तो अवश्य, लेकिन कमजोर गुप्त उत्तराधिकारी इस समस्या से हमेशाजूझते रहे। हूण घुड़सवारी में बेजोड़ थे और धातु के बने रकाब का उपयोग करते थे। मालवा के यशोधर्मन ने हूणों को मार भगाया। साथ ही गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दे डाली।
सामन्तों ने सर उठाकर गुप्त साम्राज्य को और भी दुर्बल बना दिया। बंगाल के सामन्तों ने स्वतंत्र सत्ता का उपभोग शुरू कर दिया। मौखरि वंश ने बिहार और उत्तर प्रदेश में राज सत्ता स्थापित की। पांचवीं सदी का अन्त होते-होते पश्चिमी भारत गुप्तों के हाथ से निकल गया और फलतः व्यापार और वाणिज्य से होने वाली आय के एक बड़े हिस्से से उन्हें हाथ धोना पड़ा। आर्थिक कमजोरी ने साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया। गुप्त साम्राज्य को विशाल वेतनभोगी सेना के रख-रखाव में कठिनाई होने लगी, क्योंकि धार्मिक या अन्य उद्देश्यों से ग्रामदान करने की परिपाटी जोर पकड़ती जा रही थी, जिससे उसकी आमदनी बहुत घट गयी होगी।
गुप्त साम्राज्य के पतन का एक अन्य कारण उनमें आपसी वंशानुगत मतभेद एवं निर्बल शासक थे। कुमारगुप्त के पश्चात् सिंहासन प्राप्त करना सदैव विवादास्पद रहा। गृहयुद्धों के क्रम ने साम्राज्य की स्थिरता एवं ताने-बाने को ही समाप्त कर दिया।
Question : आरंभिक जैनधर्म का सार।
(1995)
Answer : जैन धर्म मूल रूप से नास्तिकतावादी आंदोलन की उपज है। हालांकि इस धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, पर उनका स्थान जिन अर्थात् महावीर से नीचे रखा गया है। इसके अनुसार संसार अनादि काल से है और इसका रचयिता ईश्वर नहीं है। संसार के सभी प्राणी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। कर्म-फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए महावीर ने त्रिरत्न के अनुशीलन की बात कही है। यह है-सम्यव्फ़ ज्ञान, सम्यक् ध्यान एवं सम्यव्फ़ आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में आचरण पर विशेष बल दिया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित पांच महाव्रतों के पालन का विधान है: (1) अहिंसा या किसी की हिंसा नहीं करना, (2) अमृषा या झूठ न बोलना, (3) अचौर्य या चोरी न करना, (4) अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित नहीं करना, और (5) ब्रह्मचर्य या इन्द्रिय निग्रह करना। कहा जाता है कि इनमें चार व्रत पहले से चले आ रहे थे, महावीर ने केवल पांचवां व्रत जोड़ा।
जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। किसी भी रूप में जीव हिंसा को निषिद्ध माना गया है। अनासक्ति और अपरिग्रह के लिए महावीर ने नग्नता को आवश्यक माना। बाद में वस्त्र धारण करने और न करने के आधार पर जैन धर्म श्वेतांबर और दिगम्बर-दो धाराओं में बंट गया।
जैन धर्म के उपदेश और दर्शन प्रारंभ में मौखिक परम्पराओं में जीवित रहे। परन्तु तीसरी शताब्दी ई.पू. में उनको लिपिबद्ध कर लिया गया। अन्तिम रूप से इनका संपादन ईसा की पांचवीं शताब्दी में किया गया। इन्हीं के आधार पर आरंभिक जैन धर्म के बारे में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं।
Question : फ्लगभग ई.पू. 200 एवं लगभग 300 ई. के बीच की शताब्दियां भारत के सामाजिक एवं धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण भू-चिह्न हैं।य् इस प्रस्ताव का विश्लेषण कीजिये।
(1995)
Answer : ई.पू. 200 एवं 300 ई. के बीच भारत के सामाजिक- धार्मिक अवस्था में आये बदलाव काफी महत्वपूर्ण हैं। यह वह समय था जब विदेशी शक्तियों, यथा-यवन, पार्थियन, शक और कुषाणों ने देश के विभिन्न हिस्सों में शासन किया। इन विदेशी शासकों को भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था के अन्दर किस तरह शामिल किया जाये, यह समस्या उत्पन्न हो गयी थी। शास्त्रीय दृष्टिकोण से वर्ण जन्म पर आधारित होने के कारण ब्राह्मण धर्म में इनका स्वीकरण असंभव था। इस समय बौद्ध मत अपने उत्कर्ष पर था और इन विदेशी शासकों ने बौद्ध मत अपनाकर भारतीय समाज में जगह बनाना शुरू कर दिया। हारकर ब्राह्मण रूढि़वादियों ने परिस्थिति से समझौता किया और बड़ी चतुराई से इन्हें ‘पतित क्षत्रिय’ की श्रेणी देकर हिन्दू समाज का अंग बनाने लगे। विदेशियों का हिन्दू धर्म में आत्मसातीकरण जितना अधिक मौर्योत्तर काल में हुआ, उतना भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ।
कट्टर ब्राह्मणवादी मनु ने ईसा की पहली दो शताब्दियों में किसी समय ‘मानव-धर्मशास्त्र’ की रचना करके चारों वर्णों की निश्चित और स्पष्ट व्याख्या कर दी थी। हालांकि इस काल में वैश्यों एवं शूद्रों के बीच का अंतर कम हो गया था, किन्तु फिर भी मनु ने शूद्रों के लिए बड़े कठोर नियम रखे। उसने शूद्रों को तीनों उच्च वर्णों की सेवा का निर्देश दिया है और ऐसा न करने की स्थिति में कठोर सजा की व्यवस्था दी है। मनुस्मृति में 60 वर्णसंकरों का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि मनु पर्याप्त यथार्थवादी भी थे। विदेशी लोगों के आगमन से जो एक सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ, उसका एक प्रायोगिक समाधान वर्णसंकर की परिकल्पना में ही दृष्टिगोचर होता है।
विदेशियों के एकीकरण में धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान था। विभिन्न धर्मों में विदेशी शासकों का समर्थन पाने की होड़ लग गयी। भारतीय धर्मों में भक्ति भावना के पुट ने इस काम को और भी आसान कर दिया। मनुस्मृति में कहा गया है कि पवित्र व्यक्ति संस्कारों तथा ब्राह्मणों की अवहेलना करने के कारण ही यवन, शक, पहलव आदि जातियां धीरे-धीरे शूद्रों की श्रेणी में गिर गयी हैं, जबकि भागवत पुराण में यह कहा गया है कि ये जातियां विष्णु पूजन से पवित्र हो जाती हैं। बेसनगर के अभिलेख में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने खुद को भागवत कहा है और भगवान वसुदेव को उसने गरुड़ध्वज प्रदान किया था। कुषाण शासक हुविष्क की एक मुद्रा पर हरिहर की प्रतिमा का अंकन हुआ है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण किया। उसने बौद्धों की चतुर्थ संगीति का आयोजन कराया।
बौद्ध धर्म का समर्थन संपन्न व्यापारी वर्ग ने भी किया, जिनके अनुदानों से धनी बने बौद्ध विहार के भिक्षु एवं भिक्षुणी इहलोक को महत्व देने लगे। बौद्ध धर्म के स्वरूप में इस बदली परिस्थिति ने परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। आवागमन की उन्नति से तीर्थ यात्रओं में वृद्धि हुई और इसके फलस्वरूप नये विचारों का प्रसार हुआ। बौद्ध मत इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में तथा विदेशों में धर्म-प्रचारक भेजने के कार्य में बड़ा सक्रिय हो गया था, तब लोगों को धर्मान्तरित करने की प्रक्रिया में बौद्ध-मत भी नए विचार ग्रहण करने लगा। फलतः धर्म के मूल सिद्धान्तों की नयी-नयी व्याख्याएं अनिवार्य हो गयी, जिसने अन्ततः बड़े-बड़े मतभेदों को जन्म दिया और बौद्ध-मत दो प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। कनिष्क द्वारा प्रायोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध मत ‘हीनयान’ और ‘महायान’ में स्पष्ट रूप से बंट गया। रूढि़वादी बौद्ध अनुयायियों ने बुद्ध के मूल उपदेश को ही आदर्श माना और हीनयानी कहलाए। महायानी मतावलम्बियों ने दो नए परिवर्तन किये। एक तो बुद्ध को देवतुल्य माना और दूसरे ‘बोधिसत्व’ की अवधारणा शुरू की। पहले परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनायी जाने लगीं और देवताओं की भांति उनकी पूजा होने लगा। ‘बोधिसत्व’ की अवधारणा के अन्तर्गत बुद्ध के कई जन्मों की परिकल्पना की गयी, जिसने अपने हर जन्म में मानवता के कल्याण हेतु जीवन-उत्सर्ग किया। ‘मैत्रेय’ की भावी बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठा की गयी, क्योंकि ऐसा लगता था कि विश्व को कष्टों से वे मुक्ति दिला सकेंगे। महायान मत ने भारत में प्रमुखता प्राप्त की और यह मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और जापान तक भी फैल गया, जबकि हीनयान ने श्रीलंका, बर्मा और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों में अपना मजबूत आधार बनाया।
बौद्ध धर्म की भांति ही जैन धर्म में भी परिवर्तन आया। ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास जैन धर्म में भी विभाजन हो गया। रूढि़वादी जैन ‘दिगंबर’ एवं उदारवादी ‘श्वेतांबर’ कहलाए। बौद्ध धर्म की ही भांति जैन धर्म में भी मूर्तिपूजा का विकास हुआ।
बौद्ध धर्म तथा अन्य शास्त्र-विरोधी धार्मिक सम्प्रदायों के भीषण प्रहारों ने वैदिक प्रथाओं तथा ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा एवं प्रभुत्व को काफी आघात पहुंचाया। ब्राह्मण लोग, जिनकी स्थिति यज्ञों के लिए मांग में कमी हो जाने के कारण कठिन हो रही थी, जीविका के कुछ अन्य साधनों का सहारा लेने के लिए बाध्य हो गये। दूसरी ओर, नए आर्थिक एवं राजनीतिक तत्त्वों से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए तथा ब्राह्मणधर्मी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने अनेक लोकप्रिय उपासना विधियों को अपना लिया। वैदिक देवताओं के स्थान पर नवीन देववर्ग का उदय हुआ, जिनमें ब्रह्मा-विष्णु-महेश की त्रिमूर्ति बहुत विख्यात है। ब्रह्मा का रूप स्रष्टा, विष्णु का भर्त्ता एवं शिव का संहारकर्त्ता का है। धीरे-धीरे शिव एवं विष्णु अधिक लोकप्रिय और प्रचलित देवता हो गये एवं उनके अनुयायी ‘शैव’ एवं ‘वैष्णव’ कहे जाने लगे। इस नवोदित ब्राह्मण धर्म में भी वैदिक धर्म के कर्मकांडों के स्थान पर भक्ति को प्राधान्य दिया गया।
धर्म संबंधी विभिन्न लोक और जनजातीय तत्त्वों को भी शैव और वैष्णव मतों में शामिल किया गया। लोकप्रिय वासुदेव-कृष्ण, संकर्षण के वैदिक देवता नारायण-विष्णु से एकाकार होना तथा वैदिक देवता रूद्र और तमिल देवता मुरुगन से शिव का एकाकार होना ऐसी ही घटना है। लोकप्रिय लिंगोपासना तथा वृषभ-पूजन भी शैव मत से जोड़े गये। इस प्रकार नये ब्राह्मण धर्म ने अपने आधार को और भी अधिक चौड़ा कर लिया। इस काल में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों ने परवर्ती हिन्दू धर्म के लिए आधारशिला का कार्य किया।
Question : लगभग ई.पू. 2000 एवं ई.पू. 500 के बीच भारतीय उप-महाद्वीप में प्राप्य प्रमुख पुरातात्चिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये।
(1995)
Answer : पुरातात्त्विक संस्कृति से अभिप्राय उस संस्कृति का होता है, जिसके बारे में जानकारी मुख्य रूप से ऐतिहासिक लेखन द्वारा न होकर उस काल के अन्य भौतिक साक्ष्यों द्वारा होता है। भारत में 2000 ई.पू. का काल हड़प्पा संस्कृति की नागरिक अवस्था के अवसान का काल माना जाता है। इसके बाद के काल को उत्तर-हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया है जो मूलतः ताम्र-पाषाणिक है, जिसमें पत्थर और तांबे के औजार चलते थे। हालांकि तकनीकी दृष्टि से ताम्र-पाषाण अवस्था का प्रयोग हड़प्पा से पहले की संस्कृतियों के लिए होता है। भारत में ताम्र-पाषाण अवस्था की बस्तियां दिक्षण-पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण-पूर्वी भारत में पायी गयी हैं। कालक्रम की दृष्टि से ये विभिन्न स्थानों में 2000 ई.पू. से 700 ई.पू. के बीच के विभिन्न काल-खण्डों में फली-फूलीं।
दक्षिण-पूर्व राजस्थान में दो स्थलों की खुदाई हुई है, एक अहार में और दूसरा गिलुंड में। इस ताम्र-पाषाण संस्कृति को ‘अहार संस्कृति’ कहा जाता है। बनास नदी घाटी के नाम से इसे ‘बनास संस्कृति’ भी कहा जाता है। अहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। पक्की ईंटों का उपयोग ये लोग नहीं करते थे, लेकिन अपवादस्वरूप गिलुंड में ये पाये गये हैं। मुख्य मृद्भांड काले और लाल रंगों में मिले हैं, जिनमें तरह-तरह के रैखिक और बिंदीदार सफेद डिजाइन बने हैं। तांबे का प्रयोग ये व्यापक रूप से करते थे। अहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात् तांबावाली जगह है। रेडियो-कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर इस संस्कृति का आरंभ ई.पू. 2000 के आस-पास मान सकते हैं।
पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कयथा और एरण स्थलों की खुदाई हुई है। केन्द्रीय और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्र-पाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है- मालवा भांड, जो ताम्र-पाषाण मृद्भांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। इसके कुछ मृद्भांड और अन्य सांस्कृतिक सामग्री महाराष्ट्र में भी पायी गयी है। कयथा संस्कृति तीन कालखंडों में मिली है। तीसरा कालखंड ‘मालवा ताम्र-पाषाण संस्कृति’ को निरूपित करता है। नवदाटोली एक अन्य संस्कृति केन्द्र है, जिसकी खुदाई एच-डी- संकालिया ने कराई है। यह स्थल मोटे तौर पर 2 फर्लांग × 2 फर्लांग क्षेत्र में फैला है। यहां मिट्टी, बांस और फूल से बने हुए घर चौकोर और वृत्ताकार-दोनों ही प्रकार के हैं। लाल-काले मृद्भांड पर ज्यामितीय डिजाइन चित्रित हैं। तांबे का सीमित प्रयोग पाया गया है। इस स्थल की तिथि ई.पू. 1600 और 1300 के बीच निर्धारित की गयी है।
सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहां उत्खनन हुए हैं वे स्थल हैं-अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दायमाबाद, पुणे जिले में चन्दोली, सोनगांव और इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। यह नाम जोरवे स्थल के आधार पर दिया गया है जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा-नदी प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित प्ररूप स्थल है। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ लिया है, किन्तु इसमें दक्षिणी नवपाषाण के तत्त्व भी हैं। इस संस्कृति की तिथि ईसा पूर्व 1400 से 700 के बीच रखी गयी है। यों तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां, जैसे- दायमाबाद और इनामगांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गयी थीं। शवाधान के संबंध में एक विशेष बात यह थी कि अधिकतर ये कलश में संरक्षित किये गये हैं और ये कलश घरों के फर्श के नीचे रखे गये हैं। इनामगांव में चूल्हों-सहित बड़े-बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। बाद की अवस्था में पांच कमरों का मकान भी मिला है। इनामगांव ताम्र-पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें सौ से भी अधिक घर और कई कब्रें पायी गयी हैं। यह बस्ती किलाबन्द है और खाई से घिरी हुई है। जौ और गेहूं प्रमुख अनाज थे। पालतू पशुओं में गाय-बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर और घोड़ा शामिल थे।
पूर्वी भारत में गंगातटवर्ती चिरांद के अलावा वर्द्धमान जिले में पांडु राजार ढीबी तथा वीरभूम जिले में महिषाल प्रमुख ताम्र-पाषाण स्थल हैं। कुछ और स्थलों की खुदाई हुई है, जिनमें उल्लेखनीय हैं- बिहार में सेंवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नौहान। संपूर्ण साक्ष्य से चावल पर आधारित एक विस्तृत ताम्र-पाषाणयुगीन ग्राम संस्कृति का पता चला है जो लगभग ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्रब्दी के मध्य जितनी पुरानी है।
ताम्र-पाषाण संस्कृतियां 1200 ई.पू. में आकर भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में लुप्त हो गयीं। केवल जोरवे संस्कृति 700 ई.पू. तक जीवित रही। इन बस्तियों के लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ई.पू. के बाद वर्षा की मात्र घटना माना जाता है। पूर्वी भारत में ताम्र-पाषाण अवस्था के तुरंत बाद, बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था आ धमकी और उसने धीरे-धीरे लोगों को पूर्णतः कृषि जीवी बना दिया।
इसी तरह दक्षिणी भारत के कई स्थलों पर ताम्र-पाषाण संस्कृति ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। इस अवस्था में लोगों ने अधिकतर नदी-तटों पर पहाडि़यों से कम दूरी पर गांव बसाए। मध्य प्रदेश में कयथा और एरण की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनामगांव की बस्तियां किलाबन्द हैं। इसके विपरीत पूर्वी भारत के चिरांद और पांडु राजार ढ़ीबी की संरचना के अवशेष बिल्कुल सामान्य किस्म के हैं।
खिलौने की मिट्टी की लघु मूर्तियों में महिला की पुतलियां हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ताम्र-पाषाण युग के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। इनामगांव में मातृदेवी की प्रतिमा और मालवा और राजस्थान में सांड़-मूर्तिका इनकी धार्मिक मान्यताओं की ओर इशारा करते हैं। बस्ती का ढांचा और शव संस्कार विधि सामाजिक असमानता को प्रकट करते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में दफनाए गये बच्चों के शवाधानों से इस संस्कृति की दुर्बलता का पता भी चलता है। पोषाहार की कमी, चिकित्सा के ज्ञान का अभाव या महामारी का प्रकोप इसका कारण हो सकता है। सिन्धु सभ्यता के परवर्त्ती होते हुए भी ये उनके श्रेष्ठ तकनीकी ज्ञान का कोई फायदा नहीं उठा पाये।